
21-05-2025 (Important News Clippings)
To Download Click Here.
Date: 21-05-25
आमजन में टेक्नोलॉजी के प्रयोग को सहज बनाएं
संपादकीय
यह सच है कि औसत भारतीय परिवर्तन के प्रति उदासीन रहता है और तकनीकी को लेकर कम उत्साहित । अशिक्षा, धोखे का डर और आमने-सामने की बातचीत पर ज्यादा भरोसा इसके मुख्य कारण हैं। लेकिन अगर तकनीकी कुछ और सुरक्षित और सहज कर दी जाए तो यह गवनेंस को भ्रष्टाचार और अकर्मण्यता से मुक्त कर सकेगी। इसका उदाहरण हैं देश के वे लाखों अल्पशिक्षित ड्राइवर, जो गूगल से गंतव्य तक ब्रिटिश अंग्रेजी लहजे में दिए गए इंस्ट्रक्शन समझने लगे हैं। लेकिन जब बैंकों और सरकारी कार्यालयों में सर्वर डाउन से निराश होते लोग आरटीओ दफ्तर आदि में आज भी दलाल तलाशते हैं और घूस (कमीशन) में मोटी रकम देते हैं तो गवनेंस में तकनीकी के प्रयोग का पूरा मकसद ही फेल हो जाता है। ऐसे में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण पहल नामक एक पोर्टल शुरू कर रहा है, जो सिंगल विंडो से जमीन आबंटन से लेकर किस्त जमा करना, निर्माण के लिए परमिशन लेना और अन्य सभी सुविधाएं ऑनलाइन करने की सुविधा देने जा रहा है। अतिक्रमण की पहचान के लिए सैटेलाइट इमेजेज का सहारा लिया जा रहा है। गोवा पुलिस ने भी देश-विदेश के पर्यटकों को फर्जी वेबसाइट से ठगे जाने से बचाने के लिए नई वेबसाइट विकसित की है। देश के गृहमंत्री ने एक बैठक में इसकी जानकारी मिलने पर अन्य राज्यों को भी यह मॉडल अमल में लाने की सलाह दी है। आम जनता में टेक्नोलॉजी के प्रयोग को इतना ही सहज और ठगी – मुक्त बनाना होगा ।
Date: 21-05-25
‘एक राष्ट्र एक चुनाव’ का अच्छा असर पर्यावरण पर भी
प्रो. चेतन सिंह सोलंकी, ( आईआईटी बॉम्बे में प्रोफेसर, संस्थापक, एनर्जी स्वराज फाउंडेशन )
एक राष्ट्र एक चुनाव (ओएनओई) के प्रस्ताव ने पूरे देश में चर्चाओं को जन्म दिया है, जिसमें मुख्य रूप से शासन की दक्षता, लागत बचत और प्रशासनिक और सुरक्षा प्रणालियों पर बोझ कम करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसे ऐसे समाधान के रूप में सराहा जा रहा है, जो सरकारी मशीनरी को चुनाव प्रचार की तुलना में शासन पर अधिक ध्यान केंद्रित करने में सक्षम बना सकता है। साथ ही जो विभिन्न राज्यों में लगातार चुनावों के कारण होने वाले व्यवधानों को कम कर सकता है। लेकिन एक और आयाम है जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है इसका पर्यावरण पर पड़ने वाला प्रभाव ।
“चुनाव लोकतंत्र के लिए आवश्यक हैं, लेकिन इनके लिए पर्यावरण को भी कीमत चुकानी पड़ती है। हर चुनाव चक्र में लोगों की भारी आवाजाही सामग्री की छपाई, ईंधन की खपत, बिजली का उपयोग और बड़े पैमाने पर शारीरिक और डिजिटल लामबंदी होती है। 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में अलग-अलग आयोजित चुनावों की संख्या से इसका गुणा करें, तो यह पैमाना बहुत बड़ा हो जाता है। यदि भारत ओएनओई के माध्यम से लोकसभा और विधानसभा चुनावों को एक साथ कराता है तो अनुमान है कि 65 लाख करोड़ के कुल अनुमानित चुनाव व्यय में से पांच साल की अवधि में कम से कम 4 या 5 लाख करोड़ रुपए की बचत हो सकती है। यह केवल वित्तीय बचत नहीं है; यह गतिविधियों में भारी कमी को भी दर्शाता है। ओएनओई के क्रियान्वयन के माध्यम से बचाए जाने वाले उत्सर्जन कई स्रोतों से आएंगे। यात्रा एक प्रमुख योगदानकर्ता है।
हर चुनाव में लाखों मतदान अधिकारी, अर्धसैनिक बल, राजनीतिक प्रचारक और मतदाता हवाई, रेल और सड़क सहित परिवहन के विभिन्न साधनों का उपयोग करके देश भर में घूमते हैं। कम चुनाव का मतलब है कम यात्राएं, कम ईंधन की खपत और कम प्रदूषण। राजनीतिक अभियान तीव्र ऊर्जा उपयोग का एक और क्षेत्र है। हजारों रैलियां आयोजित की जाती हैं, जिनमें लाउडस्पीकर, लाइटिंग सेटअप, डीजल जनरेटर, वाहनों के काफिले और अस्थायी संरचनाओं का उपयोग किया जाता है- ये सभी बिजली और ईंधन पर चलते हैं। इसके अलावा, चुनाव के मौसम में मुद्रित सामग्री- पोस्टर, बैनर, फ्लायर्स, टी-शर्ट और प्लास्टिक के सामान की बाढ़ आ जाती है। इनमें से ज्यादातर एकल-उपयोग वाली वस्तुएं हैं जो या तो लैंडफिल में चली जाती हैं या जला दी जाती हैं, जिससे प्रदूषण में योगदान होता है।
यहां तक कि डिजिटल और प्रसारण अभियान भी पर्यावरणीय लागत वहन करते हैं। हर सोशल मीडिया विज्ञापन और वीडियो स्ट्रीम के पीछे एक डेटा सेंटर होता है, जो हर सेकंड बिजली की खपत करता है । सैकड़ों निर्वाचन क्षेत्रों और कई चुनाव चक्रों में संचयी डिजिटल पदचिह्न काफी बड़ा हो जाता है। ओएनओई इन चक्रों को एकल, समयबद्ध प्रक्रिया में संघनित कर देगा, जिससे बेहतर नियंत्रण, नियोजन और अंततः कम पर्यावरणीय दुष्प्रभाव संभव होगा।
कार्बन – तीव्रता का मतलब है कि एक इकाई जीडीपी के लिए कितना सीओटू उत्सर्जित होता है। 2023-24 तक भारत की कार्बन तीव्रता प्रति ₹100 खर्च पर 0.24 किलोग्राम सीओटू थी। इसके आधार पर, ₹5 लाख करोड़ की आर्थिक गतिविधि के परिणामस्वरूप लगभग 1.2 मिलियन टन या 12 लाख मीट्रिक टन सीओटू उत्सर्जन होगा। यह लगभग 12 लाख परिपक्व पेड़ों को काटने के बराबर है। क्योकि एक पूर्ण विकसित पेड़ अपने जीवनकाल में लगभग एक मीट्रिक टन सीओटू अवशोषित करता है। ऐसे में ओएनओई के बहुआयामी लाभ हैं। इससे पैसों की बचत होती है और प्रशासनिक तनाव कम होता है। सरकारों को दीर्घकालिक नीति पर काम करने के लिए अधिक निर्बाध समय मिलता है। और यह स्पष्ट रूप से जलवायु – लाभ भी प्रदान करता है।
Date: 21-05-25
कानून की संवैधानिकता
संपादकीय
संशोधित वक्फ कानून पर सुनवाई के समय इस कानून को असंवैधानिक, मनमाना साबित करने और उस पर अंतरिम रोक लगाने पर जोर देने वाली दलीलों पर सुप्रीम कोर्ट का इस निष्कर्ष पर पहुंचना संतोषजनक है कि संसद से पारित कानून संवैधानिकता की धारणा पर टिके होते हैं और जब तक इसका ठोस आधार न हो कि ऐसा नहीं है, तब तक अंतरिम राहत देना ठीक नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि अंतरिम राहत पाने के लिए बहुत ठोस और स्पष्ट आधार पेश करना होता है। पता नहीं कि वक्फ कानून को असंवैधानिक बता रहा पक्ष ऐसे ठोस एवं स्पष्ट आधार पेश कर सकेगा या नहीं, लेकिन वह साफ दिख रहा है कि उसकी कोशिश वेन-केन प्रकारेण इस कानून को सिरे से खारिज कराने की है। इसका संकेत इससे मिला कि वक्फ कानून को अनुचित, असंवैधानिक बताने के लिए ऐसी भी दलीलें दी गईं, जिनका कोई औचित्य नहीं बनता। इसके अतिरिक्त उन विषयों से इतर भी जाने की कोशिश की गई, जिन्हें सुनवाई के लिए तय किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने विचार के लिए जो तीन बिंदु चुने हैं, वे हैं वक्फ संपत्तियों को गैर अधिसूचित करने की प्रक्रिया, वक्फ बोडों एवं केंद्रीय वक्फ परिषद में गैर-मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति और सरकारी भूमि को वक्फ संपत्ति के रूप में वर्गीकृत करना। इन तीन बिंदुओं पर केंद्र सरकार पहले ही यह आश्वासन दे चुकी है कि इन पर बधास्थिति बनी रहेगी ।
कहना कठिन है कि वक्फ कानून की संवैधानिकता पर विचार कर रहा सुप्रीम कोर्ट किस नतीजे पर पहुंचेगा, लेकिन यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि किसी कानून पर कोई निर्णय उसकी संवैधानिकता की पूरी परख करके ही दिया जाना चाहिए। वैसा कदापि नहीं होना चाहिए, जैसा तीन कृषि कानूनों के मामले में हुआ था। इन कानूनों की संवैधानिकता की परख किए बिना ही उनके अमल पर रोक लगाकर सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून के विरोधियों को यही संदेश दिया था कि वे सही हैं। इसी कारण कृषि कानून विरोधी आंदोलन लंबा खिंचा और अंततः सरकार को न चाहते हुए भी उन्हें वापस लेने का दुर्भाग्यपूर्ण फैसला करना पड़ा। विश्व का कोई कानून ऐसा नहीं होता, जिसे परिपूर्ण कहा जा सके। यदि किसी कानून में कोई कमी – विसंगति हो तो उसे दूर किया जाना चाहिए, न कि पूरे कानून को ही खारिज कर दिया जाना चाहिए। संशोधित वक्फ कानून के विरोधी कुछ भी दावा और दुष्प्रचार करें, पुराना कानून खामियों से भरा ही नहीं, वक्फ बोडौं को मनमाने एवं दमनकारी अधिकार देने वाला भी था। इसके न जाने कितने ऐसे हैरान करने वाले प्रमाण और पीड़ित लोग बीते तीन-चार महीनों में ही सामने आए, जिनकी अनदेखी संसद में बहस के दौरान विपक्षी नेता भी नहीं कर सके।

Date: 21-05-25
क्या विशेषज्ञ समिति मायने रखती है ?
के पी कृष्णन, ( लेखक आईसीपीपी में मानद सीनियर फेलो और पूर्व अफसरशाह हैं )
हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने अपनी | वेबसाइट पर एक दस्तावेज अपलोड किया जिसका शीर्षक था, ‘नियमन निर्माण के लिए फ्रेमवर्क’ मोटे तौर पर इस पर ध्यान नहीं दिया गया। हालांकि नियमन के क्षेत्र में इसे अत्यधिक महत्त्वपूर्ण माना जा सकता है।
राज्य का सार दरअसल हिंसा और बलपूर्वक शक्ति के इस्तेमाल के उसके एकाधिकार में निहित है। लोकतांत्रिक देशों में राज्य की दमनकारी शक्ति का इस्तेमाल केवल कानून के अधिकार के साथ ही स्वीकार किया जा सकता है। बल प्रयोग में लोकतांत्रिक वैधता कानूनी प्रक्रिया और मानकों के अधीन होनी चाहिए। भारतीय संविधान एक विस्तृत प्रक्रिया बताता है, जिसके जरिये राज्य अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। इसके अलावा विशेषज्ञ और संसदीय समितियां तथा हितधारकों के साथ मशविरे जैसे मानक भी हैं, जो नतीजे लाने में भूमिका निभाते हैं।
देश में कानून लिखने का काम मुख्य तौर पर सांविधिक नियामकीय प्राधिकार (एसआरए) का है। उन्हें कानून बनाने की शक्ति दी गई है। वे निजी लोगों से एक खास व्यवहार की मांग करने वाले कानून लिख सकते हैं। इनका पालन नहीं करने के लिए जुर्माने की भी व्यवस्था की जाती है। नियमन वाली संस्थाओं पर इस अधिकार का प्रभाव ठीक वैसा ही होता है जैसा कि विधायिका द्वारा बनाए गए कानून का उदाहरण के लिए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी ने भेदिया कारोबार के कायदे तैयार किए। इन कायदों का उल्लंघन होने पर भारी जुर्माना हो सकता है। इसमें 25 करोड़ रुपये तक का भारी जुर्माना, कैद और प्रतिभूति बाजारों में कारोबार पर रोक आदि शामिल हैं। अकेले वित्तीय क्षेत्र में अनुमान है कि सभी वित्तीय एजेंसियों को मिलाकर देखें तो हर कार्य दिवस में अनुमानतः 10 ऐसे कानून सामने आए।
एसआरए द्वारा ऐसी शक्तियों के इस्तेमाल में ‘लोकतंत्र की कमी रहती ही है। उदार लोकतांत्रिक देश में अनिर्वाचित अधिकारियों के पास आम तौर पर कानून लिखने की शक्ति नहीं होती । उदाहरण के लिए सेबी अधिनियम के तहत इन नियमन को सेबी के बोर्ड द्वारा तैयार किया जाना चाहिए। मगर सेबी अधिनियम यह नहीं बताता कि ये कायदे कैसे लिखे जाने चाहिए। इसीलिए सेबी जैसे नियामक लोकतांत्रिक वैधता की विधायी प्रक्रिया के बगैर ही नियमित रूप से कानून लिख रहे थे। चौदह साल पहले 2011 में भारत सरकार ने वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग (एफएसएलआरसी) का गठन किया। इसकी अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश को सौंपी गई और इसके सदस्यों में अर्थशास्त्री, बैंकर, अधिवक्ता तथा लोक प्रशासन के विशेषज्ञ शामिल थे एफएसएलआरसी ने मार्च 2013 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस पर सार्वजनिक मशविरा भी किया गया और लोगों की टिप्पणियों से निपटने में दो साल का वक्त और लगा।
कुल मिलाकर एफएसएलआरसी एक चार वर्षीय परियोजना थी जिसने उच्च गुणवत्ता वाले कानून का मसौदा पेश किया। इस कानून के तीन घटक हैं (क) कानून की करीब 140 धाराएं बताती हैं कि नियामकों को किस तरह काम करना चाहिए (ख) एजेंसियों का बेहतर वित्तीय ढांचा हो और एजेंसियां मिले काम को अच्छी तरह करें (ग) विभिन्न वित्तीय एजेंसियों द्वारा वित्तीय और मौद्रिक आर्थिक नीति के लिए किए जाने वाले कामों का विस्तृत विवरण ।
मगर इस मसौदे भारतीय वित्तीय संहिता (आईएफसी) को कानून का रूप नहीं दिया गया। बदलाव का सामान्य सिद्धांत कारगर नहीं साबित हुआ। किंतु एफएसएलआरसी के काम का बहुत अधिक प्रभाव हुआ और उसने देश में वित्तीय आर्थिक नीति को नया आकार दिया। एफएसएलआरसी ने सभी संगठित वित्तीय कारोबारों के कायदों का एकीकरण करने की बात कही थी। इसके लिए वायदा बाजार आयोग का विलय सेबी में करने की जरूरत थी, जो 2013 में किया गया। एफएसएलआरसी ने मौद्रिक नीति की नई जवाबदेही तय की थी मुद्रास्फीति को निशाना बनाना। समिति के अधिकार बढ़ाने के लिए गैर-सरकारी सदस्य बढ़ाने की बात थी। यह 2015-16 में किया गया था। एफएसएलआरसी ने कल्पना की थी कि प्रतिभूति अपील पंचाट वह मंच होगा जहां सभी वित्तीय एसआरए के विरुद्ध अपील की जाएगी। यह रिजर्व बैंक के अलावा सभी वित्तीय एसआरए के लिए किया गया है।
एसआरए के विधायी कार्य के लिए एफएसएलआरसी ने लोकतंत्र की कमी को बोर्ड की भूमिका और संरचना विशेषज्ञता और परामर्श के माध्यम से दूर करने की सिफारिश की। नियामक नियमन का मकसद साफ करे, बताए कि किन बाजार विफलताओं को इससे ठीक किया जाएगा और इसमें क्या खर्च तथा फायदा होगा। इसके बाद कम से कम खर्च वाले उपाय को चुना जा सकेगा। सार्वजनिक मशविरा जरूरी है और फिर बोर्ड ही सभी कानूनों को अधिकृत कर सकता है। इससे कानून बेहतर बनेगा और उसकी वैधता भी बढ़ेगी।
हालांकि एफएसएलआरसी की वित्तीय संहिता को कानून का रूप नहीं दिया गया किंतु इस पर आगे बढ़ने की गुंजाइश तो हमेशा रहती है। भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण ने पहल करते हुए जून 2016 में कायदे बनाने वाली व्यवस्था शुरू की। नवनियुक्त ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवालिया बोर्ड ने भी 2017 में इसकी व्यवस्था की थी। पेंशन फंड नियामकीय एवं विकास प्राधिकरण ने 2024 में इसकी व्यवस्था जारी की। सेबी ने एक और साल तक इंजतार किया और तीन महीने पहले ऐसा कर सका। रिजर्व बैंक ने भी पिछले दिनों यह व्यवस्था जारी कर दी।
इससे हमें बदलाव के सिद्धांत का पता चलता है। सरकार में शामिल व्यावहारिक लोग अक्सर कहते हैं कि उन्हें बाहरी विशेषज्ञों की सलाह नहीं चाहिए क्योंकि उन्हें हकीकत पता है और वे दफ्तर में बैठकर ज्ञान नहीं देते रहते। देश में आर्थिक सुधारों का वास्तविक इतिहास पूरी तरह शोध और सुधार समुदाय की दास्तान है।
एफएसएलआरसी खुद भी शोध एवं सुधार करने वालों की मेहनत का फल है, जो 1990 के दशक की शुरुआत से ही चल रहा था। 2011 से 2015 के बीच एफएसएलआरसी के भीतर जमकर बहस हुई और आम सहमति बनी। विचारों को दस्तावेजों, पत्रों, ब्लॉग लेखों, वीडियो का रूप दिया गया। धीरे-धीरे लोगों को बात पसंद आई और माहौल बदल गया। इस लंबी यात्रा के जरिये भारत में विनियमन की लोकतांत्रिक वैधता के मानदंड बदल गए। अगले 10 सालों में कायदे लिखने के लिए बनाई गई अपनी ही प्रक्रिया को बेहतर बनाने, प्रत्येक वित्तीय एसआरए के भीतर क्षमता निर्माण करने के लिए पूरी प्रक्रिया का पालन करने और इन प्रक्रियाओं को कानून का जामा पहनाने का काम किया जाना चाहिए।
Date: 21-05-25
भ्रष्टाचार की परतें
संपादकीय
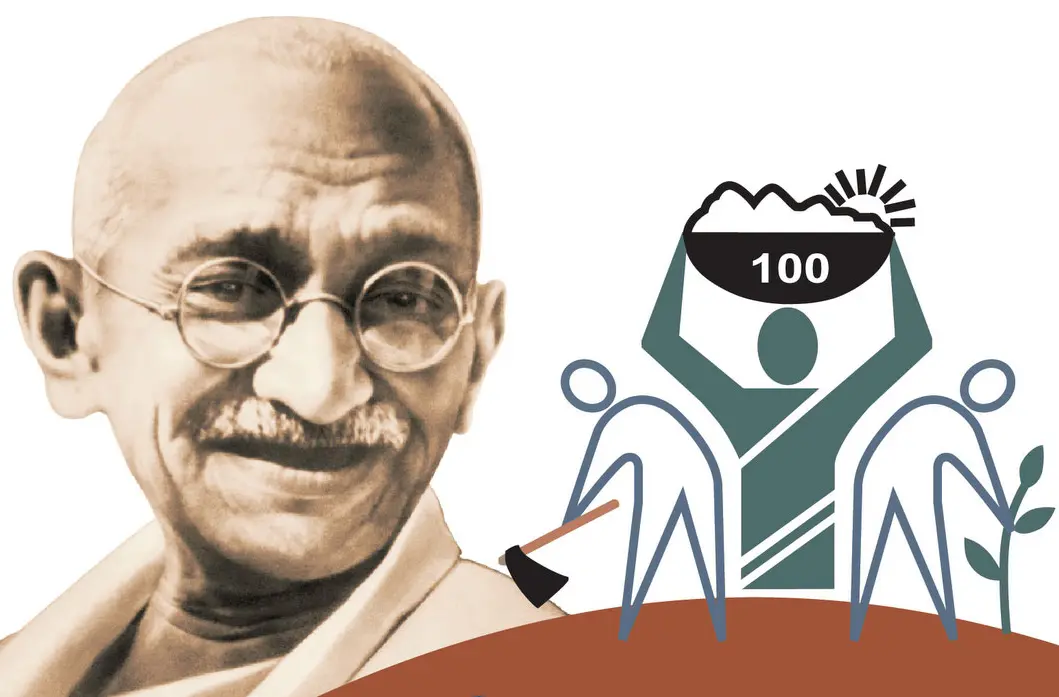
यह स्थापित तथ्य है कि अधिकतर सरकारी योजनाएं अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाती। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा की स्थिति भी इससे अलग नहीं है। इस योजना की शुरुआत इस मकसद से की गई थी कि गरीब परिवारों को साल में कम से कम सौ दिन रोजगार मिल सकेगा और उन्हें अपने भरण- पोषण के लिए किसी दूसरी योजना का मुखापेक्षी नहीं रहना पड़ेगा। मगर शुरुआती वर्षों में ही इसमें भ्रष्टाचार उजागर होने लगे थे। फर्जी नाम दर्ज कर काम देने की बड़ी चालबाजियां सामने आई थीं। उसे रोकने के कई उपाय किए गए, पर इस पर पूरी तरह विराम नहीं लग सका। इस योजना को बंद करने या इसका स्वरूप बदलने का फैसला इसलिए नहीं किया जा सका कि संविधान में इसकी गारंटी दी गई है। सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार का ताना-बाना संबंधित महकमों में ही बुना जाता है। इसका ताजा उदाहरण गुजरात में मनरेगा के तहत फर्जी तरीके से कार्य निष्पादन के दस्तावेज तैयार कर करोड़ों की रकम भुना लेने का है। पुलिस ने इस मामले में अब तक ग्यारह लोगों को गिरफ्तार किया है, जिन्हें सड़क, बांध, पुलिया आदि निर्माण के लिए सामग्री मुहैया कराने का ठेका दिया गया था।
इस घोटाले ने इसलिए तूल पकड़ा और राजनीतिक रंग ले लिया है कि इसमें वहां के पंचायत और कृषि राज्यमंत्री के दो बेटों को भी गिरफ्तार किया गया है। उनकी एजेंसियां भी मनरेगा परियोजनाओं में शामिल थीं। उन्होंने कार्यों का निष्पादन किए बगैर फर्जी दस्तावेज जमा कर भुगतान प्राप्त कर लिया। मनरेगा की जिन परियोजनाओं में उन्होंने घोटाला किया, वे वहां के आदिवासी इलाकों में चलाई जा रही थीं इसके अलावा, फिलहाल जांच में पैंतीस ऐसी एजेंसियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, जिन्होंने 2021 से 2024 के बीच सरकारी अधिकारियों से मिलीभगत करके जाली दस्तावेजों के आधार पर इकहत्तर करोड़ रुपए का भुगतान प्राप्त कर लिया। अभी तक जिला ग्रामीण विकास एजेंसी यानी डीआरडीए की जांच में सामने आए एक जिले के तथ्यों के आधार पर ये गिरफ्तारियां हुई हैं। इसलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि पूरे राज्य में इस योजना के तहत कितने बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ होगा। उन आदिवासी इलाकों में बुनियादी सुविधाओं की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है, जिनके लिए ये परियोजनाएं चलाई तो गई थीं, पर वे केवल कागजों में दर्ज होकर रह गई।
आमतौर पर गरीबों के लिए चलाई जाने वाली योजनाएं और कार्यक्रम जमीन पर कम ही उतर पाते हैं। दिखाने के लिए जो कुछ काम होते भी हैं, उनकी गुणवत्ता सदा संदिग्ध रहती है। उनमें इस्तेमाल सामग्री और कामकाज की गुणवत्ता इस कदर खराब होती है कि सड़कें, पुल- पुलिया वगैरह पहली ही बारिश में धुल कर साफ हो जाते | ग्रामीण विकास के नाम पर अनेक योजनाएं चलाई जाती हैं, केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की तरफ से, मगर वास्तव में उनसे गांवों का चेहरा कितना बदला है, कहना मुश्किल है। ऐसे वक्त में, जब अस्सी करोड़ से ऊपर लोगों को मुफ्त के राशन पर निर्भर रहना पड़ रहा है, मनरेगा जैसी रोजगार गारंटी योजना में इतने बड़े पैमाने पर व्याप्त भ्रष्टाचार विकास के दावों का विद्रूप ही कहा जाएगा। गुजरात को विकास के आदर्श के रूप में प्रचारित किया जाता है। जब वहां स्थिति ऐसी है, तो दूसरे राज्यों में इस योजना की हालत का अंदाजा लगाया जा सकता है।
Date: 21-05-25
आतंक के विरुद्ध निर्णायक कदम
जीवीएल नरसिम्हा राव, ( लेखक पूर्व सांसद हैं )
पाकिस्तान के आतंकी संगठनों, लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) और जैश-ए-मोहम्मद के मुख्यालयों तथा प्रशिक्षण ठिकानों पर सटीक हमले करने में भारत की अभूतपूर्व क्षमताओं को दुनिया ने देखा आपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति में एक आदर्श बदलाव का संकेत देता है। नया सिद्धांत सीमा पार से आतंकवाद के किसी भी कृत्य को युद्ध की कार्रवाई मानता है। अब भारत आतंकियों को दंडित करने के लिए सीमा पार जाकर आक्रामकता से मुकाबला करेगा।
ऐसे समय में जब पूरे देश में राष्ट्रवाद का जोश है और हमारे सशस्त्र बलों पर गर्व किया जा रहा है, कांग्रेस द्वारा सैन्य संघर्ष की अचानक समाप्ति पर सवाल उठा कर सरकार की सफलता को नकारने का प्रयास किया जा रहा है। संघर्ष विराम के समय और अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा इसकी पूर्व घोषणा पर सवाल उठा कर कांग्रेस ने एक ऐसा विचार गढ़ने का प्रयास किया है कि भारत ने 1971 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में स्थिति को बेहतर तरीके से संभाला था। आपरेशन सिंदूर की योजना लश्कर और जैश-ए-मोहम्मद के खिलाफ एक तेज और दंडात्मक हमले के रूप में बनाई गई थी। इसका उद्देश्य कभी एक लंबा, पूर्ण विकसित, बिना रोक-टोक वाला युद्ध नहीं था अपना मकसद हासिल करने के बाद, तब तक आपरेशन जारी रखने की कोई आवश्यकता नहीं थी, जब तक पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई नहीं करता। सात मई की सुबह आधिकारिक प्रेस वार्ता में ही यह स्पष्ट कर दिया गया था। सिंधु जल संधि को निलंबित करके पाकिस्तान पर भारी दबाव बनाने, व्यापार प्रतिबंध लगाने और उसके आतंकी ढांचे तथा हवाई ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचाने के बाद भारत ने पाकिस्तान के संघर्ष विराम प्रस्ताव पर सहमति जताई थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन-सा देश किसकी तरफ से पहल करता है, जब तक कि परिणाम हमारे उद्देश्यों के अनुरूप हों।
राहुल गांधी को अपनी पार्टी के वरिष्ठ सांसदों, शशि थरूर और पी चिदंबरम के विचारों पर ध्यान देना चाहिए था, जिन्होंने संघर्ष विराम के फैसले का समर्थन किया था। दोनों ही राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश मामलों के अनुभवी हैं। चिदंबरम ने प्रधानमंत्री की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने व्यापक युद्ध के खतरों को पहचान लिया और बुद्धिमानी से चुनिंदा लक्ष्यों तक सीमित एक संतुलित सैन्य प्रतिक्रिया का चयन किया है। शशि थरूर ने कहा कि भारत जो सबक देना चाहता था, वह दे दिया गया है।
भारत ने दृढ़ इच्छाशक्ति का परिचय दिया और आतंकियों को दंडित करने के लिए एक सशक्त और आक्रामक दृष्टिकोण अपनाया है। चाहे वह उरी पुलवामा या पहलगाम में आतंकी घटनाएं हों, भारत ने लक्षित और हवाई हमले कर जघन्य कृत्य करने वाले आतंकियों, संचालकों और प्रायोजकों को दंडित किया है। प्रत्येक कार्रवाई के साथ, भारतीय हमले पाकिस्तान में और अधिक गहरे होते गए, अधिक लक्षित तथा साहसी होते गए। इन सभी अवसरों पर दुनिया ने भारत का समर्थन किया।
इसके विपरीत, वर्ष 2004 से 2014 तक कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद से निपटने में निष्क्रिय दृष्टिकोण अपनाया। यहां तक कि 26/11 के भयावह मुंबई हमले, जिसमें 175 निर्दोष लोगों की जान चली गई। मगर भारत सरकार की ओर से कोई ठोस जवाबी कार्रवाई नहीं की गई। यूपीए ने अंतरराष्ट्रीय कार्रवाई की मांग कर आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई को दूसरे देशों के कंधों पर डाल दिया, लेकिन आतंकवादियों को न्याय के कठघरे में लाने के लिए अपनी ओर से कोई जवाबी कार्रवाई की योजना नहीं बनाई। यह दृष्टिकोण 26/11 मुंबई हमले के बाद 11 दिसंबर, 2008 को संसद में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बयान से स्पष्ट है। उन्होंने कहा, ‘… हमें अंतरराष्ट्रीय समुदाय को आतंकवाद के केंद्र, जो पाकिस्तान में स्थित है, से सख्ती और प्रभावी ढंग से निपटने के लिए प्रेरित करना होगा। आतंकवाद के बुनियादी ढांचे को स्थायी रूप से नष्ट करना होगा… अंतरराष्ट्रीय समुदाय की राजनीतिक इच्छाशक्ति को जमीन पर ठोस और निरंतर कार्रवाई में बदला जाना चाहिए।’
यूपीए सरकार की उस वक्त की प्रतिक्रिया में न तो पाकिस्तान के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की मंशा दिखाई दी और न ही उसे कोई चेतावनी दी गई। जवाबी कार्रवाई के लिए कांग्रेस की राजनीतिक इच्छाशक्ति तब भी नहीं थी, जब हमारे सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी शिविरों के खिलाफ लक्षित हमले करने की इच्छा व्यक्त की थी। उस समय के एअर चीफ मार्शल फली होमी मेजर ने बाद में खुलासा किया कि 26/11 हमले के दो दिन बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ बैठक में उन्होंने अन्य दो सेना प्रमुखों की मौजूदगी में कहा था कि भारतीय वायु सेना नियंत्रण रेखा के पार लक्षित हमले के लिए तैयार है, लेकिन सरकार ने उनकी योजनाओं को हरी झंडी नहीं दी। ऐसे में क्या कांग्रेस के पास प्रधानमंत्री पर सवाल उठाने का कोई नैतिक अधिकार हैं?
कांग्रेस द्वारा आपरेशन सिंदूर की तुलना 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध से करना सही नहीं है, क्योंकि हर संघर्ष का एक संदर्भ होता है। 1971 का भारत-पाकिस्तान युद्ध पूर्वी पाकिस्तान में दमनकारी पाकिस्तानी सैन्य शासन के अत्याचारों के खिलाफ आठ महीने लंबे गृहयुद्ध के बाद लड़ा गया था। पाकिस्तान की आंतरिक समस्या भारत के लिए एक आंतरिक समस्या बन गई थी विदेशी सहायता और मुद्रा कोष, विश्व बैंक ऋण पर निर्भर भारत की डांवाडोल अर्थव्यवस्था के समय, इंदिरा गांधी ने उचित समझा कि भारत के लिए पूर्वी पाकिस्तान में सैन्य हस्तक्षेप करना आर्थिक रूप से फायदेमंद है, बजाय इसके कि एक करोड़ शरणार्थियों का अपनी अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ पड़ने दिया जाए। इसके अलावा, इंदिरा गांधी के पास युद्ध की तैयारी करने और कूटनीतिक संपकों का उपयोग कर अंतरराष्ट्रीय समर्थन हासिल करने के लिए आठ महीने का समय था। इनमें से कोई भी आज प्रासंगिक नहीं है।
आपरेशन सिंदूर की तुलना 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध से करने का प्रयास अनुचित है, क्योंकि दोनों के संदर्भ अलग-अलग हैं। एक घटना की सफलता और परिणामों को दूसरे के चश्मे से देखना संकीर्ण और तर्कहीन है। आज भारत के हित में नया ‘मोदी सिद्धांत’ है। पाकिस्तान और पूरी दुनिया के लिए संदेश स्पष्ट है। भारत के पास बड़े विकास लक्ष्य हैं और वह उन्हें हासिल करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाना चाहता है। अगर पाकिस्तान हमारी शांति भंग करने और हमें अपने राष्ट्रीय लक्ष्यों को हासिल करने से विचलित करने की कोई कोशिश करता है, तो भारत उसे कड़ा सबक सिखाएगा । चीनी विचारक सुन त्जु ने अपनी पुस्तक में लिखा है, ‘वही जीतेगा जो जानता है कि कब लड़ना हैं और कब नहीं लड़ना है।’ प्रधानमंत्री भी यह बात अच्छी तरह जानते हैं। भारत पाकिस्तान के साथ युद्ध तभी लड़ेगा, जब ऐसा करना उसकी प्रगति के हित में हो और इसलिए नहीं कि कांग्रेस पार्टी या कुछ कट्टरपंथी ऐसा चाहते हैं।
Date: 21-05-25
उजाड़ से घिर आया संकट
पंकज चतुर्वेदी

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में बीते कुछ दिनों से गर्मी के साथ आकाश में छाए धूल के गुबार ने सांस के मरीजों के लिए जीवन का संकट खड़ा कर दिया है। हरियाणा के भिवानी में बवंडर ऐसा था कि दृश्यता 200 मीटर नहीं रह गई थी। रेत के तूफान ने राजस्थान के बीकानेर में भी लोगों को भयभीत किया वहां धूल ने सूरज को ढंक दिया और 455 डिग्री की गर्मी को घुटन में बदल दिया। कहने की जरूरत नहीं कि यह रेतीली आंधी पाकिस्तान से उठी थी। वैसे तो हर साल मानसून आने से पहले दिल्ली और उत्तर-पश्चिम भारत में ऐसे धूल भरे तूफान आना आम है। इस मौसम में सऊदी अरब और कभी-कभी सहारा जैसे दूरदराज के इलाकों से उठने वाली धूल पश्चिमी हवाओं के जरिए यहां तक पहुंच जाती है चिंता की बात यह है कि इस तरह के धूल भरे अंधड़ की संख्या और दायरा साल-दर-साल बढ़ता जा रहा है। समझना होगा कि वह सीधे- सीधे जलवायु परिवर्तन का प्रभाव है। 2015 के बाद से ऐसे अंधड़ों की संख्या बढ़ती जा रही है। अंधड़ से जान-माल का नुकसान तो होता ही है, सार्वजनिक संपत्तियों को भी खासा नुकसान होता है। अंतरराष्ट्रीय जर्नल अर्थ साइंस इंफोरमैटिक्स’ में प्रकाशित एक शोध में चेतावनी दी जा चुकी है कि अरावली पर्वतमाला में पहाड़ियों के गायब होने से राजस्थान में रेत के तूफान में वृद्धि हुई है।
भरतपुर, धौलपुर, जयपुर और चित्तौड़गढ़ जैसे स्थानों, जहां अरावली पर्वतमाला पर अवैध खनन, भूमि अतिक्रमण और हरियाली उजाड़ने की अधिक मार पड़ी है, को सामान्य से अधिक रेतीले तूफानों का सामना करना पड़ रहा है। केंद्रीय विश्वविद्यालय राजस्थान के पर्यावरण विज्ञान के प्रोफेसर एल के शर्मा और पीएचडी स्कॉलर आलोक राज के अध्ययन ‘असेसमेंट ऑफ लेंड यूज डायनामिक्स ऑफ द अरावली यूजिंग इंटीग्रेटेड’ में कहा गया है कि गांठ बांध लें कि दिल्ली, राजस्थान के गैर-मरुस्थलीय जिलों और हरियाणा का अस्तित्व अरावली पर टिका है, और अरावली को नुकसान का अर्थ है कि देश के अन्न के एक कटोरे पंजाब तक बालू के धोरों का विस्तार रेत के बवंडर खेती और हरियाली वाले इलाकों तक न पहुंचें, इसके लिए सुरक्षा परत या शील्ड का काम हरियाली और जल धाराओं से संपन्न अरावली पर्वतमाला सदियों से करती रही है। इसरो का एक शोध बताता है कि थार रेगिस्तान अब राजस्थान से बाहर निकल कर कई राज्यों में जड़ें जमा रहा है। सनद रहे कि राजस्थान से सुदूर पाकिस्तान और उससे आगे तक फैले भीषण रेगिस्तान से हर दिन लाखों टन रेत उड़ती है। खासकर गर्मी में यह धूल पूरे परिवेश में छा जाती है। मानवीय जीवन पर इसका दुष्परिणाम ठंड में दिखने वाले स्मोग से से अधिक होता है। विडंबना है कि बीते चार दशकों में यहां मानवीय हस्तक्षेप और खनन इतना बढ़ा है कि कई स्थानों पर पहाड़ की श्रृंखला की जगह गहरी खाई हो गई और इसका एक बड़ा कारण यह भी है कि उपजाऊ जमीन पर रेत की परत का विस्तार हो रहा है।
गुजरात के खेडब्रह्म से शुरू हो कर कोई 692 किमी. तक फैली अरावली पर्वतमाला का विसर्जन देश के सबसे ताकतवर स्थान रायसीना हिल्स पर होता है, जहां राष्ट्रपति भवन स्थित है। अरावली पर्वतमाला को कोई 65 करोड़ साल पुराना माना जाता है, और इसे दुनिया के सबसे प्राचीन पहाड़ों में गिना गया है। ऐसी महत्त्वपूर्ण प्राकृतिक संरचना का बड़ा हिस्सा बीते चार दशक में पूरी तरह न केवल नदारद हुआ, बल्कि कई जगह उतुंग शिखर की जगह डेढ़ सौ फुट गहरी खाई हो गई। असल में अरावली पहाड़ रेगिस्तान से चलने वाली आंधियों को रोकने का काम करते रहे हैं, जिससे एक तो मरूभूमि का विस्तार नहीं हुआ दूसरा इसकी हरियाली, साफ हवा और बरसात का कारण बनती रही।
एक अंतरराष्ट्रीय पत्रिका में छपी रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले दो दशकों में कई अन्य पहाड़ियों के अलावा, ऊपरी अरावली पर्वतमाला की हरियाणा और उत्तरी राजस्थान में कम और मध्य ऊंचाई की कम से कम 31 पहाड़ियां गायब हो गई हैं। ऊपरी स्तर पर पहाड़ियों का गायब होना नरैना, कलवाड़, कोटपूतली, झालाना और सरिस्का में समुद्र तल से 200 मीटर से 600 मीटर की ऊंचाई पर दर्ज किया गया था। याद करें कोई तीन साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार से पूछा था कि आखिर कौन हनुमान जी ये पहाड़ियां उठा कर ले गए? 1975-2019 के दौरान किए गए एक अध्ययन में पता चला कि वन क्षेत्र में सघन बस्तियां बस जाना पहाड़ियों के गायब होने के प्रमुख कारणों में से एक था।
इस अध्ययन के परिणामों से पता चला है कि 1975-2019 के बीच अरावली की 3676 वर्ग किमी. भूमि बंजर हो गई। ऐसे हालात में अंधड़ की मार का दायरा बढ़ेगा। अरावली पहाड़ का उजड़ना अर्थात वहां जंगल और जल निधियों के उजड़ने, दुर्लभ वनस्पतियों के लुप्त होने के दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। तेंदुए, हिरण और चिंकारा भोजन के लिए मानव बस्तियों में प्रवेश करते हैं, और मानव जानवर टकराव के वाकिये बढ़ रहे हैं। जान लें अंधड़ बढ़ने से भी जानवरों के बस्ती में घुसने की घटनाएं बढ़ती हैं अवैध खनन और भूमि अतिक्रमण को कम करने के लिए उपाय किए जाने चाहिए और लगातार क्षेत्र की निगरानी की जानी चाहिए। अरावली को और अधिक नुकसान हुआ तो तेज अंधड़ की मार से दिल्ली भी नहीं बचेगी। चिंताजनक तथ्य है कि बीसवीं सदी के अंत में अरावली के 80 फीसद हिस्से पर हरियाली थी जो आज बमुश्किल सात फीसद रह गई। जाहिर है कि हरियाली ख़त्म हुई तो वन्य प्राणी, पहाड़ों की सरिताएं और छोटे झरने भी लुप्त हो गए।
सनद रहे अरावली रेगिस्तान की रेत को रोकने के अलावा मिट्टी क्षरण, भूजल का स्तर बनाए रखने और जमीन की नमी बरकरार रखने वाले जोहड़ों और नदियों को आसरा देती रही है। अरावली की प्राकृतिक संरचना नष्ट होने की ही त्रासदी है कि वहां से गुजरने वाली साहिबी, कृष्णावती, दोहन जैसी नदियां लुप्त हो रही हैं। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट की एक सर्वे रिपोर्ट बताती है कि जहां 1980 में अरावली क्षेत्र के महज 247 वर्ग किमी. क्षेत्र पर आबादी थी, आज यह 638 वर्ग किमी. पर रह गई है। साथ ही, इसके 47 वर्ग किमी. में कारखाने भी हैं।