
21-01-2025 (Important News Clippings)
To Download Click Here.
अन्नदाता किसानों के प्रति सरकार नजरिया बदले
संपादकीय
केंद्र ने अंततः अपना अफसर भेजकर पिछले 55 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को आश्वस्त किया कि सरकार 14 फरवरी को एमएसपी को कानूनी गारंटी की मांग पर बात करेगी। डल्लेवाल चिकित्सा सहायता लेने पर राजी हो गए हैं। हालांकि उनका स्वास्थ्य काफी गिर चुका है। क्या सरकार को जल्द बातचीत शुरू नहीं करनी चाहिए? किसानों की मांग से अलग सरकारी अर्थशास्त्री इसकी तुलना फ्री- मार्केट के तहत बेहतर विकास दर वाले दूध, मछली, अंडा और फल से करके यह दावा कर रहे हैं कि कृषि उत्पाद भी फ्री – मार्केट के हवाले हों। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा है कि फैक्ट्री उत्पादों जैसे स्टील या सीमेंट या फिर गैर-खेती उत्पादों को मौसम संबंधी आपदा या आढ़तियों द्वारा दाम गिराने का खतरा नहीं होता। अगर आज भी देश की 58 फीसदी कृषि बारिश के भरोसे है तो दोषी कौन है ? कृषि व्यवसाय का टर्म्स ऑफ ट्रेड नकारात्मक है। यानी खाद, बीज या पेस्टिसाइड जैसे औद्योगिक इनपुट, कृषि उत्पादों की अपेक्षा ज्यादा महंगे होते गए हैं। क्या किसी और उत्पाद की महंगाई राजनीतिक रूप से सरकारों को चिंतित करती है जितना अनाज, सब्जियों की कीमतें ? और क्या स्टील और सीमेंट के दाम बढ़ने पर भी विदेश से आयात किया जाता है, जैसा गेहूं, चावल, तिलहन, दलहन, चीनी के लिए किया जाता है? अगर किसानों के सभी 23 जिंसों में तीन ( नारियल, गन्ना और जूट जिनके लिए अलग प्राइस मैकेनिज्म है) को छोड़कर सभी खेत उत्पादों के बाजार और एमएसपी के बीच के अंतर को सरकार किसानों को दे तो भी मात्र 27 हजार करोड़ रु. खर्च होंगे। यह जीडीपी का 0.1 प्रतिशत है। सी-2 फॉर्मूले पर भी यह अंतर मात्र 1.68 लाख करोड़ है। 2022-23 में उद्योगों को 2.08 लाख करोड़ कर्ज और 1.09 लाख करोड़ टैक्स छूट दी गई।
जेल से चुनाव
संपादकीय
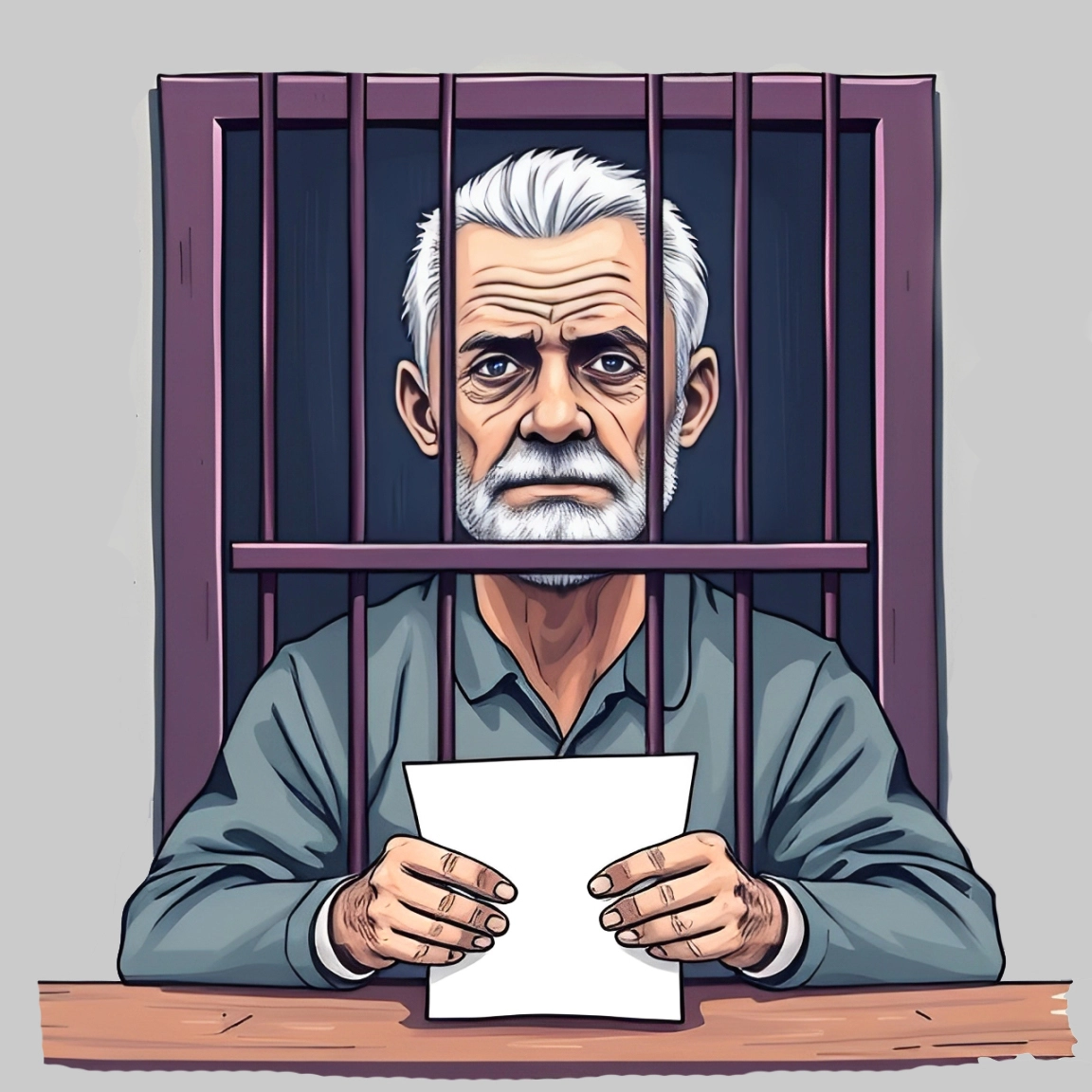 दिल्ली दंगे के आरोपित ताहिर हुसैन की ओर से चुनाव लड़ने के लिए जमानत की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने यह सही कहा कि ऐसे लोगों के चुनाव लड़ने पर रोक लगनी चाहिए। दुर्भाग्य से ऐसा तब तक संभव नहीं, जब तक मौजूदा कानून में बदलाव नहीं होता। इस बदलाव के लिए सरकार को पहल करनी होगी और उसे राजनीतिक दलों का समर्थन करना होगा। कहना कठिन है कि सभी राजनीतिक दल उस कानून को बदलने के लिए तैयार होते हैं या नहीं, जो जेल में बंद लोगों को चुनाव लड़ने की अनुमति देता है। यह अनुमति इस मान्यता के आधार पर मिली हुई है कि दोष सिद्ध न होने तक हर व्यक्ति निर्दोष है। इसके चलते ही कई लोग जेल में बंद होने के बाद भी चुनाव लड़ते हैं और चुनाव प्रचार के लिए जमानत की मांग करते हैं। इनमें वे भी होते हैं, जो गंभीर अपराध के आरोप में जेल में बंद होते हैं। विडंबना यह है कि ऐसे कई लोग चुनाव जीत भी जाते हैं, क्योंकि वे जाति, पंथ, क्षेत्र के नाम पर या फिर अपनी बेगुनाही का रोना रोकर लोगों की भावनाओं को भुनाने में समर्थ हो जाते हैं। होना तो यह चाहिए कि मतदाता अपने प्रतिनिधियों का चयन परिपक्वता से करें, लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता। इसका प्रमाण तब मिला था, जब पिछले लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत जेल में बंद खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह ने पंजाब की खडूर साहिब सीट से जीत हासिल कर ली थी। इसी तरह टेरर फंडिंग में तिहाड़ जेल में बंद इंजीनियर रशीद ने जम्मू-कश्मीर की बारामुला सीट से चुनाव जीत लिया था। इसके बाद विधानसभा चुनाव में उसे इस आधार पर चुनाव प्रचार के लिए जमानत मिल गई थी कि वह अपने दल का प्रमुख है।
दिल्ली दंगे के आरोपित ताहिर हुसैन की ओर से चुनाव लड़ने के लिए जमानत की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने यह सही कहा कि ऐसे लोगों के चुनाव लड़ने पर रोक लगनी चाहिए। दुर्भाग्य से ऐसा तब तक संभव नहीं, जब तक मौजूदा कानून में बदलाव नहीं होता। इस बदलाव के लिए सरकार को पहल करनी होगी और उसे राजनीतिक दलों का समर्थन करना होगा। कहना कठिन है कि सभी राजनीतिक दल उस कानून को बदलने के लिए तैयार होते हैं या नहीं, जो जेल में बंद लोगों को चुनाव लड़ने की अनुमति देता है। यह अनुमति इस मान्यता के आधार पर मिली हुई है कि दोष सिद्ध न होने तक हर व्यक्ति निर्दोष है। इसके चलते ही कई लोग जेल में बंद होने के बाद भी चुनाव लड़ते हैं और चुनाव प्रचार के लिए जमानत की मांग करते हैं। इनमें वे भी होते हैं, जो गंभीर अपराध के आरोप में जेल में बंद होते हैं। विडंबना यह है कि ऐसे कई लोग चुनाव जीत भी जाते हैं, क्योंकि वे जाति, पंथ, क्षेत्र के नाम पर या फिर अपनी बेगुनाही का रोना रोकर लोगों की भावनाओं को भुनाने में समर्थ हो जाते हैं। होना तो यह चाहिए कि मतदाता अपने प्रतिनिधियों का चयन परिपक्वता से करें, लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता। इसका प्रमाण तब मिला था, जब पिछले लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत जेल में बंद खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह ने पंजाब की खडूर साहिब सीट से जीत हासिल कर ली थी। इसी तरह टेरर फंडिंग में तिहाड़ जेल में बंद इंजीनियर रशीद ने जम्मू-कश्मीर की बारामुला सीट से चुनाव जीत लिया था। इसके बाद विधानसभा चुनाव में उसे इस आधार पर चुनाव प्रचार के लिए जमानत मिल गई थी कि वह अपने दल का प्रमुख है।
इससे बड़ी विडंबना और कोई नहीं कि जेल में बंद लोगों को मतदान करने की अनुमति तो नहीं होती, लेकिन वे चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र होते हैं। चुनाव लड़ने के लिए जमानत मांग रहे ताहिर हुसैन पर हिंसा भड़काने के बेहद गंभीर आरोप हैं, लेकिन इससे सांसद असदुद्दीन ओवैसी पर कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने सब कुछ जानते हुए भी उसे अपने दल से दिल्ली विधानसभा का उम्मीदवार बना दिया। यह समझा जाना चाहिए कि आतंक, अलगाव, दंगे और हत्या सरीखे गंभीर अपराध में लिप्त होने के आरोपितों को जेल में बंद होने के बाद भी चुनाव लड़ने की छूट मिलने से भारतीय लोकतंत्र का मान नहीं बढ़ता। इससे तो राजनीति के अपराधीकरण को ही बल मिलता है। उचित यह होगा कि संगीन आरोपों में जेल में बंद लोगों को चुनाव लड़ने से रोका जाए। निःसंदेह बंदियों के भी कुछ अधिकार होते हैं, लेकिन उनके लिए चुनाव लड़ने को मौलिक अधिकार बना देना बिल्कुल भी ठीक नहीं।
Date: 21-01-25
शासन का विकेंद्रीकरण करे सरकार
आदित्य सिन्हा, ( लेखक लोक-नीति विश्लेषक हैं )
 केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। इस पहल से 50 लाख केंद्रीय कर्मी और 65 लाख पेंशनर लाभान्वित होंगे। आयोग मौजूदा वेतन, पेंशन एवं भत्तों के ढांचे को महंगाई एवं जीवनयापन की लागत में वृद्धि जैसे वृहद आर्थिक संकेतकों की कसौटी पर कसेगा। विभिन्न हितधारकों के साथ साथ परामर्श के बाद आयोग इसका एक सुसंगत ढांचा तैयार करेगा। आयोग की अनुशंसाएं स्वीकार किए जाने के बाद कर्मचारियों के वेतन-भत्तों और पेंशन में बढ़ोतरी होगी, जिससे घरेलू उपभोग में तेजी आने के साथ ही समग्र आर्थिक को बड़ा सहारा मिलने की उम्मीद है। जहां तक वेतन आयोग की कार्यप्रणाली का प्रश्न है तो आयोग मुख्य रूप से मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते को नए वेतन ढांचे के साथ जोड़कर देखता है और फिर उसमें वास्तविक बढ़ोतरी को जोड़ता है। इस वास्तविक बढ़ोतरी को फिटमेंट फैक्टर कहते हैं। फिटमेंट फैक्टर में महंगाई का दायरा, कर्मियों की जरूरतें एवं वित्तीय बोझ को उठाने की सरकार की क्षमता जैसे पहलू होते हैं।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। इस पहल से 50 लाख केंद्रीय कर्मी और 65 लाख पेंशनर लाभान्वित होंगे। आयोग मौजूदा वेतन, पेंशन एवं भत्तों के ढांचे को महंगाई एवं जीवनयापन की लागत में वृद्धि जैसे वृहद आर्थिक संकेतकों की कसौटी पर कसेगा। विभिन्न हितधारकों के साथ साथ परामर्श के बाद आयोग इसका एक सुसंगत ढांचा तैयार करेगा। आयोग की अनुशंसाएं स्वीकार किए जाने के बाद कर्मचारियों के वेतन-भत्तों और पेंशन में बढ़ोतरी होगी, जिससे घरेलू उपभोग में तेजी आने के साथ ही समग्र आर्थिक को बड़ा सहारा मिलने की उम्मीद है। जहां तक वेतन आयोग की कार्यप्रणाली का प्रश्न है तो आयोग मुख्य रूप से मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते को नए वेतन ढांचे के साथ जोड़कर देखता है और फिर उसमें वास्तविक बढ़ोतरी को जोड़ता है। इस वास्तविक बढ़ोतरी को फिटमेंट फैक्टर कहते हैं। फिटमेंट फैक्टर में महंगाई का दायरा, कर्मियों की जरूरतें एवं वित्तीय बोझ को उठाने की सरकार की क्षमता जैसे पहलू होते हैं।
सातवें वेतन आयोग में आधिकारिक बढ़ोतरी 14.2 प्रतिशत हुई थी, जो संभव है कि उतनी अधिक न लगे, मगर जब इसमें आवास भत्ते यानी एचआरए जैसे अन्य पहलुओं को जोड़ें तो यह काफी अधिक दिखेगी, क्योंकि उसका आकलन नए एवं ऊंचे मूल वेतन के आधार पर किया जाता है। पेंशनरों को भी फिटमेंट फैक्टर का लाभ मिलता है और नए सिरे से आकलन में उनकी पेंशन खासी बढ़ जाती है। परिणामस्वरूप सरकारी खजाने से खर्च उसकी तुलना में काफी अधिक बढ़ जाता है, जितना प्रथमदृष्टया दिखता है। सातवें वेतन आयोग में वेतन बढ़ोतरी से सरकारी खजाने पर वास्तविक बोझ 24 प्रतिशत बढ़ा था।
आठवें वेतन आयोग से भी सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ने के आसार हैं, क्योंकि सरकारी व्यय का एक बड़ा हिस्सा पहले से ही वेतन-भत्तों और पेंशन पर खर्च हो रहा है। हालांकि अंतिम रूप से किस वेतनमान पर सहमति बनती है, यह तो राजनीतिक विवेक पर निर्भर होगा, क्योंकि कर्मचारियों की अपेक्षाओं और सरकारी खजाने के बीच संतुलन साधने की चुनौती होगी। इसके बावजूद आसार यही हैं कि आठवें वेतन आयोग में सातवें जितनी वेतन बढ़ोतरी नहीं होगी। ऐसा इसलिए, क्योंकि एक तो मुद्रास्फीति अपेक्षाकृत नरम है और पिछली बार की तरह पुराने पेंशनरों को एमकुश्त लाभ के दोहराव की उम्मीद कम है, फिर भी नए वेतनमान में मौजूदा की तुलना में खर्च 20 प्रतिशत तक बढ़ सकता है, जिससे देश के आर्थिक उत्पादन में आधे प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हो सकती है। यह तो निश्चित है कि इसके बाद कर्मचारियों की क्रय शक्ति बढ़ेगी। हालांकि इससे केंद्रीय बजट पर बोझ भी बढ़ेगा। खासतौर से तब जब सरकार पहले से ही सामाजिक कल्याण एवं विकास कार्यक्रमों पर काफी खर्च कर रही है। आठवां वेतन आयोग लागू होने के बाद बाद राज्य सरकारों पर भी वेतन बढ़ोतरी का दबाव बढ़ेगा।
यह अच्छी बात है कि सरकार वेतन बढ़ोतरी की दिशा में आगे बढ़ रही है, लेकिन यह भी उतना ही आवश्यक है कि वह अपने ढांचे को सुसंगत एवं सुगठित बनाए। यह न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन वाली संकल्पना को साकार करने का एक बढ़िया अवसर है। केंद्र सरकार अपने कर्मियों का दायरा घटाकर नगरीय निकायों और पंचायतों के स्तर पर स्थानीय शासन ढांचे को सशक्त बनाने पर जोर दे। ये स्थानीय संस्थाएं बिजली, पानी, सड़क और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं को बेहतर तरीके से चिह्नित कर उन्हें प्रभावी रूप से प्रदान करने में कहीं अधिक सक्षम हो सकती हैं। शासन-प्रशासन के विकेंद्रीकरण की पहल से सरकार सार्वजनिक सेवाओं की गुणवत्ता एवं गति बढ़ाने के साथ ही उन्हें और अधिक जवाबदेह बना सकती है। इसके लिए न केवल केंद्र से राज्यों और राज्यों से स्थानीय निकायों को जिम्मेदारियों का भार सौंपना होगा, बल्कि भीमकाय सरकारी ढांचे को भी चुस्त-दुरुस्त बनाना होगा। इसका अर्थ होगा कि कई विभागों का आकार घटाया जाए और एक जैसे विभागों का विलय किया जाए। इससे कार्यों में दोहराव नहीं होगा और सभी अपने एजेंडे की पूर्ति में ही ऊर्जा, समय एवं संसाधन लगाएंगे। इससे एक दूसरे के काम में खलल डालने की परिपाटी भी बंद होगी और शासन का ढांचा लचीला एवं प्रभावी बनेगा। जनता को भी राहत मिलेगी।
नौकरशाही के अनावश्यक बोझ को घटाने की कवायद अमेरिका में बाकायदा शुरू हो गई है। दूसरा कार्यकाल संभालने से पहले ही राष्ट्रपति ट्रंप ने एलन मस्क और विवेक रामास्वामी के नेतृत्व में डिपार्टमेंट आफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी का गठन कर अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। ट्रंप ने अनावश्यक सरकारी खर्च को घटाने के लिए एक समयसीमा भी दी है। इस कवायद में संघीय, राज्यीय एवं स्थानीय शासन के ढांचे में उन पहलुओं को चिह्नित करना शामिल है जिससे पता चले कि किसी स्तर पर कार्य में दोहराव तो नहीं हो रहा। इसके जरिये पुराने ढर्रे वाली व्यवस्था से मुक्ति दिलाना भी शामिल है। उक्त विभाग आधुनिक तकनीक के प्रयोग एवं निजी क्षेत्र के सहयोग से ऐसे सरकारी ढांचे के निर्माण को बल देना चाहता है, जो सक्षम बनकर सार्वजनिक सेवाओं की समग्र गुणवत्ता को बढ़ाने में सहायक हो। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआइ के प्रयोग और आटोमेशन यानी स्वचालन को प्रोत्साहन देने संबंधी अहम सुधार भी शामिल हैं। यह विभाग विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय पर जोर देकर निर्णयन की प्रक्रिया में सुस्ती को दूर करेगा, क्योंकि देरी से अक्सर परियोजनाओं की लागत बढ़ जाती है। तकनीकी नवाचारों पर जोर देने वाले मस्क और बाजार केंद्रित दृष्टिकोण के साथ रामास्वामी अपनी इस पहल के जरिये एक सुगठित एवं पारदर्शी सरकारी ढांचा बनाना चाहते हैं, जो बदल रही सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप तेजी से ढलकर करदाताओं के प्रति अपनी व्यापक जवाबदेही सिद्ध करे।
निःसंदेह आठवां वेतन आयोग लाखों कर्मियों एवं पेंशनरों की आकांक्षाओं की पूर्ति करेगा। अब जब इस आयोग की अनुशंसाएं सरकार का वित्तीय बोझ बढ़ाएंगी, तब वे व्यापक प्रशासनिक सुधारों की आवश्यकताओं को रेखांकित करने का माध्यम भी बननी चाहिए।
ट्रंप से उम्मीदें
संपादकीय
अमेरिका में एक नए युग का आगाज हो रहा है, जो बड़े बदलावों की ओर इशारा कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का राष्ट्रपति के रूप में यह नया दौर कैसा होगा ? राष्ट्रपति चुने जाने के बाद से ही वह कई संकेत ऐसे दे चुके हैं, जिनसे लगने लगा है कि दुनिया बदलने वाली है। ये बदलाव इस बात पर केंद्रित रहेंगे कि अमेरिका को फिर एक बार महान बनना है। यह ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ का नारा डोनाल्ड ट्रंप की एक नई पहचान बन गया है और बहुत संभावना है कि इस बार ट्रंप अपने सपने को साकार करने के लिए दुस्साहस का भी परिचय दें। पिछली बार जब वह चुनाव हारे थे, तब दुखद उपद्रव हुआ था। उन उपद्रवियों को अगर ट्रंप ने सत्ता में आते ही माफ कर दिया है, तो यह संकेत है कि आने वाले दिनों में ट्रंप का अपने समर्थकों के प्रति कितना उदार रुख रहने वाला है।
अपने समर्थकों पर उनकी कृपा जरूर बरसे, पर उनके विरोधियों के लिए भी अमेरिकी व्यवस्था में जगह रहनी चाहिए। ट्रंप ने अमेरिकी राजनीति के तेवर कलेवर को तो बदला ही है और वह वहां लोकतंत्र को भी बदलने जा रहे हों, तो कोई आश्चर्य नहीं। उनकी टीम के अनेक दिग्गज परिवर्तन के आकांक्षी हैं। न जाने कितने परिवर्तन आगामी चार वर्ष में लागू होंगे। उम्मीद करनी चाहिए कि ट्रंप की नई टीम अमेरिकी परंपराओं का यथासंभव निर्वाह करते हुए ही देश को फिर से महान बनाएगी। हालांकि, महान बनाने के अभियान पर कई सवाल भी हैं। क्या अमेरिकी निर्णायकों ने मान लिया है। कि अमेरिका अब महान नहीं रहा? इस अभियान के नाम से तो शायद यही लगता है कि अमेरिकी विचारकों ने अपने देश के महान न रह पाने की वजहों का पता लगा लिया है। उनकी नजर उन अमेरिकी चालाकियों पर भी निस्संदेह पड़ी होगी, जिनकी वजह से अमेरिकियों की अक्सर आलोचना होती है। अफगानिस्तान आज भी जीवंत उदाहरण है, डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति रहते ही अफगानियों को अपने हाल पर छोड़कर अमेरिकी सेना लौट गई थी। अफगानिस्तान में जो लोग पहले अमेरिकी प्रशासन व सेना के साथ खड़े थे, उनके साथ जो हुआ, वह त्रासद है। ट्रंप से यह उम्मीद जरूर रहेगी, अगर वह किसी बड़े बदलाव को अपने हाथ में लें, तो मैदान न छोड़ें। ट्रंप की टीम को एहसास होना चाहिए कि आज अमेरिका मैदान छोड़ने की वजह से ही अपनी महानता से वंचित हुआ है।
अनेक विद्वान यह मानते हैं कि अमेरिका को शुरू से ही भारत के साथ खड़ा रहना चाहिए था भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और अमेरिका सबसे पुराना जीवित लोकतंत्र है, पर यह अफसोस की बात है कि दोनों के बीच तालमेल वैसा नहीं है, जैसा दुनिया को लोकतांत्रिक या खुशहाल बनाने के लिए होना चाहिए। अमेरिका चूंकि वामपंथी चीन के साथ खड़ा हुआ था, तो आज चीन उसकी बादशाहत को चुनौती देने की स्थिति में पहुंच गया है। आज ट्रंप भी चीन को नजरंदाज करने की स्थिति में नहीं हैं और कम से कम अभी तक ऐसा कोई संकेत भी नहीं है। आशंका है, ट्रंप का नया दौर कहीं मौखिक हमलों या कटु उद्गारों तक ही सीमित न रह जाए। बहरहाल, भारत उनसे कम से कम तीन बड़ी उम्मीदें रखेगा, पहली उम्मीद आर्थिक एवं तकनीकी सहयोग, दूसरी उम्मीद आतंकवाद के खिलाफ ईमानदार रवैया और तीसरी उम्मीद – भारत की गुटनिरपेक्षता का सम्मान ! हालांकि, तमाम दुनिया यही उम्मीद करेगी कि ट्रंप दुनिया में चल रहे बड़े युद्धों और छद्म युद्धों को रोकेंगे, ताकि नई उबरती उभरती दुनिया में अमेरिकी महानता को फिर से बहाल किया जा सके।
Date: 21-01-25
भारतीय आईटी प्रतिभाओं की राह में रोड़े न रखे अमेरिका
एस. श्रीनिवासन, ( वरिष्ठ पत्रकार )
डोनाल्ड ट्रंप ने अब जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति का पद दूसरी बार संभाल लिया है, तो असंख्य भारतीय युवा अमेरिकी वीजा को लेकर संशय व अनिश्चय से घिरे हुए हैं। ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ (एमएजीए) के नारे का मुखर समर्थन करने वाले ट्रंप और उनके समर्थकों ने अप्रवासियों को दुश्मन नंबर एक माना था और चुनाव प्रचार के दौरान वे उन पर निशाना साधते रहे थे। हालांकि, वैध और अवैध अप्रवासियों के बीच फर्क करना चाहिए।
अमेरिका में नई सरकार की नीतियों को लेकर विशेष रूप से बेंगलुरु, हैदराबाद और चेन्नई में चिंता देखी जा रही है। सूचना प्रौद्योगिकी के मामले में देश के ये क्रमशः तीन शीर्ष शहर हैं। भारत में आईटी और बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट में तीन शहरों का दबदबा है। वर्ष 2023 में जारी आंकड़ों के अनुसार, आईटी निर्यात भारत की जीडीपी का लगभग आठ प्रतिशत है और 250 अरब डॉलर से अधिक का राजस्व पैदा करता है। इनमें से आईटी सेवाओं की हिस्सेदारी 51 प्रतिशत है। दक्षिण भारत के इन तीनों शहरों में कम से कम 30 लाख लोग आईटी उद्योगों में कार्यरत हैं। कई अन्य लोग भी विदेश में काम कर रहे हैं, जिनमें से कुछ एच1बी वीजा पर हैं। अमेरिका द्वारा जारी किए गए एच1बी या कार्य बीजा में से 70 प्रतिशत हिस्सा भारत का है। चीन की हिस्सेदारी सिर्फ 12 फीसदी है, इसलिए जब एच1बी वीजा पर किसी प्रतिबंध की बात आती है, तो भारतीय ज्यादा चिंतित हो जाते हैं।
पिछले कुछ वर्षों में भारत की शीर्ष आईटी कंपनियों जैसे टीसीएस, इंफोसिस और विप्रो ने एच1बी वीजा पर अपनी निर्भरता कम करना शुरू कर दिया है। इन कंपनियों द्वारा वीजा की जरूरत में 24 प्रतिशत से 30 प्रतिशत की कमी आई है, क्योंकि उन्होंने अपने कर्मचारियों को ‘ऑफ- शोरिंग’ के बजाय ‘नियर शोरिंग करना शुरू कर दिया है। दिलचस्प बात यह है, अमेजन जैसी कई अमेरिकी कंपनियां भारतीय पेशेवरों के लिए अधिक एच1बी वीजा की मांग कर रही हैं। एच1बी वीजा आम तौर पर भारतीयों के बीच लोकप्रिय रहा है, क्योंकि इससे ज्यादा वेतन मिलता है। साथ ही, यह अमेरिका में ‘ग्रीन कार्ड’ और स्थायी निवास पाने की राह बनाता है। दुनिया की सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को लुभाने के लिए अमेरिका ने इसे तैयार किया था और यह एक शानदार सफलता रही है।
अमेरिका में करीब 15 लाख भारतीय अप्रवासी काम करते हैं। कई लोग एफ-1 या शिक्षा वीजा से अमेरिका पहुंचते हैं। ऐसे तीन लाख छात्र हैं और उनमें से अधिकांश आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु से आते हैं। ट्रंप सरकार की नीतियों को लेकर विशेष रूप से बेंगलुरु, हैदराबाद और चेन्नई में चिंता है | भारत में सूचना प्रौद्योगिकी के ये तीन शीर्ष शहर हैं।
चेन्नई में कई छात्र, जो जनवरी में छुट्टियों पर भारत आए थे, उन्हें उनके संबंधित संस्थानों ने 20 जनवरी से पहले वापस लौटने की सलाह दी थी। कई छात्र, जो एफ-1 वीजा खत्म होने के बाद ओपीटी वीजा पर वहां रुके हैं, वे भी चिंतित हैं कि इसे आगे बढ़ाया जाएगा या नहीं? एक छात्र ओपीटी वीजा पर तीन साल तक रह सकता है, जिसके बाद ग्रीनकार्ड का रास्ता खुल जाता है। वर्ष 2023 में भारतीयों को जारी किए गए ओपीटी वीजा में पिछले वर्ष की तुलना में 41 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है। अमेरिका में 12 लाख तेलगुभाषी आबादी हैं। भारत के आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से ही सबसे अधिक संख्या में छात्र अमेरिका जाते हैं। ‘तेलुगु एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ इंडिया’ के मुताबिक, हर साल साठ से सत्तर हजार छात्र तेलुगु राज्यों से अमेरिका पहुंचते हैं। करीब दस हजार को एच1बी वीजा मिलता है और उनमें से 80 प्रतिशत आईटी क्षेत्र में कार्यरत हैं। एक अनुमान के मुताबिक, करीब दस लाख भारतीय एच1बी वीजा के लाभार्थी हैं। असली चिंता कम से कम 7.25 लाख अन्य लोगों को लेकर है, जिन्हें अवैध प्रवासी माना जाता है। इनमें से कम से कम 17,000 ने सभी कानूनी विकल्पों का उपयोग कर लिया है और उन्हें भारत वापस भेजा जा सकता है। ऐसा हुआ, तो बड़ी शर्मिंदगी होगी।
वैसे, भारत वीजा संकट में अवसर देखे, तो फायदे में रह सकता है। देश अपने उद्योगों को समृद्ध करने के लिए अपने योग्यतम इंजीनियरों, डॉक्टरों व वैज्ञानिकों को वापस ला सकता है। भारत को अपनी विशाल आबादी का लाभ उठाने के लिए योग्यतम पेशेवरों की जरूरत पड़ेगी ही। वैसे भी, भारत के पास अपनी युवा आबादी का लाभ उठाने के लिए कुछ ही दशक शेष हैं।
