
20-12-2024 (Important News Clippings)
To Download Click Here.
Crimes against humanity and an obtuse Indian stance
India’s response to a ‘crimes against humanity’ treaty aligns with its aversion to the Rome Statute and the International Criminal Court
Varsha Singh, [ Varsha Singh is Assistant Professor at the National Law University, Jodhpur, Rajasthan ]
On December 4, 2024, the UN General Assembly (UNGA) adopted a resolution approving the text of a proposed treaty governing the prevention and punishment of crimes against humanity (CAH treaty). This marks the beginning of the negotiation process among states for the conclusion of a CAH treaty. This resolution comes five years after the International Law Commission submitted the draft text of the CAH treaty to the Sixth Committee — the primary forum for considering legal questions in the UNGA. This development is a landmark in the international community’s quest to combat impunity for CAH.
There is a gap in accountability
Alongside genocide and war crimes, CAH are among the grave international crimes which the International Criminal Court (ICC), established under the Rome Statute, seeks to punish. Importantly, genocide and war crimes are also governed by dedicated treaties, i.e., the Genocide Convention of 1948 and the Geneva Conventions of 1949, respectively. However, CAH are governed only under the Rome Statute, which includes specific criminal acts such as murder, extermination, enslavement, deportation, torture, imprisonment, and rape committed as part of a ‘widespread or systematic attack directed against any civilian population, with knowledge of the attack’. CAH were first codified in the 1945 London Charter establishing the Nuremberg Tribunal to investigate and prosecute the crimes committed in connection with the Second World War, and later in the statutes of the International Criminal Tribunal for Yugoslavia, and Rwanda. However, there is no dedicated treaty for CAH yet, creating a gap in terms of accountability in the legal architecture of international criminal justice. There are three reasons justifying the need for a CAH treaty.
First, the jurisdiction of the ICC covers a limited number of states, making it challenging to punish perpetrators of CAH in non-member states. Second, the Rome Statute and the ICC only address individual criminal responsibility. A dedicated CAH treaty would allow for holding states accountable under international law for their failure to prevent the commission of CAH, as is the case with the Genocide Convention of 1948. For instance, in 2019, The Gambia filed a case before the International Court of Justice (ICJ) against Myanmar for alleged violations of the Genocide Convention against the ethnic Rohingya population. A dedicated CAH treaty would create an obligation for state parties to adopt administrative, legislative, or judicial measures to prevent the commission of CAH. Failure to meet this obligation could become the basis for the ICJ’s jurisdiction if the CAH treaty so provides. Third, a CAH treaty presents an opportunity to enlarge the scope of CAH to include, as suggested by various states in the Sixth Committee, starvation of civilian populations, gender apartheid, forced pregnancy, the use of nuclear weapons, terrorism, exploitation of natural resources, and crimes against indigenous populations.
India’s stand
India is not a party to the Rome Statute and has consistently objected to the ICC’s jurisdiction over issues such as the powers of the ICC prosecutor, the role of the UN Security Council under the Rome Statute, and the non-inclusion of ‘use of nuclear weapons and other weapons of mass destruction’ as a war crime. Further, India has argued that crimes committed only during armed conflicts — and not those committed during peacetime — should be considered CAH. Moreover, India does not favour the inclusion of ‘enforced disappearance’ as an act that can constitute CAH. Instead, India advocates for the inclusion of ‘terrorism’ as an act amounting to CAH. India’s response to a CAH treaty aligns with its aversion to the Rome Statute and the ICC. For the last five years, since 2019, India has consistently argued for an ‘in-depth study’ and thorough discussion on the need for a dedicated treaty. India’s stance at the UNGA reflects its scepticism that a CAH treaty might duplicate the already existing regime under the Rome Statute. Further, India takes issue with the exclusion of ‘terror-related acts’ and the ‘use of nuclear weapons’ from the definition of CAH in the proposed treaty. Most importantly, reiterating that it is not a party to the Rome Statute, India has stressed at the UNGA that national legislations and the jurisdiction of national courts are more appropriate fora for dealing with CAH and other international crimes.
Lead the way
Currently, India does not have domestic legislation prohibiting international crimes. In 2018, Justice S. Muralidhar of the Delhi High Court in State vs Sajjan Kumar observed that ‘neither crimes against humanity nor genocide have been made part of India’s criminal law, a lacuna that needs to be addressed urgently’. Nonetheless, there is little or no debate on the need for such laws in the domestic legal and policy spaces. The recent amendments to the criminal law were a missed opportunity to include these crimes in the penal law. This is inconsistent with India’s own insistence on the primacy of national and territorial jurisdiction for dealing with CAH. India should incorporate CAH and other international crimes into its domestic law, even if it is not a party to the Rome Statute, and lead the way in ending impunity for grave human rights violations — a role that befits a true Vishwaguru.
Date: 20-12-24
The social character of scientific knowledge
In science, not knowing is ubiquitous. The problems arise when we don’t know, or choose to overlook, where science ends and faith begins
Vasudevan Mukunth
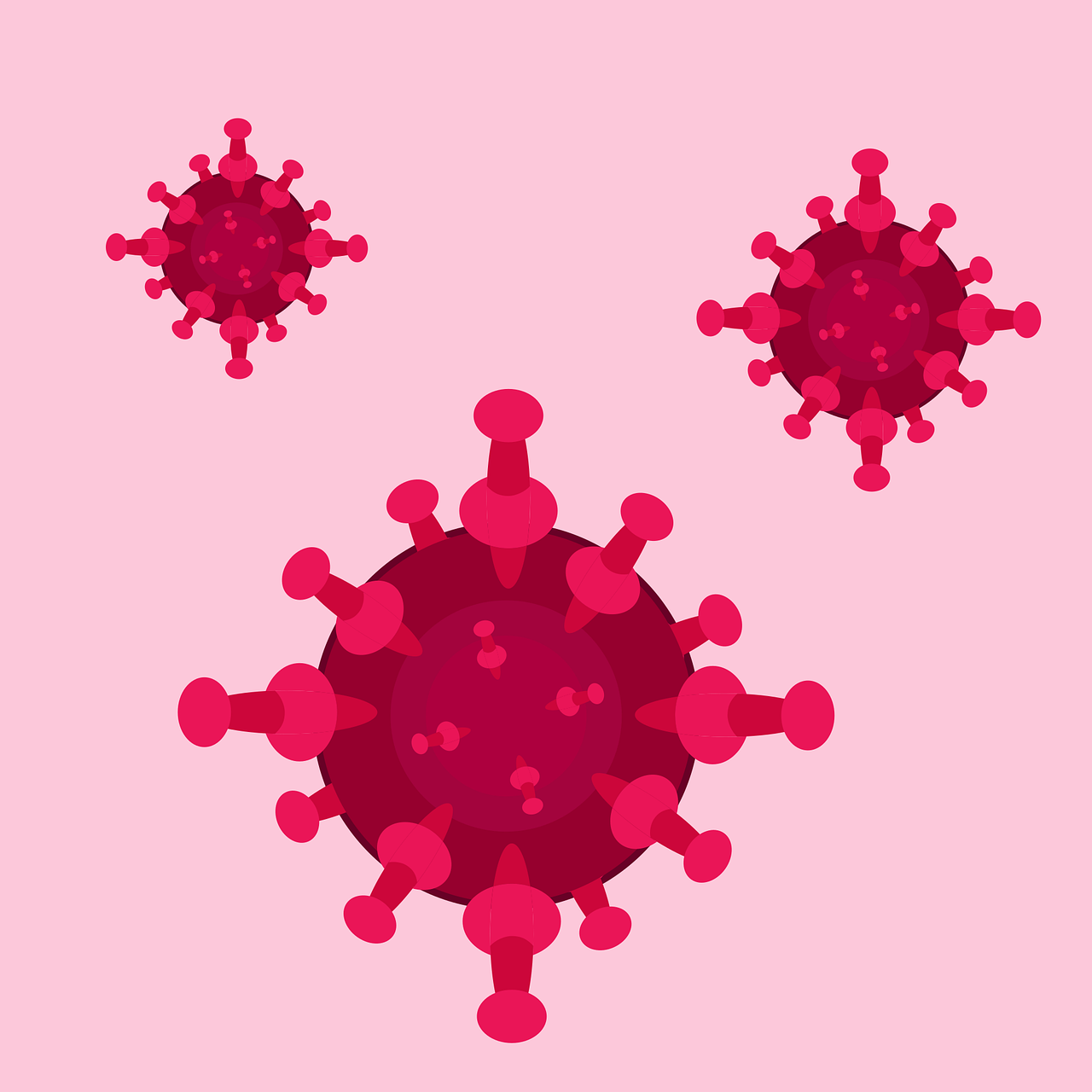
Many of us want to know how the SARS-CoV-2 virus originated. To do that, right now we need to unravel its evolution from its bat coronavirus ancestor by sequencing the genomes of animals and viruses near the outbreak site and we need to effect China’s cooperation to check whether SARS-CoV-2 could have ‘leaked’ from a lab. Where the virus came from was once singularly important because the answer could have pointed the way to avoiding similar outbreaks in future. But today, there is good reason for this question to take the back seat.
We don’t know where or how the virus originated. If it did in a lab, we would have to re-examine how we regulate research facilities and their safeguards and the manner of political oversight that won’t curtail research freedom. If the virus is au naturel, we would have to institute and/or expand pathogen surveillance, eliminate wildlife trafficking, and improve social security measures to ensure populations can withstand outbreaks without becoming distressed. But even as these possibilities aren’t equally likely (according to scientists I trust), the origin of SARS-CoV-2 is less important than it once was because the COVID-19 pandemic caused us to implement all these outcomes to varying degrees.
SARS-CoV-2 isn’t special of course: it’s still difficult to conclusively say what really happened with many things, scientifically. In 1977, a telescope in the U.S. recorded a signal from outer space that remains strange to this day. We don’t have a physical explanation for the “spooky” result of an experiment Anton Zeilinger and co. conducted in 1998. We lack a complete understanding of how general anaesthesia works its magic on the brain. Not even their makers fully know how powerful AI models work the way they do. No existing theory of nature can say what happens in intervals shorter than 10^(-43) seconds.
In fact, not knowing is ubiquitous. To quote philosopher Nicholas Rescher, “no one can say in advance what questions natural science can and cannot answer.” But science communication has taught me not all of us can know everything unless we invest considerable, perhaps even impossible, resources. Years ago, the philosopher Daniel Sarewitz wrote an article that changed my relationship with science. He argued that while we may know about the Higgs boson particle and that it gives other elementary particles their masses, we can’t truly know any of this until we learn the complicated mathematics required to make sense of it. Until then, we just have faith in the physicists who know. This relationship goes for most technical information in our lives.
Science journalists like me communicate science by providing for scientists’ claims, to quote Rescher, “the backing of a rationale that renders [their] correctness evident”, but I still demand a considerable amount of faith from readers. At some point faith also becomes trust but trust still isn’t understanding. (This said, the system of sanctions should they err provides a reasonable backstop for trust in scientists’ and journalists’ work.) The general idea here is that you pick someone you trust and you believe what they say to be true. Let’s call this the social character of scientific knowledge.
When people encounter a weighty concept scientists aren’t able to explain fully, the social character becomes more apparent than it normally is. Some people trust impassioned scientists unwilling to consider extra-scientific possibilities. Some lean towards authority figures who don’t trust science to provide the answer. Historically, people have turned to faith in the face of the unknown. The problems arise when we don’t know, or choose to overlook, where science ends and faith/trust begins. Then we fixate on answers that may never matter at the expense of answers that are already useful.
सांसदों के इस आचरण से देश की गरिमा पर चोट
संपादकीय
जब समाज या राजनीति में अनुशासन, शालीनता और मर्यादित आचरण की जगह स्वेच्छाचारिता, स्वछंदता ले ले और ऐसे आचरण को समाज या नेतृत्व पुरस्कृत करने लगे, तो यह बीमारी सीमा तोड़कर शीर्ष संस्थाओं तक पहुंच जाती है। संसद परिसर में गुरुवार को जो कुछ भी हुआ वह अकल्पनीय था। जाहिर है 75 साल के संसदीय इतिहास में ‘माननीय’ अपनी पार्टी की खैरख्वाही में दूसरी पार्टी के सांसद से धक्का-मुक्की करने लगें तो यह कहना कि भारत में प्रजातंत्र का इतिहास दो हजार साल पुराना है, मजाक लगेगा। सवाल यह नहीं है कि किसने किसको पहले धक्का दिया, यह धक्का सामूहिक था या व्यक्तिगत या पूर्व-नियोजित था अथवा अचानक? क्या औसत 15-20 लाख वोटर्स के प्रतिनिधि देश की सबसे बड़ी प्रजातांत्रिक संस्था के परिसर में अपनी बात कहने या मनवाने का यह तरीका अपनाएंगे या दूसरा पक्ष उससे ज्यादा ताकत से धक्का देकर इसका प्रतिकार करेगा ? देश की गरिमा तो तब बनती जब पहले धक्का देने वाला स्वयं माफी मांगता या प्रतिक्रिया में गिरने या चोटिल होने वाले सांसद को सब मिलकर उठाते और अपनी-अपनी गलती पर क्षोभ व्यक्त करते। देश इससे सीखता । अगर यही समसामयिक सामाजिक स्टैंडर्ड बन गया तो नीचे की सभी संस्थाएं कुछ ऐसा ही करने लगेंगी।
आर्थिक विकास के लिए भी प्रदूषण रोकें
डॉ. भरत झुनझुनवाला, ( लेखक आर्थिक एवं पर्यावरण मामलों के जानकार हैं )

वायु प्रदूषण और आर्थिक विकास में सीधा संबंध दिखता है। कंस्ट्रक्शन यानी भवन निर्माण उद्योग में उड़ने वाली धूल को रोका जाएगा तो कंस्ट्रक्शन की लागत बढ़ेगी और आर्थिक विकास सुस्त पड़ेगा। इसी प्रकार गाड़ियों और उद्योगों के उत्सर्जन एवं किसानों द्वारा पराली जलाने से प्रदूषण अवश्य होता है, लेकिन इससे अर्थव्यवस्था में माल की लागत घटती है और आर्थिक विकास को गति मिलती है। हालांकि प्रदूषण का यह केवल सीधा प्रभाव है। इसी प्रदूषण के अप्रत्यक्ष प्रभाव आर्थिक विकास के विपरीत होते हैं। जैसे भारत में वायु प्रदूषित होने के कारण विदेशी निवेशक और विदेशी पर्यटक नहीं आना चाहते हैं। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य प्रभावित होने से लोगों की औसत आयु घटती है। जो व्यक्ति 70 वर्ष तक कार्य करके आर्थिक विकास में योगदान कर सकता था, वही व्यक्ति प्रदूषण के कारण बीमार पड़ने से पचास साल की उम्र में ही निष्क्रिय होने लगता है। समग्रता में देखें तो प्रदूषण को रोकना आर्थिक विकास के लिए लाभप्रद है। यह हमारी अदूरदर्शिता ही है कि हम प्रदूषण के केवल सीधे नकारात्मक प्रभाव को देखते हैं और अप्रत्यक्ष नकारात्मक प्रभाव को अनदेखा करते हैं।
प्रदूषण पर बढ़ती हुई चिंता को देखते हुए सरकार ने अपने स्तर पर कुछ कदम उठाए हैं। पहला, सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना, दूसरा घर-घर में एलपीजी सिलेंडर का वितरण करना और तीसरा शहरों में मेट्रो रेल का विस्तार। इन कदमों को उठाने के लिए सरकार को साधुवाद, लेकिन ये कदम पर्याप्त नहीं हैं। प्रदूषण नियंत्रण में सबसे बड़ी समस्या कार्यान्वयन की है। गाड़ियों द्वारा प्रदूषण फैलाए जाने के विरुद्ध पुलिस द्वारा कम ही कदम उठाए जाते हैं। इसी प्रकार कंस्ट्रक्शन उद्योग के लिए भी व्यापक कानूनी प्रविधान हैं, लेकिन उन्हें गंभीरता से लागू नहीं किया जाता। जैसे दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने एलान किया कि 21 कंस्ट्रक्शन इकाइयों पर वायु प्रदूषण फैलाने के मामले में 8.35 लाख रुपये का हर्जाना लगाया गया है। किसी कंस्ट्रक्शन परियोजना में हजारों करोड़ रुपये के दांव को देखते हुए यह ऊंट के मुंह में जीरा है। बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी ने कभी-कभी कंस्ट्रक्शन, दिल्ली में बदरपुर बिजली संयंत्र एवं डीजल जेनरेटरों पर प्रतिबंध लगाया है, परंतु ये संकट के समय उठाए जाने वाले अल्पकालिक कदम हैं। बिल्कुल वैसे जैसे मरीज को तत्काल राहत के लिए आइसीयू में भर्ती किया जाता है। ऐसे कदमों से मूल समस्या का समाधान नहीं होता। इसी प्रकार उद्योगों द्वारा किए जा रहे प्रदूषण से निपटने में समस्या उपायों को अमल में लाने के स्तर पर जुड़ी हुई है। अधिकारी उनके मामले में सख्त कदम नहीं उठाते।
अर्थशास्त्र में ‘पब्लिक गुड्स’ यानी सार्वजनिक बेहतरी की एक अवधारणा है। जैसे एक करोड़ रुपये की लागत से कोई सड़क बनाई जाए। यदि सड़क न बनाई जाए तो उस पर जो लाखों लोग चलते हैं, उनके जूते घिसने, समय की बर्बादी एवं गाड़ियों के टायर खराब होने का खर्च मान लीजिए तीन करोड़ आता है। ऐसे में सड़क बनाना आर्थिक विकास के लिए लाभप्रद है। एक करोड़ के खर्च से तीन करोड़ का लाभ मिल सकता है। ऐसे कार्यों को पब्लिक गुड्स कहा जाता है जो मुख्यत: सरकार द्वारा प्रदान किए जा सकते हैं। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जनता से एक करोड़ का टैक्स वसूल करके सड़क बनाए। इससे जनता भी खुश होगी, क्योंकि उसे तीन करोड़ की बचत होगी जबकि एक करोड़ का टैक्स देना होगा। इस प्रकार यह विषय नीति का नहीं, बल्कि कार्यान्वयन का बनता है। सरकार को चाहिए कि वह अदूरदर्शिता छोड़े और वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए पब्लिक गुड्स पर ध्यान केंद्रित करे। गाड़ियों, कंस्ट्रक्शन एवं उद्योगों पर सख्ती करनी चाहिए। इस सख्ती से जितना जनता को नुकसान होगा, उससे कई गुना ज्यादा लाभ मिलेगा। समस्या यही है कि इन पर कार्रवाई से यातायात का खर्च बढ़ता है, मकान बनाने का खर्च बढ़ता है और उद्योगों द्वारा उत्पादन का खर्च बढ़ता है और आर्थिक विकास मंद पड़ता है। इसके बावजूद यदि सरकार इस पर अमल करे तो आर्थिक विकास को गति मिलेगी।
तीन बिंदुओं पर सरकार को नीतियां सुधारनी चाहिए। पहला पराली दहन के संबंध में है। हमें समझना चाहिए कि पराली एक आर्गेनिक उत्पाद है, जिसका उपयोग कागज अथवा बिजली बनाने में किया जा सकता है। इसे खेतों में जलाना अत्यंत हानिप्रद है, क्योंकि हम वायु प्रदूषण के साथ-साथ अपनी बहुमूल्य वस्तु को जला रहे हैं। सरकार को चाहिए कि भारतीय खाद्य निगम यानी एफसीआइ को निर्देश दे कि वह जिस प्रकार गेहूं और धान की खरीद करता है, वैसे ही वह पराली खरीदे। फिर उसे कागज उद्योग अथवा बिजली संयंत्रों को बेचा जा सकता है। सरकार को इसमें कुछ घाटा होगा, क्योंकि पराली को खेत से बटोर कर निगम के गोदाम तक लाने में खर्च आएगा, जबकि पराली का विक्रय संभवतः कम मूल्य पर होगा। इस घाटे को सरकार को वहन करना चाहिए, क्योंकि स्वच्छ वायु एक पब्लिक गुड है और उसके लिए इस खर्च का वहन किया जाना चाहिए। दूसरा कदम जलविद्युत से जुड़ा है। यह सही है कि जलविद्युत से सीधे कार्बन उत्सर्जन नहीं होता, लेकिन जल विद्युत से टिहरी जैसी बड़ी झीलों के जरिये मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है, जो पर्यावरण के लिए कार्बन से भी अधिक हानिप्रद है। जलविद्युत परियोजनाओं में जंगल के जंगल पानी में डूब जाते हैं। इससे भी वायु प्रदूषण पर असर पड़ता है। सरकार ऊर्जा के मोर्चे पर सौर एवं पवन ऊर्जा को व्यापक प्रोत्साहन दे और उस सूची में से जलविद्युत परियोजनाओं को हटाए। तीसरी नीति एयर कंडीशनर यानी एसी से जुड़ी है। एसी में बिजली की खपत ज्यादा होती है, जो अंततः प्रदूषण का कारण बनती है। इसलिए सरकार एसी पर टैक्स अधिक लगाए, जिससे उसके स्थान पर पंखों और डेजर्ट कूलर का ज्यादा उपयोग हो। प्रदूषण को लेकर अक्सर पटाखों और आतिशबाजी को भी दोष दिया जाता है, लेकिन यह उतना बड़ा नहीं, अपितु एक तात्कालिक मुद्दा भर है। इसके बावजूद ग्रीन पटाखों को प्रोत्साहन उपयोगी हो सकती है।
संसद में आचरण
संपादकीय
भारतीय संसद के प्रांगण में फिर अप्रिय स्थिति का उत्पन्न होना हर लिहाज से दुखद और निंदनीय है। दो सांसद घायल हो गए, तो कई सांसदों ने धक्का-मुक्की की शिकायत की है। आरोप-प्रत्यारोप की वजह से परिवेश ऐसा बन गया है, मानो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच शुद्ध शत्रुता हो गई हो। और तो और, धक्का-मुक्की, दुर्व्यवहार जैसे आरोपों की पुलिस तक पहुंचने की नौबत आ गई। वास्तव में, यह जो कटुता फैल रही है, उसका समय रहते उपचार करना चाहिए। अगर उपचार न किया गया, तो संसद में काफी कुछ अप्रिय होने की आशंका को बल मिलेगा। दल चाहे जो हो, जो भी सांसद धक्का-मुक्की में शामिल रहे हैं, उन्हें यह संदेश देने की जरूरत है कि संसद ऐसे किसी संघर्ष का अखाड़ा नहीं है। संसद और संविधान, दोनों ही सांसदों से उच्च गरिमा की आशा करते हैं। संसद देश की आवाजों और दलीलों का मंच है, यह किसी भी प्रकार की शारीरिक जोर-आजमाइश का मंच न बने, इसी में सबकी भलाई है। हर सांसद को फिर संसद की आचार संहिता को पढ़ना चाहिए। जो सांसद नहीं जानते, उन्हें बताना चाहिए कि संसद में ऐसे दृश्य को लोग स्वीकार नहीं करेंगे।
सांसदों को समग्रता में सोचना चाहिए कि अगर आगे एफआईआर की राजनीति बढ़ेगी, तो सभी को परेशानी होगी। संसद में तनाव कोई नई बात नहीं है। तनाव और तल्खी का इतिहास रहा है, पर बहुत कम अवसर ऐसे आए हैं, जब शारीरिक बल का दुरुपयोग देखा गया है। संसद भवन के प्रांगण में ही नहीं, बल्कि देश में कहीं भी सांसदों को ऐसे आमने-सामने नहीं आना चाहिए, जैसे गुरुवार को देश ने देखा है। लोकसभा प्रांगण में अच्छा आचरण सुनिश्चित करने की क्षमता और अधिकार जो भी नेता या अधिकारी रखते हैं, उन्हें आगे आना चाहिए। वैसे भी, यह बात छिपेगी नहीं कि वास्तव में धक्का-मुक्की किसने शुरू की। संसद भवन के प्रांगण में जगह-जगह कैमरे लगे हैं। उन कैमरों की मदद से कम से कम यह तो सुनिश्चित करना चाहिए कि सच की जीत हो और झूठ खुद को सुधारे। अगर किसी सांसद के सिर में चोट लगी है, तो यह वैसे भी गंभीर मामला है। भाजपा सांसद प्रताप सारंगी ने यही बताया है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की वजह से एक व्यक्ति उनसे टकराया और वह गिर गए। पक्ष-विपक्ष में आरोप-प्रत्यारोप लगेंगे, पर ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि सच सामने आए। यदि सच सामने न आए, तो कम से कम सभी सांसद ऐसी स्थिति फिर न बनने दें, यह भी पर्याप्त होगा।
यह समझना होगा कि उग्र राजनीति का देश नहीं है। यह अलग-अलग विचारों के बीच सद्भाव, समन्वय की राजनीति का देश है। यह भी सोचना चाहिए कि जिस महापुरुष भीमराव आंबेडकर के नाम पर अप्रिय स्थिति बनी, क्या वह स्वयं ऐसे व्यवहार की प्रशंसा करते? बाबा साहेब का संसद या संविधान सभा में जीवन ज्यादा नहीं रहा, वह दो-दो बार चुनाव हार गए, पर उन्होंने कभी भी अपने विरोधियों, अपने प्रतिद्वंद्वी दल के नेताओं के प्रति द्वेष का भाव नहीं बढ़ाया। बाबा साहेब का भी बार-बार अपमान हुआ, पर उन्होंने कभी आपा नहीं खोया। खुलकर या मुखरता से अपने विचार रखे। कभी किसी को अपशब्द नहीं कहे, कभी किसी बल प्रयोग का हिस्सा नहीं बने। ऐसे बाबा साहेब के नाम पर किसी भी प्रदर्शन या प्रति-प्रदर्शन को शालीनता की सुरक्षित सीमाओं में ही रखना होगा, ताकि संविधान के तहत देश के सर्वोच्च जन-प्रतिनिधि मंच की मर्यादा अक्षुण्ण रहे।
Date: 20-12-24
जनहित की बड़ी समस्या उठे और समाधान तक पहुंचे
विजय केलकर, ( अर्थशास्त्री व शिक्षाविद् )
हाल के वर्षों में भारतीय न्यायपालिका द्वारा स्वतः संज्ञान लेने की शक्ति पर महत्वपूर्ण बहस छिड़ी हुई है। मूल रूप से इसका मकसद सार्वजनिक या जनहित की रक्षा करना और न्याय सुनिश्चित करना है। कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं, जिन पर अगर अदालत संज्ञान न ले, तो सरकार का ध्यान ही नहीं जाएगा। वैसे, अब इस शक्ति के संभावित दुरुपयोग की जांच की जा रही है। हालांकि, यह शक्ति अदालतों के लिए अत्यावश्यक और असाधारण मामलों में हस्तक्षेप का महत्वपूर्ण उपकरण बनी हुई है।
जो मामले पहले से ही निचली अदालतों में चल रहे हैं, जिन मामलों में राजनीतिक प्रेरणा से फैसले प्रभावित हो सकते हैं, वहां भी संज्ञान लेने की परिपाटी ने चिंता बढ़ाई है। इससे न केवल अतिरेक की भावना पैदा होती है, बल्कि समाधान में भी देरी होती है। उदाहरण के लिए, कोलकाता के आर जी कर मेडिकल कॉलेज में एक प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ दुखद बलात्कार और हत्या के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया। यह ध्यान देने की बात है कि इस मामले में कोलकाता उच्च न्यायालय ने पहले ही महत्वपूर्ण कदम
उठा लिए थे। बिना जरूरत सर्वोच्च स्तर पर संज्ञान लेने से निचली अदालतों के क्षेत्राधिकार में भी तनाव पैदा हो सकता है।
कई बार स्वतः संज्ञान की शक्ति किसी मामले में प्रभावी ढंग से हस्तक्षेप करने में नाकाम रहती है। उदाहरण के लिए, शीर्ष अदालत ने कोविड 19 संकट के समय लोगों के स्वास्थ्य के अधिकार की चिंता की थी, जो संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के मौलिक अधिकार का एक प्रमुख घटक है। शीर्ष अदालत के हस्तक्षेप ने शुरू में उम्मीदें जगाई, चिकित्सा सुविधाओं पर सबका ध्यान गया, लेकिन ठोस परिणाम के अभाव ने न्यायिक हस्तक्षेप की सीमाओं को उजागर कर दिया। अगर अदालतें अपने काम में व्यस्त रहें और उनके आदेशों-निर्देशों का कोई नतीजा न निकले, तो न्यायिक शक्ति के प्रति लोगों का विश्वास घटता है।
दूसरा उदाहरण देखिए, यमुना नदी का प्रदूषण आज भी चिंता का विषय है। साल 1994 में प्रारंभिक न्यायिक हस्तक्षेप के बावजूद, इस मामले को देश के राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के पास जाने में दो दशक से अधिक समय लग गया। भारत में सबसे महत्वपूर्ण पर्यावरणीय चुनौतियों में से एक के समाधान में यह देरी स्वतः संज्ञान शक्ति की एक प्रमुख कमजोरी को दर्शाती है। हालांकि, स्वतः संज्ञान लेना महत्वपूर्ण मुद्दों की ओर ध्यान आकर्षित कर सकता है, पर इन मामलों में लंबे समय तक निष्क्रियता अक्सर न्यायिक प्रक्रिया के प्रति निराशा और मोहभंग का भाव पैदा करती है। ध्यान रहे, ऐसा उस देश में हो रहा है, जहां अनेक समस्याओं का समाधान शेष है। आज पर्यावरणीय गिरावट, सामाजिक अन्याय और शासन- प्रशासन की विफलताओं से निपटने के लिए संतुलित व निर्णायक न्यायिक पहल की बड़ी जरूरत है।
गंभीर चिंता के मामलों में अदालतों द्वारा स्वतः संज्ञान लेना बेशक सराहनीय है, लेकिन अनेक मामलों में उसके क्रियान्वयन में कमी निराश कर देती है। एक और उदाहरण देखिए, मणिपुर में जातीय संघर्ष के बीच यौन हिंसा पर सर्वोच्च न्यायालय के हालिया स्वतः संज्ञान के बाद एक समिति का गठन और मामलों को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपना यह तो दर्शाता ही है कि पूर्वोत्तर की समस्या को शीर्ष
स्तर पर गंभीरता से लिया गया है। हालांकि, अदालत के निर्देशों का कमजोर क्रियान्वयन वास्तव में व्यवस्था की कमजोरियों को उजागर करता है। पुनर्वास प्रयास और सांप्रदायिक सद्भाव की बहाली अनिवार्य है, पर इस दिशा में प्रगति धीमी और अपर्याप्त है, जिससे अनेक पीड़ितों को लंबे समय से संकट में रहना पड़ रहा है। ये कमियां न्यायिक निर्देशों को प्रभावी ढंग से लागू करने में मजबूत तंत्र की जरूरत पर भी प्रकाश डालती हैं, ताकि न्याय अदालती कक्षों से परे उन लोगों तक पहुंचे, जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है।
आदर्श स्थिति तो यही है कि ऐसे मामलों में सर्वोच्च न्यायालय अपने और उच्च न्यायालयों, दोनों के लिए दिशा-निर्देश तैयार करे। अदालती आदेशों का जमीन पर ठीक से क्रियान्वयन हुआ या नहीं, यह जांचने की व्यवस्था भी होनी चाहिए। ऐसे कदम से ही न्यायिक विश्वसनीयता व प्रभावशीलता को बल और बढ़ावा मिलेगा।
