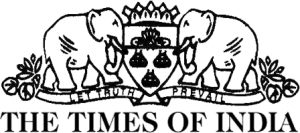18-11-2016 (Important News Clippings)
To Download Click Here
No cloistered virtue
The ends of justice are not served by invoking archaic contempt laws in Katju case

In the Soumya case the Supreme Court acquitted the accused for murder but convicted him to life imprisonment for rape, which Justice Katju criticised in his writing. The subsequent incidents were wholly unwarranted.The court invited the former judge to defend his statements in person, then chose to take umbrage at his writing, issued a contempt notice against him, and then asked security staff to escort him outside the premises. Why did the court have to go through this theatrical public confrontation, when it could have issued a contempt notice on the basis of the blog post alone?The second aspect is even more troubling: the relevance of contempt law in a free society where criticism of the judiciary is inevitable. Judges have vast powers and people will not remain silent about the exercise of such powers. Just as decisions of other branches of government attract criticism, judicial decisions would also invite the same.
The Supreme Court has held that for the judiciary to function effectively, the dignity and authority of the courts must be respected and protected at all costs. But the need to respect the “authority and dignity of the court” is borrowed from a bygone era; it has no basis in a democratic system. The law of contempt should be employed only to enable the court to function, not to prevent criticism.
In many countries contempt jurisdiction is regarded as archaic and exercised sparingly. In the US, courts no longer use contempt to silence comments on judges or legal matters. The First Amendment to the US Constitution forbids imposition of contempt sanctions on a newspaper.The English position is best demonstrated by the Spycatcher’s case in the late 1980s. After the House of Lords delivered the Spycatcher judgment, the Daily Mirror published an upside-down photograph of the Law Lords captioned, “You Old Fools.” But no contempt action was initiated against the newspaper.Lord Templeton, who was a part of the Bench, reportedly said, “I cannot deny that i am Old; It’s the truth. Whether i am a fool or not is a matter of perception of someone else … There is no need to invoke the powers of contempt.”
More recently the Daily Mail ran a photo of the three judges who issued the Brexit ruling with the caption “Enemies of the People”, which many thought was excessive. Yet the courts did not think it necessary to commence contempt proceedings.In contrast, courts in India have adopted a much more authoritative approach. When Arundhati Roy criticised the Supreme Court for vacating the stay for constructing a dam the court, although deciding that Roy had brought it into disrepute, chose not to pursue the matter saying that “the court’s shoulders [were] broad enough to shrug off [these] comments”.
Contempt proceedings were, however, initiated against Roy after she led a demonstration outside the court, with the court finding her affidavit objectionable, where she said “it indicates a disturbing inclination on the part of the Court to silence criticism and silence dissent, to harass and intimidate those who disagree with it. By entertaining a petition based on an FIR that even a local police station does not see fit to act upon, the Supreme Court is doing its own reputation and credibility considerable harm.” The court decided she had committed criminal contempt of court by “scandalising its authority with malafide intentions” and punished her with a day’s imprisonment, with fine.
Until recently, neither truth nor good faith were defences against the law of contempt in India. This was rectified only in 2006 by an amendment to the Contempt of Courts Act. But this was not followed in the Mid-Day case, where the Delhi high court sentenced employees of the publication for contempt of court for publishing content that portrayed a retired Chief Justice of India unfavourably. Mid-Day raised the defence of truth and good faith, but was not entertained.
The dilemma of law and contempt arises because of the need to balance two conflicting principles, ie freedom of expression, and fair and fearless justice. But, as Justice Krishna Iyer said, the law of contempt has a vague and wandering jurisdiction with uncertain boundaries. Such a law, regardless of public good, may unwittingly trample upon civil liberties.Further, the assumption that respect for the judiciary can be won by shielding judges from criticism misjudges public opinion. Surely an enforced silence, in the name of preserving the dignity of the judiciary, would cause resentment, suspicion and contempt, more than it would enhance respect. A mature and “broad-shouldered” approach to criticism can only inspire public confidence, not denigrate the judiciary, for justice, as Lord Atkin said, is “no cloistered virtue”.
Demonetisation
Pre-empt, don’t wait for, taxman terror
So far, the drive against black money has been ham-handed in implementation. An elementary thing would have been to wait for sufficient numbers of fresh currency notes to be printed and ready before withdrawing the old notes. The design of the notes should have been such as not to require recalibration of ATM trays. Whoever thought of printing Rs 2,000 notes bungled — liquidity calls for greater numbers of Rs 500 and Rs 100 notes, when Rs 1,000 notes are withdrawn from circulation. Rabi sowing areas should have received priority in allocation of fresh currency chests.Even now, the terms of withdrawal, deposit and exchange are being chopped and changed almost on a daily basis. How to regulate the conduct of taxmen should be thought through well, before they are unleashed on the public at large. It could be made compulsory for members of raiding teams to wear body cameras throughout the operation, to record their interaction with the subject of the raid. The composition of the raiding teams could be made diverse, drawing officers from different branches. Leave no room for regret ex-post.
Date: 18-11-16
Demonetisation
Extend the income disclosure scheme
The government should extend the Income Disclosure Scheme (IDS) that got over on September 30 till December-end. This would avoid need for any retrospective changes in the tax law to penalise those depositing more than Rs 2,50,000 by taxing them at a rate higher than the IDS rate. More to the point, it would let those who are working assorted stratagems to convert their black money held in demonetised notes into the new currency notes, gold or, dollars, paying a premium for the purpose, a chance to come clean, pay tax and hold only fully accounted for wealth. This would reduce the amount of black money, as compared to a situation in which people convert their existing hoard into a new one fully compatible with the new currency regime. Further, the premium that facilitators of such conversion collect, to add to the country’s black money, would go to the government’s coffers, as part of the tax, surcharge and penalty of 45% they would pay on disclosures under IDS.
The existing tax law allows a person to deposit cash as the current year’s income, and pay the tax applicable on it. Reportedly, the plan is to collect data on all deposits above Rs 2.5 lakh, screen the data and identity those with income that cannot be accounted for. If they have to be charged a rate higher than what people paid under IDS, some retrospective legislation might be called for and that would invite its own odium. The simpler alternative is to extend the IDS and give people one more opportunity, now that full clarity is available that the government is serious about clamping down on black money, to come clean.
But how fair is it to honest taxpayers to keep offering tax evaders an opportunity to come clean on their assets? That question was answered when IDS was first announced. These people who had not paid taxes when they were due have to pay a higher rate of tax and penalty. But once their income becomes above board, the base of taxation would rise permanently. If they are incentivised to stay below the honesty line, the exchequer would be the loser. Extending the IDS is neater.
काले धन पर चुनाव सुधार से ही लगेगी लगाम
उपयोगी साझेदार
इजरायल के राष्ट्रपति रूवेन रिवलिन की भारत यात्रा इस तथ्य को रेखांकित करती है कि दोनों के बीच के रिश्ते तेजी से पनप रहे हैं। रिवलिन भारत की यात्रा करने वाले पहले राष्ट्राध्यक्ष नहीं हैं लेकिन उनकी यात्रा दिखाती है कि दोनों देशों के बीच माहौल कुछ बदला हुआ है। खासतौर पर वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पद संभालने के बाद आया बदलाव स्पष्टï है। राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी उसके बाद ही इजरायल गए। यह किसी भारतीय राष्ट्रपति की पहली इजरायल यात्रा थी। माना जा रहा है कि आगामी वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी भी वहां की यात्रा पर जाएंगे। मोदी खुद हाल ही में कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पार आतंकी शिविरों पर किए गए सेना के हमले की तुलना इजरायल द्वारा अपने पड़ोस में किए गए हमलों से कर चुके हैं। संदेश एकदम साफ है: घरेलू राजनीतिक संवेदनशीलता और अतीत की ऐतिहासिक विरासत अब दोनों देशों के द्विपक्षीय रिश्तों में कोई गतिरोध नहीं हैं। पिछली संप्रग सरकार के कार्यकाल में दोनों देशों के नेताओं की ऐसी यात्राओं के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था।
A challenge and an opportunity
A year and a half after China and Pakistan announced plans for an Economic Corridor, the CPEC, to connect “Kashgar to Gwadar”, the two countries operationalised the trade route this week, with the first shipment moving to Gwadar port and on to the Gulf and Africa. Many of the infrastructure and energy projects that are part of CPEC, worth an estimated $46 billion, are already under way. Of this, $35-38 billion is committed in the energy sector, in gas, coal and solar energy across Pakistan, with the combined expected capacity crossing 10,000 MW. This is roughly double the current shortfall the country experiences. In addition, the 3,000-km rail and roadway project is expected to generate 700,000 jobs by 2030. While Pakistan sees CPEC as a game changer, there are many challenges. There are some misgivings domestically, with critics questioning the project’s viability, and some accusing China of launching a second “East India Company”. There are the security challenges too, especially in the western areas near the key Gwadar port, where militants ranging from Baloch nationalists to the Taliban and the Islamic State have carried out attacks. Systemic challenges include project delays in the CPEC’s first year, which the World Bank warns could prove to be an impediment to Pakistan’s overall growth. Pakistan-India tensions, unless contained, too could endanger sectors of the project where Pakistani troops are engaged in providing security. Finally, the economic slowdown in China and the political instability in Pakistan could impact the project’s future as well.
However, these internal considerations for Pakistan shouldn’t blur the bigger picture for India: CPEC is now a reality. In the past India’s reaction to the project, announced a few weeks before Prime Minister Narendra Modi’s visit to China in 2015, had turned from dismissal and disdain to disapproval and then to outright opposition. India even raised concerns over projects in disputed Gilgit-Baltistan at the UN General Assembly. Not only has the project gone ahead despite the objections, but China now sees CPEC as a physical link between its One Belt, One Road (OBOR) project and the Maritime Silk Route (MSR). India has refused to be a part of either. That Sri Lanka, Bangladesh and Afghanistan are all on board the OBOR and the MSR should give India pause. It is important for Delhi to also take a closer look at the security implications of the China-Pakistan clinch that is fast drawing in Russia in the north, all the way to the Arabian Sea, while China plans a floating naval base off Gwadar.
Date: 17-11-16
Use by date
India’s food safety authority has not been sure-footed on the matter of issuing standards for fortified foods.
On Monday, the Food and Safety Authority of India (FSSAI) announced that it is working on fortification standards for packaged food products such as cereals and biscuits. Fortification means bolstering the nutritional content of a food product by increasing essential micronutrients such as minerals and vitamins. The FSSAI has also issued draft guidelines for five fortified products — rice, wheat, salt, flour, milk and edible oil. For a country long beset by the lack of food safety standards, the new guidelines are a significant first step. However, the food safety authority has not been very surefooted about fortified foods. On the one hand, it is contemplating operationalising the guidelines for rice, wheat, salt, milk and edible oil, even before issuing a final notification. On the other hand, the agency has not specified a deadline for setting standards for packaged foods.
Such vacillation is unfortunate given that there is a growing body of opinion certifying the salience of fortified foods to combat malnutrition. In fact, the first documented evidence of food fortification was in the early 1900s in the US when vitamin B3 was added to coarsely ground corn — the staple of the poor in the country — to help combat the rise of pellagra, a disease caused by the deficiency of this vitamin. In Britain, after the First World War, the government ordered vitamins A and D to be added to margarine because butter had become a scarce commodity in the country. In India, food fortification began in the early 1960s when iodine was added to salt to combat goiter. But while the UK and the US and many other countries have stringent standards on food fortification, India has been slow to get its act together.
The FSSAI’s indecisiveness is especially troubling in view of the government’s recent emphasis on fortified food. In fact on October 16, the Minister of State for Health and Family Welfare Anupriya Patel announced that fortified food would be a key element in the government’s fight against malnutrition. Programmes such as the Mid-Day Meal Scheme, Integrated Child Development Scheme and the Public Distribution System would be mandated to buy and distribute fortified food, she had said. In a country where the unorganised sector plays a significant role in production, processing and packaging of food products, stringent standards are an elementary first step. It is unfortunate that the FSSAI has not been pro-active on the matter.
नोटबंदी अकेला इलाज नहीं
हजार-पांच सौ के पुराने नोट की बंदी को एक हफ्ता हो चला है, मगर आम लोगों की मुश्किलें खत्म होती नहीं दिख रहीं। देश अब भी बैंकों व एटीएम के आगे लाइन में खड़ा है। बीते आठ नवंबर को जब प्रधानमंत्री ने नोटबंदी की घोषणा की थी, तब उन्होंने कहा था कि इस कदम के बाद जाली नोटों का कारोबार बंद होगा, देश में काला धन घटेगा और कैशलेस इकोनॉमी यानी नगदीविहीन अर्थव्यवस्था साकार हो सकेगी। मगर यह सवाल एक हफ्ते के बाद भी हवा में तैर रहा है कि क्या महज नोटबंदी से तमाम मुश्किलों का हल निकल आएगा? और अगर वाकई ऐसा संभव है, तो इस दिशा में देश कितना आगे बढ़ा है?जाली नोट भारतीय अर्थव्यवस्था की एक सच्चाई हैं। सरकारें इनसे बचने के लिए कदम उठाती रही हैं। बार-बार नोटों में नए ‘फीचर्स’ जोड़े जाते हैं। हालांकि यह इस तरह किया जाता है कि आम लोगों को कम से कम परेशानी हो। उन्हें नए नोट के लिए यूं लाइन में न लगना पड़े। इसके लिए समय दिया जाता है, क्योंकि जाली नोट हटाने के लिए तुरंत नोटबंदी की कोई जरूरत नहीं है। असल में,फीचर्स बदल देने से जाली नोटों का कारोबार करने वालों की कमर टूटती है। उनके प्रेस या तमाम साजो-सामान बेकार हो जाते हैं।
मगर चूंकि जालसाज इसका भी तोड़ निकाल लेते हैं, इसलिए नोटों के फीचर्स में बदलाव लगातार जारी रहने वाली एक कवायद है। ऐसा सिर्फ अपने देश में ही नहीं, दुनिया के तमाम मुल्कों में होता है। लिहाजा सरकार का यह उद्देश्य दिल को छूने वाला है, पर इसे इस तरह लागू करना अच्छा नहीं माना जा सकता। इसकी वजह यह भी है कि हम नए नोट में कितने ही फीचर्स डाल लें, जालसाजों के कारण हमें उनमें कुछ दिनों के बाद बदलाव करना ही होगा। ऐसा संभव ही नहीं है कि एक बार नोट बदल लिया और हम पूरी तरह निश्चिंत हो गए। इस बार भी हम यह सोचकर चैन की नींद नहीं ले सकते कि अब जाली नोट इतिहास की चीज बन जाएंगे।
कुछ ऐसा ही हाल काला धन से निपटने के मामले में है। अनुमान यह है कि देश में काला धन का छह फीसदी नगद के रूप में है। हालांकि कुछ लोग इसे आठ तक फीसदी बताते हैं। बाकी पैसा सोना, रियल एस्टेट के रूप में, या बेनामी खातों में या देश से बाहर जमा है। काला धन इसलिए नगद के रूप में ज्यादा जमा नहीं किया जाता, क्योंकि उसका मूल्य अपेक्षाकृत कम हो जाता है। अगर आप आयकर विभाग, सीबीआई या किसी सरकारी संस्थान द्वारा की गई छापेमारी की खबरों को पढ़ें, तो पाएंगे कि जो धन-संपत्ति उनके हाथ लगती है, उनमें नगद बहुत कम होता है।
बाकी चीजों में ज्यादा काला धन है। ऐसे में, यह मानना कि सरकार के इस कदम के बाद काला धन पूरी तरह खत्म हो जाएगा, दिवास्वप्न जैसा है। वैसे भी, भ्रष्टाचार करके अर्जित धन या कर-चोरी की रकम भी काला धन है। यानी आम लोगों को इस पहल का फायदा इस रूप में मिलना चाहिए कि अब भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, राजनीतिक व्यवस्था पारदर्शी हो जाएगी, कर चोरी नहीं होगी, भ्रष्ट आचरण बंद हो जाएंगे आदि-आदि। यह सब नोटबंदी से संभव नहीं है। इसके लिए कर सुधार, पुलिस-नौकरशाही सुधार, पारदर्शी व्यवस्था, शुचिता आदि की दरकार है। अगर यह सब नहीं होता है, तो फिर कोई गारंटी नहीं कि नए नोट के माध्यम से तमाम काले काम आगे नहीं होंगे। इससे हम बेशक काला धन का जमा भंडार (छह से आठ फीसदी) खत्म कर देंगे, मगर उसके प्रवाह को रोकना संभव नहीं होगा।
देखने में यह भी आया है कि जिन लोगों के पास काला धन नगद रूप में जमा है, वे कुछ जोड़-तोड़ करके उसे बदलवा रहे हैं। इसका सीधा अर्थ है कि चोर रास्ते अब भी खुले हुए हैं। बेशक सरकार ने तमाम उपाय किए हैं, मगर उसकी मार आम आदमी ही झेल रहा है। अब हर हाथ में स्याही लगाने की ही बात लें। नए आदेश के बाद अपने पैसे दोबारा लेने के लिए आप या तो जा नहीं पाएंगे, और अगर जाएंगे भी, तो आपको तमाम मुश्किलें आएंगी। जैसे कि आपको यह साबित करना होगा कि इंक इतने दिन पुराना है। ऐसे में, यह मुमकिन है कि रुपये निकालने के लिए आप भी कुछ चोर रास्तों की मदद लें। यानी एक गलत नीति का पोषण हमारी सरकार दूसरी गलत नीति से कर रही है, इसे विडंबना ही कहेंगे।इसी तरह, नगदीविहीन अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने की बात गले नहीं उतर रही। कई देशों में आज मोबाइल से पेमेंट होता है। वहां कम राशि के लेन-देन में भी कोई मुश्किल नहीं आती। सीधे कंपनी के साथ कारोबार होता है। बैंक कोई पक्ष नहीं होता। मगर अपने देश में पिछले दस-पंद्रह वर्षों में मोबाइल की व्यापक पहुंच होने के बाद भी अब तक ऐसा नहीं हो पाया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कई प्रतिबंध लगा रखे हैं। यहां रुपयों का लेन-देन करने वाली कंपनी तब तक शुरू नहीं हो सकती, जब तक कि उसका कोई बैंक अकाउंट न हो।
बेशक यह कोशिश लंबे अरसे से हो रही है कि देश में, खासकर छोटी रकम के लिए ‘नन-बैंक पैमेंट सिस्टम’ हो, पर यह अब तक संभव नहीं हो सका है। आज भी देश में ज्यादातर खरीद-फरोख्त नगदी में होती है। ऐसे में, अचानक नोटबंदी से मुश्किलें आनी ही थीं। हमारा तंत्र अभी नगदीविहीन अर्थव्यवस्था के लिए तैयार ही नहीं है। यानी हम उस रास्ते पर बढ़ चले हैं, जिसकी हमने तैयारी नहीं की थी। जाहिर है, व्यापकता में हमें इसका लाभ नहीं मिलने वाला। मान भी लें कि इससे काला धन खत्म हो जाएगा, तब भी आम आदमी को फायदा मिलता नहीं दिख रहा है। उन क्षेत्रों में कोई बदलाव नहीं होने जा रहा, जिनसे आम लोगों का साबका पड़ता है। सवाल यह है कि क्या उसे अब रिश्वत नहीं देनी होगी? क्या पूरा तंत्र पाक-साफ हो जाएगा?
कोई भी देश इस तरह के कदम नहीं उठाता। मोरारजी देसाई की सरकार ने भी बड़े नोट बंद किए थे। लेकिन वे उस वक्त वाकई में बड़े नोट थे, और जिनका साबका आम लोगों से अमूमन नहीं था। इस बार बंदी की मार पांच सौ और हजार रुपये के नोट पर पड़ी है, जो ट्रान्जेक्शन करेंसी है, यानी उसका आम लोग भी लेन-देन में इस्तेमाल करते हैं। मेरा मानना है कि जब नोटबंदी का फैसला लिया जाता है, तो इससे मिलने वाले फायदे, इसकी लागत और किस रूप में इसे लागू किया जाए, इन सबका गुणा-भाग किया जाता है। इस बार भी किया गया होगा।मगर लगता है कि सत्ता-तंत्र का आकलन गलत था। जब 15 लाख करोड़ के नोट खत्म कर दिए गए और बैंक एक दिन में सिर्फ 10-20 हजार करोड़ रुपये का हस्तांतरण ही कर पा रहे हैं, तो यह स्थिति कब तक बनी रहेगी? क्या सरकार ने इस पर नहीं सोचा था? इस गलती की जिम्मेदारी किसकी है? नोटबंदी के फैसले के पीछे उद्देश्य जो भी रहे हों, वे आर्थिक नजरिये से उचित नहीं दिख रहे। अर्थव्यवस्था के लिहाज से यह फैसला गले नहीं उतर रहा। और रही बात इस फैसले में छिपी राजनीतिक मंशा की, तो इसका जवाब हमारे राजनेता ही देंगे।
इला पटनायक, प्रोफेसर व पूर्व आर्थिक सलाहकार, भारत सरकार
(ये लेखिका के अपने विचार हैं)
सुरक्षा परिषद में भारत की दावेदारी
जापान को सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता मिलने की बात इस कारण भी नहीं सोची जा सकती कि चीन यह कभी पसंद नहीं करेगा।
पिछले सप्ताह संयुक्त राष्ट्र की आमसभा में पंद्रह सदस्यीय सुरक्षा परिषद में सुधार और उसमें भारत की स्थायी सदस्यता की दावेदारी का ब्रिटेन और फ्रांस सहित कई सदस्य देशों ने समर्थन किया। इन देशों ने जोर दिया कि विश्व संस्था की शीर्ष इकाई को निश्चित तौर पर ऐसा होना चाहिए कि जो नई वैश्विक शक्तियों का प्रतिनिधित्व करे। पर प्रश्न है कि क्या ऐसा होना संभव है? 1945 में द्वितीय महायुद्ध की समाप्ति के बाद दुनिया भर के देशों ने मिल कर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की, जो आने वाली पीढ़ियों को महायुद्ध ही नहीं, देशों के बीच युद्ध की विभीषिका से बचाएगा। पर देखा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र के सर्वाधिक शक्तिशाली अंग- सुरक्षा परिषद- को ऐसे अवसरों पर लकवा-सा मार जाता है और वह कुछ नहीं कर पाता। अगर कभी कुछ करता भी है तो तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए इस समय लोगों की रुचि इस बात में है कि सुरक्षा परिषद, जो संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख अंग है, उसमें सुधार कैसे किया जाए। इसका कारण बताया जाता है कि वर्तमान में सुरक्षा परिषद के पांच स्थायी सदस्यों को ‘वीटो’ (निषेधाधिकार) का अधिकार प्राप्त है। ये सदस्य देश हैं- ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, रूस और अमेरिका। इनमें से किसी एक का भी वीटो बाकी चार के बहुमत को अप्रभावी कर देता है। पिछले कुछ वर्षों में वीटो के इस अधिकार का सदस्य देशों ने दुरुपयोग भी किया है, जिसके कारण कई महत्त्वपूर्ण प्रश्न अनसुलझे रह गए या उन पर त्वरित निर्णय नहीं किया जा सका।
इस स्थिति से निपटने के लिए कुछ देशों ने सुझाव दिया है कि सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी जाए या वीटो के अधिकार में संशोधन किया जाए या फिर वीटो का अधिकार ही पूर्णत: समाप्त कर दिया जाए। ये तीनों विकल्प भले एक-दूसरे के विरोधी जान पड़ें, पर इनसे संयुक्त राष्ट्र के शक्ति-संतुलन में निश्चित ही नाटकीय परिवर्तन हो सकेगा और इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र, जो वर्तमान में एक प्रकार से अप्रभावी-सा है, बहुत कुछ प्रभावी हो सकेगा। पर इन तीनों में से कोई भी प्रस्ताव पास होना तो दूर, संयुक्त राष्ट्र की बैठक में विचारार्थ लाया भी जा सकेगा, कहना मुश्किल है। इस स्थिति के लिए स्वयं संयुक्त राष्ट्र जिम्मेदार है। 1945 में सभी मित्र देशों ने आपस में तय करके एक-दूसरे को वीटो का अधिकार दे दिया और उसके बाद इस अधिकार को विधान सम्मत रूप से एक प्रकार से संरक्षित कर आपस में यह भी तय कर लिया कि कोई भी सदस्य इसमें किसी प्रकार की छेड़छाड़ करने की कोशिश नहीं करेगा। ऐसी स्थिति में इन पांच स्थायी सदस्यों के अधिकारों या शक्ति में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने या स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाने की कोशिश तभी सफल हो सकती है, जब वर्तमान सदस्यों में से कोई भी ऐसे किसी प्रस्ताव पर वीटो का प्रयोग न करे, क्योंकि स्थायी सदस्यों में से कोई भी एक सदस्य वीटो का प्रयोग कर बाकी चारों सदस्यों द्वारा पास किए गए किसी भी प्रकार के परिवर्तन के किसी भी प्रस्ताव पर ‘पूर्ण विराम’ लगा सकता है।
फासिस्ट शक्तियों के आक्रमण रोकने में लीग आफ नेशंस की विफलता और महायुद्ध के अनुभवों से मित्र राष्ट्र समझ गए थे कि अंतरराष्ट्रीय अराजकतावाद और आतंकवाद के चलते बेल्जियम, फिनलैंड और थाईलैंड जैसे छोटे देशों पर अगर उनका कोई बड़ा पड़ोसी देश आक्रमण करे तो वे अपनी सुरक्षा नहीं कर पाएंगे। ये सभी राष्ट्र सुरक्षा देने वाले थे, इसलिए नहीं कि वे इसे अपना कर्तव्य या उत्तरदायित्व मानते थे, बल्कि इसलिए कि वे स्वयं अपने को इतना शक्तिशाली समझते थे कि भावी आक्रमणकारियों का सामना कर सकें। दरअसल, इन देशों ने जर्मनी और जापान को पंद्रह-बीस वर्ष बाद की सैनिक शक्ति के सक्रियकरण पर गंभीरता से विचार किया था। भविष्य में किसी भी प्रकार के आक्रमण से निपटने के लिए अमेरिका, रूस और ब्रिटेन ही जिम्मेदार माने जाते थे। इसी कारण आवश्यक समझा गया कि इन देशों को सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट तो मिले ही, युद्ध और शांति के लिए जिम्मेदार संयुक्त राष्ट्र जैसे संगठन पर इन्हें वीटो का अधिकार भी मिले।
इस संबंध में अमेरिका और रूस को संयुक्त राष्ट्र में रखना आवश्यक था। दरअसल, यह लीग आफ नेशंस की निष्क्रियता का परिणाम था। अमेरिका लीग आफ नेशंस का सदस्य कभी नहीं रहा। सोवियत रूस 1930 में सदस्य था, पर जब 1940 में उसने फिनलैंड पर आक्रमण किया, तो उसे निकाल दिया गया। जब रूस फिर सदस्य बना तो जापान, जर्मनी और इटली ने सदस्यता वापस ले ली। लेकिन अगर अमेरिका और रूस को इस टेंट में रहना था तो वे इस बात से भी आश्वस्त होना चाहते थे कि अगर संयुक्त राष्ट्र के किसी प्रस्ताव या कार्य से उनके स्वार्थ पर किसी भी प्रकार की आंच आने की आशंका हो, तो वे उसे रोक सकें। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र के घोषणापत्र में वीटो के अधिकार का प्रावधान किया गया।
उस समय भले वीटो का अधिकार आवश्यक और उचित समझा गया हो, पर आज स्पष्ट देखा जा रहा है कि उससे लाभ की अपेक्षा हानि ही अधिक है। कई बार देखा गया है कि किसी देश में आंतरिक संघर्ष और नागरिक अधिकारों के दुरुपयोग के संबंध में संयुक्त राष्ट्र चाह कर भी इसलिए कुछ नहीं कर पाता कि उसके विरोध में सुरक्षा परिषद के पांचों सदस्यों में से कोई भी वीटो के अधिकार का प्रयोग न कर बैठे। वैसे देखा जाए तो भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका को भी सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। इसके विपरीत इस सुविधा के आलोचकों का कहना है कि ब्रिटेन और फ्रांस की शुरू से चली आ रही स्थायी सदस्यता कालदोष है।
इसके साथ ही सिंगापुर जैसे स्वतंत्र और बहुत कुछ निष्पक्ष देशों का यह भी कहना है कि बड़े देशों को वीटो का अधिकार दिया जाना अपने आप में एक प्रकार से अन्याय है। पांच देशों द्वारा संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठन के किसी कार्य को ठप कर देना ही क्या पर्याप्त बुरा नहीं है कि इसके सदस्यों की संख्या बढ़ा कर अब आठ या दस कर दी जाए! तब फिर इस पद्धति को कैसे बदला जाए। केवल इसके घोषणापत्र में संशोधन से ऐसा किया जा सकता है, यानी जब संयुक्त राष्ट्र की आमसभा के दो तिहाई सदस्य इसके पक्ष में मत दें और पांचों स्थायी सदस्यों में से कोई भी सदस्य विरोध न करे। ऐसी स्थिति में यह सोचना ही व्यर्थ है कि ब्रिटेन और फ्रांस अपना विशेषाधिकार छोड़ने को तैयार होंगे।
जापान को सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता मिलने की बात इस कारण भी नहीं सोची जा सकती कि चीन यह कभी पसंद नहीं करेगा। जर्मनी को इतने अधिक देशों के मत मिल ही नहीं सकते कि वह सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बन सके। ब्राजील को भी इस कारण स्थायी सदस्य बनाने का अवसर नहीं है कि कई दक्षिण अमेरिकी देश उसका समर्थन नहीं करेंगे। ऐसी स्थिति में स्थायी सदस्यता के लिए सबसे प्रबल दावेदार भारत ही बचता है। देश की विशालता, उसकी जनसंख्या, उसकी सुदृढ़ अर्थव्यवस्था, शांति-प्रयासों के लिए संयुक्त राष्ट्र के कार्यों में उसका योगदान और अन्य सभी क्षेत्रों में भी उसकी सुदृढ़ स्थिति और इन सभी के साथ उसके पक्ष में एक बात यह भी है कि संयुक्त राष्ट्र की आमसभा में भी पर्याप्त देशों के वोट उसे मिल सकते हैं। ऐसी स्थिति में सुरक्षा परिषद के पांचों सदस्यों में से कौन उसके विरुद्ध वीटो का प्रयोग करेगा? चीन भी ऐसा करने में कुछ हिचकेगा।
भारत की सुदृढ़ स्थिति के बावजूद इस बात की संभावना बहुत कम जान पड़ती है कि सुरक्षा परिषद के वर्तमान ढांचे में कोई परिवर्तन होगा। पर ऐसा कुछ अवश्य किया जा सकता है, जिससे सुरक्षा परिषद वर्तमान की अपेक्षा अधिक विश्वसनीय और तर्कसंगत प्रतीत हो। जिस समय सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या दस निश्चित की गई थी, उस समय संयुक्त राष्ट्र की आमसभा में कुल पचहत्तर सदस्य देश थे। तब से अब तक यह संख्या बढ़ कर एक सौ तिरानबे हो गई है और निकट भविष्य में कुछ और बढ़ सकती है। ऐसे में अगर अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ा कर दस से अठारह कर दी जाए तो पांच स्थायी सदस्य मिलाकर कुल संख्या तेईस हो जाएगी। इसके साथ ही सुरक्षा परिषद के इस नियम पर भी विचार किया जा सकता है कि सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता केवल दो वर्ष तक रह सकती है।
अगर ऐसा कुछ हो सका तो अधिक देशों को सुरक्षा परिषद की कार्य प्रणाली से परिचित होने का अवसर मिलेगा और दो वर्ष का नियम बना देने से जिन सदस्य देशों का शांति प्रयासों का रिकार्ड अच्छा रहेगा, जैसे भारत और ब्राजील, उन्हें फिर से सदस्य बने रहने का मौका मिल सकेगा। इसके साथ ही यह बात भी विचारणीय है कि पिछले साठ वर्षों में संयुक्त राष्ट्र के घोषणापत्र में कोई संशोधन नहीं हुआ है। वर्तमान स्थितियों को देखते हुए कुछ संशोधन कर देने से लोगों को यह मानने में भी सुविधा होगी कि संयुक्त राष्ट्र का संविधान पत्थर की लकीर नहीं है। इसके बावजूद आलोचकों को यह कहने को रहेगा ही कि पांचों बड़े (अगर भारत भी सदस्य बन गया तो छह) स्थायी सदस्यों के पास वीटो का अधिकार तो रहेगा ही। फिर भी हमें मानना पड़ेगा कि वीटो का प्रश्न इतना महत्त्वपूर्ण नहीं है और न ही इससे सुरक्षा परिषद की उपयोगिता या महत्त्व में कोई कमी आती है।