
18-08-2023 (Important News Clippings)
To Download Click Here.
 Date:18-08-23
Date:18-08-23
Language, Milords
SC’s handbook aimed at removing sexist descriptors for women will hopefully clean up judicial discourse.
TOI Editorials
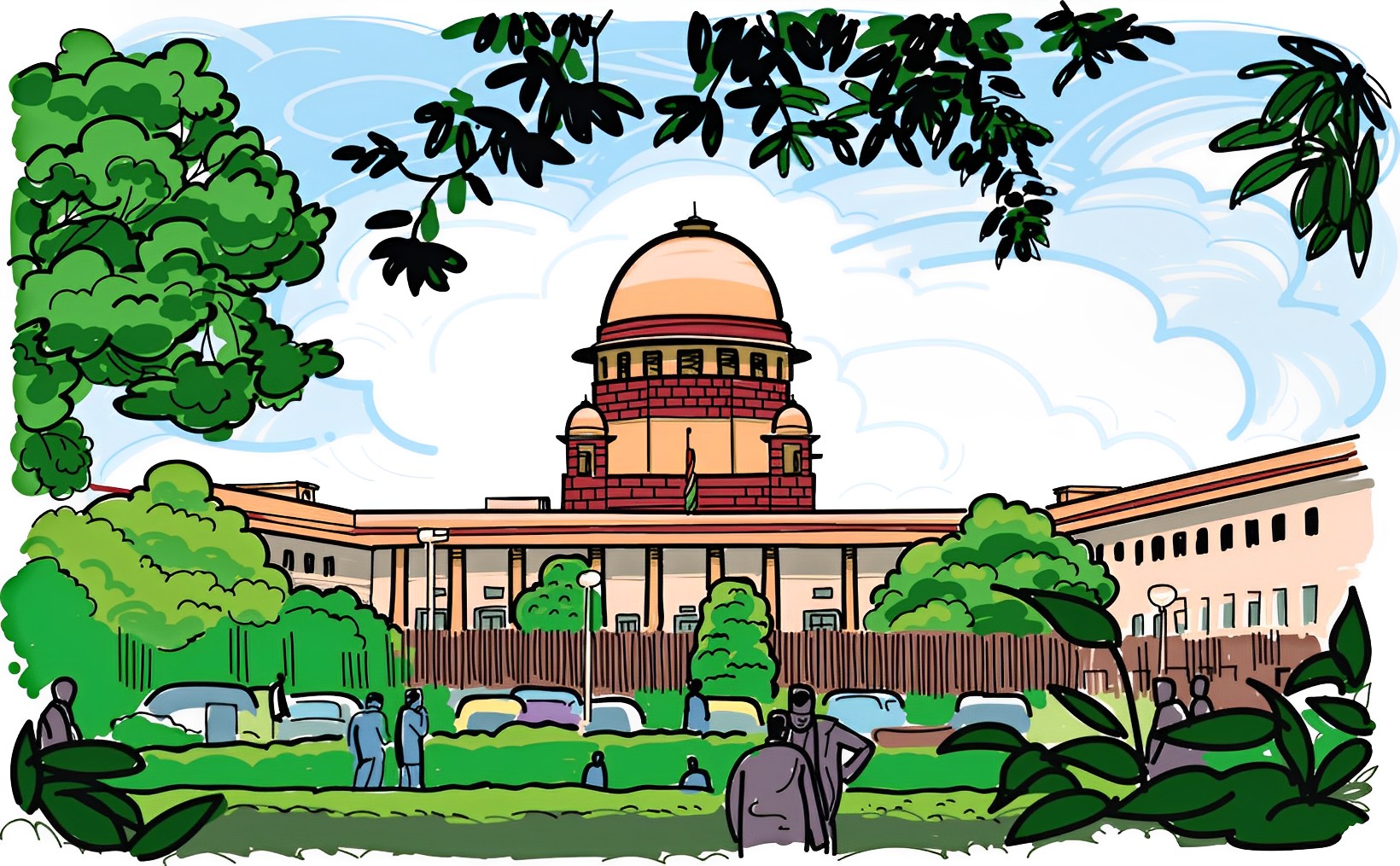
This is entirely welcome. Language articulates consciousness, and changing words is crucial to changing thoughts. The law lives through language. Words used in court have material power over our lives. Terms like housewife, chaste woman, or mistress are not neutral descriptors, they carry a payload of social judgment. They paint a picture of the male as the provider, and the ‘good’ female as dependent and docile. They question sexual freedom of women and sexual minorities. These attributed roles are the assumptions of a sexist world where men have traditionally had assets and income, and women provide sexual and domestic services. Our courts have often displayed blatantly sexist logic in judgments telling rapists to get rakhis tied by their victims or to marry them, matrimonial jurisprudence has made much of norms like mangalsutra and sindoor, or the right conduct with in-laws. Sexist stereotypes also often sway matters of separation and custody. In cases of sexual violence or abuse, women’s rights often recede into the background, and the focus is on their imagined ‘honour’. The victim’s behaviour is put on trial for how closely they live up to the ‘chaste’ norm. It’s telling that a sexual crime is cast as ‘offending the modesty of a woman’ rather than an infringement of her bodily autonomy.
This handbook might make judges and lawyers reflect on their own sympathies and instincts. It might give them pause, see things from a better angle. And that would mean setting things right for roughly half of India.
Date:18-08-23
Licence To Skill
GOI’s scheme for craftspeople is a good idea but its success critically depends on finding markets
TOI Editorials
A day after Modi in his I-Day speech said GOI will begin a scheme to aid people working in areas based on traditional skills, PM Vishwakarma was unveiled. A central sector scheme, it will offer aid of ₹13,000 crore over five years in the form of concessional loans, beneficiaries will mostly be OBCs. Craftspeople with the relevant documents will be eligible for a loan of up to Rs 3 lakh. Included in scheme design are plans to upgrade skills and integrate them with domestic and global value chains.
GOI’s statement said the scheme aims to nurture family-based practices of traditional skills. Since the skilling process happens within a closed environment, the primary challenge here is access to markets. Traditional skills globally struggle to compete on costs with modern alternatives. Some examples of traditional craftspeople cited by GOI such as toy makers and fishing net makers cannot compete on costs with factory-made alternatives. Therefore, for the investment to show results from an economic standpoint the scheme’s goal of linking them with marketing value chains will be critical. Fiscal outlays also reflect political choices and it’s no surprise that OBCs will be the principal beneficiaries.
PM Vishwakarma’s approach of soft loans will undoubtedly be of use to many engaged in traditional occupations. India’s economic transformation however requires skilling in modern jobs. Jobs in these sectors are also in sync with the aspirations of many young people in families engaged in traditional occupations. Given that, Vishwakarma is not what India needs to build up a workforce for a modern economy. That said, it’s important to preserve traditional skills as they represent an intangible cultural legacy of India. In this respect, India will do well to study the manner Japan has used both fiscal resources and legislation to preserve traditional skills while journeying to a developed country status. Vishwakarma will be of help to traditional craftspeople but its long-term impact will crucially depend on creating a market where they don’t compete with alternatives on costs.
Ensure More Bang For the CSR Buck
ET Editorials

But here’s the thing — despite the increased flow of funds, CSR impact has been limited. The requirement that businesses use CSR funds in their area of operation results in concentrating spending on education and health. Schools provide for a straightforward avenue to undertake CSR. Similarly with health, where spending includes initiatives related to dealing with hunger, malnutrition, drinking waterand sanitation. The pandemic also pushed up health-spend. Despite the major jump in environmentrelated spend, in absolute terms, it remains relatively small. And, for perspective, this kitty includes animal welfare, tree plantation and resource conservation.
For CSR spending to be leveraged and have impact, there must be a greater alignment between spending plans of individual businesses and national priorities in the sector. Using CSR funds for capital and operational expenditure will improve impact. CSR spends are marked by regional imbalance — concentrated in Maharashtra, Karnataka, Gujarat, Tamil Nadu and Uttar Pradesh, while northeast states account for less than 1%. Time to revisit how CSR funds are utilised to maximise impact.
Fighting stereotypes
Court guidelines on gender typecasting can be a catalyst for change.
Editorial
In the quest for equal rights for all, the Supreme Court of India has taken an important step by releasing guidelines to take on harmful gender stereotypes that perpetuate inequalities. Laying down a set of dos and don’ts for judicial decision-making and writing, the Handbook on Combating Gender Stereotypes helps judges identify language that promotes archaic and “incorrect ideas”, about women in particular, and offers alternative words and phrases. Instead of “affair”, it will be de rigueur to say a “relationship outside of marriage”; similarly, for “adulteress”, the preferred usage is a “woman who has engaged in sexual relations outside of marriage”. A host of derogatory and seemingly mild adjectives have been dropped too while referring to women. For instance, it is no longer “chaste” woman, “dutiful” wife, “housewife”; a plain “woman”, “wife” and “homemaker” will do. Men have not been forgotten either, with the Court striking down words such as “effeminate” (when used pejoratively), and “faggot”, with the directive, “accurately describe the individual’s sexual orientation (e.g. homosexual or bisexual)”. Pointing out that stereotypes — “a set idea that people have about what someone or something is like, especially an idea that is wrong” — leads to exclusion and discrimination, it identifies common presumptions about the way sexual harassment, assault, rape and other violent crimes are viewed, skewed against women.
One of the stereotypes the Court shatters is women who do not wear traditional clothes and smoke or drink are asking for trouble, and drives home the important point of consent. It also firmly asserts that women who are sexually assaulted may not be able to immediately report the traumatic incident. Courts should take social realities and other challenges facing women seriously, it says. It is wrong, the Court adds, to assume women are “overly emotional, illogical, and cannot take decisions”. It is also a stereotypical presumption that all women want to have children, says the handbook, and points out, “deciding to become a parent is an individual choice”. These possibilities, to be able to choose what to do in life, are still frustratingly out of reach for most of India’s women. In a largely patriarchal society, girls are often forced to pick marriage as a way out to avoid social stigma, and not education and a career. Even if things are changing, the pace is slow. To achieve gender equality, fundamental changes need to be made to shun all stereotypes. That women are more nurturing and better suited to care for others, and should do all household chores are simply wrong notions. The handbook may be a guide for judges and lawyers, but it could also be a catalyst for change right down to the societal level.
दंड को न्याय कहने से क्या वाकई न्याय मिलेगा
संपादकीय
अपराध-न्याय प्रणाली की मशहूर अवधारणा है- ‘नेचर ऑफ क्राइम शोज़ दी पैथोलॉजी ऑफ सोसायटी’ ‘अपराध की प्रकृति से समाज के मूल रोगों का पता चलता है।’ वही आईपीसी, वही सीआरपीसी और वही साक्ष्य कानून, लेकिन केरल में सजा की दर 85.6% है जबकि बिहार में 6.5% (एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार ) । समस्या कानून में इंडिया की जगह भारत या दंड को न्याय का नाम देने से हल नहीं होगी। हां, समय के साथ वैयक्तिक स्वातंत्र्य के पैरामीटर्स विस्तृत होते हैं। लैंगिक समानता, शारीरिक संबंधों को लेकर नई अवधारणाओं के परिप्रेक्ष्य में कुछ नए कानून लाना या पुराने हटाना समीचीन हैं और कोर्स के आदेश का अनुपालन भी । इसमें कोई दो राय नहीं कि 160 साल पहले सामाजिक-नैतिक मूल्य अलग थे और ऐसे में नागरिक स्वतंत्रता के बरअक्स राज्य की शक्ति ज्यादा प्रबल थी लेकिन प्रजातंत्र के 70 वर्षों में इसका दर्शनशास्त्र बदला है। अब आईपीसी, सीआरपीसी और साक्ष्य कानून का नाम भी क्रमशः भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम होंगे। गृहमंत्री ने सजा की दर में कमी पर चिंता जताते हुए इसे 90% करने को कहा और इसके लिए अनुसंधान में फॉरेंसिक साइंस की व्यापक मदद की व्यवस्था की बात भी की गई है। लेकिन यह सब इतना सहज नहीं, जितना दिखता है।
Date:18-08-23
डाटा प्रोटेक्शन की आड़ में सरकार की ताकतें और बढ़ीं
डेरेक ओ ब्रायन, ( लेखक सांसद और राज्यसभा में टीएमसी के नेता हैं, इस लेख की सहायक शोधकर्ता वर्णिका मिश्रा हैं। )
हमारे शिक्षक डेसमंड रेडन ने मुझे लोकतांत्रिक जिम्मेदारी के बारे में बताया था। पिछले हफ्ते मैंने राज्यसभा में कहा कि सरकार संसद के प्रति जवाबदेह है और संसद लोगों के प्रति। इसलिए जब संसद नहीं चलती तो इससे सरकार को जनता के प्रति जवाबदेही से पल्ला झाड़ने का मौका मिल जाता है। संसद का सुचारु रूप से नहीं चलना सरकार के हित में है।
तीन सप्ताह के मानसून सत्र में भाजपा ने 23 विधेयक पारित करवाए। इनमें से कई बुनियादी रूप से दोषपूर्ण हैं। इंडिया गठबंधन के अनेक वक्ताओं ने दिल्ली अध्यादेश पर बहस के दौरान पुरजोर तरीके से अपनी बात रखी। लेकिन दु:खद है कि मणिपुर पर संसद में नहीं बोलने की प्रधानमंत्री की हठधर्मिता के चलते इंडिया गठबंधन के दलों को तब वॉकआउट करने पर मजबूर होना पड़ा, जब डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन (डीपीडीपी) सहित अन्य विधेयकों पर चर्चा चल रही थी।
डीपीडीपी एक्ट 2023 संसदीय और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की प्रणालीगत अवमानना की बानगी है। डाटा की सुरक्षा के लिए कानून एक दशक से लम्बित था। इसमें गति लाने के लिए 2012 में एपी शाह द्वारा प्राइवेसी पर कमेटी बनाई गई। 2017 में केएस पुट्टास्वामी जजमेंट द्वारा निजता को बुनियादी अधिकार निर्दिष्ट किया गया। 2018 में जस्टिस बीएन श्रीकृष्णा की अगुवाई वाली कमेटी ने इस काम को आगे बढ़ाया। 2021 में जेपीसी- जिसका मैं सदस्य था- द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। एक साल बाद विधेयक को वापस ले लिया गया। इसके बाद नया विधेयक लोक-परामर्श के लिए रखा गया, जो कि डीपीडीपी बिल 2022 था। इस ‘लोक-परामर्श’ के तहत केवल अंग्रेजी में टिप्पणियां की जा सकती थीं और उन्हें निजी रखा गया था। सूचना प्रौद्योगिकी पर स्टैंडिंग कमेटी ने संसद द्वारा औपचारिक रूप से विधेयक को संदर्भित किए बिना ही उस पर चर्चा करने का निर्णय ले लिया। क्या आपको यहां दाल में कुछ काला नहीं नजर आता? कमेटी ने अपने सदस्यों से मशविरा लिए बिना ही रिपोर्ट बनाई और बैठक से एक रात पूर्व ही उसे उनसे साझा किया गया। वहीं केंद्र सरकार ने तमाम जांच-पड़ताल को ताक पर रखते हुए जुलाई 2023 में विधेयक के एक अज्ञात संस्करण को मंजूरी दे दी। जब मानसून सत्र शुरू हुआ तो लुटियंस की गलियों में इस विधेयक के कम से कम तीन संस्करण घूम रहे थे।
पारित किए गए अधिनियम में भी कुछ कम समस्याएं नहीं हैं। एक झटके में केंद्र सरकार ने स्वयं को इस बात के अतिशय अधिकार दे डाले कि क्या, किसके द्वारा और कहां पर कुछ कहा जा सकता है। अब सरकार के पास ये शक्तियां हैं कि वह लोकहित का हवाला देकर किसी भी सूचना तक पहुंच को अवरुद्ध कर सकती है। चूंकि ये लोकहित क्या हैं, इन्हें अच्छे-से परिभाषित नहीं किया गया है, इसलिए वह कंटेंट के प्रकाशन और उपभोग पर व्यापक प्रतिबंध लगा सकती है। इससे प्रेस की स्वतंत्रता बाधित होगी। डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड भी अब सीबीआई और ईडी जैसी उन संस्थाओं में शामिल होने जा रहा है, जिन्हें यों तो स्वायत्त होना चाहिए, पर जो सरकार के इशारों पर काम करती हैं।
तकनीकी रूप से तो यह एक स्वशासी डाटा प्रशासन प्राधिकरण है, लेकिन चूंकि इसमें पूरी तरह से केंद्र सरकार के सदस्य होंगे, इससे यह स्पष्ट होता है कि इसे रिमोट-कंट्रोल से चलाया जाएगा। केंद्र सरकार और उसकी एजेंसियां स्वयं को इस कानून की किसी भी बाध्यताओं से मुक्त रख सकती हैं, जिनमें डाटा की गैर-सहमति से प्रोसेसिंग को दंडित करना भी है। एक ऐसे समय में, जब इस बात की रिपोर्ट्स मौजूद हैं कि सरकार के आलोचकों के विरुद्ध राज्य की एजेंसियों द्वारा साक्ष्यों को प्लांट किया जाता है, यह सोचना विचलित कर सकता है कि इन नई ताकतों का और कितना दुरुपयोग किया जाएगा।
डीपीडीपी एक्ट 2023 पारदर्शिता के सबसे ताकतवर उपकरणों में से एक सूचना के अधिकार को भी अवरुद्ध करता है। इस अधिकार के तहत वे सूचनाएं भी प्राप्त की जाती हैं, जिन्हें सरकार संसद में प्रदान करने से इनकार कर देती है। लेकिन इस विधेयक ने सरकार के लोकसूचना अधिकारियों को आरटीआई आवेदनों को रद्द करने की अपरिमित शक्ति दे दी है। साथ ही, सार्वजनिक रूप से उपलब्ध निजी डाटा को इस कानून के अधिकार-क्षेत्र से मुक्त रखने का निर्णय भी दोषपूर्ण है। तकनीकी-विशेषज्ञ निखिल पाहवा ने मुझे बताया था कि ऐसा करके सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा उत्पन्न कर दिया है। इससे नागरिक थर्ड-पार्टीज़ द्वारा गैरजरूरी प्रोफाइलिंग और निगरानी से अपनी रक्षा नहीं कर सकेंगे।
Date:18-08-23
कश्मीर पर संसद का कानून, राष्ट्रपति का आदेश सर्वोच्च
विराग गुप्ता सुप्रीम कोर्ट के वकील, ( अनमास्किंग वीआईपी पुस्तक के लेखक )
सुप्रीम कोर्ट के जज और भावी चीफ जस्टिस बी. आर. गवई ने कहा है कि 70 फीसदी सरकारी मुकदमे आधारहीन होते हैं। इनकी वजह से जजों के वर्कलोड के साथ मुकदमों की संख्या बढ़ रही है। तस्वीर का दूसरा पहलू लग्जरी पीआईएल है, जहां सीनियर वकीलों की भारी-भरकम बहस से आम जनता से जुड़े मामले दरकिनार हो जाते हैं। राष्ट्रपति और संसद ने संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए अनुच्छेद-370 को निष्प्रभावी बनाते हुए जम्मू-कश्मीर को देश की मुख्य धारा से जोड़ दिया था। चार साल बाद उन याचिकाओं पर सनसनीखेज तरीके से बहस के 5 संवैधानिक पहलुओं को समझना जरूरी है :
1. भारतीय संविधान सर्वोपरि : कहा जा रहा है कि 370 रद्द नहीं हो सकता और इससे जम्मू-कश्मीर के भारत में विलय पर संशय हो गया है। जबकि हकीकत यह है कि अनुच्छेद-370 वाले चैप्टर 21 का शीर्षक ही अस्थायी और संक्रमणकालीन प्रावधान है। जो कानून अस्थायी हो, उसे अकादमिक तर्क के दम पर मूलभूत ढांचे का हिस्सा बताना बचकाना ही माना जाएगा। कश्मीर की तर्ज पर 500 से ज्यादा देशी रियासतों का प्रोफार्मा संधि पत्र के अनुसार भारत में विलय हुआ था। विलय के पहले जम्मू-कश्मीर की तर्ज पर मणिपुर समेत 62 रियासतों का पृथक संविधान था। लेकिन गणतंत्र बनने के बाद ये सभी राज्य और उनके कानून भारतीय संविधान में एकाकार हो गए। उसके 20 साल बाद इंदिरा सरकार ने राजाओं की पेंशन को खत्म कर दिया। इसलिए जम्मू-कश्मीर के भारत में एकीकरण पर हो रही अदालती बहस दुश्मन देशों के लिए ही मददगार होगी।
2. जनमत संग्रह की खतरनाक मांग : जम्मू-कश्मीर में संविधान सभा खत्म होने के बाद भारत की संसद और संविधान सर्वोच्च है। बेसिक स्ट्रक्चर सिद्धांत की आड़ में ब्रेग्जिट की तर्ज पर जनमत संग्रह जैसी बहस खतरनाक है। क्योंकि उसके बाद यह सवाल खड़ा होगा कि जनमत संग्रह पूरे भारत की बजाय सिर्फ जम्मू-कश्मीर में होना चाहिए। बहस का सिलसिला ऐसे ही बढ़ा तो 1947 में ब्रिटिश संसद से पारित कानून की वजह से भारत की आजादी को अधूरी मानने का दावा हो सकता है। मणिपुर में हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के फैसले के बाद बड़े पैमाने पर भड़की जातीय हिंसा को रोकना मुश्किल हो रहा है। इसलिए राष्ट्रीय सुरक्षा और अखण्डता से जुड़े मामलों की सुनवाई में जजों के साथ वकीलों को भी विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है।
3. कानूनी बारीकियों पर जोर : जम्मू-कश्मीर मामले पर संविधान पीठ की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने महिलाओं का सम्मान और गरिमा बढ़ाने के लिए हैंडबुक जारी करने की घोषणा की। दिलचस्प बात यह है कि किसी नियम के तहत ये गाइडलाइन्स नहीं बनीं, इसलिए इनके उल्लंघन पर दण्ड का भी विधान नहीं है। इसी तरीके से यू-ट्यूब आदि प्लेटफार्म से अदालतों की कार्यवाही का प्रसारण कानून विरुद्ध होने के साथ सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है। लेकिन कानूनी बारीकियों से परे जाकर सुप्रीम कोर्ट के इन बेहतरीन और प्रशंसनीय कदमों की लोग सराहना कर रहे हैं। इसलिए सरकारी फैसलों और संसद द्वारा पारित कानूनों के तकनीकी पहलुओं पर पूरा जोर देने की बजाय उनके व्यापक पहलुओं के अनुसार न्यायिक पुनरावलोकन होना चाहिए।
4. अदालतों की लक्ष्मण रेखा : सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें सरकार को 6 महीने के भीतर टॉर्ट कानून बनाने का आदेश दिया था। पश्चिमी देशों की तर्ज पर भारत में ऐसा कानून लागू हो जाए तो जनता को सरकारी विभागों से हर्जाना-क्षतिपूर्ति लेने का अधिकार मिल जाएगा। दूसरी तरफ सेम सेक्स मैरिज, मेरिटल रेप जैसे मामले संसद के अधिकार क्षेत्र में आने के बावजूद, उन पर अदालतों के माध्यम से कानून बनाने की अनुचित पहल हो रही है।
5. बहुमूल्य न्यायिक समय : देश की सर्वोच्च अदालत संवैधानिक संक्रमण के दौर से गुजर रही है। एक तरफ 5 करोड़ मुकदमों से पीड़ित लोगों की आंकाक्षाएं हैं। दूसरी तरफ अनेक लोग अदालत की आड़ में सियासत का खेल कर रहे हैं। संसद के कामकाज का उपयोगिता के आधार पर ऑडिट होता है। उसी तरीके से अदालतों की सुनवाई और फैसलों का निष्पक्ष मूल्यांकन समय की जरूरत है। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट में हर पक्ष के वकील को 30 मिनट, ऑस्ट्रेलिया में 45 मिनट और कनाडा में एक घंटे बहस की इजाजत होती है। बांग्लादेश में भी हर केस में वकीलों की बहस का समय तय है। पर भारत में लम्बी और उबाऊ बहसों से अदालती गरिमा के हनन के साथ गरीब जनता के मामलों की अनदेखी भी हो रही है।
कौशल को प्रोत्साहन
संपादकीय
असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले हुनरमंद लोगों को प्रोत्साहन की जरूरत लंबे समय से रेखांकित की जाती रही है। ऐसे लोग जो पारंपरिक पेशों से जुड़े हैं, हाथ का काम करते और भारतीय शिल्प को संरक्षित रखने में योगदान देते हैं, उनकी उपेक्षा और बदहाली को लेकर अक्सर लिखा-कहा जाता है। अब केंद्र ने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत ऐसे लोगों को वित्तीय मदद पहुंचाने, पहचान प्रतिष्ठित करने और उनके हुनर को बाजार में जगह दिलाने की पहल की है। इस योजना के तहत पांच फीसद ब्याज पर एक लाख और फिर अगले चरण में अधिक धन उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। इस योजना के तहत अगले पांच वर्षों में तीस लाख पारंपरिक कामगार परिवारों को लाभ मिलने का दावा है। इसमें तेरह हजार करोड़ रुपए का खर्च आएगा। निस्संदेह इस योजना से ऐसे लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा, जो मिट्टी के बरतन बनाने, चटाई बुनने, लुहारगीरी, सुनारगीरी आदि हस्तशिल्प के पारंपरिक पेशों से जुड़े हैं। ऐसे लोग प्राय: पैसे की कमी के चलते अपने पेशे को बड़ा व्यावसायिक मंच नहीं बना पाते। अपने उत्पाद को बड़े बाजार तक नहीं पहुंचा पाते। इस लिहाज से यह योजना काफी मददगार साबित हो सकती है, बशर्ते इसे संजीदगी से लागू किया जाए।
हालांकि यह पहली बार नहीं है, जब ऐसे पारंपरिक हस्तकौशल से जुड़े कामगारों को प्रोत्साहित करने के लिए कोई योजना चलाई जा रही है। पहले भी अलग-अलग प्रांतों के हस्तशिल्प को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार में जगह दिलाने के मकसद से योजनाएं चलाई जाती रही हैं। अनेक स्वयंसेवी संगठन और सरकारी केंद्र इस दिशा में लगातार प्रयासरत देखे जाते हैं। जगह-जगह विशेष हाट, बाजार और विक्रय केंद्र बना कर हस्तशिल्प को मंच देने की कोशिश की जाती रही है। मगर प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना उन सबसे इस मायने में अलग कही जा सकती है कि इसमें हस्तशिल्पियों को सीधे वित्तीय मदद उपलब्ध हो सकेगी। इससे उन्हें अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने, उन्नत बनाने की दिशा में नए ढंग से सोचने, आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल करने का अवसर मिलेगा। बहुत सारे ऐसे कामगार गुरु-शिष्य परंपरा के तहत दूर-दराज के इलाकों में हस्तशिल्प सीखते हैं। उन्होंने किसी प्रकार की व्यवस्थित शिक्षा नहीं ली है। स्थानीय जरूरतों को ध्यान में रखते हुए वे छोटी-मोटी चीजें बनाते और उन्हें बेच कर किसी तरह अपना गुजारा चलाते हैं। विश्वकर्मा योजना से उनका आत्मविश्वास बढ़ सकता है कि वे भी सुशिक्षित उद्यमियों की तरह अपने कौशल को व्यावसायिक रूप दे सकते हैं।
केंद्र सरकार का जोर कौशल विकास पर है। दुनिया भर में माना जा रहा है कि वही अर्थव्यवस्थाएं मजबूत होंगी, जिनमें कौशल विकास पर जोर दिया जाता है। इस दृष्टि से भी यह योजना स्थानीय स्तर पर कौशल विकास की दिशा में एक बेहतर कदम कही जा सकती है। मगर जिस तरह दुनिया भर में अर्थव्यवस्थाएं भारी मशीनों और थोक उत्पादन पर निर्भर होती गई हैं, उसमें स्थानीय कौशल को बड़े बाजार में कहां तक जगह मिल पाएगी, कहना मुश्किल है।हस्तशिल्प को प्रोत्साहन देने वाले पहले के प्रयासों का अनुभव यही है कि आज भी बहुत सारे लोग अपने पारंपरिक पेशे छोड़ कर किसी दूसरे रोजगार, मजदूरी या नौकरी की तलाश में देखे जाते हैं। हालांकि विश्वकर्मा योजना में ऐसे लोगों को बाजार उपलब्ध कराने की बात भी कही गई है, मगर जब तक इस पर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया जाएगा, तब तक इसके अपने लक्ष्य तक पहुंचने का दावा नहीं किया सकता।
Date:18-08-23
भाषा न्याय
संपादकीय
एक सभ्य समाज, संस्था और व्यक्ति की पहचान इससे भी होती है कि वह सामान्य व्यवहार में किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है। खासकर महिलाओं के बारे में उपयोग किए जाने वाले शब्दों, वाक्यों से उस समाज की मानसिकता का भी पता चलता है। इस मामले में भारत के अधिकतर समाजों में स्त्री के प्रति बहुत सारे असम्मानजनक शब्द चलन में हैं। वही शब्द धीरे-धीरे प्रशासनिक और अदालती कामकाज में भी घुसपैठ कर गए हैं। सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश ने ऐसे शब्दों की पहचान की और उन्हें अदालती भाषा से बाहर करने का फैसला किया। एक टीम बना कर ऐसे शब्दों की पहचान की गई, जो महिलाओं के लिए प्राय: समाज में रूढ़ और अपमानसूचक हैं।उन शब्दों की जगह प्रयुक्त हो सकने वाले शब्दों और वाक्यों के विकल्प भी तलाशे गए और फिर ‘हैंडबुक आन कांबैटिंग जेंडर स्टीरियोटाइप’ शीर्षक से तीस पन्नों की एक पुस्तिका प्रकाशित की गई। इसमें उन शब्दों की सूची दी गई है, जो अदालती कामकाज में प्रयोग होते रहे हैं। वे शब्द अदालती फैसलों तक में प्रयुक्त हुए हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि उन रूढ़ हो चुके शब्दों के बजाय उनके सम्मानजनक विकल्पों का उपयोग किया जाए। यह पुस्तिका वकीलों और न्यायाधीशों दोनों के लिए है।
यह पहली बार है जब किसी प्रधान न्यायाधीश का ध्यान अदालती भाषा में घुसपैठ कर चुके स्त्रियों के प्रति इस्तेमाल होने वाले रूढ़ और अपमानसूचक शब्दों की तरफ गया। इस साल महिला दिवस पर उन्होंने इसे लेकर न सिर्फ अफसोस जाहिर किया, बल्कि उन शब्दों को हटाने का उपक्रम भी किया। प्रधान न्यायाधीश ने पुस्तिका जारी करते हुए कहा भी कि महिलाएं पुरुष के अधीन नहीं, बल्कि संविधान में उन्हें बराबरी का हक है। उनके प्रति किसी भी ऐसे शब्द का उपयोग नहीं होना चाहिए, जिससे उनका सम्मान आहत होता हो। इस पहल से निस्संदेह अदालत की भाषा में महिलाओं की सम्मानजनक जगह बनेगी। यह उन तमाम संस्थाओं के लिए भी नजीर बनेगी, जो बिना सोचे-समझे अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। इसका असर बौद्धिक समाज और फिर उसके नीचे समाज पर भी दिखना शुरू होगा। दरअसल, शिक्षा का स्तर ऊंचा उठने के बावजूद महिलाओं के प्रति हमारे समाज का नजरिया संकीर्ण है। उन्हें अपमानित करने की मंशा से लोक और शास्त्रीय भाषा में भी बहुत सारे ऐसे शब्द गढ़ लिए गए हैं, जिन्हें गाली कहा जा सकता है।मगर इनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे शब्द गढे गए हैं, जो अपमानजनक हैं और सामान्य कामकाज की भाषा में रूढ़ हो चुके हैं। मसलन, बिन व्याही मां। सर्वोच्च न्यायालय ने इसकी जगह केवल मां शब्द का प्रयोग करने का सुझाव दिया है। ऐसे शब्दों की लंबी सूची है।
जब शीर्ष संस्थाएं भाषा को लेकर सावधानी बरतना शुरू करती हैं, तो उसका प्रभाव नीचे तक पहुंचता है और लोग सामान्य व्यवहार में भी उसे उतारना शुरू कर देते हैं। उम्मीद बनती है कि लोग अब महिलाओं के प्रति इन रूढ़ शब्दों से परहेज करेंगे। हमारे समाज में महिलाओं के प्रति लैंगिक भेदभाव के अनेक स्तर हैं, उनमें भाषा भी एक है। संविधान में महिलाओं और पुरुषों के बीच के भेद को समाप्त करने के लिए समय-समय पर कई प्रावधान किए गए, मगर उनके लिए इस्तेमाल की जाने वाली भाषा को परिष्कृत करने का प्रयास नहीं किया गया था। अब वह सुनिश्चित हो सका है। इस तरह सर्वोच्च न्यायालय की ताजा पहल महिलाओं के प्रति समुचित भाषा न्याय है।
शब्दों की पहरेदारी
संपादकीय
सबसे बड़ी अदालत ने लैंगिक रूढ़िवादिता से निपटने की दिशा में एक बड़ी पहल करते हुए वेश्या, बदचलन औरत, देह व्यापार जैसे शब्दों के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है। इसकी जगह भारतीय न्यायपालिका के प्रयोग के लिए एक नई शब्दावली तय की है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चन्द्रचूड़ ने कहा की नई शब्दावली की पुस्तिका तैयार करने का मकसद यह बताना है कि अनजाने में कैसी व किस तरह की रूढ़ियां जारी रहती हैं। आगे से दलीलों, आदेशों व फैसलों में अब इन्हीं शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। वेश्या या हुकर को यौनकर्मी, रखैल / कीप को वह महिला जिसके साथ किसी पुरुष ने शादी के बाद प्रेम संबंध या यौन संबंध बनाए हों, का उपयोग किया जाए। छेड़छाड़ को सड़क पर यौन उत्पीड़न व गृहिणी की जगह गृहस्वामिनी शब्द होगा । नाजायज की बजाय गैर-विवाहित संबंधों से पैदा बच्चा या ऐसा बच्चा जिसके माता-पिता विवाहित नहीं हैं, होगा। बिन ब्याही मां को मां लिखा / बोला जाएगा। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा फैसलों में मैने महिलाओं के लिए चोर, रखैल आदि शब्दों का प्रयोग देखा, जबकि इनकी जगह बेहतर व सम्मानजनक शब्द इस्तेमाल किए जा सकते थे। कलकत्ता उच्च न्यायालय की जस्टिस मौसमी भट्टाचार्य की समिति ने तकरीबन 40 शब्दों व वाक्यांशों का जिक्र किया है, जिनसे महिलाओं के प्रति रूढ़िवादी विचार झलकता था। न्यायपालिका में इन नये शब्दों के प्रयोग की शुरुआत निहायत ही संवेदनशील सोच का नतीजा है। अच्छी पत्नी व बुरी पत्नी जैसे कोष्ठकों को भले ही तोड़ने में वक्त लगे परंतु खुलेआम इनके संबोधन में संकोच तो आ ही सकता है। अपने पारंपरिक समाज में स्त्री के चरित्र पर छींटाकशी करने वाली भाषा ही नहीं प्रचलित है, बल्कि उन्हें गाली-गलौज के तौर पर भी खूब इस्तेमाल किया जाता है। अपने यहां स्त्री के गोपन अंगों को लेकर गाली-गलौच ही नहीं प्रचलित है बल्कि उन तमाम शब्दों का भी खुल कर प्रयोग किया जाता है, जिनकी आवश्यकता नहीं होती। हालांकि इन शब्दों से स्त्री की दशा तो नहीं सुधरेगी मगर न्यायिक प्रक्रिया के दरम्यान उसकी गरिमा सुरक्षित रह सकेगी। उम्मीद की जानी चाहिए अदालत से शुरू होने वाला यह बदलाव तेजी से मीडिया माध्यमों द्वारा प्रयोग में आते-आते आम जनता की बोलचाल में भी परिलक्षित होता जाएगा।
Date:18-08-23
कितना सुरक्षित है निजी डेटा
रजनीश कपूर
आए दिन हमें डिजिटल धोखाधड़ी के मामलों के बारे में पता चलता है। कैसे कुछ शातिर लोगों का गैंग योजनाबद्ध तरीके से भोले-भाले लोगों को ठगने की मंशा से उन्हें अपना शिकार बनाता है। उनकी मेहनत की कमाई को कुछ ही पल में फुर्र कर देता है। उसके बाद ऐसे फ्रॉड का शिकार व्यक्ति अपनी शिकायत लेकर दर- दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो जाता है। परंतु सरकार ने इस फ्रॉड को रोकने और जरूरी निजी जानकारी की सुरक्षा की दृष्टि से ‘डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल’ संसद में पेश किया है, जो अब कानून बन गया है। हाल में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद में डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल, 2023 पेश किया। इस विधेयक के तहत नागरिकों के व्यक्तिगत डाटा की सुरक्षा के अधिकार व्यवस्था करता है। सवाल है कि यदि यह बिल नागरिकों की निजी जानकारी सुरक्षा की दृष्टि से लाया गया है, तो इसका इतना विरोध क्यों? क्या विरोध केवल विरोध के लिए ही है, या इसका कोई वाजिब कारण भी है?
गौरतलब है कि नागरिकों के पर्सनल डेटा की सुरक्षा को लेकर देश भर में पहले से ही काफी बहस चल रही है। परंतु इस बहस को गति देने की पहल देश की सर्वोच्च ने अदालत ने 24 अगस्त, 2017 को अपने फैसले से की। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, ‘निजता का अधिकार लोगों का मूलभूत अधिकार है।’ नौ जजों वाली संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार बताया है। पीठ ने कहा, निजता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत दिए गए जीने के अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हिस्सा है। यहां यह समझना
जरूरी है कि इस बिल के तहत हमारे किस डेटा की सुरक्षा की बात हो रही है। ‘डिजिटल पर्सनल डेटा’ वो होता है जो आप किसी भी ई-कॉमर्स की वेबसाइट पर प्रदान करते हैं। यह डेटा वो होता है जिससे आपकी और आप जैसे करोड़ों उपभोक्ताओं की विभिन्न ई-कॉमर्स वेबसाइट पर पहचान बनती है। उदाहरण के लिए आप किसी वेबसाइट से रोजमर्रा का सामान मंगवाते हैं, तो आपका ‘यूजर नेम’, ‘पासवर्ड’, आपकी जन्मतिथि, आपके घर या ऑफिस का पता, आपका मोबाइल नंबर, पैन नंबर, आधार नम्बर आदि । इसके साथ ही आपके द्वारा मंगाए जाने वाले सामान या भोजन आदि भी आपके प्रोफाइल में अंकित हो जाते हैं। आपकी खरीदारी का मूल्य, सोशल मीडिया साइट्स पर आप किस से क्या बात कर रहे हैं, आपकी लोकेशन क्या है, आप किस लोकेशन पर ज्यादा समय बिताते हैं- ऐसी जानकारियों को ‘डिजिटल पर्सनल डेटा’ कहते हैं।
इस डेटा का दुरुपयोग बहुत आसान है। सोशल मीडिया वेबसाइट्स व ई-कॉमर्स वेबसाइट्स या मोबाइल ऐप्स आपके इस डेटा को बिना आपकी जानकारी के, अन्य ” कंपनियों को बेच देते हैं। इस ‘डिजिटल पर्सनल डेटा’ के आधार पर विभिन्न वेबसाइट्स आपके कंप्यूटर या फोन पर आपको तरह-तरह के विज्ञापन आदि दिखाते हैं, और ग्राहकों को आकर्षित करते हैं। जाहिर सी बात है कि इन विज्ञापनों से इन वेबसाइट्स को मुनाफा होता है। अमेरिका में 2016 राष्ट्रपति चुनाव में फेसबुक पर मतदाताओं को प्रभावित करने के आरोप में हजारों करोड़ का जुर्माना लगाया गया था।
ऐसा नहीं है कि निजता के बचाव की मंशा से यह पहली बार हो रहा है। इससे पहले साल 2012 में सुप्रीम कोर्ट के जज न्यायमूर्ति एपी शाह की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी जिसने प्राइवेसी कानून बनाने की सिफारिश भी की थी। लेकिन मामला ठंडे बस्ते में पड़ा रहा। उसके बाद से अब तक कई बार इस मामले पर कमेटी बनीं और विधेयक भी प्रस्तावित किए गए। परंतु ‘डिजिटल पर्सनल ‘डेटा’ की उचित सुरक्षा न हो पाने के कारण विपक्ष और जानकारों ने इसे कानून बनने नहीं दिया। विपक्ष ने आरोप लगाया था कि यह बिल निजी डेटा की सुरक्षा के नाम पर, सरकार ने अपने पास मनमानी शक्तियां इकट्ठा कर ली हैं। इसके बाद इस विधेयक को संसद की संयुक्त समिति के पास भेजा गया। उसने अपनी रिपोर्ट में कई संशोधन और सुझाव दिए । सरकार ने इन सुझावों व संशोधनों के न मानकर अगस्त, 2022 में विधेयक को वापिस ले लिया। मॉनसून सत्र में इसे दोबारा पेश किया। परंतु अबकी भी सरकार ने यह नहीं बताया पिछले के मुकाबले इस विधेयक में क्या बदलाव किए हैं।
उल्लेखनीय है कि इस विधेयक में ‘जैसा कि निर्धारित किया जाएगा’ वाक्य को 26 बार प्रयोग किया गया है। विपक्ष के अनुसार इसका सीधा मतलब यह है कि काफी कुछ अंधेरे में है, और नियमों को बंद दरवाज़े से लाया जाएगा। उसका आरोप है कि यह बिल निजता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है, और इससे सूचना का अधिकार (आरटीआई) कानून भी कमजोर होगा। जबकि सत्ता पक्ष ने जोर दिया कि बिल सिर्फ व्यक्तिगत डेटा को सुरक्षा देगा और आरटीआई पर इससे कोई असर नहीं पड़ेगा।
रूढ़िवादिता पर चोट
संपादकीय
देश की सर्वोच्च अदालत ने लैंगिक आधार पर दशकों से चली आ रही रूढ़िवादिता पर अंकुश लगाने के लिए जो पुस्तिका जारी की है, वह सुखद और स्वागतयोग्य है। प्रधान न्यायाधीश धनंजय वाई चंद्रचूड़ की यह उत्साहजनक पहल देश में समग्र सामाजिक परिवेश को बदलने में भी अपना योगदान देगी। महिलाओं और यौन अपराधों के संदर्भ में अदालतों में आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले कुछ वाक्यांशों को सूचीबद्ध किया गया है और उनकी जगह दूसरे सभ्य शब्द प्रस्तावित किए गए हैं। ऐसे लगभग 43 शब्दों को रेखांकित किया गया है, जिनके इस्तेमाल से अब अदालतों को बचना होगा। न्याय के मंदिर में महिलाओं को पूरा सम्मान और समता का लाभ देने के लिए अनुचित शब्दों का इस्तेमाल रोकना हमेशा से जरूरी रहा है। याचिकाओं की भाषा के साथ-साथ आदलती आदेशों में भी सही शब्दों का जब इस्तेमाल होगा, तो उससे महिलाओं की गरिमा की रक्षा होगी। इसमें कोई शक नहीं कि महिला पीड़ितों, अभियुक्तों और गवाहों को कमजोर करने के लिए अक्सर ऐसे शब्दों या सवालों का इस्तेमाल होता है, जिनसे वास्तव में अन्याय का ही मार्ग प्रशस्त होता है।
महिलाओं के बारे में समझ को सम्मानजनक बनाने का प्रयास करती यह पुस्तिका वस्तुत: एक न्यायप्रिय समाज के निर्माण में सहायक होगी। जब न्याय के मंदिर में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल रुकेगा, तब बाकी समाज में भी इजहार का नया ढंग आएगा। खासतौर पर न्यायाधीशों को सजग रहना होगा, ताकि ऐसी कारगर पुस्तिका का ज्ञान कागजों में ही कैद होकर न रह जाए। वास्तव में, यह काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था। हम जानते हैं कि न्याय के मंदिर में भी एक आम गरीब महिला के साथ भाषा और व्यवहार के स्तर पर प्रतिकूलता होती है। यह बात किसी से छिपी नहीं है कि पुलिस के स्तर पर भी बहुत सारे अपशब्द प्रचलित हैं। क्या अदालतें पुलिस की भाषा में भी सुधार लाने के लिए प्रयास कर सकती हैं? क्या इसी पुस्तिका को रक्षा-सुरक्षा संबंधी महकमों में भी लागू किया जा सकता है? बहरहाल, प्रधान न्यायाधीश ने अपना काम कर दिया है, अब संबंधित मंत्रालयों को भी भाषा और सोच सुधार के लिए युद्ध स्तर पर प्रयत्न करने चाहिए।
तमाम कानूनों, नियम-कायदों और प्रक्रियाओं को महिलाओं के अनुकूल बनाने की ओर इस देश को अवश्य बढ़ना चाहिए। लैंगिक असमानता को दूर करना देश के तेज आर्थिक विकास के लिए भी जरूरी है। हैंडबुक ऑन कॉम्बैटिंग जेंडर नामक यह पुस्तिका देश के आम लोगों के लिए भी पठनीय और अनुकरणीय होनी चाहिए। ऐसे सुधार केवल न्यायपालिका के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए स्वीकार्य होने चाहिए। देश में मातृशक्ति के प्रति संवेदनशीलता की बड़ी जरूरत है। आमतौर पर महिलाओं के लिए इस्तेमाल होने वाले फूहड़, वेश्या, पतित महिला, भारतीय महिला, पश्चिमी महिला, पवित्र महिला जैसे शब्दों की आखिर क्यों जरूरत है? प्रधान न्यायाधीश ने पुस्तक की प्रस्तावना में साफ लिखा है कि इसका उद्देश्य महिलाओं के बारे में रूढ़िवादिता को पहचानने, समझने और उसका मुकाबला करने में न्यायाधीशों व विधि समुदाय की सहायता करना है। हालांकि, इस पुस्तिका का पालन अनिवार्य नहीं है, पर इसकी जरूरत से भला कौन इनकार कर सकता है? इस पुस्तिका की रोशनी में आगे बढ़ने में ही नारी शक्ति का सम्मान और देशहित है।
Date:18-08-23
नाजुक पहाड़ों पर रहना सीखना होगा
कालाचांद सांई, ( निदेशक, डब्ल्यूआईएचजी, देहरादून )
हमारे पहाड़ों में बहुत नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र, जीवमंडल, जलमंडल, थलमंडल और वायुमंडल का सह-अस्तित्व है। अब यह बात किसी से छिपी नहीं है कि जलवायु परिवर्तन ग्लेशियरों, नदी प्रणाली, भू-आकृति विज्ञान, भूमि क्षरण, जैव-विविधता आदि पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। पहाड़ी नगरों में सामंजस्य पूर्ण सह-अस्तित्व या पारिस्थितिकी तंत्र की गड़बड़ी खतरे को बढ़ा देती है। इंसानी गतिविधियों या पर्यावरण में गिरावट के चलते बाहरी ताकतें आपदाओं और अचानक बाढ़ का मुख्य कारण बन जाती हैं।
पर्वतीय क्षेत्र में भूस्खलन के कई कारण हो सकते हैं। आम तौर पर पहाड़ी शहर ढलान, अस्थिरता या भू-स्खलन की संवेदनशीलता से जुड़े होते हैं, जो भौगोलिक कारकों द्वारा निर्देशित होते हैं। ढलान, ढाल, वक्रता, दिशा, ऊंचाई, लिथोलॉजी, संरचनाएं, चट्टान की ताकत, वन आवरण, निर्मित क्षेत्र, असंगठित और अर्द्ध-समेकित तलछट आदि मापदंडों के आधार पर हम एक भेद्यता मानचित्र तैयार कर सकते हैं। सर्वाधिक संवेदनशील, मध्यम संवेदनशील और सबसे कम संवेदनशील या जोखिम वाले क्षेत्रों को जान सकते हैं। इस क्षेत्र में टेक्टोनिक हलचल, नदी का प्रवाह और वृक्षों की कटाई भी पहाड़ी क्षेत्र को भूस्खलन के प्रति संवेदनशील बनाती है। इधर वनों की कटाई से भूस्खलन की आशंका बढ़ गई है। घरों के नीचे से जमीन खिसक रही है। भूमिगत जल के रिसने से पहाड़ी ढलानें कमजोर पड़ रही हैं, जिस पर गुरुत्वाकर्षण के चलते भूभाग नीचे की ओर खिसक जाता है। हालांकि, भूस्खलन मुख्य रूप से जलवायु कारक वर्षा के कारण होता है।
ध्यान देने की बात है कि वर्तमान जलवायु परिवर्तन परिदृश्य के चलते पिछले एक दशक में पहाड़ों में कम समय में ज्यादा वर्षा की आवृत्ति बढ़ गई है। कोई आश्चर्य नहीं कि प्राकृतिक कारणों की वजह से ही भूस्खलन की स्थिति बनती है। कोई एक कारण जिम्मेदार नहीं है। जलाशय की कमी, अनुचित जल निकासी प्रणाली, ढलान की कटाई, अवैज्ञानिक खनन, अवैध निर्माण, अत्यधिक चराई इत्यादि से भी भूस्खलन का संकट बढ़ता है। मोटे तौर पर इसके तीन कारण गिनाए जा सकते हैं- प्राकृतिक कारण, जलवायु-प्रेरित कारण और मानवजनित कारण।
पश्चिमी विक्षोभ एक निम्न दबाव प्रणाली है, जो भूमध्य सागर से पैदा होती है, मध्य एशिया और उत्तरी भारत में पूर्व की ओर बढ़ती है और अरब सागर से उत्पन्न होने वाले दक्षिण-पश्चिम भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून के चलते जम्मू-कश्मीर व पहाड़ों के कुछ हिस्सों में थोड़े समय के दौरान ही अत्यधिक वर्षा कराती है। यह अचानक भारी वर्षा हिमाचल, उत्तराखंड और आसपास के क्षेत्रों में होने वाले भूस्खलन व अचानक बाढ़ के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है।
ध्यान देने की बात है कि हिमालय क्षेत्र में यूरेशियन प्लेट के नीचे भारतीय प्लेट के अभिसरण ने भूगर्भीय चट्टानों को विकृत कर दिया है और जहां से ऊर्जा का निर्माण होता है, जो भूकंप के रूप में प्रकट होती है। ऐसे भूकंप से खासकर ढलान वाले क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर जमीन की सतह कमजोर पड़ जाती है। हमने गौर किया है, हर छोटे-बड़े भूकंप के चलते तुरंत भूस्खलन होता है या दरारें उभर आती हैं, उपसतह कमजोर हो जाती है और क्षेत्र में लिथो-संरचना ढीली हो जाती है।
समस्या बढ़ी है, तो जाहिर है कि सबसे बड़ा प्रश्न आज यह हो गया है कि समाधान क्या है? पहाड़ी नगर निर्माण नीतियों को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। पहाड़ी बस्तियों में उचित जल-निकासी व्यवस्था के साथ उपयुक्त नगर नियोजन को अपनाना होगा। अब हमें सुरक्षा और स्थिरता के साथ जलवायु-अनुकूलन और आपदा प्रतिरोधी समाज का निर्माण करना होगा। अब पहाड़ों पर लोगों को आपदाओं के साथ जीने के लिए शिक्षित-प्रशिक्षित करना होगा। सभी छोटे और बड़े शहरों की ‘हाई रिजॉल्यूशन मैपिंग’ और नई तकनीक का उपयोग करके भार-वहन क्षमता का सही आकलन करना होगा। मतलब अगर किसी पहाड़ या ढलान पर भार-वहन क्षमता कम है, तो वहां भवन निर्माण से बचना होगा। इसे भवन निर्माण संहिता का अनिवार्य हिस्सा बनाना होगा।
अब सिर्फ हिमालय ही नहीं, पूरे भारत में बढ़ती आबादी एक चिंताजनक मुद्दा है, इसलिए सबसे बड़ी चिंता जीवनशैली में बदलाव की है। ऐसा देखा जाता है कि जो शहर व्यापारिक केंद्र बन जाता है, वहां लोगों के बसने से उसका तेज विकास होता है। हमें अब संवेदनशील क्षेत्रों में व्यापारिक केंद्र बनाने से बचना होगा। ऐसी जगहों पर हल्के निर्माण को प्राथमिकता देनी होगी और इसके लिए विज्ञान-आधारित अच्छे वास्तु का सहारा लेना पड़ेगा। ऐसे स्थानों पर नगर निकायों को सख्ती बरतनी पड़ेगी। अभी कई व्यावहारिक कमियां हैं। अभी हम पहाड़ काटते हैं, पर उसके समाधान की ओर ध्यान नहीं देते हैं, जबकि यह अव्यावहारिक और अवैज्ञानिक है।
बचाव का कोई छोटा रास्ता नहीं है। हमें खुद को अधिक शिक्षित और जागरूक करना होगा। एक बार जब हम पारिस्थितिकी तंत्र से छेड़छाड़ करते हैं, तो उसे वापस उसी स्थिति में आने में बहुत लंबा समय लग सकता है, और इसमें लगने वाला समय ही अशांत क्षेत्र में भूमि खिसकने का खतरा पैदा करता है। यदि यह छेड़छाड़ व विकास बनाम विनाश का असंतुलन चलता रहा, तो इसकी भविष्य में बड़ी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहना होगा। कहा जा सकता है कि ऐसे में हिमालय का भविष्य बेहद असुरक्षित है। इसे प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक एक साथ सक्रिय हैं।
अब सर्वाधिक संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी बहुत जरूरी है। वर्षा गेज, पीजोमीटर, इनक्लिनोमीटर, एक्सटेन्सोमीटर, इनएसएआर की मदद लेकर चेतावनी तंत्र को मजबूत किया जा सकता है। निगरानी का सबसे अच्छा संभव तरीका है कि हिमालयी राज्यों की केंद्रीकृत परिषद का निर्माण करना होगा। इसमें अलग-अलग राज्यों के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण शामिल किए जाएं। इसमें मुख्य फोकस जमीन की सतह और उपसतह के तनाव के आकलन पर होना चाहिए। भारतीय हिमालयी क्षेत्र में आपदाओं को कम करने की दिशा में रणनीतियों के प्रभावी और कुशल निर्माण के लिए सभी प्रभावी सूचनाओं को सभी हिमालयी राज्यों द्वारा प्रसारित और साझा करने की जरूरत है।
