
17-07-2024 (Important News Clippings)
To Download Click Here.
 Date: 17-07-24
Date: 17-07-24
Her Choice? Hardly
Women are still not at the centre of abortion rights in India. Courts and doctors decide.
TOI Editorials
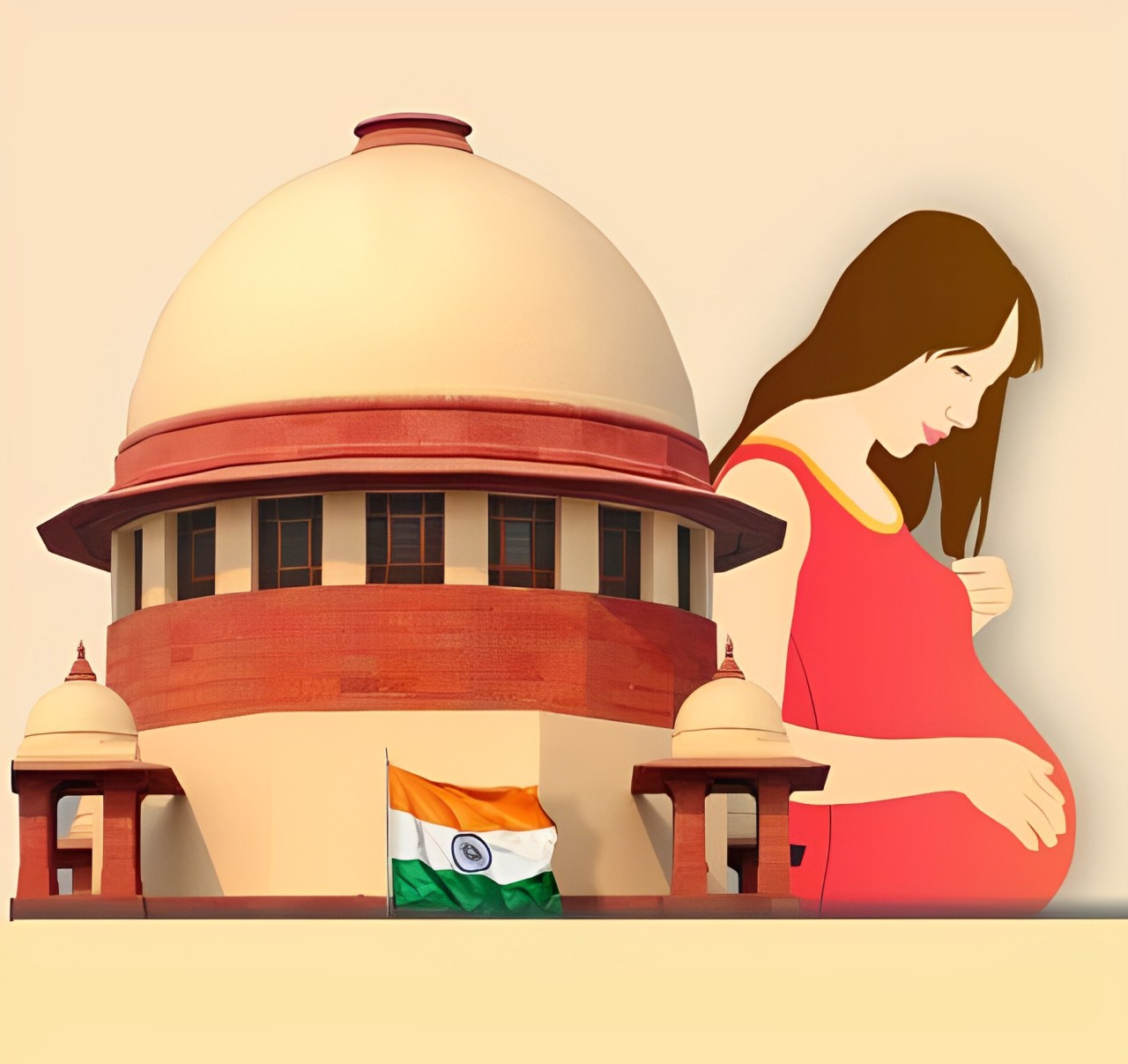
This is the state of law and paternalism. Too often, whether a case goes a petitioner’s way or not depends on how much pity her position evinces – be it on account of rape, abandonment, singlehood or foetal abnormality. The last reflects a troubling eugenic mindset. Overall, a woman has to overcome a formidable web of barriers to achieve her choice.
Where women’s rights are conditional, they can as well be denied as granted. An arbitrariness prevails. On the one hand, there is the landmark nine-judge SC Puttaswamy judgment. It said the right to make reproductive choices is deduced from a woman’s fundamental right to privacy, dignity and bodily integrity. On the other hand, there is the 1860 IPC provision criminalising abortion, which BNS hasn’t bothered to update. In 1971 the MTP Act carved out an exception to this, to enable medical practitioners to terminate pregnancies under certain conditions. But this is a very doctor centric framework. Half a century on, different doctors, then different courts, continue to use different benchmarks to permit or decline termination of pregnancy. In this high-stakes arbitration, a woman’s wishes end up being incidental.
Women end up at courts’ doors because the medical ecosystem fails them. Sometimes with moral policing, sometimes with delays, and sometimes with harsh insensitivity. Most women can’t go this route. That only 22% of abortions in the country can be considered safe, tells their tale. Now, there’s also the slippery import of an American style discourse of foetal rights, which has no cultural or legal roots in India. Instead, we need to double down on citizens’ bodily autonomy. Do more than lip service to women’s rights.
Pay Farmers Not To Farm… Paddy
Wean northwest India off from growing it.
ET Editorials
Paying farmers in Punjab and Haryana an explicit subsidy not to grow paddy, as suggested by an ICRIER policy brief released this month, makes ample sense. It’s an efficient alternative to MSP earmarked for grain, legislated increments of which have become the cause of farmer agitation in the region. The MSP programme itself has been called into question over farmers’ ability to sell crops at prices that will support farming paddy and other covered crops. To access the intended price support offered through MSP, the farmer has to go through the expenses of an entire harvest so that GoI can procure grain to be stored for food security. A subsidy not to farm paddy addresses waste in the grain storage mechanism, but, more importantly, it frees up government resources to offer support prices for a larger variety of crops that the country is deficient in.
Paying farmers not to farm may sound odd, till the ecological impact of farming is priced in. That includes irrigation, fertiliser and power costs, some of which GoI bears. In the case of paddy in Punjab and Haryana, these costs are considerable, making cultivation unviable without input subsidies alongside price supports. Then there’s the matter of ecological damage of unsustainable agriculture. All of these add up to the explicit subsidy the ICRIER paper is suggesting for weaning farmers in northwest India off growing paddy — which can be grown with less damage to the environment in rainfed parts of the country. A green revolution awaits pulses and edible oils that would benefit from both input subsidies and price support. It would also reduce India’s import dependence for these crops.
Other countries have found it expedient to pay farmers not to grow selective crops, instead of making them go through with the expense of doing so to claim support prices, and for governments to store such crops in warehouses where they rot or are eaten by rats. India can consider this agri intervention for nutritional security, sustainable farming and an evergreen revolution.
सरकार का बाजार में हस्तक्षेप कितना प्रभावी
संपादकीय
आम आदमी की रोजमर्रा की सबसे बड़ी जरूरत है तीन सब्जियां – आलू, प्याज और टमाटर । इनके अंग्रेजी नामों के प्रथम अक्षर को जोड़कर 2018 में एक लुभावनी योजना शुरू की गई, जिसका नाम था- ‘टॉप’। उद्देश्य था, इनके रखरखाव का समुचित प्रबंधन कर दामों को नियंत्रित रखना, ताकि किसान मजबूरी में इन्हें न तो माटी मोल बेचें, ना ही इनके दाम आसमानी होकर गरीब और मध्यम वर्गों को हर साल संकट में डालें। कालांतर में इस स्कीम को विस्तार देकर ‘टोटल’ नाम दिया गया था, और 22 आइटम्स जोड़े गए। नई स्कीम तो पुरानी से भी लुभावनी थी। लेकिन भंडारण क्षमता 350 लाख टन से बढ़ाकर मात्र 395 लाख टन हुई, जो कुल फल-सब्जी उत्पादन का मात्र 9.5% है। नतीजतन खुदरा महंगाई रोकने में सरकार फेल रही। आलू, प्याज, टमाटर के दाम डेढ़ से दो गुना हो गए हैं। सीआईआई की रिपोर्ट के अनुसार 30-40% फल-सब्जियां बर्बाद होती हैं हालांकि सरकारी तंत्र केवल 5-16% मानता है। याद करें, पिछले साल इन्हीं दिनों टमाटर 250-300 रुपए किलो तक बिका था। समस्या की जड़ में जाना होगा। अगर आगरा- फर्रुखाबाद का किसान दो साल पहले आलू की फसल खेत में दबा देता है, लासलगांव के इलाके का किसान प्याज और कर्नाटक का किसान टमाटर सड़कों पर फेंक देता है तो यह समस्या का दूसरा पहलू है। क्या इन योजनाओं- जिन्हें एक वैल्यू चेन स्थापित करने के लिए लाया गया था- के तहत मंडियों को आज तक एकीकृत किया जा सका है? ये तीनों उत्पाद उचित भंडारण चाहते हैं ताकि कीमतें न ज्यादा गिरें, न ज्यादा आसमानी हों। लेकिन आज भी जो टमाटर कर्नाटक का किसान 10 रुपए किलो बेचता है, दिल्ली में 150 रुपए कैसे हो जाता है ? सरकार का मार्केट इंटरवेंशन (बाजार में हस्तक्षेप ) प्रभावी है ?
Date: 17-07-24
पूर्वाग्रहों से भरी एआई भारत के लिए चुनौती-अवसर दोनों
अविजित घोष, ( नॉर्थईस्टर्न यूनिवर्सिटी के पूर्व लेक्चरर )

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) एक टेक्नोलॉजी है, जिसमें मशीन डेटा से सीखती और निर्णय लेती है। हालांकि कई बार एआई सिस्टम पक्षपातपूर्ण निर्णय लेते हैं और अपने पूर्वाग्रहों के साथ समस्याएं खड़ी कर सकते हैं। वहीं, एआई एथिक्स का उद्देश्य निष्पक्ष, सुरक्षित और लोगों के अधिकारों का सम्मान करने वाली टेक्नोलॉजी का निर्माण है। लेकिन जब एआई सबके लिए समान रूप से काम नहीं करती तो समस्याएं खड़ी कर सकती है, खासतौर पर भारत जैसे विविधतापूर्ण देश के सामने। अपने इस आलेख की तैयारी के लिए जब मैंने ‘स्टेबल डिफ्यूजन एक्सएल’ (शब्दों से तस्वीर तैयार करने वाला एआई मॉडल) से कुछ तस्वीरें तैयार कीं, तो भारतीय संदर्भ में इसने साफ-साफ भेदभाव का उदाहरण सामने पेश कर दिया। उच्च शिक्षित लोगों या ज्यादा वेतन पाने वालों के प्रस्तुतिकरण में इसने बमुश्किल ही महिलाओं को चित्रित किया, साथ ही अशिक्षित और दिहाड़ी मजदूरी करने वालों को एआई मॉडल ने बहुत सांवला दिखाया।
इस तरह के पूर्वाग्रहों के मूल में दरअसल एआई मॉडल के प्रशिक्षण में इस्तेमाल हुआ डेटा है, जो कि ज्यादातर अंग्रेजी में है और इंटरनेट पर मौजूद सामग्री से लिया गया है, जहां अमेरिकी दृष्टिकोण ही हावी है। एआई मॉडल्स, डेटा पर निर्भर है, इसलिए उच्च गुणवत्तापूर्ण डेटा का सावधानी से इस्तेमाल जरूरी है। पश्चिमी देशों में तैयार किए गए एआई मॉडल्स अक्सर भारतीय संस्कृति, भाषाई और सामाजिक आर्थिक विविधता के लिए जिम्मेदार नहीं होते हैं, जिससे उनकी प्रभावशीलता भी कम होती है। यूनिवर्सिटी ऑफ कोपेनहेगन के हालिया शोध में सामने आया कि चैटजीपीटी से जब अन्य देशों और संस्कृतियों के बारे में पूछा जाता है, तब भी वह मुख्य रूप से अमेरिकी मानदंडों व मूल्यों को दर्शाने के साथ उसे बढ़ावा देता है।
भारत में सबको साथ में लेकर चलने वाली समावेशी एआई तैयार करना इसलिए भी कठिन है क्योंकि देश का राजनीतिक और सांस्कृतिक दायरा बहुत जटिल है, जिसमें 22 आधिकारिक भाषाएं और 1652 से ज्यादा बोलियां हैं। एक आर्टिकल में सामने आया है कि चैटजीपीटी जैसी कुछ टेक कंपनियां विवादों के डर से भारत में एआई टेक्नोलॉजी अपनाने में हिचक रही हैं। इसके कारण देश में इनोवेशन और लाभकारी एआई टेक्नोलॉजी को अपनाने की गति धीमी पड़ सकती है। वहीं, जब बात ग्रामीण भारत में इसे अपनाने की हो तो एआई आधारित अनुवाद प्रणाली अंग्रेजी-केंद्रित डेटा पर प्रशिक्षित होने के कारण प्रासंगिक और बोलचाल के अनुवादों के साथ जूझती है। हालांकि इससे एआई मॉडल्स को अपनाने की गति में फर्क नहीं पड़ा है। आईबीएम की 2024 में आई रिपोर्ट के मुताबिक 59 प्रतिशत भारतीय कंपनियों ने पहले ही एआई को तैनात कर दिया है।
पश्चिमी मॉडल जिन जटिल समस्याओं की पहचान करने में विफल रहा है, उसके चलते हमें देखना चाहिए कि क्या एआई के लाभ सभी भारतीयों को समान रूप से मिल पा रहे हैं। एआई के सही मायनों में लोकतांत्रिक इस्तेमाल के लिए समुदायों को सशक्त करने की जरूरत है ताकि वे समझें कि उन्हें प्रभावित करने वाले एआई टूल्स कैसे काम करते हैं। एआई डिजाइन में मानव केंद्रित रणनीति के लिए साथ मिलकर काम करना होगा, जिसमें टेक्नोलॉजी जानकारों के साथ, डोमेन विशेषज्ञ, समुदाय के लोग भी हों। ‘एआईफॉरभारत’, ‘कलेक्टिव इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट’ जैसी पहल उदाहरण हैं। जहां ‘एआईफॉरभारत’ भारतीय भाषाओं के लिए डेटासेट व भाषा मॉडल विकसित करती है, वहीं कलेक्टिव इंटेलिजेंस लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के माध्यम से एआई में सामुदायिक लक्ष्यों को शामिल करती है। इन चुनौतियों पर सक्रियता से काम किया जाए तो भारत भी एआई सिस्टम तैयार कर सकता है। इसके लिए इनोवेशन, सांस्कृतिक रूप से संवेदनशीलता और एथिक्स की जरूरत है। अपने सांस्कृतिक ताने-बाने को संरक्षित करते हुए एआई की क्षमता का उपयोग करने का भारतीय दृष्टिकोण अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए मॉडल बन सकता है।
Date: 17-07-24
पर्यावरण के लिए भारत ही दुनिया के नेतृत्व में सक्षम
प्रो. चेतन सिंह सोलंकी, ( आईआईटी बॉम्बे में प्रोफेसर )
लगता है कि दुनिया नेतृत्व की कमी से जूझ रही है। ऐसे युग में जहां हम एआई में महारत हासिल कर रहे हैं, लोग अभी भी ऐसी सरल-सी समस्याओं से संघर्ष कर रहे हैं, जिन्हें प्रभावी नेतृत्व से हल किया जा सकता था। भारत की सिलिकॉन वैली कहलाने वाले बेंगलुरु- जो कि इनोवेशन और टेक्नोलॉजी का केंद्र है- में पीने का पानी कोई मुद्दा नहीं होना चाहिए। फिर भी, यह है। नीति आयोग के समग्र जल प्रबंधन सूचकांक के अनुसार बेंगलुरु में पानी की गंभीर कमी है। यह एक ऐसी स्थिति है, जो शहरी भारत में जल-प्रबंधन के व्यापक संकट को उजागर करती है। मेरा मानना है कि यह समस्या पानी नहीं, नेतृत्व और शासन की कमी से उपजी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अधिकांश भारतीयों को शौचालय उपलब्ध कराने की समस्या को स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से हल किया गया। अक्टूबर 2019 तक, सरकार ने ग्रामीण भारत को खुले में शौच मुक्त घोषित किया, जिसके लिए 10 करोड़ से अधिक शौचालय बनाए गए। यह मौलिक मुद्दों को प्रभावी ढंग से संबोधित करने और हल करने की प्रधानमंत्री की क्षमता को प्रदर्शित करता है। लेकिन जब ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन की समस्या को हल करने की बात आती है तो लगता है भारत ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में नेताओं की कमी है। लगता है कि कोई भी नेता इतना बड़ा नहीं है कि इस मुद्दे पर विश्व को समाधान की ओर ले जा सके।
195 देशों द्वारा पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद भी- जिसमें 2015 के स्तर से कार्बन उत्सर्जन को कम करना शुरू करने और 2030 तक उसे 45% तक घटाने पर सहमति व्यक्त की गई थी- कार्बन उत्सर्जन में कमी का कोई महत्वपूर्ण संकेत नहीं है। वास्तव में, वैश्विक कार्बन उत्सर्जन 2023 में 40 अरब टन से अधिक के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया है। यह 2022 की तुलना में 1.1% की वृद्धि को दर्शाता है, जो बढ़ते उत्सर्जन की चिंताजनक प्रवृत्ति को जारी रखता है। ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया के देश एक-दूसरे को बेवकूफ बना रहे हैं। पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर के बावजूद सीओ2 उत्सर्जन की प्रवृत्ति बढ़ रही है। सीओ2 एक ग्रीनहाउस गैस है, जो वायुमंडल में गर्मी को रोक लेती है। इसके बढ़ते स्तर से ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु-परिवर्तन होता है। तत्काल ही कठोर कार्रवाई की आवश्यकता है।
प्रधानमंत्री मोदी आज दुनिया में सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक हैं। हाल के सर्वेक्षणों के अनुसार उनकी अप्रूवल-रेटिंग 70% से अधिक रही है। उन्होंने अपनी कूटनीतिक सूझबूझ ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत का कद बढ़ाया है। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस जैसी पहल की है। वैश्विक स्तर पर भारतीय संस्कृति और मूल्यों को बढ़ावा देने की क्षमता प्रदर्शित की है। जी-20 और संयुक्त राष्ट्र जैसे मंचों में उनकी सक्रिय भागीदारी वैश्विक नीतियों को आकार देने और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में उनकी भूमिका को भी रेखांकित करती है। वे पर्यावरण-संरक्षण और जलवायु-कार्रवाई के भी मुखर समर्थक रहे हैं। इसी कड़ी में मिशन लाइफ (पर्यावरण के लिए जीवनशैली) का शुभारंभ एक अग्रणी कदम था।
मिशन लाइफ के सिद्धांतों पर चलना भारतीयों के लिए मुश्किल नहीं होगा। प्रकृति का सम्मान करना और हवा, पानी, मिट्टी, पेड़, पहाड़ों जैसे प्राकृतिक संसाधनों की पूजा करना हमारी संस्कृति का हिस्सा रहा है। जीवन के अंत तक सामग्रियों का कुशलतापूर्वक उपयोग करना भारतीयों के लिए एक आदर्श रहा है। प्रधानमंत्री की समावेशी नेतृत्व शैली ने उन्हें जलवायु संकट के माध्यम से दुनिया का मार्गदर्शन करने में सक्षम नेता के रूप में स्थापित किया है। भारत को ‘विश्व गुरु’ बनाने का उनका दृष्टिकोण जलवायु- कार्रवाई का नेतृत्व करने के लिए एक वैश्विक नेता की आवश्यकता के साथ पूरी तरह से मेल खाता है। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि मिशन लाइफ को लागू करके अपने नेतृत्व-कौशल का सही मायने में प्रदर्शन करें।
सुधार की राह देखती आईबीसी
डॉ. अश्विनी महाजन, ( लेखक दिल्ली विश्वविद्यालय के पीजीडीएवी कालेज में प्रोफेसर हैं )
इंसोल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड यानी आईबीसी के कानूनी रूप लेने से पहले दिवालियापन से निपटने के लिए लगभग एक दर्जन कानून थे। उनमें से कुछ कानून तो 100 साल से भी अधिक पुराने थे। मोदी सरकार ने इन कानूनों के स्थान पर आईबीसी के रूप में जो पहल की, उसे एक बड़ा आर्थिक सुधार माना गया। आईबीसी के अनुसार जब कोई देनदार दिवालिया हो जाता है तो उसकी संपत्ति को लेनदार आसानी से अपने कब्जे में ले सकते हैं। यदि लेनदारों की समिति के 75 प्रतिशत या उससे अधिक सदस्य सहमत होते हैं तो ऐसी कार्रवाई के लिए आवेदन स्वीकार किए जाने की तिथि से (एनसीएलटी की मंजूरी के अधीन 90 दिनों की छूट अवधि के साथ) 180 दिनों में कार्रवाई की जा सकती है। यदि तब भी ऋण का भुगतान नहीं होता तो व्यक्ति/फर्म को दिवालिया घोषित कर दिया जाएगा। आईबीसी के पीछे यह मंशा थी कि इससे ऋण की वसूली में होने वाली देरी और उससे जुड़े नुकसान स्वत: खत्म हो जाएंगे। कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देने के लिहाज से वैश्विक संस्थाएं भी आईबीसी को सराहती रही हैं। विश्व बैंक की ‘ईज आफ डूइंग बिजनेस’ रैंकिंग में भारत के 2014 में 142वें स्थान से 2019 तक 63वें स्थान तक पहुंचने में आईबीसी जैसे सुधार की अहम भूमिका मानी गई।
कारोबारी सुगमता में व्यवसाय शुरू करने और उसे बंद करने में सहूलियत जैसे दोनों पहलू शामिल होते हैं। आईबीसी ने व्यवसाय को बंद करना आसान बना दिया। हालांकि आईबीसी की घोषित अपेक्षाओं और जमीनी स्तर पर अनुभव के बीच कुछ अंतर जरूर है। आईबीसी के तहत तनावग्रस्त संपत्तियों के समाधान का प्रारंभिक बिंदु कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआइआरपी) है, जो वित्तीय लेनदारों, परिचालन लेनदारों या यहां तक कि कारपोरेट द्वारा स्वयं सीआइआरपी शुरू करने के लिए एक वसूली तंत्र है। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, आईबीसी के बाद से जनवरी 2024 तक 7,058 कारपोरेट देनदारों को सीआइआरपी में लाया गया है, जिनमें से 5,057 मामले बंद कर दिए गए और 2,001 समाधान के विभिन्न चरणों में हैं। जो मामले बंद हो गए हैं, उनमें से करीब 16 प्रतिशत में सफल समाधान योजनाएं सामने आई हैं। वहीं, 19 प्रतिशत को आईबीसी की धारा 12ए के तहत वापस ले लिया गया है, जहां बड़े पैमाने पर देनदार लेनदारों के साथ पूर्ण या आंशिक निपटान के लिए सहमत हुए। जबकि 21 प्रतिशत अपील या समीक्षा पर बंद कर दिए गए और 44 प्रतिशत मामलों में परिसमापन आदेश पारित किए गए हैं। हालांकि, समाधान के विभिन्न चरणों में अटके मामलों में देरी चिंता के रूप में उभरी है। वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान मामले को स्वीकार करने में लगने वाला औसत समय क्रमशः 468 दिन और 650 दिन रहा। यह अपेक्षित समय से कहीं अधिक है।
वित्तीय लेनदारों द्वारा दायर अपीलों के निपटारे में देरी का एक कारण यह है कि अक्सर अदालतें लेनदेन के वाणिज्यिक पहलुओं में उलझ जाती हैं। ये पहलू कानून से संबंधित बिंदुओं से नहीं, बल्कि प्राप्त मूल्य आदि के संदर्भ में लेनदारों से संबंधित होते हैं, जो समाधान योजना को मंजूरी देने का फैसला करने वाले लेनदारों की व्यावसायिक बुद्धि पर सवाल उठाने जैसा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लेनदारों की समिति (सीओसी) की व्यावसायिक समझ पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। एक बार जब सीओसी अंतिम निर्णय ले लेती है कि समाधान योजना को मंजूरी दी जाए या नहीं तो इसे अदालतों द्वारा समीक्षा का विषय नहीं बनाया जाना चाहिए। विशेषकर उस स्थिति में जब किसी कानूनी प्रविधान का उल्लंघन न हो। एस्सार स्टील मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि यह बहुसंख्यक लेनदारों की व्यावसायिक समझ है, जो संभावित समाधान आवेदक के साथ बातचीत के जरिये यह निर्धारित करती है कि कारपोरेट समाधान प्रक्रिया कैसे और किस तरीके से संपादित होनी है। एसआरईआइ मल्टीपल्स मामले में भी शीर्ष अदालत ने कहा कि समाधान योजना सीओसी द्वारा स्वीकृत हो जाने के बाद कोई संशोधन स्वीकार्य नहीं है, जब तक कि यह आईबीसी की मूल भावना के विपरीत न हो। हालांकि वास्तविकता अलग है। वीडियोकान मामले में समाधान योजना को जून 2021 में एनसीएलटी ने अनुमोदित किया, मगर यह सुप्रीम कोर्ट में अभी भी लंबित है। एसकेएस पावर जेनरेशन मामले में सीओसी ने जून 2023 में पूर्ण सहमति के साथ सारदा एनर्जी एंड मिनरल्स की योजना को मंजूरी दी, फिर भी यह मामला अभी तक अनसुलझा है। ऐसी देरी से परिसंपत्तियों के मूल्य में कमी आने की आशंका होती है। इससे लेनदारों को नुकसान हो सकता है। इसके चलते भविष्य में संभावित खरीदारों को लुभाना भी मुश्किल हो जाता है और अंतत: आईबीसी का उद्देश्य विफल हो जाएगा।
वित्तीय मामलों की स्थायी समिति की एक रिपोर्ट में कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआइआरपी) में देरी के कुछ चरणों की पहचान की गई है। इसमें पहला चरण है सीआइआरपी शुरू करने के लिए आवेदन की स्वीकृति और दूसरा एनसीएलटी द्वारा समाधान योजना को मंजूरी। सीआइआरपी आरंभ करने के लिए आवेदन स्वीकार करने से जुड़ी समस्याओं की चर्चा करें तो कभी-कभी हितधारकों के बीच असहमति के कारण भी देरी होती है। कानून कहता है कि यदि सीओसी के 75 प्रतिशत या उससे अधिक सदस्य सहमत हैं तो सीओसी द्वारा समाधान की प्रक्रिया के दौरान कुछ कार्रवाई संभव है। कई बार लेनदार और अन्य हितधारक समाधान योजना पर सहमत नहीं हो पाते हैं और इससे भी प्रक्रिया में देरी हो सकती है। दिवालियापन प्रक्रिया में शामिल विभिन्न हितधारकों जैसे लेनदार, देनदार और संभावित खरीदार के बीच विवाद एवं अदालती लड़ाई से और भी देरी हो सकती है। दिवाला और दिवालियापन के मामलों में समाधान खोजने में आने वाली प्रमुख समस्याएं कर्मचारियों की कमी से लेकर प्रक्रियाओं और उनसे संबंधित कानून के बोझिल बिंदुओं की प्रणालीगत अक्षमताओं से संबंधित हैं, जिनका दुरुपयोग भ्रष्ट और विलफुल डिफाल्टर मामलों को लटकाने के लिए करते हैं। वैसे तो, सुप्रीम कोर्ट ने आईबीसी की वैधता से जुड़े कई बुनियादी सवालों का समाधान कर दिया है, लेकिन कुछ मुद्दे सामने आते ही रहते हैं। जबकि आईबीसी जैसे किसी भी महत्वपूर्ण कानून पर लगातार समझ बनाते हुए उसमें आवश्यक बदलावों की जरूरत है ताकि अदालतों में अनावश्यक देरी से बचा जा सके।
 Date: 17-07-24
Date: 17-07-24
निजी भागीदारी में हो इजाफा
संपादकीय
बीते तकरीबन पांच साल में देश की रक्षा खरीद नीति में ‘स्वदेशीकरण’ का बड़ा लक्ष्य तय किया गया। भारत समेत किसी भी देश में ऐसे प्रयास करने के लिए पर्याप्त वजह होती हैं। यह महत्त्वपूर्ण है, खासकर एक बढ़ती असुरक्षा वाले विश्व में जरूरी हथियारों और उन्हें चलाने वाले प्लेटफॉर्मों पर अधिकतम नियंत्रण आवश्यक है। हथियारों पर विदेशी मुद्रा खर्च करने में कमी लाना एक और वांछित परिणाम है। इस बात की भी पर्याप्त वजह हैं कि यह माना जाए कि घरेलू रक्षा क्षेत्र उन बेहतरीन क्षेत्रों में से एक है जो सरकार को घरेलू अर्थव्यवस्था में नवाचार बढ़ाने के लिए उत्साहित कर सकते हैं। इसके बावजूद रक्षा खरीद के स्वदेशीकरण को समय के साथ टिकाऊ बनाने के लिए निजी क्षेत्र को सही ढंग से साथ में जोड़ना होगा। रक्षा मंत्रालय की ओर से हाल के दिनों में जारी आंकड़ों से यही संकेत मिलता है कि यह उस हद तक नहीं हो रहा है जिस हद तक वांछित है।
रक्षा मंत्रालय के मुताबिक देश का घरेलू रक्षा उत्पाद पिछले दो वित्त वर्षों से एक लाख करोड़ रुपये से अधिक है लेकिन निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी बमुश्किल एक चौथाई है और यह 2017-18 के स्तर के आसपास ही था। कई लोगों ने ध्यान दिया है कि लार्सन ऐंड टुब्रो जैसी कंपनियों ने हाल के समय में अपना रक्षा कारोबार बढ़ाया है लेकिन आंकड़े बताते हैं कि निजी क्षेत्र की ओर से ऐसा विस्तार देश के रक्षा उत्पादन में उसकी हिस्सेदारी बरकरार रख पाने भर के लायक है। रक्षा उत्पादन का अधिकांश हिस्सा रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों से ही आ रहा है। यह निश्चित नहीं है कि उनमें भारत को इस क्षेत्र की मूल्य श्रृंखला में ऊपर ले जाने की क्षमता है अथवा नहीं या फिर क्या वे ऐसा आंतरिक स्तर पर नवाचार कर सकते हैं कि जो न केवल सुरक्षा के क्षेत्र में बढ़त दे बल्कि अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में भी इसके प्रभाव को बढ़ाए। स्पष्ट है कि ‘मेक इन इंडिया’ की आकांक्षा है लेकिन हकीकत ‘मेक इन पब्लिक सेक्टर’ ही है।
यदि स्वदेशीकरण के माध्यम से निजी क्षेत्र को सही मायने में मजबूत बनाना है तो उन क्षेत्रों को चिह्नित करना होगा जहां सरकार को बदलाव करने की आवश्यकता है। एक जरूरत यह है कि रक्षा कारोबार में भारतीय कंपनियों को निवेश का सुरक्षित माहौल मुहैया कराया जाए।
ऐसा तब हो सकता है जबकि सरकार इसके लिए जरूरी दिशानिर्देश जारी करे, ये दिशानिर्देश उचित और तार्किक हों और उनके साथ खरीद की प्रतिबद्धता भी जुड़ी हो। दूसरे देशों में निजी कंपनियां बड़ा निवेश करके प्रसन्न हैं क्योंकि वहां उन्हें आश्वस्ति है कि उनका निवेश बरबाद नहीं होगा। परंतु भारत में ऐसे भरोसे का अभाव है। एक बड़े ग्राहक वाले कारोबार में ग्राहक को विश्वसनीय खरीदार के रूप में देखे जाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करना होता है ताकि निवेश को गति मिले। देश में रक्षा निजी क्षेत्र के कुछ पहलुओं को अक्सर सफल बताया जाता है। इनमें छोटे और मझोले उपक्रमों की बढ़ती उपस्थिति एक है। इसमें स्टार्टअप भी शामिल हैं। बड़े निजी निवेश के लिए स्पष्ट खाके के अभाव में ऐसी स्टार्टअप भी उचित जगह नहीं बना पाएंगी या उन्हें समुचित प्रोत्साहन नहीं मिल सकेगा। भारत को इस क्षेत्र में विदेशी निवेश से जुड़े दिशानिर्देश को भी शिथिल करने की जरूरत होगी। गत वर्ष 100 फीसदी विदेशी स्वामित्व वाली एक परियोजना को मंजूरी दी गई -स्वीडिश कार्ल-गुस्ताव राइफल, परंतु प्रौद्योगिकी स्थानांतरण की चिंताओं के कारण अन्य मामलों में हम पिछड़े हुए हैं। ऐसी चिंताओं के कारण निवेश में देरी नहीं होने दी जा सकती है। इस क्षेत्र में निजी निवेश का दायरा बढ़ाने का काम काफी समय से लंबित है।
चढ़ती कीमतों को नीचे लाने के उपाय
अरुण कुमार, ( वरिष्ठ अर्थशास्त्री )
पिछले महीने यूरोपीय संघ ने यह कहते हुए ऋण दरों में कटौती की थी कि उसने महंगाई को काफी हद तक काबू में कर लिया है। ऐसा करने वाली वह दूसरी प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्था थी, क्योंकि इससे पहले कनाडा ने भी दरों में कमी करने का एलान किया था। अब अमेरिका ने भी लगातार तीन महीने तक महंगाई कम होने के कारण यह संकेत दिया है कि जल्द ही फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में कटौती कर सकता है। जाहिर है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अनेक देश अपने यहां दरों में कमी कर रहे हैं, जिससे लगता है कि महंगाई को नियंत्रित करने में वे सफल साबित हो रहे हैं। इसकी वजह यह हो सकती है कि कोरोना महामारी, यूक्रेन संकट और फिर इजरायल-हमास जंग की वजह से वैश्विक आपूर्ति शृंखला पर जो नकारात्मक असर पड़ा था, उससे पार पाने में उन्हें सफलता मिलने लगी है। मगर भारत में हालात चुनौतीपूर्ण नजर आते हैं। यहां फल-सब्जियां ही नहीं, खाद्यान्न के दाम भी चढ़ रहे हैं।
अक्सर देखा गया है कि गर्मी बढ़ने या बारिश ज्यादा होने से फलों और सब्जियों की कीमतें बढ़ जाती हैं, क्योंकि इनके भंडारण की समुचित व्यवस्था अपने देश में नहीं है। मगर क्या वजह है कि गेहूं, चावल जैसे खाद्यान्न की कीमतें भी चढ़ रही हैं, जबकि इनका संग्रह किया जा सकता है और हमारे पास इनका पर्याप्त भंडार भी है? वह भी तब, जब इनकी रिकॉर्ड पैदावार के दावे किए गए थे और हमने निर्यात पर भी रोक लगा दी थी? साफ है, भारत में विशेषकर खाने-पीने की वस्तुओं का प्रबंधन काफी कमजोर है, और यह भी कि शायद रिकॉर्ड उत्पादन नहीं हुआ है। कुछ विशेषज्ञ कहते भी हैं कि उत्पादन के आकलन का मौजूदा तरीका गलत है, जिसमें सुधार की सख्त जरूरत है।
अभी महंगाई दो तरीकों से मापी जाती है- एक, थोक मूल्यों के आधार पर, और दूसरा, उपभोक्ता मूल्यों के आधार पर। थोक मूल्य मूलत: उत्पादकों से जुड़ा है। किसानों, फैक्टरियों या उत्पादन करने वाली इकाइयों आदि के थोक उत्पाद इसमें शामिल होते हैं। महामारी के बाद भारत में थोक मूल्य सूचकांक में काफी बढ़ोतरी देखी गई थी। एक समय तो यह 15 प्रतिशत की रफ्तार से बढ़ रहा था। मगर इसकी तुलना में उपभोक्ता मूल्य उतना नहीं बढ़ा और वह सात-आठ प्रतिशत पर बना रहा। इसके बाद थोक मूल्य नीचे लुढ़का, लेकिन उपभोक्ता मूल्य पर आधारित महंगाई में बहुत कमी नहीं आई। रिजर्व बैंक द्वारा तय चार प्रतिशत (दो प्रतिशत ऊपर या नीचे) के लक्ष्य के करीब आने में भी इसे खासा वक्त लगा। आज भी यह पांच प्रतिशत से अधिक की रफ्तार से बढ़ रही है।
सवाल है, महंगाई आम आदमी को किस तरह परेशान करती है? दरअसल, हर तबके के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का अर्थ अलग-अलग होता है। ऐसा इसलिए, क्योंकि हर वर्ग के लिए उपभोग की प्राथमिकता अलग-अलग होती है। मसलन, गरीबों के बजट में खाने-पीने की वस्तुओं की हिस्सेदारी 40 फीसदी तक होती है, जबकि अमीर तबके में यह बमुश्किल पांच प्रतिशत। इसी कारण जब खाद्यान्न के दाम बढ़ते हैं, तो गरीबों की थाली कहीं ज्यादा बिगड़ जाती है। इसके बनिस्बत, महंगाई अमीरों की बचत पर चोट करती है, क्योंकि वे अपनी बचत घटाकर ही महंगाई से लड़ते हैं, वहीं एक तबका व्यापारी वर्ग भी है, जिसके लिए महंगाई कारोबारी लाभ लेकर आती है।
ऐसे में, जरूरी है कि महंगाई से पार पाने के लिए पर्याप्त उपाय किए जाएं। इस दिशा में फूड मैनेजमेंट, यानी खाद्य प्रबंधन काफी अहम साबित हो सकता है। गेहूं, चावल जैसे उत्पादों के दाम इसलिए फल अथवा सब्जियों की तरह तेजी से ऊपर-नीचे नहीं होते, क्योंकि इनकी सरकारी खरीद होती है और एक नियत मात्रा में इनका भंडारण किया जाता है। हमें बाकी उत्पादों के लिए भी यही रणनीति अपनानी चाहिए। विशेषकर टमाटर, आलू अथवा प्याज को कोल्ड स्टोरेज में रखा जा सकता है। बाकी सब्जियों अथवा फलों को खाद्य प्रसंस्करण के जरिये सहेजने की रणनीति बनाई जानी चाहिए। मौजूदा हालात में खाद्य प्रसंस्करण और खाद्य भंडारण को बढ़ावा देना काफी जरूरी है। मगर दिक्कत यह है कि इसमें पर्याप्त मात्रा में निवेश नहीं हो रहा। निवेशकों की चिंता है कि यदि वे भंडारण करते हैं और बाद में भंडारण की सीमा कम कर दी गई, तो उन्हें औने-पौने दाम पर उत्पाद बेचने होंगे, जिससे उनको घाटा हो सकता है। लिहाजा, सरकार को एक स्थायी नीति बनानी चाहिए।
उसे न सिर्फ इन उत्पादों की खरीद करनी चाहिए, बल्कि कारोबारियों को यह भरोसा भी देना चाहिए कि दाम ज्यादा ऊपर-नीचे नहीं होंगे। इससे कोल्ड स्टोरेज करने वाले लोगों या खाद्य प्रसंस्करण करने वाली कंपनियों को एक मुकम्मल संदेश जाएगा। वैसे भी, महंगाई बढ़ने पर सरकार दखल देने में देर नहीं करती। मसलन, टमाटर-प्याज के दाम बढ़ने पर वह खुद सस्ते दामों में इनको बेचने लगती है। लिहाजा, जब हर साल तात्कालिक तौर पर यही नीति अपनाई जा रही है, तो इसे स्थायी जामा क्यों नहीं पहना दिया जाता?
विकसित देशों में यह नीति काफी कारगर रही है। वहां खाद्य प्रसंस्करण करने वाली कंपनियां उत्पादन अधिक होने पर प्रबंधन की जिम्मेदारी संभाल लेती हैं। वहां बड़ी जोत वाली कॉरपोरेट कंपनियां भी अधिक हैं, जो सुनिश्चित करती हैं कि कैसे उत्पादों का भंडारण किया जाए? जबकि, भारत में छोटे किसानों की संख्या अधिक है, जिनके पास भंडारण की उचित सुविधा नहीं है। इसलिए जो काम विदेश में कंपनियां करती हैं, उसे हमारी सरकारों को करना होगा। फसलों की सरकारी खरीद के साथ-साथ उनका भंडारण भी किया जाना चाहिए। बेशक, इस काम में प्रशासनिक चुनौतियां भी आड़े आएंगी, लेकिन ऐसा करना जरूरी है।
महंगाई कम करने में रिजर्व बैंक भी कुछ हद तक अपनी भूमिका निभा सकता है। वह मांग को नियंत्रित करके महंगाई कम कर सकता है, लेकिन जहां आपूर्ति शृंखला में गड़बड़ी है, वहां वह खाली हाथ रह सकता है। कराधान में भी सुधार आवश्यक है और हमें अप्रत्यक्ष कर को कम करना चाहिए। अभी कर-जीडीपी अनुपात 17 फीसदी के करीब है, जिसमें प्रत्यक्ष कर की हिस्सेदारी 11 प्रतिशत और अप्रत्यक्ष कर की 6 प्रतिशत है। ऐसे में, यदि हम लग्जरी उत्पादों पर ही अप्रत्यक्ष कर लगाएं, तो गरीबों को काफी राहत मिल सकेगी। मतलब साफ है कि महंगाई नियंत्रित करने में रिजर्व बैंक की उतनी भूमिका नहीं है, जितनी सरकार की है।
