
17-05-2024 (Important News Clippings)
To Download Click Here.
 Date: 17-05-24
Date: 17-05-24
It’s Courage, Not Crime
Whistleblowers strengthen democracy but face dangers. Give them strong legal protection
TOI Editorials
Whistleblowers have it tough across the world. The Supreme Court in Canberra, Australia, recently sentenced former Australian army lawyer David McBride for revealing information about alleged Australian war crimes in Afghanistan. This comes seven years after Australian public broadcaster ABC published a series of articles based on information provided by McBride. That information was separately confirmed by an Australian govt inquiry. However, it was McBride the whistleblower who was prosecuted.
From false claims to national security |Whistleblowing has a chequered history. During the American Civil War Abraham Lincoln’s govt enacted the False Claims Act (FCA) to incentivise reporting corruption in military supplies.
Interestingly, FCA remains on US statute books in an amended form and has been used over the years in cases related to fraud in military contracts and corruption in the pharma industry. But things get murky when it comes to matters of national security and wrongdoings in militaries. State interests and discipline are privileged over those seeking to spotlight internal wrongs.
Risky business | Perhaps the most high voltage case of whistle blowing related to war crimes this century was the highlighting of atrocities committed by US soldiers in Iraq’s Abu Ghraib prison. The horrific torture was exposed by Sergeant Joseph Darby. Once identified as the whistleblower, he and his family faced harassment and even death threats. Similarly, US’s NSA contractor Edward Snowden had to flee to Russia for exposing illegal mass surveillance programmes.
India’s paper tiger | India passed a Whistle Blowers Protection Act in 2014. Ironically, it hasn’t been notified to date. In any case, the Act has multiple exemptions – it doesn’t cover armed forces and is not applicable to the private sector. Nor does it provide financial incentives for whistle blowing like the American FCA. Civil society groups have argued that attacks against RTI activists and whistleblowers have increased in the absence of a legal framework. True, state secrets need to be protected for national security. But this can’t be a blanket cover to hide corruption and criminal wrongs. Democracy is strengthened by courageous whistleblowers speaking up for justice.
Date: 17-05-24
Courting The Cops, Always
SC order in the News Click case shows trial court judges are authorising detentions casually. With around 50 lakh arrests a year and thousands of remand applications a day, they must apply judicial scrutiny
Naveed Mehmood Ahmad, [ The writer is a Senior Resident Fellow at Vidhi Centre for Legal Policy ]
On Wednesday, Supreme Court declared the arrest of Prabir Purkayastha, founder of NewsClick, illegal and ordered his release from custody. Purkayastha had been in police and judicial custody since October last year, in connection with a case under provisions of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 and the Indian Penal Code, 1860.
Issue | Individual rights and national security
SC declared Purkayastha’s arrest and subsequent police remand illegal on the basis that grounds of his arrest were not communicated to him in writing. The court further held that mere filing of the chargesheet would not rectify the illegality and unconstitutionality of the arrest and grant of police custody. The court’s order is significant as it recognises the need for procedural propriety to protect individual liberties, even in cases involving national security concerns. It is, however, even more crucial for bringing attention to how remand applications are processed by magistrates and law enforcement agencies, effectively obstructing the realisation of the fundamental rights guaranteed under Articles 21 and 22.
Article 22 | Provide grounds of arrest in writing
Article 22 of the Constitution enshrines the right to be informed of the grounds of arrest, and to consult and be defended by a legal practitioner of choice. Clause (5) of Article 22 extends this protection to cases of preventive detention. Drawing from the protection that Article 22 offers, the Code of Criminal Procedure, 1973, UAPA, 1967 and other special laws require the arresting officers to inform the arrestee of the grounds of arrest. This is critical to ensure that the arrestee is able to mount a defence, protect their personal liberty and avoid unnecessary pre-trial detention.
Interestingly, these provisions do not mandate the communication of grounds of arrest to be in written form. This, in fact, was one of the grounds on which the state opposed Purkayastha’s release. A contention that SC held was “untenable in the eyes of law”. Relying on SC’s judgments in Harikisan vs State of Maharashtra (1962) and Lallubhai vs UOI (1982), the bench underlined that communication of the grounds of arrest in writing “is sacrosanct and cannot be breached under any situation”. In essence, a detailed and written communication of the grounds of arrest is critical for a fair remand hearing and to realise the purpose of Article 22.
Issue | Remand and due process
SC’s scrutiny of the events surrounding Purkayastha’s arrest and his remand hearing, however, reveals a far more concerning fact about the workings of the criminal justice system. The court noted that the entire process of securing police remand for Purkayastha was carried out in a clandestine manner, suggesting an attempt to circumvent due process of law. In fact, the failure on the part of the police to inform Purkayastha and his advocate of choice the grounds of arrest and the proposed remand application, as well as the timing of the remand proceedings –as early as 6 in the morning at the residence of the remand judge – suggest how investigative agencies may sidestep due process requirements to retain custody of the accused.
Trial courts | First line of defence
The remand judge, perhaps the only line of defence in such a situation, failed to acknowledge these concerns and to apply judicial scrutiny, instead mechanically granting police custody for seven days. Interestingly, this is not the only case in which remand proceedings have been called into question. In fact, SC itself in Arnesh Kumar vs State of Bihar (2014) categorically stated that in many cases detention is authorised in a “routine, casual and cavalier manner”, grossly affecting the liberty of citizens.
To check this practice, SC in Manubhai Ratilal Patel vs State of Gujarat And Others (2013) underscored that the act of directing remand of an accused is a judicial function and that it is “obligatory on the part of the Magistrate to apply his mind and not to pass an order of remand automatically or in a mechanical manner”.
Issue | Accountability for arrest procedures
With around 50 lakh arrests recorded every year, and thousands of remand applications heard by judges every day, the critical nature of this function cannot be overlooked, especially given the overcrowding in prisons nationwide and the minimal protections provided when an accused is in police custody. The Wednesday order of SC must prompt greater scrutiny of arrest procedures and remand proceedings. It should also foster a renewed emphasis on procedural fairness and accountability within the criminal justice system.
रोजगार सृजन की तेज होती गति
अभिनव प्रकाश, ( लेखक दिल्ली विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं )

भारत में रोजगार सृजन सदैव एक महत्वपूर्ण चुनौती रहा है। इसका मुख्य कारण जनसंख्या में अधिकांश हिस्सा युवा वर्ग का होना है। जब से नरेन्द्र मोदी ने प्रधानमंत्री का पद संभाला है, भारत में रोजगार सृजन में एक नई गति आई है। कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) ने पांच लाख से अधिक युवाओं की भर्ती की है। जबकि कांग्रेस के दस वर्षों (2004-14) के शासनकाल में केवल दो लाख भर्तियां की गई थीं। रेलवे भर्ती बोर्ड ने 4.9 लाख से अधिक युवाओं की भर्ती की है।
संघ लोक सेवा आयोग ने पिछले नौ वर्षों में 50,906 उम्मीदवारों की भर्ती की है, जो कांग्रेस शासनकाल से करीब 6,000 अधिक हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अक्टूबर 2022 में केंद्र सरकार द्वारा 10 लाख केंद्रीय सरकारी नौकरियों को भरने का लक्ष्य रखा था, जिसमें से लगभग नौ लाख उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं। इसी तरह आइटी, विनिर्माण, व्यापार और परिवहन सहित नौ संगठित क्षेत्रों में 1.5 करोड़ से अधिक नौकरियां सृजित हुई हैं।
कोविड के बाद लगभग पांच करोड़ लोग कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ के पेरोल में शामिल हुए हैं। इनमें करीब 3.5 करोड़ लोग पहली बार ईपीएफओ के दायरे में आए हैं। यानी इन्होंने संगठित क्षेत्र में नौकरियां प्राप्त की हैं। चूंकि संगठित क्षेत्र का हिस्सा भारत में रोजगार में करीब 10 प्रतिशत ही है, इसीलिए रोजगार सृजन की स्थिति के लिए असंगठित क्षेत्र के आंकड़ों को भी देखना महत्वपूर्ण होगा।
मोदी सरकार की मुद्रा योजना के माध्यम से 40 करोड़ छोटे उद्यमियों को ऋण प्रदान किए गए हैं। आठ करोड़ लोगों ने पहली बार स्वरोजगार शुरू किया है। पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से 35 लाख रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं को आसान दर पर ऋण प्रदान कर सूदखोरी से मुक्त किया गया है। इन्हें अपने व्यवसाय का विस्तार करने और अधिक लोगों को रोजगार देने में सक्षम बनाया गया है। आजीविका योजना के तहत नौ करोड़ महिलाओं को 83 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों में संगठित किया गया है, जिससे उनकी आय के अनेक मार्ग खुले हैं।
आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना ने अपने रोजगार सृजन लक्ष्य को पार करते हुए 60 लाख से अधिक नए कर्मचारियों को नामांकित किया है। कोरोना काल में इस पहल ने देश में आर्थिक पुनरुत्थान और रोजगार संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कोरोना काल में ही आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के तहत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए 3.63 लाख करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई।
इसने 1.8 लाख करोड़ रुपये के एमएसएमई ऋण को एनपीए बनने से बचाया, जिससे 1.5 करोड़ नौकरियां बचीं और साथ ही नए रोजगार भी सृजित हुए। पीएम रोजगार प्रोत्साहन योजना के तहत 1,52,900 से अधिक प्रतिष्ठानों को लाभ मिला, जिसके 1.2 करोड़ से अधिक लाभार्थी हैं। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत लगभग 13 लाख उम्मीदवारों को 56 सेक्टरों और 600 ट्रेडों में प्रशिक्षित किया गया है और 7.9 लाख को विभिन्न नौकरियों में सीधे नियोजित किया गया। ग्रामीण स्वरोजगार एवं प्रशिक्षण संस्थानों के तहत 64 पाठ्यक्रमों में 39.9 लाख से अधिक लोगों को प्रशिक्षित किया गया है और 28.11 लाख से अधिक उम्मीदवारों को स्वरोजगार में स्थापित किया गया है।
नेशनल अप्रेंटिस प्रमोशन स्कीम के तहत अब तक कुल 13.38 लाख प्रशिक्षुओं को नियुक्त किया गया है। एक वर्ष के भीतर असंगठित क्षेत्र के 29 करोड़ श्रमिकों को सरकारी ‘ई-श्रम’ पोर्टल पर पंजीकृत किया गया है। पीएम ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत 6.2 करोड़ लोगों को ट्रेनिंग दी गई है, जिससे जमीनी स्तर पर रोजगार की क्षमता बढ़ी है। पिछले नौ वर्षों में 5.47 लाख कामन सर्विस सेंटर भी खोले गए हैं। प्रत्येक केंद्र में दो से पांच लोग कार्यरत हैं। ग्रामीण डिजिटल उद्यमों का भी सृजन हुआ है, जिनमें से 67,000 से अधिक महिलाएं उद्यमी हैं।
स्टार्टअप इंडिया के तहत एससी/एसटी लाभार्थियों को 7,351 करोड़ रुपये से अधिक के ऋण दिए गए हैं। स्टैंडअप इंडिया के तहत 25,000 से अधिक एससी/एसटी उद्यमियों को बैंक ऋण और व्यावसायिक सुविधा प्रदान की गई है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने ग्रामीण क्षेत्रों में 9,54,899 नई नौकरियां सृजित करके एक नया आयाम स्थापित किया है। वित्त वर्ष 2022-23 में 448 अरब डालर से अधिक का रिकार्ड निर्यात हुआ। प्रत्येक अतिरिक्त एक अरब डालर के निर्यात से 1.5 लाख नौकरियां सृजित होती हैं। पीएलआइ योजना से भी संगठित क्षेत्रों में 60 लाख से अधिक अतिरिक्त नौकरियां सृजित हुई हैं।
भारत का लक्ष्य 2025-2026 तक इलेक्ट्रानिक्स उत्पादन क्षमता को 24 लाख करोड़ रुपये तक बढ़ाना है, जिससे 10 लाख से अधिक नौकरियां सृजित होने की उम्मीद है। बायोगैस उद्योग में 85,000 नौकरियां सृजित हुई हैं। राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन से 2030 तक आठ लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश और छह लाख से अधिक नौकरियां सृजित होने की संभावना है। सरकारी प्रोत्साहन से इलेक्ट्रानिक वाहन उद्योग में 2030 तक पांच करोड़ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नौकरियां सृजित हो सकती हैं।
रिकार्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास के कारण भी करोड़ों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित हुए। रियल एस्टेट सेक्टर में ही करीब तीन करोड़ रोजगार उत्पन्न हुए हैं। स्टार्टअप की संख्या 2014 में 350 से बढ़कर आज 1.25 लाख हो गई है। इससे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष लाखों नौकरियां सृजित हुई हैं। इस प्रकार देखा जाए तो सरकारी नीतियों के कारण बेरोजगारी दर में लगातार गिरावट आ रही है, जो आज 3.2 प्रतिशत रह गई है। इसी वजह से पिछले दस वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं।
विस्थापन का दंश
संपादकीय
दुनिया भर में हर वर्ष लाखों लोग विस्थापित होते हैं और उन्हें अकथनीय मुश्किलों का सामना करना पड़ता है मगर इक्कीसवीं सदी का सफर तय करते विश्व में भी ऐसी ठोस पहलकदमी नहीं दिखाई देती जिसमें अपनी जड़ों से उखाड़ दिए गए लोगों के दुख पर गौर किया जा सके और एक दीर्घकालिक समाधान का रास्ता तैयार हो। यह बेवजह नहीं है कि आज भी अलग-अलग देशों से बड़ी संख्या में लोग अपना घर बार छोड़ कर दूसरी जगहों पर जाने पर मजबूर कर दिए जाते हैं। अक्सर आने वाली रपटों में इस समस्या की जटिलताओं की ओर ध्यान दिलाया जाता रहा है, लेकिन अब तक विस्थापन का सिलसिला बदस्तूर कायम है। अब जिनेवा स्थित आंतरिक विस्थापन निगरानी केंद्र यानी आइडीएमसी की ताजा रपट में यह दावा किया गया है कि सन 2023 में दक्षिण एशिया में कुल उनहत्तर हजार लोगों को विस्थापन का दंश झेलना पड़ा। इसमें अकेले मणिपुर से सड़सठ हजार लोग विस्थापित हुए। यानी दक्षिण एशिया के सभी देशों में जितने लोगों को अपने ठौर से उजड़ना पड़ा, उसमें सत्तानवे फीसद लोग मणिपुर के हैं।
गौरतलब है कि सन 2018 के बाद यानी पिछले पांच वर्षों में भारत में हुआ यह सबसे बड़ा विस्थापन है देश के अन्य इलाकों में जहां बाढ़ या अन्य प्राकृतिक आपदा और रोजी-रोटी जैसी वजहों से लोगों को दूसरी जगहों की ओर अपने जीने के रास्ते की खोज में निकलना पड़ा, वहीं मणिपुर में हुई व्यापक हिंसा ने वहां हजारों लोगों को विस्थापित होने पर मजबूर कर दिया। आइडीएमसी ने अपनी रपट में इस बात का उल्लेख किया है कि मार्च 2023 में मणिपुर उच्च न्यायालय ने मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के संदर्भ में जो रुख जाहिर किया था, उसके बाद राज्य के बड़े हिस्से में हिंसक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। इसमें करीब दो सौ लोगों की जान जा चुकी है और इसकी वजह से हजारों लोगों को अपना घर छोड़ कर राहत शिविर या दूसरों जगहों पर शरण लेना पड़ा। आज भी वहां स्थिति में कोई उल्लेखनीय सुधार नहीं हुआ है। जाहिर है, एक साधारण विवाद से जो हालात पैदा हुए, उसके एक वर्ष जाने के बावजूद उसे संभालने में सरकार अब तक नाकाम है और इसका खमियाजा हिंसक संघर्ष की वजह से बेठौर हुए लोगों को भुगतना पड़ रहा है।
विश्व भर में ऐसे लोगों की एक बड़ी संख्या है, जो बहुत मुश्किल से किसी जगह पर अपना ठिकाना और उनमें से कुछ लोग घर बनाते हैं मगर इससे ज्यादा तकलीफदेह और क्या हो सकता है कि उन्हें वैसी वजहों के लिए उस जगह को छोड़ कर कहीं और जाना पड़ जाता है, जिसके लिए वे जिम्मेदार नहीं होते हैं। यही नहीं, अपने ठौर से वंचित लोग जब कहीं और जीने की जगह ढूंढने निकलते हैं तो सभ्य कही जाने वाली व्यवस्थाओं वाले लोकतांत्रिक देशों में भी उनके लिए टिकना आसान नहीं होता। इससे अफसोसनाक और क्या होगा कि विश्व के आधुनिक होने के दावों के बीच पिछले दो वर्षों में संघर्ष और हिंसा की वजह से अपना घर छोड़ने पर मजबूर लोगों की संख्या में चिंताजनक बढ़ोतरी हुई है। दुनिया के जिन हिस्सों में हालात में सुधार हो रहे थे, अब वहां भी यह समस्या अपने पांव पसार रही है। हिंसा या संघर्षो को रोकने और शांति की स्थापना करने में नाकामी दरअसल विश्व भर में अशांत इलाकों में सक्षम देशों की कूटनीतिक और रणनीतिक कवायदों के महज दिखावा होने को ही दर्शाती है।
Date:17-04-24
भारत – ईरान संबंधों का भविष्य
ब्रह्मदीप अलूने
ईरान, यूरेशिया और हिंद महासागर के मध्य एक प्राकृतिक प्रवेश द्वार है, जिससें भारत, रूस और यूरोप के बाजारों तक आसानी से पहुंच सकता है। एशिया महाद्वीप की दो महाशक्तियों, भारत और चीन, की सामरिक प्रतिस्पर्धा समुद्री परिवहन और पारगमन की रणनीति पर देखी जा सकती है। चीन की ‘पर्ल आफ स्प्रिंग’ के जाल को भेदने के तौर पर चाबहार बंदरगाह के रूप में अंतत: भारत को सफलता मिल गई है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय राजनीति में ईरान की स्थिति और कूटनीतिक दांव-पेंचों के बीच यह कहा जा सकता है कि भारत की सामरिक और आर्थिक क्षमताओं की असली परीक्षा भी अब शुरू हो रही है।
दरअसल, ईरान एक ऐसा देश है, जो राजनीतिक, कूटनीतिक, आर्थिक और सामरिक प्रतिबंधों का सामना करते हुए अमेरिका विरोधी खेमों से जुड़ने के लिए हमेशा तैयार नजर आता है। 2021 में चीन ईरान के बीच रणनीतिक रिश्तों की शुरुआत हो या मध्यपूर्व में ‘प्राक्सी’ समूहों को मजबूत बनाए रखने की कोशिश, अमेरिका की चुनौतियां ईरान ने बढ़ाई हैं। इस बीच भारत अमेरिकी सहयोग बढ़ा है, हिंद महासागर से लेकर लद्दाख तक, चीन से निपटने के लिए भारत को अमेरिका की जरूरत है, ऐसे में भारत ईरान के संबंधों के दीर्घकालीन समय तक सामान्य बने रहने को लेकर गहरी आशंकाएं हैं।
ईरान चीन की ‘बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव’ का सदस्य है और वह इसे पूर्व और पश्चिम के बीच एक सेतु होने की ऐतिहासिक स्थिति को पुन: स्थापित करने के अवसर के रूप में देखता है। ईरान में परिवहन, बंदरगाहों, ऊर्जा, उद्योग और सेवाओं की विभिन्न परियोजनाओं में चीन अरबों डालर का निवेश कर रहा है तथा वह ईरान का एक मजबूत आर्थिक सहयोगी बनकर उभरा है। ईरान के पास विश्व में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के बड़े भंडार मौजूद है। वह अपना तेल बेचने के लिए भारत को एक बड़े बाजार के रूप में देखता है।
भौगोलिक रूप से दोनों देश निकट हैं, जो इसकी लागत को कम करता है और इससे ईरान की लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था को सहारा मिल सकता है। मगर भारत वैश्विक नियमों में बंधा हुआ एक लोकतांत्रिक और जिम्मेदार देश है, इसलिए भारत ने अमेरिकी प्रतिबंधों को देखते हुए पिछले चार वर्षों से ईरानी तेल का आयात बंद कर दिया है। इससे भारत की ऊर्जा जरूरतें प्रभावित हुई, वहीं ईरान ने भी इसे ठीक नहीं समझा।
अब चाबहार बंदरगाह को लेकर भारत और ईरान के बीच समझौता पूर्ण हो गया है, इसे सामरिक और व्यापारिक दृष्टि से भारत के लिए महत्त्वपूर्ण माना जा रहा है। इसके कई भू-राजनीतिक कारण हैं। चाबहार बंदरगाह परियोजना का विकास भारत ईरान की एक प्रमुख परियोजना है। भारत, ईरान और रूस के मध्य 16 मई 2002 को इस संबंध में एक समझौता हुआ था, जिसके द्वारा ईरान होकर मध्य एशियाई राज्यों तक निर्यात करने के लिए एक उत्तर दक्षिण गलियारे का निर्माण किया जा सके।
ईरान में कैस्पियन सागर पर बने अस्तारा, बंदर अंजाली और अमीराबाद बंदरगाह रूस के अस्ताराखान बंदरगाह से बखूबी जुड़े हैं। अरब सागर के तट पर कराची बंदरगाह, ग्वादर बंदरगाह, कांडला बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह और चाबहार भी हैं। ओमान की खाड़ी में स्थित चाबहार बंदरगाह अब भारत के कब्जे में है। इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित हो गया है कि ईरान के दक्षिण समुद्र तट को भारत के पश्चिमी समुद्र तट से जोड़ने का रणनीतिक दांव कामयाब हो गया है। यहीं नहीं, इस परियोजना में अफगानिस्तान का सहयोग सामरिक संतुलन बनाने में भी मददगार होगा।
ईरान भी इस नए मार्ग को लेकर काफी उत्साहित है, क्योंकि भारत से जो माल पहले पाकिस्तान होते हुए सीधे अफगानिस्तान जाता था वह अब जहाजों के जरिए पहले ईरान के चाबहार बंदरगाह पर जाएगा और फिर वहां से ट्रकों द्वारा अफगानिस्तान पहुंचेगा। चाबहार बंदरगाह के जरिए भारत अफगानिस्तान के साथ ही मध्य एशिया, रूस, पीटर्सबर्ग, मध्य एशिया का ‘लैंड लाक्ड’ इलाके तक जुड़ जाएगा। इस प्रकार इस बंदरगाह से भारत की सामरिक, आर्थिक और भू-राजनीतिक स्थिति बेहद मजबूत होने की संभावना बढ़ेगी।
चाबहार बंदरगाह भारत की आर्थिक ताकत बनने की आशा के प्रतीक के तौर पर भी देखा जा रहा है। गुजरात के कांडला बंदरगाह से केवल छह दिनों में चाबहार पहुंचा जा सकता है। वहां से रेल या सड़क के माध्यम से सामान आगे पहुंचाया जा सकता है। यही लाभ ईरान को भी होगा। भारत को ईरान से तेल, गैस और मध्य एशिया के लिए संपर्क चाहिए, ताकि पाइपलाइन के जरिए गैस लाई जा सके। मगर चाबहार बंदरगाह को लेकर भारत की दीर्घकालीन योजनाएं ईरान की जटिल धार्मिक और वैश्विक नीतियों के चलते कैसे पूरी होंगी, इसको लेकर गहरा असमंजस है।
चाबहार बंदरगाह से भारत को होने वाले फायदों के केंद्र में ईरान, अफगानिस्तान और रूस हैं। ये तीनों देश वर्तमान में कड़े वैश्विक प्रतिबंधों का सामना कर रहे हैं। अमेरिका ने लंबे समय से तालिबान को किसी भी तरह के समर्थन को अपराध घोषित कर रखा है। ऐसे में अफगानिस्तान में काबिज तालिबान और भारत के बीच सहयोग की गुंजाइश बेहद सीमित है। यूक्रेन पर हमले के बाद रूस कड़े अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों का सामना कर रहा है।
अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के साथ-साथ आस्ट्रेलिया, कनाडा और जापान सहित कई देशों ने रूस पर साढ़े सोलह हजार से अधिक प्रतिबंध लगाए हैं। रूसी बैंकों की लगभग 70 फीसद संपत्ति जब्त कर ली गई और कुछ को वित्तीय संस्थानों के लिए ‘हाई स्पीड’ मैसेजिंग सेवा ‘स्विफ्ट’ से बाहर कर दिया गया। अमेरिका और ब्रिटेन ने रूसी तेल और प्राकृतिक गैस पर प्रतिबंध लगा दिया है। यूरोपीय संघ ने समुद्री रास्ते से कच्चे तेल के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है
चाबहार बंदरगाह वाला ईरान भी गंभीर मानवाधिकारों के उल्लंघन और परमाणु बम बनाने की कोशिशों के कारण कई वैश्विक प्रतिबंधों का सामना कर रहा है। फिर, ईरान की कूटनीति और भारत की स्थिति में गहरे अंतर्द्वंद्व और विरोधाभास हैं। ईरान के दो सबसे बड़े शत्रु राष्ट्र अमेरिका और इजराइल भारत के महत्त्वपूर्ण आर्थिक और सामरिक साझीदार हैं। भारत और अमेरिका व्यापक रणनीतिक भागीदार हैं और दोनों के बीच सहयोग व्यापार, रक्षा, बहुपक्षवाद, खुफिया, साइबर स्पेस, नागरिक परमाणु ऊर्जा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा जैसे कई क्षेत्रों में फैला हुआ है।
भारत और इजराइल के बीच गहरे द्विपक्षीय आर्थिक, सैन्य और रणनीतिक संबंध हैं। रूस के बाद इजराइल भारत का दूसरा सबसे बड़ा रक्षा आपूर्तिकर्ता है। दोनों देशों के बीच सैन्य और रणनीतिक संबंध आतंकवादी समूहों पर खुफिया जानकारी साझा करने और संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण तक विस्तारित हैं।
चाबहार बंदरगाह, वैश्विक बाजार में पहुंच बढ़ाने के लिए भारत के लिए बहुत मददगार बन सकता है। मगर ईरान, चीन और रूस के साथ निरंतर आगे बढ़ रहा है। ऐसे में अमेरिका और यूरोप ईरान की ऐसी किसी भी योजना को फलीभूत नहीं होने देंगे, जिसका व्यापक लाभ उसे मिल सके। जाहिर है, चाबहार बंदरगाह के व्यापक फायदों के लिए ईरान में लोकतांत्रिक सरकार, पुतिन का पतन तथा जिनपिंग की साम्राज्यवादी आक्रामक नीतियों जैसे व्यापक परिवर्तनों की जरूरत होगी और इसकी उम्मीद फिलहाल कहीं दिखाई नहीं पड़ती। इसके साथ ही भारत ईरान के साथ सहयोग बढ़ाने को लेकर अमेरिका, इजराइल और यूरोपीय देशों से संबंध बाधित कर ले, इसकी संभावना भी बिल्कुल नहीं है।
सुधरें जांच एजेंसियां
संपादकीय
सर्वोच्च न्यायालय ने प्रबीर पुरकायस्थ को रिहा कर दिया। प्रबीर समाचार वेबसाइट ‘न्यूजक्लिक’ के संस्थापक संपादक हैं, जिन्हें 3 अक्टूबर, 2023 इस आरोप में गिरफ्तार किया गया था कि वह चीन से पैसे लेकर भारत के विरुद्ध दुष्प्रचार करते हैं। उनकी गिरफ्तारी गैर-कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत की गई थी। जाहिर है कि उनके ऊपर लगाया गया आरोप निहायत ही गंभीर था, लेकिन जांच एजेंसियों ने वह गंभीरता नहीं दिखाई जो उन्हें दिखानी चाहिए थी। न्यायालय के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 20, 21 और 22 व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार की सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये अधिकार संविधान के तहत व्यक्ति को प्राप्त सर्वाधिक पवित्र एवं महत्त्वपूर्ण अधिकार हैं, लेकिन पुरकायस्थ की गिरफ्तारी की प्रक्रिया में उनके इसी अधिकार का मनमाने ढंग से अतिक्रमण किया गया। विधिक प्रक्रिया यह है कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए उससे पहले पूरी जांच-पड़ताल करके उसे लिखित तौर पर बताया जाए कि आखिर उसे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। इसी तरह रिमांड देने वाले न्यायिक अधिकारी का भी दायित्व बनता है कि वह सुनिश्चित करे कि जिस व्यक्ति को रिमांड पर भेजा जा रहा है, उसे लिखित में बताया जाए कि उसे रिमांड पर क्यों भेजा जा रहा है। लेकिन जांच एजेंसी ने प्रबीर के मामले में इस बेहद महत्त्वपूर्ण निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया। प्रबीर को बेहद हड़बड़ी में गिरफ्तार किया गया और इस तरह न्याय की मूल अवधारणा के विरुद्ध कार्य किया गया। इसीलिए न्यायालय ने इसी आधार पर कि अभियुक्त को उसकी गिरफ्तारी का आधार नहीं बताया गया, उसकी गिरफ्तारी और रिमांड को अवैध करार दिया और रिहा करने का आदेश दिया। यह आदेश उन सभी जांच एजेंसियों के लिए एक तमाचा भी है, और सबक भी है कि वे किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार तो कर लेती हैं, लेकिन गिरफ्तारी से पहले की जो कार्यवाहीजन्य प्रक्रियाएं होती हैं, उन्हें पूरा नहीं करतीं । परिणामस्वरूप गंभीर आरोपों के अभियुक्तों को भी रिहाई मिल जाती है और जांच एजेंसियों की किरकिरी होती है। उम्मीद की जानी चाहिए कि सर्वोच्च न्यायालय को आगे इस तरह की टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
चाबहार बंदरगाह पर रिश्तों के जहाज
विवेक काटजू , ( पूर्व राजदूत )
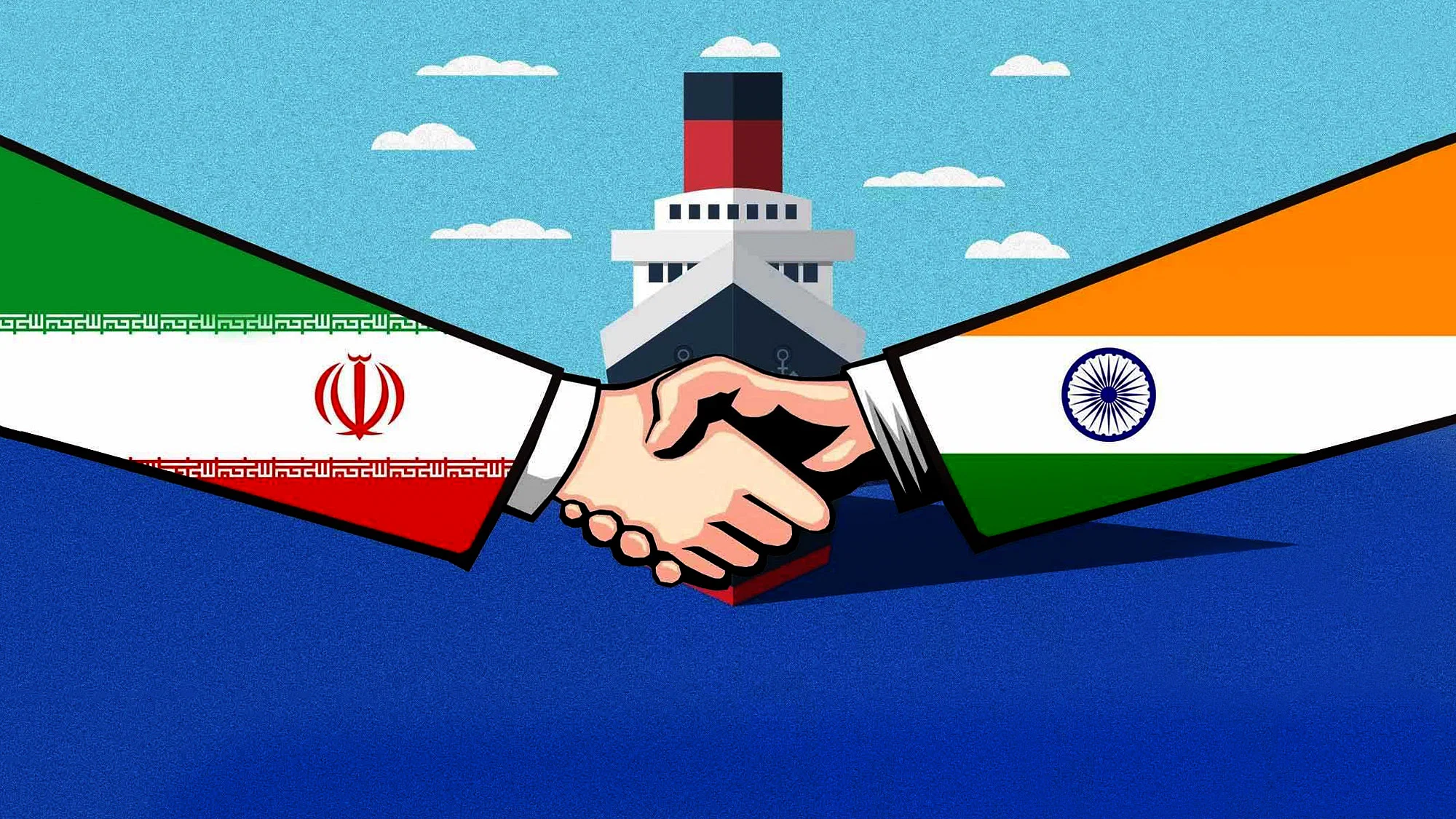
चाबहार बंदरगाह को लेकर भारत और ईरान के बीच हुआ ताजा समझौता काफी अहम है। यह आपसी रिश्ते को तो नई ऊंचाई देगा ही, कनेक्टिविटी की दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा। दोनों देशों के संबंधित मंत्रियों की मौजूदगी में इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड (आईपीजीएल), जो भारत की एक सार्वजनिक कंपनी है और ईरान के बंदरगाह एवं समुद्री संगठन के बीच यह तय हुआ है कि शाहिद बेहेश्ती बंदरगाह-चाबहार के आधुनिकीकरण में भारतीय कंपनी अगले 10 साल में लगभग 37 करोड़ डॉलर खर्च करेगी और उसका प्रबंधन व संचालन भी करेगी। इस रकम में से करीब 12 करोड़ डॉलर की धनराशि बुनियादी ढांचे के विकास में निवेश की जाएगी, जबकि शेष 25 करोड़ डॉलर बतौर कर्ज ईरान को दिया जाएगा।
चाबहार बंदरगाह को विकसित करने की भारतीय मंशा दशकों पुरानी है। यह बंदरगाह ईरान के दक्षिण-पूर्वी तट पर है, जहां से अफगानिस्तान-ईरान सीमा पर स्थित जरांज शहर के जरिये दक्षिणी अफगानिस्तान का पूरा फलक खुल जाता है। आज से 22 साल पहले 2002 में ही वाजपेयी सरकार ने दूरंदेशी दिखाते हुए जरांज से दिलाराम तक सड़क बनाने में अफगानिस्तान की मदद की थी। यह सड़क चाबहार से अफगानिस्तान और अफगानिस्तान के जरिये मध्य एशिया, आगे रूस व यूरोपीय देशों के लिए रास्ता खोलती है। इसके साथ-साथ, ईरान की सहभागिता वाला अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा भी भारत के वाणिज्यिक हितों को आगे बढ़ाने में बड़ी भूमिका अदा करेगा। हमें भूलना नहीं चाहिए कि पाकिस्तान अपने पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के जरिये अफगानिस्तान का मार्ग हमारे निर्यात के लिए कभी नहीं खोलेगा, जबकि इस्लामाबाद व बीजिंग की मंशा अफगानिस्तान को चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे से जोड़ने की भी है, जिसकी कड़ी ग्वादर बंदरगाह से जुड़ी है। ऐसे में, आर्थिक और वाणिज्यिक नजरिये से स्वाभाविक ही चाबहार बंदरगाह का विकास हमारे हित में है। इससे हमारा सामरिक हित भी जुड़ा हुआ है।
शाहिद बेहेश्ती बंदरगाह-चाबहार पर समझौते के बाद अमेरिकी प्रवक्ता ने कहा है कि ईरान से सहयोग करने वालों को वे अमेरिकी प्रतिबंध याद रखने चाहिए, जो वाशिंगटन ने तेहरान पर लगा रखे हैं। अभी हमें यह नहीं पता कि अमेरिकी प्रवक्ता की यह प्रतिक्रिया बस औपचारिक थी या फिर अमेरिकी प्रशासन ने चाबहार की अपनी नीति बदल ली है? दरअसल, 2016 में जब भारत और ईरान के बीच चाबहार को लेकर एक समझौता हुआ था, तब प्रतिबंधों के बावजूद अमेरिका ने यह एलान किया था कि चाबहार के विकास के लिए दिया जाने वाला भारतीय सहयोग प्रतिबंध के दायरे से बाहर रहेगा। लिहाजा, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ठीक ही कहा है कि चाबहार के सहयोग को संकीर्ण नजरिये से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इसका सकारात्मक प्रभाव पूरे क्षेत्र पर पड़ेगा। यह भी मुमकिन है कि भारत और अमेरिका की इस मसले पर परदे के पीछे बातचीत हुई हो, क्योंकि अमेरिकी प्रवक्ता के बयान में तल्खी नहीं थी। संभावना यह भी है कि घरेलू दबाव के चलते अमेरिका ने यह बयान दिया हो, क्योंकि इस साल वहां पर राष्ट्रपति चुनाव होने वाला है और बाइडन प्रशासन ने ईरान के प्रति काफी कड़ा रुख अपनाया है।
बहरहाल, ईरान पश्चिम एशिया का एक बड़़ा देश है। भारत के साथ उसके राजनीतिक संबंध और आधुनिक काल में, विशेषकर ऊर्जा के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग दोनों देशों के लिए लाभदायक रहे हैं। हालांकि, सच यह भी है कि अमेरिकी प्रतिबंधों के चलते कई भारतीय कंपनियों ने ईरान से दूरी बनाए रखी थी। वे वहां निवेश करने से तो बचती ही थीं, ईरानी कंपनियों के साथ साझेदारी से भी हिचकती थीं, क्योंकि उनको डर था कि ऐसा करने से अमेरिकी कंपनियों से उनका रिश्ता या अमेरिका में उनका संचालन प्रभावित हो सकता है। भारत सरकार ने भी ईरान के साथ अपने संबंधों को आगे बढ़ाने में अमेरिकी प्रतिबंधों को ध्यान में रखा है। हां, चाबहार समझौता एक अपवाद रहा। आज भी भारत-ईरान के आर्थिक और वाणिज्यिक संबंधों में अमेरिकी प्रतिबंधों का नकारात्मक प्रभाव हम आसानी से देख सकते हैं, क्योंकि भारत के चहुंमुखी हित ईरान की तुलना में अमेरिका से कहीं अधिक जुड़े हैं। फिर भी, इसका यह मतलब नहीं कि तेहरान और नई दिल्ली अपने रिश्ते आगे न बढ़ाएं। कुछ न कुछ रास्ता तो ढूंढ़ना ही पड़ता है और यही कूटनीति की चुनौती भी होती है कि एक बड़ी शक्ति अमेरिका के प्रतिबंधों से कैसे निपटा जाए?
इस पूरे मसले का एक पहलू यह भी है कि भारत के पश्चिम एशियाई देशों से गहरे हित जुड़े हैं। सामरिक और सुरक्षा के नजरिये से इजरायल नई दिल्ली के लिए अहम है, तो खाड़ी के देश हमारी ऊर्जा-सुरक्षा के लिए जरूरी हैं। अरब देशों के साथ हमारा व्यापारिक संबंध काफी मजबूत है और लाखों भारतीय वहां काम करते हैं, जिनके द्वारा स्वदेश भेजी गई रकम हमारी अर्थव्यवस्था को फायदा पहुंचाती है। भारत की पारंपरिक नीति यही थी कि वह पश्चिम एशिया की अंदरूनी राजनीति से दूर रहे। यहां के हरेक देश के साथ वह अपने संबंध आगे बढ़ाता रहा है। मगर बीते कुछ वर्षों से इस नीति में बदलाव देखने को मिल रहा है। जिस तरह से अमेरिका ने खाड़ी के कुछ देशों, खासकर यूएईके साथ इजरायल के रिश्ते बढ़ाने में परदे के पीछे से मदद की, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यूएई के सदर और अबू धाबी के शासक मोहम्मद बिन जायेद से अपने निजी रिश्ते भी मजबूत किए हैं। कुछ महीने पहले प्रधानमंत्री ने अमीरात का सफल दौरा भी किया था, जब वहां एक भव्य मंदिर का उद्घाटन हुआ था। स्वाभाविक है, इन घटनाओं को तेहरान में तीखी नजर से देखा जा रहा हो? ऐसे में, हम यह कह सकते हैं कि ताजा समझौते के जरिये भारत ने ईरान और इस क्षेत्र को एक संकेत दिया है कि वह अपनी पश्चिम एशिया की नीति में संतुलन बनाना चाहता है, जो उचित भी है।
उल्लेखनीय है कि ऐसे समझौते अमूमन चुनाव के बीच नहीं होते हैं। मगर इसका दूसरा पहलू यह है कि ईरान को विश्वास है, भारत और उसके हित को हर भारतीय सरकार आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। इतना ही नहीं, वह यह भी जानता है कि भारत की नजर चीन-ईरान-पाकिस्तान रिश्तों पर भी रहती है और ईरान जैसे महत्वपूर्ण देश में चीन और पाकिस्तान को भारत खुली छूट नहीं दे सकता है।