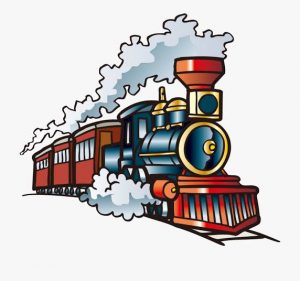17-01-2020 (Important News Clippings)
To Download Click Here.
Conditional welcome for private trains
Editorials
NITI Aayog, the Centre’s think tank, has put out a notable discussion paper for private sector participation in passenger trains across a hundred routes nationally, which can indeed be path-breaking. But the way forward, surely, is to have an independent regulatory body for investor comfort, with the specific mandate to set standards, enhance competition and oversee fair access to rail infrastructure.
The paper envisages that private operators would ply over 150 trains, with indicative investment of over Rs 22,500 crore. A two-stage bidding process is proposed, with gross revenue share the sole bid parameter. Concessionaires would get flexibility in train class composition and halts, with fixed haulage charges pre-specified in bidding documents including terminal charges, track maintenance and signalling costs. The paper promises a transparent and non-discriminatory system for dispatch and movement of trains. Further, third-party vetting by an independent safety assessor is called for.
However, this cannot work without independent and empowered regulation. It remains to be seen how and to what extent the Railways add to track capacity and signalling to accommodate expensive private trains: the move can lead to heightened congestion right across the board without stepped-up infrastructural investments along dense routes. The Railways have invited private participation in the past, for example, in the Own Your Wagon scheme of 1992, a subsequent Special Freight Train Operator scheme, and the Dedicated Freight Corridor project of 2005. But they all led to quite suboptimal results, and poor investor response, thanks to policy uncertainty and the general lack of a level playing field sans independent regulation. A change of track is clearly warranted.
Date:17-01-20
Amazon’s welcome move on small biz
ET Editorials
Commerce minister Piyush Goel is spot on: Amazon is not investing in India to do India a favour. But then, do we expect hard-headed businessmen to commit large sums of money to any project anywhere in the world as a favour? They seek profits. That is an entirely honourable motive. Workers queue up to be hired, because they want to earn a wage, the higher the better. Banks compete to lend to businesses, to make profits. In the process of businesses investing, hiring workers and taking credit, jobs get created, savers’ deposits find profitable deployment, some consumer want or need is met, and the government gets direct and indirect taxes. That is the whole point about the invisible hand of the market that Adam Smith described: people pursue their own individual interests but advance collective welfare in the process.
Where markets fail, the State steps in. The Competition Commission of India has launched an investigation into the fairness of ecommerce operations. This is all to the good. Amazon and Walmart-owned Flipkart should welcome it as something that would build public confidence in the fairness of what they do. As Kishore Biyani of the Future Group says, online and physical retail might look very different today, but are likely to converge to produce hybrid models that benefit both in a few years’ time. In the meantime, the kind of engagement that Amazon promises with India’s small and medium businesses could do wonders for this most dynamic segment of Indian industry. If Amazon enables them to sell online, they would get organised and formalised, qualify for bank credit, pay their taxes regularly and pay their employees’ statutory dues and still be better off than in the informal past, because their cost of credit would be a fraction of what it would be when drawn from informal sources.
Jeff Bezos probably underestimates the additional exports he would be able to catalyse by bringing one crore Indian small and medium businesses on to its online platform. When Amazon makes a foray, can Walmart and Reliance be far behind? Together, they would do wonders.
किसान को मिली सामूहिक सौदेबाजी की क्षमता
संपादकीय
डिजिटल टेक्नोलॉजी को शहर ही नहीं, गांव के घर-घर तक पहुंचाना प्रधानमंत्री की व्यक्तिगत देन है। इसका लाभ आमजन को सरकारी सहायता के सीधे अकाउंट में और वह भी तेज़ एवं भ्रष्टाचार-शून्य तरीके से होने से हुआ। कालेधन का भी प्रसार रुका। लेकिन, ताज़ा खबर यह है कि किसान सरकार से मिलने वाली नकद राशि से इतने सक्षम तो हो ही रहे हैं कि सही कीमत न मिलने तक अब उनमें अपने उत्पाद को रोके रखने की क्षमता विकसित हो गई है। इसका पता तब चला जब प्याज की लगातार बढ़ती कीमतों से परेशान सरकार ने जमाखोरों पर सख्ती के लिए पुलिस व आयकर विभाग से भी छापे डलवाए, लेकिन प्याज का एक टुकडा भी वैध मात्रा से अधिक नहीं मिला। यानी प्याज देश के किसानों के पास था और वे पिछले साल की तरह गिरते भाव पर नहीं बेचना चाहते थे। यह संभव हुआ कैश-ट्रांसफर और किसान सम्मान निधि से मिलने वाले पैसे के कारण। दूसरा ताज़ा उदाहरण है सोयाबीन का। अचानक इसका रेट फसल के मंडी आने के साथ ही केंद्र द्वारा निर्धारित 3710 रुपये प्रति कुंतल के न्यूनतम समर्थन मूल्य से ऊपर 4250 रुपए पर पहुंच गया। केन्द्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री ने गत 7 जनवरी को जमाखोरों को आगाह किया, लेकिन जांच में पता चला कि किसान अपना सोयाबीन अभी बाज़ार में अच्छी कीमत के इंतजार में नहीं निकाल रहा है। हाल में दूध के दाम बढ़ने पर भी किसानों को लाभ मिला, क्योंकि भारत में 65 प्रतिशत किसान खेती के साथ छोटी या बड़ी डेयरी भी रखता है। यहां ध्यान देने की बात यह है कि दूध का व्यापार किसानों का अपना सहकारी संघ करता है, लिहाज़ा दूध की कीमत में होने वाले हर एक रुपये की वृद्धि पर किसानों को 70 पैसे मिलते हैं। जबकि, सब्जी, अनाज पर केवल 30 पैसे किसान की जेब में जाते हैं। स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि किसान अपनी पैदावार का दाम तय करने में अपनी बड़ी भूमिका रखेगा। सरकार को भी सोचना होगा कि मंडी-सिस्टम की शोषणकारी व्यवस्था की जगह गांवों में ही ऐसी व्यापार इकाइयां बनाएं। इस ताकत के पीछे किसानों का आपस में व्हाट्सअप के जरिये ग्रुप तैयार करना भी है, जिससे उनमें सामूहिक सौदेबाजी की क्षमता का विकास हुआ है। किसान मजबूत होगा तो डिमांड बढ़ेगी, औद्योगिक उत्पादन बढ़ेगा, नौकरियां मिलेंगीं और वर्तमान संकट ख़त्म होगा।
Date:17-01-20
विद्यार्थियों के नारों की ताकत को कम न आंकें
एक सत्तावादी और निर्दयी शासन के खिलाफ कविता व गीत ही सबसे ताकतवर हथियार हैं
प्रीतीश नंदी, (वरिष्ठ पत्रकार व फिल्म निर्माता)
प्रख्यात शायर फैज अहमद फैज की मृत्यु के 15 महीने बाद उनकी 75वीं जयंती पर 13 फरवरी 1986 को लाहौर के अलहमरा आर्ट काउंसिल में आयोजित कार्यक्रम में प्रसिद्ध गायिका इकबाल बानो काली साड़ी पहन कर आईं। जिया-उल-हक के शासन में काला रंग विरोध और साड़ी गैर-इस्लामी मानी जाती थी। उन्होंने यहां पर मौजूद 50 हजार लोगों के सामने फैज की सबसे यादयार कविता ‘हम देखेंगे’ को गाया। उस समय फैज की कविताओं को सार्वजनिक रूप से गाने पर रोक थी और ‘हम देखेंगे’ तो 1979 में तब लिखी गई थी, जब जिया सत्ता के शीर्ष पर थे। यह एक ऐसे शायर की ओर से स्पष्ट ललकार थी, जिसने अपनी सारी जिंदगी प्रेम और सामाजिक न्याय की जरूरत की बातें करते हुए बिता दी थी। उनके शब्दों ने लाखों लोगों को राजनीतिक उत्पीड़न और तानाशाही के खिलाफ खड़ा कर दिया था। उनकी यह कविता पहली बार उनकी किताब ‘मेरे दिल मेरे मुसाफिर’ में प्रकाशित हुई और इसने तुरंत ही युवाओं को सत्ता के दमन के खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रेरित किया।
लाहौर के ऑडिटोरियम में जब इकबाल बानो की आवाज में ‘हम देखेंगे’ की पहली लाइन को गाया गया तो वहां एकदम शांति थी और उसके बाद चकित श्रोताओं ने तालियों की गड़गड़ाहट से इस शांति को भंग कर दिया। यह राजनीति को ललकार का एक ऐसा काम था, जो इस महाद्वीप के लोगों की यादों में हमेशा रहेगा। इस एक आश्चर्यजनक क्षण में इकबाल बानो ने इस कविता को एक कभी न भूलने वाले विरोध गान में बदल दिया था और यह उस समय के शासन को खुली चुनौती थी। जैसे-जैसे उन्होंने बिना डरे इसे गाना जारी रखा, तालियां और तेज हाेती चली गईं। कई बार तो उन्हें आगे गाने के लिए तालियों की आवाज के शांत होने तक रुकना पड़ता था। इन्हीं क्षणों में यह गीत दुनियाभर में सभी दमनकारी शासकों के खिलाफ विरोध का बैनर बन गया। स्टेज पर दिखाया गया यह जोश आज भी दुनियाभर में युवाओं के लिए प्रेरणा है। जिस रात पुलिस ने फैज के घर पर छापा मारा था तो उन्हें वहां इस गीत की एक भी रिकॉर्डिंग नहीं मिली थी, लेकिन एक रिकॉर्डिंग तो निश्चित तौर पर थी, जो पुलिस के वहां पहुंचने से बहुत पहले ही बाहर भेजी जा चुकी थी। फैज के जाने के करीब 35 साल बाद आज जिया को कोई याद भी नहीं करता। लेकिन, सेल फोन और वायरल मीडिया के इस दौर में भी ‘हम देखेंगे’ युवा विद्यार्थियों के लिए विरोध, साहस और प्रेरणा का कभी न भूलने वाला गीत बना हुआ है। यह हमें याद दिलाता है कि कोई भी राजनीति महान कविता को मिटा नहीं सकती। वह कविता जो लोगों को विरोध में खड़ा होने व आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है।
मैंने ढाका में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भी ऐसा होते देखा था। जब पाकिस्तानी सेना ने युवा विद्यार्थियों की आवाज दबाने की कोशिश की तो उन्होंने भी विरोध के अपने प्रिय कवि शमसुर्रहमान की कविताओं को कैंपस में गाना शुरू कर दिया था। लेकिन, कोई भी बंदूक बंगाली में स्वाधीनता व उर्दू में आजादी के उनके नारों को बंद कराने मंे कामयाब नहीं हो सकी। यह एक शब्द है, जिसको दुनियाभर के कवियों ने अनेक अर्थ दिए हैं। इसीलिए मुझे उस समय जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ जब पिछले महीने देश के प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों में से एक, कानपुर आईआईटी में मैंने जामिया मिलिया विश्वविद्यालय के छात्रों पर पुलिस के हमले के विरोध में विद्यार्थियों को ‘हम देखेंगे’ गाते हुए देखा।
फैज की यह कविता आज ललकार का गीत है। यह वह गीत है, जो अधिनायकवादी शासन से लड़ रहे सभी लोग गा रहे हैं। और यह बात कोई मायने नहीं रखती कि इसे पाकिस्तान के एक वामपंथी कवि ने लिखा था। भाषा हम सबकी है। दुनिया भर के युवा विद्यार्थियों को परिभाषित करने वाले दो गुणों विरोध और ललकार वाला है यह गीत। कुछ मूर्ख लोग (जो आज बहुत अधिक हैं) इस कविता को हिंदू विरोधी व देश विरोधी साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। यह दाेनों में कुछ भी नहीं है। यह एक सत्ता विरोधी, क्रूरता विरोधी और फासिस्ट विरोधी है। विद्रोह के बीज तो दमन की राजनीति की उपजाऊ जमीन पर ही अंकुरित होते हैं और यही वजह है कि दुनिया की बेहतरीन कविताएं उन्हीं देशों से आईं जो मुश्किल में थे। चिली के पाब्लो नेरुदा इसके उदाहरण हैं। लेकिन, विरोध करने वाले सभी कवि वामपंथी नहीं हैं। नोबेल पाने वाले मेक्सिको के ओक्टावियो पाल ने कम्युनिस्ट शासन के दमन के खिलाफ उतनी ही मजबूती से आवाज उठाई, जितने जोरदार तरीके से क्यूबा के निकोलस गुईल्लेन कास्त्रो शासन का समर्थन कर रहे थे। भाकपा के सदस्य और बंगाल के बेहतरीन कवियों में से एक सुभाष मुखोपाध्याय ने उन युवाओं पर कविताओं की एक किताब लिखी, जो अपनी पढ़ाई छोड़कर नक्सलबाड़ी आंदोलन में शामिल हो गए थे। उनकी पार्टी ने इस किताब को स्वीकृति नहीं दी, लेकिन मुखोपाध्याय युवाओं के आदर्श बन गए। आज जब किसानों की आत्महत्या कई गुना बढ़ गई है तो हमें नक्सलबाड़ी जाने वाले उन युवाओं को याद करना चाहिए, जिन्होंने पहली बार बताया था कि कृषि की हालत कितनी खराब है।
मैंने सालों से विद्रोही छात्रों को प्रेरणा देने वाले आंदोलनों को देखा है। यही वह आजादी है, जो वे मांगते हैं: पाखंड से आजादी। झूठ से आजादी। राजनीतिक कुतर्कों व दोमुंही बातों से आजादी। राष्ट्रवाद पर खोखले भाषणांे से आजादी। इसे ही वे आजादी कहते हैं। इसी आजादी के जेएनयू के युवा नारे लगाते हैं। इसकी ताकत को कभी कम न आंकें। यही है, जिसे कभी हमारे स्वतंत्रता के लिए संघर्ष के रूप में परिभाषित किया गया था। यह आज हमारे उस शासन के खिलाफ संघर्ष को परिभाषित करता है, जो यह नहीं समझती कि इस देश के लोग क्या चाहते हैं।
Date:17-01-20
दलित मुस्लिम गठजोड़ की नई पहल
बद्री नारायण, (लेखक गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान, प्रयागराज के निदेशक हैं)
नागरिकता संशोधन कानून के विरोध के बीच दलित-मुस्लिम एकता की पहल नए सिरे से होती दिख रही है। दलित एवं मुस्लिम सामाजिक समूहों के बीच राजनीतिक गठबंधन की कोशिश नई नहीं है। दलित राजनीति के एक अनोखे व्यक्तित्व जोगेंद्र नाथ मंडल ने ऐसा ही प्रयास आजादी के पहले किया था। मंडल पूर्वी बंगाल के लोकप्रिय दलित नेता के रूप में आजादी के पूर्व उभरे थे। वह अंग्रेजों के विरुद्ध चल रहे आजादी के आंदोलन में भी सक्रिय रहे। वह आंबेडकर द्वारा स्थापित शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन में सक्रिय थे। बाद में वह मुस्लिम लीग में शामिल हो गए।
वह मोहम्मद अली जिन्ना के बहुत करीबी थे। आजादी के बाद जब भारत का विभाजन हुआ तो वह संयुक्त पाकिस्तान के कानून मंत्री बने। कुछ समय बाद ही वह वहां की व्यवस्था एवं शासन पद्धति में कुछ खास समूहों और विशेष कर दलितों के लिए उपेक्षा की प्रवृत्ति का अहसास करने पर पाकिस्तान छोड़कर भारत लौट आए।
जोगेंद्र नाथ मंडल ने संविधान सभा के चुनावों में दलित-मुस्लिम गठबंधन बनाने का सफल प्रयास किया था। बाबा साहब भीमराव आंबेडकर जब संविधान सभा का चुनाव नहीं जीत पाए तो जोगेंद्र नाथ मंडल ने उन्हें बंगाल के दलित आबादी वाले चुनाव क्षेत्र से चुनाव लड़ने का आमंत्रण दिया। आंबेडकर ने इसे स्वीकार किया। इस प्रकार आंबेडकर दलित-मुस्लिम गठजोड़ की बदौलत ही संविधान सभा में पहुंच पाए।
हालांकि आजादी के बाद दलित एवं मुस्लिम अलग-अलग कांग्रेस को चुनावी समर्थन देते रहे, किंतु इसे दलित-मुस्लिम गठजोड़ बनाने के मौजूदा प्रयासों के रूप में नहीं देखा जा सकता। कांग्रेस में दलित एवं मुस्लिम समाज के अपने-अपने प्रतिनिधि थे। उन नेताओं की प्रतीकात्मक शक्ति से दलितों एवं मुस्लिमों का एक बड़ा वर्ग कांग्रेस को वोट देता रहा। आंबेडकर द्वारा बनाई गई रिपब्लिकन पार्टी को भी मुसलमानों के एक छोटे वर्ग का समर्थन मिलता रहा, किंतु समग्र रूप से मुस्लिमों और दलितों का समर्थन कांग्रेस को छोड़कर शायद ही किसी को मिला हो।
आज के अनेक दलित एवं मुस्लिम नेता भारतीय चुनावी राजनीति में दलित-मुस्लिम गठबंधन बनाने का प्रयास कर रहे हैैं। बसपा नेता मायावती ने 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में दलित-मुस्लिम गठजोड़ बनाने की कोशिश की। उन्होंने उस चुनाव में बड़ी संख्या में मुस्लिम उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारा, फिर भी बसपा अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। उनका शायद यह मानना रहा होगा कि मुस्लिम समाज के उम्मीदवारों को ज्यादा टिकट देकर उन्हें चुनावी रूप से अपने साथ लाया जा सकता है, लेकिन उनका यह राजनीतिक अनुमान गलत साबित हुआ।
उन्होंने यह समझने में भूल की कि सामाजिक समूह ‘नीर-क्षीर’ की तरह जब चाहे, जैसे चाहे नहीं मिल जाते। इसके लिए आधार तल पर सामाजिक सहभागिता, सामाजिक भाईचारा एवं राजनीतिक गोलबंदी बनाने की कोशिश करनी पड़ती है। जिस प्रकार मायावती ने अगड़ी एवं दलित जातियों में सामाजिक इंजीनियरिंग करते हुए सामाजिक भाईचारा बनाने का सघन प्रयास किया था वैसा दलित एवं मुस्लिम गठजोड़ बनाने के लिए नहीं कर पाईं।
इधर भीम सेना के नेता चंद्रशेखर आजाद ने दलित-मुस्लिम गठजोड़ बनाने के एजेंडे पर काम करना प्रारंभ किया है। उनके मुताबिक दलित-मुस्लिम गठजोड़ ही भारतीय राजनीति का भविष्य है। चंद्रशेखर के अलावा एआइएमआइएम के नेता असद्दुदीन ओवैसी ने भी अपने राजनीतिक विमर्श एवं चुनावी रणनीति में दलित-मुस्लिम गठजोड़ को महत्व देना प्रारंभ किया है। कहीं-कहीं उन्हें इस दिशा में आंशिक सफलता भी मिली है, फिर भी बड़े स्तर पर दलित-मुस्लिम गठजोड़ अभी तक विकसित नहीं हो पाया है।
इसके कई कारण है। एक तो दलित राजनीति दलित सामाजिक अस्मिता की अंत:शक्ति पर आधारित है। वहीं दूसरी ओर मुस्लिम राजनीति बहुत कुछ धार्मिक अस्मिता से बंधी है। दो विभिन्न अस्मितापरक विशिष्टता वाले समूहों में राजनीतिक गठबंधन बनने के लिए अस्मितापरक विमर्शों में परिवर्तन की जरूरत तो पड़ेगी ही। एक तथ्य यह भी है कि मुस्लिम राजनीति लंबे समय तक मुस्लिम समुदाय के उच्च वर्ग यथा अशराफ समूह के प्रभाव में रही है। अब धीरे-धीरे अजलाफ एवं पसमांदा समूह अपनी राजनीतिक शक्ति विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जब इन मुस्लिम सामाजिक समूहों में एक राजनीतिक वर्ग उभर आएगा तो इनका दलित राजनीति के साथ सहज रिश्ता बन सकता है।
दलितों एवं मुस्लिमों को कई सामाजिक अध्ययनों में कई जगह पर सांप्रदायिक दंगे के समय में आपस में टकराने वाले सामाजिक समूह के रूप में अंकित किया जाता है। हालांकि टकराहट, संघर्ष एवं दंगे के दिनों में इन दोनों समुदायों की ओर से अपने लिए सुरक्षा तलाशने के प्रयास की अनेक घटनाएं मिल जाती है लेकिन ऐसी घटनाएं हमारे राजनीतिक वृतांत के निर्माण में हाशिये पर ही रहती है।
हमें यह भी देखना होगा कि अगर ऐसा गठजोड़ मात्र नेताओं का गठजोड़ होता है तो वह क्षणिक ही होगा और उसका प्रभाव क्षेत्र में भी कम होगा, किंतु यदि यह गठजोड़ दोनों समूहों की जनता का होता है तो वह भारतीय राजनीति का प्रभावी गठजोड़ साबित होकर उभरेगा। देखना यह भी है कि ऐसा गठजोड़ अखिल भारतीय स्वरूप ले पाता है या क्षेत्रीय स्तरों पर चुनावी रणनीति के एजेंडे में ही सीमित होकर रह जाता है? चूंकि ऐसा गठजोड़ विकसित करने का प्रयास कर रहे दलित एवं मुस्लिम आधारों वाले राजनीतिक दलों का प्रभाव क्षेत्र अभी क्षेत्रीय स्तरों पर ही सीमित है ऐसे में दलित-मुस्लिम गठजोड़ राष्ट्रीय स्तर पर विकसित होने की संभावना कम ही दिखती है। अगर यह गठजोड़ विकसित भी होता है तो यह क्षेत्रीय स्तर पर ही सीमित होकर रह जाएगा।
बहुसंख्यकवादी एजेंडे से कमजोर होगा देश
श्याम सरन, (लेखक पूर्व विदेश सचिव और सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च के सीनियर फेलो हैं)
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के छात्रों और शिक्षकों के खिलाफ गत 5 जनवरी को जो हिंसा की गई, उसे अंजाम देने वालों ने भले ही नकाब पहन रखे थे लेकिन उनका राजनीतिक और वैचारिक रुझान छिप नहीं सका। दरअसल यह हमला शैक्षणिक संस्थानों, नागरिक समाज और अल्पसंख्यकों को सोचा समझा संदेश था कि यदि वे भारतीय राज्य और समाज के नए बन रहे बहुसंख्यक ढांचे का विरोध करेंगे तो उनका यही हश्र किया जाएगा।
जेएनयू में जो हुआ वह पहले जामिया और उसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में घटी घटनाओं का विस्तार था। जामिया और अलीगढ़ के बाद इन घटनाओं ने समूचे उत्तर प्रदेश को अपनी चपेट में ले लिया था। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) का विरोध करने वालों से बदला लिया जाएगा। इन सभी घटनाओं में यह देखा गया कि लोगों की संपत्ति और उनके जीवन की रक्षा के लिए बनी सरकारी मशीनरी हिंसा भड़कने पर खामोश बनी रही।
खासकर उन लोगों के खिलाफ हुई हिंसा में जो सत्ता के वैचारिक और राजनीतिक एजेंडे के खिलाफ हैं। असहमति को लेकर सरकार की प्रतिक्रिया में एक तरह की निष्ठुरता देखने को मिली जो परेशान करने वाली है। हालिया अतीत में हमने देखा है कि इस तरह का ध्रुवीकरण राजनीतिक लाभ दिला सकता है। परंतु यह एक खतरनाक खेल है जो देश के भविष्य पर बुरा असर डाल सकता है।
धार्मिक और वैचारिक आधार पर हो रहा धु्रवीकरण अक्सर एक दूसरे में गुंथ जाता है। मुस्लिम अल्पसंख्यक वर्ग और वाम धड़े को एक साथ राष्ट्रीय हित के खिलाफ माना जा रहा है। जामिया और एएमयू में और बाद में समूचे उत्तर प्रदेश और जेएनयू में जिस तरह कानून व्यवस्था कायम करने वाली मशीनरी का रुख समझौतापरक रहा वह आगे चलकर मोदी सरकार के समक्ष प्रतिरोध बढ़ाएगी। गैर भाजपा शासित राज्यों में ऐसा प्रतिरोध जोर पकड़ेगा। यह हो रहा है और सरकार के लिए बेहतर यही होगा कि वह इस समस्या से समझदारी से निपटे। यदि वह ऐसा नहीं करती है तो इससे विपक्ष का विस्तार होगा और कुछ तत्त्व प्रतिक्रिया स्वरूप हिंसा का सहारा भी ले सकते हैं। तब सुरक्षा की दृष्टि से बल प्रयोग बढ़ाना अनिवार्य हो जाएगा। इस दौरान नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों पर भी रोक लगेगी।
खतरा यह है कि इस प्रक्रिया में देश का लोकतंत्र खतरे में पड़ेगा। यदि असहमति और ङ्क्षहसा इसी प्रकार बढ़ती रही तो यह एक बड़ी त्रासदी होगी। इससे हिंसा बढ़ेगी और देश बाहरी ताकतों के समक्ष कमजोर पड़ेगा। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि अतीत में चीन ने पूर्वोत्तर की अशांति का इस्तेमाल करते हुए भारत की सुरक्षा को कमजोर किया। पाकिस्तान ने पंजाब और कश्मीर में राजनीतिक अशांति का लाभ लिया। यदि देश के हृदयस्थल में राजनीतिक संकट उत्पन्न होता है तो देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को सबसे बड़ा खतरा उत्पन्न होगा। सीमाओं की सुरक्षा की चुनौती तब और बढ़ेगी।
वाम चरमपंथ से निपटने का उदाहरण भी हमारे सामने है जहां राज्य सत्ता द्वारा अत्यधिक बल प्रयोग के बावजूद केवल सीमित सफलता हासिल हुई। राज्य द्वारा हथियारबंद दमन हिंसा फैलाने वालों तक ही सीमित नहीं रहता। अपनी प्रकृति के अनुसार ही यह एक बड़ी आबादी को अपनी चपेट में ले लेता है। इससे हिंसक प्रतिरोध कम होने के बजाय बढ़ता है। ऐसी अशांति को खत्म करने के लिए हमेशा संवाद ही काम आया है और यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया से ही संभव हुआ।
जम्मू कश्मीर का संवैधानिक दर्जा बदलने के बाद लगातार छठे महीने एक तरह की बंदी लागू है। ऐसे में देश के अन्य हिस्सों में संभावित घटनाक्रम को लेकर सचेत होने की आवश्यकता है। असंतोष को वैमनस्य में बदलने देना समझदारी नहीं होगा।
सरकार के भीतर यह अनकहा भरोसा विद्यमान है कि उसके बहुसंख्यकवादी एजेंडे का अंतरराष्ट्रीय नीति पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा। भारत एक बड़ी शक्ति और तेजी से विकसित होती अर्थव्यवस्था वाला देश है। वह अपने मित्रों और शत्रुओं दोनों जगह आलोचना करने वाली आवाज को खामोश करने की ताकत रखता है। यह भरोसा गलत है। पहली बात तो यह कि भारतीय अर्थव्यवस्था को राजनीतिक उथलपुथल से बचाया नहीं जा सकता है।
अल्पसंख्यकों की बढ़ती नाराजी और क्रोध इस पर अपना असर डालेंगे। अर्थव्यवस्था की मौजूदा मंदी देश के विभिन्न हिस्सों में बढ़ती अशांति के असर में और गंभीर होगी। ऐसे में विदेशी निवेशकों के रुझान पर नकारात्मक असर होगा। ऐसे में हमारे लिए कूटनयिक गुंजाइश भी कम होगी।
भारत ने बीते सात दशक में बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक और बहुभाषी विविधतापूर्ण लोकतंत्र के रूप में जो राजनीतिक पूंजी जुटाई है उसके लिए भी कतई सराहना की कोई भावना नहीं है। व्यापक आर्थिक और सैन्य क्षमताओं से जो क्षमता हासिल हुई है उसे बल प्रदान करने का काम हमारा सांस्कृतिक और सामाजिक प्रभाव करता है। प्रधानमंत्री मोदी के दूसरे कार्यकाल के आरंभ के बाद घटी घटनाओं जिनमें कश्मीर का संवैधानिक दर्जा बदलना, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण संबंधी निर्णय और अब सीएए शामिल है, ने देश के बाहर एक नकारात्मक अवधारणा बनाने का काम किया है।
जेएनयू जैसी घटनाएं इस छवि को और बिगाड़ेंगी। दूसरे देशों के नागरिक समाज और मीडिया से भारत पर दबाव आ सकता है। इसके साथ ही वे हमारे मित्र और शत्रु देशों की सरकारों को यह अवसर प्रदान करेंगी कि वे भारत की कीमत पर लाभ ले सकें। इससे भी हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा उत्पन्न होगा।
एक विभाजित देश, असुरक्षित भी होता है। जबकि विविध लोगों से बना एकजुट देश एक समावेशी राष्ट्र का निर्माण करता है। मौजूदा राजनीतिक प्रतिष्ठान के नेतृत्वकर्ता चाहे वे केंद्र के हों या राज्य के, उन्हें यह समझना होगा कि उनकी विभाजनकारी नीतियां देश की राष्ट्रीय सुरक्षा और बेहतरी के खिलाफ खतरनाक हो सकती हैं। उन्हें यह समझना होगा कि उनकी नीतियां देश के अल्पसंख्यकों, नागरिक समाज और कारोबारी जगत के मन में गहरा भय और आशंका पैदा कर रही हैं। सरकार को उन्हें आश्वस्त करना होगा। यदि ऐसा नहीं किया गया तो भारत धीमी पड़ती अर्थव्यवस्था से निपटने और जटिल और तेजी से बदलते भूराजनीतिक परिदृश्य में प्रभावी नहीं रह जाएगा।
केरल सरकार न्यायालय में
संपादकीय
माकपा नेतृत्व वाली केरल सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को उच्चतम न्यायालय में चुनौती देने का अर्थ है कि वामपंथी पाÌटयां हर सूरत में इसे खत्म करना चाहती हैं। केरल सरकार ने अपनी पहली विधानसभा बैठक में ही इसे वापस लेेने का प्रस्ताव पारित कर दिया। इसके पहले संसद द्वारा पारित किसी कानून को वापस लेने का प्रस्ताव किसी विधानसभा में पारित नहीं हुआ था। वैसे तो उच्चतम न्यायालय में सीएए के खिलाफ ६० से अधिक याचिकाएं लंबित हैं‚ लेकिन केरल की याचिका थोड़ी अलग है। अन्य सभी जनहित याचिकाएं हैं जबकि केरल की याचिका केंद्र के खिलाफ मूलवाद है‚ जो अनुच्छेद १३१ के तहत दाखिल की गई है। अनुच्छेद कहता है कि राज्य व केंद्र के बीच किसी भी विवाद‚ चाहे कानून से संबंधित हो या तथ्यों पर आधारित‚ की सुनवाई उच्चतम न्यायालय करेगा। इससे इसकी प्रकृति अन्य याचिकाओं से भिन्न हो जाती है। केरल सरकार ने याचिका में इस कानून के साथ पासपोर्ट कानून व फॉरनर्स एमेंडमेंट ऑर्डर में संशोधनों को भी चुनौती दी है। हालांकि तर्क वही है जो अन्य याचिकाओं में है। मसलन‚ सीएए व्यक्ति की धाÌमक पहचान पर आधारित है‚ इसलिए पंथनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। इसका कहना है कि न्यायालय भी अपने कई पूर्ववर्ती फैसलों में संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा घोषित कर चुका है। जरूरी नहीं कि उच्चतम न्यायालय इसे इसी रूप में देखे। जिसे आप पंथनिरपेक्षता के खिलाफ बता रहे हैं‚ वो कई समुदायों के धाÌमक अधिकारों की रक्षा के लिए उठाया गया कदम भी माना जा सकता है। याचिका दाखिल कर देना पर्याप्त नहीं है। केरल सरकार को एक साथ कई बातें साबित करनी होंगी। पहली‚ राज्य को संसद द्वारा बनाए कानून के खिलाफ जाने का आधार क्या हैॽ दूसरी‚ उसे पाकिस्तान में उत्पीडि़त अल्पसंख्यों को नागरिकता देने से क्या समस्या हैॽ वह इसे पंथनिरपेक्षता के खिलाफ कैसे मानती हैॽ इस तरह के अनेक प्रश्न हैं जिनको संविधानपरक जवाब देना आसान नहीं है। तो हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए। हमारा मानना है कि यह एक समय भारत के नागरिकों के साथ विभाजन के बाद हुए अन्याय का देर से किया गया परिष्कार है। केवल वोट बैंक की राजनीति के कारण इसका विरोध हो रहा है। तब भी हम उच्चतम न्यायालय के मंतव्य की प्रतीक्षा करेंगे।
ऐतिहासिक रिश्तों में महातिर की जिद
विवेक काटजू, (पूर्व राजदूत)
मलेशिया के प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद ने अंतरराष्ट्रीय संबंधों के प्रथम सिद्धांत की अनदेखी की है। इस सिद्धांत के अनुसार, किसी राष्ट्र या वहां की सरकार का दूसरे देश के अंदरूनी मामलों में दखल देना तो दूर, उस पर टिप्पणी करना भी गलत माना जाता है। मगर महातिर मोहम्मद ने यही किया, जब उन्होंने मोदी सरकार के कई फैसलों पर, जो देश के आंतरिक राजनीतिक और सामाजिक जीवन से संबंध रखते हैं, तीखी टिप्पणियां कीं। इनमें पिछले वर्ष 5 अगस्त को जम्मू-कश्मीर के संबंध में केंद्र सरकार द्वारा लिए गए फैसले भी शामिल हैं और पिछले माह अस्तित्व में आया नागरिकता संशोधन कानून भी।
कोई भी स्वाभिमानी देश ऐसी टिप्पणियों को बर्दाश्त नहीं करता और वह सामने वाले के खिलाफ ऐसे तमाम कदम उठाता है, जो वह उठा सकता है। वह ऐसा इसलिए करता है, ताकि दूसरे पक्ष को यह एहसास दिला सके कि उसकी टिप्पणी उसे कुबूल नहीं है। मोदी सरकार ने भी ऐसा ही किया। महातिर की टिप्पणी को खारिज करते हुए उसने कुछ ऐेसे कदम उठाए, जिनसे भारत की नाराजगी प्रकट हुई। इन कदमों में मलेशिया से मंगाए जाने वाले पाम तेल पर बंदिश लगाने और कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामानों के आयात पर रोक शामिल हैं। राजनयिक दृष्टि से ये कदम वाजिब हैं, क्योंकि केंद्र सरकार ने इनके जरिए मलेशिया के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय समुदाय को भी संदेश दिया है कि भारत के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप नाकाबिले बर्दाश्त है।
आखिर महातिर मोहम्मद ने ऐसा क्यों किया? वह भारत की इस प्रतिक्रिया से कुछ परेशान हैं, और अपनी परेशानी उन्होंने जाहिर भी की है। मगर साथ-साथ उन्होंने यह भी कहा है कि वह गलत को सही नहीं कह सकते और गलत कदमों के खिलाफ अपनी आवाज उठाते रहेंगे। महातिर मोहम्मद का राजनीतिक जीवन निश्चय ही अनूठा रहा है। अपने देश की सियासत पर वह दशकों से असरंदाज हैं। 1981 में उन्हें सबसे पहले प्रधानमंत्री की कुरसी मिली थी और तब उन्होंने तय किया था कि मलेशिया को वह दुनिया के औद्योगिक और विकसित देशों में शुमार करेंगे। 1990 में उन्होंने अगले 30 वर्षों में, यानी 2020 तक अपने देश को पूरी तरह से एक औद्योगिक देश बनाने का लक्ष्य रखा था। उनके इन कामों की बेशक तारीफ की जाएगी, लेकिन एक सच यह भी है कि उनकी कार्यशैली तानाशाही सरीखी रही है। वह अपनी आलोचना कतई बर्दाश्त नहीं करते और अपने पिछले कार्यकालों में उन्होंने विपक्षी नेता के साथ-साथ अपनी सरकार व पार्टी के कई नेताओं के खिलाफ भी मुकदमे चलाए और उन्हें जेल भेजा। उनके शासनकाल में मलेशिया में मानवाधिकारों का भारी हनन हुआ।
महातिर ने मलेशिया की ‘भूमि पुत्र’ नीति को भी खूब तवज्जो दी, जिसका संदर्भ मौजूदा तनाव में समझना लाजिमी है। दरअसल, मलेशिया की अधिकांश जनता और मूल निवासी मलय जाति के हैं। मगर औपनिवेशिक युग में वहां चीन और भारत से लोग भी पहुंचे थे। चीन से आए हुए लोगों ने, खासतौर से 1950 के दशक में अंग्रेजी शासन की विदाई की बाद, मलेशिया के आर्थिक और वाणिज्यिक जीवन पर अपनी पकड़ बनाई, जबकि भारतीय मूल के निवासियों की आर्थिक व राजनीतिक हैसियत बहुत कमजोर रही। वे वहां रबड़ की खेती के लिए ले जाए गए थे। जाहिर है, आजादी के बाद देश की सियासी बागडोर मलय जाति के हाथों में आई। 1960 के दशक में मलेशियाई सरकार और मलय राजनीतिक वर्ग ने यह तय किया कि देश में मलय जाति के हितों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके मद्देनजर यूनाइटेड मलय्ज नेशनल ऑर्गेनाइजेशन पार्टी का गठन किया गया, जिसमें नेतृत्व तो मलय लोगों के हाथों में रहा, लेकिन चीनियों और भारतीयों को भी उसमें शामिल किया गया। महातिर ने इस भूमि-पुत्र नीति को पूरी तरह प्रोत्साहित किया, और अंतरराष्ट्रीय जगत में कभी इसके खिलाफ आवाज उठी भी कि इसकी वजह से भारतीय मूल के निवासियों का विकास बाधित हो रहा है, तो महातिर उसे खारिज करके अपनी नाराजगी जाहिर करते रहे। वह ऐसी टिप्पणियों को मलेशिया के अंदरूनी मामलों में दखलंदाजी मानते थे। विडंबना है कि मलेशिया के मामलों में कोई टिप्पणी उन्हें बर्दाश्त नहीं, लेकिन भारत के अंदरूनी मामलों में दखल उन्हें वाजिब जान पड़ रहा है।
भारत और मलेशिया के संबंध ऐतिहासिक रहे हैं। औपनिवेशिक काल के अंत के साथ दोनों देशों के शीर्ष नेतृत्व के वैश्विक विचार भी मिलते-जुलते रहे। 1962 में चीन के आक्रमण के समय भी मलेशिया के प्रथम प्रधानमंत्री टुंकु अब्दुल रहमान ने भारत का समर्थन किया था। यहां तक कि जब मलेशिया ने भूमि पुत्र नीति अपनाई, तब भारत की प्रतिक्रिया पर उस वक्त की सरकार ने यह आश्वस्त किया था कि भारतीय मूल के लोगों के हितों की हरसंभव रक्षा की जाएगी। मगर प्रधानमंत्री महातिर ने भारत के साथ कभी गर्मजोशी नहीं दिखाई। उनकी दृष्टि में जापान, चीन और दक्षिण कोरिया मलेशिया के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने अपने देश की अर्थव्यवस्था को इन देशों के साथ जोड़ा।
भारत-मलेशिया आपसी रिश्ते उम्मीद के मुताबिक इसलिए भी आगे नहीं बढ़ सके, क्योंकि महातिर भारत और पाकिस्तान के साथ अपने देश के संबंधों को संतुलित करने में जुटे रहे, जबकि अपनी तरफ से हर भारत सरकार ने मलेशिया के साथ आर्थिक व वाणिज्यिक संबंधों को गति देने का प्रयास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो ‘एक्ट ईस्ट पॉलिसी’ के तहत इन संबंधों को नई ऊर्जा देने की कोशिश की। पूर्व प्रधानमंत्री नजीब रजाक के दौर में दोनों देशों के रिश्तों में अच्छा-खासा विकास हुआ था। तब मलेशिया की कंपनियों में भारत ने निवेश किया और रक्षा क्षेत्र में भी सहयोग खूब बढ़ा। नजीब भारत की क्षमता समझते थे और वह यह भी चाहते थे कि मलेशिया के भविष्य पर चीन हावी न होने पाए। मगर 2018 के चुनाव में महातिर मोहम्मद की फिर से ताजपोशी और भ्रष्टाचार के मामलों में नजीब रजाक की गिरफ्तारी के बाद भारत और मलेशिया के रिश्ते पटरी से उतरते हुए दिख रहे हैं। बेशक महातिर की जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने मलेशिया जाकर दोनों देशों के आपसी रिश्तों को बरकरार रखने के संकेत दिए, मगर महातिर अपने पुराने रवैये पर ही कायम जान पड़ते हैं। भारत के साथ संबंध बढ़ाने में शायद उनकी रुचि नहीं है।
Date:16-01-20
मौसम की अति
संपादकीय
पिछले सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं, यह शायद सबसे लंबी शीत लहर है। उत्तर भारत में इस समय जो सर्दी दिख रही है, वैसी अभी तक के किसी रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। जब लगभग पूरा देश सर्दी से कंपकंपा रहा है, तब देश के कई इलाके भीषण बर्फबारी और हिमस्खलन से जूझ रहे हैं। देश में आमतौर पर दो हजार मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाले पहाड़ी क्षेत्रों में सदिर्यों में बर्फबारी हो जाती है, लेकिन इस बार इससे बहुत निचली जगहों पर बर्फ पड़ रही है। पड़ोसी पाकिस्तान का हाल तो और भी बुरा है। सिर्फ बलूचिस्तान में ही बर्फबारी और सर्दी से 80 से ज्यादा लोगों की जान जाने की खबर है। और आगे अफगानिस्तान में तो समस्या कहीं ज्यादा गहरा रही है। लेकिन इस बार की ठंड का सबसे नाटकीय बदलाव कहीं दिख रहा है, तो वह पश्चिम एशिया में। अरब के रेगिस्तान में जिस तरह से बारिश, बाढ़ और बर्फबारी दिख रही है, वैसा पूरे इतिहास में कभी सुनने में नहीं आया। दुनिया के सबसे समृद्ध शहरों में गिने जाने वाले दुबई में इस बार इतनी बारिश हुई कि वहां बाढ़ ही आ गई।
वैसे भी इस शहर में ज्यादा बारिश नहीं होती, इसलिए वहां जल निकासी की व्यवस्था नहीं के बराबर है। इससे दुबई और पड़ोसी शारजाह में न सिर्फ भीषण ट्रैफिक जाम हो गया, बल्कि लोग कई दिन के लिए अपने घर में बंद रहने को मजबूर हो गए। यह वह समय है, जब वहां की अर्थव्यवस्था और आर्थिक प्रतिष्ठा में चार चांद लगाने वाला दुबई शॉपिंग फेस्टिवल होता है। दुनिया भर के पर्यटकों के लिए वहां भारी इंतजाम होते हैं। लेकिन इस बार बारिश ने इन सब पर पानी फेर दिया। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली घटनाएं पड़ोसी सऊदी अरब में हुईं, जो न सिर्फ अपने रेगिस्तान के लिए मशहूर है, बल्कि वहां की जलवायु बूंद-बूंद को तरसती रही है। इस बार न सिर्फ वहां बारिश हुई, बल्कि कुछ इलाकों में बर्फ भी पड़ गई। जॉर्डन से लगी सऊदी अरब की सीमा पर रेत के टीलों के बीच खेलने वाले बच्चे इन दिनों वहां स्नोमैन बना रहे हैं।
एशिया और अरब के कुछ हिस्सों में जिन दिनों यह हाल है, ठीक उसी समय ऑस्ट्रेलिया भीषण गरमी से जूझ रहा है। वहां के जंगलों में लगी भीषण आग से भी इस गरमी में खासा इजाफा हुआ है, दूसरी तरफ यह भी कहा जाता है कि आग लगने के तमाम कारणों में एक वहां की गरमी भी है। वैसे इस शीतलहर ने हमारे हाड़ कंपाने शुरू ही किए थे, तभी खबर आई थी कि 2019 अभी तक का सबसे गरम साल रहा है। सबसे गरम साल के बाद सबसे बड़ी ठंड का इस तरह से आगमन हैरत में डालने वाली बात भी है। हालांकि मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि इसमें हैरत की कोई बात नहीं है। वे इसे मौसम की वैसी ही अति मानते हैं, जैसी कि पिछले साल अचानक कुछ इलाकों में भीषण बाढ़ आ गई थी।
कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि मौसम चक्र बदल रहा है, इसलिए ऐसी अति की घटनाएं आगे भी बढ़ सकती हैं। यह एक चेतावनी भी है कि हमें अपने नगरों, कस्बों, गांवों और स्थानीय निकायों को मौसम की अति से निपटने के लिए तैयार रखना होगा। ऐसी तैयारियां न होने की वजह से हर मौसम हमारे यहां बहुत से गरीब और बेघर लोगों की जान लेता है। पर्यावरण बदल रहा है, इसलिए हमें अपने तौर-तरीके भी बदलने चाहिए। तैयारी न होने का एक नतीजा हमने दुबई में देख ही लिया, हालांकि वहां अति बहुत भीषण नहीं थी।
Power replay
With UDAY failing to engineer a turnaround in discom finances, government needs to rework incentive structures
Editorials
Almost five years after the launch of the Ujwal DISCOM Assurance Yojana (UDAY), there are indications that the power sector is once again in trouble. Not only have losses of state-owned distribution companies (discoms) risen, but their dues for power purchases have also surged. At the end of November 2019, dues owed by discoms to power producers, both independent and state-run entities, stood at Rs 80,930 crore. Of these, Rs 71,673 crore extends beyond the allowed grace period of 60 days. Rajasthan leads the states with the most dues, followed by Tamil Nadu and Uttar Pradesh.
These numbers suggest that, contrary to expectations, the UDAY scheme has failed to engineer a sustainable turnaround in the fortunes of the beleaguered distribution segment — the weakest link in the power chain. Reportedly, the Centre is contemplating yet another scheme to address the issues that continue to plague the sector. But, as distribution falls under the purview of states, rather than adopting an approach similar to that of the past schemes, the new scheme should focus on altering the incentive structure at the state level so as to ensure the achievement of targets. The UDAY scheme, which involved state governments taking over the debt of discoms, had three critical components: A reduction in the aggregate technical and commercial (AT&C) losses, timely revision of tariffs, and elimination of the gap between average per unit of cost and revenue realised.
While progress has been made on some of these fronts, it hasn’t been in line with the targets laid out under UDAY. AT&C losses have declined in some states, but not to the extent envisaged. Under UDAY, discoms were to bring down AT&C losses to 15 per cent by FY19. Similarly, while some states have raised power tariffs, the hikes have not been sufficient as political considerations prevailed over commercial decisions. As a result, the gap between the average cost per unit of power and the revenue realised has not declined in the manner envisaged, forcing discoms to reduce their power purchases and delay payments to power producers. This in turn has impaired the ability of power generating companies to service their debt, causing stress to the banking sector.
The new plan, reportedly, aims to address these issues by reducing electricity losses, eliminating the tariff gap, smart metering, privatising discoms, and having distribution franchisees. These would be welcome measures. But, along with these, the Centre should also look at altering the incentive structures of states in order to ensure compliance. Stiff penalties need to be imposed for not meeting the targets laid out in the new scheme.
Date:16-01-20
Slow connection
Government is responding to SC ruling, but it appears slow and reluctant in restoring fundamental rights
Editorials
In response to a Supreme Court ruling last week, the central government is restoring broadband connections to government installations and providers of essential services, hospitals, banks and the tourism sector in Jammu and Kashmir. However, the step falls far short of the complete withdrawal of curbs on public communications which the court had sought. ISPs are required to block social media sites and technology by which such a restriction can be bypassed, before providing access to institutions and essential service providers.
Institutions and offices must monitor internet usage, record users and change access credentials every day. A call will be taken on fully opening up mobile data communications after the Republic Day celebrations, the government says. This is far too tentative, considering the spectrum of fundamental rights that have been violated by the internet shutdown in Jammu and Kashmir, which is the longest ever in a democracy.
Last week, responding to petitions by Kashmir Times executive editor Anuradha Bhasin and Congressman Ghulam Nabi Azad, the Supreme Court had ruled that the internet shutdown was in violation of Article 19(1)(a) and Article 19(1)(g), which confer the freedom of speech and expression, and the freedom to practise any profession or occupation, and to operate a business, anywhere in the territory of India. Any curb on public freedoms instituted by the government must be constitutional and proportionate. The internet shutdown fails on the question of proportionality because it is of unspecified duration. Communications may be restricted for very short periods in the interest of public safety but here, there is an absence of a declared cut-off date. Moreover, this shutdown has demonstrated, like never before, that the internet has become the backbone of normal life.
Not only has the suspension of data services curtailed the freedom of speech, it has also exacted business losses in the range of Rs 18,000 crore, according to the Kashmir Chamber of Commerce and Industries, which had welcomed the SC ruling as an opportunity to seek compensation. In addition, commonplace actions like seeking medical advice and filing examination and job applications had become impossible or extraordinarily difficult.
The SC ruling was forward-looking, placing all communications shutdowns under the watch of the court. Judicial oversight would encourage governments to be less arbitrary in the future, for they would have to pass the proportionality test. The inevitability of large compensation claims, in the event of failing the test, would serve as a material deterrent. In the present case, in J&K, the government should try to comply with more alacrity because fundamental rights are at stake.
Date:16-01-20
Govern, not conquer
Using force to suppress the ‘Other’ cannot lead to peace
Dev Athawale, [Retired public servant based in Pune]
In the article, ‘Discrimination, not justice’, (IE, December 19, 2019), Pratap Bhanu Mehta, writes about “arguably, the largest student protest since the Emergency”. In the context of the failure of our governing institutions, the role of students in seeking to restore our constitutional framework is striking. On the other hand, the political class does not seem to be worried, while pursuing policies that would undermine the very structure of our constitutional democracy.
As we seek to restore our torn social fabric, and promote both democracy and pluralism, some clues from the past may be useful. In the years before Independence, the failure of the leadership — of the Congress and the Muslim League — to arrive at an honourable compact had tragic consequences. The League saw the Congress as promoting Hindu hegemony; the Congress dismissed the League as a bunch of intransigent Muslims. The result was the Partition of India, which resulted in loss of lives and property to the tune of thousands of crores. It also created a bitter, enduring enmity between communities.
But, despite Partition, millions of Muslims stayed behind in India, taking at face value the promises of the Indian Constitution — that they would enjoy equal rights of citizenship. How can we redeem those promises now?
It is here that the past may help. While the political debate on Partition has focused on what the Congress and the League did (or did not do) in the years just before 1947, if we go slightly further back in time, we can discover voices of sanity that speak directly to our troubled present. These voices can serve the present generation to remind them of the wrongs engulfing them. Here, we would be reading history not to compete with the present, but to find meaningful solutions for the future.
In particular, I draw the reader’s attention to the deliberations at the First Round Table Conference, held in London in November 1930. The conference had 89 representatives: 16 British officials, 57 delegates from British India, and 16 from the Princely States. Although the Congress had boycotted the conference, it nonetheless saw the participation of liberal Hindus like Tej Bahdur Sapru, V S Srinavasa Sastri, M R Jaykar and C Y Chintamani, as well as prominent Muslim leaders, like Aga Khan, Sir Mohmmad Shafi, Mohammad Ali, A K Fazl-ul-Huq and M A Jinnah.
In The Constitutional Problem in India, Sir Reginald Coupland has given a vivid account of the discussions in the conference. Sapru’s remarks are especially worth quoting: “It has been an article of faith with me, that no constitution has any chance of success in India unless the minorities are fully satisfied, that they have got the position of honourable safety in the new commonwealth which we are seeking to establish”. But, “the heart of youth of India on the question”, Sapru went on, “is absolutely sound”, and sooner or later a sense of “territorial patriotism” must grow among them. It would grow, added Jaykar, if the communities were given a chance of serving India together. “Give them opportunities of feeling that side by side they are working for their one country… and a great deal of the difficulty will disappear”. (Coupland, pp 120-121).
These words are highly pertinent for India today. For, what do different enactments like the anti-conversion Act, anti-beef Acts, the criminalising of triple talaq, the abrogation of Article 370, and, the introduction of NRC and CAA, mean to Indian Muslims today? Will this satisfy Muslims or dismay them? Do they feel they are treated honourably and enjoy security in the country of their choice after Partition? Do they have reason to be proud of “territorial patriotism”? Do we allow them to grow as such? Do we give them opportunities to work for their one country?
The suspicions of the present day ruling class with regard to the integrity of Muslims are deeply worrying. These are Indians who did not cross over to Pakistan, during Partition, believing that they would be treated honourably, with secure futures. The government’s perceived hostility towards them, so as to relegate them to second-rate citizens or an appendage of Hindus, is unfathomable.
Here, it would be instructive to recall what Edmund Burke had said in the context of the British subjugation of American colonies. Burke had remarked: “A nation is not governed which is perpetually to be conquered”. How long shall we use force to conquer the “others”? That seems to be the question that the students at the vanguard of the current protests are raising. We should take heed, and act wisely.