
14-12-2021 (Important News Clippings)
To Download Click Here.
 Date:14-12-21
Date:14-12-21
Why Farmers Won, People Lost
The art of selling reform has to recognise group dynamics & the effect of unequal incentives
Duvvuri Subbarao, [ The writer is a former Governor of the Reserve Bank of India ]

Economic reforms produce winners and losers. In the case of farm laws, losers were the relatively large farmers with a marketable surplus, who feared losing the protection of the minimum support price (MSP).
On the other side, potential winners were the larger public who would have benefitted by way of a cleaner environment and lower agricultural prices as market forces gradually engineered a shift in production from cereals to cash crops. The public would have benefitted too, albeit less obviously, via the alternate use of the money saved on MSP – better schools and health facilities, for example.
In theory, any reform measure where the winners gain more than the losers lose should sail through. In practice things hardly ever work out that neatly. Many real-world factors – interest group dynamics, biases and even misinformation – come in the way of the best policies getting through.
Consider for example the unequal incentives of winners and losers to mobilise and agitate for their cause. In the case of farm laws, farmers were a relatively small group, united by a single cause, each of them losing heavily if the reform went through.
On the other side, benefits of the reform would have spread thinly across the vast public; for any single individual, the reward was small, the cost of getting organised high, and the incentive to agitate quite low. In the absence of any effort to mobilise the larger, amorphous group behind its interest, the smaller group held sway.
The play-off between winners and losers is also complicated by the time dimension. For farmers, the cost if the reform went through would be immediate which therefore galvanised them into action. For the public on the other side, benefits of reform, although cumulatively substantial, would accrue over time.
How much weight will the public attach to a benefit that comes not today but later? Overburdened as people are with today’s problems, from their point of view, it’s not worth their while to invest time and effort into agitating today for a benefit tomorrow – yet another reason a small interested group gets its way.
Beyond asymmetric incentives to agitate, collective action is also hampered by ignorance. Oftentimes, winners don’t even realise what they might gain by a specific reform. Take procurement under MSP for example. Although the MSP scheme covers 23 crops, the bulk of the expenditure is on buying rice and wheat from a small segment of farmers in relatively prosperous states. Procurement then becomes in effect a silent fiscal transfer from the Centre to those states.
Juxtapose that with the acrimony that surrounds central fiscal transfers to states via the Finance Commission awards and centrally sponsored schemes. Chief ministers cry foul over their state getting less than its due. Economists hold forth on whether the transfers are efficient and equitable. Analysts pore over which states got more or less compared to prior years. And all of them fail to reckon with under the radar transfers such as those under the MSP.
As the Nobel prize winning economist Gary Becker argued there are many factors that make small, well-organised groups benefit in the political process at the cost of the vast majority. To promote the larger public good therefore, governments need to invest effort into communication and consultation to prevent the debate getting hijacked by a narrow interest group.
It’s not anyone’s case that the farmers who felt threatened by farm laws would not have come out on the streets if the government explained the case for the reform. But such a proactive effort would have helped in building a constituency for the reform.
On the usefulness of prior consultation in navigating contentious reforms, I speak with some personal experience. Back in the mid-1990s, in the Andhra Pradesh government, we were confronted with a serious resource crunch that called for politically painful expenditure restructuring. We had to chop many subsidies including raising the price of subsidised rice – the government’s flagship scheme.
Chandrababu Naidu, the CM at the time, agonised over it quite a while and then, instead of deciding on the issue right away, suggested that we put out a white paper explaining the financial situation and the difficult choices the government had to make.
Frankly, I thought this was all a waste of time since common people will not understand public finances, and in any case, they will not support a measure that would directly hurt them. How wrong I was! Naidu, politically savvy as he had always been, organised extensive dissemination of the white paper both through the government machinery and his party structure.
In several focus group meetings, I heard ordinary people, whose understanding I had underestimated, ask if they would get better roads or drinking water in their village from the money saved on the subsidy. After weeks of this, I can’t say there was total support for the subsidy cuts but the opposition to them was substantially attenuated.
We have always taken pride in our reforms being robust because they are vetted by a democratic process. But we should not risk reforms becoming hostage to the distortions of that democratic process.
Jean-Claude Juncker, the former president of the European Union, famously said, “We all know what to do, we just don’t know how to get re-elected after we’ve done it.”
Narendra Modi, arguably commanding the strongest political capital compared to any Indian leader in decades, has the challenge and opportunity of proving Juncker wrong.
More Than a Police+ Force
The armed forces need a clear role definition for necessary restructuring
Pranab Dhal Samanta
The armed forces are in a difficult spot these days, grappling with the backlash for mistakenly killing civilians in Nagaland on one end, and coming to terms with the consequences of losing the country’s first chief of defence staff (CDS) on the other. The first has triggered a stormy debate on the continuation of the Armed Forces (Special Powers) Act (AFSPA) in the northeast, while the other has brought uncertainty on how to carry forward execution of key military reforms.
Add to this the challenge of deploying more troops against an ever-increasing Chinese presence across the Line of Actual Control (LoAC), besides other existing commitments, and you have somewhat of a perfect storm — a stretched deployment profile, limited resources, a crucial gap in the leadership matrix, and a compounding threat scenario riddled with imponderables.
This is not just about withdrawing AFSPA from some areas, appointing a new CDS and dispatching more troops with better equipment to our northern borders. Those issues are immediate and certainly require urgent attention. But the real challenge is more fundamental — clarity on the role of the armed forces and, by extension, of the paramilitary, police and other security forces. This also a necessary precursor to any reform and restructuring.
Why just debate the withdrawal of AFSPA? The debate should be centred on pulling out the army from counterinsurgency operations. The Act was brought in to help the armed forces conduct operations in their own territory, amid their own citizens without being hamstrung by policing laws. From detaining suspects to taking action on homes of locals that doubled as hideouts for terrorists, AFSPA provided the closest to a battlefield environment that the army is trained to fight in.
At no point, however, was it ever envisaged to deploy the military in a permanent way in internal security roles. Given that the primary job of the armed forces is on the borders against external threats, its prolonged deployment in counter-insurgency operations within its own country was never seen as healthy practice even by the military. But on the logic that external actors were behind internal disturbances, the political executive kept justifying the decision to deploy the military.
A Constant Normal
For its part, the army also evolved through these long periods of counterinsurgency operations. It even came out with the doctrine on sub-conventional warfare in the mid-2000s, which was updated less than a decade ago. But there, too, the stated purpose was to restore normalcy from where civilian authority can assume responsibility. Yet, the army has remained deployed for decades in the northeast and in Jammu and Kashmir.
At one time, the UPA government serious considered deploying the army against the Maoists. The army opposed it, and so it fell upon the paramilitary and state police forces to take the battle forward. A decade later, despite setbacks, the police forces have made good progress, combined well across state jurisdictions to geographically, militarily and politically restrict the Maoist area of influence.
It’s vital for decision-makers to recognise that police forces have a security role distinct to that of the military. And while the latter can come in the aid of the police, it cannot be a replacement. In fact, it’s incumbent on central and state governments to constantly upgrade their police force — their capabilities and capacities — to take on terrorists and insurgents. One of the markers of a strong state is a modern, accountable police force not dependent on the military to deal with internal security challenges.
This discussion on reducing the military’s internal commitments is not new, but it’s more relevant now. The reason is Chinese deployments on the LoAC. Until now, the army could manage these commitments as well as hold the fort in border areas with Pakistan being the primary military challenge. This has changed. Today, the armed forces are being deployed on the higher reaches of the Himalayas for the second successive winter. Regardless of how the ball rolls on the political side with Beijing, the army knows it will have to commit more troops and resources for years to come on the LoAC.
The army has to also step up vigil against Pakistan, given its strategic proximity to China, accentuated further by the rise of the Taliban and Islamic radicalism in Afghanistan. In short, the demands on military’s primary role of defending India from external threats have grown manifold. And it’s not just an appreciation of increased threat, but also a striking reality on the borders. So, clearly, now would be a good time to reduce maximum military commitments to internal security, definitely in the northeast and even in the Kashmir hinterland to the extent possible.
Right-Coding CDS
Most importantly, a clear role definition on ground will unlock the potential for reforms and restructuring of the armed forces. The office of the CDS was set up precisely for this purpose — to build on the principle of jointness, starting with resource-sharing to developing joint fighting capabilities. The Chinese threat extends well beyond the LoAC to India’s air and maritime boundaries, which necessitates challenging the status quo to fashion a comprehensive response.
Here, the CDS is undoubtedly a key agency of both leadership and change. But as GoI wrestles with these issues, including the appointment of the new CDS, the time has come for it to politically revisit and repurpose the armed forces to its original mandate as a necessary first step for bigger change and transition.
Home truths on climate change
There is a gap between what the goverment says on the international stage and what it does at home
Brinda Karat, [ A member of the Communist Party of India (Marxist) Polit Bureau and a former Rajya Sabha MP ]
At the 26th session of the Conference of the Parties (COP26) to the UN Framework Convention on Climate Change, the developed countries, which continue to be the most responsible for the destruction of the biosphere, resorted to their usual tactics of bullying the less developed world to accept higher targets for controlling greenhouse emissions when they haven’t done so themselves. In fact, they have failed to even implement their earlier commitments towards funds and technology transfer.
The reasons for the climate crisis affecting the world can be found in the reckless drive for profit maximisation by global capitalism led by the U.S. and its developed country allies. This has resulted in ecological destruction in the name of development. The effort in Glasgow was to push ‘net zero’ emissions by 2050 as a standard across countries, without taking into account the cumulative emissions for which the Global North is mainly responsible. The effort by some to equate India and other developing countries with the U.S. and Europe as the worst “emitters” is also misplaced precisely for this reason of cumulative emissions. In its model of country-wise cumulative emissions, carbonbrief.org uses population as a factor in its report of October 5, 2021. It finds that “the U.S., Russia, the U.K., Japan and Canada account for 10% of the world’s population, but 39% of cumulative emissions”, while China, India, Brazil and Indonesia account for 42% of the world’s population but just 23% of cumulative emissions.
Looking inward
To find sustainable solutions, in addition to resisting the imperialist mindset of the developed world, we have to also look at the internal policies of the governments of developing countries. Most of these governments are committed to capitalist appropriation of natural and national resources. For example, the official delegation from India may have fought hard to protect sovereign decisions on the use of fossil-based energy requirements from the hypocritical demands of the Global North for additional commitments against use of coal. But in India, the government’s coal use policy is driven by its determination to hand over mineral resources, including coal, to the corporate sector. Even as India boasts of switching to solar energy to meet its emission control targets, it is privatising the coal industry, auctioning coal mines and encouraging open cast mines without the guarantee of end use, but for commercialisation and export. Thus, on the Glasgow stage, India’s ruling regime wears the crown of a developing country fighting against the aggression of developed countries on climate change responsibilities, but policies at home reflect the interests of domestic and foreign capital — coal is used as a commodity for profit, not necessarily for any development purposes.
It is a similar story on the declaration signed by over 140 countries to “halt and reverse forest loss and land degradation by 2030.” India did not sign the agreement on the ground that the declaration linked trade to land use and trade falls under the purview of the World Trade Organization. However, within India, the promotion of policies towards corporatisation of agriculture and the encouragement to contract farming on conditions set by big agri-businesses undermines food security. The pursuit of such policies domestically damages the credibility of India’s stand on international platforms.
The same declaration has important commitments to “recognise and (extend) support to smallholders, indigenous peoples and local communities.” It was convenient for the government not to sign this since it is following policies that are opposed to these commitments. In a slew of amendments proposed to existing laws and policies, the government has moved to monetise, privatise, commercialise and even militarise forests, trampling over the recognised rights of forest communities and specifically tribal communities. These measures are reflected in the proposed Forest Policy of 2018, the suggested amendments to the Forest Act of 1927, the amendments to the Forest (Conservation) Act of 1980, amendments to the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act of 1957, the changes proposed to the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act of 1957, and the adoption of the Compensatory Afforestation Fund Rules. All these changes strip the Gram Sabhas of any voice in decision-making processes, even though they are affected directly, and make it easier to handover forests to the private sector. These policies have accentuated the diversion of forests for a variety of projects. From 2013-2019, it is estimated that 96% of tree cover loss occurred in natural forests. On the other hand, the Forest Rights Act of 2006, which recognises the rights and duties of Adivasis and traditional forest-dwelling communities, is being diluted with a high rejection of claims.
Setting an example
In the 2015 COP in Paris, the Government of India had promised that it would develop carbon sinks to the equivalent of 2 billion to 3 billion tonnes of CO2 by 2030. The government set up a Green Mission for the regeneration of forests, afforestation, additional forest and tree cover, and so on. The Estimates Committee of Parliament in its 2018-2019 report on progress towards these goals slammed the government stating that it “deplores the way that an issue pertaining to the existence of the earth is being handled.” The report stated that to fulfil the promise of sequestering the CO2 target, 30 million hectares of land are required to plant indigenous trees, not monocultures or plantations as is being done at present. Where will this land come from? Planting trees along national highways or along railway tracks as is being planned will be a very small component of the required target. At present, the lands of forest-dwelling communities are being forcibly taken away and used for plantations. The Gram Sabhas are not being consulted. The method of making those communities which have the least responsibility for carbon emissions pay with their lands and livelihoods is embedded in India’s climate change strategies as far as forest policies are concerned.
The clear gap between what is portrayed as a nationalist fight on the international stage and what is followed at home is even more stark with the present regime. The government must reverse its pro-corporate policies reflected in privatisation. It needs to call off its undeclared war on the Forest Rights Act and constitutional provisions that protect Adivasi communities. It is only with the cooperation of those who have protected forests that India can make a real contribution in the efforts to control climate change and be an example to the rest of the world.
पोषण और शिक्षा में असमानता, अब बड़े फैसलों का वक्त है
संपादकीय
चाहे भ्रूण से लेकर अंतिम सांस तक मनुष्य के पोषण की समस्या हो या आय या पूंजी में असमानता की….। या फिर पिछले लगभग दो वर्षों में कोरोना के कारण शिक्षा में पैदा हुई असमानता की। गरीब और अमीर के बीच खाई बढ़ती जा रही है। चिंता यह है कि इससे कहीं बड़ा सामाजिक आक्रोश न पैदा हो। प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों द्वारा तैयार की गई विश्व असमानता रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया के 10 सबसे असमान देशों में ब्राजील के बाद दूसरे स्थान पर है जहां उच्च आय वर्ग के टॉप 10 फीसदी और निम्न आय वर्ग के 10 फीसदी के बीच आय का अंतर 22 गुना है। उधर ‘स्कूल चिल्ड्रेन ऑनलाइन-ऑफ़लाइन’ (स्कूल) के एक सर्वे में पाया कि ऑनलाइन माध्यम से शहरों में 24 फीसदी और गांवों में मात्र आठ फीसदी बच्चे हीं शिक्षा ले रहे हैं। गांवों में ऑफलाइन माध्यम से पढ़ने वाले आधे से ज्यादा बच्चे पिछले डेढ़ साल से कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं। इन सबसे ज्यादा चिंताजनक रिपोर्ट है ताज़ा एनएफएचएस सर्वे-5 के तहत भारत का हर तीसरा बच्चा या तो छोटे कद का है या आयु के मुताबिक कम वजन का है जो भविष्य में उसके सम्पूर्ण मानसिक-शारीरिक विकास में बाधक बनेगा। भारत सरकार 1975 से बाल कुपोषण की समस्या के निराकरण के लिए योजनाएं बनाती रही हैं लेकिन कुपोषण से लेकर भूखमरी के मामले में देश नीचे के एक दर्जन देशों में है। विश्व भूख सूचकांक और सरकार की एनएफएचएस रिपोर्ट पांच वर्ष तक के बच्चों में कुपोषण का जायजा लेती हैं और ये सरकारों के लिए एक आइना होते हैं जिन्हें सकारात्मक भाव से लेने की जरूरत है क्योंकि ये आंकड़े केंद्र के मंत्रालयों या राज्य सरकारों की रिपोर्ट्स से ही लिए जाते हैं। भूख सूचकांक में भारत दुनिया के 116 देशों में इस बार सात अंक गिर कर 101वें स्थान पर है। आर्थिक असमानता तो समाज बर्दाश्त कर सकता है लेकिन पोषण और शिक्षा की असमानता पीढ़ियों को प्रभावित करती है। यह सरकार के लिए वेक-अप कॉल है।
गौरव का अवसर
संपादकीय
काशी में विश्वनाथ धाम परियोजना के भव्य लोकार्पण ने यदि कुछ इंगित किया है तो यही कि हमारे धार्मिक-सांस्कृतिक स्थलों में देश की आस्था के साथ उसका गौरव भी बसता है और उसे सहेजने-संवारने की आवश्यकता है। इस आवश्यकता की पूर्ति इसलिए होनी चाहिए, क्योंकि बनारस जैसे सांस्कृतिक केंद्र हमारे समृद्ध अतीत के साक्षी हैं। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र की इस महत्वाकांक्षी परियोजना का महत्व इसलिए और अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि एक समय इसे असंभव सा माना जा रहा था। यदि यह परियोजना भव्य-दिव्य स्वरूप में साकार हो सकी तो प्रधानमंत्री की दृढ़ इच्छाशक्ति और दूरदर्शिता के चलते। इस परियोजना को आगे बढ़ाना एक जटिल कार्य था, लेकिन यह देखना-जानना सुखद है कि इसे पूरा करने में हर बाधा को सफलतापूर्वक पार किया गया और इस क्रम में कहीं कोई असंतोष भी नहीं पनपने दिया गया। स्पष्ट है कि इस परियोजना के क्रियान्वयन को एक आदर्श मानकर देश के अन्य धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थलों का विकास होना चाहिए।
धार्मिक, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक महत्व वाले सभी शहरों को उनके प्राचीन वैभव के साथ विकसित करने की आवश्यकता इसलिए बढ़ गई है, क्योंकि हमारे अधिकांश धार्मिक स्थल भीड़भाड़, अव्यवस्था और नागरिक सुविधाओं के अभाव से ग्रस्त हैं। इसके चलते न केवल पर्यटकों को तमाम समस्याओं से दो चार होना पड़ता है, बल्कि धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने में भी कठिनाई आती है। हम इसकी भी अनदेखी नहीं कर सकते कि धार्मिक स्थलों में समय के साथ अनेक कुरीतियां भी पैदा हो गईं और कुछ ने तो सनातन संस्कृति की दिव्यता को मलिन करने का काम किया। यह अच्छा हुआ कि प्रधानमंत्री ने विश्वनाथ धाम परियोजना का लोकार्पण करते हुए औरंगजेब सरीखे उन आततायियों का उल्लेख किया जिन्होंने हमारे धार्मिक स्थलों को नष्ट-भ्रष्ट किया। हम भारतवासियों को अपने समृद्ध अतीत पर गर्व करने के साथ उन घटनाओं और प्रसंगों को भी याद रखना चाहिए जो ध्वंस और अत्याचार के गवाह बने। यह परियोजना केवलहिंदू जनमानस को ही गौरव की अनुभूति कराने वाली नहीं है, बल्कि राष्ट्र के गौरव को भी सम्मान प्रदान करने वाली है। यह उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री ने विश्वनाथ धाम परियोजना का लोकार्पण करते हुए यह कहा कि यह भारत को एक निर्णायक दिशा देने और उसे उज्ज्वल भविष्य की ओर ले जाने वाली प्रेरणा बननी चाहिए। वास्तव में यह परियोजना इसके लिए एक प्रेरणास्नोत सरीखी होनी चाहिए कि राष्ट्र का विकास किस तरह से करने की आवश्यकता है। नि:संदेह देश का विकास कुछ इस तरह होना चाहिए जिससे नवीनता के साथ हमारी सदियों पुरानी प्राचीनता भी सजीव हो उठे। जब ऐसा होगा तभी सनातन संस्कृति, उसकी आध्यात्मिक यात्र और सर्वसमावेशी एवं सर्वकल्याणकारी परंपराओं को बल मिलेगा।
 Date:14-12-21
Date:14-12-21
बांध की सुरक्षा आवश्यक
संपादकीय
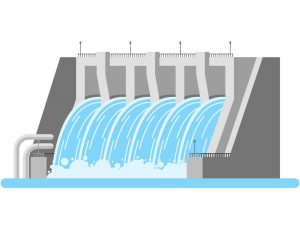
गुजरात के राजकोट में मच्छू बांध दुर्घटना के बाद वर्ष 1980 के आरंभिक दशक में बांध सुरक्षा पर केंद्रीय कानून लाए जाने का प्रस्ताव दिया गया था। हालांकि इस उद्देश्य के लिए तैयार मसौदा विधेयक एक समिति से दूसरी समिति के बीच झूलता रहा।
वर्ष 2010 में संसद में विधेयक प्रस्तुत किया गया मगर इसमें कई संशोधन किए गए और उसके बाद यह संसद के दोनों सदनों में कहीं जाकर पारित हो पाया। बड़े बांधों की संख्या के लिहाज से भारत अमेरिका और चीन के बाद तीसरे स्थान पर है। भारत को तत्काल इस कानून की जरूरत थी। देश में कुल 5,745 बड़े बांधों में 300 के करीब, 100 वर्षों से भी अधिक पुराने हो चुके हैं जबकि लभगग 1,000 बांधों की आयु 50 वर्ष पार कर गई है।
इस अवधि के बाद सामान्यत: बांधों की मरम्मत की आवश्यकता होती है। अधिकांश पुराने बांध मिट्टी या स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सामग्री से तैयार हुए हैं इसलिए जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के कारण भारी बारिश, भूकंप या अन्य किसी प्राकृतिक आपदा में ये टूट सकते हैं।
इस कानून में बांध सुरक्षा दिशानिर्देश के तहत राज्यों की सहायता का प्रावधान है। इनमें बांधों की नियमित निगरानी, निरीक्षण, परिचालन और 15 मीटर से ऊंचे सभी बांधों के रखरखाव संबंधित कार्य शामिल हैं। कानून में राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर बांध सुरक्षा समिति बनाए जाने का प्रावधान है। इसमें बांध सुरक्षा मानकों से जुड़े दिशानिर्देश भी सुझाए गए हैं। नियमों का उल्लंघन करने वालों के लिए कानून में दंड का भी प्रावधान है।
हालांकि राज्यों को यह बात खटक रही है कि इस नए कानून में बांधों के परिचालन, इनकी निगरानी और मरम्मत की जिम्मेदारी नियंत्रकों पर सौंप दी गई है। ज्यादातर मामलों में इन बांधों का नियंत्रण राज्य सरकारों के पास होता है। केवल कुछ बड़े बांधों का निर्माण एवं नियंत्रण राज्य जल-विद्युत निगमों के अधीन है।
इन सभी बांधों का रखरखाव कमोबेश ठीक तरीके से किया गया है। नए कानून के तहत बांध सुरक्षा इकाई को मॉनसून से पहले और इसके बाद, भूकंप, बाढ़ और अन्य आपदाओं या फिर दरार आदि दिखने के बाद निरीक्षण किया जाना जरूरी है। अब संसद में कानून पारित हो चुका है इसलिए राज्यों की आपत्तियों के समाधान एवं दिशानिर्देशों के क्रियान्वयन में किसी तरह का विलंब नहीं होना चाहिए।
राहुल का हिंदू
संपादकीय
पता नहीं राहुल गांधी के सलाहकार और भाषण लिखने वाले कौन हैं‚ जो उन्हें ऐसे–ऐसे प्रवचन और परिभाषाएं थमा देते हैं कि वह हास्यास्पद हो जाते हैं। इधर वह हिंदू और हिंदुत्व की गहन दार्शनिक व्याख्या कर रहे हैं‚ जिसमें वह खुद को हिंदू बताते हैं और भाजपाइयों को हिंदुत्ववादी। वह कहते हैं कि हिंदू सच को ढूंढता है और उनका रास्ता सत्याग्रह का है और हिंदुत्ववादी पूरी जिंदगी सत्ता को खोजने में लगा रहता है। वे गांधी को हिंदू मानते हैं और गोडसे को हिंदुत्ववादी। इस समूचे वक्तव्य में वह यह नहीं बताते कि हिंदुत्ववादियों के विरोध में उनको किस दबाव के अंतर्गत हिंदू हो जाना पड़ा है। और उनका अपने हिंदू होने से तात्पर्य क्या हैॽ वह जिस धर्म से जोड़कर स्वयं को हिंदू बताते हैं वह धर्म क्या है‚ उसका इतिहास क्या है‚ उसकी धार्मिक आस्थाएं क्या हैं और उसकी संस्कृति तथा जीवन पद्धति क्या हैॽ वे जिन हिंदुत्ववादियों को गरियाते जाते हैं उनके पास जय–पराजय से भरा हुआ पूरा इतिहास है। वैदिक धर्म से लेकर वेदांत तक वैचारिक दर्शन है‚ लेकिन पता नहीं लगता है कि राहुल गांधी के हिंदू के पास क्या हैॽ वह गांधी को हिंदू बताते हैं तो उन्हें ध्यान में रखना चाहिए कि गांधी कर्मकांड़ी हिंदू नहीं‚ सुधारवादी और समन्वयवादी हिंदू थे। वह हिंदू धर्म को उदार और समन्वयवादी धर्म के रूप में स्थापित करना चाहते थे‚ लेकिन इतिहास ने गांधी के हिंदुत्व को बुरी तरह पराजित कर दिया। गांधी अपने हिंदू के सहारे मुसलमानों को साथ नहीं ला सके और देश का भयावह बंटवारा हुआ। गोडसे का कृत्य एक हिंदू की हत्या का नहीं था बल्कि एक विशाल मन उदारपंथी और वैश्विक दृष्टि वाले हिंदू की हत्या का था। हैरानी की बात है कि गांधी की भौतिक हत्या के बाद गांधी की आत्मिक चेतना की सर्वाधिक हत्या तो उन लोगों ने की जिन्होंने गांधी के उपरांत देश की सत्ता संभाली। उन्होंने गांधी की दृष्टि के अनुसार न तो विभिन्न धर्मों के बीच समन्वय की संस्कृति खड़ी की और न उन्होंने देश के बंटवारे की धार्मिक पहलू का कोई उत्तर खोज पाए और ना हिंदू धर्म के जाति जैसे आंतरिक विग्रहों को खत्म कर उसे अग्रगामी धर्म बनाने की चेष्टा की। राहुल गांधी की बौखलाहट राजनीतिक शक्ति वाले इसी हिंदुत्व को लेकर है‚ जिसके विरोध की कोई दार्शनिक और वैचारिक काट उनके पास नहीं है। सिवाय इसके कि वह स्वयं को हिंदू बताएं‚ ऐसा हिंदू जिसके पास ना सर है और ना पैर। राहुल गांधी के सलाहकारों को चाहिए कि अगर वे हिंदुत्ववादियों के विरोध में हिंदू शब्द को खड़ा करना चाहते हैं तो वे उसमें ऐसा गढ़ें कि लोगों को उसमें सार तत्व नजर आए‚ भौंड़ा हास्य नहीं।
Date:14-12-21
श्री काशी विश्वनाथो विजयतेतराम!
आचार्य पवन त्रिपाठी
अद्भुत। वाकई अद्भुत था अनेक योगायोग से परिपूर्ण सोमवार का वह दिन, जब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने श्री काशी विश्वनाथ कॉरीडोर का लोकार्पण किया। उसे देश के लोगों को समर्पित किया। इस अवसर पर न सिर्फ काशी, बल्कि देश-विदेश का हिंदू जनमानस झूम रहा था। गर्वित था। खुशी के अश्रु बहा रहा था।
दरअसल, वह क्षण ही ऐसा था। क्योंकि उस समय काशी में इतिहास गढ़ा जा रहा था। या यूं कहिए इतिहास सुधारा जा रहा था। औरंगजेब एवं शाहजहां जैसे जिन मुगल बादशाहों ने काशी विश्वनाथ मंदिर सहित हमारे अनेक धार्मिंक आस्था केंद्रों को ध्वस्त किया, आज तक हम उन्हें धिक्कारने के बजाय सम्मान ही देते आए हैं। देश की राजधानी दिल्ली में शाहजहां रोड एवं औरंगजेब रोड से गुजरते हुए हमारे चुने हुए राजनीतिक आकाओं को आज तक एक बार भी यह अहसास नहीं हुआ कि इन नामों ने भारत की आस्था-अस्मिता को धूल-धूसरित करने में कोई कसर नहीं रखी थी। उलटे कुछ मतिभ्रमित इतिहासकारों ने इन मुगल बादशाहों को इतिहास का हीरो सिद्ध करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। शाहजहां के बनवाए एक मकबरे को दुनिया का सातवां आश्चर्य बताकर गर्व करने वाले लोगों की आज भी कोई कमी नहीं है भारत में।
यह मानसिकता दिल्ली के सियासतदानों तक ही सीमित नहीं रही। इसकी बानगी काशी में भी कुछ वर्ष पहले उस समय दिखाई दी थी, जब काशी विश्वनाथ कॉरीडोर के निर्माण की शुरु आत होने जा रही थी। उस समय प्रस्तावित कॉरीडोर के मार्ग में आने जा रही 300 से ज्यादा इमारतों को अधिग्रहीत करने और हटाने का काम शुरू हुआ तो यह कहकर इस कार्य का विरोध किया गया कि मोदी-योगी तो काशी के मंदिरों को ही तोड़े डाल रहे हैं, लेकिन इस विरोध का सामना करते हुए जब वे इमारतें हटीं तो ऐसे-ऐसे अद्भुत मंदिर सामने आए, जिन्हें वर्षो से किसी ने देखा ही नहीं था। पुरातत्त्व एवं वास्तु की अनमोल धरोहर ये मंदिर भी आज गंगा मैया से बाबा विश्वनाथ के मंदिर की ओर जाते हुए भक्तों एवं पर्यटकों के आकषर्ण का केंद्र बनेंगे। लोग इन्हें देख सकेंगे। इनकी भी पूजा अर्चना कर सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का कोई भी काम निर्थक नहीं होता है।
काशी विश्वनाथ कॉरीडोर के लोकार्पण समारोह में सभी भाजपाशासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों सहित देश भर से अनेक धर्माचार्यों का उपस्थित रहना भी निर्थक नहीं था। प्रधानमंत्री के साथ नौकाविहार करते हुए, काशी के घाटों का सौंदर्य निहारते हुए, इन मुख्यमंत्रियों के ध्यान में अपने राज्यों के भी तीर्थस्थल एवं घाट जरूर आए होंगे, और उन्हें लेकर उनके मन में कुछ परिकल्पनाएं भी उभरी होंगी कि कैसे किसी तीर्थ क्षेत्र का विकास किया जा सकता है। निश्चित रूप से ये सारे मुख्यमंत्री अपने-अपने राज्यों में इन परिकल्पनाओं को साकार करने का प्रयास भी करेंगे। बात चाहे उत्तर प्रदेश में काशी-अयोध्या के पुनरोद्धार की हो, या उत्तराखंड में बाबा केदारनाथ धाम के पुनरोद्धार की, ये उपलब्धियां हर हिंदू का सीना गर्व से फुला देती हैं, माथा ऊंचा कर देती हैं।
इसमें कोई शक नहीं कि जब भी किसी आक्रांता ने हमारी धार्मिंक आस्थाओं पर हमला किया होगा, तो यही सोचकर किया होगा कि इसी बहाने वह विशाल हिंदू समाज को भयाक्रांत कर सके, उस पर अपना वर्चस्व सिद्ध कर सके। खुद को इतना ताकतवर दिखा सके कि कोई उसके सामने अपनी जायज मांगें भी लेकर न जा सके। उत्तर में बाबर, शाहजहां एवं औरंगजेब तो दक्षिण में टीपू सुल्तान जैसे बादशाह इसी मंशा के साथ हिंदुओं की धार्मिंक आस्थाओं पर लगातार सदियों तक चोट करते रहे, लेकिन हम हाथ-पर-हाथ धरे बैठे रहे, कुछ न कर सके। क्योंकि हम असंगठित थे। कभी रानी भवानी, अहिल्याबाई होल्कर या महाराजा रणजीत सिंह ने काशी विश्वनाथ मंदिर या ध्वस्त किए गए किसी अन्य धार्मिंक केंद्र के पुनरोद्धार का बीड़ा उठाया तो वह उनके स्तुत्य व्यक्तिगत साहस का परिणाम था। भारत के स्वतंत्र होने एवं एक आधिकारिक गणतंत्र के रूप में सामने आने के बाद पहले प्रभासतीर्थ में सोमनाथ का उद्धार, फिर अयोध्या में श्रीराम जन्मस्थान विवाद का निपटारा एवं भव्य मंदिर निर्माण की शुरुआत, और अब काशी विश्वनाथ कॉरीडोर का लोकार्पण वास्तव में हमारे संगठित गणतंत्र की बड़ी उपलब्धियां हैं।
आधुनिक भारत में महात्मा गांधी से लेकर सरदार पटेल, डॉ. राजेंद्र प्रसाद, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी जैसे अनेक महापुरु षों के मन में भारत की ध्वस्त की गई आस्थाओं को पुनरु ज्जीवन देने का भाव रहा है। उनके विभिन्न बयानों में यह देखा भी जा सकता है, लेकिन तब के भारत का राजनीतिक नेतृत्व न जाने किस संकोच में इन महापुरुषों की भावनाओं को मूर्तरूप देने या उनका सम्मान करने का साहस नहीं जुटा पाता था। आजादी के वर्षो बाद तक हिंदू समाज भी अपने ऐसे ही शासकों की ओर मूकदर्शक बना ताकता रहा, लेकिन उसे सेक्युलरिज्म के ढोंग के सिवा कुछ प्राप्त नहीं हुआ।
1985 के बाद विश्व हिंदू परिषद एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा शुरू किए गए श्रीराम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन से हिंदू समाज के संगठन की शुरुआत हुई। इसी आंदोलन की उपज प्रधानमंत्री मोदी आज काशी विश्वनाथ मंदिर सहित देश के अनेक धार्मिंक केंद्रों के उद्धारक बनकर सामने आए हैं। 2014 में जब उन्होंने काशी जाकर कहा था कि ‘उन्हें मां गंगा ने बुलाया है’, तो बहुत से लोगों ने उनके इस वाक्य का मजाक उड़ाया था।
आज काशी का निखरता वैभव देख ऐसे लोगों की जुबान भी बंद हो गई होगी। यह काम आसान नहीं था, लेकिन काशी के राजा विश्वनाथ जी का जिस पर वरदहस्त हो, वह क्या नहीं कर सकता। वही वरदहस्त आज प्रधानमंत्री मोदी पर साक्षात नजर आ रहा है। मां गंगा एवं विेर काशी विश्वनाथ के आशीर्वाद से ही नरेन्द्र मोदी इस लक्ष्य को पूरा कर सके हैं। काशी के नये रूप, नई सज्जा को देखकर आज संपूर्ण विश्व का हिंदू समाज विजयी महसूस कर रहा है, लेकिन वास्तविक विजय तो यह काशी विश्वनाथ की है। इसलिए गर्व से कहिए श्री काशी विश्वनाथो विजयतेतराम!
सुधार का दीपक
संपादकीय
भारत में धर्मस्थलों और तीर्थों के विकास की किसी भी पहल की प्रशंसा होनी ही चाहिए। काशी में विश्वनाथ धाम का जो विकास हुआ है, उसके लिए भगवान शिव की नगरी काशी के सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरा श्रेय दिया जाना चाहिए। धीरे-धीरे अतिक्रमण और व्यावसायिक दबाव की वजह से जिस तरह से विश्वनाथ धाम की उपेक्षा बढ़ती जा रही थी, जैसे-जैसे वहां पहुंचने की गलियां संकरी होती जा रही थीं, वैसे-वैसे काशी का आकर्षण भी कहीं न कहीं प्रभावित हो रहा था। धाम की ओर जाने वाली गलियों का चौड़ीकरण नामुमकिन लगता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहां से सांसद बनने से यह काम आसान हुआ। उन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि यदि सोच लिया जाए, तो असंभव कुछ भी नहीं है। प्रधानमंत्री की इस परियोजना के मार्ग में कतई कम अड़चनें नहीं थीं, दुकानों, लोगों को विस्थापित किया गया, दृढ़ता के साथ कुछ धर्मस्थल भी हटाए गए, चंद लोग तो आज भी राजनीतिक कारणों से विरोध जता रहे हैं, लेकिन एक भव्य मंदिर परिसर के रूप में परिणाम दुनिया के सामने है। काशी विश्वनाथ के परिसर में श्रद्धालुओं के लिए बहुत बड़ी जगह निकल आई है, जिससे इस धाम के आकर्षण में चार चांद लगना तय है।
काशी से प्रधानमंत्री ने जो संदेश दिया है, उसे केवल चुनावी नफा-नुकसान के नजरिये से नहीं देखना चाहिए। प्रधानमंत्री का यह कहना खास मायने रखता है कि सदियों की गुलामी के चलते भारत को जिस हीन भावना से भर दिया गया था, आज का भारत उससे बाहर निकल रहा है। वाकई यहां अब कोई संदेह शेष नहीं है कि यह सरकार देश व समाज को बदल रही है। प्रधानमंत्री अपने आलोचकों को खूब जानते हैं, अत: उन्होंने उचित ही कहा है कि आज का भारत सिर्फ सोमनाथ के मंदिर का सौंदर्यीकरण ही नहीं कर रहा, समुंदर में हजारों किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर भी बिछा रहा है। आज का भारत सिर्फ बाबा केदारनाथ धाम का जीर्णोद्धार ही नहीं कर रहा, आज का भारत सिर्फ अयोध्या में प्रभु श्रीराम का मंदिर ही नहीं बना रहा, हर जिले में मेडिकल कॉलेज भी बना रहा है। आज का भारत सिर्फ बाबा विश्वनाथ धाम को भव्य रूप ही नहीं दे रहा है, गरीबों को पक्के मकान भी बनाकर दे रहा है।
मतलब एक ही साथ विरासत और विकास की चिंता है। हिंदुत्व की चिंता है, तो विकास की भी पूरी फिक्र है। प्रधानमंत्री ने काशी से पूरा लेखा-जोखा दिया है कि कैसे धर्मक्षेत्रों और नगरों में सुधार के लिए काम हो रहे हैं। कुल मिलाकर, पूरे देश में गौरवशाली धार्मिक प्रतीकों का पुनरोद्धार ऐसे किया जा रहा है, जैसे पहले कभी नहीं किया गया था। इन सुधारों से न केवल आध्यात्मिक, बल्कि सामाजिक और आर्थिक लाभ के भी रास्ते खुल सकते हैं। हालांकि, भारत में अब भी अनेक तीर्थ ऐसे हैं, जो गंदगी का अड्डा बने हुए हैं। जहां खाद्य में मिलावट, ठगी, छीनाझपटी, चोरी की घटनाएं खूब होती हैं। नैना देवी का हादसा हो या जोधपुर की चामुंडा माता मंदिर के पास का हादसा, संकरी गलियों में भगदड़ कितनी जानलेवा साबित हुई है, यह अलग से बताने की जरूरत नहीं है। देश में बढ़ती आबादी और जीविका की तलाश में कोने-कोने में बाजार सजाने-लगाने की परिपाटी दुखद है। अब काशी में अगर सुधार का दीपक जल उठा है, तो उसकी रोशनी तमाम तीर्थों में भी सुधार के प्रति समर्पण बढ़ाएगी।
