
10-06-2025 (Important News Clippings)
To Download Click Here.
Date: 10-06-25
Always Emerging, Never Emerged?
Domestic consumption must plug shortfall in EMs
ET Editorials
Donald Trump’s efforts to set right the US’ trade balance with the rest of the world will impact global capitalflows. Here’s how it works now: the US runs up trade deficits with emerging markets (EMS), which then park their export surpluses in US equity and debt. The size of the US economy and the proclivity of its governments to over- spend corner an oversized slice of global capital. Driving global growth, EMs tend to get by on less capital than they need. This might change if Trump manages to wean EMs off their export addiction. A US economy less dependent on imports would not allow EM trade surpluses to balloon, and would not need matching capital flows to maintain its BoP. EMs, on their part, will have to raise their domestic consumption to keep growing faster than advanced economies.
BRICS has acquired a reasonable economic heft in relation to G7 and, tellingly, has quite a way to go in reaching the latter’s consumption levels. An economic structure that requires EMS to focus on domestic demand also frees up global capital for that specific purpose. Faster- growing EMs should build their capacity to absorb capital, as Morgan Stanley’s Gokul Laroia said in an interview to this paper. Otherwise, they will remain stranded in slower-moving advanced economies. This becomes a drag when EMs pull in better metrics on indebtedness than their rich cousins.
This economic reset will not be painless, though. EMs may have to confront difficult choices over slower export growth, without a guarantee of a faster rise in living standards. Turning economies inward also imposes productivity costs and may potentially affect momentum. Capital-chasing EM growth could be rerouted. These are tough calls for EM governments, but they have no choice but adapt to the new limits being set for globalisation. Trump’s reciprocal tariffs should shake EMs out of their complacency over rising trade surpluses. His trade rebalancing effort is, however, likely to be drawn out, providing EMs some space to adjust policy.
Date: 10-06-25
सुरक्षा परिषद की उप-समितियों में पाक क्यों है?
संपादकीय
सुरक्षा परिषद की आतंकवाद के खिलाफ बनी चार उप-समितियों में से एक में पाकिस्तान अध्यक्ष और तीन में पदाधिकारी चुना गया है। परिषद के स्थायी सदस्यों अक्सर आतंकवाद झेलने वाले अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन के अलावा हमारे मित्र रूस में से किसी ने इन नियुक्तियों का विरोध नहीं किया। पाकिस्तान तालिबान पर प्रतिबंध लगाने वाली उप-समिति का अध्यक्ष है। भारत से सामरिक झड़प के बाद पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की तालिबान सरकार से एक बार फिर दोस्ती का असफल प्रयास किया ताकि बलूचिस्तान विद्रोह को खत्म करने और भारत के खिलाफ मुहिम चलाने में मदद मिले। फिर ओसामा बिन लादेन को रावलपिंडी में मारने के बाद भी क्या अमेरिका को आतंकवाद में पाकिस्तानी भूमिका के लिए कोई और सबूत चाहिए? चिंता यह कि दशकों से भारत का साथ देने वाला रूस भी इस मुद्दे पर खामोश है और पुतिन के सहयोगी ने भारत-पाक संघर्ष विराम मैं ट्रम्प की भूमिका मानी है। पाकिस्तान को इन उप-समितियों में पद देने में सभी पांच स्थायी और दस अस्थायी सदस्यों के बहुमत की हामी चाहिए। सवाल इन समितियों के प्रभावशाली होने या न होने का नहीं है। क्या पाकिस्तान जैसे देश को आतंकवाद निरोधी किसी भी वैश्विक फोरम की लीडरशिप मिलना हमारी हार नहीं है? पाकिस्तान को ये मंच दिया जाना उसकी इज्जत अफजाई करने की तरह है।
Date: 10-06-25
देश में गरीबी घट रही है और इस पर दुनिया की नजर है
मिन्हाज मर्चेंट, ( लेखक प्रकाशक और सम्पादक )
क्या भारत में गरीबी दर घट रही है? और अगर ऐसा है, तो सरकार अभी भी 80 करोड़ से ज्यादा भारतीयों को मुफ्त अनाज क्यों दे रही है?
पहले सवाल का जवाब है- हां, भारत में गरीबी दर वाकई घट रही है, और पहले से कहीं ज्यादा तेजी से आरबीआई के पूर्व गवर्नर सी. रंगराजन की अध्यक्षता वाली समिति की नई रिपोर्ट के अनुसार गरीबी दर 2011-12 में 29.5% थी, जो 2023-24 में घटकर 4.9% हो गई है। यह एक असाधारण गिरावट है। रंगराजन कहते हैं गिरावट की दर पिछले 12 साल की अवधि में 2.02% प्रति वर्ष रही है।
तब सवाल उठता है कि अगर पिछले 12 सालों में गरीबी में इतनी नाटकीय गिरावट आई है, तो सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 806.7 मिलियन भारतीयों को मुफ्त अनाज क्यों दे रही है? इसका जवाब आंशिक रूप से राजनीतिक और आंशिक रूप से वैज्ञानिक है। मुफ्त खाद्यान्न योजना को गरीबों के वोटों के लिए शुरू किया गया था, लेकिन यह पोषण संबंधी सप्लीमेंट के लिए भी थी।
सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (सीएसई) एक प्रसिद्ध पत्रिका डाउन टु अर्थ प्रकाशित करता है। इसने एक रिपोर्ट का हवाला दिया कि भारत में हर साल 17 लाख से ज्यादा लोगों की कुपोषण से मृत्यु हो जाती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 71% भारतीय पौष्टिक भोजन नहीं खरीद सकते। हालांकि गरीबी दर गिरकर 4.9% हो गई है, लेकिन पोषण एक गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है। गरीब भारतीयों का एक बड़ा हिस्सा पौष्टिक आहार नहीं खरीद सकता। इसलिए मुफ्त खाद्यान्न सहायता दी जाती है। बचे हुए पैसों को ज्यादा पौष्टिक भोजन पर लगाया जा सकता है।
जैसा कि विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने अमेरिकी सेनेटर एलिसा स्लोटकिन से कहा- सेनेटर, आपने कहा कि लोकतंत्र आपकी मेज पर भोजन नहीं लाता। वास्तव में, दुनिया के जिस हिस्से में मैं रहता हूं, वहां ऐसा होता है। आज चूंकि हम एक लोकतांत्रिक समाज हैं, इसलिए हम 800 मिलियन से ज्यादा लोगों को पोषण सहायता और भोजन देते हैं।
विश्व बैंक ने भी भारतीय गरीबी में गिरावट की पुष्टि की है। इंडियन एक्सप्रेस में लिखते हुए सी. रंगराजन और एस. महेंद्र देव (प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष) ने बताया कि विश्व बैंक ने हाल ही में 100 से अधिक विकासशील देशों के लिए गरीबी और समानता संबंधी संक्षिप्त रिपोर्ट जारी की है। इसमें कहा गया है कि भारत ने पिछले दशक में गरीबी में उल्लेखनीय कमी की है। अत्यधिक गरीबी ( क्रय शक्ति समता के संदर्भ में प्रतिदिन 2.15 डॉलर से कम पर जीवन यापन करना) 2011-12 में 16.2% से घटकर 2022-23 में 2.3% हो गई। इस अवधि में 17 करोड़ से अधिक लोग अत्यधिक गरीबी की स्थिति से ऊपर उठ गए। निम्न मध्यम आय वाले देशों के लिए गरीबी रेखा के मानदंड से नीचे के लोगों की संख्या (प्रतिदिन 3.65 डॉलर) 61.8% से घटकर 28.1% हो गई। यदि गरीबी को परिभाषित करने के लिए घरेलू आय का कट-ऑफ स्तर बढ़ा दिया जाए, तो गरीबी दर तेजी से बढ़कर 28.1% हो जाती है। यह लगभग 50 करोड़ भारतीयों का जनसांख्यिकीय समूह है, जिसे पोषण संबंधी सहायता की आवश्यकता है।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत अतिरिक्त 30 करोड़ और लोगों को शामिल किया गया है, ताकि स्पष्ट चुनावी लाभ के साथ व्यापक जनसांख्यिकीय समूह तक भी पहुंचा जा सके।
भारत में गरीबी के निरंतर प्रसार के बावजूद गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या में कमी देखी जा सकती है। 1947 में स्वतंत्रता के बाद से भारत में अकाल नहीं पड़ा है। जबकि ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के 190 वर्षों के दौरान 31 बड़े अकाल पड़े थे, जिनमें से आखिरी 1943 का बंगाल अकाल था। उसमें 30 लाख लोग मारे गए थे।
रंगराजन गरीबी दर में गिरावट को जीडीपी में वृद्धि से सही ढंग से जोड़ते हैं। वे लिखते हैं कि गरीबी का निर्धारण जीडीपी वृद्धि, कीमतों और सेफ्टी नेट जैसे फैक्टर्स से होता है। जीडीपी वृद्धि 2022-23 में 7.6% से बढ़कर 2023-24 में 9.2% हो गई, यानी एक वर्ष में 1.5% की वृद्धि। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) 2022-23 में 6.7% से घटकर 2023-24 में 5.4% हो गया यानी 1.3% अंकों की गिरावट | हालांकि इसी अवधि के दौरान खाद्य मुद्रास्फीति 6.6% से बढ़कर 7.5% हो गई है। ऐसे में लगता नहीं कि अगले चरण में कल्याणकारी कार्यक्रमों में कोई महत्वपूर्ण बदलाव होगा।
Date: 10-06-25
अमेरिका को महान से सामान्य बनाते ट्रंप
शिवकांत शर्मा, ( लेखक बीबीसी हिंदी के संपादक रहे हैं )
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को ‘मागा यानी फिर से महान’ बनाने के लिए दो मोर्चे खोल रखे हैं। बाहरी मोर्चे पर वह अमेरिका के दोस्तों और दुश्मनों से टैरिफ जंग लड़ रहे हैं। भीतरी मोर्चे पर अपनी शैक्षिक और प्रशासनिक संस्थाओं को वोक या वामपंथी विचारधारा के शिकंजे से मुक्त कराने की जंग लड़ रहे हैं। उनका मानना है कि टैरिफ जंग के बिना निरंतर बेकाबू हो रहे व्यापार घाटे को कम और निर्माण उद्योग को बहाल नहीं किया जा सकता। इसी तरह संस्थाओं को वौक विचारधारा से मुक्त कराए बिना दक्षिणपंथी विचारधारा को वहां जगह नहीं मिल सकती। महाशक्ति होने के बावजूद जंग के मोर्चों पर अमेरिका का रिकार्ड बहुत उत्साहजनक नहीं रहा है। दूसरे विश्वयुद्ध के बाद वह वियतनाम से लेकर अफगानिस्तान तक किसी जंग में स्पष्ट जीत नहीं हासिल कर पाया। इसलिए अमेरिका के अधिकांश लोग इन दोनों मोर्चों पर अमेरिका के संभावित नुकसान को लेकर चिंतित हैं। टैरिफ जंग से होने वाले नुकसान से भी बड़ी चिंता उन शैक्षिक संस्थाओं के खिलाफ छेड़ी गई जंग को लेकर है, जिनका अमेरिका को महाशक्ति बनाने में अप्रतिम योगदान रहा है।
इसमें दो राय नहीं कि कोलंबिया, हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड जैसे विश्वप्रसिद्ध अमेरिकी विश्वविद्यालय उत्कृष्टता एवं अनुसंधान के केंद्रों की जगह राजनीति प्रेरित विचारधाराओं का अखाड़ा बनते जा रहे हैं। इसके कारण देहात और छोटे शहरों में रहने वालों का एक बड़ा वर्ग मानने लगा है कि अमेरिका के शीर्ष विश्वविद्यालयों के स्नातकों में वोक विचारधारा भर रही है। इसलिए बहाना भले ही यहूदी विरोध को समाप्त करने का हो, पर ट्रंप ने असल में अपने जनाधार को बचाने के लिए यह जंग छेड़ी है। विश्वविद्यालयों से कहा जा रहा है कि छात्रों और प्राध्यापकों के चयन की प्रक्रिया, उनकी वैचारिक पृष्ठभूमि, पाठ्यक्रमों का वैचारिक संतुलन और परिसर की गतिविधियों का विवरण साझा करें। न करने पर केंद्रीय अनुदान बंद करने, टैक्स छूट समाप्त करने और विदेशी छात्रों के वीजा रोकने रद करने की धमकियां दी जा रही हैं। ऐसी शर्तें मानने के बावजूद कोलंबिया विश्वविद्यालय का अनुदान रोक लिया गया। हार्वर्ड ने अपनी स्वायत्तता का हवाला देकर सरकार को अदालत में चुनौती दी। इसके बाद विदेशी छात्रों का वीजा रोकने के सरकारी आदेश को स्थगित कर दिया गया।
विश्वविद्यालय और अकादमियां अमेरिका की वैज्ञानिक, आर्थिक और सामरिक शक्ति का स्रोत रही हैं। दुनिया भर से श्रेष्ठतम प्रतिभाएं पढ़ने-पढ़ाने और शोध करने यहां आती हैं। वे नई-नई खोज करती हैं, उनका कारोबार एवं जीवन के विभिन्न पहलुओं में प्रयोग करती हैं और अमेरिका के विकास को गति देती हैं। विकास और शक्ति की दौड़ में अमेरिका के सबसे प्रबल प्रतिद्वंद्वी चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने भी अपने बच्चों को पढ़ने के लिए हार्वर्ड भेजा था। राष्ट्रपति रीगन के शब्दों में, अमेरिका में आपकी पृष्ठभूमि को नहीं, सपनों को महत्व दिया जाता है। यही अमेरिका का सबसे बड़ा आकर्षण रहा है। इस अकादमिक आजादी पर बंदिशों और निगरानियों के अंकुश लगाने पर प्रतिभाएं दूसरे ठिकाने खोज लेंगी। हिटलर के जमाने तक विज्ञान और अनुसंधान में सबसे बड़ी शक्ति जर्मनी था । विज्ञान के एक तिहाई नोबेल पुरस्कार जर्मन जीतते थे, जिनमें अधिकांश यहूदी होते थे। हिटलर के अत्याचारों से भागकर वे सब अमेरिका चले गए और तब से अमेरिका विज्ञान एवं अनुसंधान की सबसे बड़ी महाशक्ति बना हुआ है। विज्ञान के 41 प्रतिशत से अधिक नोबेल पुरस्कार अमेरिकी जीतते हैं। दुनिया की सौ चोटी के विश्वविद्यालयों में से 36 अमेरिका के हैं, जो अमेरिका की आर्थिक सामरिक शक्ति की निर्माणशालाएं हैं। अमेरिका के इस एकछत्र राज में अब चीन सेंध मार रहा है। विज्ञान के 82 प्रतिष्ठित शोधपत्रों में छपने वाले शोध लेखों की गुणवत्ता और संख्या के आधार पर शोध संस्थाओं का वर्गीकरण नेचर पत्रिका करती है। इसमें शामिल पहली 10 शोध संस्थाओं में हार्वर्ड को छोड़कर बाकी नौ चीन की हैं। गनीमत है कि हार्वर्ड इस तालिका में चोटी पर है। नए आविष्कारों के पेटेंट के मामले में तो अमेरिका चीन के आसपास भी नहीं। उनके लिए करीब आधे आवेदन अब अकेले चीन से आते हैं। हां, प्रतिभाओं को आकर्षित करने में अमेरिका अब भी चीन से बहुत आगे हैं। हर साल दुनिया के 11 लाख से अधिक प्रतिभावान छात्र पढ़ने और शोध करने अमेरिका आते हैं। इनमें से एक तिहाई अकेले भारत के होते हैं। विज्ञान के नोबेल पुरस्कार जीतने वाले अमेरिकियों में से एक तिहाई आप्रवासी होते हैं। साफ्टवेयर बनाने वालों में 40 प्रतिशत आप्रवासी हैं और कैंसर संस्थानों में 60 प्रतिशत तक आप्रवासी विज्ञानी हैं। अमेरिका की 10 सबसे बड़ी कंपनियों में से पांच के प्रमुख आप्रवासी हैं। इनमें से दो भारतवंशी हैं।
चिंता इसकी है कि विश्वविद्यालयों के खिलाफ छिड़ी जंग से अमेरिका चीन पर हासिल अपनी उस बढ़त को भी गंवा सकता है, जो उसे विश्व की प्रतिभाओं को आकर्षित करने में हासिल है। विश्वविद्यालयों में विदेशी प्रतिभाओं का आना कम होने के साथ अमेरिकी प्रतिभाओं का पलायन भी शुरू हो गया है। गत अप्रैल में नेचर पत्रिका के एक सर्वेक्षण में भाग लेने वाले 1,600 से अधिक अमेरिकी विज्ञान शोधकर्ताओं में से 75 प्रतिशत ने कहा कि वे अमेरिका छोड़कर यूरोप, कनाडा और आस्ट्रेलिया जाने पर विचार कर रहे हैं। हार्वर्ड समेत अन्य अमेरिकी विश्वविद्यालयों में प्रवेश पाने वाले हजारों भारतीय छात्रों को अमेरिका में अपने भविष्य की चिंता सताने लगी है।
अमेरिकी विश्वविद्यालयों में पैदा हुए संकट का भारत के लिए सबसे बड़ा सबक और अवसर यह है कि इसे अपने छात्रों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए अपने शिक्षा संस्थानों में अनुसंधान एवं नवाचार का स्तर सुधारना और उसे परिणामोन्मुखी बनाना चाहिए। भारत का एक भी विश्वविद्यालय दुनिया के सौ श्रेष्ठतम विश्वविद्यालयों में नहीं है। जब चीन के पांच विश्वविद्यालय इस तालिका में स्थान पा सकते हैं तो भारत के क्यों नहीं? देश का विकास केवल तक्षशिला और नालंदा की महत्ता गाने से नहीं, आज की यूनिवर्सिटियों को वैसा बनाने और यह सुनिश्चित करने से होगा कि वे राजनीति के अखाड़े बनने की जगह प्रायोगिक अनुसंधान और नवाचार के केंद्र बनें।

Date: 10-06-25
भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में कृषि की होगी अहम भूमिका
हिमांशु पाठक और पी के जोशी, ( लेखक क्रमशः राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी, नई दिल्ली में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष हैं )

नीति आयोग की 10वीं संचालन परिषद की बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प दोहराया है। 2047 में देश अपनी स्वतंत्रता की 100वीं वर्षगांठ भी मनाएगा। कृषि क्षेत्र नवाचार, आर्थिक ताकत और पर्यावरणीय वहनीयता के माध्यम से इस लक्ष्य की पूर्ति में अग्रणी भूमिका निभा सकता है।
भारतीय कृषि में क्रांतिकारी बदलाव आए हैं और इसने भारत को खाद्यान्न की कमी का सामना करने वाले देश से खाद्य अधिशेष राष्ट्र बना दिया है। पूरी दुनिया कृषि क्षेत्र में भारत की प्रगति का लोहा मान रही है। खाद्यान्न उत्पादन में शानदार प्रगति हुई है। 1950-51 में देश में खाद्यान्न उत्पादन 5.08 करोड़ टन था मगर 2024-25 में यह 35.39 करोड़ टन के साथ उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। वर्ष 2023- 24 में भारत से कृषि निर्यात 4.08 लाख करोड़ रुपये के बराबर पहुंच गया।
विशेषताएं और चुनौतियां
कृषि विस्तार की भूमिका देश को विकसित बनाने के लक्ष्य में काफी महत्त्वपूर्ण होगी। हालांकि, यह भी सच है कि कृषि क्षेत्र स्वयं इस समय कई चुनौतियों से जूझ रहा है जिनमें जोत का घटता आकार, जलवायु परिवर्तन, संसाधनों का ह्रास, उपभोक्ता मांगों में बदलाव और तेजी से बढ़ती वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा आदि शामिल हैं। हालांकि, इसके साथ ही जैव-तकनीकी, परिशुद्ध कृषि, डिजिटल कृषि और टिकाऊ व्यवहारों में प्रगति से असंख्य संभावनाएं भी सामने आई हैं।
लचीलेपन और संपन्नता के लिए शोध
भारत में कृषि शोध कार्यों में जीनोमिक्स एवं जैव- तकनीकी, जलवायु में परिवर्तन सहन करने की क्षमता रखने वाली कृषि, परिशुद्ध एवं डिजिटल कृषि और टिकाऊ संसाधन प्रबंधन प्राथमिकता में शामिल होने चाहिए। शोध प्राथमिकताओं में कृषि विविधता भी शामिल होना चाहिए जिसका इस्तेमाल बागवानी, मवेशी और मत्स्य क्षेत्रों में संभावनाओं का लाभ लेने के लिए किया जा सकता है। आवश्यकता आधारित कृषि यंत्रीकरण, कृषि- प्रसंस्करण और कटाई के बाद फसलों का नुकसान कम से कम रखने पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। इसके अलावा कृषि – शोध नीतिगत सुधारों, बुनियादी ढांचों के आधुनिकीकरण और अद्यतन बाजार पहुंच को भी समर्थन मिलना चाहिए। वैज्ञानिकों को शौध के लिए नई तकनीकों जैसे सीआरआईएसपीआर जीन एडिटिंग, रिमोट सेंसिंग एवं भौगोलिक सूचना तंत्र, आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (एआई) एवं मशीन लर्निंग आदि का इस्तेमाल करना चाहिए।
नए नेतृत्वकर्ताओं का उद्भव
कृषि शिक्षा को केवल परंपरागत ढांचे तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए और इससे आगे निकलकर एक व्यापक एवं भविष्योन्मुखी नजरिया अपनाना चाहिए। कृषि में एआई, कृषि उद्यमशीलता, जलवायु अनुकूल कृषि, पर्यावरण अनुकूल कृषि, कृषि कारोबार प्रबंधन और कृषि निर्यात रणनीति जैसे विषयों को शामिल करने के लिए कृषि पाठ्यक्रम में सुधार किया जाना चाहिए। छात्रों की अगुवाई वाली स्टार्टअप इकाइयों के विकास के लिए कृषि – इन्क्यूबेटर विकसित किया जाना चाहिए। कृषि विश्वविद्यालयों को वैश्विक विश्वविद्यालयों और शोध तंत्रों के साथ सहयोग कर विश्व स्तरीय शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए ।
नई तकनीक का प्रसार
तकनीक के जल्द एवं प्रभावी प्रसार के लिए विस्तार सेवाओं को मोबाइल ऐप्लिकेशन, किसान हेल्पलाइन, ऑनलाइन सलाहकार प्लेटफॉर्म, व्हाट्सऐप ग्रुप और यूट्यूब ट्यूटोरियल्स का लाभ उठाना चाहिए। कृषि विज्ञान केंद्रों का आधुनिकीकरण जरूरी है और इसके लिए उन्हें उच्च कृषि-तकनीक एवं डेटा आधारित सलाहकार सेवाओं से जोड़ा जाना चाहिए। उन्हें नवाचार एवं कौशल विकास के केंद्र के रूप में विकसित करने से कृषि उत्पादन भी बढ़ेगा। किसान- उत्पादक संगठनों को विपणन एवं ज्ञान के प्रसार के केंद्र के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल, गैर-सरकारी संगठनों के जुड़ाव और ग्रामीण स्टार्टअप इकाइयों के साथ सहयोग से एक जीवंत कृषि विस्तार प्रणाली तैयार की जा सकती है।
कृषि शोध एवं विकास में निवेश
इस समय कृषि शोध एवं विकास में पर्याप्त निवेश नहीं हो रहा है और इस पर खर्च अंतरराष्ट्रीय मानदंडों से काफी कम है। भारत अपने सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 0.65 फीसदी हिस्सा शोध एवं विस्तार पर खर्च करता है। कृषि शोध एवं विकास पर भारत के जीडीपी का कम से कम 1 फीसदी हिस्सा खर्च किया जाना चाहिए तभी कृषि क्षेत्र में तकनीक का इस्तेमाल बढ़ेगा और यह दुनिया में दूसरे देशों को टक्कर दे पाएगा।
जिस विकसित भारत की कल्पना की जा रही है वह ऐसा ही हो सकता है कि उसमें प्रत्येक किसान को श्रेष्ठ विज्ञान एवं तकनीक की सुविधा मिले और ग्रामीण युवा कृषि उद्यमी बनने का सपना देख पाएं। विकसित भारत में ग्राम संकुलों में नवाचार बढ़ेगा और कृषि सम्मानित, लाभकारी एवं प्रतिष्ठित पेशा बन पाएगा ।
Date: 10-06-25
हिंसा की आग
संपादकीय
मणिपुर में कुछ दिनों की शांति के बाद फिर से हिंसा भड़क उठी है। जगह-जगह विरोध प्रदर्शन और आगजनी की घटनाएं हो रही हैं सड़कों पर सुरक्षा बलों का सख्त पहरा है। कई इलाकों में निषेधाज्ञा लागू है और इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं। इससे पहले भी राज्य को कई मर्तबा हिंसा की त्रासदी झेलनी पड़ी है। इस बार हिंसा का प्रत्यक्ष कारण भले ही मैतेई समुदाय के एक नेता समेत पांच लोगों की गिरफ्तारी है, लेकिन इसके तार वर्ष 2023 में हुई जातीय हिंसा से ही जुड़े हुए हैं। सवाल है कि जातीय आधार पर लोगों के गुस्से का ज्वार आखिर शांत क्यों नहीं हो रहा है? लोगों को भावनात्मक रूप से भड़काने के पीछे कौन है ? ऐसी क्या वजह है कि लोग किसी सामान्य घटना को भी समुदाय से जोड़ लेते हैं और सड़कों पर उतर कर उग्र व्यवहार करने लगते हैं?
मणिपुर में वर्ष 2023 से जातीय संघर्ष चल रहा है। तब से हिंसा में कई लोगों की जान जा चुकी है और मैतेई और कुकी दोनों ही समुदायों के हजारों लोगों को विस्थापन का दर्द भी झेलना पड़ा है। हिंसा का सिलसिला जारी रहने की वजह से एन बीरेन सिंह को इस साल फरवरी में मुख्यमंत्री पद गंवाना पड़ा था। उसके बाद से यहां राष्ट्रपति शासन लागू है। तब से राज्य में हिंसा की कोई बड़ी घटना सामने नहीं आई । माना जा रहा था कि अब हालत सामान्य हो रहे हैं। मगर राज्य के सिर पर शांति का यह सेहरा ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाया। दरअसल, सीबीआइ ने गत रविवार को मैतेई संगठन अरंमबाई तेंगोल (एटी) के सदस्य कानन सिंह को गिरफ्तार किया था। इसके अलावा चार अन्य लोगों की भी गिरफ्तारी हुई। इन सब पर वर्ष 2023 में हुई हिंसा से संबंधित विभिन्न आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त होने का आरोप है। जांच एजेंसी का कहना है कि आरोपी कानन सिंह मणिपुर पुलिस में हेड कांस्टेबल था, लेकिन उसे मार्च 2025 को हथियारों की तस्करी सहित विभिन्न आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त होने के कारण बर्खास्त कर दिया गया था।
सीबीआइ की इस कार्रवाई के बाद राज्य के विभिन्न हिस्सों में हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गए। इस पूरे घटनाक्रम में गौर करने वाली बात यह है कि अगर किसी व्यक्ति पर हिंसक एवं आपराधिक घटनाओं में संलिप्त होने के आरोप में कार्रवाई होती है, तो इसे समुदाय विशेष से जोड़ कर क्यों देखा जा रहा है। जांच के जरिए इस बात का पता लगाने की जरूरत है। कि कहीं कोई लोगों की भावनाओं को भड़का कर अपने निजी स्वार्थ हासिल करने की कोशिश तो नहीं कर रहा है? साथ ही प्रशासनिक अमले और जनप्रतिनिधियों की भी यह जिम्मेदारी बनती है कि वे जन आक्रोश को शांत करने के लिए संबंधित लोगों के साथ तत्काल संवाद कायम करें। प्रदर्शनकारियों को भी यह बात समझनी होगी कि हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकती। अगर उनके नेता पर लगे आरोपों को लेकर किसी तरह का संदेह है, तो न्यायपालिका पर विश्वास रखना चाहिए। सड़कों पर उत्पात मचाने और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से कुछ हासिल नहीं होगा।
Date: 10-06-25
दरकते रिश्ते
संपादकीय
भारत में विवाह एक पवित्र बंधन है, जिसमें जीवन भर के रिश्ते की बुनियाद पड़ती है। एक विश्वास के साथ युगल अपने नए जीवन की यात्रा आरंभ करता है। पति और पत्नी दोनों को भरोसा होता है कि जब भी वे मुश्किल डगर पर होंगे, तो एक-दूसरे को संभाल लेंगे। इंदौर के राजा रघुवंशी शादी के एक हफ्ते बाद अपनी मधुर स्मृतियों को सहेजने के लिए पत्नी के साथ जब मेघालय गए होंगे, तब उन्हें पता नहीं होगा कि वे कभी लौट कर घर नहीं आएंगे और उनका हनीमून एक भयावह घटना में बदल जाएगा। शिलांग में पर्यटन के दौरान यह नवयुगल लापता हो गया था। इसके बाद एक खाई में राजा का शव मिला। तब से उनकी पत्नी सोनम गायब थी। पुलिस उसे ढूंढ़ती रही। सात दिन बाद पता चला कि वह गाजीपुर में है। इसके बाद देश को झकझोर देने वाली इस घटना से पर्दा उठ गया। पुलिस का दावा है कि सोनम ने ही पति की हत्या भाड़े के हत्यारों से कराई है। उसने आत्मसमर्पण जरूर कर दिया है, लेकिन सवाल उठता है कि अगर उसे आपत्ति थी, तो उसने यह शादी ही क्यों की?
पिछले एक अरसे में नवदंपतियों के बीच बढ़ते अविश्वास और मतभेद के कारण कलह, मारपीट और तलाक के मामले बढ़े हैं। जीवन भर एक-दूसरे का साथ निभाने का जो वचन दिया जाता है, वह कुछ दिनों या महीनों में टूटने लगता है। दोनों पक्ष के परिवारों के समझाने-बुझाने पर भी कई बार पति- पत्नी साथ नहीं रहते और नवयुगल का घरौंदा बसने से पहले ही उजड़ जाता है। मगर सवाल है कि वे कौन से कारण हैं, जिनकी वजह से नवदंपतियों में टकराव की नौबत पैदा होती है। इसे समझना होगा। दरअसल, इसके पीछे अति महत्त्वाकांक्षा, सुख- सुविधाएं और अवैध संबंध तो हैं ही, वहीं परिवार के दबाव में अनिच्छा से की गई शादी भी बड़ी वजह है। फिलहाल सोनम पर जो गंभीर आरोप लगे हैं, इसका जवाब अब उसी को देना है। मगर, इस घटना ने सभी को झकझोर दिया है।
Date: 10-06-25
रिश्तों का खून न हो
संपादकीय
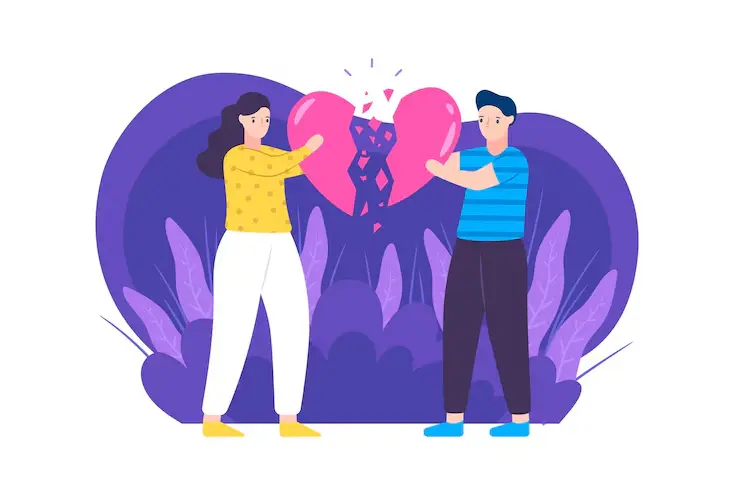
मेघालय में हुए हनीमून मर्डर के पीछे की जो सच्चाइयां सामने आ रही हैं, उन्हें लेकर समाज में न केवल गहरी चिंता, बल्कि नाराजगी का भी आलम है। एक दुल्हन जिसका विवाह मात्र सात दिन पहले हुआ था, उसने अपने कथित प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की साजिश रच डाली! तीन अपराधियों से अनुबंध किया और पति की हत्या के बाद खुद भाग खड़ी हुई। कुछ दिन फरार रहने के बाद उसने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में तब समर्पण किया, जब हत्या के अन्य तीन आरोपी पकड़े गए। तरह-तरह के कयास लगाए जा रहे थे, पर अब लगभग साफ हो चुका है कि सोची-समझी साजिश के तहत हत्या को अंजाम दिया गया है। इससे कई तरह के सवाल खड़े हो गए हैं ? मूलभूत सवाल तो यही है कि हमें रिश्तों पर कितना यकीन करना चाहिए ? पति- पत्नी के रिश्ते में जो बुनियादी यकीन और समझदारी चाहिए, वह क्या धीरे-धीरे छीजने लगी है? एक समय था, जब नए जोड़े को कुछ दिनों तक लोग घर से नहीं निकलने देते थे, पर व्यक्तिगत आजादी के दौर में एक चलन हनीमून का भी आया। अब अगर हनीमून के दौरान हत्या की नौबत आने लगे, तो हनीमून का क्या मतलब रह जाएगा ?
हनीमून तो दूल्हा और दुल्हन के लिए एक-दूसरे को जानने-समझने का अवसर है। वैसे रिश्तों में एक-दूसरे को जानना एक सतत प्रक्रिया है। राजा रघुवंशी तो अपनी पत्नी सोनम को समझने की कोशिश में लगे थे, पर सोनम के इरादे शायद पहले से ही नेक नहीं थे। अब यहां एक बड़ा सवाल है कि सोनम को जब किसी और से प्यार था, तो उसने राजा रघुवंशी से विवाह क्यों किया ? अगर किसी मजबूरी में विवाह करना ही पड़ा, तो उसके बाद भी सोनम के पास शादी से किनारा करने का मौका था । हनीमून के लिए खुद मेघालय को चुनना और वहां पहुंचकर हत्या को अंजाम देना निर्ममता ही नहीं, अक्षम्य अपराध है। आज युवाओं को सबक लेते हुए वाज़िब ढंग से मुखर होना चाहिए। उनके पास अपनी बात रखने और मनवाने के अनेक उपाय व साधन हैं, पर पता नहीं क्यों युवा कई बार उचित कदम उठाने से चूक जाते हैं? एक सवाल यह भी खड़ा हुआ है कि क्या आज के युवाओं के पास सच्चे दोस्तों का टोटा हो गया है? क्या आज युवा ऐसे लोगों के संपर्क में नहीं हैं, जो उन्हें निःस्वार्थ सही सलाह दे सकें?
यहां केवल सोनम का नहीं, उनके परिजनों का भी कुछ दोष है, जो सोनम के मन और मानसिकता को समय रहते समझ न पाए। अनेक परिवारों में पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी पर अपनी मर्जी थोपने से बाज नहीं आती है। वास्तव में, यह हत्याकांड पति-पत्नी के रिश्ते के बीच ही नहीं, बल्कि परिवार के अंदर भी सामान्य तालमेल की कमी का भयावह परिणाम है। पति-पत्नी के बीच बुनियादी समझ तो होनी ही चाहिए, ताकि दोनों एक-दूसरे को कम से कम किसी भी तरह का नुकसान न पहुंचाएं। दोनों अपने और परिवार के स्नेह व सम्मान की रक्षा के लिए सचेत हों। दोनों समाज के लिए ताकत व समाधान बनें, कमजोरी या समस्या नहीं। रिश्ते ठीक से निभाने की कोशिश वास्तव में इंसानियत है, जिसे भूलना नहीं चाहिए। गीतकार साहिर लुधियानवी का वह प्रसिद्ध गीत हर किसी के ध्यान में रहना चाहिए, जो आज अनायास मौजूं हो गया है वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन / उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा … । राजा और सोनम का अफसाना जिस बदसूरत या खौफनाक अंजाम तक पहुंच गया, वैसा फिर किसी के साथ न हो, इसके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए।
Date: 10-06-25
बेंगलुरु भगदड़ से उठे सवालों के जवाब जल्द देने पड़ेंगे
एस. श्रीनिवासन, ( वरिष्ठ पत्रकार )
फिर से वही कहानी दोहराई गई है। एक जीत का जश्न मनाने भारी भीड़ जमा होती है। यह जश्न 17 साल में पहली बार आरसीबी द्वारा आईपीएल जीतने के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा था । आयोजक, पुलिस और प्रशासन प्रशंसकों के उन्माद की कल्पना करने में विफल रहते हैं। नतीजतन, भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो जाती है और कम से कम 75 लोग घायल हो जाते हैं। इस तरह यह पूरा आयोजन एक बड़ी त्रासदी में बदल जाता है।
एक दिन बाद जब पीड़ितों और बचे लोगों के परिजनों ने खुद को संभालना शुरू किया, तो आरोप-प्रत्यारोप का खेल भी शुरू हो गया। विपक्ष ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप-मुख्यमंत्री डी के शिवकुमार के इस्तीफे की मांग की। मगर सरकार और कांग्रेस पार्टी के भीतर ही एक बड़ा विवाद सामने आ गया, जिसने सरकार की प्रतिष्ठा को धूमिल करने का काम किया। जाहिर है, यह शासकीय विफलता थी और राजनीतिक नेतृत्व बलि का बकरा तलाश रहा था। बेशक, यह आरसीबी के लिए कोई साधारण जीत नहीं थी। वर्षों की मेहनत, पसीने बहाने, कमी व निराशा के बाद यह आई थी। यही कारण है, जब अहमदाबाद से ट्रॉफी जीतने की खबर यहां पहुंची, तो लोग खुशी से झूम उठे और सार्वजनिक कार्यक्रम की सूचना मिलते ही मध्य बेंगलुरु में जमा होने लगे। राजनीतिक वर्ग भी इसमें कूद पड़ा। मुख्यमंत्री के कार्मिक व प्रशासनिक सुधार विभाग ने सम्मान की योजना बनानी शुरू कर दी। आरसीबी ने चार्टर्ड विमान से खिलाड़ियों को यहां बुलाया। उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार खुद उनकी अगवानी करने पहुंच गए। विधानसौध (विधानसभा) के सामने भव्य सार्वजनिक स्वागत समारोह की योजना बनाई गई। स्वागत समारोह के बाद एक विजय यात्रा की भी योजना बनी।
इस बीच, उप-मुख्यमंत्री के करीबी ए शंकर की अगुवाई वाली कर्नाटक राज्य क्रिकेट एसोसिएशन ने आरसीबी के साथ मिलकर विधानसौध से महज एक किलोमीटर दूर स्टेडियम के अंदर समारोह आयोजित करने के लिए इवेंट मैनेजमेंट कंपनी डीएनए इंटरटेनमेंट से बात कर ली। पुलिस कमिश्नर इन सबसे खफा थे और उन्होंने बताया कि लगातार तीन आयोजन ( एक विधानसभा के सामने, दूसरा रोड शो और तीसरा चिन्नास्वामी स्टेडियम का आयोजन ) का प्रबंधन मुश्किल हो सकता है। कहा जा रहा है, मुख्यमंत्री ने आपत्ति तो जताई, लेकिन कोई हस्तक्षेप नहीं किया। तब किया गया कि डीके शिवकुमार पूरे मामले को देखेंगे। विधानसौध के कार्यक्रम में करीब 40,000 लोग शामिल हुए। यहां भी कुछ हंगामा हुआ, पर स्थिति संभाल ली गई। विधानसौध से चिन्नास्वामी स्टेडियम तक का रोड शो रद्द कर दिया गया, लेकिन स्टेडियम के आयोजन में केवल आमंत्रित लोगों के शामिल होने की खबर उत्साही क्रिकेट प्रेमियों तक नहीं पहुंच सकी।
इस हादसे के बाद विपक्ष ने तो मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग की, मगर विभिन्न खेमों से जुड़े कांग्रेस नेताओं ने भी एक-दूसरे पर कुप्रबंधन के आरोप लगाए। मुख्यमंत्री द्वारा कैबिनेट बैठक बुलाने से ठीक पहले राहुल गांधी ने सरकार को फटकार लगाई। नतीजतन, कार्रवाई शुरू हो गई। शहर पुलिस आयुक्त के साथ-साथ चार अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को निलंबित किया गया और खुफिया प्रमुख का तबादला कर दिया गया। मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार भी बर्खास्त किए गए। न्यायिक जांच के आदेश दिए गए।
फिलहाल कई सवाल हैं, जिनके जवाब जरूरी हैं। टूनमिंट के अगले ही दिन कार्यक्रम क्यों आयोजित किया गया ? जब पुलिस ने सवाल उठाए थे, तब भी कर्नाटक क्रिकेट एसोसिएशन ने कार्यक्रम को आगे क्यों बढ़ाया ? गृह मंत्री जी परमेश्वर को इन सब बातों की जानकारी क्यों नहीं दी गई ? सिद्धारमैया, जो एक कुशल शासक माने जाते हैं, आखिर स्थिति को संभालने में विफल क्यों रहे? क्या उप-मुख्यमंत्री शिवकुमार ने उनको भरोसे में नहीं लिया? क्या उनके कथित दबदबे के कारण यह घटना हुई ? मुख्यमंत्री ने यह कहते हुए इस प्रकरण को खत्म करने की कोशिश की है कि नौकरशाही अपना काम करने में विफल रही। मगर ऐसा नहीं चलेगा, उन्हें जिम्मेदारी लेनी ही चाहिए।