
09-07-2018 (Important News Clippings)
To Download Click Here.
ठीक नहीं कर्ज माफी का सिलसिला
संजय गुप्त, (लेखक दैनिक जागरण समूह के सीईओ व प्रधान संपादक हैं)
कर्नाटक में जद(एस) और कांग्रेस की साझा सरकार ने अपने पहले बजट में किसानों की कर्ज माफी का ऐलान करके नए सिरे से यह रेखांकित किया कि अपने देश में वोट बैंक के लालच में ऐसे लोक-लुभावन कदमों का सिलसिला थमने वाला नहीं है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने 34 हजार करोड़ रुपए के कर्ज माफ करने के फैसले को इस आधार पर सही बताया कि उनके दल के साथ-साथ कांग्रेस के भी घोषणा-पत्र में किसानों का कर्ज माफ करने का वादा किया गया था। यह एक विडंबना है कि आज करीब करीब हर राजनीतिक दल किसान कर्ज माफी की बात कर रहा है। ऐसी बातें उन राज्यों में भी की जा रही हैं, जहां पहले किसानों के कर्ज माफ किए जा चुके हैं। कर्नाटक में कुमारस्वामी के पहले सिद्दारमैया ने भी किसानों के कर्ज माफ किए थे। वैसे किसान कर्ज माफी का सिलसिला संप्रग-एक सरकार के अंतिम साल में तब शुरू हुआ था, जब मनमोहन सरकार ने किसानों के 72000 करोड़ रुपए के कर्ज माफ किए थे।
उस समय विपक्ष में रही भारतीय जनता पार्टी ने इस फैसले का यह कहते हुए विरोध किया था कि यह सही नीति नहीं है और इससे देश की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ेगा। चूंकि कांग्रेस को चुनाव में इस फैसले का राजनीतिक लाभ मिला और उसके नेतृत्व में फिर से संप्रग सरकार बनी, इसलिए राजनीतिक दलों में किसान कर्ज माफी की घोषणा करने में होड़-सी लग गई। बीते एक-डेढ़ साल में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब समेत करीब एक दर्जन राज्य सरकारों ने किसानों के कर्ज माफ किए हैं। कर्नाटक में इस साल जद(एस) और कांग्रेस ने एक-दूसरे के खिलाफ विधानसभा चुनाव लड़ा। दोनों में से कोई भी इस चुनाव में सरकार बनाने लायक सीटें नहीं जीत पाया, लेकिन भाजपा को सत्ता से दूर रखने के लिए वे एक साथ आ गए। एक तरह से जनादेश जद(एस) या फिर कांग्रेस के घोषणा-पत्र के पक्ष में नहीं था, लेकिन साझा सरकार बनने के बाद कांग्रेस इसके लिए लगातार दबाव बना रही थी कि कर्ज माफी का फैसला लेने में देरी न हो। खुद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यह सुनिश्चित करने में लगे हुए थे कि बजट में कर्ज माफी की घोषणा हो जाए।
पता नहीं हमारे राजनेता यह क्यों नहीं देख पा रहे हैं कि कर्ज माफी जैसे उपायों से किसानों का कोईभला नहीं हो रहा है? कर्ज माफी के सिलसिले को देखते हुए ही केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने राज्यों को आगाह करते हुए कहा था कि अगर कर्ज माफी का सिलसिला यूं ही कायम रहा तो यह भारतीय अर्थव्यवस्था को गहरी चोट पहुंचाएगा। यह किसी से छिपा नहीं कि एक बडी संख्या में ऐसे किसान भी हैं, जो कृषि के लिए नहीं, बल्कि अपने निजी कार्यों के लिए कर्ज लेते हैं। जब उनका कर्ज माफ कर दिया जाता है तो वे किसान हतोत्साहित होते हैं, जो ईमानदारी से अपना कर्ज लौटाते हैं। यह ठीक है कि किसानों की हालत अच्छी नहीं है और उसे सुधारने के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि रह-रहकर उनके कर्ज यह जानते हुए भी माफ किए जाएं कि इससे किसी का भला नहीं हो रहा है, उल्टे बैंकों की हालत खस्ता होती जा रही है। आज अगर खेती घाटे का सौदा बन गई है और एक बड़ी संख्या में किसान मजबूरी में कृषि कार्य कर रहे हैं तो इसके लिए खराब सरकारी नीतियां जिम्मेदार हैं। हमारे नीति-नियंताओं ने समय रहते न तो कृषि के आधुनिकीकरण की चिंता की और न ही ऐसे कोई प्रयास किए, जिससे जरूरत से ज्यादा आबादी की खेती पर निर्भरता घटती।
अगर देश की आधी से अधिक आबादी कम उत्पादकता वाली कृषि पर निर्भर होगी तो फिर ग्रामीण जीवन खुशहाल कैसे हो सकता है? यह सही है कि नरेंद्र मोदी ने केंद्र की सत्ता में आते ही खेती और किसानों की दशा सुधारने पर ध्यान देना शुरू किया और उनकी सरकार की ओर से एक के बाद एक कई कदम उठाए गए, लेकिन स्थिति मेंकोई बुनियादी बदलाव होता नहीं दिखा। इसी कारण पिछले वर्ष प्रधानमंत्री ने वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का संकल्प लिया। इस संकल्प के अनुरूप बजट में यह उल्लेख किया गया कि नए वित्तीय वर्ष से फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) लागत से डेढ़ गुना कर दिया जाएगा।पिछले दिनों केंद्रीय कैबिनेट ने खरीफ की 14 फसलों के बढ़े हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित भी कर दिए। मोदी सरकार ने एक तरह से किसानों से किया गया अपना वादा पूरा कर दिया। इस पर आश्चर्य नहीं कि मोदी सरकार के इस फैसले के पीछे उसका राजनीतिक स्वार्थ देखा जा रहा है। आम तौर पर सरकारों के हर फैसले राजनीतिक मकसद से ही होते हैं। यदि खरीफ की 14 फसलों की खरीद घोषित एमएसपी पर होती है, तो भाजपा को इसका लाभ मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के आगामी विधानसभा चुनावों के साथ-साथ लोकसभा चुनाव में भी मिलसकता है।
जो भी हो, वक्त की मांग यह है कि कृषि आत्मनिर्भरता की ओर बढ़े। निजी क्षेत्र को कृषि जगत में सक्रिय होने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। बेहतर है कि इसके लिए पर्याप्त नियम-कानून बनाए जाएं, ताकि कृषि क्षेत्र में निवेश करने वालों की पूंजी सुरक्षित रहे। यह विडंबना ही है कि आज हमारेज्यादातर किसान अपनी अच्छी उपज का भी लाभ हासिल करने में समर्थ नहीं। आम तौर पर वे अपनी उपज आढ़तियों अथवा बिचौलियों को बेच देते हैं। बाद में यही उपज आम लोगों तक पहुंचते-पहुंचते महंगी हो जाती है। इस स्थिति का निराकरण इस तरह करना होगा कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिले। बेहतर होगाकि कृषि उपज की खरीद-बिक्री और वितरण का तकनीक आधारित वैसे ही कोई तंत्र बने, जैसे जीएसटी के तहत बनाया गया है। ऐसे किसी तंत्र के अभाव के कारण ही खेत से निकली उपज जब तक आम उपभोक्ता तक पहुंचती है, तब तक उसके दाम दोगुने-तिगुने तकहो जाते हैं।
सरकार के लिए यह भी आवश्यक है कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को कोल्ड चेन बनाने के लिए प्रोत्साहित करे, ताकि खाद्यान्न के साथ फल और सब्जियों की बर्बादी को रोका जा सके। अपने देश में सुरक्षित भंडारण एवं ढुलाई की उचित व्यवस्था के अभाव में 20-25 प्रतिशत खाद्यान्न की बर्बादी हो जाती है। यही बर्बादी कई बार उनके मूल्यों में अप्रत्याशित उतार-चढ़ाव का कारण बनती है। अगर राजनीतिक दल सचमुच किसान-हितैषी हैं तो उन्हें उनके कर्ज माफ करने के बजाय ऐसे काम करने चाहिए, जिससे वे अपने पैरों पर खड़े हो सकें। बारबार किसानों के कर्ज माफ करना एक तरह से उन्हें जान-बूझकर गहरे संकट की ओर ले जाना है। राजनीतिक दल किसान कर्ज माफी के जरिए वोट तो हासिल कर सकते हैं, लेकिन वे खेती-किसानी का भला नहीं कर सकते। इसी क्रम में यह भी ध्यान रहे कि फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने भर से किसानों की सभी समस्याओं का समाधान नहीं होने वाला।
Date:09-07-18
लोकसभा और विधानसभा के एक साथ चुनाव की पहल का परवान चढ़ना आसान काम नहीं
संपादकीय

लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने को लेकर विधि आयोग की ओर से बुलाई गई बैठक के पहले दिन राजनीतिक दलों के रुख-रवैये से यही संकेत मिला कि उन्हें एक साथ चुनाव का सुझाव रास नहीं आ रहा। तृणमूल कांग्रेस के प्रतिनिधि ने तो यहां तक कह दिया कि यह सुझाव अव्यावहारिक होने के साथ-साथ असंवैधानिक भी है। लगता है उन्होंने इस तथ्य से अनभिज्ञ रहना ही उचित समझा कि 1967 तक लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ ही होते थे। क्या जब ऐसा होता था तो कोई असंवैधानिक काम होता था? गोवा में भाजपा के सहयोगी दल ने एक साथ चुनाव की पहल का विरोध किया तो पंजाब में उसके पुराने सहयोगी अकाली दल ने समर्थन किया। पता नहीं पक्ष-विपक्ष के अन्य अनेक राजनीतिक दल इस मसले पर क्या कहते हैं, लेकिन इसके ही आसार हैं कि अधिकांश एक साथ चुनाव के प्रति अनिच्छा प्रकट कर कर्तव्य की इतिश्री कर सकते हैं। वैसे भी यह किसी से छिपा नहीं कि इक्का-दुक्का राजनीतिक दलों को छोड़कर अधिकांश का यही विचार रहा है कि एक साथ चुनाव की पहल सही नहीं।
उनका एक साझा तर्क यह है कि एक साथ चुनाव होने से क्षेत्रीय दल घाटे में रहेंगे। इस तर्क को पूरी तौर पर निराधार नहीं कहा जा सकता, लेकिन ऐसे उपाय किए जा सकते हैं जिससे लोकसभा के साथ ही विधानसभाओं के चुनाव कराने से क्षेत्रीय दलों को कोई नुकसान न हो। नि:संदेह ऐसा तभी संभव है जब विभिन्न राजनीतिक दल एक साथ चुनाव की चर्चा के प्रति न्यूनतम गंभीरता प्रदर्शित करें। यदि बहस में ढंग से शामिल होने से ही इन्कार किया जाएगा तो फिर किसी आम सहमति पर पहुंचने का सवाल ही नहीं उठता। यह ठीक नहीं कि राष्ट्रीय महत्व के एक गंभीर सुझाव पर ज्यादातर राजनीतिक दल अगंभीरता का परिचय दे रहे हैं। सच तो यह है कि राजनीति और चुनाव से संबंधित सुधारों के मामले में राजनीतिक दल ऐसा ही करते रहे हैं। अगर राजनीतिक तौर-तरीकों और चुनाव प्रक्रिया से संबधित सुधार लंबित पड़े हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ रहा है तो राजनीतिक दलों के नकारात्मक रवैये के कारण ही।
समझना कठिन है कि राजनीतिक दल समय के साथ बदलाव के लिए तैयार क्यों नहीं? नि:संदेह एक साथ चुनाव की पहल का परवान चढ़ना आसान काम नहीं, लेकिन यह ऐसा भी विचार नहीं जिसे अमल में लाना असंभव हो। आखिर अतीत में एक साथ चुनाव होने को एक नजीर की तरह क्यों नहीं देखा जा रहा है? कुछ संवैधानिक संशोधनों के साथ लोकसभा चुनाव संग विधानसभाओं के चुनाव करना संभव है। जो संभव है उस पर आनाकानी इसलिए ठीक नहीं, क्योंकि रह-रह कर होने वाले चुनाव अब एक व्याधि बन गए हैं। वे न केवल देश की तरक्की में बाधक हैं, बल्कि राजनीतिक माहौल में नकारात्मकता भी भर रहे हैं। इसके अतिरिक्त वे राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ भी बन गए हैं। बेहतर होगा कि जो राजनीतिक दल एक साथ चुनाव के प्रति सकारात्मक राय रखते हैं वे अपनी सक्रियता बढ़ाएं और राजनीति के साथ ही देशहित में ऐसा माहौल बनाएं जिससे इस मसले पर सार्थक बहस हो सके।
Bet on Commission’s Proposal on Bets
ET Editorials
The Law Commission’s recommendation to legalise betting in sports and gambling is welcome. If accepted, it would end a gamut of criminal activities, curb money laundering and tax evasion, and boost tax collections. The commission echoes the Justice Lodha Committee, which had advocated legalising betting in cricket and making match-fixing a criminal offence. In 1996, the Supreme Court made betting on horse races legal, saying that it involved skill rather than chance. The Law Commission has done well to suggest making this applicable to all sports (read: skill-centric games), ending a prejudiced approach. De-criminalisation of betting will bring transparency, create trails and make it less tough for law enforcement agencies to trace underground players.
Betting and gambling are state subjects. Goa and Sikkim have legalised many forms of betting and gambling. Other states must follow. Parliament can enact a model law, given that betting and gambling take place on media platforms, and states can follow this template. However, it would be easier for states to amend their own laws to legalise betting. Currently, earnings from horse races and lotteries attract income tax — 30% tax is deducted at source. GST is also charged on the distributors’ commission. With the underground betting market estimated at .`3,00,000 crore, legalising betting offers a revenue gold mine, both for the Centre and states. Allowing foreign direct investment in, say, casinos makes sense to boost tourism. The commission favours stringent and overarching regulations. Safeguards are vital, but any arbitrariness will defeat the goal of legalising betting. India should follow countries such as the UK that have robust regulation on betting and gambling, with prudent safeguards.
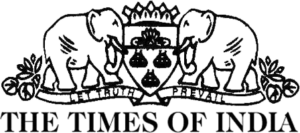
What’s Up With Messaging
WhatsApp and other platforms are not doing enough to combat fake news, rumours
Saubhik Chakrabarti(Saubhik Chakrabarti is Associate Executive Editor, ET)

It’s the message, not the medium. It’s policing, not technology. It’s society, not social networks. It’s government, not companies. That’s been the sum and substance of many commentators’ arguments as they have responded to lynchings engendered by rumours passed around in WhatsApp messages. Such a view is not wrong, not by a long shot. It’s true that if a group of people choose to believe rubbish and act violently on it, the ultimate responsibility for any horrors perpetrated is theirs. It’s also true that in many lynching cases policing has been ineffective.
Reportage in the national media has established that local police has (a) often been outnumbered by and felt powerless against a mob (b) sometimes failed to gather intelligence on dangerous rumours and (c) in a few cases exhibited appalling lack of urgency which seems best explained by the fact that some victims were ‘outsiders’, low income migrants, for example. True, too, are observations by commentators that toxic social behaviour is often a close cousin of toxic politics. And that political toxicity has increased recently. Equally valid are arguments that the Indian state is prone to censuring and hectoring carriers of information, whatever the technology employed, because that’s easier than, say, fixing law and order, and also because the private sector makes for good villains in the eyes of almost all governments.
But while all that’s true, this proposition is not true: that companies that provide communication services that allow instantaneous spread of vicious and false rumours have no responsibility at all. WhatsApp in this case and social networks in general have a responsibility to make their networks less salubrious for peddlers and merchants of falsity, fakery and downright dangerous stuff. No one is arguing that a messaging platform creates such a system that only “good” people use it for “good” purposes. That’s impossible and not even desirable because pre-defining what’s “good” is a road that inevitably leads to illiberal choices. The likes of WhatsApp, though, can and must do more, and commentators who say otherwise are being at best naive. In fact, even companies offering these services don’t seem to agree with pundits who say they are not to be blamed.
As has been reported in The Economic Times, WhatsApp is working on labelling forwarded messages so that users can at least be aware that the sender may just be passing on something he received. It’s also reportedly developing machine learning capacities to identify false/dangerous messages. Facebook is reportedly hiring what it calls public policy experts and employing people and technology to kill fake profiles, which are often sources of fake news/dangerous rumours. It’s also preventing pages that are habitual hosts of false information from carrying advertising. Little wonder then, as TOI reported, Facebook has promised the Election Commission of India that it will employ fact checkers to weed out fake news aimed at influencing voter decisions during elections, especially the next Lok Sabha polls. Facebook, again a point to be seriously noted, is voluntarily offering to run checks and block false information.
All this is good. But it’s nowhere near enough. That Facebook, which also owns WhatsApp, is even doing this much is of course thanks to the big scandal it got mired in over data privacy and misuse of personal information. That WhatsApp is responding to tragedies like lynching is because it feels that another scandal, in the country that hosts its biggest user base, may put it in serious trouble with authorities. But as technology reporters have noted WhatsApp barely has a management team in India, even though 200 million Indians use the messaging service. Of course, technology services can be run remotely with very few local hires. But that model doesn’t work when your technology service is front and centre in several public tragedies.
WhatsApp doesn’t have a public policy team in India, media reports have said. That’s a good indicator of how far away the messaging service is when it comes to behaving like a responsible corporate citizen. Technology experts have pointed out that social networking sites created the problem of fake news, not by inventing fake news, but by (a) creating a transmission technology that allows super quick spread of dangerous rubbish and (b) by taking away business from mainstream media, which generally weeds out ridiculous falsities, but not investing enough in fact checking. What’s being promised now is not enough given the scale of the problem.
Studies have shown that correcting and/or debunking a piece of fake news/dangerous rumour online takes an average of 12 hours. In 12 hours, a dangerous rumour can travel online several times around the world. It’s also established that online the volume of fact checking content is far less than the volume of fake news/ rumour. There are also behavioural issues – studies have demonstrated that people tend to circulate falsities far faster than facts, especially if such false information conforms to users’ biases. Given all this, corrective efforts by technology companies have only begun. They need to invest a whole lot more, in human resources and technology, to combat the flood of trash that flows through their communication channels. It’s not just the message, it’s also the medium.
Date:08-07-18
MSP hike is a big blunder. Farmers are producers, not objects of charity
Swaminathan S Anklesaria Aiyar is consulting editor of The Economic Times.
The big jump in minimum support prices (MSPs) for kharif crops announced by the Modi government is its biggest economic blunder. It gives farmers a fixed margin of 50% over their input costs and imputed labour cost, ignoring demand, supply and international competitiveness. This makes no economic sense for any activity, let alone farming. Modi seeks to solve a problem of agricultural over-production with incentives that will worsen over-production. Higher food prices will worsen inflation. The RBI will seek to curb this by raising interest rates, hurting industry and exports. This may help Modi win the next election, but will dent India’s long-term GDP growth and prosperity. Farmers should be treated as producers with internationally competitive potential, not as objects of charity.
They should be encouraged and helped to grow items in which India is competitive, and discouraged from growing uncompetitive crops. Providing a fixed return to all crops, regardless of competitiveness, is a recipe for producing items that neither India nor the world wants. The 50% margin chosen by the government is completely arbitrary. Can you think of any other goods or services for which this would be appropriate? It makes no sense, save in political terms of wooing all farmers. Farm distress is a reality, but does not mean growing poverty. A recent Brookings paper shows that 44 Indians per minute are rising above the poverty line, and extreme poverty will soon fall to almost nothing. The farm problem is not poverty or scarcity but excess production of several crops. The resulting glut has depressed farm prices, often below old MSP rate.
The solution is to discourage excess production, not encourage it with rising MSPs. The 50% margin over costs will raise prices above even their current uncompetitive levels, making exports even more difficult. A fixed mark-up over costs will encourage even greater use of purchased inputs and labour, which in turn will send MSPs even higher in a vicious circle. The European Economic Community once tried something similar, offering prices to farmers well above global rates to make Europe self-sufficient in food, to provide food security in the event of war with the USSR. Alas, high prices created unsold mountains of butter and meat and lakes of milk and wine. These ultimately had to be disposed of by selling them at throwaway price to the USSR, the supposed enemy. Learning from this folly, Europe shifted its subsidies from crops to farmers. Direct cash transfers to farmers replaced high prices for crops.
That finally brought supply and demand back in balance, eliminated huge surpluses, and still alleviated farm distress. India needs to learn from the EEC’s mistakes, not replicate them. Indian experience shows that subsidising goods (food, fertiliser, electricity, LPG) leads to large leakages to the undeserving and to middlemen. Experts estimate that three rupees of spending is needed to get one rupee through to beneficiaries. Modi’s supposed strategy has been to shift subsidies from goods to deserving individuals through direct benefit transfers to their bank accounts. This works only if good financial and telecom infrastructure exist. It has worked well for cooking gas.
Something similar could be attempted for agriculture. Telangana has pioneered cash grants of Rs 4,000 per acre per crop to farmers, instead of farm loan waivers. The state’s land records are in decent shape, facilitating a strategy that will fail in states with poor land records. No money goes to tenants or labourers in Telangana, a structural flaw. No limit on land ownership applies, so the biggest farmers gain most. The scheme places a big burden on the exchequer, something Telangana can afford (a rarity among states) since it has hugely improved its revenue collection. The great advantage of the model is simplicity, enabling good implementation.
The downside is that it will fail where land records are unreliable, or state governments are under fiscal stress. The model places no acreage limit, and so benefits large farmers the most, though they need the least help. A possible national strategy would start with preparatory efforts for good land records and financial infrastructure. Next should be phased moves to a cash grant of Rs 4,000 per acre per year, up to a limit of five acres per holding. This cannot be done overnight, but is a far better strategy than ever-rising MSPs. It avoids the evils of cost-plus pricing and encouraging overproduction. It will limit the cost of farm rescues while benefiting small farmers most. It will curb gluts that depress prices. If supporting farmers is politically necessary, this is the least damaging way to do it.
संवेदनाओं को नकारता समाज
डॉ. विशेष गुप्ता
दिल्ली के बुराड़ी इलाके में एक ही परिवार के ग्यारह लोगों की मौत की घटना ने देश को झकझोर कर रख दिया। अतीत में सामाजिक व आर्थिक कारणों से सामूहिक मौतों की घटनाएं देखने व सुनने को मिलती रहीं हैं। परन्तु अवलोकन बताते हैं कि भाटिया परिवार तो अच्छा मध्यमवर्गीय कारोबारी खाता-पीता परिवार था। आर्थिक परेशानी भी नहीं थी। पड़ोसियों द्वारा परिवार के सदस्य धार्मिक प्रवृत्ति के साथ बहुत विनम्र बताए गए हैं। अचानक ऐसा क्या हुआ कि तीन पीढ़ियों के ग्यारह सदस्यों को सामूहिक आत्महत्या करनी पड़ीं? यह संपूर्ण घटनाक्रम एक दिन और एक रात में घटित नहीं हो सकता। यह घटना चाहे धार्मिक रूप से अंधविासी अथवा मोक्ष प्राप्ति के लिए ही क्यों न हो, निश्चित ही यह सालों की एकाग्रचित साधना का परिणाम है। दूसरे पड़ोसी और रिश्ते-नातेदारों का इस परिवार से पूरी तरह से अनजान होना शर्तिया समाज की अंदरूनी दरकती दीवारों की ओर इशारा करता है।
इसके साथ-साथ अब जिन घटनाओं के उदाहरण मैं देने जा रहा हूं, ये घटनाएं भले ही अपने स्वभाव से एकल हों, परन्तु सभी समाज में लगातार बढ़ती संवेदनशून्यता की ओर इशारा कर रहीं हैं। आपको याद होगा कि पिछले दिनों कई पेशेवर लोगों ने खुद अपनी जीवनलीला समाप्त कर लीं। उनमें पहले अपनी बहादुरी और काबिलियत के लिए जाने वाले महाराष्ट्र के आईपीएस अधिकारी हिमांशु राय हैं। इसके अलावा यूपी के एक अपर पुलिस अधीक्षक राजेश साहनी ने भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली। लखनऊ के ही ‘‘यूपी100’ के दरोगा ने ड्यूटी से लौटकर अपनी लाइसेंसी बंदूक से गोली मारकर खुदखुशी कर ली। मुबंई के ही एक 24 वर्षीय प्रबंधन के एक पेशेवर छात्र अजरुन भारद्वाज ने होटल की 19वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। पिछले ही दिनों गुड़गांव के रेयान स्कूल की घटना में एक नाबालिग छात्र का अपने साथी की हत्या, बेटे को पढ़ाई के लिए डांटने पर मां और बहन की हत्या जैसी घटनाएं आज लगातार समाज को अंदर से झकझोर रहीं हैं। ये तो अभी केवल हाल की ही कुछ घटनाएं हैं।
आज परिवार व विवाह के ढांचे की दरकती दीवारें, रक्त संबंधों में लगातार टूटन और रातों-रात लोगों के सफल होने का जुनून जैसे कारण इस पेशेवर समाज में बदलाव की तेज रफ्तार को महसूस करा रहे हैं। वर्तमान की इस सच्चाई को प्रस्तुत करने में कोई हिचक नहीं कि तकनीकी शिक्षा, पूंजी, बाजार, सूचना तकनीकी के साथ में सोशल मीडिया जैसे कारकों के फैलाव के सामने परिवार, समुदाय से बनने वाले सामाजिक रिश्ते बौने नजर आ रहे हैं। सही बात यह है कि तेजी से भागती जिंदगी में सामाजिक रिश्तों के अहसास से बनने वाले समाज में अब यह बहस चल पड़ी है कि क्या सामाजिक और सामुदायिक रिश्तों में और कड़वाहट बढ़ेगी? क्या भविष्य पेशेवर समाज में विवाह और परिवार का सामाजिक-वैधानिक ढांचा बच पाएगा अथवा इनका पूरी तरह कायापलट हो जाएगा? क्या समाज को अब सूचना तकनीक से जुड़े आभासी समाज पर ही निर्भर रहना होगा? क्या भविष्य में परिवार की एकलता ही जीवन की सच्चाई बनकर उभरेगी अथवा इनमें भी अभी और टूटन बढ़ेगी? अगर हम यह मानते हैं कि यह दौर तेजी से बदलते समाज का दौर है तो फिर यहां सवाल यह भी है कि क्या इन रिश्तों की टूटन को बदलाव की स्वाभाविक प्रक्रिया समझा जाए या इसे नये नियंतण्र समाज का दबाव मानकर चलना बेहतर होगा? ऐसे ज्वलंत सवालों के जवाब हमें भारतीय समाज के दायरे में ही खोजने होंगे।
आजादी के आंदोलन के बाद हमारी पुरानी पीढ़ी ने जिन मूल्यों और आदशरे के साथ सामाजिक रिश्तों को परिवार के संयुक्त सांचे में ढाला, पूंजी के विस्तार, बाजार की आक्रामकता और व्यक्ति के रातो-रात सफल होने की महत्त्वाकांक्षाओं ने उसे एक ही पल में बिखेर कर रख दिया। इन रिश्तों के टूटन की खनक आज समाज में साफ सुनाई दे रही है। अवलोकन बताते हैं कि आज हर रिश्ता एक तनाव के दौर से गुजर रहा है। वह चाहे माता-पिता का हो या पति-पत्नी का, भाई-बहन, दोस्त या अधिकारी व कर्मचारी का ही रिश्ता क्यों न हो, इन सभी के बीच एक शीत भाव पनप रहा है। ध्यान रहे सामाजिक रिश्ते निरंतर संवाद की मांग करते हैं। देर-सवेर समाज में बढ़ता धन का प्रभाव, छद्म तरक्की की होड़ व सोशल मीडिया के प्रभाव से बढ़ता सामाजिक अकेलापन थोड़ा परेशान जरूर कर सकता है। परन्तु इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपसी रिश्तों के सघन संवाद के बढ़ने से न केवल भारतीय परिवारों की नींव मजबूत होगी, बल्कि इससे भविष्य में देश के सामाजिक व सांस्कृतिक ताने-बाने को भी मजबूती मिलेगी।
BETTING ON THE FUTURE
Editorial
The Law Commission has answered a question which has lingered in debate for decades, and found that it would be desirable to open sports to betting, with the caveat that it must be regulated. It has also respected the public will, insisting that this is a political decision for Parliament to thrash out. Indeed, gambling cannot be imposed on a morally sensitive public, and implementation could prove to be difficult. It would be useful to gauge the public mood through its representatives in advance. In this context, it would be useful to heed commission member S Sivakumar, who has filed his dissent, on the ground that the social implications of the move have been insufficiently examined. The theoretical logic for opening up betting is well-known and has been supported by the commission.
It is a common-sense position, and does not really require the support of Narada, Chanakya and Katyayana, who have been invoked. Legalisation would generate jobs and revenues for the government, and regulation would help contain financial crime. Unless betting is legalised, on the other hand, it will persist underground in a completely unregulated form, a fact that the Constituent Assembly was seized of. It will continue to excite the interest of fixers and mafias, will ensure the criminal intimidation of players, and remain a conduit for money of questionable colour. The commission has rightly suggested the criminalisation of fixing, with significant legal deterrence, and undescored the need for betting to be allowed only under the control of the state. State governments must ensure that illegal betting, which flourishes on street corners and on the phone network, is suppressed.
However, other suggestions for regulation may have to be thought through. The attempt to segregate “proper betting” for high stakes from “small gambling” by the poor may not survive scrutiny. The suggestion is well-intentioned and would protect the economically weaker sections, but disbarring from participation all players who get subsidies or do not pay taxes may violate the principle of equality of access. Persuasion may prove to be a more suitable protector of the vulnerable than such segregation. Bringing betting overground is an economically and socially desirable objective, but as the commission has said, it must be operated strictly within the purview of the law. Putting part of the population beyond its pale would keep a section of the business underground, defeating the purpose of the reform.
