
07-08-2020 (Important News Clippings)
To Download Click Here.
 Date:07-08-20
Date:07-08-20
Religion, Meet Politics
August 5 was a big day for Ayodhya, Modi, BJP. He must now focus on keeping India’s tryst with destiny
TOI Editorials
In an occasion marked by great pomp and religiosity, Prime Minister Narendra Modi was the cynosure of all eyes at the Ram Mandir bhoomi pujan ceremony. The soaring oratory he brought to the moment was equally a triumph for BJP too. The scene certainly gladdened the hearts of many across the country. But many will also be wondering about its deeper meaning.
For the BJP faithful, the August 5 date will have a certain ‘beautiful symmetry’. It’s when BJP came good on two of its major campaign promises: The nullification of J&K’s Article 370, and establishment of the Ram Janmabhoomi temple. Hopefully, BJP and Sangh Parivar will now settle down and have less reason to play the ‘Hindu victim’ card.
Thanks in no small measure to Modi and BJP’s rhetoric, 21st century India is increasingly aspirational. In that respect, while the PM’s desire for August 5 to gain a greater salience over the Indian psyche is understandable, his conflation of the mandir struggle with India’s freedom movement may be seen by many as overstated. No occasion since August 15, 1947, has measured up as a close seminal event in Indian history – except perhaps the adoption of the Indian Constitution on November 26, 1949, which forms the foundation of the Indian republic today.
The government should use this occasion to rededicate itself to keeping India’s tryst with destiny and fulfilling the unrealised goals of the republic. It should apply itself with vigour to reviving the economy, improving governance, and reversing the decades-long underinvestment in public health that the Covid pandemic has so starkly exposed. Aggression by China and fresh claims by Pakistan and even Nepal on our territory is another challenge that needs to be tackled. Temples and other monuments can contribute to great cultural signification and gratification, but they cannot replace improving the quality of people’s lives and boosting national well-being, which is the real deal. That’s what the government must now focus its mind and energies on. In his speech, Modi invoked nationalist spirit and described Ram as a symbol of inclusive governance and popular welfare. He should harness his popularity to ensure that the NDA’s record of governance approximates to the ideals he celebrated at Ayodhya.
Date:07-08-20
Suicide’s Aftereffects
Politicisation of Sushant Singh Rajput case is unfair to him and the public
TOI Editorials

The Mental Healthcare Act 2017 that decriminalised attempts to die by suicide aims to mitigate the suffering of the mentally ill and sees that suicide can be a voluntary act. This is part of a broader social-legal movement to recognise the right to die as part of the right to life. But IPC continues to see every suicide as coerced: “If any person commits suicide, whoever abets the commission of such suicide shall be punished.” This is why further reform is necessary, until the law is clear it need not pinpoint a crime every time there is suicide. Bear in mind that NCRB data suggests an Indian commits suicide every four minutes. Let’s treat this with sensitivity and compassion.
All of this is not to pronounce premature judgment in the Sushant Singh Rajput case. Even if it had not touched a deep chord across the citizenry, a thorough investigation into his death would have been merited given the serious nature of complaints from his family and others. What is unfortunate is the aura of witch hunting around the multiple probes, taking place along extremely politicised lines. Police from Bihar which has an NDA government and from Maharashtra which has a Maha Vikas Aghadi government are at chaotic loggerheads. Now ED and CBI are getting into the game.
This case is a dramatic reminder of the need to decolonise police and investigative agencies, so that they act genuinely in public interest instead of being swayed by governments of the day, hysterical TV anchors or social media armies. Everyone claims to know what they can’t possibly know: The exact reasons that led to Rajput’s death. Leave it to the experts, while the rest of us should desist from the temptation of shooting at one’s favourite target using Rajput’s shoulder.
Stock exchange for social enterprise
ET Editorials
A working group at capital markets regulator Sebi has brought out a welcome report on the social stock exchange (SSE), a platform for fundraising for social enterprises, and measuring and reporting social impact. The objective is to fund enterprises that seek to create ‘positive social impact’ via innovative securities, and to have robust standards of social impact assessment and attendant reporting.
While social impact bonds have been floated in India for a while – the first such project implemented by Educate Girls circa 2015 ‘covered’ 7,300 children in rural Rajasthan — the Sebi paper seeks to build an entire ecosystem to gainfully fund social enterprises, complete with information repositories, social auditors and reporting standards for social capital formation. Four key stakeholders come together for social impact bond issuance: investor, service provider, independent evaluator and outcome payer, such as a foundation or the government; the goal is to duly meet an envisaged social development objective. The SSE can be housed within existing stock exchange. Social entities can be either for-profit enterprises (FPEs), or non-profit organisations (NPOs). For FPEs, the SSE is to raise equity and social venture funds. For NPOs, zero-coupon, zero-principal bonds are also proposed, for investors who are interested in social impact and do not wish to have the funds returned to them.
The paper suggests allowing funding to NPOs on SSE to count towards corporate social responsibility commitments, which seems unexceptionable. Also, allowing philanthropic donors to claim 100% tax exemption for donations to NPOs makes perfect sense. At present, donations to private NPOs are allowed 50% tax deduction, whereas government entities get 100%. The anomaly surely needs prompt correction.
Academic research is necessary, but not sufficient
Investment in research can translate into national development only through pursuit of post-academic research
R.B. Grover is Emeritus Professor, Homi Bhabha National Institute, and Member, Atomic Energy Commission
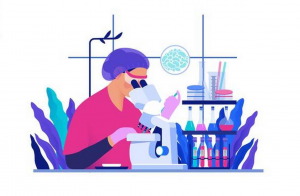
The Government of India is in the process of revisiting the Science, Technology and Innovation (STI) Policy. The policy will guide the agencies of the government mandated with funding research in higher education institutions and national laboratories. At this stage we need to ponder the question: what kind of research should be funded? That leads one to look at the nomenclature used by researchers for this purpose. Here it is pertinent to recall what William Shockley said in his Nobel lecture in 1956, that words like “pure, applied, unrestricted, fundamental, basic, academic, industrial, practical etc.” are being used frequently “in a derogatory sense, on the one hand to belittle practical objectives of producing something useful and, on the other hand, to brush off the possible long-range value of explorations into new areas where a useful outcome cannot be foreseen.”
Alternate frameworks
Experts in science and technology studies have come up with alternate frameworks and terminology to provide a comprehensive picture and avoid any value judgement. One approach was proposed by NASA in the form of Technology Readiness Levels (TRL), a type of measurement system used to assess the maturity level of a particular technology. TRL-1 corresponds to observation of basic principles. Its result is publications. TRL-2 corresponds to formulation of technology at the level of concepts. Then the TRL framework advances to proof of concept, validation in a laboratory environment, followed by a relevant environment, and then to prototype demonstration, and ending with actual deployment. The framework uses terms as applicable to aerospace applications, but one can come up with alternate terms depending on the field of application, including health sciences where the term ‘translational research’ is commonly used. The number of levels can also be adjusted to suit the application.
An alternative is to use the terminology ‘Academic Research (AR)’, and ‘Post-Academic Research (PAR)’. One can easily establish correspondence with the TRL framework, with AR corresponding to TRL-1 and the rest to higher levels. To provide some granularity, one can divide PAR into early-stage PAR, and late-stage PAR. Late-stage PAR has to be done by large laboratories (national or those supported by industry), while AR and early-stage PAR can be done at higher education institutions and large laboratories.
Both AR and PAR generate knowledge which is necessary for national development. When examined from the perspective of national development, pursuit of AR alone, while necessary, is not sufficient. AR and PAR when pursued together and taken to their logical conclusion will result in a product or a process, or a better clinical practice, or a scientifically robust understanding of human health and disease, or provide inputs for a policy decision.
It is often said that India’s investment in research is lower than that by advanced countries. Here two observations need consideration. First, countries belonging to the Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) report research statistics according to the Frascati Manual, which was first drafted in 1963, and has gone through five revisions since then. We cannot compare data with other countries without having correspondence between India’s data and data reported by others. Second, India has to decide where to increase investment: in AR or in PAR. Investment in research can translate into national development only through pursuit of PAR.
This is not a call for abandoning AR, but a call to look for useful outcomes including via spin-offs and serendipity, and to prioritise research in areas that relate to national development.
During my talks with academics on this topic, some observed that our industry has not reached a stage where they can absorb research being done by higher education institutions. This observation reveals that research being pursued is either not addressing national needs or is limited to AR. The lukewarm response of industry is a message for academia to orient its priorities to address national needs and engage in both AR and early-stage PAR and provide inputs necessary to raise the technology intensity of industry.
Pursuing AR and PAR
One can cite several examples to illustrate how AR and PAR can be pursued together. A programme in high energy physics can be designed to pursue accelerator technology along with high energy physics. Research in electro-chemistry can be accompanied by development of battery technologies.
Judging the growth of S&T based only on publications provides an incomplete picture. Why is it that industries that have high technology intensity, such as aircraft and spacecraft, medical, precision and optical instruments, and communication equipment, have a low presence in India? What should be done to increase value addition to raw materials in India? The answer lies in increasing the technology intensity of industry, which was identified as one of the goals of the STI policy issued in 2013. This needs reiteration and a mechanism should be devised to monitor progress with the objective of becoming an ‘Atmanirbhar Bharat’.
The STI policy should emphasise PAR to ensure that investment in research results in economic growth. To motivate the research community to pursue at least early-stage PAR, the reward system needs significant reorientation. The current system for rewards relies heavily on bibliometric indicators despite the knowledge that publications alone do not lead to national development. The reward system in higher education institutions and national laboratories should be reoriented to promote PAR. Academics in higher education institutions pursuing AR should pursue early-stage PAR themselves, or team up with those who are keen to pursue PAR.
In short, academic research is necessary, but not sufficient.
व्यापक असर वाली शिक्षा नीति
अरविंद कुमार (लेखक यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के रॉयल होलोवे में पीएचडी स्कॉलर हैं)
एक लम्बे विचार विमर्श के बाद केंद्र ने नई शिक्षा नीति की घोषणा कर दी जो राजीव गांधी सरकार द्वारा 1986 में बनाई शिक्षा नीति की जगह लेगी। यह देश की शिक्षा व्यवस्था में व्यापक बदलाव लाते हुए 21वीं सदी के भारत की नींव रख सकती है। इसमें छह वर्ष से पहले ही बच्चों की शिक्षा शुरू कराने पर काफी जोर दिया गया है। बच्चों के दिमाग का 85 प्रतिशत हिस्सा छह वर्ष के पहले ही विकसित हो जाता है। इस उम्र में बच्चों को सिखाने पर ध्यान नहीं देने से उनकी सीखने की क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तमाम शोध से साबित हुआ है कि बच्चों के पढ़ने की क्षमता उन्हें बचपन में मिले संतुलित आहार से प्रभावित होती है। चूंकि गरीब परिवारों के बच्चों को संतुलित आहार नहीं मिल पाता इसलिए वे कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। ऐसे बच्चे पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते। यूनिसेफ के प्रयास से अलग-अलग देशों में बच्चों के लिए पोषाहार और मध्यान्ह भोजन की व्यवस्था लागू की गई है। भारत में भी इसे आंगनबाड़ी के माध्यम से बाल-पोषाहार और प्राथमिक विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन व्यवस्था के तौर पर शुरू किया गया है। नई शिक्षा नीति में अब बच्चों को भोजन के पहले पौष्टिक नाश्ता देने की भी बात है। बच्चों के मानसिक विकास के पहलुओं पर ध्यान देने की वजह से व्यवस्था में सुधार आने की संभावना है। स्कूली शिक्षा में दूसरा बड़ा बदलाव साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स के स्ट्रीम को समाप्त करना है। अब बच्चे 11-12वीं में अपनी पसंद का कोई भी विषय का चुन सकते हैं। एक अन्य अहम बदलाव यह हुआ है कि संगीत, खेलकूद जैसे विषय मुख्य विषय बना दिए गए हैं। इसके अलावा सरकार अब स्कूलों में योग्य शिक्षकों की कमी पूरी करने के लिए चार वर्षीय बीए+बीएड कोर्स शुरू करेगी।
उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव शिक्षा को नियंत्रित करने वाली संस्थाओं को लेकर है। अब तक यूजीसी, एआइसीटीई जैसी संस्थाएं उच्च शिक्षा पर निगरानी रखती थीं, जिससे एक जैसे मामलों में उनके अलग-अलग निर्णयों की वजह से काफी दिक्कतें आ रही थीं। अब ऐसी संस्थाओं को समाप्त कर केवल एक राष्ट्रीय उच्च शिक्षा आयोग होगा। दूसरे बड़े बदलाव के तहत देशभर के विश्वविद्यालयों को ब्रिटेन की तर्ज पर शोध केंद्रित और शिक्षण केंद्रित विश्वविद्यालयों में विभाजित किया जाएगा। साथ ही तमाम डिग्री कॉलेजों को भी स्वायत्तता दी जाएगी। अगर छोटे शहरों के पुराने डिग्री कॉलेजों को स्वायत्तता मिलती है तो वहां भी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा। सभी डिग्री कॉलेजों पर विवि की निगरानी रखने की नीति का परिणाम यह हुआ कि अच्छे- खासे चल रहे डिग्री कॉलेज भी नए-नए खुले विवि की प्रशासनिक निगरानी में आ गए। नए विवि खुद ठीक से खड़े नहीं हो पाए और उन्होंने पुराने डिग्री कॉलेजों को भी डूबो दिया। सरकार अब जाकर इस समस्या को पहचान पाई है।
उच्च शिक्षा में तीसरे बदलाव के तहत अब ग्रेजुएशन चार साल का होगा, लेकिन उसमें भी बीच में कोर्स को छोड़ने का प्रावधान होगा। अगर कोई एक साल में कोर्स छोड़ता है तो उसे सर्टििफकेट, दो साल में डिप्लोमा, तीन साल में डिग्री मिलेगी। चार साल बाद रिसर्च ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगी, जिसकी बदौलत छात्र बिना एमए किए सीधे पीएचडी में प्रवेश पा लेगा। चार वर्ष के ग्रेजुएशन का मूल उद्देश्य प्रतिभावान बच्चों को शोध कार्य की तरफ मोड़ना है। ग्रेजुएशन से सीधे पीएचडी में प्रवेश की व्यवस्था ब्रिटेन के विश्वविद्यालयों में भी है, लेकिन इसे बहुत अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि ग्रेजुएशन के दौरान बहुत कम छात्र शोध करने लायक पढ़ाई कर पाते हैं। भारत में चूंकि स्कूली शिक्षा की स्थिति दयनीय है, इसलिए 12वीं पास छात्रों को ग्रेजुएशन के कोर्स को पढ़ने/समझने में काफी दिक्कत होती है। भारत की स्कूली शिक्षा पद्धति में पढ़े अमीर परिवार के बच्चों का भी इस समस्या से सामना होता है, जब वे विदेशी विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेने जाते हैं। ज्यादातर भारतीय छात्रों को एक साल का प्री-कोर्स करना पड़ता है, जिसमें उन्हें भाषा, गणित वगैरह की शिक्षा दी जाती है। चार वर्षीय कोर्स के विपरीत सरकार को दिल्ली विवि के पूर्व कुलपति प्रो. दिनेश सिंह द्वारा तैयार चार वर्षीय ग्रेजुएशन का मॉडल अपनाना चाहिए था, जिसमें पहले साल में छात्र को भाषा, कम्युनिकेशन आदि के बारे में पढ़ना होता और फिर जो कोर्स उसे पसंद आए उसमें प्रवेश लेता। हालांकि इस समस्या को सुलझाने के लिए नई शिक्षा नीति में विश्वविद्यालयों/कॉलेजों को क्रेडिट आधारित सिस्टम की तरफ बढ़ने को कहा गया है, जिसके तहत छात्र अपनी पसंद का विषय पढ़ सकता है। अगर वह विषय उसके विवि/कॉलेज में नहीं है तो दूसरे विवि से ऑनलाइन पढ़ सकता है, जिसे डिग्री कोर्स में अंकित किया जाएगा। इसका फायदा यह होगा कि बड़ी संख्या में छात्रों को नामी-गिरामी शिक्षण संस्थाओं से कोर्स करने का अवसर मिलेगा। उच्च शिक्षा में एक अन्य महत्वपूर्ण बदलाव एमफिल की डिग्री की समाप्ति है।
नई शिक्षा नीति पुरानी शिक्षा नीति से ज्यादा कारगर साबित होने की उम्मीद इसलिए है, क्योंकि ज्यादातर राज्यों में भाजपा और उसके सहयोगी दलों की सरकारें हैं। जब 1986 में शिक्षा नीति लागू हुई थी तब कुछ समय बाद 1989 से ही कई राज्यों में विपक्षी पार्टयिों की सरकारें बननी शुरू हो गई थीं। उन सरकारों ने उस शिक्षा नीति के अच्छे प्रावधानों को भी लागू करने से मना कर दिया था। जैसे तमिलनाडु ने नवोदय विद्यालयों का यह कहकर विरोध किया कि यह हिंदी थोपने की साजिश है। इस वजह से तमिलनाडु के लाखों बच्चे नवोदय विद्यालय की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पाने में असफल रहे।
![]() Date:07-08-20
Date:07-08-20
एमपीसी का सही निर्णय
संपादकीय
भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने नीतिगत दरों में बदलाव नहीं करने का एकदम उचित निर्णय लिया है। कोविड-19 महामारी के संक्रमण के मामलों में निरंतर बढ़ोतरी और देश के विभिन्न हिस्सों में लॉकडाउन लगाए जाने के कारण आर्थिक स्थितियों में सुधार की प्रक्रिया काफी धीमी है। इस बीच मुद्रास्फीति संबंधी पूर्वानुमान भी अनिश्चित हैं। समिति ने कहा है कि जरूरी सब्जियों के मामले में कीमतों पर दबाव कम नहीं हो रहा है और यह आपूर्ति के सामान्य होने पर निर्भर करता है। प्रोटीन आधारित खाद्य उत्पादों के संभावित दबाव के अलावा गैर खाद्य श्रेणियों को लेकर पूर्वानुमान अस्पष्ट हैं। पेट्रोलियम उत्पादों पर उच्च कर के कारण उपभोक्ताओं के लिए उनकी कीमत बढ़ी है और इसका परिणाम व्यापक अर्थव्यवस्था की लागत में इजाफे के रूप में देखने को मिल सकता है। मुद्रास्फीति आधारित खुदरा मूल्य सूचकांक जून में 6 फीसदी से ऊपर था जबकि मूल मुद्रास्फीति 5.4 फीसदी थी।
आपूर्ति शृंखला के निरंतर बाधित होने के कारण भी मुद्रास्फीति पर असर होगा। केंद्रीय बैंक ने अनुमान जताया है कि चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में मुद्रास्फीति ऊंची रहेगी और वर्ष की दूसरी छमाही में उसमें कमी आएगी। ऐसा आंशिक तौर पर अनुकूल आधार के कारण होगा। मुद्रास्फीति के मोर्चे पर अनिश्चितता पर करीबी नजर रखने की आवश्यकता है लेकिन इसके अलावा केंद्रीय बैंक को प्रतीक्षा करनी चाहिए और यह देखना चाहिए कि पुराने हस्तक्षेपों ने अर्थव्यवस्था को किस तरह प्रभावित किया है। ब्याज दरों में कटौती के अलावा रिजर्व बैंक ने व्यवस्था में काफी नकदी डाली है। इससे बॉन्ड बाजार और बैंकों की ऋण दर दोनों में पारेषण बेहतर हुआ है। ऐसे में अगर अभी दरों में एक और बार कटौती की जाती तो भी उसका कोई खास असर नहीं होता। रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप के कारण नकदी की स्थिति में सुधार जारी रह सकता है। आयात में गिरावट के कारण निकट भविष्य में महत्त्वपूर्ण भुगतान संतुलन की स्थिति बन सकती है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार चालू वित्त वर्ष में अब तक 56.8 अरब डॉलर तक बढ़ा है। घरेलू नकदी में इजाफा मूल्य और स्थिरता दोनों के लिए खतरा पैदा कर सकता है। इतना ही नहीं, चूंकि आर्थिक कठिनाइयां जल्द समाप्त होती नहीं दिखतीं इसलिए केंद्रीय बैंक का कुछ नीतिगत हथियार बचाकर रखना भी अहम है। नियामकीय मोर्चे पर आरबीआई ने प्रूडेंशियल फ्रेमवर्क के तहत अर्हता प्राप्त कर्जदाताओं को एक निस्तारण योजना मुहैया कराने की गुंजाइश बनाई है। हालांकि ऐसा कुछ तयशुदा शर्तों के अधीन ही किया जा सकेगा। कर्जदाता ऐसे जोखिम को मानक परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत कर सकेंगे।
आरबीआई ने वरिष्ठ बैंकर के वी कामत के नेतृत्व में एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का निर्णय भी लिया है। यह समिति निस्तारण योजनाओं के लिए वित्तीय और क्षेत्रवार मानकों के सुझाव देगी। यह सही दिशा में उठाया गया कदम है। महामारी ने ऐसे कर्जदारों को भी प्रभावित किया है जिनका ऋण चुकाने के मामले में अच्छा प्रदर्शन रहा है। उन्हें राहत की आवश्यकता है। नियामक जहां अतीत की गलतियां दोहराने से बचने की सावधानी बरतता दिख रहा है वहीं यह सुनिश्चित करना भी अहम होगा कि इस सुविधा का दुरुपयोग न होने पाए। वैसे भी हालात से निपटने की यह कोशिश, सभी क्षेत्रों के लिए ऋण अदायगी स्थगन में इजाफा करने से कहीं अधिक बेहतर है। बहरहाल, व्यापक स्तर पर देखा जाए तो मुद्रास्फीति और वृद्धि के नतीजों के उलट कंपनियों के बही खाते कितनी जल्दी दुरुस्त होते हैं यह इस बात पर निर्भर करेगा कि महामारी को कितनी जल्दी नियंत्रित किया जाता है। अगर संक्रमितों की तादाद यूं ही बढ़ती रही तो नीतिगत हस्तक्षेप की गुंजाइश भी सीमित रह जाएगी और वित्तीय स्थिरता को बड़ा खतरा उत्पन्न हो जाएगा।
Date:07-08-20
देश में किस दिशा में बढ़ रही है नाभिकीय ऊर्जा?
विनायक चटर्जी , (लेखक फीडबैक इन्फ्रा के चेयरमैन हैं)
भारत और अमेरिका के बीच ऐतिहासिक असैन्य परमाणु समझौते की घोषणा के 15 साल पूरे हो चुके हैं। इस बहुचर्चित करार पर तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह एवं अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने 2005 में सहमति जताई थी। इस समझौते से जुड़ी घटनाओं ने नई सदी के पहले दशक के उत्तराद्र्ध की भारतीय राजनीति को काफी प्रभावित किया। तत्कालीन सरकार को समर्थन दे रहे वामदलों और मनमोहन सिंह के बीच करार को लेकर तीखी झड़पें हुई थीं। समझौते को अंतिम मुकाम तक पहुंचाने के लिए डॉ सिंह ने व्यक्तिगत स्तर पर पुरजोर प्रयास किए और अपने साथ-साथ कांग्रेस के भविष्य को भी दांव पर लगा दिया था।
मार्च 2008 में इस करार पर दोनों पक्षों की ओर से औपचारिक दस्तखत होने तक कुल स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता में परमाणु ऊर्जा की हिस्सेदारी 2.9 फीसदी थी। उसके 12 साल बाद यह हिस्सेदारी बढऩे के बजाय घटी है और महज 2.5 फीसदी रह गई है।
वास्तविक उत्पादित बिजली के संदर्भ में परिदृश्य थोड़ा बेहतर है। कुल उत्पादित बिजली में परमाणु ऊर्जा का अंश पिछले 10 वर्षों में करीब एक फीसदी बढ़ा है। विडंबना ही है कि इस अवधि में कुल उत्पादित बिजली में तापीय ऊर्जा की हिस्सेदारी 3 फीसदी बढ़ गई है। ऐसा तब है जब यह माना जा रहा था कि कार्बन फुटप्रिंट घटाने की दिशा में भारत की कवायद में परमाणु ऊर्जा एक अहम घटक होगा और इससे देश को ऊर्जा सुरक्षा भी मिलेगी।
ऐसा नहीं है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार के पास नाभिकीय ऊर्जा के लिए कोई महत्त्वाकांक्षी योजना ही नहीं है। इस साल मार्च में संसद को यह बताया गया था कि पांच नाभिकीय बिजली संयंत्रों के निर्माण का काम जारी है जिनकी कुल क्षमता 7,200 मेगावॉट है। इनके अलावा 9,000 मेगावॉट की कुल क्षमता वाले छह अन्य संयंत्रों के निर्माण को मंजूरी देने के साथ वित्तीय स्वीकृति भी दी जा चुकी है। पिछले साल अमेरिका ने आंध्र प्रदेश में छह नाभिकीय रिएक्टर बनाने की सहमति जताई थी। सरकार ने नाभिकीय औषधि में निजी क्षेत्र की भागीदारी और खाद्य उत्पादों के संरक्षण के लिए कृषि में नाभिकीय उपयोग की भी अनुमति दे दी है। भारत ने हाल ही में यूरोपीय संघ के साथ भी असैन्य परमाणु सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इन सबके बावजूद यह साफ है कि असलियत अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं रही है। आखिर गलती क्या हुई? पहली बात, भारत-अमेरिका परमाणु समझौते से उपजी अत्यधिक अपेक्षाओं के बीच भारत ने नाभिकीय दायित्व विधेयक पारित कर दिया जिसमें नाभिकीय उपकरणों के विनिर्माताओं को किसी भी हादसे की सूरत में जवाबदेह ठहराने की बात कही गई है। इस वजह से कई नाभिकीय संयंत्र विनिर्माताओं ने भारतीय बाजार से अपने हाथ पीछे खींच लिए। लेकिन ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के फेलो मनोज जोशी कहते हैं कि नाभिकीय करार के पहले भी कभी हकीकत उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। पहले यह उम्मीद की गई थी कि वर्ष 2000 तक भारत में नाभिकीय ऊर्जा क्षमता बढ़कर 10,000 मेगावॉट हो जाएगी। लेकिन जोशी कहते हैं कि इस लक्ष्य को वर्ष 2020 तक भी हासिल करना किस्मत की बात होगी। इसी तरह नाभिकीय करार के बाद जैसी आसमान छूती उम्मीदें रखी गई थीं, उनमें आगे चलकर कटौती करनी पड़ी। नाभिकीय क्षमता में विस्तार से जुड़ी समस्याएं पुरानी हैं और यह शुरू से ही कमतर प्रदर्शन से प्रभावित रहा है।
भारतीय नाभिकीय परिदृश्य पर लंबे समय से नजर रखने वाले नाभिकीय भौतिकशास्त्री एम वी रमन ने एक पुस्तक में कहा था कि इस क्षेत्र के शासकीय ढांचे का भी थोड़ा दोष रहा है। इसकी सामरिक महत्ता के निहितार्थों का यह मतलब हुआ है कि परमाणु ऊर्जा आयोग एवं परमाणु ऊर्जा विभाग जैसे संगठनों पर अपेक्षाकृत कम निगरानी रही है और उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट किया है जिससे वे कम जवाबदेह रहे हैं। नियामकीय संस्था के तौर पर गठित परमाणु ऊर्जा नियामकीय बोर्ड भी सीधे परमाणु ऊर्जा विभाग को रिपोर्ट करता है जिससे उसकी नियामकीय स्वतंत्रता बाधित होती है। एक नाभिकीय करार से हमारी ही बनाई हुई ये समस्याएं दूर नहीं होंगी। इससे एकदम परे यह बात भी सच है कि इस दशक की शुरुआत में हुए फुकूशिमा परमाणु हादसे के बाद से ही वैश्विक मनोदशा नाभिकीय ऊर्जा को लेकर प्रतिकूल होती गई है। भारत में भी स्थानीय लोगों के तीखे प्रदर्शनों के चलते तमिलनाडु के कुडनकुलम संयंत्र जैसी परियोजना पर विराम लग गया है।
लेकिन असली वजह तो शायद सामान्य अर्थशास्त्र रहा है। वास्तव में, सही मायने में काम तो नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में रहा है। पिछले दशक में कुल स्थापित क्षमता में नवीकरणीय ऊर्जा का हिस्सा नाटकीय रूप से बढ़ते हुए तिगुने से भी अधिक हो गया है। इस दौरान इसकी शुल्क दरें भी बहुत तेजी से गिरी हैं। जोशी कहते हैं, ‘परमाणु बिजली के उलट भारत ने बहुत कम निवेश में ही नवीकरणीय ऊर्जा के मामले में लक्ष्य को भी पीछे छोड़ दिया है।’ हालत यह है कि आज भारत में नवीकरणीय ऊर्जा तापीय ऊर्जा की तुलना में भी बेहद प्रतिस्पद्र्धी है।
इसके उलट नाभिकीय संयंत्रों की पूंजी लागत काफी ऊंची होती है और यहां से उत्पादित बिजली भी महंगी पड़ती है। परमाणु ऊर्जा विभाग नाभिकीय बिजली की शुल्क दरें तय करता है लेकिन इसे अन्य स्रोतों से उत्पादित बिजली के शुल्कों से मुकाबला भी करना होता है। नाभिकीय ऊर्जा देश में दूसरे बिजली क्षेत्रों में हुए सुधारों से तालमेल नहीं बिठा पाई है।
क्या परमाणु ऊर्जा का भारत में अप्रासंगिक होना तय है? यह साफ है कि नाभिकीय ऊर्जा के संस्थानिक एवं नियामकीय ढांचे में सुधार किए बगैर भारत-अमेरिका परमाणु करार के वादे को पूरा नहीं किया जा सकेगा। संस्थानिक ढांचों की दशकों पुरानी मौजूदगी को देखते हुए सरकार को ऐसे सुधार करने होंगे जो इनके कामों में कटौती करें। ऐसा नहीं होने पर 10 वर्षों तक दरकिनार रही परमाणु ऊर्जा विरोधी लॉबी ही शायद आखिर में विजयी हो।
नक्शेबाजी
संपादकीय
पाकिस्तान के लिए सरहद का मामला मानो बच्चों का खेल हो कि जहां चाहा बाहें फैला कर किसी भी इलाके पर अपना दावा ठोक दिया। अभी तक वह कश्मीर और लद्दाख को अपने देश का हिस्सा बताता रहा है। अब उसने कश्मीर के सियाचिन से लेकर गुजरात के जूनागढ़ तक पर अपना दावा जता दिया है। पाकिस्तानी मंत्रिमंडल ने मंगलवार को नया राजनीतिक नक्शा जारी किया, जिसमें भारत के उन सभी इलाकों को पाकिस्तान में दिखाया गया है, जिन्हें लेकर विवाद रहा है। अब इस नक्शे को वह संयुक्त राष्ट्र में पेश करना चाहता है। पाकिस्तान ने यह कदम कश्मीर मेें अनुच्छेद तीन सौ सत्तर खत्म होने की बरसी से एक दिन पहले उठाया। इस मौके पर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री भारत के खिलाफ जम कर बरसे भी। अनुच्छेद तीन सौ सत्तर को हटाने का फैसला पाकिस्तान को फांस की तरह चुभता रहा है। इस मामले को उसने जहां मौका मिला अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उठाया, मगर कोई कामयाबी नहीं मिली। अब उसने सीधे अपने नक्शे में बदलाव कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र का ध्यान खींचने के लिए सीमा विवाद वाले देश इस तरह अपने नक्शों में बदलाव करते रहते हैं। पर इससे पाकिस्तान को सिर्फ अपनी खुन्नस मिटाने के अलावा हकीकत में हासिल क्या होगा, शायद उसे भी ठीक से नहीं पता।
कुछ समय पहले नेपाल ने भी इसी तरह अपना नया राजनीतिक नक्शा जारी कर भारत के हिस्से वाले कालापानी, लिपुलेख और लिंपियाधुरा इलाकों को अपना बताया था। पाकिस्तान भी उसी के नक्शे-कदम पर चल पड़ा है। चीन पहले ही वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास वाले कई इलाकों पर अपना हक जताता रहा है। इसे लेकर दोनों देशों की सेनाएं आमने-सामने हैं, बातचीत का दौर चल रहा है, पर अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सका है। इन स्थितियों को देखते हुए समझा जा सकता है कि पाकिस्तान और नेपाल केवल खुन्नस में या फिर वास्तव में अपने हक के लिए भारत से यह तनातनी मोल लेने को तत्पर नहीं हैं। चीन ने इन दोनों देशों में भारी निवेश किया है। पाकिस्तान पहले ही अमेरिकी सरपरस्ती छोड़ कर चीन के साथ जा लगा है। आतंकवाद के मसले पर पिछले चार-पांच सालों से उस पर अमेरिकी शिकंजा काफी कसा है, जबकि चीन लगातार अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उसका बचाव करता रहा है। चीन का अपना स्वार्थ भी है कि पाकिस्तान में अपनी पैठ बना कर वह भारत पर दबाव बना सकता है। नेपाल में भी अपनी मौजूदगी बनाने के पीछे उसका यही मकसद है कि वहां से भारतीय सेना का गतिविधियों पर वह आसानी से नजर रख सकता है। इसलिए पाकिस्तान ने यह नई नक्शेबाजी चीन के और निकट आने के मकसद से ही की है।
मगर इस तरह पाकिस्तान कभी अमेरिका, तो कभी चीन के हाथों की कठपुतली बन कर कब तक भारत से दुश्मनी निभाता रह सकता है। इमरान खान ने सत्ता की बागडोर संभाली थी, तो उन्होंने सरहद के झगड़ों और दहशतगर्दी को तरजीह देने के बजाय देश की तरक्की को तवज्जो देने का मंसूबा जाहिर किया था। मगर वे भी फिर उसी रास्ते पर लौट आए, जिस पर वहां के पुराने हुक्मरान चलते आए थे। पाकिस्तान मुफलिसी में गर्क है और किसी न किसी ताकतवर देश का दामन पकड़ कर गुजारा चलाता रहा है, ऐसे में वह सरहद के झगड़ों में पड़ कर अपना और नुकसान करेगा। जहां तक संयुक्त राष्ट्र की बात है, वहां पहले ही उसकी असलियत उजागर है, सो उसके नए नक्शे पर शायद ही कोई गौर करे।
परीक्षण अभी बाकी
डॉ. ललित कुमार
शिक्षा नीति पर दिए गए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के वक्तव्य कि नई शिक्षा नीति रोजगार देने वाली साबित होगी की परख भविष्य में ही हो सकेगी। क्रियान्वयन हमारी नीतियों का सबसे कमजोर पक्ष रहा है और आर्थिक मजबूरी तथा संसाधन का काफी हद तक दुरुपयोग हमें हमारे लक्ष्य से हरदम भटकाता रहा है। 1966 में दी गई कोठारी आयोग के शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद के 6% तक खर्च करने की संस्तुति को इतने दिन बाद हमने सैद्धांतिक रूप में इस नीति के माध्यम से स्वीकार किया है। आयोग की दूसरी महत्त्वपूर्ण संस्तुति कि समान शिक्षा प्रणाली को अपनाया जाए, अभी तक हमने सैद्धांतिक रूप में भी स्वीकार नहीं की है। 6% खर्च करने की योजना को मूर्त रूप देना शेष है। अपनी शैक्षिक योजनाओं को आंशिक सफलता से लागू करने का हमारा इतिहास हमारे संकल्प की हवा निकाल देता है। शिक्षा के अधिकार कानून को पूरी तरह लागू न करा पाना, कम विकसित राज्यों में उच्च शिक्षा का सकल नामांकन अनुपात के राष्ट्रीय औसत से काफी पीछे होना, समावेशी शिक्षा की संकल्पना के उलट शिक्षा का निजीकरण की ओर बढ़ना, 10+2+3 प्रारूप को लागू करते हुए +2 की शिक्षा को कमजोर कर डालना, अध्यापक शिक्षा की पूर्ति का 90% से अधिक निजी संस्थानों से पूरा करना, अभियांत्रिकी की शिक्षा को निजीकरण के नाम पर गर्त में धकेल देना आदि जैसे उदाहारण इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि हमें गंभीरता से अपनी योजनाओं और इनके क्रियान्वयन तथा इनके सतत मूल्यांकन पर कार्य करना ही होगा।
वर्तमान शिक्षा नीति व्यापक है और शिक्षा की वर्तमान स्थिति के आकलन के क्रम में ईमानदार भी। भारतीयता के पुट को समाहित करते हुए शिक्षा को अंतरराष्ट्रीय आकार देने की कोशिश की गई है। शिक्षक के प्रति सम्मान का भाव और उनकी पुरानी गरिमा को लौटा सकने का संकल्प भी मुखरित है। विद्यालयी शिक्षा, उच्च शिक्षा, अध्यापक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, दूर शिक्षा आदि के विकास की योजना विस्तार से वर्णित है, और इसमें कोई संदेह नहीं कि हम क्रियान्वयन की चुनौतियों को स्वीकार कर अपनी संपूर्ण शिक्षा को इस नीति की मदद से धार दे सकते हैं। विद्यालयी शिक्षा की संरचना को 10+2 से 5+3+3+4 में परिवर्तित करना मनोविज्ञान की विकास की अवस्था के अनुरूप है। विद्यालयी पूर्व तीन वर्ष को पहली एवं दूसरी कक्षा के साथ मिलाकर पांच वर्ष की शुरु आती शिक्षा; फिर तीन वर्ष की तीसरी से पांचवी; तीन वर्ष की छठी से आठवी तथा माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक को मिलाकर चार वर्षो की नौवी से बारहवी की शिक्षा की योजना शैक्षिक एवं मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अनुकूल है। इस क्रम में हमें इस संपूर्ण विद्यालयी शिक्षा को शिक्षा के अधिकार कानून के दायरे में लाकर अनिवार्य किन्तु गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की चुनौती का सामना करना चाहिए। बहुभाषावाद एवं सांकेतिक भाषा का विकास, नीति के संकल्प में मुखर हैं। नीति का यह मानना कि भाषा विकास की दृष्टि से 2-8 वर्ष की मानव अवस्था महत्त्वपूर्ण है। सही सोच है, किन्तु भाषा की क्षेत्रीय राजनीति की वजह से हमें एक राष्ट्रभाषा की स्वीकृति मिलेगी-संदेह है। यह दुखद भी है और राष्ट्रीय एवं भावात्मक विकास की दृष्टि से चुनौतीपूर्ण भी। शिक्षक को उचित स्थान देने का संकल्प प्रबल है, परन्तु नियोजित, पारा आदि जैसे शिक्षकों के बूते शिक्षा की सूरत बदलने की कोशिश करने वाला राष्ट्र शिक्षण व्यवसाय एवं शिक्षक के वृतिक विकास के साथ न्याय कर पाएगा? संदेह है। नीति ने विद्यालयी शिक्षा में ड्रॉपआउट एवं इसको दूर करने के उपाय पर व्यापक चर्चा की है, जरूरत अध्यापक शिक्षा में हो रहे ड्रॉपआउट के अध्ययन की भी है। चार-वर्षीय बी.एड पाठयक्रम की स्वीकार्यता में शिक्षाविद के एक वर्ग को संदेह है।
इस नीति के अनुसार उच्च शिक्षा में सबसे बड़ा सुधार उच्च शिक्षा की संबद्धता की प्रकृति को धीरे-धीरे समेटने का है। विश्व के विकसित राष्ट्र संबद्ध महाविद्यालय एवं संबद्ध विश्वविद्यालय का सहारा नहीं लेते और गुणवत्ता की दृष्टि से इसे सबसे निम्न दरजे का संस्थान माना जाता है। एकल विश्वविद्यालय एवं स्वायत्त महाविद्यालय के साथ उच्च शिक्षा की योजना निश्चय ही इसकी गुणवत्ता को धनात्मक रूप से प्रभावित करेगी। उच्च शिक्षा के सकल नामांकन अनुपात को 50% तक ले जाने के क्रम में हमें क्षेत्रीय विषमता को दूर करना होगा और इसके लिए उच्च गुणवत्ता वाले महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय की स्थापना प्राथमिकता के आधार पर अविकसित प्रदेशों एवं जिलों में करनी होगी। अवकाशप्राप्त शिक्षकों को मानव संपदा के रूप में अपनाने की नीति की योजना सराहनीय है और उच्च शिक्षा में यह कदम पहले औपचारिक और फिर बाद में अनौपचारिक शिक्षा के रूप में क्रान्तिकारी सिद्ध होने वाला है। विदेशी विश्वविद्यालयों को लाने एवं निजी भागीदारी को बढ़ाने के साथ यह सुनिश्चित करना कठिन प्रतीत होता है कि शिक्षा के बाजारीकरण एवं व्यावसायिकरण को क्या हम रोक पाएंगे। उच्च शिक्षा में हर स्तर पर प्रमाणपत्र देने एवं अधूरी शिक्षा को फिर से पूरी कर सकने का विकल्प अच्छा कदम है।
भारत के ज्ञान एवं पुरानी शिक्षा पद्धति को अपनाने का संकल्प नई नीति में समाहित है, किन्तु हमें राष्ट्र के चारित्रिक विकास पर कठोरता से हमारी गुरुकुल प्रणाली के अनुशासन के साथ काम करना होगा। फैला भ्रष्टाचार एवं नैतिकता का हृास हमारी बड़ी सामाजिक एवं राष्ट्रीय चुनौती हैं, और शिक्षा के माध्यम से मूल्य संचरण कर हमें राष्ट्र के नैतिक एवं चारित्रिक विकास का प्रयास भी करना ही होगा। सभी प्रकार के संसाधनों के उचित एवं उपयुक्त विकास के लिए यह जरूरी है। आज अर्थ के लिए शिक्षा और शिक्षा के लिए अर्थ के बीच सामंजस्य बैठाने की जरूरत है। हम विदेशी और निजी विश्वविद्यालयों के भरोसे अपनी उच्च शिक्षा को नहीं छोड़ सकते। ऐसी व्यवस्था समावेशी शिक्षा, कल्याणकारी राज्य, आरक्षण आदि के हमारे मूल समाजोपयोगी सिद्धांतों के रास्ते में रुकावट की तरह होगी। सामाजिक विषमता की खाई को पाटने की हमारी मूल भावना की राह में विदेशी एवं निजी भागीदारी को देश का एक वर्ग उसी तरह घातक मानता है, जैसा वह सरकारी संपत्तियों के विनिमेश को मानता है। शिक्षा के निजीकरण, व्यावसायीकरण एवं विदेशीकरण पर हमें लगातार नजर रखनी चाहिए ताकि भविष्य में चीनी वस्तुओं की तरह हमें खास शिक्षा को त्यागना न पड़े।
