
04-08-2021 (Important News Clippings)
To Download Click Here.
Date:04-08-21
वर्षों से सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अनदेखी क्यों हो रही थी?
संपादकीय
संविधान कागज के टुकड़े पर लिखी इबारत बनकर रह जाएगा, आगर सरकारें उन्हें नजरअंदाज करने लगे। इसी क्रम में न्यायपालिका के फैसले भी अर्थहीन हो जाएंगे, अगर सरकारें व संस्थाएं उन्हें न माने। सरकार के पास तो अपनी बात मनवाने के लिए पुलिस का डंडा और कानून आदि होता है, लेकिन न्यायालयों के पास अपने आदेश मनवाने को न तो पुलिस है न कोई अतिरिक्त ताकत। मानहानि के आदेश भी उसे सरकार की पुलिस के जरिए ही मनवाने पड़ते हैं। लेकिन चंद दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट भी एक जनहित याचिका के तहत यह जानकार चौंक गई कि सन 2015 में उसके द्वारा रद्द किए गए आईटी एक्ट की धारा 66-ए के तहत आज भी लोगों पर मुकदमे चल रहे हैं और निचली अदालतें सजा तक दे रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख के बाद केंद्र ने राज्यों को ताकीद की कि इस कानून का इस्तेमाल न किया जाए, लेकिन आज भी कई राज्यों की पुलिस इसे इस्तेमाल कर रही है। जब याचिकाकर्ता ने हाल ही में कोर्ट का ध्यान इस ओर दिलाया, तो कोर्ट ने कहा निचली अदालतों को तो हम ठीक कर लेंगे लेकिन सभी राज्य विस्तार से बताएं कि उनके यहां कितने मामले पिछले छह वर्षों में यानी कोर्ट द्वारा इस कानून को रद्द करने के बाद लाए गए और मुकदमे तत्काल खत्म क्यों नहीं किए गए? दरअसल सन 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इस सेक्शन को संविधान के अनुच्छेद19(1) (ए) के खिलाफ और अनुच्छेद (2) में दिए गए युव्तियुवत निर्बधों की गलत समझ’ करार दिया था। यह कानून पुलिस को शक्ति देता था कि वह इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के जरिये प्रसारित आपत्तिजनक विषय-वस्तु का संज्ञान ले सकती है। सन 2008 में कानून में इस प्रावधान के जोड़े जाने के बाद कई राज्यों की पुलिस ने सरकार के खिलाफ लोगों की टिप्पणियों का मनमाना अर्थ निकालकर उन पर केस शुरू कर दिए। हाल के दौर में यह कानून सरकारों का प्रमुख हथियार बन गया था।
Date:04-08-21
2024 में दल क्या ये 4 चुनौतियां स्वीकारेंगे?
संकेत उपाध्याय, ( वरिष्ठ पत्रकार )
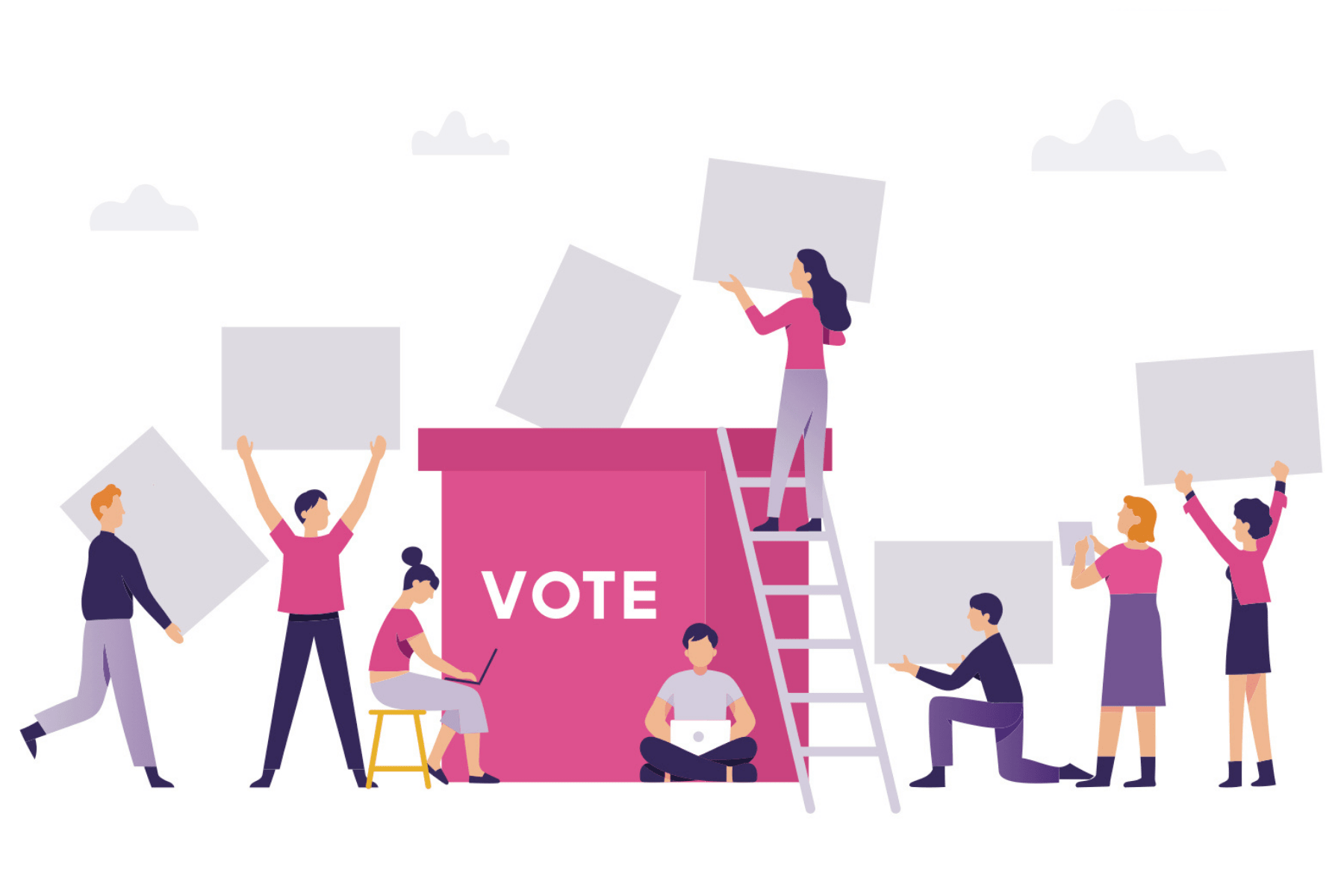
चुनावी सीजन हिंदुस्तान में हमेशा ही रहता है। चुनावी लेकिन लोकसभा चुनाव और उसकी तैयारी हमेशा महत्वपूर्ण रही है। 2009 में हार के बाद भाजपा ने 2010 से ही चुनावी यात्रा शुरू कर दी थीं। तब मुद्दा भ्रष्टाचार था। उसी पर रैली, वादे होते थे। नतीजा सबके सामने 2014 में आ गया। यह हुई इतिहास की बात। आज हम राजनीतिक दलों को चुनौती देना चाहते हैं कि इस देश में 2024 से पहले मुद्दा क्या हो? वे जो नेता तय करें या वे जिनसे जनता का सरकारें है? इससे पहले नेता अपने मुद्दों में उलझाएं, हम ऐसी 4 चीज़ें लाए हैं जो आज तक चर्चा में तो छोड़िए, पार्टी के मैनिफेस्टो तक भी नहीं पहुंचीं। ये 4 ऐसी चुनौतियां हैं, जिसपर सारे नेता एक हो जाते हैं। ये पार्टियों को खुला चैलेंज है कि क्या आप इन 4 चीजों का जिक्र 2024 के घोषणापत्र में कर सकते हैं ?
चैलेंज 1 – राजद्रोह का कानून ख़त्म करोः अंग्रेज चले गए, उनके खुद के देश से उनका बनाया यह कानून चला गया लेकिन इसका राजनीतिक उपयोग भारत में आज तक हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट तक ने इसे खत्म करने की चर्चा पर ज़ोर दिया है। लेकिन नेता यही कहते हैं कि कानून रहना चाहिए, बस उसका दुरूपयोग न हो। आज ऐसे कानून की क्या ज़रूरत जो मूल रूप से सरकार के खिलाफ बोलने पर उपयोग होता हो ? अंग्रेज धारा 124ए इसीलिए लाए थे कि कोई उस समय की सरकार के खिलाफ विरोध न करे। हमारे नेताओं ने राजद्रोह को देशद्रोह की तरह प्रस्तुत कर दिया है। यह कानून दो ही तरीके से ख़त्म हो सकता है। या तो अदालत करें या संसद में नेता। तो बया कोई पार्टी यह चुनौती स्वीकारेगी ? संसद में इसे रद्द करेगी ?
चैलेंज 2- पुलिस रिफॉर्मः भारत की पुलिसिया प्रणाली में सन् 1861 से कोई विशेष बदलाव नहीं हुआ है। आज़ादी के 75 साल बाद भी, इस व्यवस्था में एक अल्पविराम तक नहीं बदला। अंग्रेज़ों के लिए बनी व्यवस्था अब नेताओं के लिए बनी व्यवस्था हो गई है। तमाम सरकारें आरोप से घिरी रहती हैं कि वे पुलिस के डंडे के बल पर चुनाव अपने हिसाब से कर लेती हैं। विपक्ष भी हमला करता है लेकिन खुद सत्ता में आकर उसी पुलिस सिस्टम को अपने लिए इस्तेमाल करता है। जैसे उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में जिस पुलिस पर सरकारी दबाव होने का आरोप सपा ने लगाया, बैसा ही आरोप उनपर 2015-16 में लगा था। पुलिस व्यवस्था बदलने पर कई लोगों ने रिपोर्ट लिखी है, सुझाव दिए हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन की दूसरी रिपोर्ट ने 2007 में ही सुझाया कि पुलिस का राजनीतिक उपयोग इतना है कि पुलिस अब निजी व राजनीतिक इस्तेमाल का औजार बन गई है। नेशनल पुलिस कमीशन 1977, रिबेहरो समिति 1998, पद्मनाभइया समिति 2000, मलिमथ समिति 2003, यहां तक कि 2006 में सुप्रीम कोर्ट तक के निर्देश तक, करीब आठ प्रयास हो चुके हैं पुलिस सुधार के। लेकिन पुलिस नेताओं और सत्ता के चंगुल से बाहर नहीं आ पाई। तो हे किसी पार्टी में दम जो जनता से वादा कर सके कि पुलिस को आजद कर उन्हें मज़बूत बनाएंगे ?
चैलेंज 3- स्वास्थ्य पर जीडीपी का 6% खर्चः भारत स्वास्थ्य पर जीडीपी का मात्र 1.26% खर्चता है। स्वास्थ्य व्यवस्था खस्ताहाल है। नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 का कहना है कि सरकार को हेल्थ बजट 2025 तक 2.5% कर देना चाहिए। इस प्रस्ताव में तब कोरोना जैसी बीमारी के बारे में नहीं सोचा गया था। विशेषज्ञों का मानना है कि जीडीपी का 6% हेल्थ बजट होना चाहिए। डेटोल कंपनी द्वारा किए गए सर्वे में पाया गया कि स्वास्थ्य पर खर्च देश की अर्थव्यवस्था को 37% मुनाफा दे सकता है। कोरोना की मार के हे ,, यह क्यों नहीं हुआ ? क्या कोई पार्टी यह चैलेंज लेगी ? इस मुद्दे को मैनिफेस्टो में डालेगी ? चैलेंज 4- शिक्षा पर 6% खर्च: जनसंख्या नियंत्रण कानून पर खासी चर्चा हुई। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार इससे सहमत नहीं हैं। वे कहते हैं शिक्षा जो बदलाव और जागरूकता ला सकती है, वह कानून नहीं। और यह हमने होते देखा है। फर्टिलिटी रेट लगातार कम हो रही है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 1960 में एक औरत 5.91 बच्चों को जन्म देती थी। यह संख्या 1990 में 4, 2000 में 3.30 और 2018 में 2.22 हो गई। जो सफलता शिक्षा और जागरूकता फैलाकर मिली, उसके लिए कानून क्यों लाना चाह रहे हैं? असली चुनौती है कि राज्य शिक्षा पर खर्च बढ़ाएं। 1968 से हर नेशनल पॉलिसी ने सुझाव दिया है कि हम जीडीपी का 6% शिक्षा पर लगाएं। जबकि 2019-20 में भी हम सिर्फ 3.7% तक ही पे हैं। क्या यह राजनीतिक रूप से घनघोर नाकामी नहीं है ? तो नेता कम से कम घोषणापत्र में यह करने का वादा तो करें?
तो बोलो नेता लोग, है हिम्मत ? करोगे ये वादे ?
Date:04-08-21
मनमर्जी पर लगाम
संपादकीय
भारत जैसे सशक्त लोकतांत्रिक परंपरा वाले देश में यह एक विचित्र स्थिति है कि जो कानून अस्तित्व में नहीं है, उसके तहत यहां अलग-अलग राज्यों की पुलिस किसी को गिरफ्तार करे और उसे नाहक ही प्रताड़ित करे। लेकिन ऐसा पिछले करीब पांच सालों से लगातार चलता रहा, जब सुप्रीम कोर्ट ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा-66 ए को रद्द कर दिया था और पुलिस इस कानून का इस्तेमाल करके लोगों को परेशान करती रही। इस मसले पर एक महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने काफी नाराजगी जताई थी। अब सोमवार को एक बार फिर शीर्ष अदालत ने एक गैरसरकारी संगठन की याचिका पर राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और सभी राज्यों के उच्च न्यायालयों को नोटिस जारी कर इस बात पर जवाब मांगा है कि 2015 में ही रद्द हो चुकी इस धारा के तहत अब भी लोगों को खिलाफ मामले दर्ज किए जा रहे हैं। यह समूचे देश में कानून लागू करने वाले महकमे की कार्यशैली पर सवालिया निशान है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अहमियत देने, उसका मतलब समझने और उस पर अमल करने के बजाय उसे ताक पर रख कर मनमानी करने की वजह आखिर क्या रही!
गौरतलब है कि देश भर में पुलिस की ओर से मामूली बातों पर भी लोगों को गिरफ्तार या प्रताड़ित करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66ए के बेजा इस्तेमाल से जुड़ी शिकायतें जब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची थी, तब 2015 में ही उसने इस धारा को ही रद्द कर दिया था। इसके बावजूद जमीनी स्तर पर देश के अलग-अलग हिस्सों में कानून की इस धारा को हथियार बना कर इसके तहत गिरफ्तारी होती रही। पुलिस राज्य का विषय है और इस नाते राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों का यह दायित्व है कि वह लागू कानूनों की वैधता और कसौटी पर सही और न्यायिक होने का हर वक्त ध्यान रखे। सवाल है कि इतने साल पहले सुप्रीम कोर्ट में कानून की इस धारा के रद्द होने की सूचना सरकारों के पास कैसे और क्यों नहीं पहुंची! जबकि इस दौरान इस कानून के तहत कई लोगों को नाहक ही प्रताड़ना झेलनी पड़ी। एक रद्द कानून के हथियार से लोगों को परेशान करने का मुआवजा क्या होगा और इतने लंबे समय तक इस धारा के इस्तेमाल करने के लिए संबंधित महकमे कोई अफसोस जाहिर करेंगे! क्या पुलिस इस संदर्भ में जानकारी और व्यवहार को लेकर सवालों के कठघरे में नहीं खड़ी है?
यह किसी से छिपा नहीं है कि कानून के मामूली नुक्तों की वजह से किसी व्यक्ति को अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा जेल में गुजारना पड़ सकता है। इसके व्यावहारिक पहलुओं और असर के मद्देनजर ही सुप्रीम कोर्ट ने एक महीने पहले साफ शब्दों में यह टिप्पणी की थी कि जो हो रहा है वह भयानक, चिंताजनक और चौंकाने वाला है। दरअसल, सूचना प्रौद्योगिकी कानून की निरस्त धारा 66ए के तहत सोशल मीडिया पर भड़काऊ टिप्पणियां करने के दोषी किसी व्यक्ति को तीन साल तक कैद और जुर्माने की सजा का प्रावधान था। लेकिन व्यवहार में सरकारों और पुलिस ने इसका जिस तरह बेजा इस्तेमाल किया, अभिव्यक्ति की आजादी को बाधित किया गया, वह देश की लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए एक अफसोसनाक स्थिति थी। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने 24 मार्च, 2015 को ही श्रेया सिंघल मामले में इस धारा को रद्द कर दिया था। यों भी विविधताओं से भरे हमारे देश में एक मसले पर अलग-अलग क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की राय भिन्न हो सकती है। लेकिन उसकी मनमानी व्याख्या करके लोगों को परेशान, गिरफ्तार और प्रताड़ित करना लोकतंत्र को ही बाधित करने का जरिया बनेगा।
Date:04-08-21
आश्चर्य‚ किन्तु सत्य
संपादकीय
सूचना प्रौद्योगिकी कानून की धारा 66ए इन दिनों चर्चा में है। सुप्रीम कोर्ट ने 24 मार्च‚ 2015 में इस धारा को असंवैधानिक ठहराते हुए निरस्त कर दिया था। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से कई राज्यों की पुलिस इस धारा के तहत मामले दर्ज कर रही थी। पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने भी पुलिस की इस गैर–कानूनी कार्रवाईपर हैरानी जताते हुए सरकार की तीखी आलोचना की थी। वास्तव में राज्यों की पुलिस की यह कार्रवाई बताती है कि सरकार के विभिन्न अंगों और एजेंसियों के बीच समन्वय का कितना अभाव है। अगर देश की शीर्ष अदालत का कोईफैसला निचले स्तर पर अमल न हो पाए तो निश्चित रूप से यह चिंता का विषय है। अब शीर्ष अदालत ने एक गैर–सरकारी संगठन ‘पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज’ (पीयूसीएल) की याचिका पर सुनवाईकरते हुए सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को नोटिस जारी करके चार हफ्ते में जवाब मांगा है। सूचना प्रौद्योगिकी कानून की धारा 66ए के प्रावधानों के अंतर्गत सोशल मीडि़या पर आपत्तिजनक पोस्ट ड़ालने वालों के विरुद्ध पुलिस मुकदमा दर्ज कर रही थी। इस धारा में अनेक खामियां थीं। इसकी परिभाषा बहुत अस्पष्ट थी। इसके कारण पुलिस ऐसे ऑनलाइन पोस्ट ड़ालने वालों के विरुद्ध भी मुकदमा दर्ज करती थी‚ जिनके पोस्ट आपत्तिजनक श्रेणी में नहीं आते थे। इस धारा के तहत आपत्तिजनक पोस्ट ड़ालने पर तीन साल की सजा का प्रावधान था। लोगों को याद होगा कि शिवसेना के प्रमुख बाल ठाकरे के निधन के बाद मुंबई का जनजीवन अस्त–व्यस्त होने पर शाहीन और रेणु ने सोशल मीडि़या पर टिप्पणी की थी‚ जिसके कारण उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। इस घटना के बाद मुंबई की कानून की छात्रा श्रेया सिंघल ने इस कानून के विरुûद्ध सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। शीर्ष अदालत ने यह स्वीकार किया कि सूचना प्रौद्योगिकी कानून की धारा 66ए संविधान के अनुच्छेद 19(1) यानी अभिव्यक्ति की आजादी का हनन करती है। शीर्ष अदालत ने इस आधार पर इस कानून को निरस्त कर दिया था। लोकतंत्र में सभी नागरिकों को यह अधिकार है कि वे देश और समाज में होने वाली किसी घटना पर अपनी राय व्यक्त कर सकें। वास्तव में धारा 66ए लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन करने वाली थी। उम्मीद की जानी चाहिए कि पुलिस इस मृत काननू के तहत अब किसी भी नागरिक के विरुûद्ध मुकदमा दर्ज करने का दुस्साहस नहीं कर पाएगी।
Date:04-08-21
तकनीक में एक कदम और
संपादकीय

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को डि़जिटल भुगतान समाधान ‘ई–रुपी ‘ लॉन्च करते हुए कहा कि प्रौद्योगिकी अपनाने में भारत दुनिया के किसी देश से पीछे नहीं है। सच तो यह है कि नवोन्मेष और सेवा प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल में वैश्विक नेतृत्व की क्षमता रखता है। यह वाउचर आधारित डि़जिटल भुगतान सेवा है‚ जिससे सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों तक कम समय में सब्सिड़ी पहुंचाने में मदद मिलेगी। निजी संस्थान भी इसका इस्तेमाल ड़ोनेशन या अपने कर्मचारियों के उपचार–उनके बच्चों की पढ़ाई के भुगतान के लिए कर सकते हैं। अनुमान है कि 90 करोड़ लोगों को इस सुविधा से लाभ मिलेगा। यह व्यवस्था व्यक्ति विशेष और उद्देश्य आधारित है‚ जिसके तहत संबंधित व्यक्ति के मोबाइल पर एसएमएस या क्यूआर कोड़ के जरिए वाउचर मुहैया कराया जाएगा। इसका इस्तेमाल तय योजना की सेवा या उत्पाद की खरीद में होगा। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडि़या ने वित्त सेवा विभाग‚ परिवार कल्याण एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के साथ मिलकर यह व्यवस्था तैयार की है। अभी यह योजना आयुष्मान भारत जैसी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए शुरू की गई है। जल्द ही अन्य योजनाओं को भी इसमें शामिल किया जाएगा। इस सुविधा से सरकारी योजनाओं का जमीनी स्तर पर प्रभाव और विस्तार तेजी से बढ़ सकेगा। सामाजिक योजनाओं से लाभान्वित होने में आसानी होगी। सबसे बड़़ी बात तो यह कि सामाजिक योजनाओं का लाभ सीधे लक्षित व्यक्ति को मिल सकेगा। चूंकि व्यवस्था प्रीपेड़ है‚ इसलिए बिचौलियों की भूमिका खत्म हो जाएगी। अभी तक होता यह रहा है कि लोगों तक बिचौलिये लाभ नहीं पहुंचाने देते। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (ड़ीबीटी) के जरिए 300 सरकारी योजनाओं के लाभ 90 करोड़ जनता तक पहुंचाए जा रहे हैं। महामारी में 17.5 लाख करोड़ रुपये ड़ीबीटी के जरिए लाभार्थियों के खाते में भेजे गए। सीधे खाते में पैसे जाने के बाद पता नहीं चलता कि उस पैसे का उपयोग लाभार्थी किस तरीके से कर रहा है। ई–रुपी की व्यवस्था से पैसे का सही उपयोग सुनिश्चित किया जा सकेगा। बेशक‚ हाल के वर्षों में तकनीक का फायदा गरीबों तक पहुंचाने के लिए देश में डि़जिटल संसाधन जुटाने के काम में तेजी आई है और फिनटेक का बहुत बड़ा आधार तैयार हो चुका है।
Date:04-08-21
सवाल भी‚ बवाल भी‚ जवाब भी
नवल किशोर कुमार
भारत की सियासत में जाति का ताना–बाना कोई नई बात नहीं है। कहा जाता है कि जाति नहीं जाती। कहना होगा कि भारत में जाति एक सच्चाई रही है। सभी यह मानते भी हैं यानी इस एक बात पर कहीं भी किसी भी वर्ग में कोई मतभेद नहीं है। एक बार फिर जाति का सवाल मुखर हो गया है। कारण है कि जल्द ही भारत सरकार जनगणना शुरू कराने जा रही है। लेकिन इसी बीच सरकार के ऊपर जातिगत आधार पर जनगणना कराए जाने का दबाव बनाया जाने लगा है। लगभग ऐसा ही दबाव वर्ष 2011 में जनगणना के पहले भी बनाया गया था और तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार ने इसे मान भी लिया था लेकिन तब जो जातिगत जनगणना कराई गई‚ उसका क्या हुआ‚ कोई नहीं जानता। यह आज तक रहस्य ही है। लिहाजा‚ एक बार फिर से मांग की जा रही है कि जातिगत जनगणना कराई जानी चाहिए। अनेक राजनीतिक दलों‚ जिनमें सरकार में साझीदार दल भी हैं‚ यह मांग जोर–शोर से उठा रहे हैं। उनके तेवर देखकर लग रहा है कि वे इस मुद्दे पर आरपार के मूड़ में हैं। और किसी भी सूरत में इस मांग को मनवाने से पीछे नहीं हटेंगे। चाहे उन्हें इस मांग को मुद्दा बनाकर ही चुनावी मैदान में उतरने की नौबत का सामना करना पड़े ।
लेकिन इस बार का नजारा थोड़ा अलग है। केंद्र में एनडीए की सरकार है। मांग करने वालों में उत्तर भारत के अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लोगों के अलावा दक्षिण भारत से भी आवाजें मजबूती से उठ रही हैं। स्वयं एनडीए इस मुद्दे पर दो फाड़ होता दिख रहा है। मसलन‚ एनडीए के घटक जनता दल यूनाईटेड ने स्पष्ट कर दिया है कि वह जातिगत जनगणना चाहता है। एनडीए के नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तो यहां तक कह दिया है कि यदि केंद्र सरकार जातिगत जनगणना नहीं कराएगी तो वह बिहार में अपने बूते जातिगत जनगणना कराएंगे। इस सवाल पर बिहार में उन्हें मुख्य विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दल (राजद) और कांग्रेस का साथ भी मिला है। वहीं उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी (सपा) की ओर से इस मांग को चुनावी मुद्दा तक बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी इस बाबत मांग तेज कर दी है। दक्षिण भारत के राज्य तमिलनाडु में इसे लेकर पहल स्वयं राज्य के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन कर रहे हैं।
फिलहाल जो द्रश्य है‚ उसके हिसाब से गैर– भाजपाई ओबीसी (नीतीश कुमार जैसे एनडीए वाले भी) एक सुर में जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं। लगता नहीं कि केंद्र में आरुढ़ मोदी सरकार इस मांग को नजरंदाज कर पाएगी। बहरहाल‚ ऐसे में सवाल जरूर पूछा जा रहा है कि यदि केंद्र सरकार जातिगत जनगणना नहीं कराती है‚ तो क्या ये सभी पार्टियां एक साथ राजनीतिक ताकत बनकर सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी करेंगीॽ उसके पहले सवाल यह भी कि क्या यह ऐसा सटीक मुद्दा है‚ जिसके कारण ओबीसी के लोग गोलबंद हो सकेंगेॽ कहना न होगा कि ओबीसी की लामबंदी अब तक तो सशक्त ही रही है।
सियासी गलियारे में ओबीसी को यह बताने की कोशिशें भी तेज हो गई हैं कि जातिगत जनगणना से सबसे अधिक नुकसान ओबीसी को ही होगा। कहा यह जा रहा है कि यदि आंकड़े सामने आएं तो यह मुमकिन है कि ओबीसी की समृद्ध जातियां और पीछे रह गई जातियों के बीच तनाव बढ़ेगा और इसका असर राजनीतिक समीकरणों पर भी पड़ेगा। एक तरह से यह बताने की कोशिश हो रही है कि यथास्थिति को कायम रखा जाए ताकि ‘जितनी जिसकी संख्या भारी‚ उसकी उतनी हिस्सेदारी’ को टाला जा सके। सरकार का मन–मिजाज भी फिलहाल यही है।
लेकिन इस पूरे मामले में यह बात ममहत्वपूर्ण है कि आरक्षण‚ जिसका कि उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 340‚ अनुच्छेद 341 और अनुच्छेद 342 में किया गया है‚ के लागू होने के कारण समाज में हालात बदले हैं। हालांकि अनुच्छेद 341 में अनुसूचित जाति और अनुच्छेद 342 में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण के स्पष्ट प्रावधान के कारण इन वर्गों को आरक्षण देश में संविधान लागू होने के साथ ही मिलने लगा था। लेकिन अनुच्छेद 340 में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए स्पष्ट रूप से आरक्षण का उल्लेख नहीं होने के कारण सरकार को पहले काका साहेब कालेलकर आयोग बनाना पड़ा और बाद में बीपी मंडल आयोग। कालेलकर आयोग की रिपोर्ट तो तत्कालीन नेहरू सरकार ने ठंडे बस्ते में डाल दी थी लेकिन मंडल आयोग की रिपोर्ट को भारत सरकार ठंडे बस्ते में नहीं डाल सकी और रिपोर्ट समर्पित किए जाने के करीब दस साल बाद उसे लागू करना ही पड़ा। इस प्रकार ओबीसी को आरक्षण पाने के लिए 40 साल तक इंतजार करना पड़ा।
अब चूंकि सियासत में इंतजार का एक रूप संघर्ष भी होता है। यही हुआ भारतीय राजनीति में। आरक्षण को लेकर पहले लोहिया ने लड़ाई लड़ी। उन्होंने नारा दिया था–संसोपा ने बांधी गांठ‚ पिछड़ा पावे सौ में साठ। फिर बिहार में अमर शहीद जगदेव प्रसाद ने 90 और 10 का आंकड़ा दिया था और कहा कि नब्बे पर दस का शासन नहीं चलेगा। बाद के दिनों में कांशीराम ने दलित–ओबीसी एकता के लिए पहल की और 85 फीसदी की बात कही। उधर 1970 के दशक में यूपी‚ बिहार और मध्य प्रदेश आदि‚ जो भारत के बड़े राज्य हैं‚ की राजनीति तेजी से बदलने लगी। पिछड़ा वर्ग मजबूत हो रहा था। परिणाम यह हुआ कि 1977 में जैसे ही मोरारजी देसाई की सरकार बनी‚ पिछड़ा वर्ग का दबाव इतना बढ़ गया कि उन्हें मंडल कमीशन का गठन करना पड़ा। इस आधार इतना तो कहा ही जा सकता है कि ओबीसी वर्गों को अपने आरक्षण के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा है और इस संघर्ष ने देश की सियासत को भी बदला है।
मौजूदा दौर में हालत यह है कि देश के प्रधानमंत्री तक को अपनी जाति का उल्लेख करना पड़ता है। उन्हें इसकी घोषणा करनी पड़ती है कि वे ओबीसी समुदाय से आते हैं। अभी हाल ही में जब केंद्रीय मंत्रिपरिषद का विस्तार और फेरबदल हुआ तब भाजपा की ओर से इसका श्रेय लेने की कोशिश की जा रही है कि मंत्रिपरिषद में 27 ओबीसी मंत्री हैं। इस तरह यह तो तय है कि यदि भारत सरकार जातिगत जनगणना नहीं कराती है तो ओबीसी वर्ग चुप नहीं बैठेगा। वह संघर्ष करेगा। उसके लिए संघर्ष करने से यकीनी तौर पर कहा जा सकता है कि राजनीतिक समीकरण भी बदलेंगे। हालांकि यह बदलाव कितनी तेजी से होगा‚ इसका आकलन फिलहाल तो जटिल ही है। इसकी वजह यह भी है कि चुनाव के मौके पर बिखराव होना ओबीसी वर्ग का इतिहास रहा है। इन सबके बावजूद यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि ओबीसी का मुद्दा आने वाले दिनों में हर हाल में राजनीति के केंद्र में रहेगा। यदि जातिगत जनगणना करा दी जाती है‚ तो निश्चित तौर पर ओबीसी जातियों के बीच भी हलचल मचेगी लेकिन इसका एक सुखद परिणाम यह भी संभव है कि विकास के क्रम में जो पीछे रह गए हैं‚ उन्हें आगे आने का मौका मिलेगा।