
03-05-2024 (Important News Clippings)
To Download Click Here.
 Date:03-05-24
Date:03-05-24
My Marriage, My Way
Laws make marriage complicated. State’s role should only be in registering marriages, not specifying sacraments
TOI Editorials

Why is this jaw-dropping? Because up and down the country Indians get married in a glorious diversity of ways. And all of these should have equal standing in the eyes of modern law. But between the different laws that pronounce rigidities on the matter, they don’t. The judges in this instance declared, “marriage is not an event for ‘song and dance’ and ‘wining and dining’.” But why can’t it be? Or rather, in the countless cases where it already is, surely law shouldn’t ruin the party.
HMA itself has been criticised for flattening wedding practices over time. As examples, scholars point to the fading of matrilineal practices like Aliyasantana in Karnataka and Marumakkathayam in Kerala. Besides, it only refers to Sagai, Kanyadan and Saptapadi. That’s very despiriting for, say, Shubho Drishti and Arundhati Nakshatra. Not to mention all the marriages that completely sidestep the named trinity.
Is there any elegant solution to all this confusion and exclusion? Yes! The state should remain the registry for all marriages, but no longer have anything to do with sacraments and ceremonies.
The Special Marriage Act, 1954 does wear the dress of such a solution. But, from its 30-day notice to how it’s being undermined by anti-conversion laws, its embodied reality is citizen-unfriendly. Moreover, the vast majority of marriages take place under other, religion-based laws, which, like HMA, have very specific requirements for a “solemnised” marriage. What we need is a dramatically reformed version of SMA, where it becomes the sole interface between the state, law and citizens. Why should the state only recognise marriages that limit themselves to a rigid menu of options? Real India certainly doesn’t. Quite happily so. But SC reminded us how vulnerable this happiness is. Better check if your wedding meets the “appropriate ceremonies” criteria.
अधिकार और सीमा
संपादकीय
इसमें कोई दोराय नहीं कि अगर कोई व्यक्ति कानून के विरुद्ध काम करता है तो उस पर कार्रवाई होना चाहिए। मगर कानून को अमल में लाने वाली कोई एजंसी अगर अपने अधिकारों को असीमित मानने लगे और उसके रवैये से मनमानी का संकेत मिलने लगे तो सवाल उठना स्वाभाविक है। पिछले कुछ समय से प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की सक्रियता ने सबका ध्यान आकृष्ट किया है और यह धारणा बनी है कि भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों के खिलाफ कार्रवाई में तेजी आई है। मगर इसके साथ ही विपक्षी दलों ने कई बार सवाल उठाए हैं कि ईडी अपने अभियानों में सुविधा और आग्रहों के मुताबिक चुने हुए लोगों के खिलाफ कार्रवाई करती है और उसकी सक्रियता में एक खास तरह का आग्रह दिखता है। विपक्षी पार्टियों के आरोपों को यह मान कर नजरअंदाज कर दिया जा सकता कि वे अपने दल से संबंधित आरोपियों के बचाव में ईडी को कठघरे में खड़ा करती हैं। मगर यह भी सच है कि कई मौके पर खुद अदालतों की ओर से ईडी की कार्यशैली पर अंगुली उठाई गई है।
सवाल है कि किसी कानून पर अमल को लेकर ईडी अगर ईमानदार है, तो बार-बार विपक्षी दलों से लेकर अदालतों तक की ओर से उसकी मंशा पर अंगुली क्यों उठ रही है। बुधवार को नौकरी के बदले जमीन के आरोपों से जुड़े एक मामले में राज एवेन्यू कोर्ट की एक विशेष अदालत ने ईडी को फटकार लगाई और उसकी प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि वह एक जांच एजंसी के रूप में कानून के नियमों से बंधी है और वैसे आम नागरिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं कर सकती, जो संदिग्ध तक नहीं हैं। जाहिर है, यह ईडी के कामकाज के तौर-तरीकों पर एक बार फिर गहरा सवालिया निशान है, जो उसकी साख को कसौटी पर रखता है अगर इससे शासन के काम का एक ढांचा तैयार होता है तो उसका लोकतंत्र और जनता के अधिकारों पर भी प्रभाव पड़ेगा। विडंबना यह है कि ईडी के रवैये की वजह से पिछले कुछ समय से इस संबंध में कई सवाल उठे हैं।
शायद इसी वजह से अदालत ने यह भी कहा कि इतिहास से कोई सबक सीखना है तो यह देखना चाहिए कि मजबूत नेता, कानून और एजेंसियां आमतौर पर उन्हीं नागरिकों को निशाना बनाती हैं, जिनकी रक्षा का वे संकल्प लेती हैं। इस टिप्पणी को जनता के अधिकार और राज्य के कर्तव्य के संदर्भ में देखा जा सकता है, जिसमें उम्मीद की जाती है कि लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं किया जाएगा। करीब एक वर्ष पहले सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी ईडी को यह सलाह दी गई थी कि वह अपनी कार्यशैली से भय का माहौल पैदा न करे। शीर्ष अदालत की टिप्पणी इस बात का इशारा थी कि एजंसी को राजनीतिक विरोधियों पर लगे आरोपों की जांच को लेकर संतुलित रुख अख्तियार करने की जरूरत है। आखिर ऐसी शिकायतों की नौबत क्यों आनी चाहिए कि किसी एजंसी के अधिकारियों के पेश आने का तरीका कई बार भयादोहन की तरह लगने लगता है। इस तरह के व्यवहार का एक स्वाभाविक नतीजा यह होता है कि वास्तविक कारण भी संदिग्ध लगने लगते हैं। ऐसे में ईडी के सामने यह विचार करने का वक्त है कि विपक्षी दलों से लेकर अदालतों तक के बीच उसकी कार्यशैली को लेकर जैसी राय बन रही है, वह उसकी साख को किस हद तक प्रभावित कर रही है और उसे अपने तौर-तरीके में क्या सुधार करने की जरूरत है!
कुंद हो गई हमारी सोच
अखिलेश आर्येन्दु
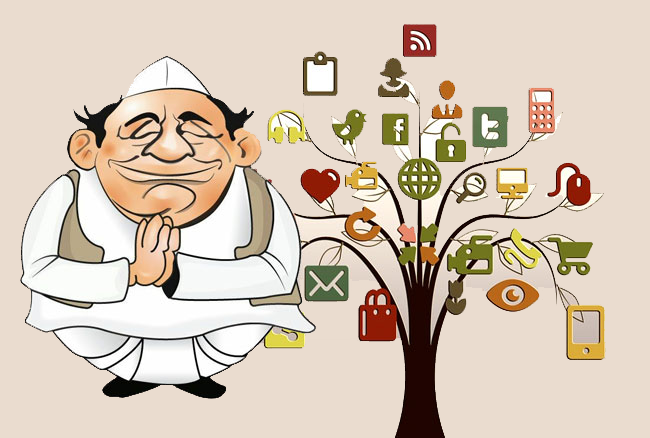
युवा वर्ग पर सोशल मीडिया का ज्यादा असर हो रहा है, इसलिए इस पर नियंत्रण की बात भी कही जा रही है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि सोशल मीडिया ने समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को भी अपनी बेबाक बात कहने, अपनी जरूरत की चीजों को जानने-समझने और किसी बात का समर्थन या विरोध करने का अवसर दिया है। आकड़ों के मुताबिक वर्तमान में भारत में 447 मिलियन से ज्यादा लोग सोशल मीडिया का उपयोग करने वाले हैं। इसका जहां समाज पर सकारात्मक असर पड़ा है वहीं नकारात्मक असर की वजह से तमाम तरह की समस्याएं, बीमारियां, तनाव, हिंसा और झगड़े-फसाद भी बढ़े हैं। सर्वाधिक नकारात्मक असर युवा वर्ग पर पड़ रहा है। समय की बर्बादी, नकारात्मक बर्ताव, नकारात्मक सोच, रूढ़ियों और गंदी प्रवृत्तियों को बढ़ावा लगातार बढ़ावा मिल रहा है। गुलामी किस तरह व्यक्ति के मन, मस्तिष्क, धन और सोच को बदली है। आधुनिक तकनीक का चमत्कारी यंत्र मोबाइल की गुलामी से समझा जा सकता है।
अपने और अपनों से दूरियां बढ़ाने में मोबाइल का असर इस कदर हुआ कि सामान्य व्यवहार, पढ़ने-पढ़ाने की आदत, सुनने-सुनाने का वक्त, सहजता जैसी जिंदगी की महत्त्वपूर्ण कवायदें भी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से गायब हो चुकी हैं। सोशल मीडिया सर्वेक्षण के आंकड़े बयां करते हैं कि पिछले दो दशक में सामाजिक सद्भावना में कमी आई है, अपसंस्कृति का लगातार विस्तार हुआ है, और मानव मूल्यों के प्रति लगाव कम हुआ है। पारिवारिक समरता, सामाजिक सदभावना और आपसी विश्वास में भी कमी आई है। यही वजह है परिवार टूट रहे हैं, रिश्तों का बाजारीकरण हुआ जिससे बड़े- बुजुर्गों के प्रति बर्ताव और सद्भाव में कमी आई हैं। आंकड़े बयां करते हैं कि 2018-19 में फेसबुक, ट्वीटर समेत कई साइटों पर 3,245 आपत्तिजनक सामग्रियां मिलने की शिकायत की गई थीं, जिनमें से 2,662 सामग्रियों को हटा दिया गया था। इन सामग्रियों में ज्यादातर वे थीं जो धार्मिक भावनाओं को भड़काने और राष्ट्रीय प्रतीकों के अपमान का निषेध करने वाले कानूनों का उल्लंघन कर रही थीं। तब से पिछले पांच वर्षों में हजारों और आपत्तिजनक सामग्रियां सोशल मीडिया की साइटों पर डाली गई, इसका प्रमाण है यूनेस्को की वह रिपोर्ट जो सोशल मीडिया के असर का बयां करती है।
सोशल मीडिया के जरिए किस तरह के अंधविश्वासों, पाखंडों, बुराइयों, नकारात्मक सोच को लगातार बढ़ावा मिल रहा है, इसकी जानकारी यूनेस्को की रिपोर्ट के जरिए देखी – समझी जा सकती है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) के रिपोर्ट के मुताबिक सोशल मीडिया से लैंगिक रूढ़ियां और दकियानूसी सोच को लगातार बढ़ावा मिल रहा है। खासकर लड़कियों की मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण पर नकारात्मक असर हो रहा है। ‘प्रौद्योगिकी अपनी शर्तों पर’ नाम की रिपोर्ट यूनेस्को ने 25 अप्रैल को जारी की है। इतने बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया पर जो सामग्री परोसी जाती है, वह मल्टीमीडिया के जरिए उपलब्ध कराई जाती है। लेकिन इससे यौन सामग्री से लेकर ऐसे वीडियो की जद में आने का खतरा है, जिनमें अनुचित बर्ताव या शारीरिक सुंदरता के अवास्तविक मानकों का महिमामंडन किया गया हो। इससे लड़कियों के लिए मानसिक तनाव बढ़ सकता है, उनके सम्मान को ठेस पहुंच सकती है। सोशल मीडिया पर जिस तरह लड़कियों के लिए नकारात्मक दिकयानूसी छवियों को गढ़ा जाता वह उन्हें विज्ञान, टैक्नॉलजी, अभियंत्रिकी और गणित विषयों में पढ़ाई से दूर ले जा सकती है। तस्वीर आधारित यौन सामग्री, एआई से तैयार झूठी तस्वीरों व वीडियो (डीपफेक) के ऑनलाइन और कक्षाओं में शेयर किए जाने से हालात और जटिल हो रहे हैं।
रिपोर्ट में इसके बचाव पर जोर देते हुए बताया गया है कि शिक्षा में और ज्यादा निवेश किया जाना चाहिए। खासतौर पर मीडिया और सूचना साक्षरता पर डिजिटल प्लेटफार्म, यूनेस्को के शिक्षानिर्देशों के अनुरूप स्मार्ट ढंग से इनका नियमन भी किया जाना चाहिए। आम आदमी सोशल मीडिया का उपयोग बड़े पैमाने पर करके खुद को संतुष्टि पा रहा है परंतु हकीकत महज इतनी ही नहीं है। कहने को तो रेलवे – टिकटिंग, लाइफ इंश्योरेंस, ई-कॉमर्स, ई-टिकटिंग और ई-गवर्नेस जैसी सुलभता सोशल मीडिया का उपहार हैं, लेकिन दूसरी तरफ अश्लीलता, हिंसा, ठगी, क्रूरता और भ्रष्टाचार के नये चेहरे भी आए। इससे नई पीढ़ी को बहुत संकुचित और स्वार्थी बना दिया है। यदि हम जीवन, परिवार और समाज की बेहतरी के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करें तो अनेक लाभ घर बैठे भी हो सकते हैं। सोशल मीडिया के अधिक इस्तेमाल के कारण सोशल एंग्जाइटी जैसी समस्या से युवा ग्रस्त हो रहा है।
लड़कियों के शारीरिक और मानसिक क्षमता पर बुरा असर सोशल मीडिया के अधिक इस्तेमाल के कारण देखा जा रहा है। धन, समय, सहजता, चिंतन और चिंता की समस्या सोशल मीडिया ने कृत्रिम ढंग से पैदा की है। अभिभावकों के लिए यह नई समस्या है। आतंकवाद, सांप्रदायिकता, नफरत, हिंसा, नई बीमारियों के चपेट में आने का डर, मांसाहार, शराबखोरी, धुम्रपान और अन्य अनेक समस्याएं सोशल मीडिया के कारण तेजी से बढ़ी हैं। इसलिए सोशल मीडिया के अच्छे-बुरे इस्तेमाल पर जरूर गौर करना चाहिए वरना इससे जीवन का बड़ा हिस्सा सोशल मीडिया के नाम होने का खतरा मडराता रहेगा और जिंदगी जीने का मायने ही कहीं सोशल मीडिया के नाम न हो जाएं। मानव मूल्यों के ख़त्म होने और इंसान का वस्तु या यंत्र के रूप में तब्दील होने का खतरा आसन्न दिखाई दे रहा है। एक संतुलित जीवन, परिवार, समाज, संस्कृति और देश के लिए सोशल मीडिया के दोनों पक्षों पर हमें खुले मन से विचार करना चाहिए। यदि कानून बनाना पड़े तो भी कानून बना कर गिरते जीवन मूल्यों को रोकने की कोशिश भी करनी होगी।
विकास बनाम न्याय का सियासी विमर्श
बद्री नारायण, निदेशक, जीबी पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान
किसी भी जनतंत्र में चुनाव मात्र जीत-हार, सरकार बनाने-गिराने का माध्यम नहीं होते हैं, ये वस्तुत: राजनीतिक चेतना को प्रेरित करने का माध्यम होते हैं। चुनाव समाज में संवाद, विकास एवं राष्ट्र निर्माण के विमर्शों को प्रेरित करने का माध्यम होते हैं। चुनाव के दिनों में ये बहसें मूलत: राजनीतिक दलों द्वारा जारी किए गए घोषणापत्रों, रैलियों में नेताओं के दिए गए भाषणों और बयानों से बनती-बिगड़ती हैं।
वैसे तो मेरा मानना है कि यह चुनाव ‘छवियों के टकराव’ का चुनाव है, जिसमें इस चुनाव के दौरान नेताओं द्वारा कही गई बातों से ज्यादा एक लंबे काल खंड में बनी-बिगड़ी उनकी छवियों का असर है। इस चुनाव में कथनी से ज्यादा ‘करनी’ की स्मृतियों एवं प्रभाव में जनता वोट डाल रही है। चुनाव में कुछ बहसें दीर्घकालिक परिवर्तन की दृष्टि से होती हैं, तो कुछ बहसें तात्कालिक लोकप्रिय प्रकृति की होती हैं। इस चुनाव में ऐसी कौन-सी बहसें हैं, जो तात्कालिक राजनीतिक लाभ या लोकप्रियता पाने की रणनीति से प्रेरित हैं। इन तमाम मुद्दों पर विचार इस चुनाव के संदर्भ में ही नहीं, वरन पूरे लोकतंत्र के विस्तार एवं उसे गहरा बनाने के लिए भी जरूरी है।
इस चुनाव में दो प्रकार की बहसें हो रही हैं। एक तरफ, भाजपा देश को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को विमर्श का विषय बना रही है। वह भारतीय समाज में राज्य द्वारा संसाधनों के वितरण के लिए गरीब, युवा, नारी एवं किसान, चार आर्थिक वर्गों को केंद्र में रखकर योजनाओं को प्रचारित कर रही है।
दूसरी तरफ, कांग्रेस अपने घोषणापत्र में अन्य वादों के साथ समाज कल्याण कार्यक्रमों को आरक्षण आधारित जाति केंद्रित सामाजिक न्याय की अवधारणा के साथ मिलाकर लोकप्रिय वादे के रूप में प्रचारित कर रही है। इसके लिए वह पूरे देश में जातीय जनगणना कराने को भी एक लोकप्रियतावादी नारे के रूप में अपने चुनावी विमर्श में इस्तेमाल कर रही है।
अगर इस चुनाव की बहसों के निर्माण की प्रक्रिया को देखें, तो साफ लगता है कि भाजपा इस चुनाव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि, सामाजिक कल्याण के कार्यक्रमों पर केंद्रित एवं विकसित भारत की संकल्पना के ईद-गिर्द रखना चाहती है। इस चुनाव में टिकट बंटवारे में परोक्ष जातीय जोड़-घटाव को छोड़ दें, तो उसने अपने घोषणापत्र एवं अपने नेताओं के भाषणों में जातीय अस्मिता की राजनीति से दूरी बनाने की कोशिश की है। वहीं कांग्रेस ने अपने चुनावी विमर्श में शुरू से ही भारतीय समाज में जाति आधारित सामाजिक अन्याय को मुद्दा बनाते हुए पारंपरिक ढंग के आरक्षण आधारित सामाजिक न्याय को लोकप्रिय बहस बनाने की कोशिश की है। इस बार अल्पसंख्यकों के संदर्भ में धार्मिक अस्मिता एवं सामाजिक न्याय के संदर्भ में जातीय अस्मिता कांग्रेस के घोषणापत्र के केंद्रीय तत्व बने हुए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इन जातीय एवं धार्मिक अस्मिताओं को न्याय-अन्याय जैसी शब्दावली में बार-बार उठाया है। कांग्रेस ने भाजपा के शासन में आने पर ‘संविधान बदल दिया जाएगा’, ‘चुनाव नहीं होंगे’ आदि अनेक भय व चिंता जगाने वाले विमर्श खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस के चुनावी विमर्श की इसी रणनीति ने भाजपा को अपने चुनावी विमर्श की रणनीति में परिवर्तन के लिए बाध्य किया। कांग्रेस के इन पारंपरिक राजनीतिक अस्त्रों का जबाब देने के लिए भाजपा ने अपने विकास, भारत गर्व एवं विकसित भारत के विमर्श के साथ ही कांग्रेस पर तुष्टिकरण की राजनीति करने का पारंपरिक अस्त्र चला दिया।
इसी तुष्टिकरण के विमर्श में जाति के साथ ही धार्मिक अस्मिता का विमर्श भी सामने आने लगा। भाजपा ने सक्षमता से इसी तुष्टिकरण के विमर्श को सामाजिक न्याय के विमर्श से जोड़ दिया। यह प्रचार शुरू कर दिया कि कांग्रेस एक धर्म के लोगों को संतुष्ट करने के लिए पिछड़ों, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के गरीबों का हक छीनकर एक खास धार्मिक समुदाय में बांट देना चाहती है। साथ ही, उसने कांगे्रस द्वारा स्वर्ण एवं संपत्ति के सर्वे की मंशा को भारतीय स्त्रियों, विशेषकर मध्यवर्गीय स्त्रियों के ‘मंगल सूत्र’ पर खतरे के वृतांत में पीरो दिया। भारतीय चुनावों में वृतांतों या ‘नैरेटिव्स’ की राजनीति में प्रधानमंत्री मोदी का यह मास्टर स्ट्रोक माना जाना चाहिए, जिसमें उन्होंने मध्यवर्गीय मानस को तो झकझोरा ही, गरीबों, पिछड़ों एवं दलितों की अस्मिताओं को भी पारंपरिक जाति आधारित सामाजिक न्याय की राजनीति के खांचे से बाहर निकाल हिंदुत्व, सामाजिक न्याय एवं विकास की आकांक्षा का संतुलित मिश्रण तैयार किया। राजनीति में यह ऐसा मारक आक्रमण है, जिसका सामना कांग्रेस के विमर्शकार कैसे कर पाते हैं, यह देखना होगा।
यह बार-बार देखने में आता है कि जाति कई बार सामाजिक न्याय के वितरण की एक इकाई के रूप में मददगार तो होती है, किंतु आगे चलकर अनेक प्रकार के सामाजिक अन्याय को जन्म भी देती है। कांगेस को यह समझना होगा कि जाति से जाति को काटना भारतीय समाज में अत्यंत मुश्किल है। हमने देखा है कि ऐसे अनेक प्रयोग अब तक विफल ही हुए हैं। आजादी के बाद सामाजिक न्याय की राजनीति के एक अनोखे प्रयोगकर्ता कांशीराम शुरुआती सफलताओं के बाद अंतत: कमजोर पड़ते देखे गए। समझना होगा कि भारतीय समाज में जाति की धार को आर्थिक विकास की प्रक्रियाओं से ही कुंद किया जा सकता है।
अगर गहराई से विवेचना करें, तो भारतीय जनतांत्रिक राजनीति को एक नई भाषा की जरूरत है, एक आधुनिक भाव बोध की भी। इसे एक नई राजनीति भी चाहिए। विकास की राजनीति की भाषा को अन्य प्रकार की राजनीति केंद्रित भाषा की तुलना में ज्यादा अधुनातन, अग्रगामी एवं प्रगतिशील तो माना ही जाता है। जैसे ही इस भाषा को हम जाति एवं धर्म आधारित राजनीतिक भाषा की सीमा में जाने के लिए मजबूर करते हैं, वैसे ही हम तीन-चार दशक पीछे की राजनीतिक परिदृश्य में पहुंच जाते हैं।
हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यासकार फणिश्वर नाथ रेणु ने अपनी कहानी पंचलाइट (पंचलैट) में एक गांव में एक ऐसे जाति विभाजित समाज का वर्णन किया है, जहां हर जाति को अपना गोल बैठता है एवं उनकी अपनी ‘पंचलाइट’ (पेट्रोमैक्स) होने की चाह होती है। वह अगर आज जीवित होते, तो स्वयं भी चाहते कि भारतीय जनतंत्र के पास एक विकासमान एवं नए भारत की अंतर्दृष्टि एवं राजनीतिक भाषा हो, जो अन्य अनेक पारंपरिक अस्मिताओं पर केंद्रित राजनीतिक भाषा एवं विमर्शों का चोला उतार फेंके।