
28-10-2024 (Important News Clippings)
To Download Click Here.
Repair, Reuse, Recycle, Reduce
Tech cos will resist 4Rs, regulators mustn’t waver
ET Editorials
Right to repair legislation that seeks to elongate the lifespan of consumer electronics and electrical appliances is emerging in several jurisdictions against resistance by producers such as Apple. The repair movement must become more broad-based for it to make deeper contributions to consumer protection and sustainability. By insisting that manufacturers of smartphones and washing machines make available parts, services and training to stretch their usable life by up to a decade, lawmakers are right in their intention to promote the circular economy. The big hurdle is the manufacturing stage, which contributes the most to resource extraction and emissions.
Their interventions, however, may be falling short. Efforts to make spares and third-party repairs widely available do not go deep enough into manufacturing processes that are designed to encourage obsolescence. Production systems that pair hardware with software identifiers are still beyond the reach of right to repair legislation. The rules are also less ambitious about the pricing of parts and repairs, which are key to aligning the production process with their goals. So long as it is cheaper to manufacture a new device than to repair an existing one, consumer choice and manufacturing will favour shorter product lifespans. Product design must be nudged into becoming modular, with more swappable parts, such as batteries, so that the ecosystem tilts towards sustainable manufacturing.
This is the big challenge that pits consumer choice against innovation. Yet, inroads are being made to address the tech dominance that creates manufacturing monopolies. Standardisation, such as ports for charging smartphones, is making headway. But it falls short in tackling the vast majority of product innovations that have become part of the standard feature set of most consumer electronic devices due to their shortened life cycles. Lawmakers tend to become cautious when sustainability comes up against innovation. This moderates the tempo of the right to repair movement. It is still a useful device to keep manufacturers from pushing the obsolescence envelope too far.
Date: 28-10-24
Gotta Plug the Green Skills Gap
ET Editorials
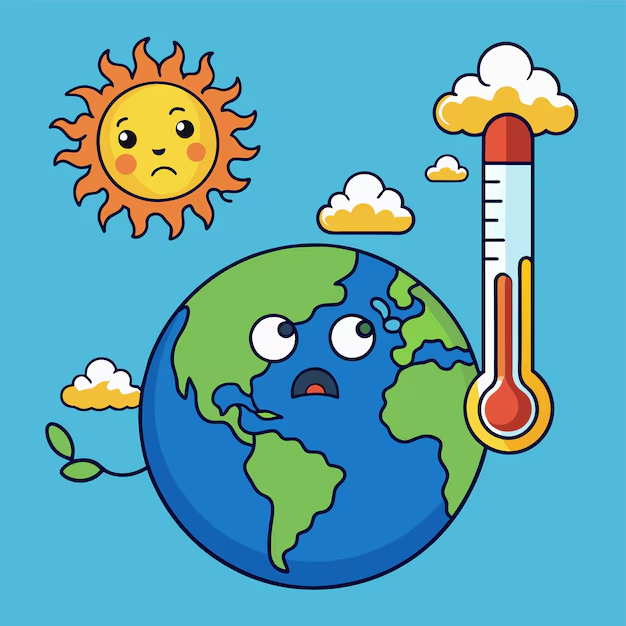
India stands at crossroads in its green transition, with the potential to become a global leader in RE. However, it, too, is facing a severe shortage of green workforce. Team Lease Degree Apprenticeship data shows that while the RE sector is estimated to create 1.7 mn jobs, the skill gap in this sector is a whopping 1.2 mn. The same holds in other areas, such as the building sector, where there is shortage of trained manpower across levels—including architects to design sustainable, thermally comfortable homes that use fewer resources and consume less energy.
India urgently needs to fill this skills gap, requiring a stronger foundation in STEM education where its performance is below par. Part of this green workforce gap is due to limited awareness. Training new workers and reskilling the existing workforce are crucial to building a robust green pipeline. However, this effort cannot be limited to urban areas or men. To create an inclusive green economy, central and state governments must actively open up more technical roles for women, ensuring that opportunities are both widespread and equitable.
The private sector holds the key to India’s e-bus push
If there is to be scale in the electric bus market in India, private sector participation is critical
Bhaumik Gowande & Sumati Kohli, [ Bhaumik Gowande is Associate Researcher at the International Council on Clean Transportation (ICCT) in India. Sumati Kohli is Researcher at the International Council on Clean Transportation (ICCT) in India ]

Public sector driven despite fleet size
Electric bus deployment in India has thus far been driven by the public sector, which was supported with financial subsidies under the national Faster Adoption and Manufacturing of (Hybrid and) Electric Vehicles in India (FAME India) scheme. Under FAME I, from 2015-19, 425 buses received approval for purchase subsidies, which rose to 7,120 buses under FAME II, which ran from 2019-24. The incentives were available to State and city transport undertakings, municipal corporations, and other public entities. But public transport buses make up only 7% of the 24 lakh registered buses in India.
Indeed, despite private buses representing 93% of the buses in India, they are not yet included in any major national schemes or special incentive programmes. While a few leading private bus operators such as NueGo and Chartered Speed have electric buses in their fleets, the numbers remain small. If there is to be scale in the electric bus market in India, the transition of private buses is critical, and there are several areas where policy can help.
A recent International Council on Clean Transportation (ICCT) study suggested that the limited availability of financing is a key hurdle for the uptake of electric buses by the private sector. Higher perceived risk-return profiles, high upfront costs, and low perceived resale value of electric buses as collateral have made financing a challenge. Uncertainty regarding battery life increases this perceived risk.
The hurdles
Studies show that electric inter-city buses can be more profitable than diesel buses over their service life. However, high interest and loan instalment costs make them less financially viable during the loan period. Despite this, private intercity bus operators in India could benefit greatly from electric buses, as they would offset rising fuel costs. Intercity buses play a major role in India’s transport, with 22.8 crore passengers daily, covering 57% of total ridership and 64% of vehicle-kilometres. Additionally, 40% of intercity trips fall within the 250 kilometre to 300 km range that current electric bus models can cover on a single charge. These operations are well suited for electric bus deployment.
As India aims to replace 8,00,000 diesel buses with electric ones by 2030, this ICCT report has highlighted the potential of offering favourable financing options such as interest subsidies and longer loan tenures to ease the financial burden. Additionally, credit guarantees, potentially rolled out through government banks and other designated financial institutions, are a way to help reduce investment risks for financiers.
Another key hurdle for private electric bus adoption is charging infrastructure. FAME-funded facilities are limited to the depots of State transport units, and as 90% of private bus operators in India manage fleets of fewer than five buses, the high land and infrastructure costs can make investing in charging facilities economically impractical. Even if the required space of 70 square metres to 120 sq.m. is available, the high cost of land lease rental could severely impact the economic viability of charging stations. Private intercity bus operators may also face challenges due to power supply interruptions, limited grid capacity, and inadequate upstream infrastructure. To accelerate private-sector electric bus adoption, it is essential to develop shared public charging infrastructure within cities and on high-traffic highways, particularly key intercity corridors. State governments could lead the development by leveraging financial subsidies offered under the PM E-Drive scheme, which aims to subsidise 1,800 bus chargers. To encourage private investment, States could also offer additional fiscal incentives or structure tenders for shared charging infrastructure on a design-build-operate-transfer (DBOT) basis, and ensure viability through guarantees of minimum daily energy consumption per charger.
A business model worth following
Another emerging business model, Battery-as-a-Service (BaaS), could reduce the high upfront costs of electric buses by separating battery ownership from vehicle ownership, as seen in China and Kenya. This model, along with battery swapping, has the potential to accelerate private electric bus adoption through usage-linked leasing and other solutions, such as Macquarie’s Vertelo platform in India. An ICCT blog discussed these in detail and highlighted how they could help transform electric bus deployment in India.
To create scale and reduce costs in the electric bus market in India, promoting uptake in the private sector is crucial. As the government forges ahead in supporting the EV transition under the new PM E-DRIVE scheme, there are opportunities for policy in the areas of financing incentives, charging infrastructure, and innovative business models to help overcome barriers to electric bus adoption by private operators.
 Date: 28-10-24
Date: 28-10-24
जमीन के समुचित इस्तेमाल का सवाल
मिहिर एस शर्मा
डेविड रिकार्डो के निधन को दो सदी, एक वर्ष, एक माह और एक सप्ताह से कुछ अधिक समय बीता है। रिकार्डो में कई खूबियां थीं: वह फाइनैंसर थे, उन्मूलनवादी थे और उदारवादी राजनेता थे। बहरहाल उन्हें आधुनिक अर्थशास्त्र के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। उन्होंने कई जरूरी आर्थिक सिद्धांत तैयार किए जिनमें घटते सीमांत प्रतिफल से लेकर व्यापार में तुलनात्मक लाभ, धन जुटाने के विभिन्न तरीकों के बीच कार्यात्मक समानता शामिल है।
परंतु अगर आज मुझे रिकार्डियन सिद्धांतों को सामने रखना हो तो वह कुछ ऐसा होगा: जब संपत्ति बढ़ती है तो पैसे खर्च होते हैं या जब तकनीक में सुधार होता है तो उसके लाभ उन लोगों तक जाते हैं जो संसाधनों पर नियंत्रण रखते हैं या उन तक जो ऐसे संसाधन की तकदीर तय करते हैं, जिसकी जगह कोई नहीं ले सकता और वह है जमीन। रेंट का रिकार्डियन सिद्धांत क्रांतिकारी सिद्धांत था जिसमें उन्होंने दिखाया कि खेती को अधिक उत्पादक बनाने वाले सिद्धांत जमीन मालिकों के लिए लाभदायक होते हैं भाड़े पर खेती करने वालों के लिए नहीं। रिकार्डो रीजेंसी वाले जमाने की ब्रिटिश राजनीतिक अर्थव्यवस्था में भू-नीति की केंद्रीय भूमिका को समझ गए थे क्योंकि उस समय की अर्थव्यवस्था, समाज और राजनीति तीनों पर भू-स्वामियों का दबदबा था। जब उन्होंने वाटरलू के युद्ध पर सट्टा लगाकर करोड़ों रुपये कमाए तो फौरन वह ग्लोसेस्टरशर चले गए और खुद को देहाती जमींदार बताते हुए संसद पहुंच गए। अज राष्ट्रीय और वैश्विक अर्थव्यवस्थाएं 200 साल पहले की तुलना में अधिक जटिल हैं। परंतु जमीन, जमीन सुधार, उसका उपयोग और मूल्य आदि 21वीं सदी के विकास और वृद्धि के केंद्र में हैं। यह कुछ इस कदर है कि अर्थशास्त्र का अनुशासन आज इन्हें उस तरह नहीं परिभाषित कर सकता जैसे रिकार्डो के दौर में किया था।
जब जमीन के मूल्य पर एकाधिकार होता है और वह साझा नहीं की जाती तो अर्थव्यवस्थाओं में गतिहीनता आ जाती है। जब जमीन की उत्पादकता में सुधार नहीं होने दिया जाता है तब आर्थिक वृद्धि में गिरावट आती है। जब जमीन के स्वामित्व से समझौता किया जाता है तो राजनीतिक जोखिम पूरी अर्थव्यवस्था को घेर लेते हैं। यकीनन जमीन का स्वामित्व, नियंत्रण और प्रबंधन शक्तिशाली राज्यों की तकदीर आज भी उसी तरह तय करते हैं जैसे रिकार्डो के समय के भूस्वामी ब्रिटिश संसद में करते थे। आज यह लगभग सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की चिंता का विषय है: अमेरिका, चीन, यूनाइटेड किंगडम और यहां तक कि भारत भी।
चीन सबसे स्पष्ट उदाहरण है। वहां का मॉडल कुछ ऐसा रहा: स्थानीय सरकारें लैंड बैंक बना सकती थीं और जमीन के भविष्य के मूल्य के बरअक्स ऋण ले सकती थीं। वे इस पूंजी का इस्तेमाल भूमि में सुधार करने में करतीं और मूल्यवर्धन का बड़ा हिस्सा पूंजी के स्वामियों के इर्दगिर्द होता। भविष्य में इसे और सुधारों में इस्तेमाल किया जाता। इस प्रक्रिया के माध्यम से पूरे देश में अधोसंरचना विकास किया गया और कई क्षेत्रों को उत्पादक बनाने में मदद मिली।
दिक्कत यह है कि कर्ज भी बढ़ा। ऋण संकट वास्तव में स्वामित्व का संकट है। जमीन और उसके मूल्य पर किसका नियंत्रण है? स्थानीय सरकार का? उन रियल एस्टेट कंपनियों का जिन्होंने स्थानीय सरकार की उस जमीन पर निर्माण करने की मांग पर प्रतिक्रिया दी? इमारत बनाने के लिए पूंजी मुहैया कराने वाले का? या केंद्र सरकार का क्योंकि चीन में अंतत: सारी शक्ति सत्ता के शीर्ष से आती है?
जमीन की कीमतें बढ़ा-चढ़ाकर पेश किए जाने के कारण अचल संपत्ति बाजार और उससे संबद्ध बाजार चीन की अर्थव्यवस्था में अन्य देशों की तुलना में बहुत बड़े हिस्सेदार हो गए। वहां सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में वे 24-30 फीसदी के हिस्सेदार हैं जबकि अन्य जगहों पर यह 15-20 फीसदी है। इसमें कमी आएगी। यानी कुछ लोगों को नुकसान होगा। अब तक सरकार की ओर से ठोस हस्तक्षेप न होने के कारण जमीन की कीमत में अनिश्चितता है और अर्थव्यवस्था जूझ रही है।
अमेरिका में राजनीतिक और आर्थिक पुनर्संतुलन को भू-नीति के अलग-अलग दृष्टिकोण आकार दे रहे हैं। रिपब्लिकन झुकाव वाले कई राज्यों में समृद्धि केवल इसलिए बढ़ रही है क्योंकि वे भूमि विकास के लिए ऐसी नीति बना रहे हैं जो उन्हें अधिक उत्पादक बना रही है और आंतरिक प्रवासन की वजह बन रही है। फ्लोरिडा और टेक्सस को लाभ हो रहा है मगर डेमोक्रेटिक कैलिफोर्निया और न्यूयॉर्क को नहीं। भविष्य में जब प्रतिनिधि सभा में सीटों का नए सिरे से निर्धारण होगा और बढ़ती आबादी के अनुसार इलेक्टोरल कॉलेज का पुनरावंटन होगा तो रिपब्लिकन प्रभाव वाले राज्यों की राजनीतिक शक्ति बढ़ेगी। चीन के उलट अमेरिका में संपत्ति पर मजबूत अधिकार हैं। जमीन का स्वामित्व सुरक्षित है। परंतु भू-बाजार बहुत सख्त और कठोर हैं। उदाहरण के लिए संपत्ति ऋण की दर दशकों से स्थिर है।
इसका अर्थ यह है कि जिन लोगों ने कम कीमत रहते जमीन खरीदी उन्हें बाद में किराये पर रहने वालों और अचल संपत्ति विकसित करने वालों की तुलना में भारी लाभ हुआ। इस बीच जिन लोगों ने कमजोर जगहों पर घर खरीदा वे उन्हें बेचकर आसानी से उन जगहों पर नहीं जा सकते जहां उनकी नौकरियां हैं। ऐसी बिक्री न होने का अर्थ है कि आवास और श्रम बाजार दोनों ‘जड़वत’ हैं।
यूनाइटेड किंगडम इस बात का उदारहण है कि जड़वत भूमि बाजार किसी समाज का क्या कर सकता है। विगत 40 सालों में उसके लगभग सभी आर्थिक लाभ पूरी तरह भू-स्वामियों को हुए हैं। खासतौर पर ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि भूमि सुधार, अधोसंरचना विकास और नए कार्यालय बनाने या घर बनाने का लेकर पुरातन प्रतिबंधों की स्थिति किसी अन्य विकसित अअर्थव्यवस्था से बुरी है। रिकार्डियन नजरिये से देखा जाए तो अगर आपके बाजार बेहद लचीले हैं और अन्य तमाम संसाधन आपके पास हैं लेकिन श्रम के मामले में लचीलापन या उपलब्धता दोनों नहीं हैं तो तमाम लाभ भूस्वामी को होते हैं।
भारत में सुधारों से जुड़ा हालिया संघर्ष देखें तो उसके मूल में भी जमीन है। भारत का श्रम बाजार भी लचीला नहीं है। वास्तव में हमारे यहां श्रम बाजार जैसा कुछ है ही नहीं। जमीन का उपयोग नौकरशाही के आदेश से तय होता है और स्वामित्व का कोई सुरक्षित रिकॉर्ड नहीं है। परंतु चीन के उलट स्थानीय सरकारों को भी भूमि बैंक बनाने के लिए या इसके बरअक्स कर्ज लेने के लिए संघर्ष करना होगा। यहां अगर कोई भूमि से लाभान्वित होता है तो वह है ऐसा बिचौलिया जो राजनेताओं और नौकरशाहों से संबंधित होता है जो जमीन के उपयोग को बदलने का प्रभाव रखते हैं। नतीजा यह है कि न तो निजी और न ही सरकारी क्षेत्र आसानी से जमीन पर निर्माण कर सकता है न बदल सकता है। कृषि में मार्जिन कम है और उद्योग में ज्यादातर निवेश कम है। इसके लिए भूमि स्वामित्व पर प्रतिबंध जिम्मेदार है।
रिकार्डो जिन सवालों को हल करना चाहते थे, उनसे ये सारे मुद्दे दूर नजर आते हैं लेकिन ये दिखाते हैं कि आर्थिक विकास के मूल में एक सवाल का जवाब है: हमें जमीन के साथ क्या करना चाहिए?
सहयोग के आयाम
संपादकीय
मौजूदा विश्व में जिस तेजी से अलग-अलग देशों और खेमों में पुराने समीकरण नई शक्ल ले रहे हैं, संबंधों के आयाम बदल रहे हैं, उसमें भारत और जर्मनी के बीच बहुस्तरीय सहयोग के नए तैयार होते रास्ते बेहद अहम हैं। जर्मनी और भारत के सातवें अंतर-सरकारी परामर्श यानी आइजीसी के आयोजन के दौरान दोनों देशों के बीच संबंधों का जो नया अध्याय खुला है, उससे काफी उम्मीदें लगाई जा रही हैं। यह सही है कि आर्थिक और सामरिक स्तर पर विश्व में कई स्तर पर खींचतान, तनाव और टकराव का माहौल चल रहा है और ऐसे में खासतौर पर भारत जैसे किसी देश के लिए सहयोग के मोर्चे तैयार करना एक कठिन चुनौती है। मगर इसी दौर में यह भी साबित हुआ है कि कुछ युद्धों और अन्य कारणों से दुनिया के ज्यादातर देश अपनी सुविधा के ध्रुवों में बंट रहे हैं, उसमें भारत अलग-अलग देशों के साथ अपने संबंधों को व्यावहारिकता और जरूरत की कसौटी पर तय कर रहा है।
गौरतलब है कि जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज के साथ भारतीय प्रधानमंत्री की बातचीत के बाद दोनों देशों के बीच कई मोर्चों पर सहयोग की घोषणा की गई। इसमें कई संधियों पर हस्ताक्षर किए जाने के साथ-साथ द्विपक्षीय रिश्तों को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता पर भी जोर दिया गया। भारत में बेरोजगारी की समस्या आम है तो जर्मनी में कुशल कामगारों की कमी है। इस लिहाज से देखें तो द्विपक्षीय बातचीत में जर्मनी में भारत के कुशल कामगारों की बढ़ती मांग और यहां के प्रशिक्षित श्रमिकों के लिए वार्षिक वीजा की संख्या बीस हजार से बढ़ा कर नब्बे हजार करने पर बनी सहमति काफी मायने रखती है। व्यापार और सामरिक साझेदारी के मोर्चे पर महत्त्वपूर्ण बातचीत के अलावा तकनीक, कौशल विकास, कृत्रिम बुद्धिमता, सेमीकंडक्टर, स्वच्छ ऊर्जा से लेकर खुफिया जानकारी साझा करने जैसे कई मुद्दों पर सहयोग की घोषणा से स्पष्ट है कि कुछ मसलों पर मतभिन्नता के बावजूद जर्मनी और भारत एक नए रास्ते की ओर बढ़ रहे हैं। हालांकि यह देखना होगा कि मुक्त व्यापार पर विश्व व्यापार संगठन की व्यवस्था को मानने के मसले पर किस हद तक सहमति बन पाती है।
ताजा बैठक में रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध में भारत की भूमिका का भी जिक्र हुआ, लेकिन ऐसा लगता है कि इस मामले में भारत ने बहुत सधे कदमों के साथ जिस तरह एक संतुलित रुख अख्तियार किया है, उसे दूसरे देश भी समझ रहे हैं। मसलन, रूस और यूक्रेन युद्ध में भारत और जर्मनी की राय अलग-अलग है। एक ओर, जर्मनी खुल कर रूस के रुख को अंतरराष्ट्रीय चिंता का कारण बताता है, वहीं भारत साफतौर पर युद्ध की निरर्थकता को रेखांकित करता है कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। हालांकि वैश्विक परिदृश्य में जर्मनी के सामने अपने पक्ष को लेकर जिस तरह की चुनौतियां हैं, उसमें भारत से भी उसे अपना साथ देने की उम्मीद होगी। मगर भारत का अपना पक्ष है और जर्मनी शायद इसे समझता है। यही वजह है कि कई क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के लिए जो भी बातचीत हुई, उस पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। फिलहाल वैश्विक स्तर पर भू-राजनीति के जैसे दांव-पेच चल रहे हैं, उसमें स्वाभाविक ही भारत के लिए थोड़ी संवेदनशील स्थिति है। मगर इस मामले में भारत ने जिस तरह सावधानी के साथ फूंक-फूंक कर अपने कदम बढ़ाए हैं, उसमें जर्मनी के साथ सहयोग का नया अध्याय भी इसका एक ठोस उदाहरण है।
शिक्षा खर्च के मामले में विश्व स्तर पर खरा उतरा भारत
हरिवंश चतुर्वेदी, ( महानिदेशक, आईआईएलएमबी स्कूल )
संयुक्त राष्ट्र की विश्व स्तर पर शिक्षा से जुड़े मामलों के लिए नीति निर्धारित करने वाली संस्था यूनेस्को का कहना है कि साल 2015 से 2024 के बीच भारत ने अपनी जीडीपी का 4.1 से 4.6 प्रतिशत शिक्षा पर खर्च किया । यह तथ्य यूनेस्को द्वारा जारी ‘शिक्षा 2030 के लिए आवश्यक कदम’ निर्देशिका में उभरकर सामने आया है। इसके अनुसार, दुनिया के हर देश को शिक्षा पर जीडीपी का चार से छह प्रतिशत खर्च करना चाहिए। यूनेस्को द्वारा जारी आंकड़ों का यह भी कहना है कि भारत में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा साल 2015 से 2024 की अवधि में कुल सरकारी व्यय का 13.5 प्रतिशत से 17.2 फीसदी तक शिक्षा पर खर्च किया गया। ये आंकड़े यूनेस्को की उस अपेक्षा के अनुरूप हैं, जो संसार की सभी सरकारों से यह मांग करती है कि वे सरकारी बजट का कम से कम पंद्रह से बीस प्रतिशत शिक्षा पर खर्च करें।
यूनेस्को के आंकड़े इसलिए महत्वपूर्ण हैं कि विश्व स्तर पर स्वीकृत सतत विकास लक्ष्य 2030 के अनुसार कुल 17 लक्ष्यों को पूरा किया जाना है, जिसमें चौथा लक्ष्य है, ‘सबको गुणवत्ता वाली समावेशी व समतामूलक शिक्षा प्रदान करना।’ 2030 तक ये 17 लक्ष्य विश्व स्तर पर हासिल हो पाएंगे, वह कहना मुश्किल है, पर दुनिया की हर सरकार को इस दिशा में ठोस प्रगति दिखाने को कहा गया है। यूनेस्को के अनुसार, पिछले कुछ वर्षों में, खासकर कोविड के बाद दुनिया भर की सरकारों का शिक्षा पर खर्च कम होता दिखा है, किंतु भारत में यह लगभग स्थिर देखा गया है। साल 2010 के बाद से मध्य व दक्षिण एशिया के देशों में शिक्षा पर विनियोग और खर्च बढ़ता हुआ पाया गया है। कुछ बहुत छोटे देशों का खर्च प्रतिशत ज्यादा हो सकता है, किंतु उनके कुल खर्चे भारत के कुल प्रावधान की तुलना में बहुत कम हैं। यूनेस्को का कहना है कि समूचे एशिया में भारत द्वारा शिक्षा पर किया जा रहा खर्च जापान और चीन से ज्यादा रहा है।
मगर क्या भारत कोठारी आयोग (1964-66) की उस सिफारिश को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ पाया है, जिसमें जीडीपी का छह प्रतिशत शिक्षा पर खर्च करने की बात की गई थी ? राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2020 ने भी 1968 में स्वीकृत शिक्षा पर जीडीपी का छह प्रतिशत खर्च करने के लक्ष्य को सम्मान दिया है। इसका कहना है कि ‘यह नीति शिक्षा पर विनियोग बढ़ाने के लक्ष्य से प्रतिबद्ध है, क्योंकि कोई अन्य विनियोग या खर्चे का प्रावधान हमारी युवा पीढ़ी को गुणवत्ता वाली शिक्षा देने पर होने वाले खर्चे से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है।’
शिक्षा पर हम कितना खर्च करते हैं, इस पर अर्थशास्त्रियों और शिक्षाविदों के बीच कोई एकराय नहीं बन पाई है। इसका एक कारण यह है कि हमारे देश में शिक्षा पर सरकारी और निजी खर्चे के आंकड़े अलग- अलग होते हैं। सरकारी खर्चों की गणना के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा इस मद में किए गए व्यय को जोड़ा जाता है। केंद्रीय स्तर पर खचों की गणना जटिल है, क्योंकि शिक्षा मंत्रालय के अलावा लगभग सभी मंत्रालय इस मद में खर्च करते हैं। अब सवाल उठता है कि देश में सरकारों द्वारा शिक्षा पर कुल कितना खर्च किया जाता है? साल 2019-20 में शिक्षा पर कुल सरकारी खर्च 8.93 लाख करोड़ रुपये आंका गया था। इसमें केंद्र सरकार का खर्च 2.27 लाख करोड़ रुपये और राज्य सरकारों का 6.66 लाख करोड़ रुपये था। चालू वित्त वर्ष में अनुमानतः 12 लाख करोड़ रुपये खर्च किया जा रहा है। भारत का वर्तमान जीडीपी करीब 3.3 ट्रिलियन डॉलर का है, जिसका शिक्षा पर अनुमानित खर्च 4.5 प्रतिशत होगा। यह विश्व बैंक के अनुमान से भी मिलता है।
यह एक शुभ संकेत कहा जा सकता है कि भारत का शिक्षा पर होने वाला सरकारी विनियोग और खर्च दुनिया के बहुत सारे देशों की तरह कम नहीं हो रहा है। किंतु भविष्य की अनेक संभावनाओं और राष्ट्रीय संकल्पों को ध्यान में रखते हुए हमें शिक्षा पर खर्ची को वर्तमान स्तर से लगातार बढ़ाना होगा। हमें नहीं भूलना चाहिए कि अगले दस वर्षों में जमीन और व्यापार के लिए विश्व युद्ध भले नहीं, प्रतिभा और मेधा के लिए देशों में कठिन प्रतिस्पर्द्धा होगी। इस प्रतिस्पर्द्धा में हम तभी जीत पाएंगे, जब हम शिक्षा और स्वास्थ्य पर अधिक खर्च करेंगे और मानव पूंजी का निरंतर विकास करेंगे।