
30-04-2024 (Important News Clippings)
To Download Click Here.
Quality Matters in the Knowledge Factory
ET Editorials

On the face of it, the decision seems alright, ostensibly ‘democratising’ access to research opportunities. But there could be aproblem. The rush to incorporate undergrads into PhD programmes could undermine research quality. Pursuit of a doctoral degree demands more than ‘creativity’. It requires rigorous critical thinking, methodological thoroughness and originality of thought. This requires going through a certain experiential period. A 2-year MA degree — MPhil was scrapped earlier — is an excellent time to prep for a PhD. Besides, completing a PhD is not just about writing a thesis but also about making a meaningful contribution to a field. Absence of empirical data to substantiate supposed benefits of the new policy doesn’t help. Transparent communication about expected outcomes and potential challenges is essential to build trust in any education system.
India wants to be a knowledge economy. The focus should not be solely on quantity — more PhD holders — but also on nurturing a culture of quality and intellectual inquiry without cutting corners. Quality needs to be paramount, even as efforts are made to enhance accessibility and inclusivity
चिप मेकर बनने के लिए हर स्तर पर तैयारी जरूरी
संपादकीय
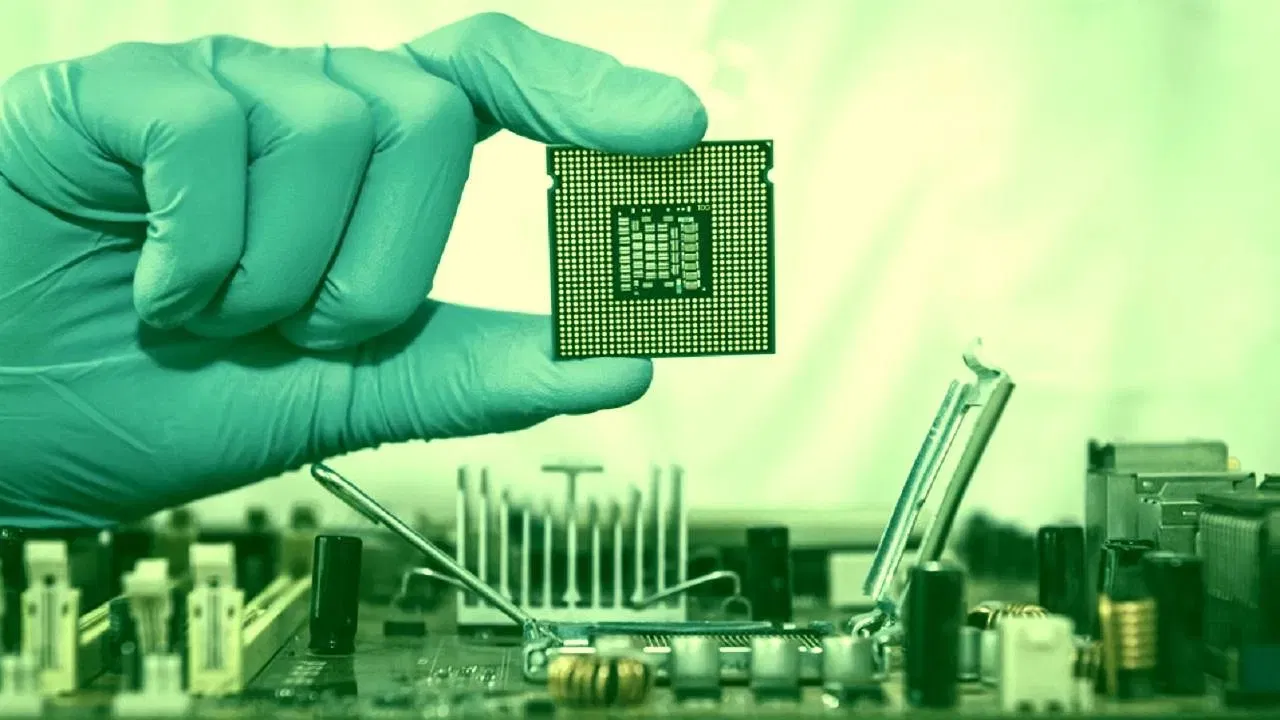
आकड़ो के अभाव में असंतुलित विमर्श
शिवकांत शर्मा, ( लेखक बीबीसी हिंदी के पूर्व संपादक हैं )
भारतीय चुनावों में जातीय और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और सत्ता के दुरुपयोग के आरोप-प्रत्यारोप आम हैं, परंतु क्या इनकी भूमिका निर्णायक होती है? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के पूर्व कार्यकारी निदेशक और प्रख्यात अर्थशास्त्री डा. सुरजीत भल्ला का कहना है कि जीवन में सुधार को लेकर लोगों की राय और नेतृत्व पर भरोसे की भूमिका सबसे बड़ी होती है। अपनी पुस्तक ‘हाउ वी वोट’ में उन्होंने पिछले सात दशकों के आंकड़ों की सहायता से सिद्ध करने का प्रयास किया है कि युद्ध और आतंक जैसी विपदाओं को छोड़ दें तो मतदाताओं के फैसले का 70 प्रतिशत उसकी इसी धारणा पर निर्भर करता है कि कौनसा नेतृत्व उसके जीवन में सुधार ला सकता है। यह सुधार नागरिक सुविधाओं के बिना संभव नहीं है और ऐसी सुविधाएं आर्थिक विकास के बिना संभव नहीं। डॉ भल्ला के आंकड़े दिखाते हैं कि कोविड महामारी की मार के बावजूद पिछले पांच वर्षों में आर्थिक विकास में तेजी के साथ-साथ आर्थिक विषमता का ह्रास भी हुआ है।
अर्थशास्त्रियों और समाजशास्त्रियों के निष्कर्ष मुख्यत: आंकड़ों पर आधारित होते हैं। आंकड़ों के बिना उपयोगी नीतियां नहीं बन सकतीं, पर आंकड़ों को लेकर दो समस्याएं हैं। पहली विश्वसनीयता की और दूसरी व्याख्या की। सरकारें आंकड़ों में मिलावट कर सकती हैं या उन्हें गढ़ भी सकती हैं, लिहाजा उनके आंकड़े पूरी तरह भरोसेमंद नहीं। अंतरराष्ट्रीय और गैर-सरकारी संस्थाओं के आंकड़ों के अपने निहितार्थ होते हैं। आंकड़े विश्वसनीय होने पर भी उनकी व्याख्या से परस्पर विरोधी निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। आंकड़ों की विश्वसनीयता और व्याख्या की इन्हीं चुनौतियों को देखते हुए बहुत से लोकतांत्रिक देशों ने आर्थिक एवं सामाजिक आंकड़ों को एकत्र करने और उनकी वस्तुनिष्ठ व्याख्या के लिए केंद्रीय बैंकों की तरह की स्वायत्त संस्थाएं बना रखी हैं। ये संस्थाएं सरकार और विपक्ष की बजट और कराधान नीतियों, उनके प्रभावों, अर्थव्यवस्था, कर्ज, बेरोजगारी, महंगाई और विकास दर जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं के आंकड़े और उनकी व्याख्या करती हैं और समय-समय पर सरकार और विपक्ष को उनकी नीतियों और उनके संभावित प्रभावों के प्रति सचेत करती हैं।
ब्रिटेन की ऐसी ही स्वायत्त संस्था का नाम ओबीआर या बजट दायित्व कार्यालय है। इसकी स्थापना 2010 में ब्रिटेन के सार्वजनिक वित्तप्रबंधन का तटस्थ और प्रामाणिक विश्लेषण करने के लिए की गई थी। यह सरकार और विपक्ष की राजस्व नीतियों का विश्लेषण करते हुए अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों और समाज के विभिन्न वर्गों पर उनके संभावित प्रभाव का पूर्वाकलन करती है। इसकी वजह से राजनीतिक दल उन लोकलुभावन वादों से बचते हैं, जिनके लिए धन जुटाने की कारगर योजना उनके पास न हो। मीडिया और गैर-सरकारी संस्थाएं भी उसके आंकड़ों और आकलन का भरोसे के साथ इस्तेमाल कर सकती हैं। ऐसी तटस्थ संस्थाएं यूरोप, अमेरिका, कनाडा, आस्ट्रेलिया समेत कुल 37 देशों में हैं, जिन्हें राजस्व निगरानी समिति या परिषद कहा जाता है। अमेरिका में बजट नीतियों की समीक्षा और अनुमोदन चूंकि संसद ही करती है, इसलिए वहां ऐसी अलग संस्था की जरूरत नहीं है। यहां तक कि ईरान, केन्या, दक्षिण अफ्रीका, मेक्सिको और चिली में भी राजस्व नीतियों पर निगाह रखने वाली स्वायत्त संस्थाएं हैं, परंतु भारत में नहीं हैं, जहां ऐसी स्वायत्त संस्थाओं की जरूरत केंद्र ही नहीं, हर राज्य में है। स्वायत्तता के लिए इन्हें रिजर्व बैंक का हिस्सा भी बनाया जा सकता है।
भारत में जिस तरह संवैधानिक संस्थाओं का राजनीतिक विरोध बढ़ रहा है, उसके चलते संभव है कि स्वायत्त बजट निगरानी संस्था का भी विरोध हो। इसके बावजूद गैर-जिम्मेदाराना लोकलुभावनवाद पर अंकुश लगाने के लिए यह जरूरी है। अन्यथा राजस्व का अधिक भाग आर्थिक विकास को गति देने वाले बुनियादी विकास के उत्पादक कामों पर खर्च होने की जगह सब्सिडी और नकद भत्ते जैसे अनुत्पादक कामों पर खर्च होने लगेगा। ऐसी संस्था होती तो सरकार से पूछ सकती थी कि अगले पांच वर्ष तक तीन चौथाई आबादी को पांच किलो मुफ्त राशन देने का क्या तुक है? इस पर खर्च होने वाले करीब दो लाख करोड़ को उद्योगों के विकास में लगाकर रोजगार क्यों नहीं बढ़ाए जा रहे या फिर इस पैसे को गरीबी रेखा से नीचे के लोगों में बांटकर गरीबी का उन्मूलन क्यों नहीं किया जा रहा? इसी तरह कांग्रेस से पूछा जा सकता था कि 30 लाख सरकारी नौकरी, हर स्नातक और हर गरीब परिवार की महिला को एक-एक लाख प्रतिवर्ष और एमएसपी की गारंटी जैसे वादों को पूरा करने के लिए लगभग 10 लाख करोड़ प्रतिवर्ष कहां से आएगा? अगर विरासत कर लगाएंगे तो उसकी दर क्या होगी? मकान और धन-संपत्ति पर ही टैक्स लगेगा या जमीन पर भी? ऐसे टैक्स का रियल एस्टेट कारोबार पर क्या असर हो सकता है और लगभग कितना राजस्व मिल सकता है? उससे आर्थिक नुकसान अधिक होगा या कर की आमद? अमेरिका में केंद्र सरकार विरासत कर नहीं, बल्कि संपत्ति कर लेती है। संपत्ति कर लगभग सौ करोड़ रुपये से ऊपर की संपत्ति पर लगता है। विरासत कर मात्र छह राज्य सरकारें लगाती हैं, जिससे बचने के लिए लोग संपत्ति बेचकर दूसरे राज्यों में चले जाते हैं। ब्रिटेन में सवा तीन करोड़ से ऊपर की संपत्ति पर 40 प्रतिशत की दर से विरासत कर लगता है।
महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा भले अपने आप में निर्णायक न हो, लेकिन यह सीधे तौर पर जीवन में सुधार लाने से जुड़ा है, इसलिए हमेशा चर्चा में रहता है। महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी और रुपये की हैसियत को लेकर तमाम आंकड़े उछाले जा रहे हैं। यदि स्वायत्त आंकड़ा संस्था होती तो उसके आंकड़े संतुलित विमर्श का आधार बन सकते थे। मुफ्त राशन लोगों की गरीबी का परिचायक है या एमएसपी की खरीद से सरकार के मत्थे पड़े अनाज के सही उपयोग का? रुपया संप्रग सरकार की तुलना में अधिक गिरा या कम? लोगों का जीवन स्तर सुधरा है या गिरा? कृषि सुधार न होने से किसानों और देश का फायदा हुआ या नुकसान? ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जो जीवन सुधार की धारणा बनाने में मदद करते हैं और चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। प्रामाणिक आंकड़ों के बिना इन पर सार्थक विमर्श संभव नहीं हो पाता। यूरोप जैसी स्वायत्त संस्था ही इसे संभव बना सकती है।
कितना सच्चा कितना झूठा
अवधेश कुमार
कांग्रेस के रणनीतिकारों का जो भी मानना हो, लेकिन उसके विचार एवं व्यवहार इन दिनों लगातार आम व्यक्ति को हैरत में डालते हैं। संपत्तियों के सर्वे और वितरण संबंधी विवाद कांग्रेस की स्वयं की देन है। इसे लेकर मचे बवंडर के बीच विदेश में कांग्रेस पार्टी की इकाई ओवरसीज कांग्रेस ऑफ इंडिया के प्रमुख सैम पित्रोदा ने उत्तराधिकार कर का बयान देकर इसे लोक सभा चुनाव के एक बड़े मुद्दे के रूप में स्थापित कर दिया है।
स्वाभाविक है कि जब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सहित समूची भाजपा कांग्रेस पर यह आरोप लगा रही है कि वह लोगों के घरों में घुसकर संपत्तियों का सर्वे करेगी तथा समान वितरण के नाम पर अपने चाहत के अनुरूप समुदाय विशेषकर मुसलमानों के बीच बांट देगी उस समय यह बयान बवंडर को और बढ़ने वाला ही साबित होना था। सैम पित्रोदा के बयान को व्यक्तिगत कह कर खारिज करना आसान नहीं है। आखिर वह कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी हैं। और सोनिया गांधी परिवार के निकटतम लोगों में माने जाते हैं। राहुल गांधी को नरेन्द्र मोदी के समानांतर विदेशों में प्रोजेक्ट करने, जगह-जगह उनका भाषण और पत्रकार वार्ता करने की पूरी कमान उनके हाथों होती है। वह कह रहे हैं कि जब हम सामान वितरण की बात करते हैं तो हमें अमेरिका जैसे ‘इन्हेरिटेंस टैक्स’ यानी ‘उत्तराधिकार कर’ पर भी विचार करना चाहिए। उनके अनुसार यहां कई राज्यों में पिता की मृत्यु के बाद संपत्ति की विरासत संभालने वाले को 55 फीसद तक कर दे कर उसके हिस्से शेष 45 फीसद आता है। इससे स्वाभाविक ही यह शंका गहरी हुई कि कांग्रेस सत्ता में आने पर वाकई विरासत कर भी लगा सकती है।
अगर राहुल गांधी ने अपने भाषणों और वक्तव्यों में लगातार जाति जनगणना के साथ वित्तीय एवं आर्थिक सर्वे की बात नहीं करते तो प्रधानमंत्री मोदी या भाजपा को इसे इतना बड़ा मुद्दा बनाने का अवसर नहीं मिलता। उनके भाषण और वक्तव्य सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं, जिनमें वह कह रहे हैं कि हम सत्ता में आने पर जाति जनगणना करेंगे और उसके बाद क्रांतिकारी कदम उठाएंगे, संपत्ति के समान वितरण के लिए वित्तीय सर्वेक्षण करा कर देखेंगे कि किसके पास किस वर्ग के पास कितनी संपत्ति है। इसके बाद जितना जिसका हक होगा उतना उसको दिया जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे सहित कांग्रेस पार्टी के अंदर कोई यह कहने को तैयार नहीं है कि हम वित्तीय और आर्थिक सर्वे नहीं करेंगे तथा समान वितरण की भी बात हमारे एजेंडे में नहीं है। इसकी बजाय कांग्रेस के नेता प्रवक्ता लगातार भारत में उद्योगपतियों, अरबपतियों को निशाना बनाते हुए इनमें से कुछ के हाथों धन सिमट जाने के वक्तव्य दे रहे हैं। चूंकि राहुल गांधी अपनी घोषणा पर कायम हैं और कांग्रेस इससे पीछे नहीं हट रही तो सैम पित्रोदा के उत्तराधिकार कर से देश में भय पैदा हो गया है। कुछ लोगों ने तो यह भी तलाश लिया कि पहले भी भारत ने विरासत कर था और स्वयं पित्रोदा कोई नई बात का नहीं कह रहे हैं। प्रकारांतर से यह स्वयं पित्रोदा के विचार का समर्थन करना ही है।
यह अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून था जो व्यवहार में नहीं उतर पाया तथा सरकारी विभागों में इतनी मुकदमे हुए जिनके खर्च उससे प्राप्त से ज्यादा हो गया। हालांकि प्रधानमंत्री का आरोप है। कि राजीव गांधी के प्रधानमंत्रीत्व काल में उसे इसलिए हटाया गया, क्योंकि उन्हें बिना कर दिए अपनी मां की संपत्ति का उत्तराधिकार लेना था। यह ऐसा मुद्दा आरंभिक दिनों में मेनका गांधी ने उठाया था। बहरहाल, भले अर्थव्यवस्था, समाज और देश के बारे में समझ रखने वाले इसे उचित न मानें, लेकिन कांग्रेस के अंदर भाव यही है कि राहुल गांधी की इन घोषणाओं आम लोगों पर बड़ा प्रभाव है और उन्हें लगता है कि कांग्रेस सत्ता में आई तो देश के धनी और संपन्न लोगों की संपत्तियां लेकर हमारे बीच बांटा जाएगा। पांच न्याय और 25 गारंटी में कांग्रेस ने ऐसी- ऐसी बातें की है जिनको धरातल पर उतारना भारतीय अर्थव्यवस्था के बूते की बात नहीं है, लेकिन इस समय कांग्रेस के थिंक टैंक या सोनिया गांधी परिवार को सुझाव देने वाले मानते हैं कि कांग्रेस को पुराने वामपंथियों की तरह क्रांतिकारी तेवर धारण करना चाहिए तभी वह अपना खोया हुआ जनाधार वापस ला सकती है तथा भाजपा को हरा सकती है। सैम पित्रोदा ने जो कहा है वह इसी सोच का विस्तार है। अमेरिका पूंजीवादी देश है, लेकिन क्रांति हुए बिना वहां वामपंथियों की ताकत हमेशा सशक्त रही है। वहां ये सत्ता, प्रशासन, न्यायपालिका, मीडिया से लेकर पूरे थिंक टैंक पर हावी हैं।
वहां के बड़े-बड़े पूंजीपति जिनमें जार्ज सोरोस जैसे लोग शामिल है, भी अपने प्रकट लक्ष्यों और घोषणाओं में आधुनिक वामपंथी ही है। उनकी दृष्टि की लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में उनकी ही सोच की अर्थव्यवस्था, समाज के बीच संपत्ति का विभाजन, अल्पसंख्यकों के विशेषाधिकार आदि के लक्ष्य से भारत जैसे विकासशील देश में बदलाव के लिए अपने थिंक टैंक विकसित करते हैं और ऐसे लोगों को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। इसलिए यह मानने का कोई कारण नहीं है कि राहुल गांधी, कांग्रेस के दूसरे नेता या सैम पित्रोदा के साथ उनके संवाद नहीं होंगे। इस अतिवादी वाम सोच में ही अल्पसंख्यकों के लिए वैसे विशेष प्रावधानों की घोषणाएं हैं। जिन्हें देखकर भाजपा के लिए यह आरोप लगाना आसान हो गया है कि संपत्ति के सर्वे के पीछे राहुल गांधी और कांग्रेस का इरादा अल्पसंख्यकों के नाम पर मुसलमानों के बीच ही उसे वितरीत करना है।
पहली दृष्टि में कहा जा सकता है कि भाजपा जानबूझकर कांग्रेस को मुस्लिमपरस्त साबित करने के लिए ऐसा कर रही है, किंतु कांग्रेस ने अभी तक इस बात का खंडन नहीं किया है कि उसकी मंशा मुसलमानों को विशेष तौर पर धन के वितरण में या आरक्षण आदि में शामिल करना नहीं है। वर्तमान युग में अपनी क्षमता, प्रतिभा की बदौलत उत्तरोत्तर आर्थिक प्रगति पर किसी भी बंधन की स्वीकार्यता नहीं है। इससे समाज के विकसित होने की मानसिकता कमजोर होती है तथा यह पूरे देश की प्रगति को उल्टी दिशा में मोड़ना है। इस तरह की सोच से भयावह अराजकता और उथल-पुथल की स्थिति पैदा होगी, जिसे संभालना कठिन होगा। चूंकि चुनाव के बीच यह मुद्दा आ गया है इसलिए देश के लोगों को तय करना है कि वह इसके साथ है या विरोध में।
न्याय में तेजी लाएंगे तीन नए कानून
विभूति नारायण राय, पूर्व आईपीएस अधिकारी
देश अपनी अठारहवीं लोकसभा को चुनने में व्यस्त है और चुनावों के शोर-शराबे में एक महत्वपूर्ण चर्चा गुम हो गई है। शनिवार 20 अप्रैल को राजधानी नई दिल्ली के एक सेमिनार में बोलते हुए देश के प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम को इंगित करते हुए कहा कि हाल में भारतीय संसद में पारित तीन नए कानूनों – भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के साथ भारत का आपराधिक न्याय संबंधी कानूनी ढांचा एक नए युग में प्रवेश कर रहा है। यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि ये तीनों कानून पहली जुलाई से अस्तित्व में आ जाएंगे। खुद प्रधान न्यायाधीश के शब्दों में, ‘मैं समझता हूं कि संसद द्वारा इन तीन नए कानूनों को पारित करने से यह स्पष्ट संदेश मिलता है कि भारत अब बदल रहा है। भारत आगे बढ़ रहा है और हमें अपने समाज के भविष्य के समक्ष आने वाली रोजमर्रा की चुनौतियों से निपटने के लिए नए कानूनी औजारों की जरूरत है।
प्रधान न्यायाधीश ने प्रचलित के स्थान पर नए कानूनों के पारित होने को एक ऐतिहासिक क्षण बताया, क्योंकि उनके शब्दों में ‘दूसरे कोई भी कानून हमारे समाज की रोजमर्रा की गतिविधियों को इन फौजदारी कानूनों से अधिक प्रभावित नहीं करते।’
ऐसा क्या है इन तीन संशोधित कानूनों में, जिनके चलते प्रधान न्यायाधीश को इनका संसद में पारित किया जाना युगांतकारी लगा? इसके लिए जरूरी है कि जिन तीन कानूनों की जगह ये नए कानून ले रहे हैं, उनकी पृष्ठभूमि, उद्देश्य और दीर्घकालीन भूमिका को समझ लिया जाए। साल 1857 के विद्रोह को दबाने और ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन अपने हाथ में लेने के बाद ब्रिटिश शासकों को संसद द्वारा पारित ऐसी संहिताओं की जरूरत महसूस हुई, जिनसे वे अपना शासन तो सुरक्षित कर ही लें और साथ यह भी दावा कर सकें कि उनकेउपनिवेश भारत में कानून और कायदे का राज्य है। इसी मकसद से 1860 के दशक में तीन महत्वपूर्ण कानून भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (इंडियन एवीडेंस ऐक्ट) ब्रिटिश संसद से पारित होकर, कुछ अपवादों को छोड़कर, देश भर में लागू किए गए।
इन कानूनों को बनाने के पीछे मुख्य उद्देश्य तो 1857 जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकना और दुनिया को ब्रिटिश राज्य के न्याय प्रिय होने का संदेश देना था, पर इनके चलते भारतीय समाज ने अभूतपूर्व सांस्कृतिक झटके महसूस किए। यह पहला मौका था, जब वर्णाश्रम पर आधारित इस समाज में न्याय के सामने सभी नागरिक समान समझे जाने वाले थे। समान अपराध के लिए ब्राह्मण और शूद्र को एक समान दंड मिलता और दोनों की गवाही की कीमत भी समान होती। मैकाले की बनाई दंड संहिता बहुत ही विस्तृत और मानव जीवन के हर पहलू को छूने वाली थी। यह हुआ भी, पर तेजी से बदलती दुनिया में कोई भी व्यवस्था डेढ़ सौ वर्षों से अधिक समय तक अपरिवर्तनीय नहीं रह सकती। एक औपनिवेशिक शासन के सुदृढ़ बने रहने में मदद करने के लिए बनाई गई संहिताओं ने बखूबी अपनी भूमिका निभाई, पर क्या एक स्वतंत्र भारत में इन्हें बदला नहीं जाना चाहिए था? विकास के पथ पर तेजी से बढ़ने की कोशिश करने वाले समाज में स्वाभाविक रूप से बड़ी आर्थिक हलचलें होनी थीं और इनसे आर्थिक अपराधों की नई श्रेणियां निर्मित होनी थीं। बहुत सारी उप-राष्ट्रीयताओं को एक बड़ी राष्ट्रीयता में समाहित करने की दुष्कर प्रक्रिया भी लंबी खिंचनी थी। इन सबसे अधिक पराधीनता में रहने के आदी नागरिकों के विशाल समूह को किसी स्वतंत्र गणतांत्रिक समाज का नागरिक बनाना भी कोई आसान काम नहीं था। इन सबके लिए जरूरी था कि हमारे कानूनों को बदलते यथार्थ के अनुकूल बनाया जाए। यह अलग बात है कि आजादी हासिल करने के 75 वर्षों बाद ही ये बहुप्रतीक्षित परिवर्तन हो सके।
हममें से जिनका भी साबका भारतीय न्याय प्रणाली से पड़ा है, उनमें से शायद ही किसी के अनुभव सुखद रहे हों। एक अनुभव जिससे सभी सहमत होंगे कि न्याय हासिल करने की पूरी प्रक्रिया बड़ी उबाऊ और थका देने वाली होती है। दीवानी मुकदमों में तो कहावत ही है कि किसी भी वाद का फैसला तीसरी पीढ़ी में होता है। फौजदारी अदालतों की रफ्तार का अंदाजा सिर्फ एक प्रकरण से लगाया जा सकता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ जब पहला आपराधिक मुकदमा दर्ज हुआ, तब उसकी उम्र 17 साल थी और जब उसे पहली सजा मिली, उसकी उम्र 57 साल हो चुकी थी। नए कानूनों के अनुसार, किसी फौजदारी मुकदमे में तीन साल के अंदर फैसला हो जाना चाहिए। यह एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि आज के दिन तो पीड़ित को छोड़कर सारे भागीदारों-जिम्मेदारों की दिलचस्पी मुकदमे को लंबा खींचने में होती है। न्याय के इन भागीदारों में पुलिस, वादकारी, वकील सभी शरीक हैं। न्यस्त स्वार्थ कोई न कोई नुक्ता तलाश कर मुकदमे की कार्यवाही को लंबा घसीटते रहते हैं और नतीजतन मुख्तार अंसारी जैसे धनवान बाहुबली दशकों छुट्टे घूमते रह सकते हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि नई व्यवस्था कैसे फैसलों के लिए तीन साल की अवधि सीमा लागू करवा सकेगी।
गृह मंत्री अमित शाह और उनके मंत्रालय को जहां वर्षों की जद्दोजहद के बाद पुरानों को बदलकर नए कानून लाने की शाबाशी मिलनी चाहिए, वहीं उन्हें न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ की यह सलाह भी याद रखनी होगी कि 1 जुलाई से लागू होने वाले इन कानूनों की सफलता या सार्थकता इन्हें लागू करने वालों की इच्छाशक्ति और नेकनीयती पर निर्भर करेगी। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ के अनुसार, इनके सफल कार्यान्वयन के लिए जरूरी है कि हम अपने फोरेंसिक विशेषज्ञों की क्षमता वृद्धि के लिए पर्याप्त निवेश करें, विवेचनाधिकारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करें और अदालती निजाम को सुधारने के लिए संसाधनों की कमी न होने दें। उनके अनुसार, नए कानूनों का सकारात्मक प्रभाव दिखाने के लिए बिना विलंब अधिकतम निवेश करने की जरूरत है। यदि हम विश्वस्तरीय आधारभूत ढांचे बनाने का दावा कर सकते हैं, तो कोई भी कारण नहीं कि हम विश्वस्तरीय अदालतें, पुलिस तंत्र या जेलें क्यों नहीं बना सकते? इनके लिए हमें बड़े पैमाने पर निवेश करने होंगे, पर इससे कौन इंकार करेगा कि विशाल भारतीय जनता को सुगम न्याय दिलाने के लिए यह करना कोई महंगा सौदा नहीं होगा।