
29-11-2022 (Important News Clippings)
To Download Click Here.
 Date:29-11-22
Date:29-11-22
Hero To Zero
Chinese protests against pandemic policies highlight the limitations of authoritarian states.
TOI Editorials
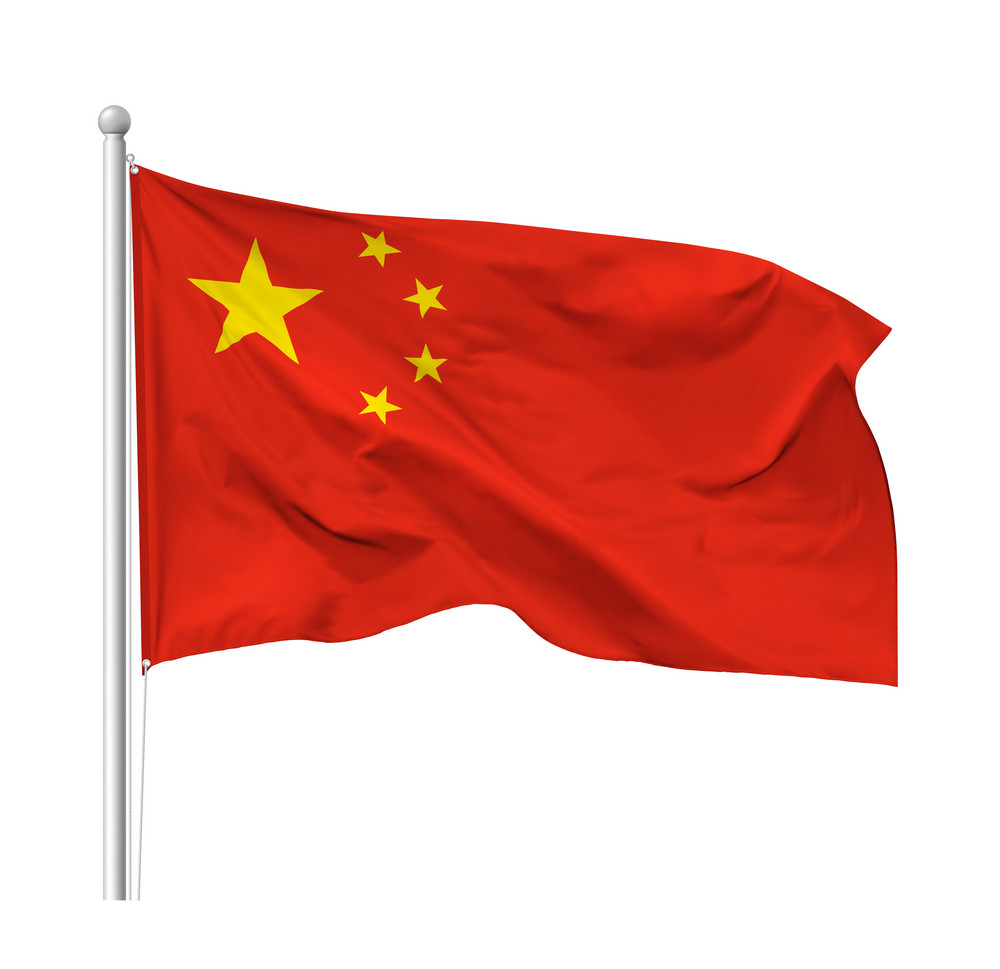
It is precisely to prevent the party-state machinery from being pulled apart by multiple interests and demands that Xi embarked on his centralisation project. He has expunged all distinctions between party and government, purged all the factions within CCP, and reimposed the authority of the party over all units of the Chinese state. This has been evident in China’s zero-Covid strategy which has become a political project. China has seen just six Covid deaths in the last six months from tens of thousands of symptomatic cases – more than acceptable conditions to ease restrictions. But it continues with snap lockdowns, mass testing and real-time tracking of citizens’ health status through smartphone apps. Increasingly, the restrictions themselves are being blamed for non-Covid deaths.
True, China wasn’t the only country to adopt a zero-Covid strategy at the beginning of the pandemic as countries from communist Vietnam to democratic New Zealand followed similar policies. However, those countries have long abandoned zero-Covid, especially after the Delta and Omicron waves proved this strategy ineffective. But China is unable to follow, having staked so much political capital, including Xi’s prestige, on the policy. With widescale protests now, the party would be even more adamant lest it is seen as weak and susceptible to public pressure.
This could damage the Chinese economy. Chinese markets fell yesterday and the yuan tumbled against the dollar, signalling a cooling of investor sentiments. But Xi’s work report presented to the recent 20th party congress already highlighted a prioritisation of security and party authority over economic growth. Thus, there are two lessons here: First, large authoritarian regimes don’t have the flexibility to effectively deal with pandemics, which are like a moving target. And second, they cannot handle the demands of sophisticated economies, as when push comes to shove, they will choose primacy of the regime over boosting growth.
कोटा-सिस्टम पर पुनर्विचार करने का समय आ गया है
नीरज कौशल, ( कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर )
भारत और अमेरिका की सर्वोच्च अदालतों ने अपने-अपने देशों में ऐतिहासिक रूप से वंचित वर्गों के लिए बेहतर अवसर रचने के लिए वैसी नीतियों और कार्यक्रमों को बदला है, जो भेदभाव को प्रोत्साहन देते थे। लेकिन दोनों के रवैयों में बहुत अंतर है। जहां अमेरिका की सर्वोच्च अदालत अफर्मेटिव एक्शन कहलाने वाले उलटे-भेदभाव (रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन) को समाप्त करने जा रही है, वहीं भारत की सर्वोच्च अदालत दूसरी अति पर जाते हुए आरक्षण को और विस्तार देना चाहती है, जो कि उलटे-भेदभाव का भारतीय संस्करण है। अमेरिका की सर्वोच्च अदालत ने 1978 के एक ऐतिहासिक फैसले में कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में दाखिले के लिए नस्ली कोटे को प्रतिबंधित कर दिया था। जबकि भारत में कोटा-सिस्टम प्रचलित परिपाटी है। हमारे यहां दाखिले और नौकरियों के लिए 22% सीटें एससी-एसटी के लिए आरक्षित रहती हैं, 29% ओबीसी के लिए और 10% आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए भी आरक्षित हैं। कोटा बढ़ाने के लिए राज्यों के स्तर पर नई श्रेणियां जोड़ी जा रही हैं।
बीते अनेक वर्षों में अमेरिकी विश्वविद्यालयों ने अश्वेतों और हिस्पैनिकों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए अनेक उपाय किए हैं, जिनमें स्कॉलरशिप देने से लेकर दाखिले के लिए नस्ल को अनेक मानदंडों में से एक बनाना तक शामिल है। मौजूदा सर्वोच्च अदालत में नौ सदस्यों की कोर्ट में से छह जज कंजर्वेटिव हैं और बहुत सम्भव है कि वे कॉलेजों में दाखिले के लिए नस्लीयता के मानदंडों को नकार दें। दूसरी तरफ भारत की सर्वोच्च अदालत ने 1992 के अपने स्वयं के उस आदेश को हाल ही में उलट दिया, जिसमें कुल आरक्षण को 50% तक सीमित रखने का निर्णय लिया गया था। 2019 में भाजपा सरकार ने घोषणा की थी कि आर्थिक रूप से कमजोर तबकों के लिए 10% के आरक्षण को संवैधानिक मान्यता देने का निर्णय न्यायालय ने लिया है। इसके बाद दाखिले और नौकरियों के लिए आरक्षण की सीमा बढ़कर लगभग 60% हो गई थी। अनेक राज्यों में तो इससे भी अधिक आरक्षण दिया जा रहा है। मिसाल के तौर पर अधिकतर पूर्वोत्तर राज्यों में आरक्षित श्रेणियों के लिए 80% या उससे भी अधिक का कोटा है। तमिलनाडु में यह 69% है। इसमें आर्थिक रूप से कमजोर तबकों के लिए हाल में घोषित 10% कोटा शामिल नहीं है। उच्च जाति समूह अकसर शिकायत करते हैं कि इतने अधिक आरक्षण के बाद उनके सामने केवल एक ही विकल्प शेष रह जाता है- अवसरों की तलाश में राज्य को छोड़कर कहीं और चले जाएं। विदेशों में बसे अनेक तमिल कहते हैं कि उन्हें आरक्षण प्रणाली के चलते देश छोड़ने पर विवश होना पड़ा। यह अनेक सवाल खड़े करता है। क्या ऐतिहासिक-अन्यायों को दुरुस्त करने की हमारी कोशिशें देश को नुकसान पहुंचा रही हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि जरूरत से ज्यादा दुरुस्त करने की कोशिश में हम विफल साबित हो रहे हैं? जिस तरह से आरक्षण के कारण अनेक गुणवान युवा उच्चतर शिक्षा के लिए विदेश चले गए हैं, कहीं स्थानीय कर्मचारियों को नौकरियों में आरक्षण देने से विदेशी निवेशक हतोत्साहित तो नहीं होंगे?
अमेरिका का उदाहरण हमारे लिए एक सबक है। वंचित समूहों के साथ ऐतिहासिक रूप से हुए भेदभाव की भरपाई के लिए नस्ल या जाति-आधारित आरक्षण ही इकलौता समाधान नहीं हैं। विश्वविद्यालय दूसरे रास्ते भी अपना सकते हैं। जैसे कि दलित या गरीब वर्ग के विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप देना। याद रखें कि बीते छह दशकों में अमेरिका में अफर्मेटिव एक्शन ने आरक्षण के बिना भी हजारों अश्वेत और हिस्पैनिक विद्यार्थियों की शीर्ष यूनिवर्सिटियों में प्रवेश पाने में मदद की है। इसी के चलते वे सरकार और कॉर्पोरेट सेक्टर में लीडरशिप पोजिशन में आ सके हैं। लेकिन भारत में किसी राजनीतिक दल में यह पूछने का साहस नहीं है कि आरक्षण कब खत्म होगा और आपको कैसे पता चलेगा कि उसने अपने लक्ष्यों को अर्जित कर लिया है? जबकि एक अच्छी नीति वही है, जो अपना मूल्यांकन करती रहे।
Date:29-11-22
यह रिवर्स मेंटरिंग का युग जिसमें बड़े छोटों से सीखते हैं
नंदितेश निलय, ( बीइंग गुड किताब के लेखक और वक्ता )
हाल ही के दिनों में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित अभिनंदन समारोह में मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा, हमें सबसे पहले जिला न्यायपालिका का चेहरा बदलना होगा। हमने अधीनता की संस्कृति को बढ़ावा दिया है। उन्होंने कहा कि कई बार जब जिला न्यायाधीश को बैठकों के लिए बुलाया जाता है, तो वे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सामने बैठने की हिम्मत नहीं करते हैं। ऐसे उदाहरण भी हैं, जब मुख्य न्यायाधीश यात्रा करते हुए उन जिलों को पार करते हैं तो न्यायिक अधिकारी जिलों की सीमाओं पर एक पंक्ति में खड़े होते हैं। ये उदाहरण औपनिवेशिक मानसिकता दर्शाते हैं। हमें इसे बदलना होगा।
जस्टिस चंद्रचूड़ की यह चिंता मानो सभी से सवाल कर रही है। क्या पद व्यक्ति को इतना बड़ा बना सकता है कि उसे दूसरे छोटे नजर आएं क्योंकि वो अधीनस्थ हैं? क्या प्रोफाइल वैल्यू, ह्यूमन वैल्यू से बड़ी होती है? मनुष्य ने समाज का निर्माण किया, लेकिन इतने विभेद खड़े कर दिए कि समान महसूस करने का भाव धुंधला-सा पड़ने लगा है। हम अलग हैं, यह हम अपनी सुविधा से मान लेते हैं, लेकिन हम सब तो एक ही हैं। फिर इस सत्य को कुर्सी या पद से इतने विभेद का सामना क्यों करना पड़ रहा है? महाभारत में महर्षि भृगु महर्षि भारद्वाज से जात-पांत को लेकर पूछते हैं तो भारद्वाज कहते हैं आपके अनुसार हम सब जाति से एक-दूसरे से अलग हैं लेकिन इच्छा, क्रोध, दुख, भूख, भय, चिंता तो सभी को समान रूप से प्रभावित करते हैं। फिर हम अलग कैसे हैं?
पद पाना और उस पद को अपनी जिम्मेदारी और मानवीयता से विशिष्ट बनाना ही कर्तव्य है। पर बॉस-सबोर्डिनेट का द्वैत ऊंच-नीच के भाव को बनाकर रखना चाहता है। ऐसा क्यों है? हमारे मुल्क को स्वतंत्र हुए तो कई दशक हो गए। फिर कोई अपने पद से इतना बड़ा कैसे हो सकता है कि उसे दूसरे छोटे नजर आते हों? तमाम संस्थाओं में यह देखा जा सकता है। कोई किसी से पद में बड़ा है तो यह भी मान लिया जाता है कि वह अपने सबोर्डिनेट से ज्यादा जानता भी है, और समझता भी है। स्टीफन मिचेल ने च्वांगत्सू के शब्दों पर अपनी टिप्पणी में कहा था, कुछ लोगों के पास एटलस कॉम्प्लेक्स होता है, मानो वे दुनिया को कंधों पर ढोते हैं। उनका मानना है कि दुनिया उनके बिना नहीं चल सकती। ऐसा एटलस सिंड्रोम ‘मैं’ का भाव पैदा करता है और टीम भावना गौण हो जाती है। अगर हम कॉर्पोरेट्स में देखें तो वहां भी बॉस-सबोर्डिनेट का भाव चरम पर रहता है। व्यक्तिगत अहंकार इस कदर हावी हो जाता है कि लोग जैसे-जैसे बड़े पदों पर आसीन होते हैं, मुस्कराना भी छोड़ देते हैं। यहां तक कि उनके मैसेज भी एक या दो शब्द में होते हैं।
चार्ल्स डर्बर अपनी किताब ‘अटेंशन की खोज’ में ईगो-सर्फिंग की चर्चा करते हैं, यानी अपने नाम की घटनाओं के लिए इंटरनेट पर खोज करना। डर्बर का तर्क है कि आज के माहौल में सामाजिक समर्थन की कमी है, जिसके कारण लोगों में ध्यान आकर्षित करने की होड़ मच जाती है। इस तरह की आदत यह दिखाती है कि कैसे व्यक्ति अक्सर बातचीत को अपनी ओर मोड़ने के लिए कई तकनीकों का उपयोग करते हैं। अर्थव्यवस्था और संस्कृति में परिवर्तन- जैसे कि इंटरनेट- ने व्यक्तिवाद व अहंकार को बढ़ा दिया है। लेकिन यह युग तो रिवर्स मेंटरिंग का भी है। यिन-चे चेन ने अपने शोध ‘इफेक्ट ऑफ रिवर्स मेंटरिंग’ के द्वारा जनरेशन एक्स और वाई में लोगों की पेशेवर विशेषताओं को देखते हुए पारंपरिक-परामर्श कार्यों पर रिवर्स मेंटरिंग के प्रभाव का पता लगाया। रिवर्स मेंटरिंग में जूनियर कर्मचारी भी वरिष्ठ का मार्गदर्शन करते हैं। अध्ययन का निष्कर्ष है कि एचआर की सहायता से संगठन में रिवर्स मेंटरिंग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। यह अधीनस्थ-संस्कृति पर ब्रेक भी लगाएगा।
मतांतरण रोधी कानून
संपादकीय
यह अच्छा हुआ कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष यह कहा कि वह छल-कपट और जोर-जबरदस्ती से कराए जाने वाले मतांतरण को रोकने के लिए कानून बनाएगी। और भी अच्छा होता कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप करने के पहले ही केंद्र सरकार इस नतीजे पर पहुंच चुकी होती कि ऐसे किसी कानून की आवश्यकता है। वह इससे अनभिज्ञ नहीं हो सकती कि देश के विभिन्न हिस्सों में छल-बल और लोभ-लालच से मतांतरण कराया जा रहा है। मतांतरण में लिप्त तत्वों का दुस्साहस इतना अधिक बढ़ गया है कि वे यह काम खुलेआम कर रहे हैं। इससे राज्य सरकारें भी अवगत हैं, लेकिन वे कुछ विशेष नहीं कर पा रही हैं। दुर्भाग्य से इनमें वे राज्य सरकारें भी शामिल हैं, जिन्होंने छल-कपट और प्रलोभन से कराए जाने वाले मतांतरण के खिलाफ कानून बना रखे हैं। यह किसी से छिपा नहीं कि देश के जिन नौ राज्यों में मतांतरण रोधी कानून हैं, वहां भी निर्धन-वंचित वर्ग के लोगों को धोखा या लालच देकर मतांतरित किया जा रहा है। स्थिति यह है कि मतांतरण में लिप्त तत्व दलितों-आदिवासियों को धोखा देने के लिए भगवा वस्त्र धारण कर रहे हैं। मतांतरण में लिप्त कई ऐसे समूह और संगठन हैं, जो विदेश से अवैध तरीके से चंदा प्राप्त करते हैं। यद्यपि अवैध तरीके से चंदा हासिल करने पर रोक लगाई गई है, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि उस पर पूरी तरह से लगाम लग सकी है।
अब जब केंद्र सरकार इस नतीजे पर पहुंच गई है कि मत-मजहब प्रचार की स्वतंत्रता का अनुचित लाभ उठाया जा रहा है, तब फिर उसे मतांतरण रोधी कानून बनाते समय यह देखना होगा कि इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग रुके। उसे यह भी देखना होगा कि केवल कानून का निर्माण ही पर्याप्त नहीं। उस पर सही तरह अमल भी होना चाहिए। मतांतरण में लिप्त संगठन हतोत्साहित होने और दिखने चाहिए। अभी तो वे बेलगाम ही अधिक दिख रहे हैं। इसका एक कारण यह है कि उन्हें समय रहते उनके किए की सजा नहीं दी जा पाती। केंद्र सरकार इसकी भी अनदेखी नहीं कर सकती कि मतांतरण ने देश के विभिन्न हिस्सों में किस तरह सामाजिक ताने-बाने को बदल दिया है। मतांतरण के माध्यम से न केवल देश के सांस्कृतिक स्वरूप को बदला जा रहा है, बल्कि एक तरह से राष्ट्रांतरण किया जा रहा है। क्या यह किसी से छिपा है कि ईसाई मिशनरियों ने किस तरह पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में जनसंख्या असंतुलन पैदा कर दिया है? पिछले कुछ समय से यही मिशनरियां छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा के आदिवासी बहुल इलाकों में सक्रिय हैं। वे निर्धनों की सेवा का ढोंग ही अधिक करती हैं। उनके जैसी ही हरकतें दीन की दावत देने वाले अनेक दावा संगठन भी कर रहे हैं।
 Date:29-11-22
Date:29-11-22
अनदेखी करना अनुचित
संपादकीय
चीन में कोविड के मामलों में फिर तेजी की खबरें आ रही हैं। वहां पिछले कुछ समय के सर्वाधिक संक्रमण मामले देखने को मिल रहे हैं। इसके साथ ही वहां सरकार की ‘कोविड शून्य’ नीति का भी जमकर विरोध हो रहा है। संक्रमण के मामलों में यह इजाफा ओमीक्रोन प्रकार के एक और ज्यादा संक्रामक उप प्रकार की वजह से हो सकता है। तथ्य तो यही है कि यह वायरस अभी भी फैल रहा है और लगातार अपना स्वरूप बदल रहा है। हालांकि अन्य देश कोविड के साथ जीने की दिशा में आगे बढ़ चुके हैं। परंतु कोविड के साथ जीने के लिए जरूरी नीतियों का प्रभावी क्रियान्वयन तभी हो सकेगा जब सरकार इस पर निरंतर ध्यान देगी। सवाल यह है कि क्या भारत सरकार ने अपना ध्यान भटक जाने दिया है। चीन के उलट भारत ने लगभग सारी संवेदनशील आबादी को टीके की दो खुराक लगवा दी हैं। परंतु कोविड के साथ जीने के लिए नियमित बूस्टर खुराक लेना और नए उन्नत टीके लगवाना भी आवश्यक है। बूस्टर खुराक या एहतियाती खुराक के मामले में भारत का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा है। ऐसे में सरकार के लिए यह आवश्यक है कि वह इस बात पर नजर डाले कि देश के टीकाकरण कार्यक्रम को किस तरह नए ढंग से संचालित करने की आवश्यकता है ताकि 2023 में देश में कोविड की कोई नई लहर न आए।
देश के टीकाकरण कार्यक्रम में दो टीकों का बोलबाला रहा- एक तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित ऑक्सफर्ड / एस्ट्राजेनेका के टीके का लाइसेंसशुदा भारतीय संस्करण कोविशील्ड और दूसरा भारत बायोटेक का कोवैक्सीन। शुरुआत में भारत में बूस्टर खुराक के रूप में इन्हीं दो टीकों की तीसरी खुराक देने को कहा गया था। बाद में अगस्त में सरकार ने कॉर्बेवैक्स टीके को बूस्टर खुराक के रूप में मंजूरी दे दी। हालांकि टीकों के मिश्रण के मामले में और अधिक विज्ञान सम्मत अनुशंसाओं की आवश्यकता है। आदर्श स्थिति में तो इस बात के अध्ययन होने चाहिए थे कि क्या बूस्टर खुराक को लेकर अन्य रुख बेहतर साबित हुए हैं? उदाहरण के लिए ब्रिटेन में जिन लोगों ने ऑक्सफर्ड का टीका लिया था उन्हें बूस्टर खुराक के रूप में एमआरएनए का टीका लगाया गया। इसके अलावा बाद में अन्य नए और प्रभावी टीके भी विकसित किए गए हैं जिन्हें भारत में निर्मित किया जा सकता है। भारत बायोटेक के नाक से दिए जा सकने वाले टीके इनकोवैक को भी भारत के औषधि महानियंत्रक ने हाल ही में आपात इस्तेमाल की इजाजत दे दी है। बिना एमआरएनए टीकों की लाइसेंसिंग या आयात के भी अनेक अन्य विकल्प मौजूद हैं। ध्यान रहे कि पश्चिमी देशों की टीकाकरण योजना में यही टीके प्रमुख थे। विशेषज्ञों से इस बारे में मशविरा किया जाना चाहिए कि इन टीकों को किस प्रकार लिया जाए कि पहले कोविशील्ड या कोवैक्सीन की खुराक ले चुके लोगों को बेहतरीन बचाव मिल सके। कुछ टीकों को इस प्रकार उन्नत बनाया गया है ताकि वे ओमीक्रोन प्रकार के अलग-अलग रूप से निपट सकें। अब तक कोविड का यही प्रकार सबसे संक्रामक नजर आया है।
समय कीमती है। देश में 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए बूस्टर खुराक की शुरुआत किए हुए जल्दी ही एक वर्ष से अधिक समय हो जाएगा। दुनिया भर के श्रेष्ठ व्यवहार पर नजर डालें तो लोगों को दो मूल खुराकों के अलावा दो बूस्टर खुराक दी गई हैं। ऐसे में अब समय आ गया है कि जरूरतमंदों या लगवाने के उत्सुक लोगों को चौथी खुराक भी मुहैया कराई जाए। सरकार इस उम्मीद के भरोसे नहीं रह सकती है कि कोविड-19 महामारी पूरी तरह पीछे छूट चुकी है। अभी भी वायरस का स्वरूप बदलने या स्थानीय स्तर पर महामारी के प्रसार से लोगों की जान जा सकती है या भारी आर्थिक नुकसान हो सकता है। कोविड के साथ जीने का अर्थ उसकी अनदेखी करना नहीं है।
Date:29-11-22
प्रतिभा और योग्यता वाली व्यवस्था बनाम आरक्षण
जैमिनी भगवती, ( लेखक पूर्व भारतीय राजदूत, विश्व बैंक के ट्रेजरी विशेषज्ञ और वर्तमान में सेंटर फॉर सोशल ऐंड इकनॉमिक प्रोग्रेस में प्रतिष्ठित फेलो हैं )
देश के उच्चतम न्यायालय ने 7 नवंबर को अपने फैसले में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के वास्ते 10 प्रतिशत आरक्षण की अनुमति देने वाले 103 वें संविधान संशोधन को बनाए रखने के लिए मुहर लगा दी। इस आरक्षण के लाभ की पात्रता के लिए परिवार की सालाना आमदनी 8 लाख रुपये से कम होनी चाहिए और साथ ही आवासीय संपत्ति और खेती करने लायक जमीन 5 एकड़ से कम होनी चाहिए।
इस 10 प्रतिशत आरक्षण के दायरे में अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) शामिल नहीं होंगे। अब कुल आरक्षण का दायरा 59.5 प्रतिशत तक का होगा, जिसमें एससी, एसटी और ओबीसी के लिए क्रमशः 15 प्रतिशत, 7.5 प्रतिशत और 27 प्रतिशत आरक्षण और इसके साथ ही ईडब्ल्यूएस के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण शामिल होगा। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण के बिना भी तमिलनाडु में पहले से ही आरक्षण का दायरा 69 प्रतिशत के स्तर पर है।
7 नवंबर के फैसले के तीन न्यायाधीश पक्ष में जबकि दो विरोध में थे। उच्चतम न्यायालय का बहुमत वाला फैसला गरीबों के पक्ष में था, चाहे उनकी जाति या सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। विशेषतौर पर बहुमत के इस फैसले पर राय रखते हुए न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी ने कहा, ‘हमारी स्वतंत्रता के 75 वर्ष बाद हमें आरक्षण की प्रणाली पर फिर से सोचने की आवश्यकता है। ‘वहीं एक अन्य न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला ने भी बहुमत की ओर से टिप्पणी करते हुए कहा कि ‘आरक्षण को निहित स्वार्थ नहीं बनने दिया जाना चाहिए।’
अदालत में बहुमत की राय पिछड़ेपन के आधार पर दिए जाने वाले आरक्षण को कम करने या यहां तक कि खत्म करने के पक्ष में प्रतीत होती है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उन दो न्यायाधीशों में से एक थे जिन्होंने इस मामले में इस आधार पर असहमति व्यक्त की थी कि आय पर आधारित आरक्षण दरअसल आरक्षण के अब तक के स्वीकृत मानदंडों का उल्लंघन करता है।
आरक्षण के पक्ष से जुड़ी तर्कों में गायब रहने वाली बात यह है कि सामाजिक रूप से वंचित लोगों को शैक्षणिक स्तर पर या नौकरी के मौके के लिए सफलतापूर्वक प्रतिस्पर्धा करने में कैसे सक्षम बनाया जा सकता है। निश्चित तौर पर सरकारी और निजी स्कूलों तथा कॉलेजों में योग्यता आधारित छात्रवृत्ति के साथ आरक्षण की भी आवश्यकता है।
यह उच्चतम न्यायालय के इस फैसले पर ही आधारित है जिसमें कुछ राज्य सरकारों के सामाजिक पिछड़ेपन या निवासी होने के आधार पर उच्चतम स्तर तक का आरक्षण देने के लिए कानून बनाने का इरादा भी शामिल है और इस तरह के आरक्षण के अपने अलग निहितार्थ हैं।
दिलचस्प बात यह है कि 11 नवंबर के फैसले के चार दिनों के भीतर, झारखंड विधानसभा ने सामाजिक पिछड़ेपन या आर्थिक आवश्यकता के आधार पर कुल आरक्षण का कोटा 59.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 77 प्रतिशत कर दिया। यह अतिरिक्त 17.5 प्रतिशत आरक्षण, झारखंड के निवासियों के लिए होगा जो 1932 के भूमि रिकॉर्ड से निर्धारित किया जाएगा।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अनुसार इस संबंध में राज्य विधानसभा विधेयक तब प्रभावी होगा जब केंद्र सरकार इस कानून को न्यायिक समीक्षा से परे रखने के लिए इस कानून को नौवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए आवश्यक संशोधन करेगी।
हालांकि, 2007 में उच्चतम न्यायालय ने फैसला सुनाया था कि कोई भी कानून भले ही नौवीं अनुसूची में शामिल हो लेकिन यह इस समीक्षा से नहीं बच सकता है कि यह संविधान के ‘मूल ढांचे’ का उल्लंघन करता है या नहीं। अन्य राज्य अपने संबंधित राज्यों के सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित लोगों के लिए अधिक आरक्षण बढ़ाने के लिए झारखंड का अनुसरण कर सकते हैं। हालांकि इसके चलते पिछड़ेपन की पुष्टि या निवासी होने के सत्यापन से संबंधित विवाद अनिवार्य रूप से अदालतों में अंतहीन कानूनी उलझनों को जन्म देंगे।
तमिलनाडु में कई विश्लेषकों और द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम (द्रमुक) पार्टी ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10 प्रतिशत कोटा से एससी, एसटी और ओबीसी को बाहर रखने पर अपना कड़ा विरोध जताया है। कांग्रेस पार्टी ने शुरू में ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण का समर्थन किया था, लेकिन बाद में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए इस नए कोटा से एससी, एसटी और ओबीसी को बाहर रखने के बारे में संदेह जताया है।
कई अन्य लोगों ने टिप्पणी की है कि अधिकांश भारतीय परिवारों की सालाना आमदनी के लिहाज से देखा जाए तब प्रति वर्ष 8 लाख रुपये की आमदनी अधिक है और यह भी स्पष्ट नहीं है कि असंगठित क्षेत्रों में काम करने वालों की आमदनी का अनुमान पूरी पारदर्शिता और विश्वसनीयता से कैसे लगाया जाएगा।
इतिहास के पन्ने को पलट कर देखें तो ब्रितानी हुकूमत की ‘फूट डालो और राज करो’ नीति के कई उदाहरणों में से एक 16 अप्रैल, 1932 का ‘कॉम्युनल अवार्ड’ यानी अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व से जुड़ी योजना की घोषणा है। इसके तहत प्रांतीय चुनावों के लिए नियम निर्धारित किए गए और फिर मुसलमानों, यूरोपियन, सिखों, भारतीय ईसाइयों और एंग्लो-इंडियन के लिए अलग निर्वाचक मंडल स्थापित किए गए।
सामाजिक रूप से भेदभाव का सामना करने वाले दलित वर्गों के लिए भी अलग निर्वाचन क्षेत्र के आवंटन की व्यवस्था की गई जिनमें वे अकेले मतदान कर सकते थे। महात्मा गांधी ने दलित वर्ग के लिए इस तरह के अलग निर्वाचन व्यवस्था बनाने का विरोध किया और गैर-मुसलमानों के लिए निर्धारित सीटों में से उन्हें अधिक सीटें आवंटित की गईं। अन्य निर्धारित सीटें, उद्योग और भूस्वामियों को आवंटित की गई थीं। मुसलमानों और दलित वर्ग के लिए आरक्षित सीटों की कुल संख्या भी सूचीबद्ध है।
7 जुलाई, 1925 को भारत के तत्कालीन विदेश मंत्री फ्रेडरिक ई स्मिथ ने ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में भारत को एक देश के रूप में खारिज करते हुए टिप्पणी की कि ‘भारत को एक इकाई के रूप में देखना उतना ही बेतुका है जितना कि एक इकाई के रूप में यूरोप की बात करना…ऐसा कोई राष्ट्र कभी नहीं रहा।’ ऐसा लगता है कि प्रमुख भारतीय राजनीतिक दल स्मिथ को सही साबित करने पर आमादा हैं क्योंकि आजादी के बाद आरक्षण में बार-बार वृद्धि ने सामुदायिक स्तर के आंतरिक संबंधों को और अधिक बांट दिया है।
सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित लोगों को अच्छी छात्रवृत्ति सहित गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के बजाय, लगातार केंद्र और राज्य सरकारों ने कोटा बढ़ाने का सहारा लिया है। वर्ष 1970 के दशक में, भारत में उच्चतम आयकर दर 90 प्रतिशत से अधिक थी और यह बात अच्छी तरह से स्थापित हो चुकी है कि उच्च कराधान ही कर छूट वाले देशों में पूंजी पलायन को बढ़ावा देता है। इसी तरह, लगातार बढ़ते आरक्षण कोटा ने प्रतिभाशाली लोगों को भारत छोड़ने के लिए प्रेरित करने में योगदान दिया है। ऐसे में निष्कर्ष यही निकलता है कि भारत के असाधारण मानव संसाधनों को देश में बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए हमें अगले 10 वर्षों में सभी जाति, समुदाय और आय-आधारित आरक्षणों को समाप्त करने की आवश्यकता है।
Date:29-11-22
देशों-महाद्वीपों की खेती में विविधता पर जोर
सुरिंदर सूद
देश में विदेशी और नई किस्म के फलों और सब्जियों की खेती तेज गति से बढ़ रही है क्योंकि इनकी मांग काफी बढ़ गई है और इनमें ज्यादा मुनाफा पाने की गुंजाइश भी है। इन दिनों लोगों में विविध प्रकार के अपेक्षाकृत पौष्टिक तथा प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थों को खाने की आवश्यकता को लेकर जागरूकता बढ़ रही है। महामारी के दौरान इस रुझान को एक नई गति मिली जिसने गैर-पारंपरिक फलों और सब्जियों की खपत और बढ़ा दी है जिससे इन चीजों के आयात और घरेलू उत्पादन दोनों में वृद्धि हुई है।
इन वस्तुओं का आयात केवल एक वर्ष में लगभग दोगुना हो गया है और यह 2020 के लगभग 360,000 टन से 2021 में रिकॉर्ड 721,000 टन तक पहुंच गया। इस वक्त घरेलू उत्पादन में सालाना 10 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी का अनुमान है। भारत में अब उगाए और उपभोग किए जा रहे विदेशी पौधों की सूची काफी लंबी हो रही है।
उनमें से सबसे सामान्य एवोकैडो, कीवी और ड्रैगन फ्रूट जैसे फल, ब्रसेल्स स्प्राउट्स, तोरी, शतावरी, रंगीन गोभी, शिमला मिर्च, बेबी कॉर्न और चेरी टमाटर जैसी सब्जियां और सलाद में ब्रोकली, अजवाइन, और पार्सले है। फूजी सेब, लाल अंगूर, विभिन्न प्रकार के बेर और मंदारिन संतरे, पोमेलो (एक प्रकार का अंगूर) और कुछ अन्य दुर्लभ फल और सब्जियां भी बड़ी मात्रा में आयात की जाती हैं।
महानगरों में लक्जरी होटल, रेस्तरां या सुपर मार्केट में अक्सर आने वालों को छोड़कर अधिकांश भारतीय हाल तक इनमें से कई चीजों से अपरिचित थे। अब ये टियर-2 और टियर-3 शहरों में फल और सब्जी की दुकानों में आसानी से उपलब्ध हैं। इनके अलावा भी कुछ अनूठे खाद्य पदार्थ हैं जो पारंपरिक रूप से जंगल से एकत्र किए जाते हैं और इनका उपभोग मुख्य रूप से स्थानीय लोगों द्वारा किया जाता है, लेकिन अब उद्यमी किसान इसे व्यावसायिक स्तर पर उगाते हैं।
इनमें जापानी फल (पर्सिममोन), अंबरेला (भारतीय जंगली आलू बुखारा), जंगली जलेबी या कोडुक्कपुली (कैमाचिल), करोंदा (करांदा चेरी), और बुद्धाज हैंड (फिंगर्ड सिट्रॉन) शामिल हैं। कृषि मंत्रालय के अनुमान के अनुसार वर्ष 2021-22 में 28 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में विदेशी फल उगाए गए थे। वर्ष 2000 के दशक की शुरुआत में ऐसी फसलों का क्षेत्र लगभग नगण्य था। स्वदेशी तरीके से उत्पादित और आयातित बीजरोपण सामग्री (बीज और पौधे) की बढ़ती उपलब्धता और इन असामान्य लेकिन अधिक कीमत वाले कृषि उत्पादों के लिए ई-कॉमर्स सहित नए मार्केटिंग चैनलों के उभार ने उनकी खेती को सरल किसानों के लिए पूंजी जुटाने का एक आभासी माध्यम बना दिया है।
हालांकि, एक उल्लेखनीय बात यह है कि घरेलू खेती में इतनी तेजी से विस्तार के बावजूद, इन उत्पादों की 80-85 प्रतिशत मांग अब भी आयात के माध्यम से पूरी की जाती है। इसे उनकी स्थानीय खेती में वृद्धि की व्यापक क्षमता के संकेत के रूप में देखा जाना चाहिए। देश के विभिन्न क्षेत्रों में काफी विविधता से भरी कृषि-जलवायु परिस्थितियों की वजह से लगभग सभी प्रकार के फलों या सब्जियों को वर्ष के अलग-अलग समय पर उगाने का मौका मिल जाता है।
दिलचस्प बात यह है कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र विदेशी फलों और सब्जियों के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र के रूप में उभरे हैं। वहीं मध्य प्रदेश इन फसलों वाले 11.3 लाख हेक्टेयर क्षेत्र के साथ सबसे आगे है जबकि महाराष्ट्र 11.2 लाख हेक्टेयर क्षेत्र के साथ थोड़ा ही पीछे है।
इन फलों और सब्जियों का वार्षिक उत्पादन मध्य प्रदेश में लगभग 1.2 करोड़ टन और महाराष्ट्र में 1.1 करोड़ टन होने का अनुमान है। सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना असामान्य फलों और सब्जियों के अन्य प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं, हालांकि इन उत्पादों की कुछ खेती अब लगभग सभी राज्यों में होती है। सरकार के एकीकृत बागवानी विकास मिशन के माध्यम से कीवी, एवोकैडो, पैशन फ्रूट, ब्लूबेरी, ड्रैगन फ्रूट, अंजीर, मैंगोस्टीन, पर्सिमन, रैमबुटन्स और स्ट्रॉबेरी जैसे कई नए फलों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के सोलन में मौजूद बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय ने उत्तरी पहाड़ी क्षेत्रों में एवोकैडो, कीवी और हेजलनट जैसी चीजों को उगाने के लिए उपयुक्त तकनीक विकसित की है ताकि अधिक उपज हो सके।
इसी वजह से हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और अन्य जगहों पर इन फसलों के लिए बड़े पैमाने पर पौधे लगाए गए हैं। इसी तरह, लुधियाना के पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने उत्तर-पश्चिम के मैदानी क्षेत्रों में खेती के लिए अंजीर, स्ट्रॉबेरी, खजूर, ब्रोकली, चीनी गोभी, सलाद, अजवाइन, मीठी मिर्च और बेबी कॉर्न जैसी फसलों के कई प्रकार तैयार किए हैं।
दिल्ली का भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पॉलि-हाउस के नियंत्रित पर्यावरणीय परिस्थितियों में विदेशी पौधों को उगाने के लिए प्रौद्योगिकी को बढ़ावा दे रहा है। 1990 के दशक में भारत में शुरू की गई ड्रैगन फ्रूट की स्वदेशी खेती, सबसे दर्ज की गई सफलता की कहानियों में से एक है। वजन घटाने के लिए अच्छा समझा जाने वाला यह चमकीले रंग का मीठा स्वाद वाला फल अब महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर-पूर्वी राज्यों और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में व्यापक रूप से उगाया जाता है।
हाल ही में, महाराष्ट्र के कई किसानों ने, विशेष रूप से सांगली जैसे पश्चिमी जिलों में, गन्ना, अंगूर, सोयाबीन और सब्जियों जैसी पारंपरिक फसलों के बजाय ड्रैगन फ्रूट पर ध्यान देना शुरू कर दिया है क्योंकि इसके लिए कम पानी और नकदी की आवश्यकता होती है, लेकिन बाजार में इसकी अधिक कीमतें मिलती हैं।
इसी तरह, केरल के कई किसानों ने अपनी खेती में विविधता लाते हुए धान या मसालों जैसी पारंपरिक फसलों से लेकर उच्च मूल्य वाली विदेशी फसलों, जैसे मध्य अमेरिका से आए बटरनट स्क्वैश, वियतनाम से आए गैक फल और चीन से आए लोकाट पर जोर देना शुरू कर दिआ है। अन्य राज्यों के किसानों को भी इन प्रगतिशील किसानों का अनुकरण करने और अच्छा प्रतिफल पाने के लिए अपनी फसल में ऐसे उच्च मूल्य वाले विदेशी फलों और सब्जियों को शामिल करने की आवश्यकता है।
असंतुलित होते नगर
ज्योति सिडाना

शहरीकरण का नकारात्मक प्रभाव कहीं न कहीं विकास और निर्माण परियोजनाओं को संदेह के घेरे में लाता है। नगरीय स्वायत्तशासी संस्थाओं में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण और शीर्षस्थ संस्था नगर निगम कहलाती है। सामान्यत: बड़े शहरों या महानगरों में नगर निगम की स्थापना की जाती है, ताकि बिजली, पानी, सड़क, यातायात, संचार, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, जल निकास व्यवस्था, नालियां, सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण तथा रखरखाव, पार्क, खेल के मैदान, पशुशाला निर्माण आदि कार्यों का सुचारु संचालन हो सके। वैश्वीकरण के बाद नगरीय विकास समावेशी विकास की एक आवश्यक शर्त बन कर उभरा है। पर नगरों के असमान विकास, महानगरों का असुरक्षित परिवेश और नगरीय संस्कृति में उत्पन्न होते तनाव नगरीय विकास की पुनर्समीक्षा के लिए हमें बाध्य करते हैं।
देश के कई राज्यों में बढ़ती नगरीय जनसंख्या की समस्याओं का व्यवस्थित तरीके से प्रबंधन करने के उद्देश्य से नगर निगम संस्थानों को विभाजित करने का फैसला लिया गया। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर राजस्थान में भी कोटा, जोधपुर और जयपुर शहर के नगर निगमों को दो भागों में विभाजित किया गया था। ऐसा करने के पीछे नगरीय विकास विभाग का कहना था कि इन तीनों शहरों में जनसंख्या दस लाख से ज्यादा हो गई है। ऐसे में वार्ड बड़ा होने से पार्षद अपने क्षेत्र में विकास कार्य बेहतर तरीके से नहीं करवा सकते हैं। उदाहरण के लिए कोटा नगर निगम का विभाजन कोटा उत्तर और कोटा दक्षिण के रूप में किया गया। इसमें कोई दो राय नहीं कि यह विभाजन विकेंद्रीकरण का एक स्पष्ट उदाहरण है, जिसका उद्देश्य कोटा के हर क्षेत्र में विकास का समान रूप से विस्तार करना है। तेज गति से बढ़ते हुए नगर का लाभ सभी को मिल सके और नगर में समन्वित विकास का माडल मूर्त रूप ले सके, इसके लिए यह विभाजन एक सकारात्मक कदम कहा जा सकता है। पर सवाल है कि क्या वास्तव में यह विभाजन संतुलित विकास कर पाया है, इसका विश्लेषण किया जाना आवश्यक है। विकास में अगर निजी उद्देश्य (राजनीतिक या प्रशासनिक) शामिल हों जाते हैं, तो विकास का कोई भी माडल सकारात्मक परिणाम देने में सक्षम नहीं हो सकता।
अनेक आरोपों-प्रत्यारोपों के बावजूद इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कोटा की जो सूरत बदल रही है, वह आने वाले समय में कोटा को राजस्थान के एक खूबसूरत शहर के रूप में स्थापित करेगी। हाल ही में स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 की रैंकिंग जारी की गई, जिसमें कोटा दक्षिण 141वें और कोटा उत्तर 364वें पायदान पर रहा। इस असमानता और असंतुलित विकास को जन सहभागिता और जनचेतना के माध्यम से दूर किया जा सकता है। दोनों निगमों को अपने-अपने क्षेत्र की समस्याओं और जरूरतों को समझ कर तथा जनता से संवाद करके विकास नीतियों को तय करना होगा। विकास तो हो रहा है, लेकिन अगर विकास का प्रारूप जनता से संवाद करके तय किया जाए कि वह किस तरह का विकास चाहती है, तो राज्य में जमीनी लोकतंत्र को वास्तविक रूप दिया जा सकता है। इसके लिए राजनेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों की प्रतिबद्धता और जन सहभागिता महत्त्वपूर्ण कदम कही जा सकती है। तब नगर निगम का यह विभाजन जन कल्याण और समस्याओं के समाधान की दिशा में सकारात्मक भूमिका निभा सकता है।
इसके साथ ही असंतुलित और अनियोजित शहरी विकास ने देश के समक्ष अनेक चुनौतियां उत्पन्न की हैं। मसलन, नगर पर्यावरण की सुरक्षा के लिए चुनौती बन रहे हैं, क्योंकि हरित क्षेत्र को नगर के विकास के लिए समाप्त किया जा रहा है। ऐसे में जलवायु परिवर्तन ने अनेक नगरों के अस्तित्व को चुनौती दी है, खासकर समुद्र के किनारे बसे नगर अब मानव निर्मित आपदाओं से अछूते नहीं हैं। दूसरा, नगरों में कच्ची बस्तियां बड़ी संख्या में स्थापित हुई हैं, जहां रहने वाले लोग नगरीय जनसंख्या से संबंधित उच्च और मध्यवर्ग की अनेक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, पर खुद न केवल गरीबी के शिकार, बल्कि आवश्यक संरचनात्मक सुविधाओं से वंचित हैं। साथ ही तीव्र प्रौद्योगिकीय विकास ने नगरों में अनेक परंपरागत व्यवसाय करने वाले समूहों के लिए खतरा उत्पन्न किया है। तीसरा, सड़कों का निर्माण नगरीय क्षेत्र में भ्रष्टाचार का एक महत्त्वपूर्ण पक्ष है। पहली बारिश के बाद ही नवनिर्मित सड़कें प्रशासनिक और राजनीतिक प्रबंधन की पोल खोल देती हैं। चौथा, अपराध की दृष्टि से भी नगर तुलनात्मक रूप से अधिक असुरक्षित हैं। लोगों के बीच किसी प्रकार के संवाद का भी अभाव देखा जाता है, इसलिए पड़ोस में क्या हो रहा है, लोगों को खबर भी नहीं होती। या कहें कि भावनाशून्यता, संवादहीनता और व्यक्तिवादिता की प्रवृत्ति नगरीय जीवन का अहम हिस्सा बन चुकी है।
ऐसे में सवाल है कि क्या स्मार्ट शहर अत्याधुनिक होंगे, जिनमें निम्न वर्ग या हाशिये के वर्ग का कोई स्थान नहीं होगा और केवल वही लोग निवास करेंगे, जिन्हें आधुनिक प्रौद्योगिकी की विशेषज्ञता हासिल है? क्या ये शहर बहुमंजिला इमारतों के ऐसे जंगल होंगे, जिनमें व्यक्तिवादिता का मूल्य निवास करता है और आमने-सामने के संबंधों के स्थान पर मोबाइल और कम्प्यूटर वैचारिक आदान-प्रदान का केंद्र बनेंगे। ऐसा लगता है कि शहरों में केवल शक्तिशाली ही रह सकता है या फिर यों कहें कि शक्तिशाली बन कर ही रहा जा सकता है।
इन तमाम पहलुओं पर विचार करने के बाद कहा जा सकता है कि यह आवश्यक नहीं कि जो शहर तकनीकी दृष्टि से उन्नत या अधिक विकसित हों, वे स्मार्ट सिटी भी हों? इसी तरह जो नागरिक आधुनिक तकनीक के ज्ञान से युक्त हों वे स्मार्ट नागरिक भी हों? नगरीय जनसंख्या में तीव्र गति से होने वाली वृद्धि यहां उपलब्ध संसाधनों पर अत्यधिक दबाव उत्पन्न कर रही है, जिसके कारण भोजन, पानी, ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन, रोजगार आदि क्षेत्र चुनौती प्राप्त करते नजर आ रहे हैं। इसलिए आज आवश्यकता इस बात की है कि उपलब्ध संसाधनों को प्रभावी तरीके या स्मार्ट तरीके से प्रयुक्त करना आना चाहिए, ताकि सतत विकास की अवधारणा को मूर्त रूप दिया जा सके।
स्मार्ट सिटी की अवधारणा को मूर्त रूप देने के लिए उपर्युक्त सभी पक्षों पर गहन चिंतन की आवश्यकता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि स्मार्ट सिटी इसलिए विकसित कर रहे हैं कि पूंजीवाद और तकनीकी-पूंजीवाद को निरंतरता मिल सके? कहीं कारपोरेट जगत को ज्यादा से ज्यादा लाभ दिलाने के लिए तो हम ऐसा नहीं कर रहे है? कहीं ऐसा न हो कि शहर और स्मार्ट शहर के बीच के संबंध केंद्र और परिधि के संबंध या विकसित और अविकसित नगर के संबंध बन कर रह जाएं?
चीन में चिंता
संपादकीय
चीन से जो तस्वीरें आ रही हैं, उनसे किसी को भी चिंता का एहसास हो सकता है। दुनिया के ज्यादातर देशों में कोरोना महामारी काबू में आ चुकी है, पर चीन में अब भी यह वायरस लॉकडाउन का कारण बना हुआ है। दरअसल, चीन कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए शून्य-कोविड नीति पर चलता आ रहा है। दिसंबर 2019 से ही चीन के लोगों ने लॉकडाउन के लंबे दौर देखे हैं। यह लॉकडाउन कितना कड़ा होता है, इसकी कल्पना भारत जैसे उदार देशों में कम ही लोग कर सकते हैं। वहां घर का दरवाजा खोलने तक की इजाजत लोगों को नहीं मिलती है। खाने-पीने का वही सामान मिलता है, जो सरकार देती है। चीनी लॉकडाउन का मतलब है, जीवन का पूर्णत: बाधित हो जाना। चूंकि चीन सरकार ने कडे़ लॉकडाउन के दम पर ही अपने लोगों को महामारी के समय बचाया था, इसलिए उसे संक्रमण को रोकने का यही सबसे कारगर तरीका लगता है, लेकिन जाहिर है, लंबे लॉकडाउन से तंग आ चुके लोग अब सड़कों पर उतरने लगे हैं। दरअसल, शून्य-कोविड नीति के खिलाफ चीनियों में व्यापक गुस्से और विरोध की भावना है। बताया जाता है कि सरकार ने लॉकडाउन में कुछ राहत दी है, लेकिन लोग इसे ऊंट के मुंह में जीरा मानते हैं।
चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की आलोचना भी खूब हो रही है। चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग के अनुसार, देश में सोमवार को संक्रमण के 39,452 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि रविवार को 40,347 नए मामले दर्ज किए गए थे। भारत में कोविड को लेकर नेताओं और संबंधित विभागों की बयानबाजी भले ही खत्म हो गई है, पर चिंतित चीन में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियन ने कहा है कि हम मानते हैं, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व और चीनी लोगों के समर्थन से कोविड-19 के खिलाफ हमारी लड़ाई सफल होगी। पिछले दिनों पश्चिमी शिनजियांग क्षेत्र में जो घातक आग लगी थी, उसे भी लोग सख्त कोविड उपायों से जोड़कर देख रहे हैं। जो लोग विरोध कर रहे हैं, उन्हें उल्टे इरादों वाली ताकत कहा जा रहा है, इससे भी विरोध और प्रदर्शन का आकार बढ़ा है। ध्यान रहे, चीन एक ऐसा देश है, जहां शासन सोशल मीडिया को पसंद नहीं करता है। सोशल मीडिया से मिलने वाली चुनौती चीनी सत्ताधीशों को हजम नहीं होती। शासन की अनुदारता या अनुशासन के लिए कड़ाई को अब बहुत से लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। लोग सामने आकर विरोध कर रहे हैं। चीनी सरकार को आम लोगों की पीड़ा को संवेदना के साथ समझना चाहिए। विरोध प्रदर्शन मुख्य रूप से बीजिंग और शंघाई में हो रहे हैं, जगह-जगह बैरियर लगाए गए हैं, लेकिन तब भी लोग खुलकर सड़कों पर उतर रहे हैं।
चीन में ताजा कड़ाई का मामला इसलिए भी सामने आ गया, क्योंकि बीबीसी के संवाददाता के साथ भी मारपीट हुई है। शायद चीनी सैन्य अधिकारियों को पता न था कि वे बीबीसी संवाददाता को परेशान कर रहे हैं, मगर उनकी परेशानी अब बढ़ गई है। वैसे भी, किसी विरोध-प्रदर्शन को कुचलने की कोशिश चीनी प्रशासन को ज्यादा मुफीद लगती है। विरोध की आवाज को कुचलने का पुराना चीनी इतिहास रहा है। ज्यादा चिंता वाली बात यह है कि अगर चीन में अब भी कोरोना संक्रमण तेज है, तो दुनिया को ज्यादा सचेत रहना होगा। क्या कोरोना वायरस का नया संस्करण आया है? पहले भी कोरोना वायरस चीन से ही निकलकर दुनिया में फैला था। अत: सबको सावधान रहना होगा।
Date:29-11-22
पड़ोस में खींचतान का कोई अंत नहीं
विभूति नारायण राय, ( पूर्व आईपीएस अधिकारी )
पाकिस्तान में पिछले एक हफ्ते में जो कुछ घटा, वह प्रत्याशित था। अप्रत्याशित था तो सिर्फ इतना कि सारे रहस्य और तनाव के बीच अंत किसी फुस्स फुलझड़ी-सा हुआ। भारतीय पाठकों को यह अजीब लगेगा कि तीन महीने तक पाकिस्तानी प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया सिर्फ एक सेनाध्यक्ष की तैनाती के ईद-गिर्द घूमता रहा और वह तैनाती थी सेनाध्यक्ष के रूप में किसी लेफ्टिनेंट जनरल की तरक्की। उन्हें यह भी दिलचस्प लगेगा कि इस बीच बहसों के दौरान भारत का जिक्र इस टिप्पणी के साथ आता रहा कि ज्यादातर भारतीय तो अपने वर्तमान सेनाध्यक्ष का नाम तक नहीं जानते और पाकिस्तानी इस नियुक्ति को राष्ट्रीय विमर्श का केंद्र बनाए हुए हैं। हर वह व्यक्ति, जो पाकिस्तानी समाज व राजनीति में दिलचस्पी रखता है, जानता है कि क्यों सेनाध्यक्ष का पद वहां सबसे ताकतवर और गृह, विदेश या रक्षा संबंधी अनेक मामलों में अंतिम फैसला लेने वाला ओहदा होता है।
देश में खास तरह का तनाव तो पिछले आठ महीनों से चल रहा था, जब इमरान खान की सरकार राष्ट्रीय असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव के चलते गिर गई थी। एक अपरिपक्व खिलाड़ी की तरह हर बार गलत चाल चलने वाले इमरान ने इस बार जीवन की सबसे बड़ी गलती की और खुलेआम फौज पर हमले करना शुरू कर दिया। यह किसी से छिपा नहीं कि एक राजनेता के रूप में इमरान की छवि को सेना ने ही पिछले दो दशकों में बाकायदा एक प्रोजेक्ट के तहत गढ़ा था। 2018 के आम चुनावों में उनकी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के लिए दूसरे दलों से जीत सकने वाले उम्मीदवारों को तोड़ने या निर्वाचन बूथों के अधिकारियों को प्रभावित करने से लेकर धन व बाहुबल की व्यवस्था तक की जिम्मेदारी सेना ने उठाई थी। इसके बावजूद उन्हें स्पष्ट बहुमत न मिला, तो सेना ने अपने प्रभाव वाले कई क्षेत्रीय दलों से पीटीआई का गठबंधन करा इमरान की सरकार बनवा दी। पर जल्द ही सेना को महसूस होने लगा कि इमरान किसी गरम आलू की तरह हैं, जिन्हें देर तक मुंह में नहीं रखा जा सकता और उगलने में भी कम रुसवाई नहीं है।
तीन साल में जब देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई और कूटनीतिक महाज पर पाकिस्तान एकदम अलग-थलग पड़ गया, तब सेना को होश आया कि सारी असफलताओं का ठीकरा तो उसी पर फूट रहा था। यह एहसास होने पर कि उन्होंने सदन के बहुमत का विश्वास खो दिया है, इमरान ने बेशर्मी से फौज से जरूरी संख्या बल जुटाने की मांग शुरू कर दी और जब सेना ने खुद को अराजनीतिक और न्यूट्रल कहा, तो इमरान और उनकी सोशल मीडिया सेल ने फौज को जानवर, मीर जाफर, मीर बाकी और न जाने क्या-क्या कहा।
पहले तो फौज हक्का-बक्का रह गई, पर फिर जमीन में एड़ियां गड़ाकर उसने खुद पर लगे आरोपों का जवाब देना शुरू कर दिया। इतिहास में पहली बार खुफिया एजेंसी आईएसआई के प्रमुख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, जिसमें उन्होंने सार्वजनिक रूप से इमरान खान को झूठा घोषित कर दिया। उनके मुताबिक, दिन में सेना को गरियाने के बाद रात के अंधेरे में इमरान या उनके दूत सेनाध्यक्ष जनरल बाजवा से मुलाकात करते हैं और अनुरोध करते हैं कि फौज सरकार पर दबाव बनाए और जल्द चुनावों की तारीखें तय कराए। इसी बीच जनरल बाजवा के रिटायरमेंट की तारीख 29 नवंबर करीब आई, तो उन्होंने यह भी मांग की कि नए सेनाध्यक्ष की नियुक्ति उनकी सहमति से की जाए, अन्यथा जनरल बाजवा को ही चुनावों तक सेवा विस्तार देकर रखा जाए और नया प्रधानमंत्री अगला सेनाध्यक्ष नियुक्त करे। अपनी कोई भी इच्छा पूरी न होते देख इमरान ने आखिरी हथियार के रूप में ‘लॉन्ग मार्च’ की घोषणा कर दी, जिसके तहत लाखों समर्थकों के साथ उन्हें इस्लामाबाद घेरकर तब तक बैठना था, जब तक कि सरकार अगले चुनाव की तारीख न दे दे। पर वह भूल गए कि पाकिस्तान में कोई ‘लॉन्ग मार्च’ फौज के आशीर्वाद के बिना सफल नहीं हो सकता।
इमरान के ‘लॉन्ग मार्च’ के शुरू होते ही ऐसी प्रत्याशित-अप्रत्याशित घटनाएं घटीं, जिनका जिक्र ऊपर किया गया है। सेना का समर्थन खत्म होने के बाद इमरान की गतिविधियां पंजाब व खैबर पख्तूनख्वा तक सीमित रह गईं। उनका ‘लॉन्ग मार्च’ भी लाहौर से रावलपिंडी के बीच ही निकल सका और बिना कोई लक्ष्य हासिल किए विसर्जित हो गया। इस बीच संयुक्त मोर्चे की सरकार में अंतिम फैसले लेने वाले, लंदन में निर्वासित बैठे नवाज शरीफ ने स्पष्ट कर दिया था कि अगले सेनाध्यक्ष की नियुक्ति उनकी मर्जी से ही होगी। सारी बंदरघुड़कियों के बावजूद उन्होंने लगभग प्रत्याशित ढंग से जनरल आसिम मुनीर को नया सेनाध्यक्ष नियुक्त कर दिया।
जनरल आसिम इमरान के प्रधानमंत्रित्व काल में डीजी, आईएसआई थे और उन्होंने प्रधानमंत्री को उनके पारिवारिक सदस्यों के भ्रष्टाचार की जानकारी देने का दुस्साहस किया था, नतीजतन उन्हें हटा दिया गया। इमरान की नापसंदगी जगजाहिर थी, इसलिए आश्चर्य नहीं कि जनरल आसिम मुनीर को नया सेनाध्यक्ष बना दिया गया है। अप्रत्याशित तो वह पटाक्षेप है, जो सनसनी से भरपूर इस पूरे घटनाक्रम के अंत में हुआ।
इमरान खान, उनकी पार्टी के सदस्य और देश के राष्ट्रपति आरिफ अल्वी या दूसरे जनरल शाहिद शमशाद मिर्जा को उत्तराधिकार सौंपने की पैरवी करने वाले निवर्तमान सेनाध्यक्ष जनरल बाजवा समेत सभी ने बिना किसी ना-नुकर के इस फैसले को स्वीकार कर लिया। इमरान खान ने रावलपिंडी में ‘लॉन्ग मार्च’ की तारीख भी उसी दिन रखी थी, जब नए नाम का एलान होना था, पर उसमें बजाय किसी आंदोलन की घोषणा के मार्च को ही खत्म करने का फैसला सुना दिया गया। इमरान ने प्रांतीय विधानसभाओं से अपने विधायकों के इस्तीफे की घोषणा जरूर की, पर इसे भी उनकी अन्य खाली-पीली धमकियों की तरह लिया जा रहा है।
इमरान को मजाक में आजादी के बाद पाकिस्तानी सेना के सामने भारत से भी बड़ी चुनौती के रूप में पेश किया जा रहा है। कई अन्य घटनाओं की तरह पहली बार किसी सेनाध्यक्ष ने अपने अंतिम सार्वजनिक भाषण में स्वीकार किया कि फौज पूर्व में देश की आंतरिक राजनीति में भाग लेती रही है और वायदा किया कि भविष्य में ऐसा नहीं करेगी। देखना है कि इस वायदे पर उनके उत्तराधिकारी कब तक टिकते हैं?
