
29-05-2024 (Important News Clippings)
To Download Click Here.
 Date: 29-05-24
Date: 29-05-24
Elderly Gaps
Health insurers have mostly bypassed senior citizens. That’s the market a new entrant must cover
Editorial

India’s insurance regulations may be tweaked to dismantle the wall between life and non-life insurers. If that happens, LIC, the market leader in life insurance, will consider getting into health insurance. It’s well placed to do so, with an annual profit in excess of ₹40,000cr and its share price having almost doubled since Oct. The big question is, what will this mean for consumers.
Dissatisfaction amidst plenty | Health insurance is highly competitive. At end-2023, there were 29 insurers underwriting health policies, the largest segment of the non-life market. It’s also fast growing. Health insurance premium in 2023 expanded 21%, which was seven percentage points faster than the overall growth in non-life segments.
The numbers are at odds with consumer experience. A survey by insurance broker Policybazaar showed that while 96% of the sample was aware of health insurance, only 43% owned a policy. Two of the three most important reasons for insubstantial ownership were a feeling that premiums are too high and that policies are complex in terms of ailments excluded from coverage etc.
Lopsided market | India’s health coverage is dominated by govt sponsorship, but the premium is raised overwhelmingly from private policies. Insurance regulator Irdai’s data showed that 550 million people have health cover. About 54 of every 100 covers are govt-sponsored. But ₹91 of every ₹100 collected as premium come from individual and group policies.
Gaps galore | Standalone health insurers have sidestepped govtsponsored health coverage. This group of insurers concentrates on the private market and has a far lower claims payout ratio than PSUs and private general insurers. How does that really help when GOI data showed that a mere 6% of the population with an individual health cover are senior citizens even though Irdai encourages their coverage? The most vulnerable group is excluded mainly because the hike in premium is particularly steep for that demographic. A new entrant needs to figure out how to fill the large gap in India’s health cover. Will LIC be that insurer?
The question of Palestine’s UN membership
C.S.R. Murthy, [ is former Professor of International Organization at JNU, New Delhi. He is the author of ‘India in the United Nations: Interplay of Interests and Principles’ ]
Israel’s war on Gaza has raised several ethical, political, and diplomatic questions. One diplomatic development that has attracted a lot of interest is Palestine’s renewed application for membership of the United Nations (UN). Ironically, its quest is stuck at the UN Security Council (UNSC) due mainly to the geopolitical calculations of the U.S., which argued that membership should follow and not precede a negotiated solution to the long-standing conflict.
This is not the first time that Palestine has attempted to obtain UN membership. In 2011 too, its request was opposed by the veto-bearing U.S. in the UNSC. Since then, Palestine enjoys only non-member observer status.
This year, in April, after the UNSC failed to agree on Palestine’s request because of the lone veto cast by the U.S. in its capacity as a permanent member, the UN General Assembly (UNGA) stepped in to voice support to the Palestinian application. On May 10, the UNGA overwhelmingly adopted a resolution affirming Palestine’s eligibility to assume full membership in the UN. It also urged the UNSC to favourably consider Palestine’s request.
Norms and politics
The UN requires membership seekers to be “peace loving” states and to be able and willing, in its judgment, to carry out the obligations of the Charter. While the criteria were liberally interpreted, the procedural threshold laid down for admission turned out to be decisive and difficult, and was dictated by the political exigencies of the five permanent members (P5) in the UNSC at any given time. As such, membership applications require recommendation without the express opposition of any of the P5 before the UNGA accepts the admission request. In other words, the UNSC’s recommendation is ruled out if any of the P5 casts a negative vote by exercising their veto power, whereas no such veto power applies in the UNGA except that the decision should be cleared by a two-thirds majority.
When Cold War politics stalled numerous admission requests in the UNSC in early years, the UNGA sought the World Court’s opinion on whether the UNGA had the power to admit states in the absence of the UNSC’s recommendation. The Court ruled in 1948 that the UNSC’s recommendation is a prerequisite for the UNGA to exercise its power. Subsequently, the deadlock in the UNSC was broken to recommend all pending applications. This marked successive decades of steady increase of the total membership from the 51 founding members to 193 today. It would not be off the mark to note that membership of the UN is invariably viewed as a sought-after confirmation of sovereign statehood of the countries which gained independence from foreign rule or occupation.
The example of Mongolia is comparable to Palestine’s plea. When Mongolia’s membership application was stuck in the UNSC, the UNGA intervened with a resolution similar to what was done in the Palestine case, suggesting that Mongolia deserves a favourable recommendation by the UNSC. Eventually Mongolia became a member in 1961.
India’s approach
India joined 142 member countries in supporting the UNGA in the May 2024 resolution favouring Palestine’s case for membership. India opined that membership status could enhance the prospect of a two-state solution to the protracted Israel-Palestine conflict. Notably, India’s position to the membership question is now entirely in line with the approach articulated during the Nehruvian era — that UN membership should be open to all state applicants without discrimination. In fact, there is not a single instance of India opposing any country’s membership so far. India supported Pakistan’s admission to the UN in 1947 and also representation of the People’s Republic of China’s in 1971, despite a prolonged border conflicts with the latter.
While it is true that the U.S. or the former USSR/Russian Federation stood in the way of many applicants’ prospects of becoming UN members, China is not free from blame either. After being seated in the UNSC in 1971, the People’s Republic of China vetoed newly liberated Bangladesh’s membership application.
What is the way forward?
Clearly Palestine cannot assume full membership bypassing the UNSC and the U.S. China and Russia are apprehensive that such bypassing could become a precedent for the admission of Taiwan or Kosovo later. In a less likely scenario, the U.S. might refrain from casting yet again its veto or abstain from voting, as an expression of displeasure with Israel for ignoring its advice to cease attacks against Gazan civilians, thereby paving the way for the UNGA’s approval of Palestine’s membership. Israel might protest and quit the UN. If the UNSC stalemate continues, the UNGA could possibly consider keeping Israel out of its deliberations. Such a bold tactical move, which is short of Israel’s suspension or expulsion that would be impractical without the UNSC’s recommendation, has precedents. South Africa in the apartheid era and the Serb Republic of Yugoslavia during the brutal ethnic cleansing era were barred from participating in the UNGA.
Apart from these theoretical options, accretion of participatory privileges to Palestine, just short of the power to vote in the UNGA and eligibility to be elected to other major principal organs of the UN, from September would signal that might cannot become right in this age.
जंगलों की कटाई अब कारोबार पर भी भारी पड़ेगी
अंशुमान तिवारी, ( मनी – 9 के एडिटर )
बीते बरस दुबई में पर्यावरण बचाने की जुटान यानी कोप – 28 की बैठक में जब दुनिया के महान नेता भाषणों की जलेबी बना रहे थे, उस वक्त कुछ अखबारों में एक खबर कौंधी | पता चला कि दुबई की एक कंपनी ब्लू कार्बन ने अफ्रीका में जंगल खरीद लिए हैं। इस कंपनी के मालिक शेख अल मकतूम दुबई के सुल्तान के कुनबे से आते हैं। जंगल खरीदना बड़ी बात नहीं मगर इन्होंने तो कुछ और ही किया। ब्लू कार्बन ने जिम्बाब्वे का 20%, लाइबेरिया का 10%, जाम्बिया का 10%, तंजानिया का 8% हिस्सा खरीद लिया। इस भूमि पर जंगल हैं। इन चार अफ्रीकी देशों में जितना जंगल अमीरात की कंपनी ने खरीदा है, वह यूके के क्षेत्रफल के बराबर है! इससे पहले अक्टूबर में अल मकतूम की कंपनी ने केन्या में जंगल खरीदने का एक बड़ा सौदा किया था। खरीदे गए जंगलों के क्षेत्रफल का ब्योरा नहीं बताया गया, मगर इस सौदे की जानकारी केन्या की सरकार की तरफ से दी गई। दुबई की इस कंपनी ने पाकिस्तान में भी जंगल खरीदे हैं। ब्लू कार्बन की पैरेंट कंपनी ग्लोबल कार्बन इन्वेस्टमेंट ने अकेले जाम्बिया के सौदे से 1.5 अरब डॉलर कार्बन क्रेडिट हासिल किए हैं।
बर्बादी का लेनदेन : 1997 में क्योटो में तय हुआ था कि उद्योगों और देशों को पर्यावरण की तबाही और ग्लोबल वार्मिंग घटाने के लिए कार्बन का उत्सर्जन रोकना होगा। यह काम चुटकियों में तो होना नहीं था, इसलिए खुला कार्बन क्रेडिट और कार्बन ऑफसेट का बाजार कंपनियों को अपना कार्बन फुटप्रिंट कम करना होता है। इसके दो रास्ते हैं। एक वे उत्पादन में कार्बन वाली ऊर्जा के इस्तेमाल को कम करें और दूसरा वो जितना धुआं छोड़ रहे हैं उसके बदले उतनी ही ऑक्सीजन पैदा करने वाले किसी प्राकृतिक संसाधन में निवेश करें।
सनद रहे कि ऑक्सीजन तो केवल जंगल ही पैदा कर सकते हैं। कार्बन क्रेडिट एक तरह का लाइसेंस है, जिन्हें दिखाकर उद्योग कार्बन उगलते रह सकते हैं। क्योंकि इनके बदले कहीं कोई जंगल उतनी ही टन ऑक्सीजन बना रहा है। कार्बन क्रेडिट सरकारें या अंतरराष्ट्रीय संगठन जारी करते हैं। मसलन अमेरिका में कैलिफोर्निया की सरकार कार्बन उत्सर्जन करने वाले बिजली घरों और गैस कंपनियों को कार्बन क्रेडिट देती है। जबकि कार्बन ऑफसेट का बाजार फर्क है। यह कार्बन बेचने खरीदने वालों के बीच चलता है। जैसे किसी कंपनी ने जंगल बढ़ाकर उत्सर्जन कम किया तो वह इस क्रेडिट को किसी दूसरी कंपनी को बेच सकती है, जिसे कार्बन फुटप्रिंट कम करना है।
अफ्रीका की होड़ : इस बाजार पर कब्जे के लिए दुबई के शेखों ने गरीब अफ्रीका को धर लिया। अफ्रीका के जंगल हर साल करीब 600 टन सीओ2 सोख सकते हैं, जो दुनिया के लिए भी इको सिस्टम से ज्यादा है। अफ्रीका का अपना उत्सर्जन नगण्य है। अफ्रीका के लिए कार्बन क्रेडिट सबसे बड़ा निर्यात होने वाले हैं। अगले छह साल में यह महाद्वीप करीब 300 मिलियन कार्बन क्रेडिट बेच सकता है। दुबई के शेख को जंगलों की खरीद के साथ अगले 30 साल के लिए कार्बन क्रेडिट बेचने का अधिकार मिल गया है। ब्लू कार्बन अगले एक दशक में कार्बन क्रेडिट की सबसे बड़ी कारोबारी हो सकती है। अफ्रीका में कार्बन क्रेडिट पर टैक्स और कारोबार के नियम भी नहीं बने हैं। सरकारें भ्रष्टाचार का उत्पादन करती हैं। अरब के शेखों के लिए यह बाजार लपकना आसान है।
बाजार का खेल : कोप-दुबई में यह बात साफ हो गई थी कि दुनिया अपना कार्बन उत्सर्जन कम करने वाली नहीं है। सभी देशों ने कार्बन उत्सर्जन बढ़ाने के लक्ष्य रखे हैं। इसलिए अब बाजारों में कार्बन क्रेडिट की होड़ मचेगी। उद्योगों को कार्बन उत्सर्जन कम करना होगा और कंपनियां तलाशेंगी अफ्रीका जैसे बाजार जहां कार्बन सोखा जा सके। मार्केटसैंड मार्केट की रिपोर्ट का अनुमान है कि कार्बन क्रेडिट का बाजार 2022 में 332 अरब डॉलर था, जो सालाना 31% की बढ़त के साथ 2028 में 1.6 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगा। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा कंप्लायंस के बाजार का है यानी वे क्रेडिट जो कंपनियों को खरीदने ही होंगे। मसलन, भारतीय निर्यातकों को यूरोप में निर्यात पर कार्बन टैक्स चुकाना होगा। कार्बन तो कम होने से रहा तो फिर उन्हें कंप्लायंस क्रेडिट (कहीं दूसरी जगह ऑक्सीजन उत्सर्जन की गारंटी) खरीदने पड़ सकते हैं। मार्च 2022 में अबू धाबी में दुनिया का पहला कार्बन क्रेडिट मार्केट भी शुरू हो गया है। कार्बन क्रेडिट के मौजूदा बाजार में पारदर्शिता नहीं है। कार्बन वैल्यूएशन के नियम स्पष्ट नहीं हैं। कोप की बैठक के बाद हाय-तौबा मची है कि अफ्रीका का कार्बन मार्केट सस्ते में लुट रहा है।
और भारत : भारत ने भी कार्बन उत्सर्जन घटाने का वादा नहीं किया। बल्कि कोयला जलाने के नए लक्ष्य तय किए हैं। कल्पना करें कि भारत में कार्बन क्रेडिट का घरेलू बाजार हो तो वह कैसा होगा। क्या उत्तराखंड, हिमाचल, कश्मीर, मध्य प्रदेश और मध्य-पूर्व के राज्य बाकी देश का कार्बन सोखने की कीमत वसूलेंगे? क्योंकि इसी तरीके से बाजार चलने वाला है। मगर भारत के पास जंगल हैं कितने ? वास्तव में, यूके की प्रतिष्ठित एजेंसी यूटिलिटी बिल्डर के मुताबिक जंगल गंवाने में भारत दुनिया का दूसरा सबसे कुख्यात मुल्क है! अगर आप देश के किसी हिस्से में जंगलों के कटने की खबर सुन रहे हैं तो समझिए कि भारत अपना सबसे कीमती बाजार गंवा रहा है। जल्द ही इनकी जरूरत समझ आएगी जब यूरोप के बाजार में भारत के निर्यातकों से कार्बन की खपत और उत्सर्जन का हिसाब मांगा जाएगा!
Date: 29-05-24
दलबदल विरोधी कानून ने उलटे दलबदल को बढ़ाया है
मयूरी गुप्ता, ( विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी में रीसर्च फेलो
पिछले कुछ वर्षों में राजनेताओं ने दलबदल विरोधी कानून का फायदा उठाने के लिए नित नए तरीके ईजाद किए हैं। दलबदल विरोधी कानून या संविधान की दसवीं अनुसूची- 1985 में लागू किया गया था। कानून जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया था, उसमें बहुत कम सफलता हासिल कर पाया है उलटे दसवीं अनुसूची ने उन समस्याओं को और विकट बना दिया, जिनका उसे समाधान करना था। उसने बड़े पैमाने पर दलबदल का मार्ग प्रशस्त किया। इसका मुख्य कारण राजनीतिक दलों में विभाजन और विलय को दी गई छूट थी। इन छूटों ने वास्तव में कई तरीकों से दलबदल को और सुविधाजनक बना दिया है। 2003 में, परिच्छेद 3 के तहत विभाजन वाली छूट को हटा दिया गया था। हालांकि, विभाजन और विलय इन दोनों ही अपवादों के संयुक्त उपयोग से दलबदल विरोधी कानून के क्रियान्वयन पर जो असर पड़ा, वह समझने जैसा है।
लोकसभा और यूपी-हरियाणा विधानसभा के स्पीकर्स द्वारा दिए गए निर्णयों के विश्लेषण से एक पैटर्न का पता चलता है, जहां दलबदल के कारण अपात्रता से बचने के लिए विधायकों द्वारा विभाजन और विलय की छूट का उपयोग बार-बार किया गया था। इसे मोटे तौर पर ‘विभाजन के बाद विलय’ कहा जा सकता है। इन उदाहरणों में, एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि (या जनप्रतिनिधियों का एक समूह) उस राजनीतिक दल से अलग हो गया, जिसमें वे शामिल थे, और विधायक दल के एक-तिहाई सदस्यों का समूह बनाकर विभाजन की छूट का लाभ उठाया। फिर अलग हुए विधायकों के पूरे समूह का दूसरी पार्टी में विलय हो गया। यह मानते हुए कि वे पूर्ण रूप से विलय करेंगे, उन्होंने किसी अन्य पार्टी के साथ वैध-विलय को लागू करने के लिए दो-तिहाई सदस्यों की आवश्यकता को आसानी से पूरा कर लिया। उदाहरण के लिए, 1997 में यूपी के जनता दल विधायक राजाराम पांडे ने दो अन्य लोगों के साथ मिलकर जेडी (राजाराम) गुट बनाने के लिए पार्टी में विभाजन कराया। 2000 में जेडी (राजाराम ) का लोजपा में विलय हो गया। 2002 में राजाराम पांडे ने लोजपा से अलग होकर लोजपा (राजाराम) गुट बना लिया। अंत में पांडे 2003 में सपा में शामिल हो गए।
ऐसा ही पैटर्न लोकसभा और हरियाणा विधानसभा में भी देखने को मिला। मार्च 1992 में लोकसभा सांसद भूपतिराजू विजयकुमार राजू ने तेलुगु देशम पार्टी से अलग होकर टीडीपी (वी) का गठन किया। कुछ ही महीनों के भीतर अगस्त 1992 में उन्होंने पूरे गुट का कांग्रेस (आई) संसदीय दल में विलय कर दिया। इसी तरह हरियाणा में करतार सिंह भड़ाना और 16 अन्य विधायकों ने 13 अगस्त 1999 को हरियाणा विकास पार्टी से अलग होकर एचवीपी (डेमोक्रेटिक) का गठन किया और 3 दिनों में हरियाणा लोकदल में विलय कर लिया। यह बताता है कि कैसे विभाजन और विलय अक्सर तेजी से होते हैं, कभी-कभी तो एक ही दिन में भी जैसे यूपी विधानसभा से मित्रसेन यादव ने 4 मार्च 1994 को सीपीआई से अलग होने का फैसला किया और उसी दिन सपा में विलय कर लिया। इन मामलों में विधायकों द्वारा कई बार पार्टी बदलने के बावजूद वे अपात्र घोषित नहीं हुए।
महाराष्ट्र में दो अवसरों पर अपात्रता से बचने के लिए एक नया पैटर्न तैयार किया गया, जिसे ‘विभाजन के बाद विलय नहीं कहा जा सकता है। दोनों उदाहरणों में, एक समूह ने विधायक दल में आवश्यक दो-तिहाई बहुमत जुटाया, अलग गुट बनाया और बाद में अन्य दलों के साथ सरकार बना ली या सरकार में शामिल हो गए। 2003 के बाद से, बड़े पैमाने पर दलबदलुओं के लिए उपलब्ध एकमात्र छूट परिच्छेद 4 के तहत विलय है। इसके अनुसार विभाजित होने वाले किसी भी गुट का किसी भी दल के साथ विलय या एक अलग समूह नहीं बनने के बावजूद, विभाजन और विलय की राजनीतिक जुगलबंदी ने अलग होने वाले विधायकों को महाराष्ट्र में अपात्रता से बचा लिया। इन हथकंडों ने दलबदल विरोधी कानून को निष्प्रभावी बना दिया है।
तूफान और गर्मी
संपादकीय
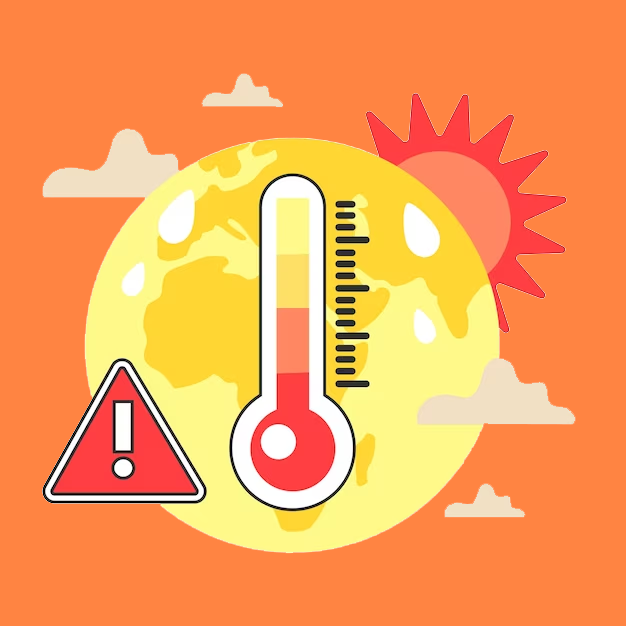
भारत आजकल प्रतिकूल मौसमों की मार झेल रहा है और इसमें सबसे त्रासद मिजोरम में हुआ भूस्खलन है। चक्रवात रेमल के वार से पश्चिम बंगाल तो किसी तरह संभलने लगा है, पर पूर्वोत्तर भारत में अनेक स्थानों पर बहुत बुरी स्थिति बन गई है। खराब मौसम के चलते बचाव प्रयासों में बाधा आ रही है। रेमल के असर से बिहार में भी कई स्थानों पर बारिश हुई है और उत्तर प्रदेश में भी इसके असर की संभावना है। मिजोरम में भूस्खलन व बारिश ने आइजोल को देश के बाकी हिस्सों से काट दिया है। मौसम की मार इतनी तगड़ी है कि राष्ट्रीय राजमार्ग-6 पर आवाजाही बंद हो गई है। पूर्वोत्तर में कई जगह चट्टानों के गिरने से कई अंतरराज्यीय राजमार्ग बाधित हो गए हैं। अधिकारी इंतजाम में लगे हैं, पर नुकसान का वास्तविक आकलन भारी बारिश के थमने के बाद ही किया जा सकेगा। आइजोल के बाहरी इलाके में पत्थर की खदान के ढहने से बीस से भी ज्यादा लोगों की मौत हुई है और अनेक लोग लापता हैं। असम में भी लोगों की मौत हुई है। नदियों का जलस्तर बढ़ गया है, तो बड़ी संख्या में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है।
चक्रवात रेमल ने बांग्लादेश में भी तबाही मचाई है। बांग्लादेश और भारत के पश्चिम बंगाल में लाखों लोगों को एहतियातन विस्थापित किया गया है। भारत और बांग्लादेश को अगर मिला लें, तो चालीस से ज्यादा लोगों की मौत की आशंका है। तूफान और भारी बारिश की वजह से बड़ी संख्या में लोग जख्मी हुए हैं। ज्यादातर इलाकों में विद्युत आपूर्ति बाधित है और बारिश के थमने के बाद ही आपूर्ति व्यवस्था सुधर सकती है। पश्चिम बंगाल में अकेले बिजली के 1,200 से ज्यादा खंभे गिरे हैं। तकलीफ से भरे ऐसे समय में सभी प्रभावित राज्य सरकारों को पूरी सक्रियता के साथ काम करना चाहिए। जिन लोगों ने घर-बार गंवा दिया है, उनके प्रति पूरी संवेदना होनी चाहिए। राहत कार्य में संसाधन की कमी आड़े नहीं आनी चाहिए। चक्रवात और उसके बाद बारिश के चलते कोलकाता महानगर पर भी भारी असर हुआ है। पश्चिम बंगाल के साथ ही पूर्वोत्तर के राज्यों में सड़क, रेल और हवाई यातायात प्रभावित हुआ है। समुद्री चक्रवात हमारे दौर का एक स्याह सच है, जो रह-रहकर हमें रुलाने लगा है। अत: हमें समुद्री तटों पर ऐसे इंतजाम या ऐसी बसावट के बारे में सोचना होगा, ताकि चक्रवात की स्थिति में कम से कम नुकसान हो। समुद्र तटीय इलाकों में किसी भी प्रकार के निर्माण के संबंध में मुकम्मल नीति होनी चाहिए।
देश में तूफान और बारिश से अलग एक विशाल क्षेत्र ऐसा भी है, जहां पारा अपने आसमान को छू रहा है। गांवों से कहीं ज्यादा शहर के लोग परेशान हैं। कंक्रीट के जंगलों में रात के समय में गरमी से राहत नहीं मिल रही है। घर-द्वार तप रहे हैं। आगजनी की आशंका बढ़ गई है। अनेक इलाकों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया है। अस्पतालों को उचित ही सजग और तैयार रहने के लिए कहा गया है। आंकडे़ स्पष्ट नहीं हैं, पर उत्तर भारत में पारा मौत की वजह बनने लगा है। बड़ी संख्या में लोग लू के चलते बीमार हैं। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के छह राज्यों के लिए रेट अलर्ट जारी किया है। अनुमान यही है कि आने वाले कुछ दिनों तक गरमी का प्रकोप ऐसे ही जारी रहने वाला है। गरमी, धूप और लू से बचने के लिए लोगों को स्वयं भी सचेत रहना होगा। बच्चों, बुजुर्गों का खास ध्यान रखने की जरूरत है। राहत की खबर यही है कि मानसून तीन-चार दिन में केरल में दस्तक देगा।
Date: 29-05-24
अब किसी को नहीं सुन रहा इजराइल
अश्विनी महापात्र, ( प्रोफेसर जेएनयू )
दक्षिणी गाजा पट्टी में राफा पर इजरायली हमले के खास निहितार्थ हैं। बेशक, इस हमले में 40 से अधिक आम फलस्तीनियों की मौत हुई है और दुनिया भर में इसकी निंदा जारी है, लेकिन ऐसा लगता है कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सोच-समझकर अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में ऑपरेशन प्रोटेक्टिव शील्ड (जुलाई, 2014), ऑपरेशन कास्ट लीड (दिसंबर, 2018), ऑपरेशन वॉल गार्जियन (मई, 2021) जैसी फौजी कार्रवाइयों के बावजूद इजरायल को इसलिए सफलता नहीं मिल सकी थी, क्योंकि सैन्य ऑपरेशन के बाद अंतरराष्ट्रीय दबाव में उसे संघर्ष-विराम करना पड़ता था और हालात पूर्ववत हो जाते थे। ऐसे संघर्ष-विराम में दोनों पक्षों द्वारा कैदियों की अदला-बदली की भी बात होती थी, लेकिन करीब एक करोड़ इजरायलियों की सुरक्षा का कोई स्थायी समाधान नहीं निकल पाता था।
अब इजरायली प्रधानमंत्री इस परिपाटी को बदलते हुए दिख रहे हैं। इस युद्ध में हमास की मंशा यही लग रही थी कि अक्तूबर, 2023 में हमले के बाद संघर्ष-विराम कर लिया जाएगा और इजरायली बंधकों के बदले फलस्तीनी कैदियों को छुड़ाकर स्थिति सामान्य बना ली जाएगी। मगर नेतन्याहू अब इस समस्या का स्थायी समाधान चाहते हैं। उनकी योजना मानो दुनिया के नक्शे से गाजा पट्टी को मिटा डालने की है, ताकि हमास को सिर छिपाने की कोई जगह न मिले। इससे ही इजरायलियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी। इजरायल का यह भी मानना है कि जब उत्तर और मध्य गाजा से फलस्तीनियों को दक्षिणी इलाकों में आने को कहा गया था, तब आम लोगों की भीड़ में कुछ हमास के लड़ाके भी यहां पर आ गए, जो रह-रहकर इजरायली सुरक्षा बलों को चुनौती देते रहे हैं। उसकी यह सोच उन हमलों से पुष्ट होती है, जो बीते दिनों इजरायल पर हुए हैं। माना जाता है कि उत्तर और मध्य गाजा में हमास ने अपना ठिकाना फिर से बना लिया है।
यही कारण है कि इजरायली प्रधानमंत्री अंतरराष्ट्रीय समुदाय की अवहेलना करते दिख रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि वह किसी दबाव में आकर सैन्य कार्रवाई बंद नहीं करेंगे। अंतरराष्ट्रीय बिरादरी से उनकी नाराजगी की एक वजह फलस्तीन को राष्ट्र का दर्जा देने वाले देशों की बढ़ती संख्या भी है। अब तक संयुक्त राष्ट्र के 195 सदस्य देशों में से 143 राष्ट्र फलस्तीन के पक्ष में हैं, जिनमें नया नाम आयरलैंड, नॉर्वे व स्पेन का है।
इतना ही नहीं, पिछले मार्च महीने में सुरक्षा परिषद् ने गाजा में संघर्ष-विराम और बिना शर्त इजरायली बंधकों की रिहाई संबंधी एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसका अमेरिका ने कोई विरोध नहीं किया, जबकि इससे पहले तक वह इजरायल के पक्ष में खड़ा रहा है। फिर, वाशिंगटन ने इजरायल को भेजी जाने वाली हथियारों की खेप भी टाल दी और राफा पर हमले की सूरत में इसे रद्द करने की चेतावनी दी थी, जिसे इजरायल ने नजरंदाज कर दिया है।
हालांकि, इन सबकी कीमत आम फलस्तीनी चुका रहे हैं। तकरीबन 10 लाख फलस्तीनी विगत अक्तूबर के बाद से पलायन करके दक्षिणी गाजा पट्टी में आ चुके थे, लेकिन ताजा हमले के बाद वे वापस उत्तर व मध्य इलाकों में लौटने लगे हैं। माना जा रहा है कि तीन लाख, 60 हजार फलस्तीनी राफा छोड़कर वापस लौट चुके हैं। जबकि, हालिया हमले में लगभग 1,000 लोगों की मौत के साथ अब तक तकरीबन 40 हजार फलस्तीनी इस युद्ध की भेंट चढ़ चुके हैं। फिर भी, इजरायल इसलिए नहीं पसीज रहा, क्योंकि उसकी नजर में यही आखिरी मौका है, जब वह हमास को जड़ से खत्म कर सकता है। स्पष्ट है, यह एक मानसिक खेल है, जो दोनों पक्षों की ओर से खेला जा रहा है।
ऐसे में, सवाल यही है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय अब क्या कर सकता है? अमेरिका बार-बार इजरायल से यही पूछ रहा है कि आखिर वह चाहता क्या है? वाशिंगटन के मुताबिक, समझौता ही इस जंग का अंतिम रास्ता है। मगर फलस्तीनी प्रशासन भी फिलहाल झुकने को तैयार नहीं है, क्योंकि इससे उसके पक्ष में बन रही सहानुभूति कम हो सकती है। जिस तरह से दुनिया भर के देश उसके पक्ष में गोलबंद हो रहे हैं, विशेषकर अमेरिकी विश्वविद्यालयों में उसके पक्ष में प्रदर्शन हो रहे हैं, उससे उसमें यह भरोसा बना है कि अंतरराष्ट्रीय समर्थन उसके साथ है।
यह माना जा रहा था कि मिस्र, सऊदी अरब जैसे देश मिलकर इस मसले का हल निकाल लेंगे और हमास पर दबाव डालेंगे, ताकि वह कहीं और चला जाए। मगर इजरायल फलस्तीन जैसे किसी समुदाय का ही पक्षधर नहीं दिख रहा। वह गाजा पट्टी पर अपना अधिकार चाहता है। यही कारण है कि वह दो-राष्ट्र के सिद्धांत की भी मुखालफत करता है, जबकि तमाम शांतिप्रिय राष्ट्र इस सिद्धांत के हिमायती हैं।
कुछ लोग तर्क देते हैं कि इजरायल के भीतर जो फलस्तीन समर्थक आवाजें उठ रही हैं, वे इजरायलियों की अपनी सरकार से नाराजगी का संकेत है। मैं इससे सहमत नहीं हूं। इजरायल में जहां-कहीं छिटपुट संख्या में फलस्तीन समर्थक हैं, खासतौर से वेस्ट बैंक में, वहीं विरोध-प्रदर्शन हो रहे हैं। इसका बहुत ज्यादा अर्थ नहीं है। लिहाजा, सवाल यही है कि आखिर इस युद्ध का अंत कैसे हो? इजरायल फलस्तीन का पूर्ण सफाया चाहता है और उसकी नजर में फलस्तीनियों की मौजूदगी उसकी एक करोड़ आबादी की सुरक्षा को दांव पर लगाना है, पर यह व्यावहारिक समाधान नहीं हो सकता। तो, क्या दो-राष्ट्र का सिद्धांत ही समाधान है? अगर हां, तो यह कैसे संभव होगा? इन्हीं सवालों के जवाब में इजरायल-फलस्तीन समस्या का हल भी छिपा है।
तमाम संभावनाओं को देखें, तो उचित हल यही है कि दो-राष्ट्र के सिद्धांत को मान लिया जाए। तभी अंतरराष्ट्रीय समुदाय का दबाव फलस्तीनियों पर पड़ेगा और शांति-बहाली का प्रयास हो सकेगा। ऐसा करने पर शांति-सेना गाजा में तैनात हो सकेगी। दिक्कत यह है कि इस युद्ध को रोकने के लिए कोई भी कुछ खास करता नहीं दिख रहा। अरब देश चुप हैं। इस्लामी राष्ट्र भी कुछ नहीं कह रहे। ईरान ने इस मामले में काफी हद तक कदम बढ़ाए थे, लेकिन एक हवाई हादसे में अपने राष्ट्रपति की दुखद मौत और घरेलू चुनौतियों के कारण वह भी फिलहाल शांत पड़ता दिख रहा है। बाकी देश स्थिति पर निगाह जरूर बनाए हुए हैं, लेकिन वे निष्क्रिय ही जान पड़ते हैं। नतीजतन, यह युद्ध दिन-ब-दिन वीभत्स होता जा रहा है।