
28-05-2020 (Important News Clippings)
To Download Click Here.
 Date:28-05-20
Date:28-05-20
Calamities Galore
In a month of multiple disasters, stretched administrations must counter the heatwave too
TOI Editorials
As Covid cases continue to rise despite a two-month lockdown, the pandemic has stretched thin India’s state capacity, caused economic devastation, and seriously worsened life for its poorer citizens. Unfortunately it is not the only crisis in town. Last week super cyclone Amphan left behind a trail of destruction in Bengal. This week locust swarms have been making waste across different states even as north India (along with southeast Pakistan) acquired the unhappy distinction of being the hottest part of the planet. If governments now have to tackle multiple emergencies simultaneously that too may be a new normal. Just connect the dots with climate change.
There is a direct link between environmental destruction and the increase in zoonotic outbreaks over the last 20 years. Unprecedented locust crises blighting farmlands in several countries in recent years are linked to warmer seas enabling better breeding grounds for these insects. On global warming, note that despite the cut in emissions caused by lockdowns 2020 is threatening to prove the hottest year since measurements began.
All of this underlines how urgent it is that the world comes together to heed Nature’s message. When the climate talks resume, countries must increase their emission cut commitments, bridge the chasm between developed and developing blocs over climate finance and tech transfers, and script a credible path to keeping global temperature increase limited to less than 2°C above pre-industrial levels by 2100. That’s the long-term mitigation. Meanwhile there is much that needs to be done here and now.
Already sapped by Covid and the lockdown, locust affected farming communities must get crop insurance in timely and fair fashion. In addition many of them will now face water woes because of the heatwave. As will many migrant workers still on the long journey home. Local governments need to mobilise strongly and cooperatively to keep people hydrated, provide heat shelters, and medical help for heat exhaustion. As the NDMA guidelines spell out, weaker sections of society are extremely vulnerable to the adverse impacts of heatwaves. Activities like construction which have gotten restarted will again need to hit pause in the scorched regions. The only way forward now is to build resilient infrastructure and communities, which can stand their ground even in the face of overlapping disasters. At present too much of India is too vulnerable.
Stimulus: The Faster, Bigger, the Better
ET Editorials
Dire forecasts of GDP growth plunging deep into the negative territory might or might not be precise, but precision is not the point. They are akin to a threat to life that sends adrenaline pumping through the body, priming it to fight or flee. These forecasts of India’s FY21 GDP shrinking by anything up to 6.8% should send policymakers to stop saying they are open for another round of fiscal stimulus and actually unleash one. It is welcome that the government has announced measures to transfer some purchasing power to the poor and offered some loans to the MSMEs. These steps are akin to putting a dying man on life support. It is not enough to let him lie there. More has to be done to put him on his feet and get him running. That calls for a large dose of investment, which would put purchasing power in the hands of people.
The government, RBI and Sebi need to work together to create a vibrant market for corporate bonds. That is essential for large-scale infrastructure investment. Buying out the debt of stalled real estate and other infrastructure projects, acquiring majority ownership in them and completing them is what a State-owned vehicle needs to do, to create the demand to meet which companies would issue bonds. Let some special vehicles set up by the government buy these corporate bonds and start selling them, instead of holding them to maturity. Credit default swaps and the entire range of derivatives to hedge against interest rate and currency risk must be made available, for the bond market to flourish. Once the bond market is established, domestic and foreign funds would start trading them, deepening the market and encouraging fresh bond issuance to finance fresh investment.
All the investment does not have to be done by the government. For example, the government has opened up coal mining to private sector, including foreign investment. If energetic efforts are made to materialise such investment, that would generate much upstream and downstream investment. Funds alone do not a stimulus make, but funds are key.
Date:28-05-20
e-Learning Not the Same as Learning
ET Editorials
The lockdown has forced schools and colleges to experiment with e-learning. That is welcome. However, digital cannot, and should not, become the default mode. Brick-and-mortar classrooms and educational institutions play a vital role in moulding minds and in training young people to function as groups and within groups, negotiating relationships, hierarchies and imbibing the cultural codes that constitute society. The push to create online resources in the wake of the pandemic will address a critical gap in the Indian education system, catering to students outside of the thin band of elite institutions, who are often unable to access opportunities and resources, especially if they are either ahead of the curve or require remediation.
It has to be ensured that this push of digital content does not result in a homogenised education system, one that fails to leverage the country’s diversity. The move by the government and public institutions to step in, while allowing for private providers to function, is welcome. The decision to increase the number of DTH channels from three to 12 under the Swayam Prabha scheme, in order to reach those who have access to TV but not to the internet, will help circumvent the technology divide. Under Swayam Prabha, the central government has made provisions to share airtime, four hours daily, with states to telecast local language educational content. It would be even better to digitise Doordarshan’s terrestrial broadcast, so that the number of available broadcast channels goes up, allowing dedicated regional channels for different classes to come up.
Making new textbooks available to the ePathshala portal, use of radio and community radio and podcasts and special e-content for the visually and hearing impaired are good initiatives.
Date:28-05-20
Make Our Cities Worker-Friendly
Gautam Bhan ,[ The writer teaches at the Indian Institute for Human Settlements, Bengaluru]
To consider the desperate journeys of lakhs of migrant workers as only ‘a desire to get back home’ erases the fact that the conditions in our cities didn’t allow them a meaningful choice of whether to go or stay. This is as much a push as a pull. Not recognising what makes urban life so vulnerable for so many does injustice to them, ignores the continuing impact on resident workers, and threatens any chance of a meaningful and equitable economic recovery.
The lockdown has shown us that many urban households have no more than 15 days of resilience at any given time. One of the reasons is the relationship between poverty, infrastructure and services in our cities. Everyday life in urban India is a world of multiple transactions of small amounts of cash. Urban workers constantly pay for services every day, or at very high frequency, just to live: for a public toilet, for small meals from a vendor, for that day’s water, towards last-mile transport, in fees for informal healthcare, to secure shelter, for a small phone recharge. This is not the world of salaried workers, monthly bills and accessible credit.
These infrastructures of daily survival are not just of uncertain quality and legality, but they are also expensive. Scholars use the term ‘poverty premium’ to describe the irony that the poor pay more for basic services (water, sanitation, transport, rent, healthcare) as a percentage of their income than the elite. If urban poverty lines just added rent and transport costs, for example, the picture of our cities would change completely. Put simply: urban workers are not newly vulnerable because of Covid-19 — they have always been so. The lockdown has broken coping mechanisms they had devised in the absence of non-cash access to the basics of human life — an absence of social infrastructure with a small ‘i’.
What does this mean for economic recovery? If people are to recover along with the economy — and both need each other — then building the patchwork infrastructures of urban social protection must be a key focus. If this is done in ways that are employment-absorbing, locally rooted and ecologically sensible, it can be the engine that revives local economies, and not just the formal world of industrial estates, salaried workers, firms, banks and enterprises.
The policy instrument for this is an urban employment scheme consciously directed towards the production of social infrastructure. In the short term, it will stabilise wages and address the debt that workers are leaving the lockdown with. In the mid-term, it could enable non-wage savings for working families by reducing the costs of everyday life, allowing a greater resilience against the next shock and improving human development outcomes.
Many states have already realised that without wage-enabled demand, supply-side stimulus packages cannot revive local economies or protect households. Himachal Pradesh and Odisha have already passed urban employment guarantees, though they do not clearly lay out enough direction to what this employment should generate for cities.
Directing urban employment programmes towards social infrastructure can take many forms. In food, it would mean setting up local last-mile delivery systems using para-transit workers, rickshaws and street vendors for an expanded food security programme. In housing, it would mean the upgrading of vulnerable neighbourhoods. In health, it means building neighbourhood-level infrastructure for environmental health — sanitation, waste, water, sewage — as well as the new public health infrastructure our cities will need: community quarantines, small dispensaries, mohalla clinics, health posts near transport exchanges, workplaces, markets and on public streets where so many work and live.
An urban employment scheme that produces this infrastructure can partner with residents and workers to design, build and maintain these systems, recognising that they have always been the people who have built these infrastructures, and not just treat them as ‘beneficiaries’.
Governments are — and will — remain starved for revenue for new infrastructure investments. This is precisely why urban employment programmes to build social infrastructure are timely. Such programmes don’t need vast capital outlays when scaled, designed and rooted locally. Even incremental improvements can lead to substantial household gains, especially in health. Upgrading water and sanitation in vulnerable neighbourhoods has been done at under Rs 15,000 per household.The technology, design potential and expertise exist to do this, if we prioritise investing admittedly scarce resources.
Our economic recovery should not rely on the desperation of workers to return to cities. It is not clear whether they will return, or return to the same cities they left — unless cities can demonstrate that they have addressed what made them leave. Industries able to incentivise workers, and cities that consciously build social safety nets, will be the ones to see workers return.
The fortune of others
Society needs to regain moral compass, address plight of people in cities whose precarious livelihoods keep them steps away from destitution.
Sanjib Baruah , [ The writer is professor of political studies, Bard College, New York. He is the author of In the Name of the Nation: India and its Northeast.]
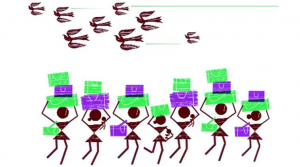
Epidemics are “not random events that afflict societies capriciously and without warning,” says historian Frank Snowden in his book Epidemics and Society: From the Black Death to the Present. “On the contrary, every society produces its own specific vulnerabilities.”
The critical vulnerabilities of Indian society that the COVID-19 pandemic has exposed are undoubtedly those laid bare by the humanitarian crisis that unfolded as the nation-wide lockdown took effect. The searing images of the endless ordeal of tens of thousands of famished and exhausted “migrant workers” trying to make their way back to their home villages to escape starvation in cities where they work, will endure long after the pandemic is over.
The world’s severest lockdown dealt a body blow to their insecure and fragile urban livelihoods, and many of them also faced imminent eviction. With public transportation shut down, many began their long journeys on foot over distances that could span hundreds of miles. A large number of them died of heat, exhaustion and starvation; and quite a few were killed in horrific accidents.
Reverse migration of this kind is not how epidemics and migration have historically been linked together. This history is mostly of the fortunate few fleeing urban contagion to places where the chances of survival are better. This happened at the time of the Black Death in Europe in 1348; and in more recent years, during the SARS outbreak in China, and in New York City during the current pandemic.
To be sure, reverse migration to villages by the working poor is not new to the history of epidemics in India. During the plague panic in colonial Bombay — which gave us the infamous Epidemic Diseases Act of 1897 — more than half the city’s population left for the countryside fleeing the disease as much as the colonial state’s authoritarian response to it. But they were caught between the plague-ridden city and the famine-stricken countryside, and the flow of migrants soon became a two-way process. It produced a crisis of labour supply in the city’s important cotton textile industry that led to a shift in the balance between capital and labour which worked to the advantage of workers — albeit temporarily.
The multitudes escaping Indian cities more than a century later, however, are mostly employed in an informal labour regime in industries and service sectors increasingly characterised by outsourcing and contracting-out arrangements. Without the moral imagination and political will to launch a massive social intervention, it is unlikely that the shock to the labour supply will yield even modest wage or welfare gains for these workers.
A report by the Stranded Workers Action Network, which its authors describe as “distress-biased” because it draws on data collected from those who made distress calls to the network, found the majority of them to be factory or construction workers on a daily wage. The rest earned their daily wages as drivers, domestic workers, and self-employed workers — among them were street vendors and those engaged in zari embroidery work. It is not a representative sample, but the figures convey some idea of the circumstances that pushed them to the brink; only about 6 per cent of those who reached out to the network received full wages during the lockdown and about 78 per cent received no payments. Ninety-nine per cent of the self-employed — among them, street vendors and rickshaw pullers — earned no money at all during the lockdown.
That such important segments of India’s urban workforce are “migrant workers”— and the fact that we refer to these poor fellow citizens as migrants — is itself quite telling. They are not all migrants in a strict sense. It is their precarious employment and the high cost of permanent relocation in cities that make them oscillate between urban India and their home villages. Many male seasonal migrants leave their families behind and return to their villages when old age or illness makes them unemployable.
A 2012 volume of essays on internal migration in India published by the UNESCO distinguishes three types of rural to urban migrants: (a) permanent, (b) semi-permanent or long-term circular and (c) seasonal and temporary or circular migrants. Significant segments of India’s informal or unorganised economy escape official statistical recording. Seasonal or circular rural-to-urban migrants, for example, are a major segment of the workforce in India’s formidable construction industry. Yet neither the Census nor the National Sample Survey, says Ravi Srivastava, who has studied internal migration extensively, “adequately capture seasonal and/or short-term circular migration”. He and his research team have tried to get a handle on the phenomenon with a number of micro-level field surveys to complement macro data.
The difficulties encountered by Srivastava and Rajib Sutradhar in surveying construction workers in Delhi and its satellite towns are revealing. First, the gruelling work schedule of construction workers — long hours and seven days a week with no rest day — made access to them difficult. Second, the construction sites that included the living areas for workers are guarded by private security guards creating another set of hurdles. Several interviews “had to be abandoned half-way due to the hostility of security staff and/or contractors”.
When the term informal sector began to be used in development studies in the 1970s it was thought of as a residual — even temporary — niche peculiar to the urban economies of developing countries. As Dutch sociologist Jan Breman puts it, informal economy activities were expected to “fade away with the expansion of the formal economy”. But during the successive decades “informality turned out to be not a waiting room but an end station for the swelling workforce locked up in it”.
The informal or the unorganised sector now accounts for nearly half of India’s GDP and 80 to 90 per cent of the labour force (including non-plantation agriculture). Outsourcing of work to smaller firms and contractors has informalised even many organised sector industries. With the erosion of labour rights and social protection associated with formal sector jobs, it is not surprising that our cities now host thousands of people whose precarious livelihoods keep them steps away from destitution.
But a far more deleterious effect of informalisation is that we now seem to be on the verge of abandoning even the aspiration for an inclusive future. With informal employment dominating the economy, laws regulating working conditions are now nothing more than aspirational. Still, it boggles the moral imagination that soon after the historic exodus, in the middle of the pandemic, a number of state governments decided to dilute labour laws turning the clock back on legal working hours from eight-hour days to 12-hour days (six-days a week). And this with the half-baked intention of attracting businesses that might leave China.
One can only hope that our society will regain its moral compass and re-discover the quality that Adam Smith — popularly thought of as the high priest of capitalist individualism — called sympathy. No matter how selfish we suppose human beings to be, he said, “there are evidently some principles in his nature, which interest him in the fortune of others, and render their happiness necessary to him, though he derives nothing from it, except the pleasure of seeing it.”
Rising tide
China’s effort to tighten grip on Hong Kong with tough laws may not help its cause
EDITORIAL
Protests and violence returned to Hong Kong on May 24. In scenes that became all-too-familiar through much of last year, police used water cannons, tear gas, and pepper spray, as a protest march descended into clashes between protesters and riot police. The weekend’s march had originally been planned ahead of a debate in Hong Kong’s Legislative Council (LegCo) on a new national anthem bill, which would punish anyone who insulted China’s anthem with up to three years in prison. The protest assumed significance when two days before the march, China’s central government stunned Hong Kong’s pro-democracy parties by tabling a new national security bill, as the National People’s Congress met in Beijing. The bill, expected to be passed when the NPC’s annual session ends on Thursday, urges Hong Kong’s legislature to pass national security laws “as soon as possible”. Else, the bill leaves open the possibility that Beijing could bypass LegCo, declaring that the NPC is “authorized to draft laws” on security for Hong Kong. What has concerned pro-democracy activists in Hong Kong is a new provision for China’s national security organs to “set up institutions” in the Special Administrative Region.
Under the Basic Law that has governed Hong Kong since 1997, the SAR has a high degree of autonomy “to enjoy executive, legislative and independent judicial power, including that of final adjudication”; only defence and foreign affairs are to be handled by Beijing. Article 23 of the law requires Hong Kong to pass national security legislation, but the law makes clear it is Hong Kong’s legislature that enjoys the power to make and repeal laws — the bedrock of the “one country, two systems” model. In 2003, a national security bill allowing the shutting down of seditious newspapers and carrying out warrantless searches was withdrawn after protests. Beijing now argues that last year’s protests, blamed on “external forces”, underlined the need for a new law to curb “acts of secession and subversion”. The timing of the move may reveal its motivations. Hong Kong’s legislative elections are in September and the pro-Beijing camp fears losing control of LegCo, even if its unusual rules have stacked it with pro-Beijing lawmakers. Only half of the 70 seats are directly elected; the rest are nominated. Yet such is the rising tide of support for pro-democracy parties that Beijing worries it could lose the two-thirds majority needed for any amendments to the Basic Law. The pro-democracy camp swept November’s district council elections, seen as a referendum on the youth-driven protests. A record 70% turnout won the pro-democracy candidates 390 of 452 seats. The elections demonstrated that public support for full democracy is growing. The new piece of legislation is aimed at tightening Beijing’s grip over Hong Kong, but it may well end up having the opposite effect. Hong Kong cannot be won without its people.
Date:28-05-20
Helping supply chains recover
Not a fiscal stimulus, but cutting government expenditure, removing price controls, and opening up trade will help
Vipin P. Veetil & Kumar Anand , [ Vipin P. Veetil is Assistant Professor at IIT-Madras and Kumar Anand is an economist based in Delhi ]

The Indian government has announced a sizeable fiscal stimulus, which some commentators believe can help revive the economy. There are, however, good reasons to doubt this belief. Much of the decline in output is due to supply chain disruptions generated by the lockdown. Government spending can do little to alleviate this. Putting money in the hands of people can increase the demand for goods but cannot increase the supply of goods and services.
In modern economies, the production of goods happens through complex supply chains that traverse geographical boundaries. Upstream sectors like ‘mining’ produce metals that are in turn used to produce machines. These machines are used to sow seeds, harvest crops, and transport fuel. Finally, the harvested crops are used by downstream sectors to produce flour and bread. At each step, machines and labour combine to produce goods which are the inputs for sectors further downstream.
Reduction in output
Under the lockdown, numerous inputs have not moved from their producers to their users. These disruptions may not at first generate a reduction in consumer goods like bread. However, the availability of consumer goods will begin to decline as bakers run out of flour, and mills exhaust their stocks of wheat. And there is no way to guarantee the flow of essential goods while suspending the production of non-essential goods. Automotive spare parts may be non-essential in the short run, but become essential as food-carrying trucks begin to break down. How far is the long run? This is difficult to say; there may be some variation across goods.
The supply chain disruptions are going to be amplified by labour shortage as workers remain at home. Countries like India are likely to experience a greater reduction in output on this count than, say, Europe or the U.S. because of the higher labour intensity of production (think of the difference in unloading of goods in the port at Rotterdam and the port at Kochi). Poorer countries are less likely to be able to substitute locked down labour with capital because of the dearth of capital in these nations.
As economies emerge out of the lockdown, entrepreneurs, workers, and consumers must adjust to the new reality. The world supply chain must adapt. Firms may, for instance, choose to source inputs from suppliers in their geographical proximity to minimise the risk of future disruptions. This involves building productive capacity at new locations, all of which requires investments fuelled by savings. Furthermore, the investments must be guided by price signals. Within a market economy, the movement of prices provides the incentive and information needed to adapt and grow. As economist Ronald Coase put it, prices are bundles of information wrapped in an incentive. As the prices of some inputs rise, the buyers of these inputs look for alternate suppliers, and firms which did not hitherto produce the good have an incentive to do so. The key to economic recovery lies in millions of such adjustments through which firms locate new providers of inputs, new buyers of their output, and build factories at new locations.
Why stimulus packages won’t help
Unfortunately, market adjustment processes are likely to be disrupted by government stimulus packages. Governments spend by printing money, raising debt, or increasing taxes. Irrespective of the way in which the expenditure in funded, resources are transferred from private entrepreneurs to government bureaucrats. When governments print money, they draw resources through inflation. Bureaucrats tend to be less efficient than profit-motivated firms in allocating scarce resources. Bureaucrats have little incentive or information to bring about the granular supply chain adjustments necessary to revive growth. As the stimulus package kicks in, economic efficiency is likely to decline and so are the chances of a timely recovery of output.
So what can the government do? The experience of West Germany after World War II has a useful lesson. Beginning mid-1944, Allied bombing disrupted the German supply chain by targeting bottleneck sectors like electric power generation. This destruction of the supply chain devastated the German economy. Per person food production fell to about half of its pre-war level. Two years later, this changed after Chancellor Ludwig Erhard lifted price controls and cut taxes. West German entrepreneurs re-established a thriving supply chain through which goods went from upstream sectors to final consumers. By 1950, per capita income in West Germany had reached its pre-war level.
The recent supply chain disruptions are likely to last long. The path to recovery lies in cutting government expenditure, removing price controls, and opening up trade.
रिवर्स माइग्रेशन ज्यादा दिन तक संभव नहीं है
संपादकीय
राजनीति में साफगोई का स्थान नहीं होता। उत्तर भारत के तमाम राज्यों की सरकारों ने पहले तो ‘प्रतिलोम प्रवास’ (रिवर्स माइग्रेशन) यानी राज्य से बाहर गए मजदूरों की ‘घर वापसी’ का पुरजोर विरोध किया। बसें नहीं दीं, सीमा पर पुलिस से पिटवाया और ट्रेन चलने की इजाजत देने में भी आनाकानी की। लेकिन, जब हर तरफ से दबाव पड़ा तो सरकारों के बयानों में यू-टर्न आया। ‘जो जहां है, वहीं रहे’ से बदलकर नया बयान आया ‘वो आएं, बहुत काम है राज्य में, हम उन सभी को काम देंगे’। कुछ सरकारों के मुखिया ने तो यहां तक कहा कि अगर बाहर के राज्य श्रमिक चाहते हैं तो उन्हें यहां की सरकार से इजाजत लेनी होगी। इन बयानों के पीछे केवल राजनीतिक हित है, वर्ना क्या इन्हें मालूम नहीं कि रोजगार पाने की स्थिति रहती तो ये गरीब सैकड़ों किलोमीटर दूर रोटी की तलाश में जाते ही क्यों? शायद इनकी अर्थशास्त्र की समझ थोड़ी कम है। रोजगार के अवसर तथा औद्योगिक वातावरण तैयार करने में दशकों लग जाते हैं। हां, अगर ये सरकारें वाकई संजीदा हैं तो कुछ महीनों के लिए ये कृषि और संलग्न क्षेत्रों में उपलब्ध लचीलेपन का इस्तेमाल कर इन मजदूरों को लोन देकर भुखमरी से बचा सकती हैं। इससे कृषि और संबंधित उद्यमों में कुछ रफ़्तार आ सकती है। आर्थिक सिद्धांत के अनुसार अगर एक मजदूर की कृषि में उत्पादकता 1 रुपया है तो उसी मजदूर की उद्योग में उत्पादकता 3.5 और सेवा क्षेत्र में 4.2 रुपया हो जाती है। इसका कारण है उद्योग और सेवा क्षेत्र में निवेश। यही कारण है कि दीर्घकाल तक घर वापसी मजदूरों के लिए संभव नहीं है। दूसरा, इन सरकारों को यह भी मालूम होना चाहिए कि एक मजदूर देश में कहां जाए, कहां रहे और क्या व्यवसाय चुने, यह उसका संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (घ) (च) और (छ) के तहत मौलिक अधिकार है। अगर एक राज्य में मजदूर को केवल खेती के सीजन में 400 रुपए रोज मिलते भी हैं और बाकी दिन नहीं तो वह केरल में 700 रुपए रोजाना और साल के 365 दिन कमाने जाएगा ही। हां, केंद्र को इनके कल्याण के लिए श्रम कानून में बदलाव करना होगा, ताकि भविष्य में प्रतिलोम प्रवास जैसा संकट न पैदा हो।
Date:28-05-20
बेहिसाब, बेलगाम… विदेशी डिजिटल कंपनियां
विराग गुप्ता, सुप्रीम कोर्ट के वकील
पांच दशक पहले एक गाना बहुत मशहूर हुआ था। उसमें राज कपूर का जूता जापानी और टोपी रूसी थी, फिर भी हीरो का दिल हिंदुस्तानी था। वक्त बदल गया और अब करोड़ों हिंदुस्तानियों के दिलों पर डिजिटल ने कब्ज़ा कर लिया और विदेशी डिजिटल कंपनियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को टोपी पहनाना शुरू कर दिया। टोपी पहनाने के लिए सोशल मीडिया कंपनियों ने भारत के संचार-तंत्र पर और फिर ई-कॉमर्स कंपनियों ने 130 करोड़ लोगों के बाज़ार पर कब्ज़ा कर लिया। अब लॉकडाउन के संकट का फायदा उठाकर अमेज़न प्राइम और नेटफ्लिक्स जैसे ओटीटी प्लेटफार्म मनोरंजन के 2 बिलियन डॉलर के बाज़ार पर कब्जा करने की जुगत भिड़ा रहे हैं। OTT यानी ‘ओवर द टॉप’ की कंपनियां मनोरंजन के कार्यक्रम बनाने और उसके डिजिटल प्रसारण के धंधे में पिछले कई सालों से लगी हुई हैं। पिछले कई महीनों से मॉल और मल्टीप्लेक्स बंद हैं तो ओटीटी पर नई फिल्मों की रिलीज़ शुरू होने लगी है। फिल्मों का तीसरा सबसे बड़ा वैश्विक बाज़ार भारत में है। इससे लाखों लोगों को रोजगार के साथ सरकारों को टैक्स की बड़ी आमदनी होती है। फ़िल्में समाज को प्रभावित करने के साथ बच्चों को बेहतर नागरिक बनाने में मददगार होती हैं। इसी वजह से फिल्मों में अश्लीलता, हिंसा, शराब, ड्रग्स, पोर्न आदि को रोकने के लिए सेंसर बोर्ड की सख्त व्यवस्था बनाई गई है। पिछले कुछ महीनों से ओटीटी प्लेटफार्म्स में हसमुख और पाताललोक जैसे हिंसक और अश्लील कार्यक्रमों को बड़ों के साथ बच्चे भी मजे लेकर देख रहे हैं। रोटी-कपड़ा और मकान के बजाय भारत में बच्चों के लिए भी मोबाइल जरूरी बना दिया गया है। मोबाइल के माध्यम से डिजिटल कंपनियों का पूरा कारोबार चल रहा है। लॉकडाउन के संकट में लोगों को रोजगार के बजाय ई-कॉमर्स से शराब की होम डिलीवरी दी जा रही है। 130 करोड़ की आबादी वाले देश में डिमांड और सप्लाई लोकल है, लेकिन डिजिटल बाजार में विदेशी कंपनियां वोकल हैं।
गांव, कस्बे और जिलों में पुरानी तरह के हजारों सिनेमा हॉल बंद होकर मैरिज हॉल और मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स में तब्दील हो गए। अब ओटीटी की डिजिटल आंधी में जब मल्टीप्लेक्स भी बंदी के मुहाने पर हैं, तो उसे कौन रोक सकता है? बोस्टन कंसल्टेंसी की रिपोर्ट के अनुसार अगले 3 सालों में ओटीटी कंपनियों का भारत में पांच बिलियन डॉलर का बाज़ार हो जाएगा। टेक्नोलॉजी और विदेशी पूंजी की बड़ी ताकत से लैस ये कंपनियां बाज़ार में अपना एकाधिकार स्थापित करने में सफल हो रही हैं। विदेशी कंपनियों को कानून और टैक्स के दायरे से बाहर रहने की सहूलियत मिलने से भारतीय उद्योग दौड़ से बाहर हो रहे हैं। पिछले तीन महीनों में आपदा प्रबंधन कानून (डीएमए) के तहत श्रम, किराया और वेतन भत्तों के नियमों में बदलाव हो गए। ओटीटी कंपनियों के लिए कुछ महीने पहले एक निजी संस्था ने स्वैच्छिक कोड ऑफ़ कंडक्ट बनाया, पर अधिकांश कंपनियां किसी भी नियम के दायरे में नहीं आना चाहती हैं। सरकार यदि ओटीटी कंपनियों पर सेंसर बोर्ड के नियम और टैक्स व्यवस्था लागू करने में विफल हो रही है तो फिर परंपरागत सिनेमा कारोबारियों को भी सेंसर बोर्ड और टैक्स नियमों की जकड़न से मुक्ति क्यों नहीं मिलना चाहिए?
लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया भी लॉकडाउन के कठिन दौर की वजह से अनेक संकटों का शिकार हो गया है। ऑस्ट्रेलिया के प्रतिस्पर्धा आयोग ने संकट के मूल कारण को पहले ही पहचान लिया था। अखबारों की न्यूज़ से फेसबुक और गूगल जैसी कंपनियों को बड़ी आमदनी होती है। आयोग ने सोशल मीडिया कंपनियों से कहा है कि न्यूज़ से हो रही आमदनी को ऑस्ट्रेलियाई अखबारों के साथ शेयर करना होगा। भारत में अनेक भाषाओं में प्रकाशित होने वाले एक लाख से ज्यादा अखबार और पत्रिकाओं से लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। नियमों के अनुसार मीडिया के कारोबार में विदेशी कंपनियां भारत में सीधे तौर पर नहीं आ सकतीं। भारत में रजिस्टर्ड अखबार व टीवी मीडिया को जटिल नियमों का पालन करना होता है। दूसरी तरफ डिजिटल कंपनियां भारत से सालाना 20 लाख करोड़ से ज्यादा का कारोबार करने के बावजूद यहां के क़ानून व टैक्स के दायरे से अभी तक बाहर हैं। इन कंपनियों को जवाबदेह बनाने की बजाय लॉकडाउन के दौर में केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों को सरकारी विज्ञापन देने के लिए ड्राफ्ट गाइड लाइन बनाई है।
आज़ादी के बाद जब संविधान बना, तब न तो मोबाइल था और न ही इंटरनेट। संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार डिजिटल जैसे नए मामलों पर केंद्र सरकार को क़ानून बनाने और कार्रवाई का अधिकार मिला है। संघीय व्यवस्था में राज्यों के पास क़ानून और व्यवस्था का अधिकार होने के बावजूद, उन्हें विदेशी डिजिटल कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करने की शक्ति नहीं मिली। कोरोना के पीछे चीन और WHO की कोई साजिश है, इसकी जांच अब भारत के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्ष वर्धन के नेतृत्व में बेहतर तरीके से जरूर होगी। लेकिन, कोरोना के खौफ में कारोबार बढ़ाने वाली डिजिटल कंपनियों के नेटवर्क को भारत के कानून और टैक्स के दायरे में कब लाया जाएगा? डिजिटल इंडिया में आत्मनिर्भर भारत को सफल बनाने के लिए अब संसद, सरकार, अदालत और कैग को बड़ी भूमिका निभानी होगी।
![]() Date:28-05-20
Date:28-05-20
नाकामी का सबब ?
संपादकीय
लॉकडाउन के कड़े प्रावधानों के दौरान सरकार जिस माध्यम के जरिये गरीबों तक राहत पहुंचाना चाहती थी वह अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरा।
26 मार्च को सरकार ने कहा था कि जन धन बैंक खाता धारक महिलाओं को तीन महीने तक हर माह 500 रुपये की राशि दी जाएगी। यह राशि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज का हिस्सा थी और आशा की जा रही थी कि कोविड-19 महामारी का प्रसार रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन से ठप पड़ी अर्थव्यवस्था ने वंचित वर्ग के सामने जो दिक्कतें पैदा की हैं, उन्हें इससे कुछ राहत मिलेगी। बहरहाल 20 मई तक इस राशि की दो किस्तें जारी होने के बाद भी आधी से भी कम खाताधारक महिलाओं ने यह राशि खाते से निकाली। सरकार को इसकी जानकारी तब लगी जब ऐसे 20 करोड़ खातों पर नजर डाली गई।
यह बात चिंतित करने वाली है। इससे यह बात उजागर होती है कि देश की कल्याण व्यवस्था में कमियां हैं जिन्हें जल्द से जल्द दूर किए जाने की आवश्यकता है। परंतु इससे यह भी स्पष्ट होता है कि बहुचर्चित प्रत्यक्ष लाभ अंतरण व्यवस्था शायद अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरी। खासकर संकट के समय वह कारगर नहीं रही। महामारी जैसे आपातकालीन स्थिति में कम समय में जरूरतमंदों तक पहुंचने का यह तरीका संतोषजनक साबित नहीं हुआ। यह स्पष्ट नहीं है कि आखिर उक्त खातों का इस्तेमाल क्यों नहीं हुआ। शायद लोग लॉकडाउन के कड़े प्रावधान के बीच एटीएम नहीं जा पाए होंगे या शायद पैसा उन लोगों के पास नहीं पहुंचा जिनको उसकी वाकई अत्यधिक आवश्यकता थी। यह स्पष्ट है कि भारत को आम परिवारों का बेहतर खाका रखने और उन्हें समझने की आवश्यकता है। ऐसी कल्याण योजना जो सूचना के अभाव में काम करती है वहां उसे जुड़े लोगों को कभी समुचित तरीके से नहीं समझा जा सकता। ऐसा नहीं है कि कल्याण व्यवस्था केवल ग्रामीण गरीबों को देख पाने में नाकाम रही बल्कि शहरी गरीब और आंतरिक प्रवासी भी इसे लेकर बेहद संवेदनशील हैं क्योंकि उन तक पहुंच के पर्याप्त साधन नहीं हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि कल्याण योजनाओं पर व्यय बढ़ाने के कई सुविचारित सुझाव भी शायद वास्तव में मददगार न साबित हों। केवल पैसे डाल देने से समस्या हल नहीं होती है बल्कि उसे जरूरतमंदों तक पहुंचना भी चाहिए।
प्राथमिकताओं में संतुलन कायम करना अहम है। हम प्रत्यक्ष लाभ अंतरण की संभावनाओं को शून्य नहीं कर सकते। परंतु यह भी स्पष्ट है कि मौजूदा हालात जैसे वक्त में राशन और पके खाने जैसी चीजें ज्यादा मददगार हैं। ऐसे में इस तरह की राहत मुहैया कराने वाली योजनाओं को पूरी तरह बंद नहीं किया जाना चाहिए। यह भी आवश्यक है कि लाभ की सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने और उसका हस्तांतरण संभव बनाने की कोशिश होनी चाहिए। उदाहरण के लिए एक देश, एक राशन कार्ड की योजना यह सुनिश्चित करने में मदद कर सकती है कि प्रवासी श्रमिक अपना राशन दूर देश में बैठे अपने परिवार के साथ साझा कर सकें।
यह सही है कि सरकार ने महामारी के दौरान योजना से जुड़ी दिक्कतों को उजागर किया था। उदाहरण के लिए राशन की दुकानों में ऐसी प्वाइंट ऑफ सेल मशीनें ज्यादा नहीं हैं जो चालू हालत में भी हों। बहरहाल इन समस्याओं को हल किया जा सकता है। सबसे महत्त्वपूर्ण है यह समझना कि कल्याण योजनाओं के लाभार्थी कौन हैं। ग्रामीण भूमिहीन, महिलाएं, शहरी गरीब और प्रवासी आदि वंचित वर्गों को उनकी जगह और आंकड़ों के साथ कल्याण योजनाओं में शामिल करना होगा।
Date:28-05-20
आर्थिक पैकेज से निजी क्षेत्र को मिलेगा काफी कुछ
ए के भट्टाचार्य
सरकार ने कोविड-19 महामारी के चलते आर्थिक पैकेज की घोषणा करते समय निजी क्षेत्र पर जितना जोर दिया, उसकी कोई भी अनदेखी नहीं कर पाया होगा। करीब एक सप्ताह पहले पांच किस्तों में 21 लाख करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा की गई ताकि कोविड-19 के झटके से अर्थव्यवस्था को उबारा जा सके। इस पैकेज में नीतिगत बदलावों की पर्याप्त खुराक थी, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र की भूमिका बढ़ाई जा सके।
इसके तहत एक नई सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम नीति की घोषणा की गई ताकि सरकारी स्वामित्व वाले उद्यमों की भूमिका केवल सरकार द्वारा परिभाषित रणनीतिक क्षेत्रों तक सीमित की जा सके। यहां तक कि रणनीतिक क्षेत्रों में भी चार से अधिक सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को चलने की मंजूरी नहीं दी जाएगी। जल्द ही रणनीतिक क्षेत्रों की एक सूची तैयार की जाएगी। इस समय गैर-रणनीतिक क्षेत्रों में मौजूद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों का एक निश्चित समयावधि में निजीकरण किया जाएगा।
मार्च 2019 के अंत में सार्वजनिक क्षेत्र के केंद्रीय उद्यम (सीपीएसई) 339 थे, जिनमें कुल निवेश 16.4 लाख करोड़ रुपये था। उनका कुल शुद्ध लाभ महज 1.42 लाख करोड़ रुपये था। इनमें 70 से अधिक सीपीएसई को 2018-19 में करीब 31,600 करोड़ रुपये का कुल घाटा हुआ था। कुल सीपीएसई में 56 स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध थे और उनका बाजार पूंजीकरण घट रहा है। उनका बाजार पूंजीकरण मार्च 2019 के अंत में घटकर 13.7 लाख करोड़ रुपये पर आ गया था और इसमें पिछले कुुछ महीनों के दौरान निश्चित रूप से और गिरावट आई होगी। मगर उनके रिजर्व एवं सरप्लस 9.93 लाख करोड़ रुपये और नेट वर्थ 12 लाख करोड़ रुपये है। सरकार ने शेयरधारक के रूप में इन सीपीएसई से 2018-19 में 72,000 करोड़ रुपये का लाभांश अर्जित किया।
अगर रणनीतिक क्षेत्रों में परिचालित कुछ सीपीएसई को छोड़कर अन्य को आगामी एक-दो साल में बिक्री के लिए पेश किया गया तो भारत में निजी क्षेत्र के सामने इतने अच्छे विकल्प होंगे कि उसके लिए किसी एक का चयन करना कठिन होगा। यह भी सही है कि इन सीपीएसई में से कुछ की मौजूदा वित्तीय स्थिति एवं लाभप्रदता को देखते हुए उनके बहुत अधिक लिवाल नहीं होंगे। मगर फिर भी बहुत से सीपीएसई निजी क्षेत्र के खरीदारों के लिए बहुत अधिक आकर्षक रहेंगे। निजी क्षेत्र इन सीपीएसई को खरीदने के लिए पर्याप्त पूंजी के अभाव की शिकायत कर सकता है। मगर वे ऐसे अधिग्रहणों की खातिर बोली लगाने के लिए किसी विदेशी कंपनी से गठजोड़ सकते हैं या विदेशी बाजारों से पूंजी जुटा सकते हैं। कुल मिलाकर अगर योजना के मुताबिक नई सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम नीति को लागू किया गया तो इसके सामने 1990 के दशक के आखिरी वर्षों में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर किया गया निजीकरण भी फीका पड़ जाएगा।
कोविड-19 पैकेज में कुछ और ऐसे नीतिगत बदलाव हैं, जिनका मकसद भारतीय अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र की भूमिका बढ़ाना है। अब निजी क्षेत्र की कंपनियों को देश के उस अंतरिक्ष कार्यक्रम में अपनी पैठ बढ़ाने की मंजूरी दी जाएगी, जो अब तक भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) और उसकी सरकार के स्वामित्व वाली इकाइयों के लिए आरक्षित था। केंद्र शासित प्रदेशों में विद्युत वितरण कंपनियों का भी निजीकरण किया जाएगा।
जब सरकार सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के तहत छह हवाई अड्डों के विकास को मंजूरी देगी तो निजीकरण और बढ़ेगा। विमानन कंपनियों को अपने विमान उड़ाने के लिए और हवाई क्षेत्र मुहैया कराया जाएगा। आयुध निर्माणी बोर्ड के तहत आने वाली 41 फैक्टरियों का निगमीकरण किया जाएगा। इससे वे स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध हो सकेंगी और उनके परिचालन में निजी क्षेत्र की पूंजी की भागीदारी बढ़ेगी। इन फैक्टरियों में 80,000 से अधिक कामगार हैं। ये हर साल 5 लाख करोड़ रुपये से अधिक कीमत के बहुत से हथियारों एवं रक्षा उपकरणों का उत्पादन कर रही हैं।
यह भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर मोदी सरकार के नजरिये में अहम बदलाव है। मोदी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल के शुरुआती वर्र्षों में औद्योगिक परियोजनाओं के लिए जमीन अधिग्रहण पर प्रतिबंधों को ढीला करने की कोशिश की थी मगर वह कड़े राजनीतिक विरोध के कारण इस मुहिम में सफल नहीं हो सकी। तभी से मोदी सरकार ऐसे किसी कदम से बच रही है, जिसे बड़े उद्यमों को लाभ पहुंचाने के रूप में देखा जाए। इस सरकार के नजरिये में बदलाव का पहला संकेत सितंबर 2019 में दिखा, जब इसने भारतीय कंपनियों के लिए बड़ी कर रियायत की घोषणा की। कंपनियों के लिए निगम कर की दर घटाकर 25 फीसदी कर दी गई, बशर्ते कि वे अन्य छूट नहीं लेती हैं। अब कोविड-19 पैकेज में ऐसे कई कदम उठाए गए हैं, जो अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र को बड़ी भूमिका देते हैं।
मगर फिर भी निजी क्षेत्र सरकार द्वारा करीब एक सप्ताह पहले घोषित पैकेज के उपायों से नाखुश है। इसकी वजह यह तथ्य हो सकता है कि पैकेज में सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उपक्रमों (एमएसएमई) को छोड़़कर किसी भी क्षेत्र विशेष के लिए राहत के प्र्रावधान नहीं किए गए। इस निराशा की एक वजह यह भी है कि न उद्योग को और न ही व्यक्तिगत करदाताओं को कोई कर रियायत दी गई।
मगर जैसा कि पहले बताया गया है कि यह कहना गलत होगा कि इस पैकेज में निजी क्षेत्र को कुछ नहीं मिला। यह हो सकता है कि उद्योग को कर लाभ नहीं मिले हों। मगर इस सुधार पैकेज में ऐसी कई चीजें हैं जो निजी क्षेत्र को वे नए अवसर मुहैया कराती हैं जिनके लिए वह वर्षों से इंतजार कर रहा है। निजी क्षेत्र को कर लाभ नहीं होने का दुखड़ा रोने के बजाय यह मांग करनी चाहिए कि करीब एक सप्ताह पहले घोषित इस पैकेज के उपायों को जल्द लागू किया जाए।
Date:28-05-20
भारत का अपना ‘न्यू डील’ पल
विनायक चटर्जी , (लेखक फीडबैक इन्फ्रा के चेयरमैन हैं)
कोविड संकट के कारण उत्पन्न मौजूदा परिस्थितियों पर की जा रही तमाम आर्थिक टिप्पणियों में विंस्टन चर्चिल की मशहूर उक्ति ‘किसी भी संकट को कभी व्यर्थ न जाने दो’ की आजकल अक्सर चर्चा हो रही है। लेकिन इसमें यह महत्त्वपूर्ण संदेश भी निहित है कि ऐसे चुनौतीपूर्ण हालात में आदर्श रूप से नीति-निर्माताओं को परंपरागत समझ से बाहर आकर मौजूदा समय के लिहाज से प्रासंगिक एकदम नए तरह के समाधान लेकर आने चाहिए।
अरबों रुपये का सवाल यह है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को एक ब्लैक होल में तब्दील होने से बचाने के लिए सही मायने में कितने बड़े राहत पैकेज की दरकार है? सरकार के समक्ष रखे गए तमाम सुझाव ‘राहत पैकेज के मुख्य घटक’ तालिका में दिए गए हैं।
करीब 30 लाख करोड़ रुपये का अनुमानित पैकेज देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का करीब 14 फीसदी है। मौजूदा समय में भारतीय अर्थव्यवस्था को इतने बड़े स्तर पर हस्तक्षेप की जरूरत है। इससे साफ जाहिर होता है कि परंपरागत तौरतरीकों पर आगे बढऩे से किसी भी तरह की बात नहीं बनने वाली है।
अब सवाल यह खड़ा होता है कि 30 लाख करोड़ रुपये का बंदोबस्त कहां से किया जा सकता है? मेरे हिसाब से इसके लिए संसाधन इस तरह जुटाए जा सकते है:
► केंद्रीय बजट के राजकोषीय घाटे को बढ़ाकर चार फीसदी राशि जुटाई जा सकती
► राष्ट्रीय नवीकरण-प्रथम चरण (अक्टूबर 2020 तक) का सृजन कर पांच फीसदी राशि जुटाई जाए
► राष्ट्रीय नवीकरण- द्वितीय चरण (नवंबर 2020 से मार्च 2021 तक) के माध्यम से पांच फीसदी राशि का इंतजाम किया जाए
इस समाचार पत्र में पिछले महीने प्रकाशित अपने लेख में मैंने कहा था कि राष्ट्रीय नवीकरण कोष (एनआरएफ) अपने आप में एक ऐतिहासिक पहल होगी। यह काफी हद तक रूजवेल्ट की तरफ से 1930 के दशक में लाए गए ‘न्यू डील’ कार्यक्रम या द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद यूरोप के पुनर्निर्माण के लिए लाए गए ‘मार्शल प्लान’ जैसा होगा।
एनआरएफ 50 वर्षों के लिए गठित एक कोष होगा जिसमें पहले 10 वर्षों के लिए पुनर्भुगतान पर रोक होगी। उसके बाद सभी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष करों या दूसरे रचनात्मक साधनों पर 1-2 फीसदी उपकर लगाकर इस फंड को धीरे-धीरे बढ़ाया जा सकता है। (क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के साथ अनौपचारिक चर्चा में यह संकेत मिला है कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए वे भी एक विश्वसनीय पहल के तौर पर इस नई सोच वाली योजना का स्वागत कर सकती हैं।)
एनआरएफ के लिए 60 फीसदी वित्त का इंतजाम सरकार घरेलू बाजार से उधारी जुटाकर कर सकती है। और बाकी 40 फीसदी राशि की व्यवस्था अंतरराष्ट्रीय बाजार से मित्रवत रुख रखने वाले विकास वित्त संस्थानों के जरिये किया जा सकता है। कुछ उसी तरह जैसे बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए जापान से 0.5 फीसदी ब्याज पर 60 वर्षों के लिए एक लाख करोड़ रुपये जुटाए गए हैं।
लेकिन हमें ध्यान रखना होगा कि इस दिशा में आधे-अधूरे प्रयासों का कोई फायदा नहीं होने वाला है। 1930 के शुरुआती वर्षों में छाई महान आर्थिक मंदी ने रूजवेल्ट के न्यू डील कार्यक्रम के लिए बुनियाद तैयार की थी जिसमें बड़े पैमाने पर किए गए लोक निर्माण एवं वित्तीय सुधार कार्यक्रमों के प्रभाव अमेरिकी अर्थव्यवस्था को आने वाले कई दशकों तक महसूस होते रहे। लिहाजा एनआरएफ में मुख्य रूप से जोर एक बेहद असरदार लोक निर्माण कार्यक्रम चलाने पर दिया जाना चाहिए। इसके दायरे में उन परियोजनाओं को रखा जाना चाहिए जो भारत के दूरदराज के इलाकों में बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा कर सकें।
लेकिन हम किस तरह का लोक निर्माण कार्यों की बात कर रहे हैं ?
► ये परियोजनाएं ऐसी हों जो बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा करने के साथ ही स्थायी परिसंपत्ति का निर्माण करे और उनका बहुस्तरीय प्रभाव भी हो।
► स्वास्थ्य ढांचे को नए सिरे से गठित करने की जरूरत- अगर कोविड ने कोई एक काम किया है तो वह यह है कि किसी देश में स्वास्थ्य ढांचे की स्थिति वहां के लोगों की जिंदगी और मौत का फर्क पैदा कर सकती है।
► वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं में होने वाले बदलाव से फायदा उठाने का मौका- कोविड महामारी से उबरने के बाद की दुनिया में कंपनियां अपने विनिर्माण एवं वैल्यू चेन गतिविधियों को चीन से हटाकर किसी और देश में ले जाकर अपना जोखिम कम करने की सोच रही हैं। ऐसे में भारत के लिए इस निवेश का कुछ हिस्सा अपने यहां आकर्षित करने का एक बढिय़ा मौका है।
इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए मेरी राय में ये पांच तरह के लोक निर्माण कार्यक्रम कारगर हो सकते हैं:
तटीय आर्थिक क्षेत्र (सीईजेड): सागरमाला परियोजना में अंतरराष्ट्रीय जहाजरानी से करीबी संपर्क रखने वाले अत्यधिक एकीकृत लॉजिस्टिक एवं विनिर्माण केंद्र बनाने के लिए ऐसे 14 क्षेत्रों की पहचान की गई थी। ये परियोजनाएं सरकार के लिए विदेशी पूंजी आकर्षित करने और निवेशकों के लिए चीन के बाहर वैकल्पिक निवेश गंतव्य की तलाश का मकसद पूरा करते हैं। सीईजेड को विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) का उन्नत संस्करण होने के साथ ही भारत में कारोबार करने से जुड़ी सारी नकारात्मक बातों से दूर रखना चाहिए।
नदी संपर्क परियोजना: पानी की अधिकता वाली नदियों को कम पानी उपलब्धता वाली नदियों से जोडऩे का विचार कई दशकों से चर्चा में रहा है। इस तरह की विशाल परियोजना के पारिस्थितिकी एवं पर्यावरणीय प्रभावों को लेकर पुरजोर तर्क दिए जाते रहे हैं लेकिन यह भी साफ है कि आने वाले दशकों में बढ़ते शहरीकरण एवं वृद्धि को देखते हुए पानी की मांग में होने वाली खासी बढ़ोतरी को पूरा करने के लिए जल ढांचागत क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश की जरूरत है। भारत न्यू डील परियोजना के तहत अमेरिका में नदियों को जोडऩे के लिए बनाए गए टेनेसी वैली प्राधिकरण की तर्ज पर अपने कदम आगे बढ़ा सकता है।
राज्यों की नई राजधानियों का निर्माण: कोविड संकट ने बड़े महानगरों को बुरी तरह प्रभावित किया है। इससे बड़े शहरी क्षेत्रों का विखंडन और शहरी वृद्धि का बड़े शहरों के बाहर भी फैलाव एक अच्छे विचार के तौर पर सामने आया है। यह न केवल स्वास्थ्य के लिहाज से बल्कि क्षेत्रों के बीच आर्थिक असमानता कम करने के लिहाज से भी अच्छा है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार और कर्नाटक जैसे राज्यों में अगर नई राजधानियों का निर्माण होता है तो ये दोनों ही मकसद पूरा होंगे।
नल से जल: वर्ष 2024 तक सबको जलापूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार की तरफ से लाई गई यह परियोजना भी सफलतापूर्वक क्रियान्वित होने की स्थिति में ऐसा असर डालेगी कि दशकों तक उसे महसूस किया जाता रहेगा।
नए एम्स अस्पताल: दिल्ली का अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) नेहरू काल में बनाया गया था लेकिन इतने वर्षों बाद भी स्वास्थ्य सुविधा के मामले में वही अस्पताल शिखर पर है। समय आ गया है कि एम्स अस्पताल के निर्माण की सोच को दिल्ली के बाहर भी विस्तार दिया जाए और देश भर में ऐसे 22 अस्पतालों के निर्माण का प्रस्ताव तेजी से अमल में लाया जाना चाहिए। यह एक ऐसी परियोजना है जो कम कीमत पर स्तरीय स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने की कोरोना-पश्चात जरूरत के लिहाज से भी अनुकूल है।
यह निश्चित रूप से इतिहास में भारत का अपना ‘न्यू डील’ वाला अहसास है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मई को जीडीपी के 10 फीसदी हिस्से के बराबर 20 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज की घोषणा कर इस मौके को दोनों हाथों से लपकने की कोशिश की है।
मंदी का दुश्चक्र
संपादकीय
भारत की अर्थव्यवस्था एक बार फिर भयंकर मंदी के दुश्चक्र में फंस गई है। हालात की गंभीरता बता रही है कि आने वाला वक्त और संकटपूर्ण होगा। इस वक्त जिस तरह के हालात बन गए हैं, उनसे निपटने में केंद्र और राज्य सरकारों के हाथ-पैर फूल रहे हैं। अर्थशास्त्री परेशान हैं, कुछ सूझ नहीं रहा कि मंदी से कैसे निकला जाए। हालांकि पिछले पांच महीनों में रिजर्व बैंक और केंद्र सरकार ने पैकेज घोषित तो किए हैं, लेकिन वे इस वक्त ऊंट के मुंह में जीरे से ज्यादा साबित हो नहीं रहे। इस बार क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने जो आकलन व्यक्त किया है, उसके मुताबिक चालू वित्त वर्ष में अर्थव्यवस्था शून्य से पांच फीसद नीचे जा सकती है। अगर ऐसा हुआ, जैसे कि हालात दिख भी रहे हैं, तो आने वाले तीन-चार साल तक भारत इस संकट से उबर नहीं पाएगा। इससे पहले फिच और मूडीज का आकलन भी कमोबेश यही रहा है।
इसमें कोई संदेह नहीं कि पिछले दो महीने के दौरान देश में पूर्णबंदी जारी रहने से अर्थव्यवस्था को भारी धक्का पहुंचा है। किसी भी देश में अगर दो महीने तक औद्योगिक गतिविधियों को एकदम ठप कर दिया जाए तो इससे होने वाले नुकसान का आकलन कर पाना कठिन नहीं है। उसके गंभीर नतीजे ही बताते हैं कि क्या से क्या हो गया। भारत में पूर्णबंदी के दौरान रेल, हवाई सेवाएं, सभी तरह के सार्वजनिक और निजी परिवहन सब बंद रहे। कोयला, बिजली, पेट्रोलियम, सीमेंट जैसे प्रमुख क्षेत्रों में उत्पादन ठहर गया। रियल एस्टेट से लेकर सारे छोटे-बड़े कारखाने, फैक्ट्रियों में कोई काम नहीं हुआ, यानी जरूरी सेवाओं को छोड़ कर कहीं कोई उत्पादन नहीं हुआ। इसका दूसरा खौफनाक पक्ष यह रहा कि काम बंद होते ही ज्यादातर नियोक्ताओं ने कामगारों की छुट्टी कर दी। संगठित क्षेत्र में छंटनी और भारी वेतन कटौती का दौर जारी है। जबकि पूर्णबंदी का ऐलान करते वक्त प्रधानमंत्री ने नियोक्ताओं से ऐसा नहीं करने की अपील की थी। असंगठित क्षेत्र के कामगारों की दुर्दशा पूरी दुनिया देख रही है।
भले कहा जा रहा हो कि हालात कोविड-19 की वजह से खराब हुए हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि भारत में आर्थिक गिरावट का दौर पिछले दो साल से बना हुआ है। पूर्णबंदी की वजह से तो पर्यटन, नागरिक उड्डयन, मनोरंजन, रियल एस्टेट, आटो मोबाइल उद्योग जैसे कई प्रमुख क्षेत्र जो बड़े पैमाने पर रोजगार देते हैं, लड़खड़ा गए हैं। सरकार कह रही है कि छोटे और मझौले उद्योगों को बिना किसी गारंटी के कर्ज दिया जाएगा। बाजार में पैसा डालने के लिए रिजर्व बैंक बार-बार रेपो और रिवर्स रेपो दर में कटौती कर रहा है, ताकि बैंक कर्ज और सस्ता करें। लेकिन कर्ज लेने वाले नहीं हैं। सब अनिश्चितता के खौफ से घिरे हैं। बैंक कर्ज सस्ता होने का एक असर यह भी पड़ रहा है कि सावधि जमा पर भी ब्याज दरें काफी गिर गई हैं। ऐसे में जिन लोगों की आमद का एकमात्र साधन बैंक में जमा रकम से अर्जित ब्याज होता है, उनके सामने भी मुश्तकिलें खड़ी होने लगी हैं। मंदी की मार चौतरफा है। राज्य सरकारों का राजकोषीय घाटा तेजी से बढ़ रहा है। अर्थशास्त्रियों की ओर से सुझाव यह भी आ रहे हैं कि सरकार को राजकोषीय घाटे की चिंता छोड़ मौद्रीकरण के रास्ते पर चलना चाहिए। बेहतर हो कि अब सरकार दलगत राजनीति से ऊपर उठ कर प्रमुख अर्थशास्त्रियों की टीम बनाए और मंदी से निकलने के लिए जो उपाय बताए जाएं, उन पर ईमानदारी से काम हो।
चीन तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है
शशांक, पूर्व विदेश सचिव
भारत और चीन का सीमा-विवाद एक बार फिर सतह पर आ गया है। पूर्वी लद्दाख में कई जगहों पर तनातनी इसलिए बढ़ गई है, क्योंकि पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (चीन की सेना) के सैनिक वास्तविक नियंत्रण रेखा पार करके भारतीय सीमा में घुस आए हैं। गैलवान नदी घाटी में विशेष तनाव दिख रहा है। आखिर चीन की सेना इस तरह घुसपैठ क्यों कर रही है? ऐसा करने के पीछे उसका मकसद क्या है? इसके बारे में फिलहाल बीजिंग की तरफ से आधिकारिक बयान का इंतजार है, लेकिन चीन के इस दुस्साहस की कई वजहें हो सकती हैं।
सबसे बड़ा कारण तो कोरोना वायरस के जन्म का खुलासा करने को लेकर चीन पर बढ़ता वैश्विक दबाव है। दरअसल, भारत ने पिछले दिनों विश्व स्वास्थ्य संगठन में कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष का पद संभाला है। जिस विश्व स्वास्थ्य महासभा में भारत को यह जिम्मेदारी सौंपी गई, उसने यह भी फैसला लिया कि कोरोना वायरस के जन्म की हकीकत एक स्वतंत्र जांच कमेटी पता लगाएगी। चीन इस पर सहमत तो हो गया है, लेकिन जिस तरह से विश्व स्वास्थ्य संगठन में ऐसी किसी स्वतंत्र जांच से जुड़े नियम नरम किए गए हैं, उससे तो यही लगता है कि बीजिंग खुले दिल से विश्व स्वास्थ्य महासभा के फैसले के साथ नहीं है। अब चूंकि यह तय है कि कोरोना वायरस का सच खोजा जाएगा और यह पता करने की कोशिश होगी कि चीन से शुरू होने के बावजूद इस वायरस का प्रकोप यूरोप और अमेरिका में ज्यादा क्यों दिखा, इसको लेकर बीजिंग तनाव में है। संभव है, इसी खुन्नस में वह सीमा-विवाद को हवा देकर भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा हो।
मौजूदा तनातनी की एक वजह चीन की महत्वाकांक्षी परियोजना ‘बेल्ट रोड इनीशिएटिव’ का भारत द्वारा विरोध भी हो सकती है। हालांकि, तमाम वैश्विक ताकतें भी चीन की इस मंशा के खिलाफ हैं। इस परियोजना के तहत चीन कई देशों में बुनियादी ढांचे का निर्माण कर रहा है, लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर देश इसकी भारी कीमत चुका रहे हैं। चीन बेशक निर्माण-कार्यों में इन देशों की आर्थिक मदद करता है, लेकिन कर्ज न चुका पाने की स्थिति में चीनी कंपनियां वहां प्रशासनिक नियंत्रण हासिल कर लेती हैं। रणनीतिक तौर पर श्रीलंका का महत्वपूर्ण हंबनटोटा बंदरगाह इसका एक बड़ा उदाहरण है, जिस पर फिलहाल 99 वर्षों के लिए बीजिंग का नियंत्रण हो गया है।
तीसरा कारण चीन का यह आंकना हो सकता है कि भारत किस हद तक उसका प्रतिरोध करने में सक्षम है। चीन जहां-तहां अपना बल दिखाता रहा है। दक्षिण चीन सागर में तो वह कृत्रिम द्वीप तक बना चुका है और किसी बाहरी ताकत की सागर में आवाजाही बाधित करता रहा है। पिछले वर्ष ‘फ्रिडम ऑफ नेविगेशन’ के तहत जब अमेरिका ने यहां अपने जहाज भेजे थे, तब चीन ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई थी। ऐसा करने के लिए बीजिंग अपने पड़ोसी देशों की चिंताओं पर भी ध्यान नहीं देता। दक्षिण चीन सागर में चीन के बढ़ते हस्तक्षेप के खिलाफ तो फिलीपींस संयुक्त राष्ट्र न्यायाधिकरण भी गया था, जहां उसे जीत मिली थी और दक्षिण चीन सागर में चीन के एकाधिकार को खारिज कर दिया गया था। मगर बीजिंग ने दबाव बनाकर फिलीपींस को इस बात के लिए राजी कर लिया कि वह द्विपक्षीय तरीके से विवाद का निपटारा करेगा।
चूंकि भारत की नजदीकी इधर अमेरिका से बढ़ गई है, ऐसे में इंडो पैसिफिक यानी हिंद और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाले भौगोलिक हिस्से में नई दिल्ली को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। क्वाड (भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान का सामरिक समूह) में प्रगति हुई है और इसमें अब विदेश मंत्री स्तर पर बातचीत होने लगी है। इसीलिए भारत के बढ़ते रुतबे को चोट पहुंचाने की कोशिशों में चीन जुटा हुआ है। अपनी इसी मंशा के तहत वह अनेक एशियाई देशों पर दबाव बनाकर भारत को घेरने का प्रयास कर रहा है। पिछली नेशनल पीपुल्स कांग्रेस (राज्य सत्ता के सर्वोच्च अंग की बैठक) में बीजिंग ने 2050 तक दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य, आर्थिक और तकनीकी ताकत बनने का लक्ष्य तय किया है। इसीलिए मौजूदा राष्ट्रपति शी जिनपिंग का कद कई मामलों में चीन में साम्यवादी विचारधारा के संस्थापक माओत्से तुंग से बड़ा कर दिया गया है। चूंकि एशिया में चीन की राह सिर्फ भारत रोक सकता है, इसलिए जुबानी तौर पर साथ-साथ चलने की बात करने के बावजूद बीजिंग नई दिल्ली पर दबाव बनाने का कोई मौका छोड़ना नहीं चाहता।
अभी लद्दाख में जिन निर्माण-कार्यों के ऊपर मौजूदा विवाद का ठीकरा फोड़ा जा रहा है, उस पर तो भारत ने करीब दशक भर पहले अपना काम शुरू कर दिया था। हिमालय की विशाल पर्वत शृंखलाओं की वजह से लद्दाख के सीमावर्ती इलाकों तक पहुंच बनाने के लिए भारत ने बहुत पहले से यहां बुनियादी ढांचे और सड़कें आदि बनाने शुरू कर दिए थे। यह इसलिए भी जरूरी था, क्योंकि सीमा पर तैनात हमारे सैनिकों को वक्त पर रसद आदि मिल सके। चीन ने इसे पहले तवज्जो नहीं दी थी, लेकिन अब वह भारत के विरोध की सीमा को जांचना चाहता है। इसलिए इसे डोका ला विवाद की अगली कड़़ी भी कहा जा सकता है।
सवाल यह भी है कि आखिर चीन के साथ हमारा सीमा-विवाद क्यों बना हुआ है? उल्लेखनीय है कि दोनों देश करीब 3,500 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं। मैकमोहन रेखा अनौपचारिक तौर पर भारत और चीन को बांटती है, लेकिन तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश के बीच चीन इसे नहीं मानता। भारत जहां इन इलाकों पर अपना दावा छोड़ने को तैयार नहीं है, वहीं अक्साई चिन को भी नई दिल्ली अपना हिस्सा मानती है। अच्छी बात है कि सन 1962 के अलावा कभी भी दोनों देश इसके लिए जंग के मैदान में आमने-सामने नहीं आए हैं। चूंकि सीमांकन का काम अंतिम रूप से अब तक नहीं हुआ है, इसलिए दोनों देशों के सैनिक एक-दूसरे के इलाकों में आते-जाते रहे हैं। मगर बीच-बीच में यह तनाव इसलिए गहरा जाता है, क्योंकि चीन किसी न किसी योजना के तहत सीमा-विवाद को हवा देता है। तो क्या इस बार उसकी मंशा लद्दाख के सीमावर्ती इलाकों को अपने कब्जे में लेने की है? उम्मीद है, पहले की तरह इस बार भी उसकी मंशा जल्द स्पष्ट हो जाएगी।