
27-10-2021 (Important News Clippings)
To Download Click Here.
 Date:27-10-21
Date:27-10-21
Baby Steps Won’t Do
Wide state-level variances in infant mortality rate show where India’s going wrong on this key goal
TOI Editorials
Infant mortality rate (IMR) is a keenly tracked measure of public health. It’s seen as a proxy for both overall health of a society and healthcare quality. GoI’s annual sample registration survey (SRS) is a demographic survey that tracks changes in IMR. In 2019, India’s IMR was 30 infant deaths per 1,000 live births. It represents not just an annual improvement but also a better performance compared to the IMR of 50 in 2009. Yet, the situation is not satisfactory in this most vital of indicators.
Higher incomes often translate into improvements on many counts. In IMR, however, there’s no evidence of a tight link between the two. For instance, Nepal with just over half of India’s per capita GDP, has a lower IMR. Sri Lanka’s IMR is close to that of EU at a fraction of the per capita income. If it’s not income, neither is state capacity a watertight indicator. Iraq, Syria and Libya, three countries where state capacity has been undermined by civil war, do better than India. The answer may lie in the starkly uneven performances of India’s states.
Mizoram and Nagaland, the two standout performers with the IMR level of Scandinavia, do far better than states such as Haryana which have a much higher per capita income. The pattern repeats itself. Bihar has recorded a noteworthy improvement over a decade and its 2019 IMR of 29 was lower than the national average. UP and MP are outliers, performing poorly, with the latter’s IMR of 46 being worse than war-torn Yemen. The key appears to be a state’s political culture, which influences policy priorities. On this most basic of health indicators, India has a moral and policy imperative to do far better.
Preparing For Outbreaks
The Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission aims to build a robust public health infrastructure
Bharati Pravin, [ The Union Minister of State for Health and Family Welfare ]
COVID-19 overburdened the country’s health system and services. The early months of the outbreak were particularly taxing for the States with weaker health systems. The inability of the private sector to share the burden drove the point home that healthcare services cannot be left to independent forces.
Aims of ABHIM
The Pradhan Mantri Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission (ABHIM) is another addition to the arsenal we have to prepare for such oubreaks in the future. This was launched with an outlay of ₹64,180 crore over a period of five years. In addition to the National Health Mission, this scheme will work towards strengthening public health institutions and governance capacities for wide-ranging diagnostics and treatment, including critical care services. The latter goal would be met with the establishment of critical care hospital blocks in 12 central institutions such as the All India Institute of Medical Sciences, and in government medical colleges and district hospitals in 602 districts.
The importance of laboratories and their lack of readiness during an outbreak in terms of having a robust surveillance system and diagnostic interface has never been more pronounced than in recent times. The government will be establishing integrated district public health labs in 730 districts to provide comprehensive laboratory services. The current labs for different programmes shall be integrated to deliver clinical, public health surveillance and diagnostic services for predicting outbreaks, epidemics, and more.
ABHIM will focus on supporting research on COVID-19 and other infectious diseases, including biomedical research to generate evidence to inform short-term and medium-term responses to such pandemics. The government also aims to develop a core capacity to deliver the ‘one health’ approach to prevent, detect, and respond to infectious disease outbreaks in humans and animals. The plan to achieve that bio-security preparedness and pandemic research strengthening would be realised via four regional National Institutes for Virology, the regional research platform for the World Health Organization Southeast Asia Region, and nine Biosafety Level III laboratories.
Boosting surveillance
In India’s endeavour to keep ahead of the infectious organisms that bring our life to a halt, expanding and building an IT-enabled disease surveillance system is on the cards too. A network of surveillance labs will be developed at the block, district, regional and national levels for detecting, investigating, preventing, and combating health emergencies and outbreaks.
Surveillance will get a huge boost with 20 metropolitan surveillance units, five regional National Centre for Disease Control branches, and an integrated health promotion platform in all the States. The points of entry will be reinforced with 17 new points of entry health units upgrading 33 existing units. The upgraded and intensified system of surveillance will be in addition to a state-of-the-art national digital health ecosystem for IT-enabled healthcare service delivery, for managing the core digital health data and for ensuring national portability in the provision of health services through a secure system of electronic health records. This will be based on international standards and easily accessible to citizens.
A major highlight of the current pandemic has been the requirement of local capacities in urban areas. The services from the existing urban primary health centres will be expanded to smaller units – Ayushman Bharat Urban Health and Wellness Centres and polyclinics or specialist clinics. The urban primary health centres will be established closer to the community to meet the needs of the urban population and polyclinics willguarantee care through improved access to expanded high-quality services and establish referral linkages.
सवालों के घेरे मे एक और वैश्विक रपट
ए. सूर्यप्रकाश, ( लेखक संवैधानिक मामलों के विशेषज्ञ एवं वरिष्ठ स्तंभकार हैं )
बीते दिनों ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी जीएचआइ, 2021 रिपोर्ट जारी की गई। कई पैमानों पर इसके निष्कर्ष संदिग्ध प्रतीत होते हैं। कथित तौर पर विश्व में भुखमरी की स्थिति को दर्शाने वाली इस रपट में भारत को पाकिस्तान, बांग्लादेश और अन्य दक्षिण एशियाई देशों से भी नीचे रखा गया। इस रपट को तैयार करने में जो पुराने आंकड़े और दोषपूर्ण प्रक्रिया अपनाई गई, उससे इस रपट पर सवाल उठने स्वाभाविक हैं। वैश्विक एवं क्षेत्रीय स्तर पर भुखमरी की स्थिति का पता लगाने के लिए यह रिपोर्ट चार बिंदुओं पर तैयार की गई। इनमें पहला बिंदु अल्पपोषण से जुड़ा है। दूसरा बिंदु चाइल्ड वेस्टिंग यानी लंबाई के अनुपात में कम वजन से संबंधित है।तीसरा बिंदु चाइल्ड स्टंटिंग यानी आयु के अनुसार कम लंबाई का है। चौथा बिंदु बाल मृत्यु दर का है। इन बिंदुओं का जुड़ाव पांच साल से कम आयु के बच्चों से है। इस रपट में भारत को 116 देशों में से 101वें स्थान पर जगह दी गई, जिसमें वह कई दक्षिण एशियाई देशों से भी नीचे है। इसमें भारत को 27.5 का स्कोर प्राप्त हुआ। वहीं 18 देश ऐसे हैं जिन्हें पांच से भी कम स्कोर मिला। इसमें कम स्कोर बेहतर प्रदर्शन माना जाता है। भारत पिछले वर्ष 94वें स्थान पर था, लेकिन इस साल फिसलकर 101वें पायदान पर पहुंच गया। उसकी तुलना में 65वें स्थान पर श्रीलंका, 76वें स्थान पर नेपाल और 92वें स्थान पर पाकिस्तान दिखाया गया।
जीएचआइ की रैकिंग में पांच वर्ष से कम आयु के जिन बच्चों के आंकड़े लिए गए, वे 2016 से 2018 के हैं। अब चाहे तस्वीर उससे बुरी हो या बेहतर, लेकिन वे आंकड़े मौजूदा जमीनी हकीकत को नहीं दर्शाते। इतना ही नहीं रपट तैयार करने में एफएओ के जिन आंकड़ों को आधार बनाया गया, उन्हें जुटाने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई गई, वह भी सवालों के घेरे में है।दरअसल, एफएओ के लिए ये आंकड़े गैलप नाम की संस्था ने टेलीफोन पर सर्वे के आधार पर तैयार किए। सर्वेक्षणकर्ताओं ने कोविड-19 के दौरान रोजगार की स्थिति, नौकरी या कारोबार में नुकसान जैसे सवाल भी पूछे। जबकि इस दौरान सरकार ने खाद्य उत्पादों की सुनिश्चित आपूर्ति के लिए एक व्यापक अभियान चलाया, लेकिन लोगों से यह पूछा ही नहीं गया कि क्या उन्हें खाद्य उत्पाद मिलते रहे। इस तथ्य में भी उतनी ही विसंगति है कि अल्पपोषण को वैज्ञानिक रूप से मापने के लिए लंबाई और वजन मापना आवश्यक है, लेकिन हंगर इंडेक्स मेंगैलप के फोन से हुए सर्वे पर ही भरोसा कर लिया गया।
विवादित पेच केवल इतने ही नहीं हैं।रैंकिंग में शुरुआती 18 देश वर्ष 2000 में 5 या 5.5 से कम वाले दायरे में थे, जिन्होंने अपनी स्थिति कायम रखी है। हालांकि, 2000 में जिस चीन का स्कोर 13.5 था, वह भी अब 5 से कम के दायरे में आ गया है। कहा जा रहा है कि कई वैश्विक संस्थाओं ने इस रैंकिंग के लिए आंकड़े जुटाए। ऐसे में क्या चीन के संदर्भ में इन आंकड़ों परभरोसा किया जा सकता है। विशेषकर इस बात को देखते हुए कि कोरोना की जांच को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी डब्ल्यूएचओ को धमकाना हो या फिर ईजआफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में विश्व बैंक को प्रभावित करना, दोनों ही मामलों में चीन की दबंगई से इन आंकड़ों की विश्वसनीयता भी संदेहास्पद हो जाती है। लिहाजा चीन द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों की गहन रूप से परख-पड़ताल की जानी चाहिए थी, क्योंकि जब डब्ल्यूएचओ कोरोना की जांच को लेकर चीन के झांसे में आ सकता है तब हंगर इंडेक्स के लिए उसके आंकड़ों पर कैसे भरोसा किया जा सकता है?
ग्लोबल हंगर इंडेक्स भी अतीत में आई वैश्विक संस्थानों की उन तमाम रिपोर्ट के ही ढर्रे पर है, जो भारत की गलत तस्वीर पेश करती रही हैं। हंगर इंडेक्स तैयार करने में हुई गड़बड़ियां पेरिस के रिपोर्टर्स विदाउट फ्रीडम के प्रेस फ्रीडम इंडेक्स और स्वीडिश एजेंसी वी-डेम द्वारा पेश की गई डेमोक्रेसी रिपोर्ट, 2020 की याद दिलाती हैं। उक्त रपट में भारत से बेहतर ‘लोकतंत्र की स्थिति’ उस मालदीव में बताई गई थी, जहां केवल मुस्लिम ही देश के नागरिक हो सकते हैं और जहां शरई कानून लागू हैं।
एक स्पष्ट रुझान यह भी दिखता है कि जबसे चीन ने संयुक्त राष्ट्र के लिए अपना वित्तीय योगदान बढ़ाया है, तबसे वह इस वैश्विक संस्था और उसकी एजेंसियों के कामकाज को प्रभावित करने की कोशिशों में जुटा है। यही बात पश्चिम की कई अकादमिक, पेशेवर संस्थाओं और विश्वविद्यालयों पर भी लागू होती है, जो विभिन्न विषयों पर स्वतंत्र सर्वेक्षण और रैंकिंग जारी करते हैं। समय आ गया है कि इन संस्थानों के वित्तीय स्रोतों की कड़ीजांच-पड़ताल कराई जाए। हाल के वर्षों में विश्व बैंक और डब्ल्यूएचओ के रवैये को देखते हुए भारतीय एजेंसियों को पूरी तरहसतर्क हो जाना चाहिए। विशेषकर एशिया में एक और आर्थिक एवं सामरिक शक्ति के रूप में भारत के उभार से चिंतित होते चीन को देखते हुए यह आवश्यक हो जाता है।भारत की तरक्की की राह में चीन किसी भी प्रकार से अवरोध पैदा करने में जुटा हुआ है। ऐसी कई दलीलें हैं जो विश्वास दिलाती हैं कि ये वैश्विक संस्थान चीन के शिकंजे में फंसकर वही रिपोर्ट तैयार करते हैं, जो चीनी एजेंडे के अनुकूल हो। मिसाल के तौर पर भारत के वैश्विक वैक्सीन उत्पादन में अग्रणी होने के बावजूद डब्ल्यूएचओस्वदेशी कोवैक्सीन को मान्यता देने में आनाकानी कर रहा है। देश में 11.20 करोड़ से अधिक लोग कोवैक्सीन की खुराक ले चुके हैं और उसकी क्षमताओं पर भी कोई सवाल नहीं उठे। फिर भी डब्ल्यूएचओ के इस अवरोध से लाखों भारतीय विदेश जाने से वंचित हो रहे हैं। आखिर डब्ल्यूएचओ किसकी शह पर ऐसा कर रहा है?
संभवत: सबसे बड़ा मजाक यह है कि दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह देश इन वैश्विक संस्थाओं पर अपनी मर्जी थोप रहा है कि वे लोकतंत्र और अन्य पैमानों पर भारत की बदरंग तस्वीर दिखाएं। ऐसे में इन तथाकथित वैश्विक रिपोर्ट का प्रतिकार किया जाए, जो शोध, जांच और विश्लेषण के मूल सिद्धांतों पर ही न खरी उतरती हों।
 Date:27-10-21
Date:27-10-21
कार्बन की कम खपत में भारत का फायदा
अजय शाह, ( लेखक पुणे इंटरनैशनल सेंटर में शोधकर्ता हैं )

हवा में सीओ2 बहुत अधिक है क्योंकि औद्योगिक युग के आरंभ से ही हम इंसान जीवाश्म ईंधन जलाते आ रहे हैं। वायुमंडल में उत्सर्जित कुल सीओ2 में भारत के उत्सर्जन का योगदान 3.1 फीसदी है। यह समस्या हमने नहीं निर्मित की है: इसे अमीर देशों ने जन्म दिया है।
सीओ2 के कारण हुए प्रदूषण में कमी करने के लिए पूरी दुनिया संघर्ष कर रही है। वर्तमान में विश्व स्तर पर सीओ2 का सालाना उत्सर्जन 55 गीगाटन हो चुका है। पेरिस समझौते में बातें इतनी नरमी से कही गई हैं कि उनका उल्लंघन संभव है। ऐसे में बड़ी आपदाओं की संभावनाओं को समुचित रूप से कम करने के लिए उत्सर्जन को सन 2055 तक समाप्त करना होगा। मौजूदा गति से देखें तो 2055 तक उत्सर्जन के 80 गीगाटन वार्षिक हो जाने का अनुमान है। इन तीन बड़े आंकड़ों 55, 80 और शून्य का आकलन करने की आवश्यकता है। आज दुनिया सालाना 55 गीगाटन कार्बन उत्सर्जन कर रही है और अगर पेरिस समझौता कारगर रहा तो यह आंकड़ा स्थिर रहेगा। सन 2055 में हमारे 80 गीगाटन उत्सर्जन करने का अनुमान है जबकि हमें उसे शून्य करना है। इसके लिए प्रयास करने होंगे। सीओ2 को शून्य करने का अर्थ है मौजूदा तेल और कोयला आधारित उद्योगों में भारी बदलाव। महज 35 वर्ष में ये बदलाव हासिल करना आसान नहीं है।
भारत का कार्बन उत्सर्जन सन 2001 के एक गीगाटन वार्षिक से बढ़कर आज 2.6 गीगाटन प्रति वर्ष हो गया है। इसमें सालाना 5 फीसदी की संयुक्त वृद्धि हुई। जबकि वैश्विक उत्सर्जन के मामले में हम 2000 के 4 फीसदी से बढ़कर आज 7 फीसदी पर पहुंच गए हैं। उत्सर्जन के चौथे सबसे बड़े स्रोत के रूप में भारत पर तब ध्यान दिया जाएगा जबकि वह मजबूती से बदलाव न शुरू कर पाए। भारत में सूर्य की रोशनी पर्याप्त मात्रा में है लेकिन हाल के दशकों में ऊर्जा उत्पादन में कार्बन का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है। जबकि इस अवधि में चीन और ब्रिटेन समेत कई देशों का प्रदर्शन भारत की तुलना में बेहतर रहा है।
यदि भारत कार्बन आधारित भविष्य की ओर बढऩा चाहता है तो दो चीजें उसकी राह रोकेंगी। पहली है पूंजी की लागत। भारत में अचल संपत्ति निवेश परियोजनाएं अब अंतरराष्ट्रीय परिसंपत्ति मूल्यांकन माहौल में नियोजित की जा रही हैं। दुनिया भर में परिसंपत्ति प्रबंधकों के व्यापक संसाधन अब पर्यावरण, सामाजिक और संचालन (ईएसजी) आधारित विश्व के अनुरूप तैयार हो रहे हैं। इसके चलते कार्बन आधारित बिजली संयंत्रों की पूंजी की लागत अधिक है जबकि नवीकरणीय परियोजनाओं की कम। यदि भारतीय कंपनियां जीवाश्म ईंधन का प्रयोग करना चाहती हैं तो उन्हें इसके लिए पूंजी की अधिक लागत का सामना करना होगा। ईएसजी निवेश के लिए यह आवश्यक है कि बड़ी कंपनियां कम उत्सर्जन करें। गूगल जैसी कंपनी ताप बिजली नहीं खरीदती। ईएसजी आधारित निवेश की नई दुनिया भारत की ऊर्जा कंपनियों और ग्राहकों पर दबाव बनाती है कि वे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कार्बन उत्सर्जन न करें।
दूसरी समस्या है विकसित देशों के नजरिये की। लोगों को विज्ञान पढ़ाना बहुत मुश्किल है लेकिन बीते 30 वर्षों में बहुत बड़ी तादाद में लोगों को यह समझ में आया है कि सीओ2 एक प्रदूषक है जो पूरी दुनिया को प्रभावित कर रही है। यह भी कि अगर हमने हवा में इसका स्तर कम नहीं किया तो समस्या कम होने के बजाय बढ़ती ही चली जाएगी। प्यू रिसर्च सेंटर ने 17 विकसित देशों में शोध किया जिसे गत माह प्रकाशित किया गया। इसके मुताबिक 72 फीसदी लोगों को लगता है कि वैश्विक जलवायु परिवर्तन सभी लोगों को नुकसान पहुंचाएगा और 80 फीसदी लोग इससे निपटने के लिए अपने जीवन और काम में बदलाव लाने को उत्सुक थे। करीब 52 फीसदी लोगों को यकीन नहीं था कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय इस समस्या को समाप्त करने के लिए पर्याप्त कदम उठा रहा है अथवा नहीं।
ऐसे लोगों की तादाद बढ़ी है और इसके कारण विकसित देशों के नेताओं का नजरिया बदला है क्योंकि उन्हें लोकतांत्रिक जवाबदेही निभानी पड़ रही है। इसके अलावा उन्हें औसत मतदाताओं के नजरिये में आए बदलाव का अनुसरण करना होगा। इसके चलते अर्थ नीति के विभिन्न हिस्सों में बदलाव संभव है। इससे ईएसजी निवेश को आकार देने वाले नियम और अधिक गहन हो सकते हैं। विकसित देशों के आयात में शामिल कार्बन पर कर लग सकता है। यदि कोई देश जलवायु के प्रश्न पर कुछ ज्यादा कट्टर है तो यह विदेश नीति में लेनदेन का हिस्सा बन सकता है।
प्यू रिसर्च के सर्वेक्षण में पाया गया कि विकसित देशों के 78 फीसदी लोग सोचते हैं कि चीन जलवायु परिवर्तन के लिए एक बुरा कारक है। यह सही है कि आज चीन बहुत अधिक मात्रा में सीओ2 का उत्सर्जन करता है लेकिन उसने जलवायु परिवर्तन को भी तेजी से अपनाया है। चीन में प्रति व्यक्ति उत्सर्जन 2013 में अपने उच्चतम स्तर पर था। चीन में बौद्धिक क्षमता भी है और जरूरी नीतिगत ढांचा भी है जिसकी मदद से चीन के राजनेता यह दिखा सकते हैं कि वे जलवायु परिवर्तन के लिए प्रयासरत हैं। यह बात चीन को लेनदेन की कूटनीति में बढ़त प्रदान करती है।
भारत ने सीओ2 की समस्या नहीं पैदा की है लेकिन हमें अपने हित में काम करना होगा। अंतरराष्ट्रीय परिसंपत्ति मूल्यांकन के अधीन भारत में कार्बन आधारित निवेश को पूंजी की लागत में इजाफे के चलते क्षति पहुंची है। वर्ष 2016 से 2020 के बीच वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रक्रिया का ध्यान कट्टर डॉनल्ड ट्रंप से निपटने पर केंद्रित था। ऐसे में जब पूरी दुनिया 2055 तक उत्सर्जन समाप्त करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है अंतरराष्ट्रीय संबंधों का बदलता माहौल बताता है कि कार्बन खपत कम करने में भारत का फायदा है।
ऊर्जा संकट और विकल्प
संजय वर्मा
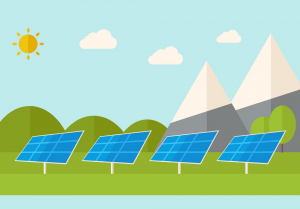
बिजली उत्पादन का मौजूदा परिदृश्य देखें तो पता चलता है कि इसके लिए हम स्वदेशी और आयातित कोयले पर निर्भर हैं। लेकिन यह निर्भरता कई मुश्किलों का सबब बन रही है। कोयले के घटते स्रोत (घरेलू खदानें और विदेश से आयात) जल्द ही ऐसी स्थितियां पैदा कर सकते हैं, जिनमें हमें विद्युत उत्पादन के दूसरे स्रोतों पर आश्रित होना पड़ेगा। दूसरी समस्या यह है कि वायु प्रदूषण और जलवायु संकट की चुनौतियों के मद्देनजर कोयले से बनने वाली बिजली के विकल्प तलाशने की मजबूरी खड़ी हो गई है। देश में ऐसी कई योजनाओं पर काम भी चल रहा है जिनमें कोयले वाली बिजली से हट कर पनबिजली या परमाणु बिजली या फिर सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि के उत्पादन पर जोर दिया जा रहा है।कोयले की जगह लेने वाले सारे विकल्पों के अपने-अपने आकर्षण हैं, लेकिन व्यावहारिकता की कसौटी पर सभी में कोई न कोई दिक्कतें हैं। इससे यह संभव लगता नहीं है कि ये विकल्प जल्द ही कोयले की जगह ले पाएंगे। बिजली उत्पादन के लिए कोयला कितना बड़ा सहारा है, इसकी पुष्टि इस तथ्य होती है कि फिलहाल भारत में सबसे ज्यादा यानी उनसठ फीसद बिजली कोयले से बनाई जा रही है। इसे तापीय (थर्मल) बिजली कहा जाता है। इसके बाद दूसरा स्थान हाइड्रो इलेक्ट्रिक यानी जलविद्युत का है। जलविद्युत परियोजनाओं से देश में सत्रह फीसद बिजली बनाई जाती है। बाकी बची नौ फीसद बिजली जीवाश्म ईंधन या प्राकृतिक गैस से, तीन फीसदी परमाणु बिजलीघरों में और करीब बारह फीसदी बिजली अक्षय ऊर्जा के स्रोतों यानी सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा से मिलती है।
मामला अकेले बिजली उत्पादन की सहूलियत का नहीं है। उत्पादित बिजली की कीमत भी एक बड़ा पहलू है। सबसे सस्ती बिजली कोयले से मिलती है। लेकिन हाल में जिस तरह कोयले संकट गहराया और ताप बिजलीघरों ने विदेश से आयातित महंगे कोयले से बिजली बनाई तो उससे बनी बिजली की कीमत भी बढ़ गई। विद्युत वितरण कंपनियों ने महंगी बिजली खरीदने से इनकार कर दिया। अगर आगे चल कर विद्युत आपूर्ति कायम रखने के लिए उन्हें यह बिजली खरीदनी पड़ी तो साफ है कि कंपनियां इसका बोझ उपभोक्ताओं पर डालेंगी। ऐसी स्थिति में दो या तीन गुना ज्यादा कीमत उपभोक्ताओं को चुकानी पड़ सकती है।
परमाणु बिजलीघरों से मिलने वाली बिजली के बारे में भी कहा जाता है कि दूसरे स्रोतों की तुलना में यह भविष्य में काफी सस्ती पड़ेगी, लेकिन फिलहाल देश में इसका उत्पादन पैदावार दो से तीन फीसद ही है। इसके अलावा परमाणु ईंधन के लिए हमारा देश न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप (एनएसजी) की मेहरबानी पर निर्भर है। एक अन्य बेहतर विकल्प सौर ऊर्जा के रूप में मिल सकता है।भारत एक वैश्विक सौर गठबंधन समूह (एसएजी) का भी सदस्य है और देश में सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए कई योजनाओं पर काम चल रहा है। लेकिन अक्षय ऊर्जा का यह स्रोत अभी बहुत भरोसा नहीं पैदा कर पाया है। जिन तटीय इलाकों में विशालकाय सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए गए हैं, वहां आने वाले चक्रवाती तूफानों के कारण इनके क्षतिग्रस्त होने की खबरें अक्सर मिलती रही हैं। यही नहीं, सौर बिजली की कीमत अभी भी कोयले से मिलने वाली बिजली के मुकाबले चौदह फीसद तक महंगी है। हालांकि आम लोगों को अपने घरों की छतों पर सौर पैनल लगाने को उत्साहित किया जा रहा है, लेकिन पैनल लगाने की शुरुआती कीमत आम लोगों को इस बारे में ज्यादा प्रेरणा नहीं दे पाई है। जीवाश्म ईंधन और प्राकृतिक गैस से चलने वाले बिजलीघरों की बात की जाए, तो इससे जुड़ा तथ्य यह है कि इन बिजलीघरों, कारखानों और वाहनों को चलाने में जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल होता है और भारत अपनी जरूरत का अस्सी फीसद तेल विदेशों से आयात करता है।हमारा देश कुछ समय पहले तक इसके लिए इराक और सऊदी अरब पर निर्भर था। अब भारत अपनी जरूरत के तेल का बारह फीसद ईरान से आयात कर रहा है। वर्ष 2018 में भारत ने ईरान से सात अरब डालर का तेल आयात किया था। असल में ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंध लगाए जाने के बाद मई, 2019 से वहां से भारत को तेल आपूर्ति तकरीन ठप्प हो गई, जिससे तेल के लिए सऊदी अरब और इराक पर निर्भरता बढ़ी।
हालांकि इन सारी समस्याओं के समाधान की कुछ राहें भी खुली हैं। जैसे हाल में देश में राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन को हरी झंडी दिखाई गई है।इस योजना का उद्देश्य देश को ग्रीन हाइड्रोजन का निर्यातक देश बनाने का है। हाइड्रोजन ऐसा ईंधन है जो स्वच्छ है और एक बार दक्षता हासिल होने के बाद इससे अनंत काल तक असीमित ऊर्जा पाई जा सकती है। समस्या दबाव डाल कर इसका भंडार करने की है, क्योंकि यह अत्यंत विस्फोटक होने के कारण दुर्घटना का कारण भी बन सकती है। उम्मीद है कि राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन में इससे जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान निकाल लिया जाएगा। हाइड्रोजन ईंधन के अलावा स्वच्छ ऊर्जा के जिन अन्य स्रोतों का उल्लेख सरकार के स्तर पर किया जा रहा है, उनमें बिजली से चलने वाली कार, बस और ट्रक अग्रणी हैं।इसके अलावा ईंधन के रूप में गैस के इस्तेमाल और पेट्रोल में एथेनाल के मिश्रण से तैयार होने वाले ईंधन से वाहन चलाने की योजना भी उल्लेखनीय हैं। गन्ने के शीरे से निकाला गया एथेनाल एक स्वच्छ ईंधन है, लिहाजा इसे जला कर बनाई जाने वाली बिजली कई मायनों में दूसरे विकल्पों से बेहतर मानी जाती है। भारत में भी एथेनाल से ऊर्जा हासिल करने का चलन शुरू हो चुका है। कुछ राज्यों में प्रायोगिक तौर पर बसें और ट्रेनें तक एथेनाल से चलाई जा रही हैं। आने वक्त में निश्चित ही मोटर वाहनों को एथेनाल मिश्रण वाले ईंधन वाले इंजनों से युक्त किया जा सकता है जिससे तेल पर हमारी निर्भरता कुछ कम होगी।
बिजली चालित वाहनों और सौर ऊर्जा पर चल रही जोर-आजमाइश कुछ राहत भरे नतीजे ला सकती है। लेकिन इस पूरे प्रकरण में जो सबसे मुश्किल काम है, वह तकनीक का हस्तांतरण है। जब बिजली कोयले की जगह सौर पैनल लगेंगे तो बराबर मात्रा में बिजली पाने में भारी निवेश और जरूरत के मुकाबले कम उत्पादन के जोखिम को सहना पड़ेगा। इससे आर्थिक विकास की रफ्तार में कमी आ सकती है और फैक्ट्रियों के संचालन की गति धीमी पड़ने से लेकर रोजगार का संकट भी आ सकता है। लेकिन ध्यान रखना होगा कि जब लक्ष्य बड़े हों, धरती को भावी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखने जैसे उद्देश्य सामने हों तो इन चुनौतियों से हर हाल में निपटने का खतरा उठाना ही होगा।
जलवायु सुधारने के लिए जुटेंगे दुनिया के देश
मदन जैड़ा, ( ब्यूरो चीफ )
भारत सहित दुनिया के तमाम देश जब कई तरह के जलवायु खतरों का सामना कर रहे हैं, तब 31 अक्तूबर से ब्रिटेन के ग्लास्गो में शुरू होने जा रही 13 दिवसीय जलवायु वार्ता काप-26 पर सबकी निगाहें हैं। बैठक कितनी महत्वपूर्ण है, इसका अंदाजा इसी से हो सकता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित 120 देशों के राष्ट्राध्यक्ष व शासनाध्यक्ष इसमें हिस्सा ले रहे हैं। मोदी 2015 में पेरिस में हुई काप-21 जलवायु वार्ता में भी शामिल हुए थे। दरअसल, पेरिस समझौते के तहत जो समझौते हुए थे, अब उन्हें प्रभावी रूप से जमीन पर उतारने और उससे आगे बढ़कर उत्सर्जन में कटौती के लक्ष्यों को नए सिरे से निर्धारित करने की जरूरत है। इसलिए बैठक का पूरा ताना-बाना उत्सर्जन में बड़ी कटौती और शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्यों पर केंद्रित रहेगा।
पेरिस समझौते के तहत दुनिया के तमाम देशों ने कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के अपने लक्ष्य घोषित किए थे, जिन्हें 2030 तक पूरा होना है। 1 जनवरी, 2021 से पेरिस समझौते का विधिवत क्रियान्वयन भी शुरू हो चुका है, लेकिन 2015-2020 के दौरान जलवायु प्रभावों को लेकर जो विभिन्न अध्ययन सामने आए हैं, वे चिंता बढ़ाते हैं। पहली चिंता यह है कि पेरिस समझौते के तहत सदी के अंत तक तापमान बढ़ोतरी को दो डिग्री से नीचे रखने की बात कही गई है। लेकिन आईपीसीसी के नए अध्ययन बताते हैं कि यह लक्ष्य काफी नहीं है। यदि जलवायु खतरों से बचना है, तो इसे 1.5 डिग्री तक सीमित करना होगा, क्योंकि डेढ़ डिग्री की तुलना में दो डिग्री की बढ़ोतरी के प्रभाव कहीं ज्यादा खतरनाक हैं।
हालिया अध्ययन यह भी बताते हैं कि पेरिस समझौते के तहत स्वयं घोषित लक्ष्यों के जरिये दुनिया में अभी जिस रफ्तार से कार्य हो रहा है, वह दो डिग्री के अनुकूल नहीं है। यदि इस प्रकार जलवायु खतरे से निपटने का कार्य जारी रहता है, तो तापमान में बढ़ोतरी तीन डिग्री से भी ज्यादा हो सकती है। जबकि दो डिग्री के बजाय डेढ़ डिग्री के लक्ष्य को नए सिरे से निर्धारित करने की जरूरत है। इसलिए संयुक्त राष्ट्र की तरफ से पूरी दुनिया को कहा गया है कि वे कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के लिए अपने नए लक्ष्य निर्धारित करें।
भारत का यह भी मानना है कि ऐतिहासिक रूप से अधिक कार्बन उत्सर्जन के लिए औद्योगिक राष्ट्र जिम्मेदार हैं। ये राष्ट्र आज विकसित देश हैं, इसलिए उन्हें अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा। उन्हें जलवायु कोष में 100 अरब डॉलर की राशि देने के अपने वादे को पूरा करना होगा, ताकि इस राशि को गरीब एवं विकासशील देशों को जलवायु खतरों से निपटने के लिए मदद के रूप में प्रदान किया जा सके। हालांकि, यह राशि बहुत पहले तय हुई थी। यदि अब दुनिया शून्य उत्सर्जन की ओर बढ़ती है, तो उसके लिए 2050 तक प्रतिवर्ष 1-2 खरब डॉलर निवेश की जरूरत होगी। राशि बड़ी है, लेकिन जलवायु खतरों से होने वाली क्षति इससे कई गुना ज्यादा होगी। भारत चाहता है कि धनी देश जरूरतमंद देशों से हरित तकनीकें भी साझा करें। भारत का तीसरा बिंदु यह है कि आगे जलवायु खतरों से निपटने के लिए दुनिया के प्रयासों में सभी को एक तराजू पर नहीं तौला जाए। विकसित देशों के लक्ष्य ज्यादा बड़े होने चाहिए। भारत जैसे देशों के पास, जिनके समक्ष विकास की चुनौती है, गरीबी दूर करने के लक्ष्य हैं, उनके लिए औद्योगिकीकरण बंद करना संभव नहीं है और न ही उनके लिए तेजी से ऊर्जा रूपांतरण संभव है। इसलिए नेट जीरो जैसे लक्ष्य अपनाने के लिए उन्हें बाध्य नहीं किया जाना चाहिए।
भारत भी अपने लक्ष्यों को संशोधित कर सकता है। इसकी कई वजहें हैं। पेरिस समझौते के तहत उत्सर्जन की तीव्रता 33-35 फीसदी कम करने के करीब 60 फीसदी लक्ष्य को वह 2019 तक ही हासिल कर चुका है। इसलिए 2025 तक वह आसानी से यह लक्ष्य हासिल कर लेगा। इसके बाद भारत ने 450 गीगावाट हरित ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ई-मोबिलिटी जैसी कई बड़ी योजनाएं शुरू की हैं, जो अगले 10 वर्षों में उत्सर्जन में काफी कमी लाएंगी। इसलिए यदि प्रधानमंत्री वहां अपने लक्ष्यों में बढ़ोतरी का एलान करते हैं, तो इससे भारत को जलवायु वार्ता में बढ़त हासिल होगी। यहां यह बताना जरूरी है कि भारत की स्थिति जलवायु मोर्चे पर अभी भी काफी अच्छी है।
