
26-06-2020 (Important News Clippings)
To Download Click Here.
 Date:26-06-20
Date:26-06-20
Federalism In Times Of Covid
Pandemic has injected operational unitariness, deserving strict scrutiny by Supreme Court
Abhishek Manu Singhvi is a member of parliament, jurist, former additional solicitor general of India and national spokesperson of the Congress party.
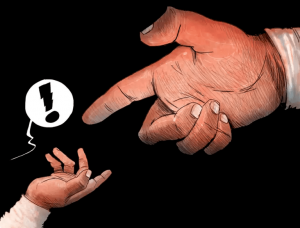
Federalism is a strange creature, full of paradoxes. Nowhere mentioned in the Indian Constitution (not even in the Preamble), federalism is nevertheless a part of its basic structure and unamendable even by a constitutional amendment! While secularism and socialism were included in the Preamble in 1977, federalism was not.
Our founding fathers, beset by apprehensions about the fissiparous tendencies of the nascent republic amidst the divisive, surcharged and fractious ambience of Partition and violence, consciously designed the Indian Constitution as largely a unitary one (charitably called quasi-federal). Yet, in operational reality over seven decades, it has become more and more federal. Finally, turning full circle, Covid has perhaps again made our system significantly more unitary.
Covid has injected operational unitariness in this system and deserves strict scrutiny by the apex court. Read literally, the Disaster Management Act, especially Sections 35, 62, 65, gives a carte blanche to central authorities to do anything and direct anyone down to any sub state unit. Courts must decide whether the dubious fusion of powers from list 1 entry 81 and list 3 entries 3, 6 and 29 gives the Centre power to give far reaching directions, for example, the one relating to mandatory payment of wages under section 10(2) (i) or the supposed mandatory use of the Aarogya Setu app (even after the 9 judge privacy ruling). Legally, I would respond in the negative to both queries.
Unlike the US, where several sovereign, independent countries ceded sovereignty to create a new nation with limited central government powers (the classic example of bottom up federalism), the Indian Republic was the opposite case of limited top down federalism. Our framers put the maximum powers in the exclusive central list 1; allowed full state takeover by the Centre under Article 356 and the sending of central forces to states under Article 355 (both antitheses of federalism); made the Centre the residuary legatee of all unspecified legislative powers by putting a residuary entry only in list 1; created a long concurrent list 3 (present in very few Constitutions), where central legislation trumps state legislation; empowered the Centre to legislate even on exclusive state subjects by special invasive Articles like 249, 250 and 253 (for national interest, during emergencies and to implement treaties).
Scholars have traced the fascinating journey of “unintended, inadvertent or accidental” federalism achieved by India despite the contrary original intent of our founders. Federalism is desirable as an inalienable component of shared/ participatory democracy, acting as a valuable safety valve to channelise the 3Ds of discomfort, dissatisfaction and dissent to decentralised institutions of governance, thereby quarantining conflicts at sub units and preventing explosions at the Centre.
These six facets of unintended and accidental federalism include linguistic federalism, the creation of states on linguistic lines and the stability of the three language formula. Prompt, efficacious and punitive judicial review of President’s rule and floor tests – with cases like Uttarakhand, Karnataka 1 & 2, Maharashtra, Jharkhand, Goa, Arunachal et al mandating floor tests in 48 to 72 hours – have deprived over adventurous invaders of constitutional propriety from enjoying the fruits of their acrobatics. Since 2000, there have been hardly 10 such escapades (as against 100 till 2000) and most have been judicially invalidated, establishing judicial federalism.
The 72nd and 73rd constitutional amendments entrenched 3 tier panchayati raj governance and has the largest number of locally empowered deciding administrative and monetary issues, a triumph of panchayat federalism. Economic federalism was ushered in with delicensing liberalisation from 1991 onwards, which made state CMs at least three times as powerful as a central Cabinet minister. Fiscal federalism has resulted in effective devolution – whether shareable revenues or grants – of about 43% of all central government receipts to states, as against barely 31% a decade ago. Finally, coalition governance and regional political parties are a victory of political federalism.
A major threat to federalism is partisan political appointments of governors, as central government agents acting more royally than the King. This dyarchy of divided sovereignties between appointed governors and elected CMs was most severely castigated, using trenchant words, both by Ambedkar in the Constituent Assembly as also by the Sarkaria Commission.
It has fallen on deaf political ears, irrespective of political colour and the only solution appears to be to appoint renowned international academics, scientists or Nobel laureates as governors. Homilies regarding non-political appointees are not going to work and umbilical cords cannot be severed magically. Absent such drastic reform, the even bigger one of abolition of this post should be considered.
Another threat is the increasingly different political colour of 60% plus of the Indian political map from the colour of the central ruling dispensation. Antagonistic, confrontational and vindictive political approaches rooted in such reasons will be the beginning of the end of the gains of federalism. Statesmanship and perspicacity of an extraordinary degree are required, seen more in the breach (the GST Council being a rare exception).
It is vital in Covid times to recalibrate and reimagine genuine consultative mechanisms for better federal governance. Though states and CMs were drawn into the consultative matrix later on, the initial lockdown decision was completely unilateral. Most of the migrants’ intractable problems arise from such state exclusion. No interstate council has been operationalised as an institutional mechanism for collegiate federal decision making during Covid.
History will judge us harshly if we fritter away the triumphs of federalism in planet Earth’s most diverse spot.
On our own
How did India manage to lose its neighbourhood? Answers lie at home
Pratap Bhanu Mehta , [ The writer is contributing editor, The Indian Express.]
As the border stand-off with China deepens, India will have to think of all possible strategic options that give it leverage in this crisis. One element often discussed in this context is new arrangements with a variety of powers. Many strategic experts are salivating at the prospect of an even closer alliance with the US. This is a propitious moment to mobilise international opinion on China. The degree of global alienation with the Xi Jinping regime is unprecedented. But can this be translated into concerted global action to exert real pressure on China? India should pursue all possible avenues. But we should also have a clear-eyed view of the limitations of what new alliances or arrangements can do for India.
It is important to remember that international relations are formed in the context of a country’s development paradigm. India’s primary aim should be to preserve the maximum space for its development model, if it can actually formulate one. India is not unique in this respect. The US-China relationship may have had its origins in the strategic attempt to create a Sino-Soviet split. But for decades, this relationship was sustained not by a strategic logic, but by the logic of the political economy of development in both the US and China, where they reciprocally depended on each other. What has changed profoundly in the US is the view that this arrangement largely benefitted big business in America at the expense of its own domestic manufacturing base.
The political legitimacy of the development model waned, and it is this fact that will largely be the driver of the US-China relationship. The question for India is not just whether the US has a stake in India’s development, which it might. But it is, rather, to ask whether India’s development needs will fit into the emerging US development paradigm. Will the very same political economy forces that create a disengagement with China also come in the way of a closer relationship with India? Some sections of American big business might bat for India; but the underlying political economy dynamics are less propitious. Will the US give India the room it needs on trade, intellectual property, regulation, agriculture, labour mobility, the very areas where freedom is vital for India’s economy? Will a US hell-bent on bringing manufacturing jobs back to the US, easily gel with an “atma nirbhar” Bharat? To see what is at stake, we just need to look at the way in which friction over the development paradigm is driving tensions on trade, taxation and regulatory issues between the US and EU.
There is sometimes a complaint in the US that India is invited but refuses to come to the table with enthusiasm. There is some truth to this, despite the salutary cultural and political momentum in this relationship. But the drivers of this have often been legitimate differences over development, including climate change. It has also been that, at various points, that ask was antithetical to India’s other strategic commitments. India was wise to stay out of the war in Iraq, it was wise not to spurn Russia entirely, and it is wise not to throw its weight behind the US’s Iran policy. There is more maturity in the US to understand India’s position. But there is a section of India’s strategic community that sees India’s reluctance to go in with the US, hook line and sinker, as a kind of ideological wimpishness, not a sign of more deeply thought out realism, which it has been.
It is an odd moment in global affairs, where there is recognition of a common challenge emanating from China, but no global appetite to take concerted action. An interesting example might be the global response to the BRI. Many countries are struggling to meet their BRI debt obligations. Many Chinese loans have become a millstone around the debtor countries’ necks. But it is difficult to see the rest of the international community helping all these countries to wean their regimes away from dependence on Chinese finance. Similarly, there are now great concerns over frontier areas of conflict like cyber security and space. It is difficult to imagine concerted global action to create rules in these area, partly because Great Powers like the US and Russia will always want to maintain their exceptionalism. So we are in a paradoxical world where the strategic necessity of the rest of the world to come together on China has never been higher; yet the appetite for concerted action has never been weaker. Fundamentally, few countries are going to put their money where their mouth is.
The value of global alliances and public opinion in settling our local conflicts has always been limited for two reasons. First, the international community has not been very effective in neutralising low cost asymmetric options exercised by some powers. This is the tactic Pakistan has used. Second, what military options India can exercise, fortifying defences, gaining strategic leverage in areas where we can, is for military experts to decide. But don’t count on the fact that the world will support an Indian escalation beyond a point. The efforts of the international community, in the final analysis, will be to try and throw cold water on the conflict; no one has a serious stake in the fate of the terrain India and China are disputing. At the end of the day, India has to manage China and Pakistan largely on its own.
The logic of the Chinese opening so many fronts together is baffling. Reassuringly, it could mean China is overreaching. Less reassuringly, it could mean that rather than displaying strategic coherence, China is now a regime that, like so many authoritarian regimes of the past, is willing to damage itself and the world. Such regimes are always harder to handle because it is not straightforwardly interest that drives them. Even as we deal with the military situation on the border, the test of India’s resolve will be its ability to return to some first principle thinking about its own power. How does it create the space for accelerating its development — in the long run, the only cornerstone of a defence policy? How does it stay true to its greatest strength, its political identity as a liberal, pluralistic democracy? How did India, in its quest for global prestige, manage to lose its own neighbourhood? Our major vulnerabilities are all at home, and so are the solutions.
Can online learning replace the school classroom ?
E-learning is out of reach for many students coming from the disadvantaged sections

The COVID-19 outbreak has disrupted the academic year, cancelled classes and examinations across the country. To ensure that students do not miss out on their studies, schools moved classes online, forcing students to attend lectures via their gadgets. However, this has also sparked a debate on whether the increased amount of screen time helps students learn or if it impedes their progress. While Maharashtra has banned online classes from pre-primary to Class II, Karnataka and Madhya Pradesh have extended the ban till Class V. In a discussion moderated by Puja Pednekar, Kiran Bhatty and Reeta Sonawat look at the pros and cons of online learning. Edited excerpts:
Has screen time for students increased because of online classes?
Reeta Sonawat (RS): No, I do not think that online classes have increased screen time. Children are anyways hooked to screens whether it is in the form of television, mobile or computer. Children have been addicted to screens even before the COVID-19 pandemic began. They have been using the screen for eight to nine hours daily. When it comes to online lessons, most schools are not depending only on screens. They are giving students a blended approach by including various activities in their lessons. At pre-school level, children are asked to do painting or craft. Some schools conduct yoga sessions; ask students to experiment in the kitchen, make a salad at home. Children only have to watch their screens during storytelling sessions. But those too are designed creatively to engage students. So, there is a bit of screen time, but it is interspersed with hands-on activities.
What we need to understand is that if we do not hold these classes, we will be hampering the child’s brain development. In early childhood, the child’s brain develops every day. So, we cannot afford to miss even a single day. And for brain development, children need to receive the right kind of stimulation, which only teachers can provide. They have been trained to provide age-appropriate stimulation.
Kiran Bhatty (KB): Looking at the screen for long periods of time can be harmful. And since schools have shifted to online instruction, it does imply long hours of screen time for the child. And that doesn’t seem to be a healthy way of learning. In addition to the impact on their health, online learning from home can also be very isolating and lonely for the child. They don’t have their peers around them and are sort of learning by themselves. Even the teachers’ role becomes limited. Children do not get the kind of supervision that they would in a classroom. Parents might be too busy with their own work to supervise online learning. These factors impact learning.
Also, many children, especially those attending government schools, are being deprived of education during the pandemic as they do not have access to online facilities. They are actually missing out on their lessons. Though some families may have access to digital technology, there might not be enough devices for the personal use of all the family members. The parents may be working from home and need to use their computers. So, each household needs to have several gadgets that they can distribute among all of them so that that is really not possible for a large section of the population.
Many schools are holding online lessons for children in kindergarten as well. What are the dangers of exposing children to screens at such a young age?
RS: Exposing children to screens from a young age is not right. It can hamper their overall development. The light emitted from the screen can strain children’s eyes and could lead to vision problems throughout their lives. Watching a screen is also a passive activity that can make children lethargic and affect their thinking skills. Often, parents expose children to screens right from a young age — using videos to get toddlers to eat without a fuss is a common parenting method. This can lead to several behavioural problems.Schools should also keep this in mind while creating online content for younger kids. The lessons should be designed in such a way that the child only spends a few minutes looking at a screen. This can be done by integrating different activities into the lessons.
The Karnataka High Court has asked for guidelines on online learning. What do you think some of these guidelines should include?
KB: So, I think there are multiple issues surrounding online learning, which haven’t been thought through. There has been a rush to switch to online classes almost overnight. That’s why, some courts have asked the government to come up with guidelines on online instruction. They want to know what online classes entail, what it means, how is it going to happen and what will be its impact.
RS: The Early Childhood Association (a think tank on pre-primary education) has prepared detailed guidelines to be followed in online learning. Schools should be opened only if they are able to follow these guidelines.
Unfortunately, many of the balwadis and anganwadis (government-run creches and daycare facilities) might be located in congested areas, which may be hotspots.
Many countries have started re-opening their schools. But in India, where metro cities — Mumbai, Chennai and Delhi — are reporting an increase in the number of COVID-19 cases, is it viable to open schools?
KB: What’s worrying is the fact that the entire conversation has shifted to the use of technology. It is not just about computers and smartphones, even watching Doordarshan amounts to screen time. Nobody (in India) is really talking about turning schools into safe places, where education can resume. Education is not just about information or content delivered to students via screens. It is about a lot more. And most of it takes place through the social interactions in a school, with peers, with the teachers. Since online classes have begun, all that has been cut out. And I think that would have other kinds of developmental and cognitive impact on the child and their development. It is high time that we started to talk about how the school actually can be made a space that is safe again, for children to come back to, rather than make a complete switch to online learning.
RS: Schools may be reopening abroad, but we cannot compare that to the situation in India. The schools that have opened in these countries are taking utmost precautions. For instance, they are using tissue boxes for every class. Students can dump their used tissues in these boxes. But the waste generated is so huge, and it will also require to be discarded safely. Do Indian schools have that kind of infrastructure? Also, it is difficult to make children sit in the classroom wearing masks, without touching it. Or for them not to touch other children and their masks.
What will education look like once schools reopen post COVID-19? Will online lessons continue and what will be the learning level of the students?
KB: There is a large section of the population that is unable to access technology and that’s a huge concern. Children belonging to migrant families might have moved far away from their schools. I know government school teachers in Delhi were trying to reach some of the students whose mobile numbers they have, but they are not able to reach them, they have disappeared. And these are kids who are going to be out of school soon. We don’t know whether their families will return to the cities and what’s going to happen to them. Teachers are doing enough to develop better online modules, based on activities, but how many children are benefiting from it? The problem is that our policy has always neglected the marginalised child. That is why we still have so many children who are not in school. All our policies tend to focus on those who already have access to certain facilities. We just forget the invisible — the poor and the marginalised.
RS: If we stop online education, even the children who have access to technology will lose out. So, stopping online classes is not the solution. Instead, we need to work on providing technology to these [disadvantaged] children. Some non-government organisations are already working on these issues. They are providing smartphones, electronic tablets and teaching children to make use of technology. We need more such initiatives.
So what are the alternatives that can ensure that students don’t fall back academically because of this or any other pandemic that might arise in the future?
KB: During this pandemic, many of the policy fault lines — across all sectors — have come to the fore. Most of all in public health. The fact that our public health system is not geared towards such situations has become evident and obvious to everyone. Even within the education sector, it has become clear that we have not invested in our education system in a way that it can take care of a situation like this. Going forward, we have to start thinking on these lines. We need to improve our education system in such a way that we do not have to keep schools closed in such situations. We need to make it possible for the students to have a safe environment in schools even during a pandemic. We need to ensure that there is no shortage of teachers. Itis not just about online instruction, but also about preparing action plans to deal with students who have lost out on education because of the pandemic. A majority of the students who were unable to access technology in this pandemic may become drop-outs. This goes against their fundamental right to education.
RS: We (Early Childhood Association) have suggested that during pandemics, schools can be opened in a staggered manner, with 50% students attending every alternate day. This will help avoid crowded classrooms and give schools time to clean up their premises. Temperature checks of teachers, students and non-teaching staff should become mandatory. Teachers should not give students any books to carry home. Social distancing should be followed strictly by teachers and students. Second, it will be better to give priority to opening schools for marginalised and migrant children, as they might not have access to technology. We can create separate safe spaces for these children.
मांग बढ़ाने के सराहनीय प्रयास
संपादकीय
एमएसएमई सेक्टर की नाराजगी है कि मांग न होने से वे उत्पादन नहीं बढ़ा सकते। आरोप है कि बैंकों की ब्याज-दर और प्रक्रियात्मक जटिलता, उन्हें कर्ज लेने से डराती है। लेकिन शायद मांग की कमी जल्दी ही दूर हो सकेगी, क्योंकि लॉकडाउन में किसानों के हाथ में पैसे देकर उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए किए गए प्रयास अब परवान चढ़ेंगे। इसमें पहला है, किसानों के बम्पर उत्पाद की रिकॉर्ड सरकारी खरीद। हालांकि यू.पी सहित कुछ राज्य सरकारें अपने लक्ष्य से काफी पीछे हैं, लेकिन म.प्र, हरियाणा, पंजाब ने लक्ष्य से बेहतर खरीद की है। सबसे बड़े अनाज उत्पादक यूपी का पिछड़ना केंद्र के लिए चिंता का विषय है। कुल मिलाकर किसानों के हाथ मार्च के बाद से अब तक करीब 1.16 लाख करोड़ रु. आएंगे। साथ ही पीएम किसान सम्मान निधि के 2000 रु. भी 8.37 करोड़ किसानों को मिले हैं यानी कुल मिलाकर करीब 1.33 लाख करोड़। मनरेगा में भी मजदूरी 180 से बढ़ाकर 202 करने, गांव पहुंचे प्रवासी मजदूरों के लिए, अलग से गरीब कल्याण रोजगार योजना में 50 हजार करोड़ रु. की व्यवस्था भी ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था में मांग पैदा करने में बड़ी भूमिका निभाएगी। मनरेगा में लॉकडाउन के 1 हफ्ते बाद से अभी तक 17,622 करोड़ रु. का भुगतान हुआ है। अर्थ-व्यवस्था के सभी 3 सेक्टरों में केवल एक कृषि ही है जो धनात्मक विकास दर के साथ आने वाले समय के लिए भी यही परफाॅर्मेंस सुनिश्चित कर चुकी है। मानसून के अच्छे आसार हैं व किसान उत्साहित हैं। प्रवासी मजदूर भी जमीन का समुचित उपयोग कर रहे हैं। भारत में 65 फीसदी आबादी किसानों की है और अगर उनकी माली हालत बेहतर होती है तो तमाम उपभोक्ता सामान की खरीद बड़े पैमाने पर होगी, जिससे एमएसएमई सेक्टर का उत्पादन व रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। लोगों की आय बढ़ेगी तो मांग में इजाफा होकर अर्थ-चक्र चलने लगेगा। लेकिन केंद्र को उत्तरप्रदेश सरीखे सुस्त राज्य सरकारों को भी जगाना होगा।
Date:26-06-20
जब हम चीन को विरोधी नहीं मानते तो वह क्यों मानता है?
चीन ने इस समय एक शांत सीमा को अस्थिर करने का जोखिम क्यों लिया, आखिर उसकी मंशा क्या है?
शशि थरूर, पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद
दिल्ली में अभी भारत-चीन के बीच 15 जून को हुए टकराव की गूंज थम नहीं रही है। ऐसे में शायद यह बड़ा सवाल पूछने का समय है कि इस घटना का एशिया के दो बड़े देशों के बीच संबंधों पर क्या असर होगा? सवाल यह भी है कि यह त्रासदी क्यों हुई? चीन ने एक शांत सीमा को इस तरह अस्थिर करने का जोखिम क्यों लिया? भारत में इस बात पर सर्वसम्मति है कि यह चीनी सैन्य दस्ते का एलएसी पर अपनी स्थिति को मजबूत बनाने का सुनियोजित कदम है। केवल पेट्रोलिंग के बजाय, उन्होंने उस जगह से भी आगे अपनी स्थायी मौजूदगी बना ली है, जिसपर चीन दावा करता है। उसका उद्देश्य गलवान और श्योक नदी के संगम तक चीनी सेना की मौजूदगी बढ़ाना लगता है, जिससे गलवान घाटी भारतीय सीमा से बाहर हो जाए। चीन ने ऐसे बयान जारी किए हैं कि गलवान घाटी हमेशा से ही चीन की थी।
इसकी आशंका कम है कि बीजिंग युद्ध जैसी कोई नाटकीय योजना बना रहा है। बल्कि, उसके कदमों का उद्देश्य छोटे सैन्य अतिक्रमण कर, स्थानीय सामरिक उद्देश्यों के लिए कुछ वर्ग किमी क्षेत्र हथिया लेना और फिर शांति की घोषणा कर देना लगता है। आपसी सहमति से डिसएंगेजमेंट की घोषणा हो जाएगी, दोनों पक्ष दावा करेंगे कि संकट खत्म हो गया है, लेकिन दरअसल यह चीन की पहले से बेहतर स्थिति के साथ खत्म होगा।
एक साल में ऐसे कई घटनाक्रमों के साथ चीन एलएसी को वहां मजबूत कर लेगा, जहां वह चाहता है, ताकि जब कभी सीमा समझौते की बात हो तो इन नई वास्तविकताओं को देखा जाएगा और समझौता उसके पक्ष में रहेगा। यही उसकी लंबे समय की योजना है। बीजिंग कहता रहा है कि सीमा समझौते को भावी पीढ़ी के लिए छोड़ देना चाहिए क्योंकि वह जानता है कि हर गुजरते साल के साथ भारत की तुलना में चीन की आर्थिक, सैन्य और भूराजनैतिक स्थिति मजबूत होती जा रही है। इसीलिए भारत को फिर से यथास्थिति बनाने और उसी स्थिति में लौटने पर जोर देना चाहिए जो अप्रैल 2020 से पहले थी। यह बहुत अस्पष्ट है कि क्या चीन यह बात मानेगा। दोनों देशों ने सीमा पर और सेना भेजी है और लंबे टकराव की आशंका लगती है।
गलवान घाटी की त्रासदी और चीनी सेना की कार्रवाई ने भारतीय जनता के बीच चीन के खिलाफ विद्वेष भड़का दिया है। इससे नई दिल्ली में बैठे उन लोगों को बल मिला है, जो सोचते हैं कि भारत को अमेरिका और क्षेत्र के अन्य लोकतंत्रों के साथ चीन के खिलाफ खड़े होना चाहिए। बीजिंग पर भरोसा न करने के कई कारण हैं। जैसे, भारत के कट्टर-दुश्मन पाकिस्तान के साथ चीन का ‘ऑल-वेदर’ गठजोड़, जिसमें उसने अरबों डॉलर निवेश किए हैं। साथ ही चीन अक्सर पाक का पक्ष लेेता रहता है। फिर भारत के पड़ोसियों नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और बांग्लादेश तक में उसकी अच्छी वित्तीय मौजूदगी है, ताकि वह नई दिल्ली के पारंपरिक प्रभाव को कम कर सके। साथ ही यूएन सिक्योरिटी काउंसिल या न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में भारत की स्थायी जगह का चीन द्वारा विरोध भी कारण हैं।
शीत युद्ध खत्म होने के साथ, बीजिंग के पास भारत से संबंध के दो विकल्प थे: पहला अमेरिका के प्रभुत्व का वैकल्पिक ध्रुव बनाने के लिए भारत को रूस के साथ स्वाभाविक सहयोगी के रूप में देखना या अपनी खुद की महत्वाकांक्षाओं के चलते उसे संभावित विरोधी के रूप में देखना। ऐसा लगता है कि भारत-अमेरिका के बीच उभरे मजबूत रिश्तों को देख चीन मान चुका है कि भारत उसका विरोधी है, जबकि भारत ने बीजिंग के विरुद्ध अमेरिका का सहायक बनने से इनकार कर दिया है और चीन भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापार सहयोगी है।
चीन की इस नकारात्मक धारणा के मजबूत होने के शायद ये कारण हो सकते हैं: भारत का अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ क्वाड (चतुष्कोणीय) व्यवस्था में शामिल होना, सोवियत के साथ अपने पुराने ‘लगाव’ को बढ़ाना (जिसमें ताजिकिस्तान में भारतीय सेना का बेस बनाना भी शामिल है), चीन की ‘बेल्ट एंड रोड’ पहल की आलोचना करना, चीन के प्रभुत्व की आशंका के चलते एशिया में क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी से भारत का बाहर आना और भारत का ‘इंडो-पैसिफिक’ क्षेत्र में और दक्षिण चीन सागर में अमेरिका की स्थिति का समर्थन करना। लेकिन नई दिल्ली खुद को चीन का विरोधी नहीं मानती। भारत ऐतिहासिक रूप से गठजोड़ न करने वाला देश रहा है और उसकी कभी किसी एक के लिए ही रणनीति बनाने की इच्छा नहीं रही है। नई दिल्ली को डोनाल्ड ट्रम्प का अमेरिका कभी खास विश्वसनीय सहयोगी नहीं लगा। बतौर प्रधानमंत्री पांच बार चीन जा चुके मोदी ने आठ महीने पहले ही ‘दो देशों के बीच सहयोग के नए युग’ की शुरुआत बताई थी।
ऐसा लगता है कि वह युग आठ महीने में ही खत्म हो गया। मौजूदा घटनाक्रम में असंतुष्ट भारत, अमेरिका की तरफ जा सकता है। चीन को शायद इससे फर्क नहीं पड़ता। बीजिंग ने तय कर लिया है कि वह भारत को उसकी जगह याद दिलाने का जोखिम उठा सकता है, फिर भले ही वह जगह विरोधी खेमे में हो।
चीन को सही राह पर लाने का तरीका
शंकर शरण , (लेखक राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर एवं वरिष्ठ स्तंभकार हैं)
लद्दाख में चीन के साथ विवाद को लेकर प्रधानमंत्री की ओर से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में माकपा नेता सीताराम येचुरी ने भारत सरकार को पंचशील पर चलने की सलाह दी। किसी को सीताराम येचुरी से पूछना चाहिए कि क्या वह जानते हैं कि उस समझौते में क्या था? चूंकि येचुरी की पार्टी माओभक्त थी इसलिए उनकी पार्टी के साहित्य में पंचशील होने का सवाल ही नहीं। यदि स्वत: प्रेरणा से उन्होंने पढ़ा हो तो उनके बयान से इसकी झलक नहीं मिलती। पीकिंग (अब बीजिंग) में 29 अप्रैल, 1954 को हुआ यह समझौता भारत और तिब्बत के संबंध पर हुआ था। इस समझौते के शीर्षक में ही दर्ज है-चीन के तिब्बत क्षेत्र और भारत के बीच व्यापार और संबंध के बारे में समझौता। मात्र छह अनुच्छेदों के इस समझौते में कुल नौ बार तिब्बत का नाम आया है। पांच अनुच्छेदों में इसी का वर्णन है कि भारत-तिब्बत संबंध लगभग पूर्ववत चलते रहेंगे।
1951 तक तिब्बत स्वतंत्र देश था जब चीनी कम्युनिस्टों ने हमला कर उस पर कब्जा शुरू किया। मार्च 1947 में दिल्ली में एशियन रिलेशंस कांफ्रेंस में तिब्बत और चीन, दोनों ने स्वतंत्र देशों की तरह हिस्सा लिया था। 1914 में भी शिमला में चीन, तिब्बत और भारत ने आपसी सीमांकन समझौता किया। अभी चीन 1890 के दस्तावेज का हवाला देकर डोकलाम को अपना बताता है तो 1914 वाले दस्तावेज के अनुसार तिब्बत भी स्वतंत्र देश है। चूंकि नेहरू जी ने चीनी कम्युनिस्टों को तिब्बत हड़पने दिया इसलिए उसी के एवज में चीन ने भारतीय और तिब्बती जनता को संतुष्ट करने के लिए पंचशील समझौते के बहाने उन्हें बहलाने का उपाय किया। इस समझौते का संपूर्ण कथ्य यही था कि तिब्बत और भारत के सांस्कृतिक, व्यापारिक, सामाजिक संबंध पहले जैसे चलते रहेंगे-बिना किसी पासपोर्ट, वीजा या परमिट आदि के। क्या येचुरी यह मांग करते हैं?
पंचशील समझौता स्वयं प्रमाण है कि भारत और तिब्बत के संबंध कितने स्थापित, खुले और पारस्परिक थे, जिसमें चीन का कोई दखल न था। इसी दखल का रास्ता खोलने को पंचशील को बहाना बनाया गया। अंगुली पकड़कर गर्दन पकड़ी गई। येचुरी बताएं कि किसने पंचशील समझौते को रौंदा? क्या उसके अनुच्छेद 2 और 5 के अनुरूप भारत और तिब्बत के लोग पहले की तरह इस पार से उस पार मिलने-जुलने या खरीदारी करने जा रहे हैं? यदि नहीं तो पंचशील की नसीहत किसलिए? तिब्बत पर कब्जे के बाद 1952-53 में कोरिया संकट के समय पीकिंग में भारतीय राजदूत ने कम्युनिस्ट चीन की मंशा की चेतावनी शुरू में ही दे दी थी, लेकिन नेहरू जी कम्युनिज्म से सम्मोहित थे और अपनी महत्ता एवं सद्भावना पर स्वयं फिदा रहते थे। उन्हें चीनी नेताओं से कृतज्ञता मिलने की कल्पना थी, पर उन्हें धोखा मिला।
यदि सीताराम येचुरी और उनके सहयोगी पंचशील समझौते का पालन चाहते हैं तो उन्हें डंका पीट कर चीन से कहना चाहिए कि वह उसे लागू करे, वरना तिब्बत अपनी मुक्ति और उसकी सहायता के लिए भारत उसी तरह स्वतंत्र है जैसे कोई भी उपनिवेश अपनी मुक्ति के लिए होता है। किसी उपनिवेश की मुक्ति के लिए उसका साथ देना लोकतांत्रिक अधिकार है। प्रसिद्ध हिंदी लेखक निर्मल वर्मा ने तिब्बत को संसार का अंतिम उपनिवेश बताया था। इस सच्चाई को रेखांकित करना और तदनुरूप अपना धर्म निभाना ही हमारे लिए सही उपाय है। तभी चीन से हमारे संबंध मैत्रीपूर्ण बनेंगे जैसे कम्युनिस्ट सत्ता से पहले थे।
पंचशील समझौता दिखाता है कि भारत को तिब्बत पर अपनी साझी चिंताओं, व्यापारिक और सांस्कृतिक जरूरतों पर बोलने का पूरा अधिकार है। हमारे नेता और बुद्धिजीवी तिब्बत रीजन ऑफ चाइना की शब्दावली में सदैव चाइना पकड़ते हैं और तिब्बत भूल जाते हैं। होना उलटा चाहिए। हम सदैव तिब्बत का नाम लें और चीन को टोकें। हमारा पड़ोसी तिब्बत रहा है। चीन उसके पार है। पंचशील समझौता होते समय उसकी चर्चा इसी नाम से होती थी। कई पत्र-पत्रिकाओं में शीर्षक ही था-भारत तिब्बत समझौता। इसके दो दशक बाद भी दुनिया भर के नक्शों में तिब्बत अलग देश दिखता था। दुर्भाग्यवश हमारे नेता लोग जिन गंभीर चीजों का नाम लेते हैं उसका अर्थ नहीं समझते। चीन समझता है। वह यथार्थवादी है। इसीलिए वह तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को अपशब्द कहता है। उनसे भारतीय नेताओं के मिलने पर विरोध करता है, पर हमें जो करना चाहिए वह नहीं करते।
चीन द्वारा 1951 में तिब्बत पर हमले के बाद ही विश्व जनमत ने भारत की ओर देखा था। तिब्बत से सर्वाधिक प्रभावित होने वाला पड़ोसी भारत था। भारत द्वारा चीन का समर्थन करते रहने से ही दुनिया चुप रही। वरना तब तक चीन महाशक्ति तो क्या, मान्यताप्राप्त देश तक नहीं था। संयुक्त राष्ट्र में 1971 तक फारमूसा-ताइवान को मान्यता थी। चीन के साथ अमेरिका ने 1978 तक कूटनीतिक संबंध तक नहीं बनाए थे। तिब्बत हमारे राष्ट्रीय हित का प्रश्न है। इस पर चुप्पी रख कर हम अपनी हानि करते रहे हैं। इसीलिए चीन से हमारे संबंध बराबरी पर नहीं आते। यदि चीनी विश्वासघात के बाद भारत ने डटकर तिब्बती स्वतंत्रता का मुद्दा उठाया होता तो चीन को हमारे साथ सद्भाव बनाने की चिंता हमसे अधिक होती। तिब्बत की स्थिति भी सुधरती, क्योंकि वह उसकी शर्त होता।
जिस पंचशील से हमने धोखा खाया उसी को फिर से उठाकर यानी तिब्बत से अपने संबंध को प्रमुखता देकर हम सही मार्ग पर आ सकते हैं। आज तिब्बत असहाय लगता है, पर यदि भारत ने इसे विश्व मंच पर पुन: ला दिया तो ऐसा नहीं रहेगा। चीनी सत्ता ने अपने देश में तानाशाही को औजार बनाया है तो हम लोकतांत्रिक स्वतंत्रता को बना सकते हैं। तिब्बतियों को अपना शांतिपूर्ण वैचारिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक अभियान चलाने में सहायता देना हमारे हाथ में है। उन्हें इससे वंचित रखना हमारी मानवीय संवैधानिक प्रतिज्ञा के विरुद्ध है। सरकार न सही, विविध सामाजिक-गैर राजनीतिक लोग तिब्बत के लिए आवाज उठा सकते हैं। जैसे हांगकांग की स्वायत्तता पर चीनी हमले के विरुद्ध दुनिया भर में लोग बोल रहे हैं। भारत की सुरक्षा और तिब्बत के प्रति हमारा कर्तव्य आपस में जुड़े हैं। तिब्बत पर चीनी औपनिवेशिक सत्ता स्थाई नहीं है। किसी भी घटनाक्रम से हालत बदल सकते हैं। हमें अपना धर्म निभाना चाहिए।
Date:26-06-20
स्वास्थ्य ढांचा सुधारने का सुनहरा मौका
डॉ. सूर्यकांत , (लेखक किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ के रेस्पिरेटरी मेडिसिन विभाग के प्रमुख हैं)
पूरी दुनिया इन दिनों कोविड-19 नामक महामारी से जूझ रही है। इसका इलाज खोजने के लिए विश्व भर के वैज्ञानिक रात-दिन एक किए हैं। योगगुरु स्वामी रामदेव ने इसकी आयुर्वेदिक दवा बनाने का दावा किया है। अगर यह कारगर होती है तो आयुर्वेद की महत्ता एक बार फिर स्थापित हो जाएगी। आयुर्वेद दुनिया की सबसे पुरानी चिकित्सा विधा है। आयुर्वेद को नए आयाम तब मिले जब आज से लगभग 2600 वर्ष पहले सुश्रुत ने इसमें शल्य क्रिया जोड़ी। बाद में मर्हिष चरक ने इसका काफी प्रचार-प्रसार किया। सुश्रुत एवं चरक द्वारा बनाए गए मानक, सूत्र, पद्धतियां धीरे-धीरे पूरे विश्व में विभिन्न चिकित्सा पद्धितियों के सूत्रधार बने। आज से 2300 वर्ष पहले ग्रीक के विद्वान हिप्पोक्रेट्स ने भी चिकित्सा के कुछ सूत्र प्रतिपादित किए जो आगे चलकर आधुनिक चिकित्सा के आधार बने। इसे बाद में एलोपैथी मेडिसिन नाम दिया गया।
16वीं शताब्दी से आधुनिक चिकित्सा भारत में आई और धीर-धीरे भारत की मूल चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद कमजोर होती गई। आधुनिक चिकित्सा के आने के बाद इस विधा के मेडिकल कॉलेज भी खोलने की आवश्यकता पड़ी। इसी क्रम में फ्रेंच उपनिवेश के अधीन पांडिचेरी में 1823 में भारत ही नहीं, बल्कि एशिया का सबसे पहला मेडिकल कॉलेज खोला गया। इसके बाद पुर्तगाली उपनिवेश के अंतर्गत गोवा में स्थापित रॉयल हॉस्पिटल को 1842 में मेडिकल कॉलेज में विकसित किया गया। तत्पश्चात ब्रिटिश शासकों ने 1835 में पहले कलकत्ता मेडिकल कॉलेज और बाद में मद्रास मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। आगे चलकर अंग्रेजों द्वारा भारत में तीसरा मेडिकल कॉलेज लाहौर में 1860 में खोला गया। इसी श्रृंखला में मेडिकल शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए अंग्रेजों ने किंग जॉर्ज पंचम के 1905 में भारत आगमन के अवसर पर भारत के चौथे मेडिकल कॉलेज किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया।
ब्रिटिश शासन काल में भारत में कुपोषण, महामारी और संक्रामक रोगों की भयावहता देखने को मिली। देश में कालरा, स्माल पॉक्स तथा प्लेग से लाखों भारतीयों की मृत्यु हुई। शायद यही कारण था कि अंग्रेजों ने देश की चिकित्सा व्यवस्था को सुदृढ़ किया। 1873 में बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1880 में टीकाकरण अधिनियम तथा 1897 में ऐपिडेमिक डिजिजेस एक्ट बनाया गया। 1930 में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हाईजीन एंड पब्लिक हेल्थ, 1933 में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया तथा 1939 में पहला रूरल हेल्थ ट्रेनिंग सेंटर एवं ट्यूबरकुलोसिस एसोशिएसन ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। इसके साथ ही 1940 में ड्रग एक्ट की स्थापना भी की गई।
आजादी के बाद स्वास्थ्य विभाग के विकास के लिए देश की पंचवर्षीय योजनाओं में विभिन्न योजनाओं को शामिल किया गया, जिसके अंतर्गत स्तरीय सरकारी अस्पतालों का निर्माण तथा नए मेडिकल कॉलेज खोले गए। दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान 1956 में तथा चंडीगढ़ में 1962 में पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीटयूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च की स्थापना की गई। इसके पश्चात चिकित्सा के क्षेत्र में प्रगति काफी धीमी रही। 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्रीत्व काल में छह नए आयुर्विज्ञान संस्थानों की नींव रखी गई, जो 2012 में कार्यरत हो पाए। 2013 में एक और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की नींव रायबरेली में रखी गई। अखिल भारतीय आर्युिवज्ञान संस्थानों की संख्या में उल्लेखनीय प्रगति 2014 से 2019 के बीच हुई। इस दौरान सात नए संस्थान प्रारंभ हुए तथा 14 अन्य संस्थानों को प्रारंभ करने की प्रक्रिया चालू की गई। यह चिकित्सा के क्षेत्र में एक बड़ी छलांग है।
कोविड-19 महामारी के बहाने यह सुनहरा अवसर है कि देश में स्वास्थ्य के ढांचे को स्तरीय एवं सुदृढ़ किया जाए। विश्व चिकित्सा की रैंकिंग में भारत 145वें स्थान पर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार आधुनिक चिकित्सा के चिकित्सकों एवं जनसंख्या का अनुपात 1:1000 होना चाहिए, जबकि भारत में इसका अनुपात 1:11000 है। इसी प्रकार नर्स एवं जनसंख्या का अनुपात 1:500 होना चाहिए, जबकि भारत मे इसका अनुपात 1:3000 है। भारत में कुल 549 मेडिकल कॉलेज एवं चिकित्सा संस्थान हैं और 566 डेंटल कॉलेज हैं। जिनमें प्रतिवर्ष एमबीबीएस में प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या 78,333 एवं बीडीएस में प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या 26,960 है। भारत में कुल 4035 सरकारी हॉस्पिटल एवं 27951 डिस्पेंसरिज संचालित हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में 5624 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर एवं 25743 प्राइमरी हेल्थ सेंटर और 1,58,417 सब-सेंटर्स कार्यरत हैं। सेंट्रल गवर्मेंट हेल्थ स्कीम के अंतर्गत 37 शहरों में 288 एलोपैथिक एवं 85 आयुष डिस्पेंसरीज स्थापित की गई हैं। भारत में कुल ब्लड बैंक 3108 तथा आई बैंक 469 हैं।
विश्व स्वास्थ्य रैंकिंग में शीर्ष दस स्थानों पर आने वाले देश जैसे स्पेन, इटली, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, रूस आज कोरोना वायरस के संक्रमण से बुरी तरह प्रभावित हैं। इन देशों में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य का आधारभूत ढांचा भारत से कहीं बेहतर है। फिर भी महामारी के चलते उनक यह मजबूत ढांचा भी ध्वस्त होता दिख रहा है। भारत को इससे सबक लेते हुए खास तौर पर ग्रामीण स्तर के स्वास्थ्य ढांचे पर विशेष ध्यान देना होगा। आधुनिक चिकित्सा के साथ-साथ भारत की पारंपरिक चिकित्सा विधाओं को भी विकसित एवं मजबूत करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये चिकित्सा विधाएं सिर्फ उपचार पर आधारित नहीं हैं, बल्कि बीमारियों से बचाव तथा शरीर की रोगों के प्रति लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता (इम्युनिटी) को बढ़ाने के सिद्धांत पर भी कार्य करती हैं।
![]() Date:26-06-20
Date:26-06-20
आत्मघाती कदम
संपादकीय
देश के कई बड़े बंदरगाहों ने चीन से आने वाले माल की मंजूरी रोकने का निर्णय लिया है। इससे उद्योग जगत को माल पहुंचने में अप्रत्याशित देरी होनी तय है। उनके इस कदम से इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को खासतौर पर दिक्कत होगी। इसमें मोबाइल फोन भी शामिल हैं। इस समय देश में चीन के मोबाइल फोन ब्रांड का दबदबा है, हालांकि उनकी असेंबली और अंतिम रूप देने का अधिकांश काम भारत में होने लगा है। परंतु भारतीय ब्रांड भी काफी हद तक चीन से आने वाले कलपुर्जों पर निर्भर हैं या फिर उनमें ऐसे पुर्जे लगे हैं जो चीन से आयात किए जाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि हर खेप को खोलकर दोबार देखा जा रहा है। यह एकदम अफसरशाही किस्म की प्रताडऩा है।
परेशान करने वाली बात यह है कि ऐसा तब किया जा रहा है जबकि सीमा शुल्क विभाग और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) की ओर से इस विषय में कोई लिखित या मौखिक निर्देश नहीं जारी किया गया है। यह मनमाना कदम है जो जानकारी के मुताबिक कुछ खुफिया सूचनाओं के बाद उठाया गया है। यह कदम आत्मघाती और अतार्किक है। जाहिर है ऐसा करने वाले आर्थिक सिद्धांतों की बुनियादी समझ भी नहीं रखते। उन्हें भारतीय कारोबारी ढांचे की भी समझ नहीं है। विनिर्माण आधारित अर्थव्यवस्था में चीन से होने वाले आयात की बात करें तो चीन के कुल निर्यात का केवल 3 फीसदी भारत आता है। जाहिर है इसे रोकने से चीन की अर्थव्यवस्था को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इतना ही नहीं चीन को होने वाला भारतीय निर्यात भी हमारे कुल निर्यात का 6 फीसदी है। दूसरे शब्दों में कहें तो चीन के साथ कारोबार भारतीय निर्यातकों के लिए अधिक महत्त्वपूर्ण है, न कि चीन के निर्यातकों के लिए। क्या अघोषित व्यापारिक युद्ध में उलझे अधिकारियों को यह सारी बात पता नहीं होगी? यकीनन निर्णय लेते वक्त ये आंकड़े समुचित अधिकारियों को बताए गए होंगे। अगर ऐसा नहीं किया गया तो यह गलती है। अगर जानकारी होने के बावजूद इन्होंने मंजूरी में देरी होने दी है तो उन्होंने महामारी के कारण पहले से संकट से जूझ रही देश की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाई है।
यह बात ध्यान देने लायक है कि एकीकृत आपूर्ति शृंखला वाले विश्व में कई क्षेत्र चीन से कच्चे माल के आयात पर निर्भर हैं। जाहिर है किसी भी भौगोलिक क्षेत्र पर अत्यधिक निर्भरता खतरनाक हो सकती है और पूरी दुनिया के उत्पादक अपनी आपूर्ति शृंखला विविधतापूर्ण करना चाहते हैं। भारतीय उत्पादकों को भी ऐसा ही करना चाहिए। परंतु आ चुके माल की आपूति में अफसरशाही बाधा उत्पन्न करके ऐसा नहीं किया जा सकता। इससे केवल उन निर्माताओं और कंपनियों को परेशानी होगी जिन्हें कच्चे माल की आवश्यकता है। अगर यह रवैया लंबे समय तक कायम रहा तो उन्हें उत्पादन रोकना पड़ेगा। ऐसे समय में जबकि हर कदम आपूर्ति और मांग बढ़ाने पर केंद्रित होना चाहिए उन्हें नुकसान पहुंचाना ठीक नहीं। यह कदम जरूरी तौर तरीकों से एकदम विपरीत है और सरकार के कारोबारी सुगमता बढ़ाने और अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के तमाम हालिया दावों के खिलाफ जाता है।
निश्चित तौर पर चीन जिस तरह वैश्विक कारोबारी व्यवस्था में आक्रामकता के साथ अपना वजन बढ़ा रहा है, वैसे में उसके प्रति अविश्वास की तमाम वजह हैं। खासतौर पर भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका विशेष प्रभाव है। परंतु उसका हल इस बात में निहित है कि भारत अपनी प्रतिस्पर्धा बढ़ाए, अन्य देशों के साथ करीबी कारोबारी रिश्ते बनाए और चुनिंदा आपूर्ति शृंखला में चीन का स्थानापन्न तलाश करे। चीन की चुनौती से निपटने के लिए क्या करना है, इस विषय में अफसरशाहों को बेहतर सलाह दिए जाने की जरूरत है।
भरोसे की पहल
संपादकीय
सहकारी बैंकों को रिजर्व बैंक की निगरानी में रखने का फैसला केंद्र ने इनके उपभोक्ताओं का भरोसा बढ़ाने और सरकारी योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचाने के मकसद से किया है। पिछले कुछ समय में कई सहकारी बैंकों में घोटाले सामने आने से उपभोक्ताओं का भरोसा कमजोर होने लगा था। खासकर पंजाब एवं महाराष्ट्र सहकारी बैंक में हुए व्यापक घोटाले के बाद सहकारी बैंकों की साख को जबर्दस्त झटका लगा था। उसमें हजारों खाताधारकों का पैसा डूबने का खतरा पैदा हो गया था। तब रिजर्व बैंक के हस्तक्षेप से उन्हें उबारने का प्रयास किया गया। केंद्र के ताजा फैसले से उपभोक्ताओं का भरोसा निस्संदेह बढ़ेगा। सहकारी बैंकों को वित्तीय लेन-देन के क्षेत्र में काम करने की अनुमति देने के पीछे मकसद था कि उनके जरिए छोटी कमाई और निवेश करने वालों को मदद मिलेगी। वे इनके माध्यम से अपने कारोबार आदि को आगे बढ़ाने के लिए कर्ज भी ले सकेंगे। सहकारी बैंकों, समितियों का संचालन चूंकि स्थानीय स्तर पर होता है और उसमें सदस्यों को अपनी सुविधा के अनुसार नीतियां बनाने का अधिकार होता है, इसलिए उन्हें रिजर्व बैंक की निगरानी से दूर रखा गया था। इसी तरह गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां भी काम करती रही हैं। इनका कामकाज बैंकों की तरह होते हुए भी बिल्कुल भिन्न होता है। मगर कुछ सहकारी बैंकों ने नियम-कायदों की अनदेखी करते हुए न सिर्फ अपना आकार बढ़ाना शुरू किया, बल्कि अनियमितताओं के रास्ते भी खोल दिए। इससे स्वाभाविक ही सहकारी बैंकों का मकसद कहीं हाशिये पर चला गया। सरकार के ताजा कदम से उनकी मनमानी रोकने में मदद मिलेगी।
फिलहाल करीब पंद्रह सौ शहरी और अट्ठावन बहुराज्यीय सहकारी बैंक हैं, जिनसे साढ़े आठ करोड़ से ऊपर ग्राहक जुड़े हैं। इन बैंकों के ग्राहक छोटे कारोबारी, अनियोजित क्षेत्रों में काम करने वाले लोग होते हैं। वे अपनी छोटी-छोटी बचत इन बैंकों में रखते और अपने कारोबार आदि के लिए छोटे-छोटे कर्ज लेते हैं। पर कुछ सहकारी बैंक बड़े स्तर पर धोखाधड़ी करने वालों का सहयोग करते देखे गए हैं। जैसे नोटबंदी के दौरान कुछ सहकारी बैंकों ने बड़े पैमाने पर नोट बदले थे। तब भी इन बैंकों पर कड़ी निगरानी रखने की जरूरत रेखांकित की गई थी। पीएमसी जैसे बहुराज्यीय सहकारी बैंक तो अपनी शाखाएं फैलानी और बड़े कारोबारियों को अपने साथ जोड़ कर सरकारी योजनाओं में सेंध लगाना शुरू कर दिया था। सरकार का मकसद है कि देश का हर नागरिक बैंकिंग प्रणाली से जुड़े, ताकि गरीब परिवारों के लिए चलाई जा रही योजनाओं का पैसा उनके खाते में सीधा पहुंच सके। पर सहकारी बैंक इस मकसद में रुकावट पैदा कर रहे थे।
केंद्र ने गरीबों, गरीबी रेखा से नीचे बसर करने वाले लोगों, स्वसहायता समूहों आदि के लिए अनेक योजनाएं चला रखी हैं। कोरोना संकट के समय मुद्रा ऋण योजना के तहत छोटे कर्जदारों को ब्याज में दो प्रतिशत का लाभ देने की घोषणा भी की है। पर सहकारी बैंकों का कारोबार संदिग्ध होने से वे लाभ वास्तविक उपभोक्ताओं तक पहुंचा पाना संदेह के दायरे में आ गया है। सरकार ने अनेक उपभोक्ता वस्तुओं पर से सबसिडी हटा कर उनका पैसा सीधे गरीब नागरिकों के खाते में डालना शुरू किया है। मनरेगा जैसी योजनाओं का पैसा भी सीधे खाते में पहुंचाया जाता है। ऐसे में अगर बैंकिंग प्रणाली में पारदर्शिता नहीं होगी, तो उन योजनाओं का मकसद हाशिए पर जाना स्वाभाविक है। सहकारी बैंको पर रिजर्व बैंक की निगरानी से पारदर्शिता आने की उम्मीद बनी है।
Date:26-06-20
विवशताओं के बीच ग्राम पंचायतें
वीरेंद्र कुमार पैन्यूली
पिछले महीने पंचायत पदाधिकारियों से बातचीत में प्रधानमंत्री ने लौटते प्रवासियों के कारण गांवों में कोरोना संक्रमण के संभावित प्रसार को रोकने में सावधानी बरतने का सुझाव दिया था। तब तक ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक और कृषि गतिविधियां शुरू करना तय हो चुका था। इन दोनों गतिविधियों के संदर्भ में भी गांवों में कोरोना संक्रमण रोकथाम आवश्यक था। स्वाभाविक रूप से औद्योगिक क्षेत्रों, नजदीकी बाजारों और मंडियों में बंदी हटने से गांवों में भीतरी और बाहरी लोगों का आवागमन बढ़ना था। इसलिए गांवों में कोरोना संबंधी दिशा-निदेर्शों के पालन की आवश्यकता थी। पर इनका अनुपालन ग्राम पंचायतों के नेतृत्व में ही होना वांछित है। आखिरकार ग्राम पंचायतें ग्राम सरकार हैं। पर ऐसे में जब ग्राम पंचायतों और उनके पदाधिकारियों को कोरोना योद्धा का सम्मान दिया जाना था, गांव पंचायतों में पर्याप्त धन, कार्याधिकार और कर्मचारियों को आपात स्थिति प्रबंधन के लिए तुरंत पहुंचाया जाना था, उसके बजाय लगभग सभी राज्य सरकारों को संक्रमण संबंधी निगरानी के लिए ग्राम पंचायतों पर हावी होकर काम करवाना आसान लगा। जबकि यह तिहत्तरवें संविधान संशोधन और विभागीय विषयों और कामकाजों में पंचायतों को संवैधानिक मान्यता दिए जाने के बाद नैतिक नहीं है।
पंचायती राज संस्थाओं की अवहेलना पहले भी होती रही है। जिला योजनाएं, जिन्हें नीचे से आए सुझावों के बाद प्रस्तावित और पारित किया जाना होता है उन पर और तत्संबंधी बजट पर प्रभारी मंत्री और जिलाधिकारी कलम चलाते रहे हैं। राज्य सरकारें समय पर पंचायती राज चुनावों को टालती रही हैं। उसी मनोवृत्ति से आज भी जब पंचायतों के पास पंद्रह दिनों तक प्रवासियों को खिलाने, रखने के लिए बजट नहीं है और न पंचायतों के पास इतना धन है कि पहले वे खर्चा करें, बाद में वापसी भुगतान के लिए बिल पेश करें, राज्य सरकारें बिना अग्रिम धन दिए उनसे प्रवासियों के एकांतवास, संपर्क सूत्र तलाश, निगरानी और रिपोर्टिंग जैसे काम कराना चाहती हैं।
बात सिर्फ धनाभाव की नहीं है। सरकारी कर्मचारी, जिनमें शिक्षक और अन्य पेशेवर भी हैं, पंचायतों के अधीन काम नहीं करना चाहते। वे पंचायतों को हीन भाव से देखते हैं। मुख्य सचिव, सचिव या जिलाधिकारी पंचायत कर्मियों को कोरोना संक्रमण से जुड़े मामलों में काम करने के आदेश दे रहे हैं। वे उनसे एक पुलिसिया खबरी के तौर पर भी काम लेना चाहते हैं, जो लुक-छिप कर आने वालों, अपने संपर्कों और यात्रा के विवरण न देने वालों, एकांतवास से भागने वालों की खबर प्रशासन को देते रहें। हिमाचल के मुख्य मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पंचायत प्रधानों को कहा कि वे गांवों में बाहर से आने वालों की सूचना दें तथा जिन घरों में लोगों को एकांतवास में रखा गया है उन घरों में निशान लगाएं और निगरानी करें, ताकि वे एकांतवास का उल्लंघन न करें। बिहार सरकार का भी आदेश है कि राज्यों और जिलों की सीमाओं को पार कर जो लोग लुक-छिप कर गांवों में पहुंच रहें हैं उनकी सूचना ग्राम पंचायतें उन्हे दें और फिर उन्हें एकांतवास में रखा जाए। छत्तीसगढ़, झारखंड, ओड़ीशा सब लगभग ऐसा ही निर्देश अपनी पंचायतों को दे रहे हैं।
चूंकि कोरोना से अब तक की पूरी लड़ाई में आपातकाल-सी स्थिति बना कर केंद्र और राज्य सरकारें तथा नौकरशाही जनता से अपने आदेशों-निदेर्शों का अनुपालन करवाती रही हैं, इसलिए ग्राम पंचायतों के संदर्भ में भी वे उन्हें ग्राम सरकार न मान कर राज्य सरकारों के आधीन अंग या कर्मचारी मान कर व्यवहार कर रहे हैं। अगली कतार के कर्मचारियों का व्यवहार भी कोई भिन्न नहीं रहा है। चोरी-छिपे आने वालों को आपदा प्रबंधन और महामारी नियंत्रण के नियमों के अंतर्गत यहां तक डर दिखाया जा रहा है कि उन पर अपनी यात्रा और संपर्कों आदि की सही जानकारी न देने पर हत्या के प्रयास जैसी धाराओं में मुकदमा दायर हो सकता है, इसलिए प्रधान को मुकदमेबाजी के परिप्रेक्ष्य में भी कानूनी खानापूरी करनी होगी।
एकांतवास केंद्रों में आत्महत्याओं, दुष्कर्मों और नशाखोरी जैसे कृत्य भी हो रहे हैं उसकी जवाबदेही प्रधानों के सिर पर अलग है। स्वास्थ्य सुविधाएं न होने के कारण एकांतवास केंद्रों में बीमारों की हालत बिगड़ने और मौतें भी प्रधान की परेशानी बढ़ा देती हैं। प्रधानों को दस्तावेजीकरण भी करना है- प्रवासी की पिछली यात्रा का इतिहास, उसके संपर्क में कौन आए आदि। जो मास्क नहीं पहन रहा है, जो खुले में थूक रहा है, जो गांव में सामाजिक दूरी का पालन नहीं कर रहा है, उस पर आपराधिक मामले दर्ज कराने लगे, तब तो वह निरंतर मुकदमेबाजी में रहेगा।
जहां तक संस्थागत या घर में एकांतवास में लौटते प्रवासियों को रखने का सवाल है, सालों से बंद, टूट-फूट या अन्य कारणों से जो घर रहने लायक नहीं हैं या जहां पर्याप्त जगह नहीं है, वहां पंचायतें कैसे एकांतवास नियमों का अनुपालन करवा पाएंगी। कई भ्रांतियों के चलते आम जन अपने नजदीक किसी को घर में एकांतवास में भी रखने का विरोध करते हैं। अब तो घरों में एकांतवास में रहते लोगों का विरोध करने के मामले इसलिए भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि नए सरकारी दिशा-निदेर्शों के अनुसार जिन रोगियों में संक्रमण के लक्षण कम हैं, उन्हें अस्पतालों में भर्ती करने की जरूरत नहीं है।
अक्सर पंचायती भवनों और स्कूलों का उपयोग एकांतवास केंद्रों के तौर पर किया जा रहा है, उनमें पानी, बिजली और शौचालयों की बहुत खराब स्थिति है। शौचालयों की गंदगी में उनके उपयोग से भी लोग बचना चाहते हैं। गावों में पंचायतों में सफाईकर्मी न के बराबर हैं। स्कूलों में भी सामान्य समय में भी नियमित सफाईकर्मिर्यों की कमी रहती है। इस सत्य की भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि अब भी कतिपय क्षेत्रों में महिला प्रधानों और अन्य आरक्षित कोटे से जीते पंचायत प्रधानों या पदाधिकारियों को न तो अपेक्षित सम्मान मिलता है और न ही उनको स्वतंत्रता से काम करने दिया जाता है।
ऐसी स्थितियों के बीच ग्राम पंचायतों के माध्यम से कोरोना से लड़ाई में दबंग हावी हो सकते हैं। इस क्रम में एकांतवास तोड़ने या एकांतवास केंद्र अपने आसपास न चाहने वाले दबंगों का कोप भाजन भी बनना पड़ा है। महिला प्रधानों को अकेले ऐसी स्थितियों से निपटना आसान नहीं है। एकांतवास केंद्रों में दुष्कर्म, नशाखोरी के भी समाचार आए हैं। खुलेआम लोग घर-एकांतवास भी तोड़ते दिख रहे हैं। लोगों में आपसी मनमुटाव भी हो रहे हैं। पर्याप्त संसाधनों के अभाव में पंचायतों को लौटते प्रवासियों को एकांतवास करने की जिम्मेदारी देने को ज्यादातर लोग न्यायसंगत नहीं मानेंगे।
निस्संदेह ग्राम पंचायतों को अपनी-अपनी ग्राम सभाओं के प्रति तो जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। उपराष्ट्रपति वेंकया नायडू ने भी इस बार के पंचायती राज दिवस पर कहा था कि पंचायतों को अपनी जिम्मेदारी निर्वहन के लिए फंड, फंक्शन और फंक्शनरी दिए जाने चाहिए। यानी उन्हे धन मुहैया कराना चाहिए, उन्हें कार्य सौंपे जाने चाहिए और कर्मचारी, कार्यकर्ता दिए जाने चाहिए। जब गाम पंचायतों को काम सौंपा गया है, तो उन्हें उसके लिए धन भी दिया जाना चाहिए और उपयुक्त स्वास्थ्य और सुरक्षा कर्मचारी भी दिए जाने चाहिए। राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों से भी उनकी योजनाओं को जानने के लिए अनुरोध करना चाहिए, न कि उन्हें आदेशित-निर्देशित करना चाहिए।
स्पष्ट है कि विकेंद्र्रित रणनीति के जरिए ही कोरोना को हराया जा सकता है। इसके लिए ग्राम पंचायतों में रणनीति बनाने की क्षमता बढ़ाना आवश्यक है। खुद पंचायतों को भी ऐसे नवाचार और पहल करनी चाहिए, जिससे वे राज्य सरकारों की खबरी बने रहने के बजाय अपने से ग्राम सभाओं में नियोजन और कार्यान्वन के लिए इस दीर्घावधि दिख रहे कोरोना काल के लिए अपेक्षित धन, सहूलियतें और कर्मचारियों को जुटा सकें।
सही फैसला
संपादकीय
केंद्र सरकार ने एक महत्त्वपूर्ण फैसले में देश के सभी सहकारी बैंकों और बहुराज्यीय सहकारी बैंकों को रिजर्व बैंक के निरीक्षण के दायरे में लाए जाने की घोषणा की है। माना जा रहा है कि रिजर्व बैंक की देखरेख में इन बैंकों का परिचालन बेहतर ढंग से हो सकेगा। अब तक रिजर्व बैंक केवल वाणिज्यिक बैंक की ही देखरेख करता है। पिछले कुछ समय से देश के कई सहाकारी बैंकों में घोटालों के मामले आते रहे हैं। इसके कारण सहकारी बैंकों के जमाकर्ताओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दरअसल, घोटाले के कारण बैंक के कामकाज पर लंबे समय तक रोक लग जाती है,जिसके कारण जमाकर्ता ग्राहकों को अपना ही पैसा निकालने के लिए लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है। यही नहीं सहकारी बैंकों में होने वाले भ्रष्टाचार और घोटालों के कारण जमाकर्ताओं के मन में अपनी पूंजी डूबने की आशंका बनी रहती है। अभी पिछले ही दिनों पंजाब एंड महाराष्ट्र सहकारी बैंक में घोटाले का मामला उजागर हुआ था। इसके बाद बैंक के जमाकर्ताओं को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। इन घोटाले के बाद पूरे देश में हर रोज नई-नई अफवाहें भी फैल रही थीं। इसलिए सरकार सहकारी बैंक के जमाकर्ताओं की पूंजी को सुरक्षित रखने के लिए इन बैंकों को रिजर्व बैंक के देखरेख में लाने का फैसला करना पड़ा है। इसके लिए सरकार को बैंकिंग नियमन अधिनियम में संशोधन करना पड़ा। अब जल्द ही सरकार इस आशय का अध्यादेश लाएगी। अब तक सहकारी बैंक सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार द्वारा निर्धारित नियमों के अधीन काम करती रही हैं। सहकारी बैंक छोटे वित्तीय संस्थान हैं, जो कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र के किसानों के विकास में मदद करने के लिए ऋण देते हैं। जैसा कि नाम है उसी के अनुरूप इन बैंकों की स्थापना सहयोग और सहकार की अवधारणा पर की गई थी। व्यक्तियों के समूह या संस्थाओं द्वारा किसी समान उद्देश्य की प्राप्ति करने के लिए जो प्रयास किए जाते हैं, उसे सहकार कहा जाता है। किसानों को बिचौलिये और साहूकारों के शोषण से बचाने में सहकारी बैंकों की अग्रणी भूमिका रही है, लेकिन देश में माफिया तंत्र और भ्रष्ट अधिकारियों के चलते इन सहकारी बैंकों की हालत खराब होती चली गई। उम्मीद की जाती है कि सरकार के इस फैसले के बाद सहकारी बैंक अपनी भूमिका का अच्छी तरह निर्वाह कर पाएंगे।
बड़ी ताकतों से संतुलन साधने के निहितार्थ
जोरावर दौलत सिंह, फेलो, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च, दिल्ली
भारत और चीन के बीच 15 जून की झड़प ने आखिरकार हिमालयी सीमा पर शांति के चार दशक के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। चीन द्वारा हड़पी गई जमीन को खाली कराने से लेकर शीत युद्ध के आह्वान तक प्रतिक्रियाएं तीखी रही हैं। साल 1950 से न सही, इधर दो दशकों से चीन की बढ़त की चर्चा चल रही है। भारत-चीन संबंधों ने बहुत कुछ देखा है, जुड़ाव से लेकर वर्ष 1959 के नाटकीय अलगाव तक। 1962 में एक छोटा, पर घातक युद्ध हुआ और उसके बाद के दशकों में न युद्ध-न शांति की स्थिति रही। आखिरकार 1988 में दोनों देशों को कूटनीतिक सफलता मिली और संबंधों में एक सलीका बना, जिसके तहत सीमा विवादों को सुलझाए बिना आगे बढ़ने की राह बनी। मूल आधार यह था कि शांतिपूर्ण दायरे में संबंधों में विकास की रफ्तार रहेगी, मगर 15 जून की झड़प से दोनों देशों के बीच रही सहमति पर चोट पड़ी है।
स्पष्ट है, रिश्ते का अगला चरण एक शांतिपूर्ण सीमा पर निर्भर है, मगर इसका अर्थ सिर्फ यथास्थिति की बहाली नहीं होनी चाहिए। यदि यथास्थिति से हमारा आशय दो परमाणु संपन्न बड़े देशों से है, जो फिर से आक्रामक कवायद शुरू कर रहे हैं, तो यह स्थिति ज्यादा नहीं टिकने वाली। अब समीक्षा और एक नए संघर्ष-प्रबंधन ढांचे को लागू करने का समय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस विवाद को क्यों नहीं सुलझा सकते? चीनी विद्वान यूं सन ने समाधान में बाधा डालने वाली प्रमुख समस्या का एक सारांश पेश किया, ‘चीन के साथ सीमा समाधान में भारत जो रियायतें चाहता है, वे कठोर प्रतिबद्धताएं हैं, जिन्हें बाद में पलटा नहीं जा सकता। इसके विपरीत, चीन अमेरिका-चीनी रणनीतिक प्रतिस्पद्र्धा में भारत की तटस्थता चाहता है, जो अल्पकालिक और आसानी से समायोज्य है।
रणनीतिक इरादों में अनिश्चितता की इस समस्या का निकट भविष्य में कोई कारगर समाधान नहीं है। हालांकि नए मानदंडों के जरिए सीमा स्थिर करना दोनों देशों के हित में संभव है। सबसे विवादास्पद है सीमा पर अनेक स्थानों पर बफर जोन में रचनात्मक दृष्टि रखना और हिंसक झड़पों से बचने के लिए समन्वय के साथ गश्ती की व्यवस्था करना। नई व्यवस्था बनाने के लिए यह जरूरी है। उत्साह या बड़बोलेपन में कई लोगों ने भारत-चीन संबंधों के टूटने की घोषणा तक कर दी। हमें ऐसे अतिरेक या आक्रामकता से बचना है। दोनों देशों के बीच रिश्ते कोई अचानक मुश्किल में नहीं पड़े हैं, इसके संकेत कुछ समय से स्पष्ट मिल रहे थे।
वास्तव में, हमारी चीन नीति असम्मत रही है। बेल्ट रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) से नौसेना सुरक्षा और 5-जी की उच्च तकनीक तक, दिल्ली अपनी बयानबाजी व कार्यों में मुखर रही है। यहां तक कि भू-राजनीतिक क्षेत्र में अमेरिका को जोड़ने में भी भारत नाकाम ही हुआ है। एशिया में भी दिल्ली चीन के पड़ोसियों को भविष्य की बाधा के रूप में आंकती रही है। पारंपरिक सहयोगी रूस के साथ भी हाल के वर्षों में सरकार की नीति पुरानी भू-रणनीति की याद दिलाती है। हमारे नीति-निर्माताओं की इस बात के लिए आलोचना की जा सकती है कि वे विश्वसनीय रणनीति के बिना ही चीन के संदर्भ में प्रतिस्पद्र्धात्मक कदम उठाते रहे। नई दिल्ली की असली नाकामी यह है कि व्यापक विदेश नीति के ढांचे में उसकी नीतिगत कथनी और करनी मेल नहीं खा रही हैं। चीन के साथ निरंतर जुड़ाव बहुध्रुवीय दुनिया में अग्रणी शक्ति के रूप में उभरने की एक भव्य रणनीति का हिस्सा था। इसकी बजाय, दिल्ली ने खुद को खाली खजाने व अप्रत्याशित साझीदारों के साथ चीन के खिलाफ कर लिया है। इतिहास बताता है, जब बड़ी ताकतों के साथ भारत के सकारात्मक व सशक्त संबंध थे, तब उसे चीन गंभीरता से लेता था। इतिहास यह भी दर्शाता है कि भारत के लिए शक्ति का संतुलन किस हद तक फायदेमंद हो सकता है।
भारत-अमेरिका और भारत-सोवियत (रूस) संबंधों ने भारत-चीन संबंधों को स्थिर रखने का काम किया और तभी भारत अपने हितों को पहचानने व आगे बढ़ाने में मजबूती से बना रहा। ऐसा तभी हुआ, जब स्थितियां भारत के अनुकूल थीं और वह चीन के साथ परस्पर लाभप्रद संबंधों को आकार देने में सक्षम था। तभी अंतरराष्ट्रीय माहौल का चतुराई से लाभ उठाने और एक परिष्कृत चीन नीति बनाए रखने में भी भारत ज्यादा सक्षम था।
