
23-06-2025 (Important News Clippings)
To Download Click Here.

Date: 23-06-25
Coding For The End
UK’s assisted dying bill is a momentous law. The conversation must start in India
TOI Editorials
Third time lucky. After rejecting versions of the bill in 1997 and 2015, UK lower house voted for a law to allow assisted dying in England and Wales. This means patients terminally ill, as defined in law, and likely to die within six months, can apply for an exit. The legislation will have to be set in motion within four years (2029). If delayed in the Lords – it’s highly contested and the lower house win was by just 23 votes – the bill will lapse. It may not be done and dusted yet, but a historic social change has begun. Exhaustive debates and tweaks to the bill included dropping provision of a judge having to sign off on the decision. Importantly, no other person is ‘obliged’ to take part. Patients will have to administer the drugs, whatever is decided, themselves, so it’s a first step to active euthanasia. Reportedly, UK govt estimates there may be 4,000 such patients.
To legislate on assisted dying is never a straight road in any country. Fears and concerns are real that vulnerable, disabled and older people risk being coerced to use the law, to reduce the financial and care burden on the family. UK bill’s penalty for coercion is a 15-year jail. While such fears have been voiced to reject assisted dying, the Indian reality is that terminally ill people and families are often left to fend for themselves as a result of lack of access to treatment and/or unaffordability of care. At the privileged end of affordability/access, there is little policy or regulations to limit life-sustaining interventions inappropriate at end-of-life stage. The Supreme Court upheld advanced directives, the right to refuse treatment: passive euthanasia. UK’s bill is an opportunity to take further the conversation around a 360-degree end-of-life care that includes palliative care and covers assisted dying for the terminally ill.
अब तो खुलें दुनिया की आंखें
संपादकीय
इजरायली हमलों से दो-चार ईरान पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहते हुए उसके तीन परमाणु ठिकानों पर बम बरसाए कि ईरान आतंक का समर्थन करने वाला दुनिया का नंबर एक देश है। ईरान पर अमेरिकी हमले की विश्व भर में प्रतिक्रिया के बीच कश्मीर से आई खबर से यह स्पष्ट हुआ कि पहलगाम पर बर्बर आतंकी हमला पाकिस्तान से आए लश्कर के तीन आतंकियों ने किया था।
इन तीन आतंकियों को शरण, समर्थन और सहयोग देने वाले पहलगाम के ही दो कश्मीरियों-परवेज अहमद और बशीर अहमद को एनआइए ने गिरफ्तार किया। इन दोनों ने यह माना कि उन्हें पता था कि पाकिस्तान से आए आतंकियों का इरादा क्या था। पूरी दुनिया को पता है कि इन आतंकियों ने पहलगाम में 26 निर्दोष लोगों को उनका मजहब पूछकर बर्बर तरीके से मारा।
इस दिल दहला देने वाले आतंकी हमले की सारी दुनिया और यहां तक कि पाकिस्तान के साथ खड़े चीन, तुर्किये आदि ने भी निंदा की, लेकिन जब भारत ने जवाब में आपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के नौ प्रमुख आतंकी अड्डों को ध्वस्त किया तो कई देशों के सुर बदल गए। पाकिस्तानी सेना ने अपने आतंकी अड्डों को नष्ट किए जाने से चिढ़कर भारत पर ड्रोन और मिसाइल दागने की कोशिश की, लेकिन भारत ने उसके कई एयरबेस तबाह करने के साथ उसकी सेना को पंगु बना दिया।
यह आश्चर्यजनक है कि चीन और तुर्किये तो पाकिस्तान के साथ खुलकर खड़े हुए ही, अमेरिका एवं अन्य पश्चिमी राष्ट्र यह कहने से साफ-साफ बचे कि भारत ने पाकिस्तान पर जो सैन्य कार्रवाई की वह उचित है और ऐसा करना उसका अधिकार था। कई देश तो भारत को उपदेश देने लगे कि वह सैन्य टकराव टालने की कोशिश करे।
जब पाकिस्तानी सेना ने भारतीय सेना की आक्रामकता से बचने के लिए चीन, अमेरिका के साथ भारत से भी संपर्क किया तो भारत ने सैन्य कार्रवाई स्थगित कर दी, लेकिन ट्रंप इसका श्रेय लेने में जुट गए कि उन्होंने कथित संघर्ष विराम कराया और दोनों देशों को परमाणु युद्ध से बचा लिया। यह दावा सही नहीं था और अब तो इसकी पुष्टि हो गई कि अमेरिकी राष्ट्रपति फर्जी दावा कर रहे थे।
उनके इस दावे पर भारतीय प्रधानमंत्री ने उन्हें आईना भी दिखाया। इसके बावजूद अपने पहले कार्यकाल में पाकिस्तान से धोखा खाने वाले ट्रंप उसे अपना प्रिय देश बताने लगे और हद तो तब हो गई जब उन्होंने पाकिस्तान के जिहादी सोच वाले सेना प्रमुख आसिम मुनीर को वाशिंगटन बुला लिया।
अच्छा हो कि अमेरिका सहित विश्व के प्रमुख राष्ट्रों की आंखें खुलें और वे आतंकवाद पर अपनी निर्लज्ज दोहरी नीति का परित्याग करें। भारत को इस दोहरे आचरण के संदर्भ में अपनी बात जोर-शोर से कहनी होगी-विशेषकर पाकिस्तान के नए-पुराने हमदर्द चीन और अमेरिका के समक्ष तो और अधिक मजबूती के साथ।
जवाबदेही है जरूरी
संपादकीय
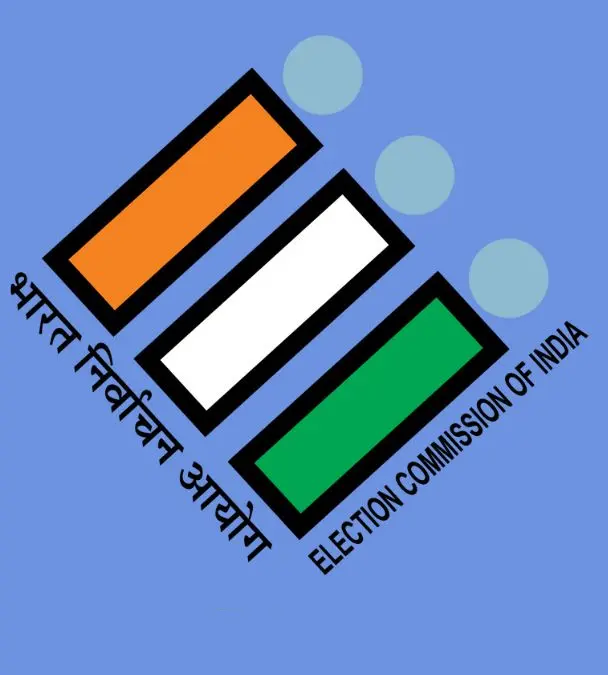
चुनाव आयोग ने कहा है कि मतदान केंद्रों की वेबकास्टिंग फुटेज सार्वजनिक करना सही नहीं है। इससे मतदाताओं या समूहों की पहचान करना आसान हो जाएगा। मत देने या मत न देने वाला, दोनों ही असामाजिक तत्वों के दबाव, भेदभाव या धमकी का शिकार हो सकते हैं। यह मतदाताओं की सुरक्षा, गोपनीयता व जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950-51 में निर्धारित कानूनी प्रावधानों व सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन होगा। लो सभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को दिए जवाब में आयोग ने यह कहा जिसमें चुनाव धांधली के आरोपों के बाद सीसीटीवी फुटेज की मांग की गई थी। इससे पहले गांधी ने सोशल माडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, वोटर लिस्ट ? मशीन रीडेबल फार्मेट नहीं देंगे, सीसीटीवी फुटेज ? कानून बदल कर छिपा दी। आगे उन्होंने लिखा- साफ दिख रहा है – मैच फिक्स है और फिक्स किया गया चुनाव, लोकतंत्र के लिए जहर है। दरअसल, आयोग के अनुसार, चुनाव के दौरान ली गईं तस्वीरें, वीडियो व बेवकास्टिंग सिर्फ पैंतालीस दिन तक सुरक्षित रखी जाएंगी। किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव नतीजों को अदालत में चुनौती नहीं दी जाती तो पैंतालीस दिन बाद यह डाटा नष्ट कर दिया जाएगा। कांग्रेस इसका शुरू से ही दोहरा रही है कि यह डाटा साल भर तक सुरक्षित रखा जाता था। कांग्रेस इसे चुनाव आयोग व मोदी सरकार की मिली भगत ठहराते हुए लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म करने की साजिश बता रही है। बेशक, आयोग के तर्क अपनी जगह उचित हैं मगर उसे सरकार के दबाव में आए बगैर अपनी स्वायत्तता का ख्याल रखना चाहिए। विपक्षी दलों की दलीलें सुनना उसका जिम्मा है। आशंकाओं व चिंताओं को मिटाने के प्रति उसे जवाबदेह भी होना होगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था में न केवल विपक्षी राजनीतिक दल, बल्कि स्वयं मतदाता भी अपनी जिज्ञासाएं रखने को स्वतंत्र है। मतदाताओं की सुरक्षा व गोपनीयता निश्चित रूप से बेहद जरूरी हैं। मगर अपने उम्मीदवार के पक्ष-विपक्ष या धांधली के आरोपों की पुष्टि कराना भी दलों का जिम्मा है। अव्वल तो गांधी को बगैर सबूतों के इतने गंभीर आरोप लगाने से बचना चाहिए परंतु आयोग को भी उनकी आशंकाएं मिटाने का भरपूर प्रयास करना होगा। पैंतालीस दिन किसी भी आशंका या आरोप के लिए कम नहीं कहे जा सकते। आयोग को वरिष्ठ पदाधिकारियों को बुला कर अति सुरक्षित व गोपनीय व्यवस्था में विवादित फुटेज दिखाने का प्रावधान भी जोड़ना होगा । लोकतांत्रिक व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही अति आवश्यक है।
Date: 23-06-25
महाशक्ति बनने की निर्भरता जरूरी
हरीश शिवनानी
पूरी दुनिया का ध्यान इस समय जब ईरान- इस्राइल और गाजा संघर्षों में उलझा है, इसी दौर में भारत, अमेरिका सहित अनेक देश एक अन्य महत्त्वपूर्ण मुद्दे पर उलझे हैं। यह मुद्दा है धरती के गर्भ में पाए जाने वाले उन 17 दुर्लभ खनिजों का जिनके बगैर ऑटोमोबाइल और सैन्य-रक्षा सहित विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों का निर्माण संभव नहीं है। पिछले कुछ महीनों में हालात ज्यादा विकट होने चले हैं। ‘रेअर अर्थ’ की श्रेणी में आने वाले दुर्लभ खनिज वाणिज्यिक, औद्योगिक संसाधन भर नहीं हैं, ये तकनीकी संप्रभुता, रक्षा तैयारियों और औद्योगिक, आर्थिक और सैन्य महाशक्ति बनने की संभावनाओं की नींव हैं।
रेअर अर्थ मेटल 17 धातु तत्वों का एक समूह है, जिसमें 15 लैंथेनाइड्स धातुओं के अलावा स्कैंडियम भी और नियोडिमियम शामिल हैं। इनमें चुंबकीय, ल्यूमिनसेंट और इलेक्ट्रोकेमिकल के विशेष गुण होते हैं, जिनका उपयोग आधुनिक उच्च तकनीक उद्योग में किया जाता है। स्मार्टफोन, लैपटॉप और इलेक्ट्रिक वाहन बनाने के साथ मिसाइल, राडार और अत्याधुनिक हथियार बनाने के लिए ये ‘अनिवार्य तत्व’ हैं। रेअर अर्थ मैग्नेट सामान्य आयरन मैग्नेट से 20 गुना अधिक ताकतवर होता है, और कारों तथा कई अन्य उपकरणों में लगने वाली इलेक्ट्रिक मोटरों को बनाने के लिए जरूरी है। यूएस भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण डेटा पर आधारित एक नये ग्लोबल मैप के मुताबिक यों तो कई देशों में इन दुर्लभ तत्वों के भंडार हैं, लेकिन सर्वाधिक चीन में 44 मिलियन मीट्रिक टन भंडार हैं। चीन के बाद अफ्रीका, मोरक्को और दक्षिण अफ्रीका, चिली, ब्राजील, यूक्रेन और ग्रीनलैंड में दुर्लभ अर्थ मेटल्स के विशाल भंडार हैं। दिक्कत यह है कि इन देशों में इनकी खुदाई और प्रोसेसिंग महंगी है। इससे भारी मात्रा में प्रदूषण भी निकलता है। इन सब में चीन के पास ही इनकी प्रोसेसिंग की क्षमता है। वर्तमान में दुर्लभ पृथ्वी धातुओं का 61 प्रतिशत भंडार चीन में है, और पूरी दुनिया में 90 फीसद का वही निर्यात करता है।
इन तत्वों को एक-दूसरे से अलग करना जटिल है। इसीलिए इन्हें ‘रेअर’ माना जाता है। रेअर अर्थ की वैश्विक सप्लाई चेन में चीन का दबदबा है। आधुनिक इंडस्ट्री में इनका महत्त्व यों समझा जा सकता है कि चीन ने जब अप्रैल में रेअर अर्थ मैग्नेट समेत छह तरह की बहुमूल्य धातुओं के निर्यात पर रोक का फैसला किया तो वैश्विक कंपनियों में खलबली मच गई और ऑटोमोबाइल उद्योग को विशेष रूप से झटका लगा क्योंकि इलेक्ट्रिक वाहनों में इस्तेमाल होने वाले शक्तिशाली इंजन मैग्नेट नियोडिमियम से बनते हैं ।
भारत में भी टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, बजाज मोटर्स दबाव में आ गए। सुजूकी कंपनी को अपनी स्विफ्ट कार का निर्माण कुछ समय के लिए स्थगित करना पड़ा। ऐसा नहीं है कि भारत में ये दुर्लभ तत्व नहीं मिलते; भारत के पास तो विश्व में पांचवा सबसे बड़ा दुर्लभ खनिज भंडार है – करीब 6.9 मिलियन मीट्रिक टन दुनिया में भारत की हिस्सेदारी छह फीसद है। इनमें केरल में थोरियम सैंड के अलावा आंध्र प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान में भी इनके भंडार हैं; लेकिन दुनिया भर की आपूर्ति का भारत में एक प्रतिशत हिस्सा ही उत्पादित होता है। इन खनिजों की तलाश, खदान का काम मोटे तौर पर सरकार के जिम्मे रहा है। ब्यूरो ऑफ माइंस और परमाणु ऊर्जा विभाग ये काम करते हैं। खनन और शोधन का काम ‘इंडियन रेयर अर्थस लिमिटेड’ के पास रहा है, लेकिन यह विडंबना है कि भारत अभी ऐसी तकनीक, मैकेनिज्म नहीं खड़ा कर पाया है, जो इन खनिजों से मैग्नेट बना कर खुद की जरूरतें पूरी कर सके।
भारत में जितने भी दुर्लभ अर्थ मैग्नेट उपयोग में आते हैं, वे अधिकतर चीन से आयात किए जाते हैं। 2023-24 में भारत ने 2270 टन और पिछले वित्तीय वर्ष में 53,748 मीट्रिक टन मैग्नेट आयात किए थे। इनका करीब अस्सी फीसद चीन से आयात हुआ । इस हालात को देखते हुए भारत ने अपने दुर्लभ खनिजों को रणनीतिक संपत्ति की तरह देखना शुरू कर दिया है। इसी रणनीति के चलते भारत ने पिछले 13 वर्षों से जापान के साथ चल रहे समझौते को निलंबित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसके तहत ‘इंडियन रेयर अर्ड्स लिमिटेड’ द्वारा खनन किए गए खनिज विशेषकर नियोडिमियम जापान भेजे जाते थे, लेकिन भारत ने तय किया है कि अपने घरेलू उद्योगों की जरूरतों को प्राथमिकता देगा और चीन पर निर्भरता कम करेगा। भारत के लिए वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बनने के लिए यह अब अनिवार्य हो गया है कि दुर्लभ तत्वों की तकनीक में अपने प्रतिद्वंद्वी देश पर निर्भरता को घटाते हुए वह आत्मनिर्भरता के प्रयासों में तेजी लाए।
Date: 23-06-25
युद्ध की आंच से कोई न रहेगा अछूता
अलोक जोशी

इजरायल – ईरान जंग में जिस बात की आशंका थी, वह घटित हो चुकी है। ईरान के तीन परमाणु केंद्रों- फोडों, नतांज और इस्फहान पर हमले के साथ अमेरिका इस युद्ध में कूद पड़ा है। खबरें हैं, ईरान में युद्ध संबंधी रणनीतिक फैसले लेने वाली शीर्ष कमेटी ने होर्मुज जलडमरूमध्य मार्ग को बंद करने की सिफारिश की है। अब तो इस क्षेत्र से जहाजों के हटने की सूचनाएं भी आने लगी हैं। साफ है, यह युद्ध बढ़ गया है। सवाल है, इस मार्ग की इतनी चर्चा क्यों हो रही और इसके बंद होने से हम पर क्या असर होगा ? असल में, भारत से स्थल मार्ग से यूरोप जाना हो, तो सबसे अच्छा रास्ता अफगानिस्तान और ईरान होकर निकलता है, और समुद्र से जो रास्ता बनता है, वह अगर जमीन साथ-साथ चले, तो फिर ईरान के पास, यानी ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी होकर जाता है। यहीं है होर्मुन जलडमरूमध्य जहां से दुनिया के सबसे ज्यादा तेल टैंकर गुजरते हैं। इस मार्ग की अहमियत इससे समझिए कि कच्चे तेल या तैयार पेट्रोलियम उत्पादों के अंतरराष्ट्रीय कारोवार का करीब पांचवां हिस्सा इसी जलमार्ग से गुजरता है।
इजरायल की सैन्य व गुप्तचर क्षमता के जो कसीदे पढ़े जाते रहे हैं, उनसे लगता था कि ईरान तुरंत घुटनों पर आ जाएगा। मगर ईरान ने जैसा जवाबी हमला किया, उससे पूरी दुनिया चौंक गई और अब तो साफ लगने लगा है कि संघर्ष जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। अगर यह युद्ध जल्दी खत्म नहीं हुआ, तो पहले से खस्ताहाल दुनिया की अर्थव्यवस्था और भी बड़ी परेशानी में घिर सकती है। इसके संकेत दिखने भी लगे हैं। एक बैरल कच्चे तेल के दाम एक दिन में ही दस डॉलर उछलकर 78 डॉलर पर पहुंच गए थे, हालांकि, उसके बाद कुछ नरमी दिखी, लेकिन ऐसी भी नहीं कि लोग निश्चिंत हो सकें।
कच्चे तेल के कारोबार पर नजर रखने वाले ज्यादातर लोग आज चिंतित हैं और काफी डरावनी भविष्यवाणी भी कर रहे हैं। उनमें से ज्यादातर का मानना है कि कच्चा तेल 78 डॉलर प्रति बैरल के नीचे तो नहीं ही टिकेगा, हालात बिगड़े, तो यह 120 से लेकर 140 डॉलर तक की ऊंचाई भी दिखा सकता है। हालांकि, अभी तक तेल के दामों पर बहुत असर नहीं दिखा था, तो इसकी एक बड़ी वजह यह रही कि इजरायल या अमेरिका की तरफ से किसी कार्रवाई की आशंका में ईरान तेजी से अपने भंडार का तेल निर्यात करने में जुट गया था। सैटेलाइट तस्वीरों और आंकड़ों के आधार पर टैंकर ट्रैकर्स वेबसाइट ने इसकी जानकारी दी है। जानकारों का कहना है कि ईरान न सिर्फ अपने भंडार का तेल निर्यात कर रहा है, बल्कि उसी तेजी से तेल निकालकर भंडारों में डाल भी रहा है। उसकी कोशिश है कि अमेरिका के युद्ध में शामिल होने से पहले वह ज्यादा से ज्यादा तेल निर्यात कर दे।
हालांकि, इस किस्से का एक अन्य पहलू भी है कि तेल या पेट्रोलियम उत्पादों का व्यापार दुनिया की राजनीति में बहुत अहम भूमिका निभाता रहा है। इसलिए यहां बहुत सारे निहित स्वार्थ तरह-तरह के कथाक्रम बताते मिलते हैं। एक तरफ कहा जा रहा है कि ईरान जल्दी से जल्दी तेल निकालकर बेचने में जुटा है, तो दूसरी तरफ यह भी बताया जा रहा है कि चीन के तट के पास ईरान के तेल टैंकरों में करीब चार करोड़ बैरल कच्चा तेल खरीदारों का इंतजार कर रहा है।
ईरान के कच्चे तेल का सबसे बड़ा खरीदार चीन है। हालांकि, वह काफी सस्ते दाम पर यह तेल खरीदता है। मगर जानकारों का कहना है कि इस वक्त चीन में तेल की मांग काफी कम हो गई है। दरअसल, वहां इलेक्ट्रिक कारों का चलन बढ़ना इसकी बड़ी वजह है। इसीलिए वहां के तेल शोधन या रिफाइनिंग में भी पिछले महीने 1.8 प्रतिशत की गिरावट दर्ज हुई है, यानी ईरान का तेल कहां बिकेगा, यह सवाल बड़ा हो रहा है।
यह वाकई चिंताजनक परिदृश्य है, अगर ईरान ने होर्मुग के रास्ते जहाजों का आना-जाना बंद कर दिया, तो अनेक देशों के लिए संकट खड़ा हो जाएगा। भारत के लिए यह मुश्किल चुनौती है, क्योंकि इसका आधे से ज्यादा प्राकृतिक गैस और 40 प्रतिशत कच्चा तेल इसी रास्ते से आते हैं। शायद इसीलिए केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि फिलहाल हमारे पास पेट्रोलियम पदार्थों का पर्याप्त भंडार है। साथ ही, उन्होंने यह भी कहा कि अगर हालात ऐसे ही बने रहे, भारत फारस की खाड़ी के बाहर के स्रोतों और रास्तों से कच्चे तेल के आयात पर विचार कर रहा है।
यह तो रही होर्मुज मार्ग बंद होने की बात, यदि यह खुला भी रहा, तब भी जोखिम बढ़ने के कारण इससे आने वाले जहाजों का बीमा प्रीमियम 60 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ चुका है। इसका असर सिर्फ कच्चे तेल की आवक पर नहीं, बल्कि भारत से समुद्री रास्ते से होने वाले ज्यादातर निर्यात पर भी पड़ना तय है। वहीं, भारत से यूरोप या अमेरिका की तरफ जाने वाली उड़ानों को अब ईरान या युद्धक्षेत्र से बचकर निकलना होता है। इसकी वजह से यात्रा का समय, दूरी और खर्च बढ़ गया है। हवाई किराये में बढ़ोतरी इसका स्वाभाविक असर है। पेट्रोल-डीजल के दामों में वृद्धि शायद तत्काल न हो, लेकिन पेंट, साबुन जैसे जिन उद्योगों में कच्चा माल पेट्रोलियम उत्पादों से आता है, वहां महंगाई बढ़ने का डर शुरू हो गया है।
सबसे चिंताजनक स्थिति अर्थव्यवस्था वा सरकारी खजाने के लिए हो सकती है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इका ने हिसाब लगाया है कि अगर होर्मुज समुद्री मार्ग बंद हुआ, तो भारत को सिर्फ पेट्रोलियम आयात के खाते में हो अरबों डॉलर की चपत लग सकती है। ईरान पर इजरायली हमले के पहले कच्चे तेल का दाम 64-65 डॉलर प्रति बैरल था। एजेंसी का कहना है, इसमें दस डॉलर की बढ़त पर ही भारत को करीब 14 अरब डॉलर ज्यादा चुकाने पड़ेंगे और सरकारी घाटे में जीडीपी का 0.3 प्रतिशत का बोझ बढ़ जाएगा।
भारत अपनी जरूरत का 80 फीसदी कच्चा तेल आयात करता है। और अगर कहीं तेल का दाम 120 से 140 बैरल की तरफ चढ़ने लगा, तब कल्पना ही की जा सकती है कि सरकारी खजाने को कैसा झटका लगेगा। तब महंगाई को दोबारा फन उठाने से रोकना असंभव होगा। ऐसे में, कामना यही करनी चाहिए कि अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच जल्दी शांति कायम हो एवं यह खतरा जल्द से जल्द टल जाए।
