
18-07-2025 (Important News Clippings)
To Download Click Here.

Date: 18-07-25
Fuel Folly
Washington’s new tariff plan for those who buy Russian oil is hypocritical & will hurt US too
TOI Editorials
After insulting Zelenskyy in Feb, pausing intelligence sharing with Kyiv in March, and weapons supplies in March and May, Trump finally has a plan to stop Putin. He’s going to hit Russia and its trade partners with “very serious tariffs”. Not immediately-Putin gets 50 days to finish the business he started in 2022. But as a big buyer of Russian oil, India should take note. Trump’s threatened to impose 100% tariff on countries that buy Russian goods after the expiry of his deadline, and if he doesn’t waver, or forget-neither unlikely-the concessions won through a trade deal could be lost.
Will tariffs work? Not directly, because Russia and US have never been more decoupled economically since the collapse of Soviet Union. US bought goods worth just $3bn from Russia last year, and sold $500mn worth, down from $29bn and $6bn, respectively, before the start of the war in 2022. That’s why Putin must be checkmated through secondary tariffs on his major oil buyers like China, India and Brazil.
Fossil fuels are a very big part of Russia’s GDP (16%), and make up over half of its exports (55%). By the third anniversary of the war, Russia had earned about $1tn from fossil fuel exports. India, which used to buy just 1% of its oil from Russia before the war, now sources 40%, so the threat of 100% tariff on exports could make it pivot again. And China, which buys 20% of its oil from Russia, might also find 100% tariff discouraging.
Russia could be hurt, but at what cost? Plugging the Russian pipeline is bound to drive up oil prices, which could increase inflation in most places, including US. Add to that the US-specific price rise resulting from 100% tariff on China, India and other US trade partners, and the political risk might be too much for Trump’s Republicans.
Above all, Trump’s threat-backed by Nato secretary-general Mark Rutte – smacks of hypocrisy. After ordering the world not to buy Russian oil, US continued buying enriched uranium from Russia for its nuclear plants. Even when it announced a ban on Russian uranium imports from 2027, it gave a waiver to its largest operator of reactors. Likewise, Rutte’s Europe is still buying gas from Russia, and won’t stop till the end of 2027. So, Trump and Rutte’s threat is less about conviction than convenience. India must play by the same rule.
Date: 18-07-25
Adding Muscle to SBI’s Core Strength
Bank’s move may trigger other PSB issues
ET Editorials
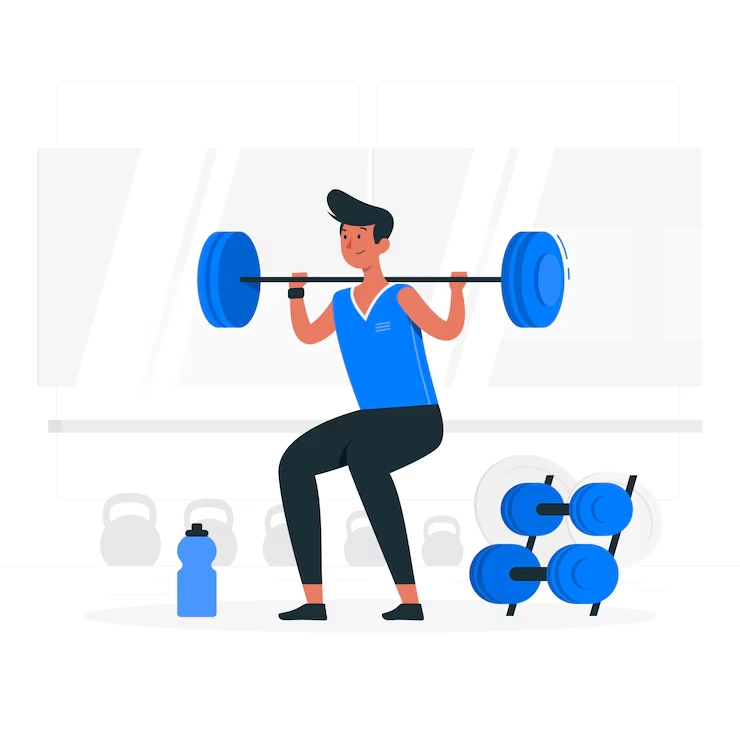
SBI is raising equity from institutional investors to bolster its capital base amid a strong cycle, with the *25,000 cr Qualified Institutional Placement (QIP) having started on Wednesday. The share sale will be followed by a *20,000 cr bond issue, together amounting to ₹45,000 cr and strengthening the country’s largest bank. SBI has seen its market capitalisation more than double since the pandemic, but its capital adequacy has been trailing profits. The equity and bond issues are designed to set that balance right. The bank maintains a higher capital buffer because of its systemic importance, and this round of fundraising will augment it. Gol’s stake in the bank will come down slightly but will stay well above a majority holding.
The issue represents a strengthening of the health of PSBs that GoI had to recapitalise during a bad loan crisis a decade ago. But in recent years, stateowned banks have outpaced their private sector rivals in feeding India’s post-Covid credit recovery. Their financial metrics are improving, and they will find the capital markets supportive. Tapping markets is also a good option when the pace of raising deposits trails credit growth. Banks have been lending aggressively to households to feed a consumption boom. Economic and demographic changes are affecting household savings behaviour and diverting a bigger share into equities.
The SBI issue also provides Gol a pathway to trim its holdings in PSBs to desirable levels. Gol has adjusted its divestment priorities from balancing the budget to a more holistic approach incorporating PSU asset value, earnings potential and capacity buildup. Financial sector disinvestment has proved to be difficult. With banking being in one of its strongest cyclical phases, the SBI issue could be a precursor to capital-raising by other PSBS. They are also being encouraged to scale up subsidiaries in insurance and MFS prior to listing, which supports a gradual approach to divestment that yields higher value.
Date: 18-07-25
यूएस को हमारी उतनी ही जरूरत, जितनी हमें उनकी
संपादकीय
एक ओर रूस से तेल खरीदने वाले भारत जैसे देशों पर सेकंडरी टैरिफ की धमकी और दूसरी ओर भारत से जल्द व्यापार समझौते का भरोसा यह है ट्रम्प की कार्यशैली। टैरिफ 19% करने की धमकी के बाद भारतीय वार्ताकार अमेरिका में वार्ता दुबारा शुरू करेंगे। भारत अपने बढ़ते मध्यवर्ग के कारण एक बड़ा बाजार और विस्तार लेती चौथी बड़ी इकोनॉमी है, जिसे अमेरिका नजरअंदाज नहीं कर सकता। इन दिनों ट्रम्प नीति से रू-ब-रू होने के बाद वार्ताकारों को एक बात तो स्पष्ट हो गई होगी कि ट्रम्प जिद्दी नहीं हैं। वे सौदेबाजी कर रहे हैं। कृषि हमारी कमजोर नस है जबकि ट्रम्प को कृषि बाहुल्य 444 काउंटीज में से (अधिकांश मध्य अमेरिका में हैं) 433 में 77% से ज्यादा वोट मिले थे। लिहाजा वे उनके कृषि उत्पाद खासकर सोयाबीन, मक्का और कपास भारत में बेचना चाहते हैं। लेकिन ये जेनेटिकली मोडिफाइड हैं और भारत में प्रतिबंधित हैं। इस पर कोई समझौता किए बिना भारत को एक सीमा तक लचीला रुख अपनाना होगा, क्योंकि हमारे उत्पादों की लागत ज्यादा होने के बावजूद अमेरिका उन्हें कम टैरिफ पर लेता रहा है। हमारे लिए स्टील, एल्युमीनियम और तमाम अन्य उत्पाद अमेरिका को बेचना जरूरी है क्योंकि ईयू नाटो के जरिए आंखें दिखा रहा है। बहरहाल, हम ट्रम्प की सौदेबाजी से विचलित न हों, क्योंकि अमेरिका को भी भारत की उतनी ही जरूरत है।
Date: 18-07-25
नागरिकता पर सभी दलों को स्वस्थ बहस की जरूरत है
विराग गुप्ता, ( सुप्रीम कोर्ट के वकील )
बिहार में वोटर लिस्ट पर हंगामे के बाद चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश और दूसरे राज्यों में चुनावों से काफी पहले वैज्ञानिक तरीके से सत्यापन प्रक्रिया पूरी करने की मांग की है। दूसरी ओर हिमंत बिस्वा सरमा ने एनआरसी का राग छेड़कर संवैधानिक मामले में सियासी पेचीदगी बढ़ा दी है। पश्चिम में नागरिकता के कठोर नियम हैं, लेकिन भारत में नागरिकता का मसला संसदीय विफलता, सत्ता की सियासत और प्रशासनिक भ्रष्टाचार की बलि चढ़ रहा है। नागरिकता से जुड़े 6 बिंदुओं पर सभी दलों को स्वस्थ बहस की जरूरत है।
1. एनआरसी : 1951 की जनगणना के अनुसार पहला राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) बना, लेकिन उसके बाद अपडेट नहीं हो पाया। नागरिकता कानून के अनुसार 2003 में एनआरसी के संशोधनों को लागू करने की मुहिम 2019 में सुप्रीम कोर्ट के ठंडे बस्ते में चली गई। असम समझौते को लागू करने के लिए नागरिकता कानून में जोड़ी गई धारा 6-ए को सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने पिछले साल वैध करार दिया। बिहार में वोटर लिस्ट का सत्यापन चुनावों के पहले कराने पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नसीहत तो दी है, पर नागरिकता से जुड़े अनेक लम्बित मामलों की सुनवाई और फैसले के लिए सुप्रीम कोर्ट में कई सालों से संविधान पीठ का गठन ही नहीं हुआ है।
2. एनपीआर : जनसंख्या का कानून 1948 में बना, लेकिन राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) के लिए 2003 में जाकर नियम बने उसके अनुसार भारत के सभी सामान्य निवासियों के लिए एनपीआर में रजिस्ट्रेशन जरूरी है। 2010 में पहला एनपीआर तैयार होने के पांच साल बाद उसे अपडेट किया गया था। लेकिन आधार कार्ड की तरह एनपीआर में विवरण होना नागरिकता का आधिकारिक सबूत नहीं है।
3. सीएए : नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को दिसम्बर 2019 में मंजूरी मिली। उसके अनुसार पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से गैर- मुस्लिम धार्मिक अल्पसंख्यक शरणार्थियों को भारत की नागरिकता मिल सकती है। उस कानून के अनुसार शरणार्थियों को नागरिकता लेने के लिए भारत में निवास के प्रमाण के तौर पर 20 तरह के दस्तावेजों में से एक और पड़ोसी देश के निवास के प्रमाण के तौर पर 9 में से एक दस्तावेज को देने की जरूरत है। सीएए और रोहिंग्या शरणार्थियों जैसे मामले सुप्रीम कोर्ट में सालों से लम्बित हैं। इसलिए वोटर लिस्ट में पहचान के बावजूद विदेशी लोगों के खिलाफ निर्वासन की कार्रवाई के लिए गृह मंत्रालय को एक्शन लेना होगा।
4. आधार : सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2015 में कहा था कि आधार कार्ड के जरूरी नहीं होने के बारे में भारत सरकार बड़े पैमाने पर मीडिया में प्रचार करे। लेकिन कोर्ट के अनेक आदेशों और अंतिम फैसले को धता बताकर सरकार ने पिछले दरवाजे से आधार को जरूरी बना दिया। अभी बिहार में आधार को मान्यता देने की मांग करने वाली पार्टियां वोटर कार्ड को आधार से लिंक करने का विरोध कर रही हैं। दो साल पहले सुप्रीम कोर्ट में दिए शपथ पत्र के अनुसार फार्म-6 बी के लिए आधार जरूरी नहीं है इसके बावजूद चुनाव आयोग ने 66.23 करोड़ वोटरों का आधार क्रमांक एकत्रित कर लिया है। लंबी नींद से जागने के बाद सरकार ने सख्ती बढ़ाई है। लेकिन जांच के बगैर निजी एजेंसियों द्वारा जारी करोड़ों आधार अब सरकार के साथ चुनाव आयोग के गले की हड्डी बन गए हैं।
5. नागरिकता : सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले के अनुसार वोटर लिस्ट की आड़ में चुनाव आयोग नागरिकता की पड़ताल नहीं कर सकता। एनआरसी और नागरिकता का मामला केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन आता है। लेकिन अनुच्छेद-326 के अनुसार 18 से ऊपर के नागरिकों का नाम वोटर लिस्ट में शामिल करने के बारे में चुनाव आयोग को संविधान से संपूर्ण अधिकार हासिल हैं। इसीलिए आधार और ड्राइविंग लाइसेंस के लिए मंजूरी के बावजूद फर्जीवाड़े वाले राशन कार्ड की मान्यता मुश्किल है।
6. वोटर लिस्ट: बिहार में 1% वोटों के फेरबदल से सरकार का गणित बदल गया था। इसलिए भ्रष्ट तरीके से वोटर लिस्ट में गलत नाम शामिल करवाना या सही वोटरों का नाम हटाना, दोनों गलत हैं। राज्य सरकारों के स्थानीय प्रशासन की मनमर्जी और भ्रष्टाचार को सख्ती से नियंत्रित करके आयोग अपनी साख बढ़ा सकता है। स्वतंत्र, पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण आयोग की संवैधानिक जिम्मेदारी है।

Date: 18-07-25
बाजार समर्थक हों नीतियां
संपादकीय
यह बात लंबे अरसे से समझी जा रही है कि एक तरफ शुल्कों की दीवार खड़ी कर दूसरी तरफ औद्योगिक नीति के जरिये देसी उद्योगों को सब्सिडी दी जाती है तो उसके कई बुरे नतीजे होते हैं। उनमें से एक है भारी भरकम देखी औद्योगिक समूह तैयार हो जाना।
यह बात भारतीय नीति निर्माताओं को ज्यादा अच्छी तरह समझ आनी चाहिए थी क्योंकि यह आजादी के बाद भारत के आर्थिक इतिहास का हिस्सा है। सन 1990 के दशक में जाकर उदारीकरण ने अर्थव्यवस्था में कुछ हलचल पैदा की। लेकिन अब कुछ संकेत इस बात की चिंता पैदा करने लगे हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था के सबसे हालिया दौर में उदारीकरण के बाद के चलन के ये पहलू उलटने लगे हैं। अर्थशास्त्री अजय छिब्बर ने हालमें हुए कुछ शोधों का जिक्र करते हुए इसी समाचार पत्र में लिखा कि किसी भी एक क्षेत्र के कुल उत्पादन में कुछेक बड़ी फर्मों की बड़ी हिस्सेदारी का चलन पिछले एक दशक में बढ़ गया है साथ ही इन कंपनियों की कीमत तय करने की ताकत भी बढ़ गई है। ऐसे क्षेत्रों में छोड़ नहीं होने के बारे में जो निष्कर्ष आए हैं वे भी परेशानी बढ़ाने वाले हैं। विरोधाभास वह है कि जो क्षेत्र ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, उनमें कदम रखने में उतनी ही ज्यादा बाधाएं हैं। पहली बार कदम रखने वालों को उस क्षेत्र में पहले से काम कर रही कंपनियों के आकार के साथ तुलना कर कमतर समझ लिया जाता है।
अगर इन बातों को एक साथ रखकर देखें तो परेशान करने वाली तस्वीर उभरती है भारत की वृद्धि अपेक्षाकृत छोटी संख्या में मौजूद बड़े कारोबारी घरानों के निवेश और उनके परिचालन विकल्पों पर निर्भर रह गई है। इनमें से कई पर अभी भी कुछ खास परिवारों का ही नियंत्रण है। ऐसा दांचा जरूरी नहीं कि उत्पादक निवेश तैयार करे वा उपभोक्ताओं को प्रतिस्पर्धी दबावों से संबद्ध लाभ दिलाए। निवेशक और टीकाकार आकाश प्रकाश इसी अखबार में लिखते हैं कि भारतीय कारोबार अल्पावधि के मुनाफे पर अधिक जोर देते हैं और निवेश पर कम। ऐसे में बाजार ढांचे का यह स्वरूप कैसे बरकरार है? आंशिक रूप से ऐसा शायद इसलिए हुआ क्योंकि वर्तमान के कुछ सर्वाधिक उत्पादक क्षेत्रों मसलन दूरसंचार और ई-रिटेल में नेटवर्क की ऐसी बाह्यताएं शामिल होती हैं जो पहले से मौजूद बड़े आकार की कंपनियों को लाभ पहुंचाती हैं। परंतु यह भी मानना होगा कि काफी हद तक द्वेष नीतिगत चयनों पर भी जाएगा।
देश ने सचेतन ढंग से ऐसी औद्योगिक नीति और सरकार द्वारा निर्देशित निवेश को चुना जिसने अनिवार्य ढंग से बड़े कारोबारी समूहों को सशक्त बनाया। सरकार के लिए वह आसान होता है। कि वह ऐसी कंपनियों वाले कॉरपोरेट के साथ सहयोग करे बजाय ऐसी नीतियां बनाने के जो कई छोटे कारोबारियों को प्रोत्साहन दें। कुछ लोग कहेंगे कि यह वृद्धि और उत्पादकता के लिए बुरी खबर नहीं है। आखिर जापान, कोरिया जैसे देश और यहां तक कि अमेरिका ने भी 19वीं सदी के आखिर में जाइबात्सु चाइबोल और रॉबर बैरंस जैसे धनवान समूहों की मदद से वृद्धि हासिल की। इन समूहों ने सरकार के साथ सहयोग किया और रेलवे तथा इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे नए क्षेत्र विकसित किए। बहरहाल अंतर यह है कि इससे कार्यकुशलता में भी सुधार हुआ है क्योंकि उन्हें हमेशा टैरिफ के जरिये बचाया गया और निर्यात बाजार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित किया गया।
विदेश में कामयाब भारतीय कंपनियां कुछ संदिग्ध व्यापारिक उपयोगिता प्रदर्शित कर सकती हैं लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर कामयाबी का शिखर छूने वाली कंपनियां यकीनन एक समस्या हैं। जैसा कि रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन कह चुके हैं, देश में सफलतम कारोबारियों की नई नस्ल विश्वस्तरीय उत्पाद या अंत- रराष्ट्रीय ख्याति वाले ब्रांड नहीं तैयार कर रही है। यह भी कहा जा सकता है कि वे उस निवेश संसाधन की खपत कर रहे हैं जिसे अन्यथा किसी और जगह पर लगाया जा सकता था। बुनियादी समस्या इन कंपनियों में नहीं है क्योंकि वे तो बस अधिक से अधिक मुनाफा कमाने में लगी हैं। दिक्कत नीतिगत दिशा में है क्योंकि आर्थिक खुलापन बढ़ाने और सरकारी नियंत्रण कम करने की जरूरत है। परंतु हो इसका उलटा रहा है।
Date: 18-07-25
सुरक्षा परिषद और भारत की दावेदारी
सुशील कुमार सिंह
ब्रिक्स देशों का सम्मेलन बीते छह सात जुलाई को ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में संपन्न हुआ, जहां कई ज्वलंत मुद्दे उठे और इन्हीं में एक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तत्काल सुधार से संबंधित भी था । ब्रिक्स देशों के नेताओं ने सुरक्षा परिषद को और अधिक लोकतांत्रिक, प्रभावी और कुशल बनाने की वकालत की है। खास बात यह भी रही कि सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य के रूप में चीन और रूस ने संयुक्त राष्ट्र में तुलनात्मक रूप से बढ़ी हुई भूमिका निभाने की ब्राजील और भारत की इच्छा का समर्थन किया है। वैसे देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का मामला दशकों पुराना है। यदि अमेरिका जैसे देश वास्तव में इस मसले पर गंभीर हैं, तो सुरक्षा परिषद में बड़े सुधार को सामने लाकर भारत को स्थायी सदस्य के रूप में उसमें जगह दी जानी चाहिए। कई वर्ष पहले रूस ने जोर दिया था कि स्थायी सदस्यता के लिए भारत मजबूत दावेदार है। दुनिया के कई देश इस मामले में भारत के साथ खड़े दिखाई देते हैं, लेकिन नतीजे वहीं के वहीं हैं ।
पिछले वर्ष भारत दौरे पर आए संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस ने कहा था कि संयुक्त राष्ट्र का मौजूदा स्वरूप विश्व की बदलती जरूरतों के मुताबिक नहीं है और इसमें सुधार नितांत आवश्यक है। अब ब्रिक्स सम्मेलन में चर्चा के बाद यह मुद्दा एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। ब्रिक्स देशों के नेताओं ने जोर दिया है कि सुरक्षा परिषद में ‘सुधार वैश्विक दक्षिण के हितों के अनुरूप होना चाहिए। यानी यह सुधार विकासशील देशों की भूमिका को विस्तार देने से भी होना जुड़ा जाना चाहिए। वैसे विश्व स्वास्थ्य संगठन से लेकर विश्व व्यापार संगठन पर भी सवाल उठते रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र की उपयोगिता और उसकी सफलता तथा विफलता की लकीर भी कमोबेश छोटी-बड़ी रही है। संदर्भ यह भी है कि किसी भी संगठन या परिषद को यदि सुधार और बदलाव से विमुख कर लंबे समय तक रखा जाए, तो उसमें गैर उपजाऊ तत्त्व स्वतः शामिल हो जाते हैं। दुनिया में भारत का बढ़ता कद मौजूदा समय में पूरी धमक के साथ प्रतिबिंबित करता है कि सुरक्षा परिषद में फेरबदल के साथ उसे स्थायी सदस्य बनाया जाए। तभी वैश्विक हित के साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में संतुलन संभव है।
विदित हो कि संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्यों में भारत भी शुमार था और अब तक वह सुरक्षा परिषद का आठ बार सदस्य भी रह चुका है। आखिरी बार वर्ष 2021-22 में अस्थायी सदस्य के रूप में भारत ने अपनी भूमिका निभाई थी। मगर पूरी योग्यता और व्यापक समर्थन के बावजूद अभी तक उसे स्थायी सदस्यता नहीं मिल पाई है। हालिया परिप्रेक्ष्य में देखें, तो ब्रिक्स सम्मेलन में एक बार फिर इस मुद्दे की गूंज सुनाई दी है। ब्रिटेन भी सुरक्षा परिषद के विस्तार का समर्थन करता रहा है, इतना ही नहीं वह भारत, जापान, ब्राजील समेत अफ्रीकी देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट देने की बात कह चुका है। पिछले आठ दशकों से चली आ रही इस व्यवस्था में बुनियादी परिवर्तन की मांग अक्सर उठती रही है। दुनिया ने कई तरह के आकार और प्रकार को ग्रहण कर लिया है, मगर सुरक्षा परिषद पांच स्थायी सदस्यों अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और रूस के अलावा दस अस्थायी सदस्यों के साथ यथावत स्थिति में है। ऐसे में अब परिवर्तन का समय आ चुका है।
असल में सुरक्षा परिषद की स्थापना वर्ष 1945 की भू-राजनीतिक और द्वितीय विश्व युद्ध से उपजी स्थिति को देख कर की गई थी, लेकिन आठ दशकों में बहुत कुछ बदल चुका है। देखा जाए तो शीतयुद्ध की समाप्ति के साथ ही इसमें बड़े सुधार की गुंजाइश थी, जो नहीं किया गया। पांच स्थायी सदस्यों में यूरोप का प्रतिनिधित्व सबसे ज्यादा है, जबकि आबादी के लिहाज से वह मुश्किल से पांच फीसद स्थान घेरता है। अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका का कोई सदस्य देश इसमें स्थायी नहीं है, जबकि संयुक्त राष्ट्र का पचास फीसद कार्य इन्हीं से संबंधित है। सुरक्षा परिषद के ढांचे में सुधार इसलिए भी होना चाहिए, क्योंकि इसमें अमेरिकी वर्चस्व दिखता है भारत की सदस्यता के मामले में दावेदारी बहुत मजबूत दिखाई देती है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से चीन को पीछे छोड़ कर पहला सबसे बड़ा देश बन गया है, जबकि अर्थव्यवस्था के मामले में दुनिया का पांचवां बड़ा देश है। ऐसे में भारत की दावेदारी कहीं अधिक मजबूत है। इतना ही नहीं भारत को विश्व व्यापार संगठन, ब्रिक्स और जी 20 जैसे आर्थिक संगठनों में प्रभावशाली माना जा सकता है।
एल 69 समूह जिसमें भारत, एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के 42 विकासशील देशों की अगुआई कर रहा है, वह भी सुरक्षा परिषद् में सुधार की मांग करता रहा है। अफ्रीकी समूह में 54 देश हैं, जो सुधारों की वकालत करते रहे हैं। इनकी मांग है कि अफ्रीका के कम- से कम दो राष्ट्रों को ‘वीटो’ की शक्ति के साथ स्थायी सदस्यता दी जाए। यदि भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता मिलती है, तो चीन जैसे देशों के ‘वीटो के दुरुपयोग पर न केवल अंकुश लगेगा, बल्कि व्याप्त असंतुलन को भी पाटा जा सकेगा। गौरतलब है कि अपनी स्थापना से अब तक सुरक्षा परिषद की सफलताओं के साथ कई नाकामियां भी जुड़ी रही हैं। यह बात सकारात्मक है कि इसके गठन के बाद तृतीय विश्व युद्ध नहीं हुआ, मगर दुनिया कई युद्धों से गुजरी है। रूस और यूक्रेन के बीच अभी युद्ध जारी है। हाल में ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष हुआ। इजराइल और हमास तो संघर्षरत हैं ही। इससे पहले अमेरिका के नेतृत्व में वर्ष 2003 में इराक पर आक्रमण, वर्ष 2008 में रूस का जार्जिया पर हमला, अरब-इजराइल युद्ध, 1994 में रवांडा का जनसंहार और 1993 में सोमालिया में गृहयुद्ध सुरक्षा परिषद की विफलता की कहानी है।
माना जाता है कि जिस स्थायी सदस्यता के लिए भारत पिछले कुछ वर्षों से प्रयासरत है, वह वर्ष 1950 के दौर में आसानी से सुलभ थी। आवश्यकता की दृष्टि से देखें, तो भारत को इसका स्थायी सदस्य इसलिए होना चाहिए, क्योंकि सुरक्षा परिषद प्रमुख निर्णय लेने वाली संस्था है। प्रतिबंध लगाने या अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के फैसले को लागू करने के लिए इस परिषद के समर्थन की जरूरत पड़ती है। ऐसे में एशिया में शांति और स्थिरता की दृष्टि से भारत को स्थायी सदस्यता मिलनी ही चाहिए। चीन द्वारा सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान के आतंकवादियों को सूचीबद्ध करने में बार-बार अड़ंगा लगाना इस बात को पुख्ता करता है। स्थायी सदस्यता मिलने से भारत को वैश्विक पटल पर अधिक मजबूती से अपनी बात कहने की ताकत मिलेगी और चीन की चाल कमजोर होगी। इसके अलावा बाह्य सुरक्षा खतरों और भारत के खिलाफ सुनियोजित आतंकवाद जैसी गतिविधियों को रोकने में भी मदद मिलेगी।
Date: 18-07-25
राजनीतिक सोच का बघार
संपादकीय

महत्त्वपूर्ण शैक्षणिक बदलाव के तहत राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) ने कई बदलाव किए हैं, जिनमें अकबर को क्रूर पर सहिष्णु, बाबर को निर्मम आक्रमणकारी कहा है जबकि औरंगजेब को सैन्य शासक बताया है, जिसने गैर-मुसलमानों पर जजिया लगाया था। हालिया प्रकाशित एक्सप्लोरिंग सोसाइटी : इंडिया एंड बियॉन्ड नये पाठ्यक्रम की पहली पुस्तक बताई जा रही है जिसमें दिल्ली सल्तनत, मराठों व औपनिवेशिक युग की चर्चा है। इसमें नोट में छात्रों से आग्रह है कि क्रूर हिंसा, कुशासन व सत्ता की गलत महत्त्वाकांक्षाओं के ऐतिहासिक मूल को निष्पक्षता से समझें । अतीत की घटनाओं के लिए आज किसी को जिम्मेदार भी न समझें, जोड़ा गया है। दिल्ली सल्तनत के उत्थान-पतन,प्रतिरोध, विजयनगर साम्राज्य, मुगलों व उनका प्रतिरोध तथा सिखों के उत्थान की चर्चा है। बाबरनामा को स्वीकारने के बावजूद मंदिरों के विध्वंस की बात भी है। छात्रों को देश के इतिहास से परिचित करवाने के नाम पर सरकार के रुझान के अनुरूप तैयार किया नया पाठ्यक्रम पहले से ही विवादों में है। अकबर पर शामिल अबुल फजल की टिप्पणी- मैं शर्म से भर गया, चूंकि मैं खुद मुसलमान नहीं था, इसलिए दूसरों को मुसलमान बनने के लिए मजबूर करना मेरे लिए अनुचित था इस मंशा का स्पष्ट उदाहरण कही जा सकती है। बेशक, भारतवर्ष ने सैकड़ों वर्षों गुलामी झेली है मगर नई पौध को बरगलाने वाली भाषा में उसे परोसना न्यायोचित नहीं कहा जा सकता। गुलामों के साथ सारी दुनिया में अपमानजनक बर्ताव होता रहा है, जिज्ञासू छात्र वयस्क होने पर स्वयं इतिहास का अध्ययन कर वैचारिक परिपक्वता इख्तियार कर सकते हैं। पाठ्यक्रम में काशी और मथुरा के मंदिरों का विध्वंस और सिखों, सूफियों तथा पारसियों के उत्पीड़न की चर्चा शामिल करने का तात्पर्य क्या है। यह स्पष्टीकरण कि शैक्षणिक ढांचे को आलोचनात्मक सोच की ओर बदलाव का संकेत माना जाना चाहिए, को राजनीति से प्रेरित कहना गलत नहीं होगा। सवाल सच-झूठ का भी नहीं है। नायकों – खलनायकों तथा विकल्पों-विरोधाभासों को लेकर खींची गई यह रेखा बाल मन पर संदेह के बीज भी बो सकती है। हकीकत यह है कि इतिहास को किसी कीमत बदला नहीं जा सकता। पूर्वाग्रहों के आधार पर उसकी तोड़-मरोड़ भले की जाती रहे।