
15-07-2025 (Important News Clippings)
To Download Click Here.
Date: 15-07-25
Loosen the Noose. Power up the Grid
Ease nuclear law to draw in private capital
ET Editorials
To grow, India’s needs to diversify its energy sources, and it must be clean due to its climate commitments. Nuclear energy is one such option, but its growth has been stymied in India due to stringent supplier liability in the event of an accident. Now, Gol is contemplating a total recast of laws governing atomic energy, including Civil Liability for Nuclear Damage. The country produces around 3% of its power in nuclear reactors in contrast with France where the share is 64%. The way forward is thro- ugh private investment in nuclear energy in a departure from an earlier government-led initiative. This requires liabilities to be reset to levels acceptable to suppliers that are skittish about potential unlimited damages contained inexisting legislation.
There is some urgency because nuclear power generation has grown slowly through inter-governmental ventures. Projects have run into geopolitical concerns and resistance from local communities. Targets for the next couple of decades are ambitious and require a market-driven approach if they are to be met. India needs to harmonise its liability regulations with international rules to draw interest from private investors. It has signed a global convention on nuclear liability but is yet to ratify it.
The liability issue is a necessary, but not sufficient, condition for the growth of nuclear power in India. Efforts to draw private investment into coal-based power plants have run into a thicket of subsidies that plague electricity generation. Political imperatives of subsidised power have stymied the growth of an efficient market for electricity, and successive bailouts to state-owned utilities have not rectified the distortions. Private capital is reluctant to venture into power generation unless India fixes its distribution issues. This could be an issue with nuclear power as well. But it is a good start to address supplier liability, without which nuclear energy will remain confined to its current rate of growth, acceptable neither to energy security nor to sustainability.
Date: 15-07-25
Roads to Faster, Fairer Infra Growth
ET Editorials
A growing highway network is vital for a growing economy- not just for moving people and goods, but also for spurring local development and job creation. Since 2014, India’s highway network has expanded by 60%, growing from 91,287 km to 146,195 km by 2024. However, progress hasn’t come without hurdles. As Nitin Gadkari informed parliament last December, more than 44% of major infrastructure projects, inclu- ding national highways (NH), are facing delays. Reasons range from land acquisition bottlenecks and delays in statuto- ry clearances to encroachment issues, law and order concerns, poor contractor performance, and unforeseen events.
To address these roadblocks and accelerate the pace of NH construction, ministry of road transport and highways has announced a new approach. Instead of assigning projects to states, it will now offer multiple highway projects to each identified state and let them prioritise the ones they wish to take up first. The rationale is simple: states are better equipped to manage land acquisition, rehabilitation of affected communities and the required clearances. By giving states more control, the ministry hopes projects can be rolled out faster – especially those where much of the groundwork is already done. Gol has set a target of constructing 10,000 km of highways in 2025-26, slightly lo- wer than the 10,421 km target for 2024-25.
This new model could work well- if states rise to the occasion. They know their regional priorities best, but must ensure balanced development and avoid letting politics dictate project choices. If implemented in the right spirit, this shift could pave the way for faster, fairer infrastructure growth, which will not just benefit the states concerned but also the nation as a whole.
Date: 15-07-25
Women, STEM careers and a more receptive industry
World Youth Skills Day is a reminder that industry is losing out by not investing in STEM careers for India’s women
Kanta Singh, [ is the Country Representative, a.i. at UN Women India and is a part of Team UN in India ]
Antara Lahiri, [ is the Director, Micron Foundation, Asia and Europe. Micron Technology and the Micron Foundation focus on expanding access to STEM education and pathways to high-tech careers of the future ]
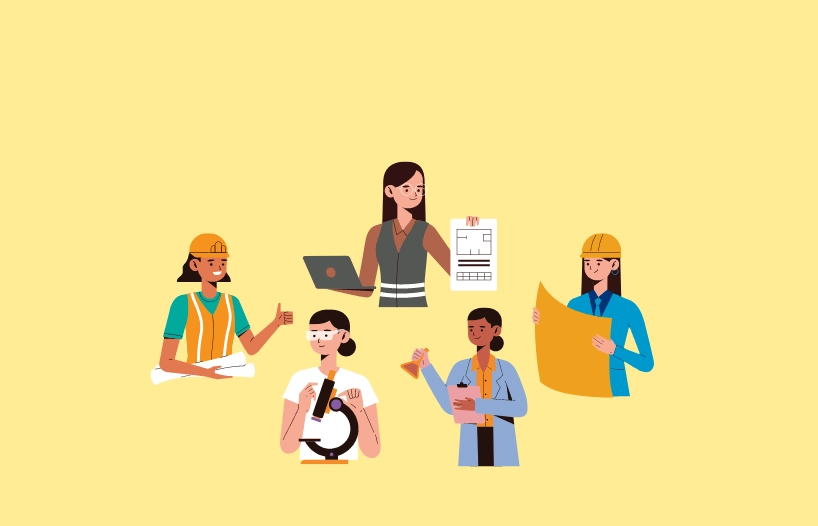
Every year on July 15, as we observe World Youth Skills Day, we are reminded that skills development is fundamental to reducing unemployment and promoting decent work. India faces a critical paradox: 43% of India’s STEM graduates are women, the highest proportion among major economies globally. Yet, women represent only 27% of the STEM workforce, limiting women’s access to career opportunities offered by the STEM sector.
According to the Periodic Labour Force Survey (PLFS) 2023-24, India’s overall female labour force participation rate (FLFPR) has risen to 41.7%, a meaningful jump after years of stagnation. However, the increase is sharper for rural women (47.6%) than in urban areas (25.4%), reflecting barriers in formal employment, workplace safety, and societal expectations. In STEM, the paradox is more pronounced. According to the UNESCO Institute for Statistics (2021), only 31.5% of researchers worldwide are women. This education-employment gap reflects systemic barriers that industry is uniquely positioned to address. The economic stakes are clear. According to estimates by the McKinsey Global Institute, enabling 68 million more women to participate in India’s workforce could boost India’s GDP by up to $700 billion by 2025. Similarly, the World Bank suggests that achieving a 50% female workforce participation rate could elevate GDP growth by 1%.
Government vision and STEM skilling
The New Education Policy (NEP) 2020 paved the way for higher retention and opportunities in the fields of STEM. The nodal Ministry of Education (MOE) has integrated education with skills development and life skills training. The Government’s renewed focus on revitalising Industrial Training Institutes (ITIS) and expanding vocational skilling is bringing high-quality technical education and training closer to villages and small towns, ensuring broader access for youth across rural India.
This progress aligns with the Prime Minister’s vision of Viksit Bharat (or developed India), where women’s economic mobility forms the cornerstone of inclusive development. The share of the gender budget in the total national Budget has increased from 6.8% in 2024-25 to 8.8% in 2025-26 with 14.49 lakh crore in allocation toward gender-specific programmes.
Further, the Union Budget 2025-26 introduced term loans for women entrepreneurs, new National Skill Training Institutes, and investments in technology-driven skilling. India’s policy framework, from Skill India to Digital India, and from ‘Beti Bachao, Beti Padhao’ to PM Vishwakarma Yojana, has the right intent. However, government policy alone cannot bridge the education-employment gap. Industry must transform from passive recruiter to active enabler of women’s career transitions.
Industry as the missing link
Industry plays a critical role in bridging the gap between skilling and employment, especially for women. Persistent social norms, such as the belief that “mechanical means masculine” or that “coding isn’t for girls”, continue to create invisible barriers for skilled women entering technical fields. These stereotypes are well-documented in multiple studies, including those by the World Bank and UNESCO, which highlight how gendered perceptions limit women’s participation in STEM and technical trades. Evidence also shows that women do not leave STEM fields due to a lack of ability, but instead because workplaces are often unwelcoming, families lack awareness of career opportunities, and roles remain deeply gendered. Addressing these perceptions, alongside ensuring workplace safety, equitable pay, and support for career transitions related to marriage, childbirth, and caregiving, is key to unlocking the full potential of the workforce.
India’s private sector is increasingly stepping up, with many companies championing structured mentoring programmes, industry-linked training initiatives and partnerships with educational institutions to create direct pathways from classrooms to careers. One such initiative is the UN Women’s WeSTEM programme, being implemented in collaboration with the Governments of Madhya Pradesh and Gujarat, and supported by the Micron Foundation. This programme provides access to skills and bridges the talent gap. By engaging families and community leaders, conducting workplace safety sessions, and introducing women role models in classrooms, the programme recognises that skill-building requires a shift in mindsets to be effective.
A blueprint for industry leadership
Industry partnerships with educational institutions, mentorship networks linking professionals with students, and workplace policies that accommodate life transitions and ensure safety, can bridge the education-employment gap. The question is not whether India can afford to invest in women’s STEM careers. It is whether industry can afford not to. By equipping women and girls with the skills and training needed to succeed in STEM fields, we can create a more inclusive and robust society. When a woman earns, her voice and impact echoes across dinner tables, shop floors, policy rooms and entire industries. And in that voice lies the blueprint of a future ready India.
Date: 15-07-25
चुनाव आयोग का आचरण संदेह से परे होना जरूरी
संपादकीय
अगर चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था भी सूत्रों के हवाले से खबर देने लगे, अगर अधूरे फॉर्म को डेटा (75% फॉर्म्स भरने का दावा) के रूप में पेश किए जाने का झूठ और विशेष गहन समीक्षा के दूसरे दौर में बीएलओ द्वारा पैसे लेकर ऑनलाइन फॉर्म देने के वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हों, तो संस्था पर सवाल उठते हैं। आयोग पर सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं कि जब सर्वोच्च अदालत ने समयाभाव और समीक्षा की प्रक्रिया की दुरूहता पर सवाल किया और अगली सुनवाई की तिथि 28 जुलाई तय की तो उसके बाद बगैर किसी आंकड़े या आधिकारिक बयान के मीडिया में सूत्रों के हवाले से खबर दी गई कि बिहार की वोटर लिस्ट में विदेशी घुसपैठिए शामिल हैं। जैसे ही सोशल मीडिया में हजारों अधूरे फॉर्म्स की सच्चाई वायरल जिनमें न तो अधिकांश फॉर्म भरने वालों के हस्ताक्षर थे, न ही कोई दस्तावेज तो कुछ पत्रकारों पर स्थानीय अफसरों द्वारा कार्रवाई की बात कही जाने लगी। बताया जा रहा है कि फॉर्म अपेक्षित संख्या में छपे नहीं हैं, लिहाजा आधे-अधूरे फॉर्म्स को अपलोड करके तीन चौथाई काम खत्म होने का दावा किया जा रहा है। जबकि चुनाव आयोग से संविधान निर्माताओं ने दिशा-निदेशक आचरण की अपेक्षा की थी। यही कारण है कि चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया सर्वोच्च अदालत के जज के समतुल्य रखी गई थी ताकि राजनीतिक दबाव न हों।
Date: 15-07-25
मताधिकार और नागरिकता का पेचीदा सवाल
अरविंद जैन, ( लेखक सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील हैं )

बिहार में मतदाता सूची की विशेष गहन समीक्षा मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले में विपक्षी दलों की और पैरवी में लगे वकील – संसद कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी थी कि इस समीक्षा की आड़ में निर्धन, अशिक्षित, दलित और वंचित तबके के लोगों को मतदाता सूची से बाहर करने का षड्यंत्र किया जा रहा है और सत्ताधारी दल के इशारे पर चुनाव आयोग मनमानी कर रहा है। जब चुनाव आयोग के वकील राकेश द्विवेदी ने कहा कि मताधिकार के लिए नागरिकता अनिवार्य है और आधार, राशन, चुनाव, पैन कार्ड आदि को नागरिक होने का प्रमाण नहीं माना जा सकता तो न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और जायमल्या बागची ने कहा कि नागरिकता की जांच का काम तो गृह मंत्रालय का है, न कि चुनाव आयोग का। इस पर आयोग की और से जवाब दिया गया कि उसे अनुच्छेद 326 के तहत भी अधिकार प्राप्त हैं।
फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने मतदाता सूची के पुनरीक्षण पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया है। अब 28 जुलाई को मामले की अगली सुनवाई होगी। पुनरीक्षण प्रक्रिया जारी रखने की हरी झंडी दिखाने के साथ ही शीर्ष अदालत ने इस प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए आधार, वोटर, राशन कार्ड आदि दस्तावेजों को मान्य करने का सुझाव देते हुए मतदाता सूची अधिसूचित करने से पहले सभी पक्षों को अवगत कराने का भी निर्देश दिया। यह निर्देश भी दिया कि बिना अवसर दिए किसी का नाम न हटाया जाए। चुनाव आयोग 2003 के बाद मतदाता बने व्यक्तियों की नागरिकता संबंधी दस्तावेजों की जांच में आधार राशन या चुनाव कार्ड को प्रामाणिक दस्तावेज नहीं मान रहा था। संवैधानिक संस्था होने के नाते चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट के सुझावों- निर्देशों का सम्मान करना ही चाहिए, पर इस बार दुविधा बहुत बड़ी है। पेच इस पहलू में फंसा हुआ है कि मतदाता होने के लिए भारत का नागरिक होना अनिवार्य है और नागरिकता संशोधन कानून के अनुसार नागरिकता के लिए विशेष रूप से 2004 के बाद भारत में पैदा हुए व्यक्ति को यह प्रमाणित करना अनिवार्य है कि जन्म के समय उसके माता-पिता भारत के नागरिक थे हैं। अथवा दोनों में से एक नागरिक है और ‘घुसपैठिया’ नहीं है। यही वह वर्ग है जो पहली बार मतदाता बनेगा। ऐसे में इस कवायद से जुड़े तमाम सवाल केवल बिहार चुनाव और वहां की मतदाता सूची तक ही सीमित नहीं रहेंगे। इसकी गूंज आने वाले चुनावों में भी सुनाई देगी। बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण के दौरान नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार जैसे देशों के लोगों के नाम आने के संकेतों के बीच इसकी मांग जोर पकड़ रही कि मतदाता सूची सत्यापन का काम पूरे देश में किया जाए। चुनाव आयोग ने ऐसा करने को कहा भी है।
सैद्धांतिक रूप से भारतीय नागरिकता जन्म और निवास के आधार पर तय की गई है। संविधान लागू होने के कुछ समय बाद भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में प्रविधान किया गया कि अगर किसी व्यक्ति का भारत में जन्म हुआ है तो उसे भारत का नागरिक माना- समझा जाएगा। नागरिकता कानून में जनवरी, 2004 से संशोधन किया गया कि 7 जुलाई, 1987 के बाद, किंतु 7 जनवरी, 2004 से पहले भारत में पैदा हुआ व्यक्ति भारत का नागरिक माना-समझा जाएगा, बशर्ते जन्म के समय उसके माता या पिता भारत के नागरिक हों। 7 जनवरी, 2004 के बाद जन्मा व्यक्ति भारत का नागरिक तभी होगा, जब उसके माता-पिता भारत के नागरिक हों या दोनें में से एक भारत का नागरिक हो और दूसरा ‘घुसपैठिया’ न हो नागरिकता कानून को लेकर सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1970 उस साल एक अप्रैल से लागू हुआ। 1970 से पहले जन्म या मृत्यु का पंजीकरण अनिवार्य नहीं था। इसलिए हर नागरिक के पास जन्म प्रमाण पत्र होना असंभव है। हालांकि 1970 के बाद जन्में तमाम नागरिकों के पास भी जन्म प्रमाण पत्र नहीं होगा। अधिकांश के पास पासपोर्ट, राशन कार्ड, आधार, पैन और ड्राइविंग लाइसेंस जैसे दस्तावेज तो हैं, लेकिन माता-पिता के जन्म का प्रमाण पत्र नहीं होगा। पासपोर्ट भारतीय नागरिकों को ही जारी किया जाता रहा है, मगर वह भी सिर्फ यात्रा दस्तावेज है। इस बहस में कुछ और सवाल उभरते हैं। देसी-विदेशी महिला (पुरुष) से विवाह का पंजीकरण अभी तक अनिवार्य नहीं है। अनाथ और लावारिस व्यक्तियों की नागरिकता का क्या होगा? एकल या अविवाहित मांओं के बारे में भी सोचना पड़ेगा या नहीं? 2015 में सर्वोच्च न्यायालय ने एबीसी बनाम दिल्ली राज्य जैसे मामले में फैसला सुनाया था कि अविवाहित माँ को अपने बच्चों की संरक्षता के लिए पिता की मंजूरी की जरूरत नहीं होगी। उसके आदेश में कहा गया था कि जब भी किसी एकल अभिभावक या अविवाहित मां अपने बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करे तो सिर्फ एक हलफनामा पेश किए जाने पर बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाए। इस निर्णय के बावजूद जन्म प्रमाण पत्र के लिए ‘आनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम’ में अभी भी बच्चे के पिता का नाम बताना अनिवार्य है। अन्यथा पंजीकरण संभव नहीं। यदि किसी मामले में मां की उम्र 18 साल से कम (नाबालिग है तो मौजूदा ‘सिस्टम’ सूचना स्वीकार नहीं करता। अगर 2025 में भी जन्म प्रमाण पत्र लेना इतना आसान नहीं तो अनुमान लगाया जा सकता है कि बिहार या बंगाल में वोट बनवाना कितना मुश्किल काम हो सकता है।
राजनीतिक प्रयोगशाला में देर-सबेर नागरिकता संशोधन कानून अपनी उपयोगिता निभा सकता है, लेकिन न्यायपालिका भी सत्ता का आईना है, जिसमें लोकतंत्र की नाव यथार्थ से थोड़ी दूर, मगर सुरक्षित दिखाई देती है । बहस के दौरान की गई अदालती टिप्पणियां फैसलों में प्रायः विलुप्त हो जाती हैं। देश में कानून का राज है, किसी दल विशेष का नहीं। इसलिए कानून का पालन और न्याय व्यवस्था में अटूट आस्था बनाए- बचाए रखना जरूरी है। मताधिकार के लिए नागरिकता अनिवार्य तो हैं, लेकिन चुनावी फायदे के लिए कानून को राजनीतिक अखाड़ा बनाना लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं होगा।
Date: 15-07-25
नीयत पर संदेह
संपादकीय
चुनाव आयोग ने पूरे देश में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू करने के लिए सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को सक्रिय कर दिया है। कुछ विपक्षी दलों व अन्य लोगों ने इस प्रक्रिया को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था। हालांकि जुलाई के अंत तक निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रव्यापी पुनरीक्षण पर अंतिम फैसला लेने की भी चर्चा है। अधिकांश राज्यों में 2002 से 2004 के दौरान मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण किया गया था। आयोग की बेवसाइट के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी में उपलब्ध सूची 2008 की है, जबकि उत्तराखंड में आखरी गहन पुनरीक्षण 2006 में होने की सूचना है। अवैध विदेशी प्रवासियों के नाम मतदाता सूची में शामिल होने के विवाद के बाद बिहार में यह बहस गरम हुई। इसी वर्ष बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, जबकि असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु व पश्चिम बंगाल में भी अगले वर्ष होंगे। बूथ स्तर के कर्मचारियों का आरोप है कि घर-घर जाकर की गई जांच में बड़ी संख्या में नेपाल, बांग्लादेश व म्यामांर के अवैध प्रवासियों के नाम मतदाता सूची में मिले। इस सारी कवायद पर संदेह व्यक्त करने वालों के अनुसार चुनाव आयोग द्वारा मांगे जा रहे दस्तावेज लोगों के पास उपलब्ध नहीं हैं। साठ फीसद से भी कम नागरिकों के पास पक्का मकान है, केवल 14% वयस्क दसवीं तक पढ़े हैं। सवाल है, बड़ी संख्या में बिहारी मजदूर रोजगार के सिलसिले में अन्य राज्यों में जा चुके हैं, उनका नाम इस सूची में शामिल करने का जिम्मा कौन लेगा। हाशिए पर खड़े लोग, दलितों, वंचितों व गरीबी रेखा के नीचे गुजार करने वालों से दस्तावेजों की सूची मांगना गैरवाजिब है। उस पर भी जिनके नाम पहले ही मतदाता सूची में मौजूद हैं और वे तीन-चार बार अपना मत प्रयोग कर चुके हैं। हैरत है कि इतने व्यापक स्तर पर बनाए गए आधार कार्ड पर सरकार और उसका समूचा तंत्र विश्वास क्यों नहीं कर पाता। सबके लिए एक सामूहिक व्यवस्था क्यों नहीं दी जाती। देश के हर नागरिक के लिए एकमात्र परिचय पत्र की व्यवस्था हो, जिसके मार्फत समूची जनसंख्या का सटीक अंदाजा भी हो और वही नागकिता की पहचान बने। उसी को मतदानपत्र, लाइसेंस, पैन, बैंक अकाउंट आदि से जोड़ा जाए। आम नागरिक को तनाव देना व सरकारी महकमों के चक्कर काटने के लिए मजबूर करना या हर कुछ दिनों बाद दस्तावेजों की गड्डियां मुहैया कराना कब तक चलता रहेगा। निःसंदेह सरकार की नीयत पर शक की गुंजाइशें कम नहीं हो रहीं ।
Date: 15-07-25
नहीं चेते तो क्रोध पड़ेगा भारी
सुरेश भाई
हिमालय में बाढ़ और भूस्खलन के चलते पर्यटकों और यात्रियों को बार-बार रोकना पड़ रहा है। गांव में रहने वाले लोग भारी बारिश के चलते रातभर सो नहीं पाते हैं। ऐसी भी सैकड़ों बस्तियां हैं जिनके आसपास विकास के नाम पर चारागाह, जंगल, खेती, पुराने रास्ते, नहरें क्षतिग्रस्त हुए हैं और वहां से लोग भूस्खलन की डर से सुरक्षित स्थान की तरफ भाग जाते हैं। इस विषम परिस्थिति में गर्भवती महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग सबसे अधिक तकलीफ में हैं।
पुराने समय में हिमालय के पर्वतीय अंचल में जब बरसात प्रारंभ होती थी तो लोग अपने मवेशियों को लेकर जंगल में घास के बीच में छानियां बनाकर निवास करते थे। जहां से वे दूध, घी, मक्खन बनाकर बेचते थे और उसके बदले उन्हें साल भर की राशन खरीदना होता था। तब उनके चारों ओर आज की जैसी आपदा की स्थिति नहीं थी और बारिश में लोगों को अपनी खेती-बाड़ी में बारहनाजा (एक ही खेत में 12 प्रकार की फसल) की फसलें तैयार होती दिखाई देती थी । हिमालय के नीचे मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले लोग भी बरसाती मौसम में नदियों में बहकर जाने वाली उपजाऊ मिट्टी, पानी को अच्छी फसल के संकेत मानते थे। अब वह पुराना समय चला गया है। गत वर्ष 2023-24 में जिस तरह की बाढ़ मध्य हिमालय से लेकर हिमाचल, जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों में 500 से अधिक लोग मारे गए थे। उसकी पुनरावृत्ति सन 2025 की शुरुआती बरसात में ही दिख रही है। बरसात के मौसम का प्रभाव उत्तराखंड और हिमाचल पर सबसे अधिक है। केदारनाथ जाने वाले रुद्रप्रयाग-गौरीकुंड राष्ट्रीय राजमार्ग पर पिछले वर्षों से सड़क चौड़ीकरण के बाद दर्जनों डेंजर जोन बने हुए हैं। जहां पर इस बार भी सोनप्रयाग के पास पहाड़ खिसकने से लगभग 1300 यात्रियों को रेस्क्यू करना पड़ा। जून के अंत में यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर सिलाई बैंड के पास निर्माण कार्य में लगे 18 मजदूरों में से 9 मजदूर बहकर लापता हो गये थे। यहां पर बहुत लंबे समय से औजरी, डाबरकोट, कुथनौर, पालीगाड़, सिलाई बैंड, किसाला आदि स्थान भू- धंसाव के लिए संवेदनशील बने हुए हैं। 2023-24 की बरसात में भी यहां पर लगातार निर्माण का मलबा सड़क पर बहकर आया था। इसके बावजूद भी करोड़ों खर्च करने के बाद इस मार्ग को चौड़ीकरण करने से पहले भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र को बचाने के लिए जो वैज्ञानिक उपाय होने चाहिए थे उस पर ध्यान नहीं गया है, जिसके कारण लंबे समय से हर बरसात में यह स्थान यमुना नदी की तरफ टूट कर बह जाता है। यमुनोत्री आने-जाने वाले तीर्थयात्री बड़ी मुश्किल से इस भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र से जान जोखिम में डालकर गुजरते हैं। जानकी चट्टी से यमुनोत्री तक 6 किमी के पैदल रास्ते पर भी एक दर्जन ऐसे संवेदनशील स्थान वैज्ञानिकों ने चिह्नित किए हैं जहां भूस्खलन का खतरा बना हुआ है। इस बार भी यहां पर लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। अतः जरूरत है कि बहुत चौड़ी सड़क के स्थान पर जहां से भूस्खलन लगातार हो रहा है उस एरिया तक पहुंच बना करके ट्रीटमेंट करने पर ध्यान देना चाहिए। सड़क मार्ग को इस डेंजर जोन पर अधिक चौड़ा करने की कोशिश करेंगे तो आने-जाने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। दूसरी ओर स्याना चट्टी के पास यमुना नदी पर झील बनने का खतरा बना हुआ है। जिस पर उत्तरकाशी के जिलाधिकारी प्रशांत आर्य लगातार नजर बनाए हुए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी यहां भूस्खलन क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण किया है। गंगा की सहायक नदी अलकनंदा, भागीरथी, भिलंगना, बालगंगा उफान पर हैं, लोग भारी बारिश और बाढ़ का सामना कर रहे हैं। हिमाचल में पिछले 15 दिनों में लगभग 17 स्थानों पर बादल फटे हैं। अब तक लगभग 100 लोगों की जिंदगी चली गई है और 55 लोग लापता हैं। लगभग 80 हजार की आबादी पर भूस्खलन का खतरा मंडरा रहा है। पूर्वोत्तर राज्यों में दक्षिण-पश्चिम मानसून पहुंचते ही हाहाकार मच गया। ब्रह्मपुत्र समेत 10 नदियां उफान पर है। सिक्किम में भूस्खलन से सेना का एक शिविर दब गया जिसमें तीन जवान शहीद हो गए थे और 6 लोग लापता हैं। असम और अरुणाचल प्रदेश में भी 10- 10 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। 10 हजार लोग राहत शिविरों में रखे गए हैं। असम और मणिपुर में चार लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं।
प्रभावित लोग महसूस कर रहे हैं कि हिमालय की भौगोलिक संरचना को नजरअंदाज करके जिस तरह से फोरलाइन मार्गों का निर्माण, वनों का कटान, बहुमंजिली इमारतें, हिमालय की संवेदनशील धरती के साथ विकास के नाम पर अनियोजित छेड़छाड़, बार-बार भूकंप आना, अनियंत्रित पर्यटन और पंचतारा संस्कृति ने अधिक उपभोग करने की चाह में संकट पैदा कर दिया है। निर्माण कार्यों में प्रयोग होने वाले विस्फोट से मलबा नदियों में एकत्रित होकर बाढ़ के हालात पैदा कर रहा है। निर्माण कार्य में लगी जेसीबी मशीनों ने भी पहाड़ को हिला कर रख दिया है। जो हिमालय की भूगर्भिक बनावट के लिए बहुत खतरनाक है। यहां के पर्यावरण और जीवनशैली के अनुरूप विकास की नई रेखा खींचनी होगी और हिमालय पर विकास के नाम पर हो रहे मैदानों के अनुरूप जैसी छेड़छाड़ को रोका जाए।
