
13-05-2022 (Important News Clippings)
To Download Click Here.
Bell the Bail Cat on A Permanent Basis
ET Editorials
The Supreme Court’s directions to the Allahabad High Court to grant bail to 1,500-odd first-time offenders who have been languishing in jail for 10 years is the right decision. It turns the spotlight on a malaise that afflicts India’s justice system. Courts need to conduct a thorough audit to identify reasons for high pendency rates and put in place measures to ensure resolution of cases in a time-bound manner. Granting bail for crimes where bail is applicable must become a default, not the first recourse.
The high court is hearing cases filed in the 1980s. It is not unlikely that another decade could be spent before the cases of these undertrials languishing in jail are taken up. The Allahabad High Court tops the pendency charts even as it works steadily to reduce its backlog. But it is not the only one, with pendency afflicting the entire judicial system. Pendency rates are rapidly rising in some high courts like Andhra Pradesh, Telangana and Karnataka. There are 5. 6 million cases stuck in high courts across India, with 41% cases pending for five years or more, and 21% for 10 years or more. Vacancies on the bench, hearing of frivolous cases, litigants bypassing subordinate courts and endless continuances by lawyers are among the factors that result in cases persisting for years, even decades, on end. Ignorance of the law and lack of access to legal services means a large number of those charged being unable to seek bail, let alone get proper advice.
The apex court move is humane. But it is a band-aid that it has applied before. It is time for a systemic response that does away with a triage method. Justice should be fair and speedy. A slow-moving justice system institutionalises inequity by victimising those without resources.
बराबरी एक सपना है या साकार होने वाला सच?
हरिवंश, ( राज्यसभा के उपसभापति )
सृष्टि की उत्पत्ति के साथ ही शायद प्रकृति ने सौगात में यह सवाल दिया है इंसान को कि बराबरी एक सपना है या साकार होने वाला। विश्व-श्रेष्ठ फ्रांसीसी अर्थशास्त्री थॉमस पिकेटी की नई चर्चित किताब ‘ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इक्विलिटी’ (समता का संक्षिप्त इतिहास) में इसी यक्षप्रश्न का उत्तर है। तथ्यों, विश्लेषण व संदर्भों के साथ।
अर्थशास्त्रियों में ‘राॅक स्टार’ विशेषण पाने वाले पिकेटी वर्ष 2013 में ही विश्वविख्यात हो गए थे, संसार में सर्वाधिक बिकने वाली अपनी पुस्तक ‘कैपिटल इन द ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी’ (21वीं सदी में पूंजी) से। आर्थिक विकास दर पर पचास वर्षीय पिकेटी के एक सूत्र ने दुनिया में नई बहस को प्रेरित किया था। उन्होंने बताया था कि पूंजी पर आय आर्थिक विकास की रफ्तार से अधिक होती है। इस कारण पैसे वाले तेजी से समृद्ध होते हैं, शेष पीछे रह जाते हैं। इसी से सामाजिक विषमता बढ़ती है। वर्ष 2001 में वे ‘टाप इनकम्स ओवर द ट्वेंटीएथ सेंचुरी’ लिख चुके थे। 2019 में पुनः उनकी किताब ‘कैपिटल एंड आइडियोलाजी’ विश्वव्यापी चर्चा का केंद्र बनी। ये तीनों किताबें औसतन हजार पन्नों से अधिक की थीं। पूंजी, विचारधारा, समता जैसे गम्भीर विषयों पर उनके शोध, लेखन और पुस्तकों ने सरकारों नीतियों पर भी गहरा असर डाला।
अपनी नई पुस्तक ‘ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इक्विलिटी’ का आरंभ वे अपने पाठक के एक सवाल से करते हैं। ‘आप (यानी पिकेटी) जो कुछ लिखते हैं, बहुत रोचक है, पर क्या आप इसे संक्षिप्त नहीं कर सकते, ताकि आपके शोध को अपने मित्रों और परिवार से साझा कर सकूं?’ पिकेटी बताते हैं यह किताब आंशिक रूप से वर्षों से पूछे जा रहे इस सवाल का जवाब भी है। विगत 250 वर्षों में संसार में संपदा के केंद्रीकरण, पूंजी और विचारधारा और कर लगाने की पद्धति के विशद् अध्ययन के बाद पुस्तक के निचोड़ में वे कहते हैं कि ‘मैं अपेक्षाकृत आशावान हूं।’ उनकी बातों का सार है कि उतार-चढ़ाव की गति या आंदोलनों के साथ संसार की यह दीर्घकालीन यात्रा अधिक समता की ओर है। संभव है किसी खास दशक में कहीं विपरीत चीजें हों, पर समाज उसे दीर्घकाल में सही कर देता है।
पिछले कुछ दशकों में बढ़ी विषमता को लेकर संसार में चिंता व निराशा रही है। उस दौर में पिकेटी का यह निष्कर्ष आश्वस्तकारी है। पिकेटी की दृष्टि में ऐतिहासिक साक्ष्यों की प्रबल धारा हमें आशावान होने का आधार देती है। अपने विशद् अध्ययन से वे बताते हैं कि शताब्दियों से इंसान व संसार पुरजोर समता की ओर बढ़ रहा है।
पिकेटी ने इतिहास व मानव समाज के बड़े आंदोलनों-पड़ावों को चुना है, अपने अध्ययन के लिए कि यह यात्रा कैसे समता की मंजिल की ओर अग्रसर है। सामाजिक संघर्ष का इतिहास इसे गति देता रहा है। पूंजीवाद, क्रांतियां, साम्राज्यवाद, दासता के खिलाफ युद्ध और अंततः कल्याणकारी राज्य का उद्भव। हिंसा, आपदा, प्रतिक्रांति के बावजूद मानव समाज सही तरीके से अधिक समतापूर्ण समाज की ओर बढ़ रहा है। वे यह भी स्वीकार करते हैं कि हम और बेहतर कर सकते हैं। सामाजिक, वैधानिक व राजकोषीय नीतियों में आवश्यक कदम उठाकर और शिक्षा व संस्थानों की व्यवस्था को और मजबूत कर।
कुछेक सौ वर्षों पहले तक धारणा थी कि विषमता प्राकृतिक विधान है। सर्वोदयी दादा धर्माधिकारी ने कहा था कि कार्ल मार्क्स के पहले किसी देवदूत या धर्मदूत ने यह नहीं कहा कि गरीबी का अंत संभव है, या कि यह ईश्वर की देन नहीं, बल्कि मानव व्यवस्था की उपज है। 17वीं सदी में हाब्स व लॉक के प्राकृतिक समता के सिद्धांत या रूसो के सामाजिक करार की बात ने एक नई चेतना-ऊर्जा दी थी, मानव समाज को। 18वीं सदी तक मानव समाज गैर बराबरी के खिलाफ मुकम्मल सपना देखने की स्थिति में आ गया था।
फ्रांस में हुई क्रांति के तीन सौ सालों बाद, साक्ष्यों के अध्ययन के आधार पर विश्व-मशहूर अर्थशास्त्री पिकेटी बता रहे हैं कि मानव समाज की ऐतिहासिक यात्रा बराबरी की ही ओर अग्रसर है। इस अर्थ में यह निष्कर्ष, इतिहास के उन सभी चर्चित-अचर्चित नायकों, घटनाओं, मोड़ों के प्रति कृतज्ञता बोध है, जिनसे गुजरते हुए इंसान एक समतापूर्ण समाज की मंजिल की ओर पांव बढ़ाता रहा है।
बेलगाम आचरण की बानगी
संपादकीय
इससे बड़ी विडंबना कोई और नहीं हो सकती कि भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चलाने वाली एजेंसी सीबीआइ के इंस्पेक्टर ही भ्रष्ट आचरण में लिप्त पाए जाएं। सीबीआइ ने दिल्ली में तैनात अपने चार सब इंस्पेक्टरों को उगाही के आरोप में जिस तरह गिरफ्तार किया उससे यही पता चल रहा है कि इस एजेंसी में ऐसे भी तत्व हैं जो बेलगाम हो चुके हैं और अपने अधिकारों का हर तरह से दुरुपयोग करने में लगे हुए हैं। इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि सीबीआइ ने इन सब इंस्पेक्टरों को बर्खास्त करते हुए यह कहा कि वह भ्रष्टाचार और अन्य तरह के कदाचार को सहन नहीं कर सकती, क्योंकि उसे उन कारणों की तह तक जाने की जरूरत है जिनके चलते उसके कर्मचारी-अफसर बिना किसी भय और संकोच के अपराधियों की तरह व्यवहार करने लगते हैं। क्या सीबीआइ इंस्पेक्टरों को जरूरत से ज्यादा अधिकार हासिल हैं या फिर उनके कामकाज की कहीं कोई निगरानी नहीं होती? इन प्रश्नों पर गंभीरता से विचार-विमर्श किए जाने की जरूरत है।
बर्खास्त किए गए सीबीआइ के चार सब इंस्पेक्टरों को चंडीगढ़ के एक कारोबारी को धमकाकर उससे पच्चीस लाख रुपये मांगने का आरोप है। यह बेहद गंभीर मामला है। यह कहना कठिन है कि यह अपने ढंग का इकलौता मामला है या फिर इसे अपवाद की संज्ञा दी जा सकती है, क्योंकि इस तरह के प्रकरण पहले भी सामने आ चुके हैं जिनमें सीबीआइ कर्मचारी और अफसर अवैध काम करते अथवा भ्रष्टाचार में शामिल पाए गए हैं। दुर्भाग्य से इनमें कुछ शीर्ष स्तर के अफसर भी रहे हैं। इसका कारण यही हो सकता है कि सीबीआइ के कर्मचारी और अधिकारी जवाबदेही से मुक्त हैं। ध्यान रहे कि जब भी कोई जांच एजेंसी पारदर्शी ढंग से काम नहीं करती और वह जवाबदेही के दायरे से भी बाहर होती है, तो उसके कर्मचारियों और अधिकारियों के बेलगाम होने का खतरा कहीं अधिक बढ़ जाता है। सीबीआइ जैसी संस्था के लिए यह आवश्यक ही नहीं, बल्कि अनिवार्य है कि वह न केवल अपने कामकाज में पारदर्शिता लाए, बल्कि अपनी छवि के प्रति सतर्क भी रहे। उसके बेलगाम और भ्रष्ट अधिकारी न केवल उसकी छवि पर प्रहार करते हैं, बल्कि उसके प्रति आम जनता के भरोसे को भी कम करते हैं। उचित यह होगा कि केंद्र सरकार सीबीआइ की छवि की चिंता करे। इसके अतिरिक्त उसे उन कारणों का भी निवारण करना होगा जिनके चलते कई राज्यों ने यह आरोप लगाते हुए उसे अपने यहां के मामलों की जांच करने से रोक दिया है कि यह केंद्रीय सत्ता की कठपुतली के रूप में काम करने वाली एजेंसी है। यह चिंता की बात है कि ऐसे राज्यों की संख्या बढ़ती चली जा रही है।
 Date:13-05-22
Date:13-05-22
स्वनियमन समाधान नहीं
संपादकीय
बीते कुछ महीनों में एडटेक बाजार में तेज उछाल को लेकर जो जश्न का माहौल था, कारोबारी कदाचार की खबरें सामने आने के बाद अब उसमें खामोशी नजर आ रही है। कम से कम एक यूनिकॉर्न (एक अरब डॉलर से अधिक मूल्यांकन वाली कंपनी) को एक उपभोक्ता को हर्जाना देना पड़ा क्योंकि उसने भ्रामक विज्ञापन दिए थे। सरकार ने दिसंबर में उपभोक्ताओं को एडटेक के गलत आचरण के बारे में जो मशविरे दिए थे उसके बाद इस उद्योग पर ध्यान देने वालों को लगा था कि राज्य के हस्तक्षेप से इस क्षेत्र में हो रही तेज कमाई पर लगाम लग सकती है। जनवरी में भारतीय एडटेक संघ का गठन किया गया ताकि एक साझा आचार संहिता बन सके तथा उसका पालन किया जा सके। सभी बड़े नाम इसमें शामिल हुए। संहिता में नैतिक बिक्री व्यवहार, विपणन संचार, ऋण संबंधी व्यवहार तथा रिफंड आदि बातें शामिल की गईं। एक दो स्तरीय शिकायत निवारण प्रणाली भी बनायी गई।
यह एक चतुराईपूर्ण कदम था। केवल इसलिए नहीं कि एडटेक कारोबार अपनी प्रकृति में व्यापक निजी शिक्षा क्षेत्र की तुलना में बहुत अधिक वाणिज्यिकृत हो चुका था, हालांकि वह भी बहुत तेजी से बराबरी की ओर बढ़ रहा है। भारत में इसकी शुरुआत एक छोटे कारोबार के रूप में हुई थी जहां यह तकनीकी और प्रबंधन शिक्षा की मांग पूरी करता था तथा ट्यूशन सेवाओं के पूरक के रूप में काम करता था। निगरानी के दायरे के बाहर काम करने के कारण इसने उपभोक्ता विपणन के वे तमाम हथकंडे अपना लिए जिनका अकादमिक जगत से कम और छवि निर्माण से ज्यादा लेनादेना था। शिक्षकों के विज्ञापन देना और उन्हें रेटिंग देना, लोकप्रिय कार्यक्रमों का प्रायोजन करना तथा संदेहास्पद उत्पत्ति वाले रेफरल विज्ञापन देना, ऋण की व्यवस्था करना और वित्तीय सेवा उद्योग की तरह रिफंड आदि की प्रासंगिक सूचनाओं को छोटे अक्षरों में छापने जैसे काम किए जाने लगे। जब तक एडटेक उद्योग व्यापक प्रसार वाले निजी शिक्षण क्षेत्र के सामने हाशिये पर रहा तब तक इसकी ओर ज्यादा ध्यान नहीं गया। लेकिन महामारी के आगमन के बाद हालात बदल गए। स्कूल बंद हो गए और सरकारी स्कूलिंग व्यवस्था के ठप पडऩे के बाद ऑनलाइन शिक्षण की मांग तेजी से बढ़ी। ऐसे में उत्पन्न अंतर को पाटने का काम एडटेक क्षेत्र ने किया। महामारी के कारण दो वर्ष तक स्कूल बंद रहे और एडटेक उद्योग को होने वाली फंडिंग 2019 के 50 करोड़ डॉलर से बढ़कर 2020 में 4 अरब डॉलर और 2021 में 6 अरब डॉलर पार कर गई। इस क्षेत्र में पांच यूनिकॉर्न तैयार हो गईं। इसमें से काफी पैसा किंडरगार्टन से कक्षा 12 (के-12) तक के क्षेत्र में आया। 2018 से दुनिया भर में के-12 क्षेत्र में जितने स्टार्टअप तैयार हुए उनमें भारत की हिस्सेदारी 37 फीसदी रही। इससे हालात तेजी से बदले। अच्छी हैसियत वाले शहरी उपभोक्ताओं से बाजार ग्रामीण, अद्र्धशहरी और शहरों के अल्प आय वर्ग वाले हिस्से में स्थानांतरित हो गया। एडटेक कंपनियों ने इन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया, ऐसे में उन्होंने अपारदर्शी विपणन व्यवहार अपनाया और आखिरकार सरकार को मशविरा जारी करना पड़ा। स्वनियमन के मानक बनाने वाली संस्था का गठन सही दिशा में उठाया गया कदम है लेकिन इससे आधी समस्या का ही समाधान होगा। भारत में स्व नियमन को मिलीजुली सफलता ही मिली है। विज्ञापन जगत में यह कुछ क्षमता से काम करता दिखता है लेकिन मीडिया में यह कम प्रभावी और सूक्ष्म वित्त क्षेत्र में तो यह लगभग नाकाम ही है।
अगर जुर्माना नहीं लगाया गया तो यह कहना मुश्किल है कि एडटेक संघ गड़बड़ी करने वालों पर अंकुश लगा पाएगा या नहीं। उपभोक्ता अदालतों तक भी सबकी पहुंच नहीं है। संघ ने सरकार को सूचित किया है कि उसने स्वनियमन के लिए संस्था बनायी है लेकिन शिक्षा मंत्री ने कहा है कि वह इस क्षेत्र पर नजर बनाये रखेंगे। यह अच्छा निर्णय है।
कठघरे में अदालत की भाषा
प्रमोद भार्गव

महात्मा गांधी ने भी अदालतों में अंग्रेजी के प्रयोग पर आपत्ति जताते हुए कहा था कि अंग्रेजी से बेहतर होगा कि हिंदी का प्रयोग बोलचाल और देश की आधिकारिक भाषा के तौर पर तो किया ही जाए, न्यायालयों में भी इसका प्रयोग होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो लोगों को न्यायिक प्रक्रिया पूरी तरह समझ नहीं आएगी। इसलिए राष्ट्रीय और क्षेत्रीय भाषाओं का अदालतों में प्रयोग होना आवश्यक है। उनका कहना था कि जब तक हम हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिला देते और अन्य स्थानीय भाषाओं को उनका अपेक्षित महत्त्व नहीं दिला देते, तब तक स्वराज्य की सारी बातें अर्थहीन रहेंगी। गांधीजी ने अदालतों में क्षेत्रीय भाषाओं की यह पैरवी 1918 में इंदौर में संपन्न हुए हिंदी साहित्य सम्मेलन के आयोजन में कही थी। प्रधानमंत्री ने उसी बात पर जोर दिया है।
दरअसल, जिस कानून की भाषा अशिक्षित आमजन की समझ में नहीं आती, उसके पालन की अपेक्षा उससे करना व्यर्थ है। इसीलिए प्रधानमंत्री ने कानून बनाते समय ही मूल कानून के साथ सरल भाषा में उसकी व्याख्या जोड़ने की बात कही है। इस प्रयोग पर अमल होता है, तो कानून न्यायाधीशों और अधिवक्ताओं की समझ के दायरे से बाहर निकल कर आम नागरिक की समझ में भी आने लगेगा। स्थानीय भाषा में अदालतों को काम करने में कोई असुविधा नहीं होगी, क्योंकि आज भी देश की सभी जिला और तहसील स्तरीय अदालतें स्थानीय भाषाओं में लगभग पूरा काम करती हैं। केवल चिकित्सा और न्यायिक जाचें अंग्रेजी में होती हैं। इनके भी निष्कर्ष क्षेत्रीय भाषाओं में दिए जा सकते हैं।
हालांकि अब भी उच्च और उच्चतम न्यायालय केवल अंग्रेजी में काम करते हैं। इसके पीछे उनका तर्क है कि उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को देश के किसी भी राज्य में स्थानांतरित होकर जाना पड़ता है। इनमें वे भी राज्य होते हैं, जिनकी भाषा न्यायाधीश की भाषा से भिन्न होती है। पर यह तर्क उचित नहीं है। क्योंकि संघ लोकसेवा आयोग की परीक्षा पास करके जो लोग जिलाधीश और जिला दंडाधिकारी बन कर देश भर में जाते हैं, वे न केवल स्थानीय भाषा में दिए आवेदनों पर कार्रवाई करते हैं, बल्कि राजस्व न्यायालयों का कार्य भी करते हैं। राजस्व से संबंधित दस्तावेज स्थानीय भाषाओं में होते हैं और वकील उन्हीं भाषाओं में पैरवी करते हैं। अंतत: राजस्व न्यायालयों के फैसले भी स्थानीय भाषा में ही आइएएस देते हैं। स्थानीय भाषा में फैसले आने से कोई भाषागत विसंगति भी देखने में नहीं आती।
यह अच्छी बात है कि अब न्यायपालिका और विधायिका में स्थानीय भाषाओं में न्यायालयों का काम करने पर सहमति बन रही है। इससे अंग्रेजी की कथित रूप से बना दी गई अनिवार्यता के चलते जो प्रतिभाएं खिलने से पहले ही मुरझा जाती हैं, वे भी प्रोत्साहित होकर फलेंगी। शिक्षा में आरक्षण का लाभ लेकर वंचित समुदाओं के जो विद्यार्थी प्रवेश पा रहे हैं, उन्हें अंग्रेजी माहौल के चलते आत्मघाती कदम उठाने तक को विवश होना पड़ रहा है। साफ है, यह प्रभुत्व व्यापक रूप लेकर हिंदी और भाषाई माध्यमों से पढ़ कर आने वाले युवाओं में घातक हीनता का बोध पैदा कर रहा है। इसलिए अब समय आ गया है कि अंग्रेजी बनाम हिंदी की बहस को भारतीय भाषाओं की निरीहता के रूप में देखा जाए? अगर ऐसा होता है तो इसके न्यायिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और शैक्षिक पहलुओं पर गंभीरता से विचार कर भाषाई समस्या का तार्किक और व्यावहारिक सामाधान निकालना संभव होगा।
इसमें कोई दो राय नहीं कि वर्तमान भूमंडलीकृत उदारवादी और आधुनिक तकनीक आधारित वैश्विक फलक पर अंग्रेजी का अपना महत्त्व है। मगर इससे यह आवश्यक नहीं हो जाता कि न्याय, शासन-प्रशासन और उद्योग-व्यापार के रोजमर्रा के काम उस भाषा में हों, जिसे देश की अट्ठानबे प्रतिशत जनसंख्या जानती ही नहीं। जिस बहस और फैसले को वादी-प्रतिवादी समझ ही न सकें, उसे न्याय कहें या अन्याय! मुठ्ठीभर लोग जिस न्याय प्रक्रिया और उसके परिणाम से निकले निष्कर्ष को समझते हों, यह लोकतंत्र की भावना के विरुद्ध सीधे-सीधे साजिश है।
देश की सभी निचली अदालतों में संपूर्ण कामकाज हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में होता है, पर उच्च और उच्चतम न्यायालयों में यही काम केवल अंग्रेजी में होता है। यहां तक कि जो न्यायाधीश हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं जानते हैं, वे भी अपीलीय मामलों की सुनवाई में दस्तावेजों का अंग्रेजी अनुवाद कराते हैं। यह देश और संविधान की विडंबना ही है कि अनुच्छेद-19, 343, 346, 347, 350 और 351 में कहीं भी अंग्रेजी की बाध्यता नहीं है। अनुच्छेद-19 में भारत के सभी नागरिकों को ‘अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता’ दी गई है। यह अभिव्यक्ति संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किसी भी भारतीय भाषा में हो सकती है। मगर संविधान द्वारा प्राप्त यह बुनियादी अधिकार उच्च और सर्वोच्च न्यायालय की देहरी पर जाकर ठिठक जाता है। यहां अपीलें और यचिकाएं अंग्रेजी में ही विचार के लिए स्वीकार की जाती हैं।
किसी भी मुकदमे के दो बिंदु अहम होते हैं। एक, प्रथम सूचना प्रतिवेदन और दूसरा याची, अभियुक्त और साक्षी के बयान। प्राथमिकी स्थानीय भाषा में लिखी जाती है और फरियादी, आरोपी और गवाह भी अपने बयान अपनी-अपनी भाषा में देते हैं। कभी-कभी इनके बयानों के अनुवाद अर्थ का अनर्थ भी कर देते हैं। ऐसे में संविधान का प्रजातांत्रिक न्यायवादी आग्रह उच्च न्यायालयों की देहरी पर ही खारिज कर दिया जाता है।
दुनिया में जितने भी देश महाशक्ति के दर्जे में आते हैं, उनकी अदालतों में मातृभाषा चलती है। यूरोपीय देशों में जैसे-जैसे शिक्षा और संपन्नता बढ़ी, वैसे-वैसे राष्ट्रीय स्वाभिमान प्रखर होता चला गया। फ्रांस ने 1539 में लैटिन को अपनी अदालतों से बेदखल किया। जर्मनी ने अठारहवीं सदी में लैटिन से पिंड छुड़ा लिया। इंग्लैंड की अदालतों में एक समय जर्मनी और फ्रांसीसी भाषाओं का ही बोलबाला था। यहां अंग्रेजी बोलने पर हजारों पाउंड का जुर्माना लगा दिया जाता था, लेकिन 1362 में जर्मन और फ्रांसीसी को पूरी तरह बहिष्कृत कर अंग्रेजी को इंग्लैंड की अदालतों में आधिकारिक भाषा बना दिया गया। रूस, चीन, जापान, वियतनाम और क्यूबा में भी मातृभाषाओं का प्रयोग होता है। इन देशों से भारत और भारतीय अदालतें कोई सबक या प्रेरणा लिए बिना अंग्रेजी को अब तक ढोती चली आ रही हैं। गोया, अदालतों को अब स्वप्रेरणा से इस भाषायी रंगभेद की दासता से मुक्त होने की जरूरत है। शीर्ष अदालत अगर यह पहल करती है, तो देखते-देखते भारतीय भाषाएं प्रशासन के क्रियाकलापों का सशक्त माध्यम बन जाएंगी। इस पहल से आमजन की न्याय-प्रक्रिया में समझ और संप्रेषणीयता तो बढ़ेगी ही, शासन-प्रशासन मानवता के कल्याण का वाहक भी बनने की दिशा में अग्रसर होगा।
निजता का सम्मान जरूरी
संपादकीय
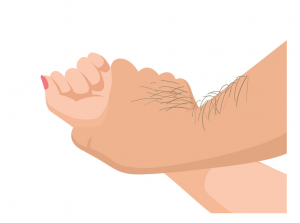
नई कार्य-संस्कृति
संपादकीय
पिछले दो दिन में तीन घटनाएं बिल्कुल अलग-अलग घटीं, लेकिन ये तीनों हमें एक सकारात्मक दिशा में ले जाती हैं। इनमें सबसे ताजा खबर झारखंड की है, जहां वरिष्ठ आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया और पूछताछ के लिए पांच दिन की रिमांड भी हासिल कर ली है। कुछ ही दिनों पहले जब उनके करीबियों के यहां निदेशालय का छापा पड़ा, तो नोटों की इतनी गड्डियां मिलीं कि उनकी तस्वीरें देखकर पूरे देश ने दांतों तले उंगली दबा ली थी। सिंघल झारखंड की खनन सचिव हैं और छापे की इन खबरों से ही लोग समझ पाए कि इस राज्य की अथाह खनिज संपदा किन्हें समृद्ध कर रही है। झारखंड की इस घटना के साथ एक खबर उत्तर प्रदेश से आई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को राज्य के पुलिस महानिदेशक का तबादला कर दिया। उनके खिलाफ आरोप थे- विभागीय कार्यों में रुचि न लेना और अकर्मण्यता। यह शायद पहली बार हुआ है कि किसी इतने बड़े अधिकारी का अकर्मण्यता के आरोप में तबादला किया गया हो। तीसरी खबर भारतीय रेलवे से आई। रेलवे बोर्ड ने एक ही दिन में प्रथम श्रेणी के 19 बड़े अधिकारियों को जबरन रिटायर कर दिया। ये वही अधिकारी हैं, जिन्हें कामकाज की समीक्षा में अक्षम पाया गया था। इन अधिकारियों को पहले ही चेतावनी दे दी गई थी, लेकिन जब बात नहीं बनी, तो उन्हें स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति दे दी गई।
सरकारों द्वारा किए गए ये फैसले हमें हैरत में डाल सकते हैं, लेकिन देश के निजी क्षेत्र में ऐसा नियमित तौर पर ही होता है। कंपनी क्षेत्र में सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के कामकाज की समीक्षा की एक पक्की व्यवस्था होती है, लगातार असफल रहने वालों को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है, और भ्रष्टाचार को किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं किया जाता। यही कारण है कि निजी क्षेत्र की कार्य-कुशलता सरकारी क्षेत्र के मुकाबले हमेशा ही बहुत अच्छी रहती है। सरकारें भी अगर इस कार्य-संस्कृति को अपनाती हैं, तो यह स्वागत-योग्य है।
नौकरशाही को हमेशा से भारतीय तंत्र के सबसे अड़ियल हिस्से के तौर पर देखा जाता रहा है। दुनिया भर में धारणा यही है कि भारत में बदलाव की सबसे बड़ी बाधा उसकी नौकरशाही है, जो किसी भी अच्छी नीति को फाइलों और उन पर लगे लाल फीतों में उलझा देने की क्षमता रखती है। उसके पास अधिकार तो बहुत हैं, लेकिन दीर्घकालिक जवाबदेही कुछ भी नहीं। इसमें बदलाव के लिए देश में दो बार प्रशासनिक सुधार आयोग भी बने, लेकिन उनकी ज्यादातर सिफारिशों को उन फाइलों के हवाले कर दिया गया, जो आज तक धूल फांक रही हैं। यह बात सही है कि कंप्यूटर और सूचना तकनीक के आगमन से प्रशासन के तौर-तरीकों में बहुत सारी चीजें बदली भी हैं, मगर सच्चाई यही है कि नौकरशाही पर अभी भी पूरी तरह से लगाम नहीं लग सकी है। एक बात तय है कि देश के महाशक्ति बनने के नए सपने और नौकरशाही के पुराने तौर-तरीके, दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकतीं। इन सपनों को जमीन पर उतारने के लिए नौकरशाही को आमूल-चूल ढंग से बदलना ही होगा। इसलिए यह जो बदलाव दिख रहा है, वह बड़ी उम्मीद बंधाता है। हालांकि, सिर्फ दो-तीन अच्छे उदाहरणों से अब काम चलने वाला नहीं है। जरूरी है कि नौकरशाही के सभी स्तरों पर ऐसी एक स्थायी व्यवस्था बने, जो इसे एक नई कार्य-संस्कृति में ढाल दे।
Date:13-05-22
पुलिस में अपनी मंजिल से दूर महिलाएं
मजा दारूवाला, ( वरिष्ठ सलाहकार, सीएचआरआई )
हाल ही में उत्तर प्रदेश ने राज्य के पुलिस बल में महिलाओं की संख्या को 20 प्रतिशत तक बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर पुलिस भर्ती अभियान की घोषणा की है। साल 2013 में ही केंद्र सरकार ने राज्यों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी थी कि हर पुलिस स्टेशन में कम से कम 10 महिला कांस्टेबल और तीन सब-इंस्पेक्टर की तैनाती होनी चाहिए। राष्ट्रीय स्तर पर स्त्रियों के अनुपात का नीतिगत बेंचमार्क 33 प्रतिशत है, मतलब देश में कुल पुलिसकर्मियों में महिलाएं 33 प्रतिशत होनी चाहिए। गौर करने की बात यह है कि बिहार में 2010 में पुलिस बल में दो प्रतिशत से भी कम महिलाएं थीं, मगर 2019 तक 25.3 प्रतिशत हो गईं, यहां पुलिस में महिलाओं की हिस्सेदारी में सबसे तेज वृद्धि देखी गई।
ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च ऐंड डेवलपमेंट (बीपीआरऐंडडी) के अनुसार, देश में अभी भी ऐसे राज्य हैं, जहां चार प्रतिशत महिला पुलिसकर्मी भी नहीं हैं। तत्कालीन जम्मू-कश्मीर राज्य में न्यूनतम 3.31 प्रतिशत महिलाएं पुलिस बल में थीं। सरकारी आंकड़े बता रहे हैं कि पुलिस लिंगानुपात में बिहार अभी सबसे बेहतर स्थिति में है। भारत को महिला पुलिसकर्मियों के मामले में साल 2010 में 4.25 प्रतिशत से बढ़कर 2021 में 10.49 प्रतिशत से ऊपर जाने में एक दशक से अधिक का समय लग गया है। इसके उलट, मलेशिया और चीन में क्रमश: 18 एवं 14 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मी हैं। इंग्लैंड में 33 प्रतिशत से अधिक महिला पुलिसकर्मी होने का दावा किया जा सकता है।
ऐसा नहीं कि पुलिस बल में रिक्तियां नहीं हैं, राष्ट्रीय औसत लगभग 21.4 प्रतिशत है, पर आम चलन यही है कि किसी भर्ती में महिलाओं की बहाली एक तिहाई से अधिक न हो। इस दर से, जैसा कि ‘इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020’ बताती है, बिहार को 33 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मियों तक पहुंचने में तीन और साल लगेंगे, जबकि मध्य प्रदेश जैसे राज्य को 180 साल लग जाएंगे। भर्ती में कांस्टेबल स्तर की रिक्तियों को भरने पर जोर दिया जाता है, जबकि मुख्य जांच व पर्यवेक्षी भूमिकाएं पुरुषों के लिए बनी रहती हैं। नतीजतन,स्त्रियाँ खुद को निम्न श्रेणी में समूहबद्ध पाती हैं। जिन राज्यों में महिला पुलिसकर्मियों का प्रतिशत सर्वाधिक है, जैसे बिहार एवं हिमाचल प्रदेश, वहां भी अधिकारी स्तर पर सिर्फ छह और पांच प्रतिशत महिलाएं हैं।
फिर भी पुलिस बल में महिलाओं की संख्या बढ़ाने का इरादा स्वागतयोग्य है। साल 2015 और 2020 के बीच, महिला पुलिसकर्मी के मामले में तमिलनाडु 13 से 19 प्रतिशत, गुजरात चार से 16 प्रतिशत व तेलंगाना तीन से आठ प्रतिशत पर पहुंच गया। अन्य राज्य पिछड़ गए या फिर स्थिर पाए गए, जैसे मिजोरम (6.8 से सात प्रतिशत), सिक्किम (आठ से 8.4 प्रतिशत), और ओडिशा (8.8 फीसदी से 9.1 प्रतिशत)।
सामान्य रूप से यह बहाना बनाया जाता है कि महिलाएं अपनी शारीरिक और मानसिक दृढ़ता की कमी का हवाला देते हुए पुलिस में शामिल होने के लिए तैयार नहीं होती हैं। खतरनाक कार्रवाई और शारीरिक कौशल पर कई बार ज्यादा निर्भरता के बावजूद वास्तव में पुलिस के जिम्मे बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं, जिनमें अधिक दिमाग के इस्तेमाल की जरूरत पड़ती है।
पुलिस में रोजमर्रा के अधिकांश कार्यों में स्थानीय समुदायों के साथ संवाद, शिकायत निवारण, सुलह, समस्या समाधान, गश्त, अपराध रोकथाम, यातायात नियमन, गंभीर अपराध दर्ज करना, सुबूत जुटाना, रिकॉर्ड रखना और अदालत में पेश करना शामिल है। इन सभी कार्यों के लिए कुशल बुद्धि, संवाद कौशल और ज्ञान की जरूरत पड़ती है। पुलिस को सड़कों पर नागरिकों के साथ लड़ाई में भाग लेने या हर दिन सशस्त्र लुटेरों को रोकने की जरूरत नहीं है। इन हालात में भी महिलाएं बहादुरी से खुद को बरी करती नजर आ रही हैं। केरल के पूर्व पुलिस महानिदेशक जैकब पुन्नूस का कहना है, ‘महिलाओं को पुलिस में जितनी नौकरी चाहिए, उससे कहीं अधिक अच्छी पुलिसिंग के लिए पुलिस बल में महिलाओं की जरूरत है।’ यह सच है।
फिर भी पुलिस बल में महिलाओं को ज्यादा संख्या में शामिल करने के लिए संस्थागत तैयारियों का अभाव है। अलग शौचालय की व्यवस्था, काम के उचित घंटे, और फ्लेक्सी-टाइम (सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं) देने की अनिच्छा से लेकर, आदेशों को स्वीकार करने तक और गहन पितृ-सत्तात्मक प्रतिरोध तक अनेक समस्याएं हैं, जिन्हें दूर करना चाहिए। यौन उत्पीड़न समितियों और सख्त आदेशों के माध्यम से कार्यस्थल पर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने में सक्षम नहीं होना पुलिस के लिए भी एक गंभीर मुद्दा है। पुलिस बल में किसी भी अनुचित व्यवहार के लिए शून्य सहनशीलता की नीति होनी चाहिए। ध्यान रहे, यहां बदमाशी और उत्पीड़न के मामले कम रिपोर्ट किए जाते हैं।
2019 की पुलिसिंग रिपोर्ट की स्थिति पर आधारित एक सर्वेक्षण में एक चौथाई पुलिसकर्मियों ने कहा कि उनके थाने/क्षेत्राधिकार में कोई यौन उत्पीड़न समिति नहीं है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बिहार, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में पुलिस बल में महिलाओं के खिलाफ पूर्वाग्रह उच्चतम स्तर पर है, यानी इन राज्यों में कर्मियों के यह मानने की सबसे अधिक आशंका है कि महिला पुलिसकर्मी कम कुशल होती हैं और उन्हें अपने व घर पर ध्यान देना चाहिए। संस्थागत आवास की कमी भी उन्हें सामाजिक रूप से ज्यादा परेशान करती है। दूसरों को सुरक्षा देने से पहले महिलाओं को अपने पेशेवर परिवेश में सुरक्षित और सम्मानित महसूस करने में सक्षम बनाना होगा। पुलिस बल की छवि भले आकर्षक न हो, लेकिन रोजगार की जरूरत और बेहतर जीवन के अवसरों की स्वाभाविक महत्वाकांक्षा अक्सर इस पर हावी हो जाती है।
महिलाओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा को कम करने के लिए भी महिला पुलिसकर्मियों की बड़ी जरूरत है। पुलिस बल में जब समानता की स्थिति होगी, तो महिलाएं भी ज्यादा संख्या में उसमें शामिल होंगी। जाहिर है, महिलाएं उन क्षेत्रों में ज्यादा जाती हैं, जहां उनका स्वागत होता है। बिहार एक प्रमाण है, परंपराओं से बंधे हुए इस राज्य में जब महिलाओं को सामूहिक रूप से पुलिस बल में शामिल होने का मौका मिला है, तो वे अपनी इच्छा से आगे आई हैं।
