
12-04-2025 (Important News Clippings)
To Download Click Here.
Destination India, Better the Journeys
ET Editorials
 India’s outbound tourism is booming amid global tensions and economic headwinds. By 2027, India is projected to become the world’s 5th-largest outbound travel market, with spending expected to touch $89 bn. Overseas expenditure hit $31.7 bn in FY24 — a 25% jump from the previous year. Japan has become a favoured destination for Indian travellers — there was a 53% increase in visitors since 2019. Vietnam has captivated Indian tourists, with new direct flights more than tripling passenger traffic to the Southeast Asian country. The number of Indians travelling abroad is expected to continue increasing, fuelled by rising disposable incomes and an expanding middle class.
India’s outbound tourism is booming amid global tensions and economic headwinds. By 2027, India is projected to become the world’s 5th-largest outbound travel market, with spending expected to touch $89 bn. Overseas expenditure hit $31.7 bn in FY24 — a 25% jump from the previous year. Japan has become a favoured destination for Indian travellers — there was a 53% increase in visitors since 2019. Vietnam has captivated Indian tourists, with new direct flights more than tripling passenger traffic to the Southeast Asian country. The number of Indians travelling abroad is expected to continue increasing, fuelled by rising disposable incomes and an expanding middle class.
But inbound tourism is sluggish. In 2023, 4.3 mn Indians travelled to Southeast Asia, while just 750,000 Southeast Asians came to India. To reverse this, India needs more than glossy campaigns and relaxed policies. The basics must be fixed: transport, connectivity, infrastructure and, above all, traveller experience. India has just 166,000 branded hotel rooms as of late 2024, and the quality of unbranded ones is patchy. Safety, air quality and honest service matter. So does ease of entry. While rivals like Thailand and the UAE offer seamless visas, India’s complex process is a deterrent. The country must also shake off its reputation for touts and overcharging.
India’s travel potential is vast, but it’s competing in a global market where tourists have options — and expectations. Cleanliness, efficient public transport, responsive service and ease of access can make or break a visitor’s experience. Cultural richness alone won’t cut it if the basics fall short. Tourism is not just about footfalls but about repeat visits and positive word-of-mouth. The journey to becoming a global tourism magnet begins at home — with reliability, not just beauty.
2047 तक स्वर्णिम भारत बनाने में कुपोषण बाधक
संपादकीय
जीडीपी के पैमाने पर ऊंची छलांग लगाने के बावजूद देश में कुपोषण की समस्या पर काबू पाने की रफ्तार धीमी है। किसी कल्याणकारी राज्य का मुख्य कार्य होता है बच्चे को कुपोषण-जनित नाटेपन या दुबलेपन से बचाना और आईएमआर (जन्म से पांच वर्ष की अवस्था के बीच प्रति हजार बच्चों में काल का ग्रास बने बच्चों का दर) शून्य करने का प्रयास करना । डब्ल्यूएचओ की परिभाषा के अनुसार कुपोषित बच्चे अगर बच भी गए तो उनका कॉग्निटिव (संज्ञात्मक) ज्ञान आजीवन कमजोर रहेगा और वे पिछड़ जाएंगे। भारत में नाटापन अभी भी चिंताजनक है जबकि दुबलापन कम करने में भी अपेक्षित तेजी नहीं मिली है। विगत 35 साल के आंकड़े बताते हैं कि आईएमआर कम करने में लगभग सभी सरकारें असफल रहीं। 1991 में यह दर 93 थी यानी हर दस में लगभग एक बच्चे की मृत्यु हो जाती थी। 2000 में यह दर 70 हुई, 2010 में 49, 2020 में 29.85 और 2025 में 24.98 है। अगर यही गति रही तो 2047 तक स्वर्णिम भारत बनाने में कुपोषण बाधक बन सकता है। ऐसा नहीं है कि सरकारें इस समस्या पर सजग नहीं हैं लेकिन स्वास्थ्य सुविधाओं का सुदूर गांवों तक न पहुंचना, संस्थागत डिलीवरी के दौरान और बाद में अपेक्षित स्तर का केयर न मिलना, प्रसूता को पहले से बेहतर पोषण देने के लिए समुचित प्रोत्साहन देना अभी भी पूरी तरह नहीं हो पा रहा है। जन चेतना जगानी होगी ।
Date: 12-04-25
यूएस-चीन की नूराकुश्ती में हमारे लिए एक अवसर है
पवन के. वर्मा, ( पूर्व राज्यसभा सांसद व राजनयिक )
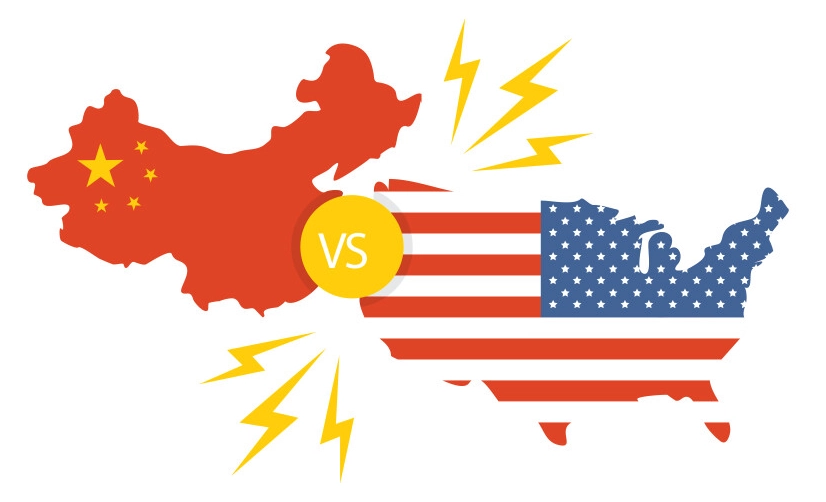 ट्रम्प के बेतुके टैरिफ-युद्ध ने वैश्विक संकट को जन्म दिया है। हालांकि अमेरिका की यह नूराकुश्ती विशेषकर चीन के साथ चल रही है, जिस पर उसने 145 प्रतिशत टैरिफ थोप दिया है। लेकिन यह सभी देशों के लिए चुनौती है, खासकर भारत जैसी प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए। इस तरह की चुनौतियां फौरी झटका तो देती हैं, लेकिन उनमें एक अवसर भी होता है। अब यह हम पर है कि क्या हम इस अवसर का उपयोग अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और भविष्य में इसी तरह की चुनौतियों के लिए खुद को बेहतर तरीके से तैयार करने के लिए कर सकते हैं?
ट्रम्प के बेतुके टैरिफ-युद्ध ने वैश्विक संकट को जन्म दिया है। हालांकि अमेरिका की यह नूराकुश्ती विशेषकर चीन के साथ चल रही है, जिस पर उसने 145 प्रतिशत टैरिफ थोप दिया है। लेकिन यह सभी देशों के लिए चुनौती है, खासकर भारत जैसी प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए। इस तरह की चुनौतियां फौरी झटका तो देती हैं, लेकिन उनमें एक अवसर भी होता है। अब यह हम पर है कि क्या हम इस अवसर का उपयोग अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और भविष्य में इसी तरह की चुनौतियों के लिए खुद को बेहतर तरीके से तैयार करने के लिए कर सकते हैं?
भारत को इस टैरिफ-युद्ध पर संतुलित, रणनीतिक प्रतिक्रिया अपनानी चाहिए, जो उसके आर्थिक हितों की रक्षा करे, अवसरों का लाभ उठाए, बिना सोचे-समझे की गई प्रतिक्रियाओं के नुकसान से बचे और लोकलुभावनवाद के बजाय व्यावहारिकता पर आधारित रहे। बेकार का पलटवार किसी काम का नहीं। 2019 में भी जब भारत ने स्टील और एल्युमीनियम ड्यूटी के जवाब में अमेरिकी वस्तुओं पर टैरिफ लगाया था तो उससे हमें बहुत कम हासिल हुआ था। इसके बजाय, भारत को अपनी घरेलू अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, व्यापार साझेदारी में विविधता लाने और खुद को दोफाड़ हो रही वैश्विक व्यवस्था में एक स्थिर विकल्प के रूप में स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
चीन अमेरिका से जोर-आजमाइश करने का जोखिम उठा सकता है क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था हमसे कहीं मजबूत है। अलबत्ता अमेरिका-चीन के बीच आर-पार का ट्रेड-वॉर वैश्विक मांग को कम कर सकता है, आपूर्ति शृंखलाओं को बाधित कर सकता है और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को एशिया में निवेश पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर सकता है। इसमें हमारे लिए एक अवसर है- लेकिन केवल तभी, जब हम अपने पत्ते सही तरीके से खेलें।
ये अवसर क्या हैं? इनमें सबसे महत्वपूर्ण है लागतों की प्रतिस्पर्धात्मकता में आमूलचूल सुधार करके और ‘ईज़ ऑफ डुइंग बिजनेस’ के अपने एजेंडे को तेजी से आगे बढ़ाकर अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना। भारत के कॉर्पोरेट क्षेत्र में एक उल्लेखनीय आत्मसंतुष्टि आ गई है और देश में और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कुछ कैप्टिव-बाजारों के अस्तित्व ने इनोवेशन और प्रोडक्शन-लाइनों की गुणवत्ता और मात्रा में सुधार को धीमा कर दिया है। देश में आर्थिक प्रतिस्पर्धा पर अकसर एकाधिकार रखने वाले उद्योग-घरानों की ग्रोथ का असर पड़ता है, क्योंकि उन्हें अपने आर्थिक प्रदर्शन को उन्नत करने में कोई वास्तविक प्रोत्साहन नहीं दिखता है।
सरकार ने बिजनेस को आसान बनाने के लिए उतना नहीं किया है, जितना करना था। हमारी अर्थव्यवस्था में अभी भी बहुत ज्यादा लालफीताशाही, बेकार के कानून, बदनाम ‘इंस्पेक्टर राज’ और भ्रष्टाचार है। 2020 के ग्लोबल ईज़ ऑफ डुइंग बिजनेस सूचकांक के अनुसार हम 190 देशों में से 63वें स्थान पर हैं। अभी हमें बहुत काम करना बाकी है।
चीन पर ट्रम्प के टैरिफ ने भारतीय निर्माताओं के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स और टेक्सटाइल जैसे क्षेत्रों में उत्पन्न होने वाले अभाव की पूर्ति का अवसर दे दिया है। लेकिन इसका लाभ उठाने के लिए भारत को अपने घरेलू उद्योग को अधिक प्रतिस्पर्धी बनना होगा। उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाएं एक अच्छी शुरुआत हैं, लेकिन श्रम कानूनों, बुनियादी ढांचे और व्यापार-सुगमता में अभी भी बड़े सुधारों की दरकार है। दुर्भाग्य से, अंतरराष्ट्रीय प्रबंधन विकास संस्थान के 2024 वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक में हम अभी 39वें स्थान पर ही हैं।
चीन की एक बड़ी कमजोरी यह थी कि वह निर्यात के डेस्टिनेशन के रूप में अमेरिका पर बहुत ज्यादा निर्भर था। भारत को इस तरह के जोखिमों को कम करने के लिए अपनी व्यापार साझेदारी में विविधता लानी चाहिए। ये सच है कि अमेरिका हमारे लिए एक महत्वपूर्ण बाजार है, लेकिन हमें यूरोपीय संघ, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के साथ भी व्यापार का विस्तार करना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया और यूएई के साथ हाल ही में संपन्न व्यापार समझौते सही दिशा में उठाए गए कदम हैं, लेकिन इस तरह के और सौदों- खास तौर पर यूके-ईयू के साथ- को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
चीन के आर्थिक प्रभुत्व का मुकाबला करने के अमेरिका के प्रयास हमारे हित में हो सकते हैं। अमेरिका पहले से ही चीनी आपूर्ति शृंखलाओं के विकल्प तलाश रहा था और भारत- अपनी बड़ी वर्कफोर्स और लोकतांत्रिक साख के चलते इसका एक स्वाभाविक दावेदार है।
अमेरिका से अधिक खतरनाक चीन
बलबीर पुंज, ( लेखक वरिष्ठ स्तंभकार हैं )
द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक और सैन्य शक्ति बनकर उभरा। तब से अमेरिकी डालर वैश्विक आरक्षित मुद्रा के रूप में हावी रहा है, जिससे वाशिंगटन को पूरी दुनिया पर बढ़त हासिल हुई। करीब 80 से अधिक देशों में 750 अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं। अमेरिका पिछले सात दशकों से शेष विश्व का एजेंडा निर्धारित करता आ रहा है। 1991 में विघटन होने तक साम्यवादी सोवियत संघ ही अमेरिका से प्रतिस्पर्धा में था। सोवियत संघ के बिखरने के बाद अब ‘साम्यवादी-अधिनायकवादी’ चीन ही ‘लोकतांत्रिक’ अमेरिका के वर्चस्व को सीधी चुनौती दे रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चर्चित टैरिफ नीति को भी चीन को बैकफुट पर धकेलने का दांव माना जा रहा है। इसके लिए ट्रंप को कुछ लोग सनकी तक कह रहे हैं, परंतु ट्रंप के फैसले एक सोची-समझी और दूरगामी योजना का हिस्सा हैं। गैर-हिस्पैनिक श्वेत तबके के रूप में अमेरिका का एक बड़ा वर्ग ट्रंप की संरक्षणवादी और प्रवासी-विरोधी नीतियों के साथ खड़ा है। इस वर्ग के समक्ष अपनी पहचान और अस्तित्व बचाने का संकट है। 1960 में अमेरिका में इस वर्ग की आबादी 85 प्रतिशत से अधिक थी, जो 2020 में घटकर लगभग 58 प्रतिशत रह गई। इसका अर्थ है कि उसके अल्पसंख्यक होने का खतरा है। यह स्थिति अमेरिका को एक भयावह गृहयुद्ध की ओर धकेल सकती है, जिसे ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ यानी मागा से प्रेरित नीतियों से टालने का प्रयास किया जा रहा है।
इसमें कोई संदेह नहीं कि अमेरिका दुनिया को अपने अनुसार चलाने का प्रयास करता रहा है। उसने नैतिकता की दुहाई देकर 1955 में वियतनाम पर हमला किया, जो 20 वर्ष पश्चात अनुमानित 30 लाख से अधिक लोगों की मौत और अमेरिकी पराजय के साथ समाप्त हुआ। 1971 में पूर्वी पाकिस्तान (बांग्लादेश) संकट के समय भी उसका रवैया सही नहीं था। अमेरिका ने स्वार्थवश पाकिस्तान के सैन्य तानाशाहों से अच्छे संबंध रखे। 1979-89 में अफगानिस्तान से सोवियत संघ को खदेड़ने के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान-सऊदी अरब की मजहबी सहायता से जिहादी जंग को सहारा दिया और तालिबान को अफगानिस्तान में स्थापित कराया। हालांकि 2001 में न्यूयार्क में हुए आतंकी हमले के बाद उसने अपनी नीति बदली और अफगानिस्तान में तालिबान को निशाना बनाया। जब नए निजाम से भी बात नहीं बनी तो कालांतर में फिर तालिबान के साथ समझौता कर लिया। ‘सामूहिक विनाश के घातक हथियारों’ को ध्वस्त करने के नाम पर 2003 में इराक पर हमला किया और हजारों लाशें बिछाने के बाद तानाशाह सद्दाम हुसैन को फांसी पर लटका दिया। स्पष्ट है कि अमेरिका का दोहरा रवैया एवं सुविधावादी दृष्टिकोण दिखता रहा है।
अमेरिका की तुलना में चीन को परिभाषित करना अधिक जटिल है। वहां का राजनीतिक ढांचा एकदलीय वामपंथी अधिनायकवाद पर आधारित है, जबकि आर्थिकी 1978 से विकृत पूंजीवाद से ग्रस्त है। इस व्यवस्था में लोकतंत्र, मानवाधिकार और असहमति की कोई गुंजाइश नहीं। मानवीय श्रम को मशीन के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है, जिससे चीन सस्ते उत्पादन का ‘वैश्विक कारखाना’ बन गया है। सभ्यतागत पूर्वाग्रह के कारण चीन के मंसूबे साम्राज्यवादी भी हैं। इस क्रम में वह दशकों पहले तिब्बत को निगल गया तो अब भारत सहित अनेक देशों के साथ उसका सीमा विवाद है। वह निर्धारित अंतरराष्ट्रीय समुद्र मार्गों पर अनर्गल दावा करता रहता है।
साम्यवादी चीन इतना शक्तिशाली कैसे बना? इसका कारण भी अमेरिका ही है, जिसने चीन को अपने लिए बड़े बाजार के रूप में देखा। उसने 1999 में चीन से द्विपक्षीय व्यापार समझौता किया। इसके दो वर्ष बाद चीन विश्व व्यापार संगठन में शामिल हो गया। यह चीन के आर्थिक उभार का केंद्र बिंदु था। विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2000 में चीन का सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी एक ट्रिलियन (लाख करोड़) डालर और प्रति व्यक्ति आय लगभग 960 डालर थी। तब अमेरिकी जीडीपी 10 ट्रिलियन डालर और अमेरिकी प्रति व्यक्ति आय 36,000 डालर से अधिक थी। यानी तब चीन अमेरिकी आर्थिकी के 10 प्रतिशत के बराबर ही था। ढाई दशक बाद चीन अमेरिकी आर्थिक क्षमता का 65 प्रतिशत हो गया है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष-आइएमएफ के अनुसार 2025 में चीनी जीडीपी 19.5 ट्रिलियन डालर और प्रति व्यक्ति आय लगभग 14,000 डालर है। वहीं, अमेरिकी जीडीपी 30 ट्रिलियन डालर और प्रति व्यक्ति आय तकरीबन 90 हजार डालर है। चीन की प्रगति का मुख्य कारण उसकी अधिनायकवादी व्यवस्था और दुनिया भर में सस्ती दरों पर वस्तुओं का बड़े पैमाने पर आयात करना है। इसी के बल पर चीन का व्यापारिक लाभ एक ट्रिलियन डालर से अधिक हो गया है। अमेरिका की बात करें तो चीन के साथ उसका व्यापार घाटा 295 अरब डालर जबकि भारत के साथ करीब 100 अरब डालर का है। यह स्थिति तब है, जब 1985 में भारत की प्रति व्यक्ति आय चीन के बराबर लगभग 300 डालर थी। उसकी आर्थिकी आज भारत की पांच गुना हो गई है। अभी भारत दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति है।
कुछ लोग सवाल उठा सकते हैं कि चीन के आर्थिक-सामरिक विस्तार से परेशानी क्या है? यह ठीक है कि अमेरिका और चीन दोनों ही दबंग देश हैं, जो विश्व को अपनी शर्तों पर हांकना चाहते हैं और दोनों ही अपनी साम्राज्यवादी मानसिकता को नैतिकता-सिद्धांतों का चोला पहनाते रहते है, परंतु दोनों में बुनियादी अंतर भी है। चीन में साम्यवाद प्रेरित अधिनायकवादी व्यवस्था है। वहां न तो कोई चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग से सवाल कर सकता है और न ही कोई उन्हें वैधानिक रूप से हटा सकता है। अमेरिका एक जीवंत लोकतंत्र है और वहां मानवाधिकारों का सम्मान है। ट्रंप से सवाल किए जा सकते हैं और ऐसा हो भी रहा है। उनके कुछ सहयोगी ही उनकी टैरिफ नीति पर सवाल उठा रहे हैं। संवैधानिक बाध्यता के कारण ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल तक ही राष्ट्रपति रह सकते हैं। इसलिए अमेरिका की तुलना में चीन भारत सहित शेष विश्व के लिए कहीं अधिक बड़ा खतरा है।
 Date: 12-04-25
Date: 12-04-25
स्त्री-पुरुष अंतर पाटना जरूरी
संपादकीय
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की नईरिपोर्ट ‘वीमेन ऐंड मेन इन इंडिया 2024’ उत्साहवर्धक प्रगति और निरंतर बरकरार चुनौतियों की ओर संकेत करती है। रिपोर्ट के अहम निष्कर्षों में से एक है देश की श्रम शक्ति, शासन और आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं की बढ़ती मौजूदगी ध्यान देने वाली बात है कि महिलाओं की श्रम शक्ति भागीदारी 2017-18 के 23.2 फीसदी से बढ़कर 2023-24 में 41.7 फीसदी हो गई। यह बड़ी उपलब्धि है मगर पुरुषों की 77.2 फीसदी भागीदारी से काफी कम है और विश्व बैंक के अनुसार दुनिया भर में महिलाओं के 50 फीसदी भागीदारी के औसत से बहुत कम है। इससे पता चलता है कि न केवल अवसरों में अंतर है बल्कि व्यवस्थागत हालात भी ऐसे हैं जो महिलाओं को हतोत्साहित करते हैं। किंतु उत्साहित करने वाली बात यह है कि ग्रामीण और शहरी दोनों ही इलाकों में वेतन के बीच अंतर लगातार कम हो रहा है। जुलाई से सितंबर 2023 और अप्रैल से जून 2024 के बीच शहरी महिलाओं के वेतन में सबसे ज्यादा 5.2 फीसदी इजाफा देखा गया।
फिर भी इस बदलाव के साथ-साथ एक अन्य महत्वपूर्ण रुझान देखने को मिला और वह है मुफ्त के घरेलू कामों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ना। समय के इस्तेमाल से जुड़े टाइम यूज सर्वे के मुताबिक ‘परिवार के सदस्यों के लिए बिना वेतन घरेलू काम’ की अवधि महिलाओं के लिए 236 मिनट है, जबकि पुरुष रोजाना इसमें औसतन 24 मिनट ही देते हैं। इससे दोहरे बोझ की बात पता चलती है। महिलाएं कमाने बाहर भी जा रही हैं और घर के भीतर पूरा काम भी संभाल रही हैं। इससे श्रम शक्ति में भागीदारी की महिलाओं की क्षमता कम हो जाती है और दिखाती है कि सामाजिक मानक घरेलू श्रम की कद्र नहीं करते। यह रिपोर्ट विनिर्माण, व्यापार और अन्य सेवाओं के क्षेत्र में महिलाओं के नेतृत्व वाले प्रतिष्ठानों की संख्या में इजाफा बताती है। यह न केवल महिलाओं में बढ़ती उद्यमिता की भावना को दर्शाता है बल्कि पता चलता है कि उपक्रमों के स्वामित्व में स्त्रियों की हिस्सेदारी बढ़ रही है। महिलाओं का वित्तीय समावेशन भी बढ़ा है मगर आधार कम है। मार्च 2024 में सभी बैंक खातों में महिलाओं के स्वामित्व वाले खाते 39.2 फीसदी थे और कुल जमा में महिलाओं की हिस्सेदारी 39.7 फीसदी था। ज्यादातर महिला खाते देश के दक्षिणी और पूर्वी हिस्सों में थे। पूंजी बाजारों तक पहुंच का भी विस्तार हुआ है और महिलाओं के डीमैट खाते 2021 से 2024 के बीच तीन गुना बढ़े हैं। मगर पुरुषों के खाते उनसे अधिक ही बने हुए हैं।
निर्णय लेने वाले पदों पर रिपोर्ट मिले-जुले नतीजे दिखाती है। पंचायती राज संस्थानों में स्त्री-पुरुष संख्या लगभग बराबर है मगर लोक सभा में महिलाओं की संख्या घटी है। यह कुल महिला प्रत्याशियों के रुझान के अनुरूप ही है। चुनावी राजनीति में महिलाओं की भागीदारी पर जोर के बावजूद 18वीं लोक सभा में कुल निर्वाचित सदस्यों में केवल 13.6 फीसदी महिलाएं हैं। यह चिंताजनक है क्योंकि सर्वोच्च विधायी स्तर पर महिलाओं का समुचित प्रतिनिधित्व उनके लिहाज से संवेदनशील नीतियों के निर्माण और सार्थक क्रियान्वयन के लिए आवश्यक है। व्यापक सुरक्षा चिंताएं, सामाजिक धारणाएं और पारिवारिक बाधाएं अब भी महिलाओं की भागीदारी की राह रोक रही हैं। इन्हें हल करने के लिए सार्वजनिक सुरक्षा में सुधार करना होगा और व्यापक जागरूकता अभियान के साथ स्त्रियों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ानी होगी। भारत को अगर आने वाले दशकों में तेज आर्थिक वृद्धि हासिल करनी है तो महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना जरूरी है।
ठिठके कदम
संपादकीय
अमेरिकी राष्ट्रपति को अब शायद यह बात समझ आने लगी है कि उनकी रणनीति बहुत कारगर साबित नहीं होने वाली। शायद इसीलिए अब बातचीत की संभावना भी खोजी जाने लगी है। सत्ता की बागडोर संभालते ही जिस तरह उन्होंने दुनिया के तमाम देशों को पहले धमकाया और फिर पारस्परिक शुल्क लगा दिया, उससे उन्हें शायद यकीन था कि सारे देश उनके आगे घुटने टेक देंगे और अमेरिका की अर्थव्यवस्था कुलांचे भरनी शुरू कर देगी। मगर पारस्परिक शुल्क लगाने के साथ ही दुनिया भर में उनका विरोध शुरू हो गया। बाजार नीचे की तरफ लुढ़कने शुरू हो गए। खुद अमेरिका में ट्रंप को अभूतपूर्व विरोध का सामना करना पड़ा। ऐसे में उन्होंने अपनी शुल्क नीति पर विराम लगाना पड़ा। कुछ देशों पर उन्होंने नब्बे दिनों के लिए अपनी शुल्क नीति पर रोक लगा दी। हालांकि चीन के साथ उनका शुल्क युद्ध रोज एक नया मोड़ लेता दिख रहा है। अब चीन ने भी अमेरिका पर सवा सौ फीसद का जवाबी शुल्क लगा दिया है। फिर भी अमेरिका को लगता है कि चीन जल्दी ही घुटने टेक देगा और वह ट्रंप से बातचीत की मेज पर आएगा पर चीन ने दूसरे देशों को अमेरिका के खिलाफ अपने पक्ष में एकजुट करना शुरू कर दिया है।
डोनाल्ड ट्रंप की पारस्परिक शुल्क नीति से सबसे अधिक नुकसान खुद अमेरिका को होता नजर आ रहा है। चीन ने दूसरे देशों को कुछ रियायत के साथ अपने उत्पाद बेचने की पेशकश शुरू कर दी है। उसके बाजार पर बहुत प्रतिकूल असर नजर नहीं आ रहा चीन का निर्यात प्रभावित होने से अमेरिकी बाजार में जरूर सुस्ती पसरनी शुरू हो गई है। हालांकि ट्रंप ने माना कि कुछ बड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए दवाएं देनी पड़ती हैं। मगर अमेरिकी नागरिक महंगाई की मार को बहुत देर तक झेलने की स्थिति में नहीं हैं। जिन देशों पर पारस्परिक शुल्क लगाने की तिथि नब्बे दिनों के लिए टाल दी गई है, उनमें भी आधार शुल्क दस फीसद लागू है। इसी से वहां महंगाई बढ़ गई है। अगर ट्रंप अपनी जिद पर अड़े रहते हैं और नब्बे दिन बाद पारस्परिक शुल्क लागू करते हैं, तो दूसरे देश भी वैसा करने को तैयार हैं। यहां तक कि यूरोपीय संघ भी उनके इस फैसले के विरोध में है और उसने अपने जवाबी शुल्क की तारीख नब्बे दिन के लिए टाल दी है। इस तरह ट्रंप को अपने ही सहयोगियों का कड़ा विरोध झेलना पड़ रहा है।
ट्रंप की पारस्परिक शुल्क नीति से सबसे अधिक विश्व व्यापार संगठन की नीतियों का उल्लंघन हो रहा है। उचित ही उसने भी ट्रंप के इस कदम पर कड़ा एतराज जाहिर किया है। विश्व व्यापार संगठन का गठन ही इस इरादे से किया गया था कि दुनिया के देश आसान नियम-शर्तों के साथ वाणिज्य व्यापार कर सकें। उसमें गरीब देशों को शुल्कों में रियायत देने और अमीर देशों से कुछ शुल्क वहन करने की अपेक्षा की गई थी। उसी नीति के तहत अमेरिका को गरीब देशों से आयात होने वाली वस्तुओं पर शुल्क देना पड़ता था । ट्रंप ने उस नियम को दरकिनार कर दिया है। इस तरह पूरी दुनिया की आपूर्ति श्रृंखलाएं प्रभावित होंगी और वाणिज्य व्यापार के नए समीकरण बनेंगे, जिससे व्यापार युद्ध का खतरा गहराता जाएगा। मगर आर्थिक विशेषज्ञों को यकीन है कि जिस तरह ट्रंप के कदम ठिठकने लगे हैं, वे फिर से इस नीति पर विचार करेंगे।
ट्रंप के पीछे हटने का अर्थ
संपादकीय
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ज्यादातर देशों पर लगाए गए टैरिफ को अचानक 90 दिनों के लिए स्थगित करने का फैसला किया है। यह फैसला उनके स्वभाव के अनुरूप प्रतीत नहीं होता। हालांकि क़दम उन्होंने उठा लिया है जिसका वैश्विक बाजार पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। उनके फैसले से वैश्विक बाजार में जो हलचल और अनिश्चितता का माहौल पैदा हुआ था, उसमें थोड़ा ठहराव आ गया है। ट्रंप के फैसले को लेकर स्वयं उनके देश अमेरिका और दुनिया के अन्य देशों में प्रतिक्रिया हो रही थीं। उन्होंने इसका संज्ञान लिया और अपने फैसले को 90 दिनों तक स्थगित कर दिया। हालांकि उनकी इस फैसले से चीन अपवाद रहा है। शायद ट्रंप को यह आभास हो गया है। कि व्यापार युद्ध के मसले पर पूरी दुनिया के विरुद्ध मोर्चा खोलने की बजाय अपने प्रमुख व्यापारिक प्रतिद्वंद्वी चीन को निशाना बनाया जाए। यही वजह है कि ट्रंप ने चीन से आयात शुल्क की दर बढ़ाकर 145 फीसद कर दी है। दूसरी ओर, चीन की प्रतिक्रियाओं से यह लग रहा है कि अमेरिका ने जो टैरिफ युद्ध शुरू किया है, उससे उसने आखिर तक लड़ने का मन बना लिया है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि चीन यह समझ रहा है कि वह अमेरिका से अकेले लड़ नहीं सकता है, इसीलिए वह विभिन्न देशों को साथ लेकर एक संयुक्त मोर्चा बनाने का प्रयास कर रहा है। इतना ही नहीं, बल्कि चीन की ओर से यह भी कहा गया है कि भारत और चीन दोनों बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश हैं, इसीलिए इस मामले में दोनों को साथ मिलकर काम करना चाहिए। लेकिन चीन को इस मामले में कोई खास सफलता नहीं मिल रही है। इस पूरे मामले में भारत का रुख बहुत सकारात्मक रहा है। उसने किसी तरह की जल्दबाजी नहीं की है, और प्रतिक्रियात्मक कदम नहीं उठाया है। भारत और अमेरिका के बीच इस मसले को लेकर द्विपक्षीय वार्ता चल रही है, उम्मीद है कि भारत इस पर अपना पक्ष मजबूती से रख सकेगा और जोर देगा कि भविष्य के व्यापार में उसे भारी टैरिफ का दबाव न झेलना पड़े। लेकिन भारत के सामने दुविधा की स्थिति है कि उसे चीन और अमेरिका के साथ व्यापारिक संबंधों में संतुलन बनाकर चलना होगा क्योंकि दोनों बड़े व्यापारिक साझेदार हैं। अब तक भारत ने धैर्य और समझदारी से काम लिया है, और उम्मीद है कि अपनी इसी तरह की नीतियों के चलते वर्तमान परिस्थितियों के अपने पक्ष में झुकाने में सफल हो जाएगा।