
11-04-2025 (Important News Clippings)
To Download Click Here.
Now, justice
Rana’s extradition allows Indian prosecutors to probe his Pakistan links
Editorial
Seventeen years after the Mumbai 26/11 terror attacks, India is preparing for the trial of Tahawwur Hussain Rana, who was extradited by the United States this week. The extradition of a co-conspirator in the planning of the attacks that left 166 people dead is proof of the success of India’s counter-terror diplomacy with the U.S., and the tenacity of Indian investigators. Mr. Rana was first arrested by the U.S. in 2009, as an accomplice of David Headley, the Lashkar-e-Taiba (LeT) operative tasked by Pakistan to carry out the reconnaissance for targets in Mumbai by LeT terrorists, as well as for being a part of a plan to attack a newspaper office in Copenhagen. As Mr. Headley’s childhood friend and colleague, Mr. Rana, a Canadian-American citizen and a former Pakistan military doctor, helped plan the attacks and facilitate his multiple entries to India, including once after the attacks, according to U.S. prosecutors. While Mr. Rana was not convicted for the Mumbai attacks in the U.S. trial, he was convicted for his LeT terror links and involvement in the Copenhagen conspiracy, and spent some part of a 14-year sentence in U.S. prisons. His extradition will allow Indian prosecutors to put on trial one of the men charge-sheeted in absentia for the 26/11 attacks; to extract more information on his Pakistan links; and to further the cause of justice after the dastardly attacks that brought the nation to a standstill. Ajmal Kasab, the only one of the 10 LeT gunmen caught alive, was convicted and hanged in 2012.
The prosecutors of the National Investigation Agency, who have followed the 26/11 trail since 2009, will now need to conduct a similar and unimpeachable time-bound trial. The government would also need to investigate certain unanswered questions: including whether Mr. Rana continued to have provable links with the Pakistani military; whether there is more evidence on the extent of Pakistan’s official complicity, and why the U.S. chose to enter into a plea bargain with Mr. Headley, giving him immunity from extradition despite a treaty with India. When compared to Mr. Rana, he was clearly the more provably diabolical and culpable agent for the conspiracy. It is also curious that the U.S., that had been tracking Mr. Headley even before the 26/11 attacks, did not alert Indian authorities of his return to India for another reconnaissance operation in early 2009. It is hoped that Mr. Rana’s trial will turn the spotlight back on Pakistan, and generate enough pressure on it to cooperate in the prosecution of seven LeT terror commanders, including Hafiz Saeed who planned, trained and equipped the terrorists for the attacks. To that end, Mr. Rana’s extradition is a significant step in the quest for justice and closure for the victims of the 26/11 attacks and their families.
Date: 11-04-25
Are existing mechanisms effective in combating judicial corruption?
Sanjay Hegde, Alok Prasanna Kumar, [ Senior Advocate based in Delhi, Alok Prasanna Kumar is Co-founder of vidhi centre for Legal Policy ]
Last month, unaccounted cash was reportedly recovered from the official residence of former Delhi High Court judge, Justice Yashwant Varma. In response, Chief Justice of India Sanjiv Khanna initiated an in-house inquiry into the matter. Justice Varma has since been repatriated to his parent High Court in Allahabad and will not be assigned any judicial work until the Supreme Court-mandated inquiry is completed. Are existing mechanisms effective in combating judicial corruption? Sanjay Hegde and Alok Prasanna Kumar discuss the question in a conversation moderated by Aaratrika Bhaumik. Edited excerpts:
Is impeachment an effective mechanism for judicial accountability, given its reliance on political consensus?
Sanjay Hegde: Far from being a mechanism for accountability, the process of impeachment is designed to shield judges. Unless a motion garners the support of two-thirds of the members present and voting, as well as an absolute majority in each House of Parliament, the judges cannot be removed. To assume that the threat of impeachment acts as a deterrent is misguided, given how rarely such proceedings succeed. What is needed instead is an internal mechanism within the judiciary to transparently address serious misconduct. Such a system would go a long way in reinforcing public confidence in the institution.
Alok Prasanna Kumar: Impeachment upholds judicial independence by insulating judges from political retaliation. To this end, the process is intentionally rigorous, requiring both a detailed parliamentary procedure and proof of ‘misbehaviour or incapacity.’ These high thresholds are meant to deter the executive from using impeachment to remove judges who are seen as inconvenient.
We also tend to assume that judicial independence has always existed, but it is a relatively modern concept. Historically, judges served to deliver the monarch’s justice, not to check state power or protect individual rights. This began to change with the rise of constitutional democracies.
Are legislative reforms required in the Supreme Court’s in-house procedure for addressing judicial misconduct?
SH: The in-house procedure was established to prevent the misuse of legal processes against the judiciary, especially when judicial decisions displease the executive. A key precedent is Delhi Judicial Service Association v. State of Gujarat (1991), where the Supreme Court intervened after the Chief Judicial Magistrate of Nadiad was mistreated by Gujarat police officials, and issued guidelines for arresting judicial officers. To guard against misuse, the judiciary introduced an internal inquiry mechanism before allowing prosecution. Nonetheless, this framework could benefit from legislative intervention.
APK: Corruption cases are particularly difficult to prosecute in a country like ours, where enforcement institutions are weak, the capacity to secure convictions is limited, and judges enjoy a degree of institutional protection. A striking example is the recent acquittal of former Punjab and Haryana High Court judge Nirmal Yadav, nearly 15 years after a Supreme Court-mandated inquiry committee found sufficient evidence to prosecute her. That said, I agree with Sanjay that there is certainly scope for strengthening the in-house procedure.
Should inquiry reports under this mechanism be made public?
APK: Yes. We have seen a welcome shift towards transparency in the Supreme Court’s handling of the Justice Yashwant Varma case. In an age where judicial conduct is closely scrutinised through social and mass media, opacity in cases of alleged judicial corruption is no longer viable. However, such transparency cannot remain an ad hoc response to crises; it must be institutionalised. At the same time, it is essential that the inquiry process upholds the principles of natural justice and safeguards the rights of the accused. While rigid procedural rules may not be feasible, a balanced framework is necessary — one that commands the confidence of all stakeholders and prevents the inquiry process from becoming the subject of further litigation.
SH: I agree that increased transparency in the functioning of inquiry committees is welcome. However, in this particular case, the Court’s decision appears to have been shaped by the extraordinary level of public speculation. By proactively releasing the video purportedly showing the recovery of unaccounted cash, the Court pre-empted any perception that it was shielding a member of the higher judiciary. Had the footage surfaced through other unofficial channels, it could have severely undermined institutional credibility. That said, such decisions must be made with caution and evaluated on a case-by-case basis, ensuring that the accused’s right to a fair trial remains fully protected. The Court could also benefit from appointing dedicated communications personnel to prevent misinformation and bolster public confidence.
The Justice Varma case has renewed calls to revive the National Judicial Appointments Commission. Should the government have a say in judicial appointments?
SH: The government already holds a seat at the table. The real question is whether it should wield a blank cheque. Even before the collegium finalises its recommendations, informal consultations with the executive are often undertaken. After the names are forwarded, the government retains the power to flag Intelligence Bureau inputs for the collegium’s reconsideration. There have also been several instances where the government has stalled appointments by simply sitting on the recommendations. This de facto executive veto has prevented many deserving judges from reaching the Supreme Court.
APK: We should no longer call it the collegium system; it now resembles a search-and-selection committee. While the High Court and Supreme Court collegium recommend names, the Union government follows a pick-and-choose approach. This has dissuaded many deserving candidates from subjecting themselves to an opaque and often humiliating process. Ultimately, it does not matter whether judges are appointed by the government, the judiciary, or a combination of the two. What matters is transparency. The D.Y. Chandrachud-led collegium made progress on this front by publishing resolutions that detailed the rationale behind each recommendation. Regrettably, the practice has been discontinued.
Should the Judicial Standards and Accountability Bill, 2010, be reconsidered?
APK: I don’t think so. It fails to address several critical gaps. What we need is a more calibrated and institutional response. The first step should be to define clear, enforceable judicial standards. Consider the issue of familial ties in the judiciary — every judge should be mandated to disclose relatives practising in the same court. Once disclosed, either the judge must be transferred or the relative barred from appearing before that court. Merely setting up more oversight bodies is not the solution. These institutions would inevitably be staffed by retired judges, thereby perpetuating the same structural flaws we seek to remedy.
SH: More than legislative reform, we need to focus on the fact that the legal profession already operates through an informal system of peer review. Long before a judge becomes entangled in a corruption scandal, there are usually murmurs within the corridors of the court. A meaningful step forward would be to institutionalise this peer review process by systematically incorporating inputs from bar associations and fellow judges. This would strengthen internal accountability.
Should contempt of court laws be liberalised to permit greater public scrutiny of judicial conduct?
APK: We can liberalise contempt of court laws, but unless there are consequences for judges who invoke them arbitrarily, such reforms will have little impact. It is also important to assess the context in which contempt is initiated — does it stem from a judge’s anger or fear, or is it a measured institutional response to someone deliberately spreading falsehoods to undermine public trust in the judiciary? That said, there must be space for good-faith discourse on judicial corruption without the spectre of criminal contempt looming over those who voice legitimate concerns.
ट्रम्प के टैरिफ पर भारत ने समझदारी दिखाई है
संपादकीय
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने चीन पर टैरिफ दर 125% (यह एक किस्म का अघोषित व्यापार प्रतिबंध ही है) करते हुए दुनिया के 70 मुल्कों (जिसमें भारत भी है) को अगले तीन माह 10% दर वाली बेस टैक्स श्रेणी में रखा है। अमेरिकी वित्त मंत्री से जब पूछा गया था कि यह प्रतिशोधात्मक टैक्स केवल चीन पर ही लगेगा या अन्य देश भी इसकी जद में आ सकते हैं तो उनका जवाब था कि ‘खराब खिलाड़ियों पर नजर रहेगी और ऐसा कहकर उन्होंने तत्काल वियतनाम, जापान, दक्षिण कोरिया और भारत का नाम लिया था। लेकिन भारत ने होशियारी की अमेरिका से द्विपक्षीय व्यापार-वार्ता शुरू करके। यह इस बात की स्वीकारोक्ति थी कि हम किसी भी किस्म की अमेरिका-विरोधी गोलबंदी में शामिल नहीं होंगे। ट्रम्प की घोषणा के बाद वाणिज्य मंत्री ने भारतीय निर्यातकों को चेतावनी दी कि वे लालच में आकर चीन से कम टैरिफ पर सामान लेकर नई घटी अमेरिकी टैरिफ दर पर अमेरिका को बेचने की हिमाकत भूलकर भी न करें। यह चेतावनी सामयिक है । द्विपक्षीय व्यापार में दीर्घकालीन भरोसा एक बड़ा फैक्टर होता है क्योंकि उत्पाद की तकनीकी, सर्विस – आफ्टर सेल्स और सुरक्षा शर्तें देखनी होती हैं। इस पैमाने पर अमेरिका, फ्रांस या रूस पर चीन के मुकाबले भारत को ज्यादा भरोसा रहा है। फिर अमेरिका हमारा सबसे बड़ा व्यापार – पार्टनर भी रहा है।
मंदी आई तो क्या होगा ?
डॉ. भरत झुनझुनवाला, ( लेखक अर्थशास्त्री हैं )

कई विश्लेषकों का मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति से अमेरिका सहित विश्व अर्थव्यवस्था में मंदी आ सकती है। इस विषय को समझने के लिए पहले ट्रंप की दृष्टि को समझना होगा। ट्रंप इससे चिंतित हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों का लाभ बढ़ रहा है और अमेरिका द्वारा पूरे विश्व से भारी मात्रा में ऋण लिया जा रहा है, लेकिन अमेरिकी श्रमिकों के वेतन सपाट बने हुए हैं।
वर्ष 2000 से 2023 के बीच अमेरिकी कंपनियों का लाभ 500 अरब डॉलर से बढ़कर 3,500 अरब डॉलर हो गया। इसमें सात गुना वृद्धि हुई। इसी अवधि में अमेरिका द्वारा लिया जाने वाला ऋण 5.6 ट्रिलियन (लाख करोड़) डॉलर से बढ़कर 33.2 ट्रिलियन डॉलर हो गया।
इसमें भी लगभग छह गुना वृद्धि हुई, लेकिन इसी अवधि में एक अमेरिकी श्रमिक का औसत वेतन 335 डॉलर प्रति सप्ताह से बढ़कर 375 डॉलर प्रति सप्ताह ही हो पाया। इसमें मात्र 12 प्रतिशत की वृद्धि हुई। ट्रंप का लक्ष्य है कि अमेरिकी श्रमिकों के वेतन में वृद्धि हो और अमेरिका द्वारा लिया जाने वाला ऋण घटे, क्योंकि इतनी भारी मात्रा में ऋण लेने से अमेरिका की आर्थिक संप्रभुता पर संकट आ सकता है।
ट्रंप द्वारा आयात कर यानी टैरिफ बढ़ाने से अमेरिका में आयातित होने वाली वस्तुओं के दाम में वृद्धि होगी। जैसे, जो विदेशी कार वर्तमान में 20,000 डॉलर में बिक रही है, वह आयात कर आरोपित होने के बाद 25,000 डॉलर में बिकेगी। इस कारण अमेरिकी नागरिकों की खपत में गिरावट आ सकती है। जो परिवार 20,000 डॉलर में कार खरीदने को उत्सुक था, वह उसी कार को 25,000 डॉलर में खरीदने से शायद हिचकेगा।
अमेरिका में खपत घटने से मंदी आ सकती है। जेपी मार्गन बैंक ने मंदी की 60 प्रतिशत तक आशंका व्यक्त की है। हालांकि मेरी समझ से यह आकलन सही नहीं है। कहानी का दूसरा पहलू देखें तो आयातित कार महंगी होने से अमेरिका में उत्पादित कार सस्ती पड़ने लगेगी। अमेरिकी कार का उत्पादन बढ़ेगा। मान लीजिए 20,000 डॉलर की अमेरिकी कार के उत्पादन में 1,000 डॉलर का पार्ट भारत से बनकर आता है।
ट्रंप द्वारा आयात कर बढ़ाने के कारण यह पार्ट अब 1,300 डॉलर में आयातित होगा। अमेरिकी कार का विक्रय मूल्य 20,000 से बढ़कर 20,300 डॉलर हो जाएगा। तुलना में आयातित कार 25,000 डॉलर में आयातित होगी। इसलिए पार्ट्स पर बढ़े हुए आयात कर को अदा करना अमेरिकी उद्यमियों के लिए लाभप्रद होगा और अमेरिका में उत्पादन बढ़ेगा। इसके अतिरिक्त, अमेरिकी सरकार को 300 डॉलर की आय होगी, जिससे सरकार का वित्तीय घाटा कम होगा और अमेरिका का ऋण कम होगा।
हालांकि इसमें दूसरा संकट यह है कि यदि दूसरे देशों ने जवाबी आयात कर में वृद्धि की तो अमेरिकी निर्यात प्रभावित होंगे, जिससे वहां के उद्यमों को नुकसान पहुंचेगा। निश्चित ही कुछ क्षेत्रों में ऐसा होगा, लेकिन यह नुकसान न्यून ही होगा। हर देश के उद्यमी दूसरे बाजार की खोज करेंगे। जैसे अमेरिका में टोयोटा का ट्रक महंगा पड़ने के कारण अमेरिकी निर्माता ट्रक का उत्पादन बढ़ाएंगे।
अमेरिका में उत्पादन बढ़ने से वहां श्रम की मांग बढ़ेगी। इसका अंतिम प्रभाव सकारात्मक होगा। इसी प्रकार भारत में अमेरिका से आयातित होने वाले माल के स्थान पर घरेलू उत्पादन बढ़ेगा। जैसे अमेरिका से आयातित होने वाले बिजली के उपकरणों के स्थान पर बिजली के घरेलू उपकरणों का उपयोग बढ़ेगा। इस उठापटक में कुछ समय तक बाजार में मंदी आएगी, परंतु दीर्घकाल में प्रभाव सकारात्मक होगा।
मूल बात यह है कि टैरिफ बढ़ाने से अमेरिकी अर्थव्यवस्था में उत्पादन करना अधिक लाभप्रद हो जाएगा। घरेलू उत्पादन बढ़ने से वहां पर श्रमिकों की मांग बढ़ेगी और श्रमिकों के वेतन भी बढ़ेंगे। अमेरिका में एक्साइज ड्यूटी एवं आयात कर की वसूली बढ़ेगी। घरेलू कंपनियों का लाभ बढ़ेगा। वे अधिक कर अदा करेंगी। इन सब कारणों से अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। ट्रंप की नीति मूल रूप से सही है।
टैरिफ नीति का दूसरे देशों पर अल्प समय में नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। जैसे भारत से 1,000 डॉलर मूल्य के कलपुर्जे बेचने वाले उद्यमों के निर्यात प्रभावित होंगे। भारत में उत्पादन के स्तर पर तत्काल कुछ गिरावट आएगी। भारतीय कंपनियों के मुनाफे पर दबाव बढ़ेगा। इसी प्रकार दूसरे देशों में उत्पादन घटने से संपूर्ण विश्व में मंदी आ सकती है। यह मंदी कितने समय तक होगी, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि दूसरे ग्राहक कितने समय में उपलब्ध हो जाते हैं। जैसे कार के पार्ट्स को बनाने वाले भारतीय उद्यम के लिए यह संभव होगा कि वह यूरोप अथवा दक्षिणी अमेरिका में उत्पादित होने वाली कार के लिए पार्ट्स बनाकर निर्यात करें।
वर्तमान वैश्विक अर्थव्यवस्था को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। इसमें एक हिस्सा अमेरिका का, जिसका विश्व अर्थव्यवस्था में लगभग 26 प्रतिशत हिस्सेदारी है। दूसरा भाग शेष विश्व का, जिसका हिस्सा 74 प्रतिशत है। 74 प्रतिशत अर्थव्यवस्था वाले देशों में अब आपसी व्यापार बढ़ेगा। बिल्कुल वैसे जैसे जमींदारी समाप्त होने पर किसानों ने दूसरे बाजार शीघ्र ही पकड़ लिए थे। इस प्रक्रिया में कुछ समय लग सकता है, लेकिन अमेरिका को निर्यात बाधित होने के कारण, जो मंदी आएगी वह दीर्घकालिक नहीं होगी।
भारत इस संकट से निपटने को लेकर सुदृढ़ स्थिति में है। भारत द्वारा अमेरिका को निर्यात किए जाने वाला माल हमारे देश की आय का मात्र 2.1 प्रतिशत है। यह संपूर्ण निर्यात बंद हो जाए तो भी 2.1 प्रतिशत का बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें से कुछ माल हम दूसरे देशों को निर्यात कर सकेंगे।
जैसे दूध बिकना कम हो जाए तो किसान खोया बनाकर दूसरा बाजार पकड़ लेता है। हालांकि अमेरिकी बाजार को छोड़ने में कठिनाई होगी। हमें अमेरिका-केंद्रित विश्व को पीछे छोड़कर बहुकेंद्रित विश्व की ओर बढ़ना चाहिए। टैरिफ मामले का सार यही है कि ट्रंप द्वारा टैरिफ बढ़ाना अमेरिकी नागरिकों के लिए लाभप्रद हो सकता है, जो शेष विश्व के लिए अल्प समय में हानिकारक, किंतु दीर्घकाल में नए विश्व के निर्माण में मददगार होगा।
आखिर कठघरे में
संपादकीय
पिछले महीने जब अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई आतंकी हमले के एक अहम आरोपी तहव्वुर राणा की भारत को प्रत्यर्पित करने के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया था, तभी यह साफ हो गया था कि उसे भारत लाने के दिन अब करीब आ गए हैं। हालांकि उसके अपराधों की गंभीरता के मचेनजर यह पहले भी स्पष्ट था कि उसके लिए राहत की कोई सूरत नहीं बनने जा रही है। मगर अब गुरुवार को आखिरकार उसे भारत प्रत्यर्पित कर दिया गया और इसी के साथ मुंबई में 26 नवंबर, 2008 को हुए आतंकी हमले में मारे गए लोगों और अन्य पीड़ितों के परिजनों के लिए इंसाफ की एक और उम्मीद मजबूत हुई है। तहबुर राणा का प्रत्यर्पण कराने के लिए भारत की ओर से काफी समय से लगातार कोशिशें जारी थीं और उसमें निरंतरता का ही यह नतीजा है कि इस दिशा में एक बड़ी कामयाबी मिली। जाहिर है, अब भारतीय कानूनों के तहत राणा को न्याय के कठघरे में खड़ा होना पड़ेगा, जिससे बचने के लिए उसने अमेरिका में अपने सभी दांव आजमा लिए थे।
गौरतलब है कि लश्कर-ए-तैयबा की योजना के मुताबिक जिस गिरोह ने मुंबई में बड़े पैमाने पर एक साथ आतंकी हमला किया था और उसमें एक सी चीखठ लोग मारे गए थे, तहब्बुर राणा ने उसमें मुख्य साजिशकर्ता की भूमिका निभाई थी। लेकिन तब उसे पकड़ा नहीं जा सका। पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक राणा उसके बाद भी अपने आतंकी साथी डेविड कोलमैन हेडली के साथ अन्य देशों में आतंकी हमले करने की योजना में सक्रिय रहा। मगर डेनमार्क में हमले की योजना को अंजाम देने के पहले ही जब वह अमेरिकी एजेंरियों की पकड़ में आया, तब जाकर उसकी आतंकी करतूतों का रास्ता रुका वरना यह कहना मुश्किल है कि मुंबई में आतंकी हमलों की तरह वह और कितने आम लोगों की जान लेने का सूत्रधार बनता। पकड़ में आने के बाद अमेरिका में वर्ष 2013 में उसे डेविड कोलमैन हेडली के साथ मुंबई में आतंकी हमले को अंजाम देने और डेनमार्क में इसी तरह का बड़ा हमला करने की योजना बनाने का दोषी करार दिया गया तब वहां की अदालत ने राणा को चौदह वर्ष कैद की सजा सुनाई थी। नगर जब भारत की ओर से अपने कानूनों के तहत कठघरे में खड़ा करने के लिए उसके प्रत्यर्पण की कोशिशें चल रही थीं तक उसने इसे रोकने के लिए अपना पूरा जोर लगा दिया था। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस संबंध में कहा था कि मुंबई आतंकी हमलों के साजिशकर्ता तहर राणा को भारत को प्रत्यर्पित कर दिया जाएगा। मगर वह जिस स्तर का संवेदनशील मामला था, उसमें कई बार आखिरी समय में अड़चन खड़ी होने की आशंका बनी रहती है। शायद इसीलिए राणा को भारत लाने में कामवाली को केंद्रीय एजेंसियों के सबसे महत्त्वपूर्ण प्रत्यर्पण और भारत की एक अहम कूटनीतिक जीत के तौर पर देखा जा रहा है। मगर यह भी सच है कि इसके लिए भारतीय खुफिया एजेंसियों को करीब डेढ़ दशक तक लगातार प्रयास करना पड़ा। इस मसले पर पाकिस्तान ने भले ही तहब्बुर राणा के पिछले दो दशकों से कनाडाई नागरिक होने का हवाला देकर पल्ला झाड़ने की कोशिश की है, इसके बावजूद अब यह उम्मीद की जा सकती है कि मुंबई हमलों में पाकिस्तान स्थित ठिकानों से काम करने वाले आतंकी संगठनों और उनसे जुड़े आतंकवादियों की भूमिका कुछ और खाफ होकर उभरेगी।
भारत की जीत
संपादकीय
अंततः मुंबई में 26/11 के आतंकी हमले में आरोपी तहब्बुर राणा विशेष विमान से राजधानी दिल्ली पहुंच गया। राणा को अमेरिका से प्रत्यार्पित किया गया है। इस आतंकी को दिल्ली ले आना भारत की आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक बड़ी जीत है। लोगों को याद होगा कि दो महीने पहले व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में राणा को कानून का सामना करने के लिए भारत भेजने पर सहमति व्यक्त की थी। राणा पेशे से चिकित्सक है जिसका जन्म पाकिस्तान में हुआ था। बाद वह कनाडा चला गया और वहां का नागरिक बन गया। मुंबई आतंकवादी हमले के मुख्य साजिशकर्ताओं में एक अमेरिकी नागरिक डेविड कोलमैन हेडली उर्फ दाउद गिलानी का राणा करीबी सहयोगी रहा है। 26 नवम्बर, 2008 को मुंबई में आतंकी हमला हुआ था जिसमें करीब 175 लोगों की मौत हो गई थी जिनमें 26 विदेशी नागरिक थे। मुंबई के ताज होटल, सीएसटी और कामा अस्पताल समेत कई जगहों पर हमला हुआ था। इस दौरान पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आतंकी अजमल कसाब जीवित पकड़ा गया था।
कसाब को कानूनी प्रक्रिया में दोषी पाया गया था। अदालती कार्यवाही के बाद उसे 2012 में फांसी दे दी गई । कसाब के विरुद्ध दायर चार्जशीट में राणा, हेडली के नाम का भी उल्लेख है। आरोप है कि राणा ने पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और हरकत-उल-जिहादी इस्लामी के आतंकवादियों के साथ मिल कर देश की आर्थिक राजधानी मुंबई पर हमले की साजिश रची थी। अमेरिका की खुफिया एजेंसी एफबीआई ने 2020 में राणा को गिरफ्तार किया था। उसकी गिरफ्तारी भारत के कूटनीतिक दबाव के कारण हुई थी। उससे जांच एजेंसियों की पूछताछ में पता चला कि मुंबई आतंकी हमले में राणा का भी हाथ है। अब भारत की जांच एजेंसियां राणा से पूछताछ करेंगी। उम्मीद है कि इस जांच में हमले में पाकिस्तान की भूमिका की पुख्ता जानकारी मिल सकेगी। हालांकि यह पहले भी प्रभाणित हो चुका है कि इस हमले की साजिश पाकिस्तान में रची गई थी। भारत के पास इस बात के पुख्ता प्रमाण हैं लेकिन पाकिस्तान यह कभी स्वीकार नहीं करेगा। हालांकि उसका चेहरा एक्सपोज हो चुका है।
Date: 11-04-25
अब सार्क का विकल्प
डॉ ब्रह्मदीप अलूने
बिम्सटेक क्षेत्रीय बहुपक्षीय संगठन है। यह बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती और समीपवर्ती क्षेत्रों में स्थित देशों का प्रतिनिधित्व करता है, दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच संपर्क मार्ग बनाता है। तथा हिमालय तथा बंगाल की खाड़ी की पारिस्थितिकी को भी जोड़ता है।
भारत के लिए बिम्सटेक रणनीतिक और भू-राजनैतिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण संगठन है, जिसे चीन और पाकिस्तान के प्रभाव से दूर रख कर पड़ोसी देशों से बेहतर और स्थिर संबंध बनाए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सहयोगात्मक पहल यह संगठन सार्क का बेहतर विकल्प बनता दिखाई दे रहा है। बिम्सटेक के सदस्य देशों में भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, भूटान और नेपाल शामिल हैं। इनमें से अधिकांश देश दक्षिण एशिया के हैं। करीब आठ सालों से दक्षिण एशिया के देशों के महत्त्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन सार्क का कोई सम्मेलन नहीं हुआ है, और भारत और पाकिस्तान के खराब रिश्तों के चलते यह संगठन अप्रासंगिक हो गया है।
वहीं नरेन्द्र मोदी सरकार ने अपनी ‘पड़ोसी पहले’ नीति और ‘एक्ट ईस्ट’ नीति के एक हिस्से के रूप में बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग या बिम्सटेक के लिए बंगाल की खाड़ी पहल पर अधिक ध्यान केंद्रित किया है, जो सार्क का बेहतर विकल्प बन सकता है। खासकर बिम्सटेक में पाकिस्तान के न होने से विभिन्न देशों के बीच राजनीतिक निर्णयों में बेहतर समझबूझ देखने को मिल सकती है। बैंकॉक में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के अलूने प्रमुख मोहम्मद यूनुस और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात से दोनों देशों के रिश्ते पटरी पर लौटने की उम्मीद पुनः बंधी है। भारत और बांग्लादेश, दोनों पड़ोसी देश हैं, और दोनों के राष्ट्राध्यक्ष कूटनीतिक संबंधों के महत्त्व को बेहतर समझते हैं। बांग्लादेश के लिए भारत बहुत महत्त्वपूर्ण देश है, और बांग्लादेश का कोई भी राजनीतिक दल इसे नकार नहीं सकता, वहीं बांग्लादेश की भू-रणनीतिक स्थिति भारत की सामरिक सुरक्षा की दृष्टि से बेहद महत्त्वपूर्ण है। बांग्लादेश बिम्सटेक और बीबीआईएन पहलों का महत्त्वपूर्ण घटक है, रणनीतिक रूप से
महत्त्वपूर्ण समुद्री मार्गों के निकट स्थित है तथा दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार है। भारत और बांग्लादेश के बीच सुविधाजनक व्यापार समझौता है दोनों देश एशिया प्रशांत व्यापार समझौते, सार्क अधिमान्य व्यापार समझौते और दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौते के सदस्य हैं, जो व्यापार के लिए टैरिफ व्यवस्था को नियंत्रित करते हैं।
म्यांमार के साथ भारत के अच्छे संबंध हैं, जो सुरक्षा, व्यापार और क्षेत्रीय स्थिरता के दृष्टिकोण से महत्त्वपूर्ण हैं। भारत म्यांमार को ‘पूर्व की ओर देखो’ नीति का महत्त्वपूर्ण हिस्सा मानता है। म्यांमार की रणनीतिक स्थिति दक्षिण- पूर्व एशिया में स्थित है, और यह कई दृष्टिकोणों से महत्वपूर्ण है। म्यांमार की सीमाएं भारत, चीन, थाईलैंड, लाओस, बांग्लादेश और अंडमान सागर से जुड़ी हुई हैं, जिससे यह देश क्षेत्रीय राजनीति और वैश्विक रणनीतिक मामलों में अहम स्थान रखता है। इस समय न बांग्लादेश में लोकप्रिय सरकार है, और न ही म्यांमार में इन दोनों देशों में सैन्य प्रभाव वाली सरकारें हैं, और यह स्थिति चीन जैसे साम्यवादी देश के लिए मुफीद नजर आती है। म्यांमार में गृह युद्ध की वजह से भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में उग्रवाद, आतंकवाद और ड्रग तस्करी का जोखिम बढ़ गया है। म्यांमार की स्थिरता से भारत की करोड़ों डॉलर लागत वाली कलादान मल्टीमॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना के लिए भी खतरा पैदा हो गया है। यह परियोजना, पूर्वी तट को उत्तरी पूर्वी राज्य से जोड़ने के लिहाज से काफी अहम है। म्यांमार की सैन्य सरकार और बागी जातीय संगठनों के साथ रिश्तों में संतुलन बनाए रखना भारत के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण है।
वहीं बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता के कारण कट्टरपंथी ताकतें मजबूत हो रही हैं। तथा इससे भारत के उत्तर-पूर्व के कई राज्यों की आंतरिक सुरक्षा प्रभावित हो सकती है। बैंकॉक में बिम्सटेक शिखर सम्मेलन के दौरान म्यांमार के वरिष्ठ जनरल मिन आंग स्लाहंग से भी भारत के प्रधानमंत्री की मुलाकात हुई तथा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के साथ कनेक्टिविटी, क्षमता निर्माण, बुनियादी ढांचे के विकास और अन्य क्षेत्रों पर चर्चा हुई।
बांग्लादेश और म्यांमार के राष्ट्र प्रमुखों से भारतीय प्रधानमंत्री की मुलाकात बहुप्रतीक्षित थी और कूटनीतिक दृष्टि से जरूरी भी थी। भारत दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा और प्रभावशाली देश है, और इसके कारण इस क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और इसका क्षेत्रीय और वैश्विक अर्थव्यवस्था में महत्त्वपूर्ण योगदान है। भारत का प्रभाव दक्षिण एशियाई देशों में शिक्षा, कला, साहित्य और संगीत के क्षेत्र में भी है। भारत का दक्षिण एशिया में अत्यधिक महत्त्व है, जो उसके राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक प्रभाव से स्पष्ट होता है। बिम्सटेक का प्रमुख उद्देश्य सदस्य देशों के बीच आर्थिक- तकनीकी सहयोग बढ़ाना है। यह विभिन्न क्षेत्रों जैसे व्यापार, निवेश, परिवहन, ऊर्जा और संसाधनों के साझा उपयोग में सहयोग को प्रोत्साहित करता है। बिम्सटेक के माध्यम से सदस्य देश जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाओं, पारिस्थितिकी और सतत विकास जैसे मुद्दों पर मिल कर काम कर सकते हैं। यह संगठन साझा संसाधनों का उपयोग और उनके संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करता है जिससे सभी सदस्य देशों का लाभ हो।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिम्सटेक को मजबूत करने के लिए कई पहलों का प्रस्ताव रखा है। भारत आपदा प्रबंधन, सतत समुद्री परिवहन, पारंपरिक चिकित्सा और कृषि में अनुसंधान एवं प्रशिक्षण पर भारत में बिम्सटेक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगा। भारत द्वारा हर साल बिम्सटेक बिजनेस समिट आयोजित करने की पेशकश भी बहुत महत्त्वपूर्ण है। उम्मीद है कि बिम्सटेक देशों में आपसी समझ बूझ बढ़ेगी तथा बांग्लादेश और म्यांमार में लोकतंत्र स्थापित होगा। अंततः भारत के पड़ोसी देशों में स्थिरता भारत के हित में ही है, और बिम्सटेक उसका बेहतर माध्यम बनता दिखाई दे रहा है।
शुल्क संग्राम
संपादकीय
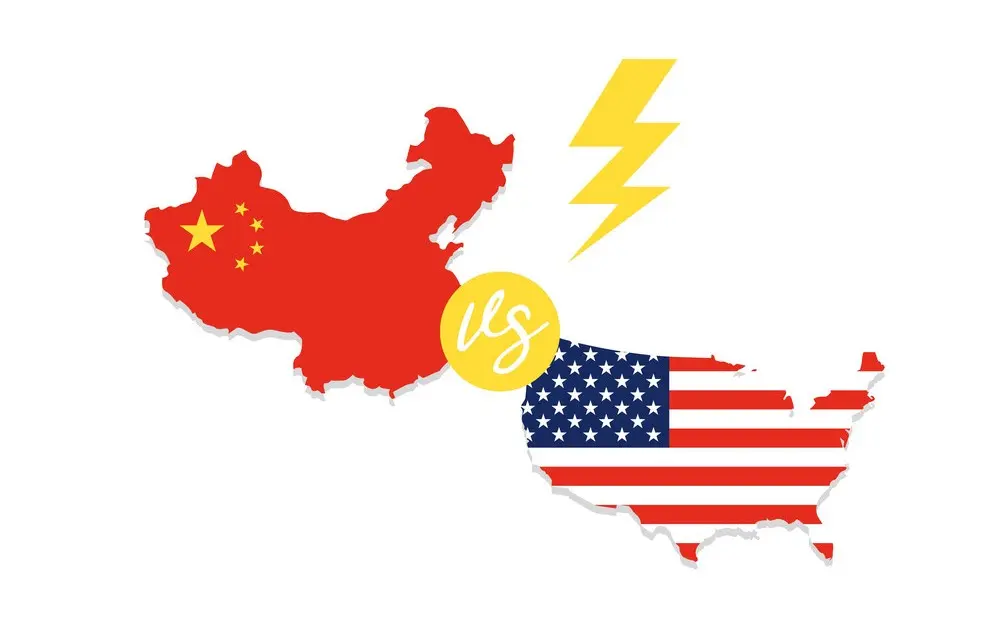
अमेरिका और चीन के बीच सीमा शुल्क संग्राम का तेज होना विचारणीय है। इस संग्राम की शुरुआती शिकायतें भी इन्हीं दोनों देशों के बीच हुई थी। एक लंबे समय तक अमेरिकी रियायतों का चीन ने खूब लाभ उठाया है और अब चीनी उत्पादों पर लगाए गए 125 प्रतिशत सीमा शुल्क से चीन बुरी तरह बौखला गया है। बीजिंग ने गुरुवार को चेतावनी दी है कि वह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा चीन पर शुल्क को बढ़ाकर 125 प्रतिशत करने के बाद आराम से नहीं बैठेगा। चौन ने यह भी दोहराया है कि अमेरिकी टैरिफ पूरी दुनिया के खिलाफ है। हालांकि, बाकी तमाम देशों को ट्रंप प्रशासन ने 90 दिन की राहत दी है | अतः अब यह स्पष्ट हो गया है कि अमेरिका का टैरिफ युद्ध वास्तव में चीन के खिलाफ है। दरअसल, एक लंबे समय तक अमेरिका से मिले सहयोग की वजह से भी चीन की भारी तरक्की हुई है। 1980 के दशक में चीन को आर्थिक मदद और तकनीक देने के साथ अमेरिका ने एक विकसित चीन की आधारशिला रखी थी। उसके बाद फिर चीन ने पलटकर नहीं देखा है। वह अपनी विकास यात्रा में अब अमेरिका से भी आगे निकलने की कोशिश में है। अब ट्रंप अमेरिका को फिर मजबूत बनाने की कवायद में चीन को खास तौर पर अगर निशाना बना रहे हैं, तो वास्तव में यह एक भूल सुधार की तरह ही है।
इतना तो साफ हो चुका है कि चीन और अमेरिका के बीच सीमा शुल्क संग्राम के कारण दोनों ही देशों को सर्वाधिक घाटा है। इन दोनों देशों में महंगाई, व्यापार संकट और बेरोजगारी का खतरा है। चीन ने पूरी ताकत के साथ कहा है कि वह आराम से नहीं बैठेगा और चीनियों को वैध अधिकारों और हितों से वंचित नहीं होने देगा। दूसरी ओर, बीजिंग नए सिरे से बातचीत के भी पक्ष में भी है। अगर बातचीत से बात बन जाती है, तो चीन चैन की बंसी बजाएगा, वरना उसने पहले ही अमेरिका को चेतावनी दे रखी है कि वह किसी भी मोर्चे पर वाशिंगटन के साथ लड़ने के लिए तैयार है।
हालांकि, यह लड़ाई पूरी दुनिया के लिए ठीक नहीं है। अमेरिका दूसरे देशों के साथ बातचीत के पक्ष में है। वह अवश्य यह कोशिश करेगा कि बातचीत से ही व्यापार संतुलन को अपने पक्ष में झुका ले। विशेष रूप से भारत जैसे देश के साथ बातचीत का रवैया ही बेहतर है। यह प्रक्रिया पहले से ही चलती रही है और हो सकता है, ट्रंप के समय इसमें तेजी आ जाए, पर इतना तय है कि अमेरिका को अपने मित्र देशों के साथ मिलकर टैरिफ के झगड़े को सुलझा लेना चाहिए।
अमेरिका को चीन से जो शिकायत है, उसको समझना भी जरूरी है। अमेरिकी कदम का चीन ने ही सबसे तीखा विरोध किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने चीनी समकक्ष शी जिनपिंग को स्मार्ट तो कहा है, लेकिन ट्रंप को शायद लगता है कि चीन जमीनी रूप से अमेरिका व अमेरिकियों का सम्मान नहीं करता है। सम्मान की कमी की चर्चा ट्रंप ने साफ तौर पर की है। क्या 125 प्रतिशत टैरिफ के बाद चीन अपनी नीतियों में बदलाव करेगा ? क्या दूसरे देशों को केवल बाजार समझने की नीति बदलेगी ? भारत के संदर्भ में ही अगर देखें, तो चीन खुले रूप से भारत को एक बाजार समझता है, लेकिन भारत के साथ वह सामरिक तनाव भी बनाए रखना चाहता है। अमेरिका के साथ अगर चीन का संघर्ष बढ़ा, तो उसे भारत की भी अहमियत बेहतर समझ में आएगी, लेकिन इसके लिए भारत को आत्मनिर्भर होने की अपनी यात्रा को हर हाल में तेज करना होगा।