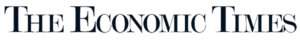10-06-2016 (Important News Clippings)
To Download Click here.
Date: 10-06-16
आठ फीसदी से ज्यादा की आशा में कई बाधा
शंकर आचार्य
देश के बीते वर्षों के समान उच्च विकास दर हासिल करने की ऐसी कई वजहें हैं जो बताती हैं कि स्थायी तौर पर इसकी संभावनाएं कम हैं। इसकी 10 वजह गिना रहे हैं शंकर आचार्य
वर्ष 2003-04 और 2010-11 के बीच भारत की 8 फीसदी से अधिक की आर्थिक वृद्घि दर ने यह उम्मीद पैदा कर दी कि देश कभी भी दोबारा उस दर को हासिल कर सकता है। लेकिन कई वजहें हैं जो बताती हैं कि स्थायी तौर पर ऐसा होने की संभावना काफी कम है। पहली बात, विद्वानों के मुताबिक सन 1950 से 2010 तक 60 साल की अवधि में दुनिया के केवल तीन देशों ने तीन दशक या अधिक समय तक 7.5 फीसदी की सतत विकास दर हासिल की है। ये मुल्क हैं दक्षिण कोरिया, ताइवान और चीन। कोई भी और देश दो दशक तक भी तेज विकास दर हासिल नहीं कर सका। हालांकि कई देशों में कम समय में तीव्र विकास के दौर देखने को मिले। दूसरी बात, विश्व अर्थव्यवस्था के प्रमुख औद्योगिक कारोबारी देश एक ऐसे समय में पहुंच गए हैं जहां ठहराव नजर आ रहा है। कम से कम आर्थिक विस्तार में धीमापन तो साफ महसूस किया जा सकता है। यह बात वैश्विक मंदी के बाद से ही महसूस की जा रही है। यूरोप, जापान और काफी हद तक अमेरिका के लिए यह बात सही है। अब जबकि हाल के वर्षों में चीन के तेज विकास में गिरावट आई है और वह दो अंकों से फिसलता हुआ 6 फीसदी पर आ गया है तब तत्काल सुधार दूर की कौड़ी नजर आ रहा है। ये चारों अर्थव्यवस्थाएं ही मिलकर दुनिया की कुल अर्थव्यवस्था के दो तिहाई के बराबर हैं। आश्चर्य नहीं कि विश्व व्यापार के आकार में भी गिरावट आई है और यह वैश्विक वित्तीय संकट के पूर्व की तुलना में काफी कम हुआ है। ऐसे में कहा जा सकता है कि निजी स्तर पर विभिन्न देशों के लिए वैश्विक आर्थिक माहौल उतना सकारात्मक नहीं है जितना पहले था।
कुल मिलाकर भारत के लिए भी मजबूत, स्थायी आर्थिक सुधारों की संभावना मजबूत नहीं दिखती। सन 1990 और 2000 के दशक के आरंभ में आर्थिक सुधारों की बौछार के बाद सुधारों ने गति खो दी है। वर्ष 2014 तक संप्रग के एक दशक के कारोबार में बहुत कम सुधार देखने को मिले। मोदी सरकार के पहले दो साल के कार्यकाल में जहां आर्थिक नीतियों के मोर्चे पर कुछ सुधार देखने को मिला है, वहीं सतत और मजबूत आर्थिक सुधारों की संभावना कमजोर ही नजर आई। आलेख में आगे मैं जिक्र करूंगा उन 10 चुनौतियों की जिन पर पर्याप्त काम नहीं हुआ है:
- श्रम आधारित विनिर्मित निर्यात का विस्तार पूर्वी एशिया के बेहतर प्रदर्शन करने वाले देशों का आधार रहा है। सस्ते और अकुशल कर्मियों की भरमार के बावजूद देश का रिकॉर्ड इस मोर्चे पर कमजोर बना हुआ है। इसके लिए मोटे तौर पर रोजगार विरोधी श्रम कानून, कमजोर बुनियादी शिक्षा, कमजोर बुनियादी ढांचा और लॉजिस्टिक शृंखला तथा कारोबारी सुगमता की राह की अन्य अड़चनें जिम्मेदार हैं।
- व्यापक तौर पर देखें तो भविष्य की आर्थिक वृद्घि दीर्घावधि में देश की मानव संसाधन तैयार करने की कमजोर नीतियों और कार्यक्रमों से प्रभावित होगी। खासतौर पर प्राथमिक शिक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में। 50 करोड़ की मजबूत श्रम शक्ति और बढ़ता जननांकीय लाभ एक ऐसी संपत्ति है जिसे बहुत भरोसेमंद नहीं कहा जा सकता है क्योंकि बच्चे स्कूली शिक्षा और पोषण के मोर्चे पर ही संघर्षरत हैं। ज्ञान आधारित विश्व अर्थव्यवस्था में देश ऐसे कैसे प्रगति करेगा?
- विकास का काम बंटे हुए, अस्पष्टï और भ्रष्टïाचार से आच्छादित भू बाजार में अटका हुआ है। इसके लिए काफी हद तक वर्ष 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून के रूप में मिली संप्रग की विरासत को जिम्मेदार माना जा सकता है। मोदी सरकार ने संशोधन का प्रयास किया लेकिन विफल रही।
- कुछ अपवादों के साथ देश का बुनियादी ढांचा भी अपर्याप्त बना हुआ है। यह बात बिजली क्षेत्र और शहरी बुनियादी सेवाओं के लिए खासतौर पर सही है। बिजली पारेषण, वितरण और मूल्य निर्धारण में चूक ने पूरी व्यवस्था को हिलाकर रख दिया है। वर्ष 2015 की उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) भी समस्याओं के पूर्ण निराकरण का दावा नहीं करती।
- कृषि वृद्घि एवं विकास पर भी जल संसाधनों के कुप्रबंधन का साया मंडरा रहा है। उदाहरण के लिए पानी और बिजली का कम मूल्य लगातार जलाशयों और जलवाहियों के सूखते जाने और जल संकट की वजह बना हुआ है। जलवायु परिवर्तन, उच्च यूरिया सब्सिडी और पानी की खपत वाली फसलों को प्रोत्साहन ने भी समस्याओं में इजाफा किया है।
- सरकारी क्षेत्र के दबदबे वाली बैंकिंग व्यवस्था गहरे संकट में है। सरकारी बैंकों का फंसा हुआ कर्ज बहुत ज्यादा है। केंद्रीय बैंक और मौजूदा सरकार ने बैंकों की बैलेंस शीट की समस्या को सामने लाने का काम किया है लेकिन समस्या निदान का एक ठोस खाका सामने आना बाकी है। इस बीच नए ऋण में धीमापन देखने को मिला है।
- देश में शहरीकरण की प्रक्रिया बहुत जटिल है। इसमें भूमि नियोजन को किफायती बनाने पर कतई ध्यान नहीं दिया गया है। न ही नगरीय वित्त व्यवस्था, सेवा प्रावधान और पर्यावरण स्थायित्व को लेकर कुछ खास तवज्जो है। अगले 15 सालों में शहरी आबादी में करीब 20 करोड़ का इजाफा होगा। अगर सबकुछ यथावत रहा तो सामुदायिक संकुलन के आर्थिक लाभ खत्म हो सकते हैं। नगरीय निकायों, वित्त व्यवस्था और प्रशासनिक सुधार ही शहरीकरण की चुनौती के मूल में है। इस दिशा में कुछ खास नहीं हो रहा।
- वृहद आर्थिक स्तर पर देखें तो राजकोषीय घाटे का उच्च स्तर वृहद आर्थिक प्रबंधन पर हावी है और इसने बीते तीन दशकों के दौरान इसके प्रदर्शन को प्रभावित किया है। हाल के दिनों में कुछ सुधार के बावजूद समेकित घाटा अभी भी जीडीपी के 6 फीसदी से अधिक है। इससे ब्याज दरें उच्च बनी हुई हैं और देश वृहद आर्थिक झटकों को लेकर संवेदनशील नजर आ रहा है। इतना ही नहीं मुद्रास्फीति में कमी के बीच जीडीपी की तुलना में सरकारी कर्ज का 65 प्रतिशत तक का अनुपात और बढ़ रहा है। देश के सार्वजनिक वित्त की प्रमुख ढांचागत समस्या है कमजोर राजस्व आधार और लोकलुभावन खर्च। यह आगे भी चुनौती बना रह सकता है
- वर्ष 2012-13 में जीडीपी के 5 फीसदी के बराबर तक उछलने के बाद भुगतान संतुलन में चालू खाते का घाटा बीते तीन सालों से 1-2 फीसदी के दायरे में बरकरार है। इससे एक तरह की आश्वस्ति का भाव पनपा है। यह पूरा समायोजन कच्चे तेल की कीमतों तथा अन्य जिंस कीमतों में आई गिरावट से उत्पन्न हुआ है। जीडीपी में निर्यात की हिस्सेदारी कम हुई है। जब तक भारत की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता में इजाफा नहीं होता है और तेल कीमतों को लेकर हमारी संवेदनशीलता बरकरार रहती है तब तक बाहर से आने वाले धन में कमी और पूंजी की आवक में अस्थिरता असहज करने वाले स्तर तक बढ़ सकती है।
- अंत में, अधिक तेज आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए बड़े प्रशासनिक सुधारों को अंजाम देना होगा जो काफी समय से लंबित हैं।
इस परिदृश्य में तो 8 फीसदी से अधिक की विकास दर को लगातार बरकरार रखना टेढ़ी खीर लग रहा है। हां, हम 6 फीसदी के आसपास की दर की उम्मीद कर सकते हैं।
Date: 10-06-16
इच्छा मृत्यु मुद्दे पर कानूनी बहस का दिलचस्प होगा नतीजा
श्यामल मजूमदार
अगर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय पैसिव यूथनैश्या (बाह्यï जीवन रक्षक उपकरण हटाकर किसी असाध्य बीमारी से पीडि़त को स्वाभाविक रूप से मरने देना) संबंधी मसौदा विधेयक पर आम जनता से मिलने वाले प्रतिसाद को सार्वजनिक करता है तो यह बात स्वागतयोग्य होगी। गत माह इस विधेयक को अपनी वेबसाइट पर अपलोड करते हुए मंत्रालय ने कहा था कि वह अंतिम निर्णय लेने से पहले 19 जून तक इस विषय पर जनता की राय जानना चाहता है। ऐसे उच्च भावनात्मक मुद्दे पर लोगों की राय रोचक होगी क्योंकि दुनिया भर में जीवन के अधिकार और सम्मानजनक मृत्यु के अधिकार को लेकर गहन बहस चलती रही है।
Date: 09-06-16
धरोहर की जगह
अपनी विरासत को सहेजना-संजोना हर जागरूक राष्ट्र का कर्तव्य है। ऐतिहासिक धरोहर से उसके सांस्कृतिक विकास का पता चलता है|
अमेरिकी सरकार ने भारत से चोरी गई दो सौ से ज्यादा कलाकृतियां और ऐतिहासिक महत्त्व की वस्तुएं लौटा कर अपने सांस्कृतिक भाईचारे की नई मिसाल पेश की है। यह धरोहर अंतरराष्ट्रीय तस्करी गिरोहों ने मंदिरों, संग्रहालयों आदि से चुरा ली थी। इनमें से कुछ कलाकृतियां दो हजार साल से ज्यादा पुरानी हैं। निश्चय ही इससे भारत के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विकास का अध्ययन करने वालों को काफी मदद मिलेगी। भारत की प्राचीन मूर्तियों, कलाकृतियों, ऐतिहासिक महत्त्व की वस्तुओं की अंतरराष्ट्रीय बाजार में खासी मांग है। कई वस्तुओं की मुंहमांगी रकम मिल जाती है। यही वजह है कि तस्करी करने वाले गिरोह ऐसी चीजों को चुराने की फिराक में रहते हैं। कई देशों में ऐसी वस्तुओं-कलाकृतियों आदि की नीलामी करने वाली बड़ी-बड़ी कंपनियां हैं। कई मौकों पर भारत सरकार के लिए मुश्किल भी खड़ी हो जाती है, जब किसी ऐतिहासिक धरोहर को नीलामी के लिए प्रदर्शित किया जाता है। करीब दो साल पहले गांधीजी की निजी उपयोग की कुछ वस्तुओं को ब्रिटेन में नीलामी के लिए प्रदर्शित किया गया तो यहां दबाव बनना शुरू हो गया कि भारत सरकार को उन्हें किसी भी तरह वापस लाना चाहिए। तब सरकार को काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। कुछ मौकों पर बोली के लिए रखी गई ऐसी ऐतिहासिक वस्तुओं को कुछ उद्योगपतियों और संपन्न लोगों ने खरीद कर सहेजा या फिर सरकार को वापस दे दिया। मगर अब भी बहुत सारी कलाकृतियों और ऐतिहासिक वस्तुओं का पता लगाना या उन्हें वापस लाना कठिन बना हुआ है। मसलन, रवींद्रनाथ ठाकुर के चोरी गए नोबेल पदक का अब तक पता नहीं चल पाया है। कोहेनूर हीरा वापस लाने का दबाव काफी समय से बनता रहा है, पर उसे वापस लाना मुश्किल बना हुआ है। अपनी विरासत को सहेजना-संजोना हर जागरूक राष्ट्र का कर्तव्य है। ऐतिहासिक धरोहर से उसके सांस्कृतिक विकास का पता चलता है। मगर जब ऐसी कोई वस्तु चोरी करके दूसरे देश में पहुंचा दी जाती है तो उसे वापस लाना कठिन हो जाता है। इसलिए अब कई देशों ने तय किया कि वे तस्करों से बरामद वस्तुओं को संबंधित देशों को वापस लौटाएंगे। इस क्रम में भारत को ऐतिहासिक महत्त्व की बहुत सारी चीजें विभिन्न देशों से प्राप्त हो चुकी हैं। अमेरिका से वापस मिली वस्तुएं शायद अब तक की सबसे बड़ी धरोहर है। इनमें से ज्यादातर चीजें वहां चलाए गए आॅपरेशन हिडन आइडल के दौरान बरामद की गई हैं। अच्छी बात है कि बहुत सारे देशों ने महत्त्वपूर्ण कलाकृतियों, ऐतिहासिक महत्त्व की वस्तुओं आदि की चोरी पर नकेल कसने के मकसद से ऐसे अभियान चलाने की नीति बना रखी है। इससे ऐसी चीजों की तस्करी पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। अमेरिका ने ऐसी वस्तुएं वापस कर भारत की धरोहर को समृद्ध किया है। पर हमारे यहां इस बात पर भी ध्यान देने की जरूरत है कि संग्रहालयों, मंदिरों आदि में रखी बेशकीमती और नायाब कलाकृतियों, ऐतिहासिक दस्तावेजों आदि की सुरक्षा कैसे की जाए। संग्रहालयों की निगरानी में मुस्तैदी की कमी के तथ्य अनेक मौकों पर उजागर हो चुके हैं। कई बार इनकी देखरेख करने वालों की चोरों से मिलीभगत के तथ्य भी उजागर हो चुके हैं। इसके अलावा रखरखाव में संजीदगी न होने के कारण अनेक दस्तावेज धूप, गरमी, सीलन वगैरह के चलते विरूपित या नष्ट हो जाते हैं। इसलिए चोरी गई वस्तुओं को दूसरे देशों से प्राप्त करने के साथ-साथ इन कमजोर पहलुओं पर भी ध्यान देने की जरूरत है।
Date: 09-06-16
विवाद का परदा
यों सभी जानते हैं कि पंजाब में नशे की समस्या दिनोंदिन गहराती गई है और यह गंभीर चिंता का कारण बन चुका है।
फिल्मों के प्रदर्शन और उस पर पाबंदी को लेकर विवाद पहले भी होते रहे हैं, लेकिन ‘उड़ता पंजाब’ को लेकर पैदा हुए टकराव ने जिस तरह राजनीतिक शक्ल ले ली है, वैसा कम देखा गया है। हालत यह है कि एक ओर सीबीएफसी यानी केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष पहलाज निहलानी ने इस फिल्म के लिए आम आदमी पार्टी से धन मिलने तक की आशंका जता दी है। दूसरी ओर, अरविंद केजरीवाल ने इस फिल्म को रोकने की कोशिश में भाजपा के शामिल होने का आरोप लगाया है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भी फिल्म के पक्ष में खुल कर अपनी राय जाहिर की है। लेकिन इस सबसे अलग एक फिल्म में प्रस्तुत कुछ दृश्यों और संवादों की वजह से रोके जाने या उसे बदलने की सलाह देने को हमेशा एक कलात्मक अभिव्यक्ति को बाधित करने के तौर पर देखा गया है। सेंसर बोर्ड की ओर से भी ऐसी ही दलील दी गई है। दरअसल, इस फिल्म के विवाद की वजह इसका विषय है, जिसमें पंजाब में नशे की शिकार युवा पीढ़ी को दिखाया गया है। लेकिन खबरों के मुताबिक इस क्रम में गालियां या अपशब्दों का जिस पैमाने पर इस्तेमाल किया गया है, सेंसर बोर्ड की निगाह में वे बेहद आपत्तिजनक हैं। सेंसर बोर्ड को इस बात पर भी आपत्ति है कि फिल्म के नाम में पंजाब शब्द क्यों है। इसलिए तकरीबन नब्बे दृश्यों पर कैंची चलाने के अलावा यह भी सलाह दी गई है कि फिल्म के नाम में से भी पंजाब को हटाया जाए, तभी इसे सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। सवाल है कि अगर फिल्म में बड़ी तादाद में युवाओं को नशे की गिरफ्त में दिखाया गया है और यह पंजाब की गलत तस्वीर है तो इसका फैसला पंजाब या दूसरे इलाकों के दर्शक करेंगे या लोगों को इस सवाल से रूबरू भी नहीं होने दिया जाएगा! फिल्म के निर्माता अनुराग कश्यप ने इसे सेंसर बोर्ड की तानाशाही कहा है और इसके लिए अदालती लड़ाई में जाने का फैसला किया है। इससे पहले जितनी भी फिल्मों से जुड़े विवाद अदालत के पास पहुंचे, उन्होंने इसे कला और अभिव्यक्ति की आजादी से जुड़ा मामला बता कर उसके सही या गलत होने का निर्णय दर्शकों पर छोड़ देने का पक्ष लिया। यों सभी जानते हैं कि पंजाब में नशे की समस्या दिनोंदिन गहराती गई है और यह गंभीर चिंता का कारण बन चुका है। आगामी विधानसभा चुनावों में इसका मुद्दा बनना तय माना जा रहा है और इसी मसले को फिल्म में दिखाया गया है। इसलिए माना जा रहा है कि विवाद की जड़ जितनी फिल्म है, उससे ज्यादा कुछ राजनीतिक दलों के भीतर राज्य में विधानसभा चुनावों के मद्देनजर उसके प्रभावों की आशंका है। लेकिन आखिरकार यह सेंसर बोर्ड पर निर्भर है कि वह फिल्म को जारी करता है या नहीं। तो जिन मानदंडों के तहत सेंसर बोर्ड ने ‘उड़ता पंजाब’ के प्रदर्शन पर सवाल उठाया है, क्या वह बाकी तमाम फिल्मों के बारे में यही मानदंड अपनाता है? पिछले दिनों कई ऐसी फिल्में प्रदर्शित हुर्इं, जिनमें कुछ प्रस्तुतियों को लेकर आपत्ति जाहिर की गई थी। लेकिन एक फिल्म के लिए लागू शर्तें दूसरी फिल्म के संदर्भ में लागू नहीं होतीं। हो सकता है कि अभिव्यक्ति की आजादी की दलील पर कुछ फिल्मों में गैरजरूरी या आपत्तिजनक दृश्य और संवाद परोसे गए हों। क्या इसे दर्शकों के विवेक पर नहीं छोड़ दिया जाना चाहिए कि वे फिल्म को कैसे देखते हैं!
Myth and reality
Art and culture are going through a right-wing phase, though Hindu art forms have never been targeted in India.
As one who is thought of as belonging to the “world of culture”, I would say that the first two years of the Narendra Modi government have been the most disturbing times that I can recall. It has been a period when the political context has forced me to ask difficult questions of what this nation really is as a cultural identity. An ideational collapse has occurred and you can see it even these paragraphs. I find I have used the word culture to describe what is essentially religious.
Would I have done this some years ago? I would not have. This too is a remarkable achievement by the present dispensation. It is not that Prime Minister Narendra Modi has stood up at the ramparts of the Red Fort and made a proclamation to the effect that India that is Bharat has one culture, in body, mind and soul, and it’s name is Hindutva. He has not done that. In fact he has, both in India and abroad, spoken of “sabka saath”, but his colleagues and political partners have blatantly espoused Hindutva. And he has not contradicted them.
Hindus have been told by Hindutva’s spokespersons that for the last 60 plus years, this country has victimised and marginalised them. We have reached a point where this manifest untruth now carries the ring of historical truth. Hindus have been quite happily celebrating every festival with pomp, in fact the sizes of pandals during Ganpati utsav or Durga puja have only increased, the number of young people who visit temples has clearly been on the rise over the past decade or more and, let us not forget the proliferation of sadhus and gurus that dot our topography. If anything the Hindu, is far from being sunk or mass converted. But the fear of such a happening has been implanted in every Hindu mind.
Religious violence is not a creation of this government. The Congress can never atone enough for 1984. But there is a shift in the way society has taken to this new Hindutva political craftsmanship and that is for me the most worrisome trend. Today, violence of the religious/cultural kind is not just a tool of party politics and their attached lumpen outfits, today it is owned and worn on the sleeve with aplomb.
It is said with barely concealed anger if a Hindu celebrates his religion, he is accused of being right-wing but a Muslim is never asked that question. Let us think about this, seriously. In this world’s context, can we ever make this statement and actually believe it is true? If there is any community that has been globally vilified, it is the people of the Islamic faith, yet we are convinced that they have greater acceptance than the middle and upper class Hindu. There is enough data to prove that Muslims and Dalits are the most backward communities in this nation. There is no doubt that parties in and out of power including the Congress and many Muslim leaders wearing various political hats have only exploited the average Muslim voter, but should this make “us” insensitive to “their” real conditions? Worse is to think that Muslims are receiving benefits at Hindus’ cost. This idea in itself entrenches an underlying cultural thought — that this is a Hindu land and that Muslims are guests. Not to forget the allied belief that Muslims are terrorists or possible terrorists, unless Hindu thought has touched them, and just in case you did not know, Sufism is quintessentially Hindu!
Another invented truism being spread around is that the education system has made people anti-Hindu and pro-religious minorities. Even more laughable is the assertion that leftist academicians with the connivance of western socialist scholars have wiped out Hindu goodness and achievements from our history. If we were to visit the innumerable religious studies, art and language departments around this country, we will find more PhDs that are seeped in Hindu religiosity than of the other kind. But from what the naysayers claim, India by now should have become a mini-Soviet Union, but we are not, and thank goodness for that.
For all the Hindu pride that is demanded of us, the last few years have witnessed a strong misogynist (let us remember that this is not just a male attitude) and pro-upper caste/class articulation of India. There is clearly a cultural strategy to linearise Hindu sanskriti and within it engulf all that has in the past and present questioned its organisation. In the eulogisation of Hindu history I also smell a strong whiff of appropriation combined with the establishment of a certain idea of the Hindu — one that emanates from the middle classes. There has been no attempt to address issues of gender, multiple genders or caste. If anything there is a suppression of such discourses. Suppression today is not enforced via a dictatorial ban, it is mobilised using fear.
The world of the arts, especially the classical and wannabe classical community (nobody cares about the rest) has heralded this government, for they believe that they are the true representatives of Bharatiya sanskriti. All of sudden many Hindutvas have emerged out of closet. There is clearly a streamlining of what is artistically Indian, where religious Hindu inclined art forms are being pushed forward. Art and culture are going through a right-wing phase, even though at no point in India’s independent history were the Hindu art forms targeted. Hasn’t Bharatanatyam always been the “number one” symbol of Indian antiquity?
We should not allow people to subsume culture into religious belief systems. But I now wonder whether the larger society really cares to engage with this thought. Sociologists, activists and cultural liberals vouch for India’s syncretic identity providing us many living examples of wonderful people. But do these small pockets matter anymore? If anything they are being used to certify the real Indian – the one who accepts the Hindu as that mythic being.
As I end this piece, I feel another achievement of this government, at least in me — cultural pessimism.
Date: 10-06-16
Bring on real estate investment trusts
It is time real estate investment trusts (Reits), investment vehicles akin to a mutual fund, took off. They now have a tax regime that suits their requirements. Timely launch will boost returns for Reits, help developers saddled with debt, offload inventory and reduce bad loans on the banks’ books. Typically, Reits own commercial properties such as apartment complexes, shopping malls, hotels, office buildings. Rentals from properties owned and managed by them form a substantial slice of their revenues. Reits will also help finance the physical infrastructure of India’s rapid urbanisation.
The Blackstone Group and its partner Bangalore-based Embassy Group have reportedly hived off their portfolio of assets into a separate company, which would be the first step to unlock value through a listing. Sebi has already put in place a robust regulatory framework for Reits. A wait for market conditions to improve further to transfeer ownership to Reits could prove indefinite. The best time to get going is now.
Tax policy is conducive now for investment in Reits. This Budget scrapped the dividend distribution tax that business trusts have to pay when the asset-holding company, a special purpose vehicle, pays dividends. The case was compelling as Sebi rules mandate both the SPV and business trust to distribute 90% of their operating income to investors. Dividend income is tax-exempt in the hands of the unitholder. Interest income is also exempt from tax at the level of Reits, but not in the hands of investors. Rightly, these tax incentives open up opportunities for property developers to raise funds in the domestic markets, instead of listing such vehicles overseas. It also enables a wider set of investors to participate in and gain from the real estate boom.
Date: 10-06-16
Sack Nihalani
India can’t afford a film certification head who’s clueless about films
Prime Minister Narendra Modi’s speech to a joint session of US Congress elicited as many as nine standing innovations in the course of 45 minutes. He played masterfully on the many common points between the idea of India and the idea of America as well as how their histories have intersected, making the best presentation of India’s case by an Indian leader one has seen in a very long time.
One of the common points he didn’t mention but could just as well have is that while America has Hollywood, India has Bollywood. Not only is the term ‘Bollywood’ derived from ‘Hollywood’, both do a great deal to enhance the soft power and appeal of two democracies – India and America – to other countries. Enhancing India’s appeal is surely also the objective of Modi’s bravura diplomacy abroad. That’s all the more reason for India to nurture, rather than choke, its vibrant film industry. But not only does the current head of India’s Central Board of Film Certification (CBFC) not get this – leading to an unprecedented and joint protest against his policies from some of the biggest and most reputed names in Bollywood – he looks fundamentally clueless on what films are about.
As much is suggested by some of the cuts enjoined on ‘Udta Punjab’. They include deletion of words like ‘election’, ‘MP’, ‘MLA’, ‘party’, ‘Parliament’ and references to Punjab as well as places in Punjab. The common factor here seems to be that references to politics as well as to places are seen as forbidden territory for cinema. This is unprecedented. The strongest films – including Indian films – have been rooted in places and are often about politics and social evils. If such rules are enforced, a future Satyajit Ray or Shyam Benegal can never emerge in India.
Crores of rupees are invested in films. Procedures followed by the board must be predictable and limited – not arbitrary, whimsical and excessive. Its job is only to certify films, not to censor let alone dictate to the filmmaker what he should be saying. Nihalani is in gross overreach of his brief and a competent replacement must be found for him. More broadly speaking posts in education and culture should not be seen as ‘soft’ jobs, given to candidates whose main qualification is political sycophancy rather than talent and understanding. Else India’s soft power quotient will plummet under NDA, no matter how brilliantly Modi makes India’s case abroad.
Date: 09-06-16
‘Civil society in India remains vibrant’
But there is evidence of a problem regarding its FCRA regulations, and reason to be concerned, says UN Special Rapporteur Maina Kiai.
The Central government has acted against a number of NGOs in India in the past two years for allegedly violating the Foreign Contribution (Regulation) Act. In a recent analysis report, the UN Special Rapporteur on rights to freedom of peaceful assembly and of association, Maina Kiai, said the FCRA regulations in India do not meet the International Covenant on Civil and Political Rights’ (ICCPR) proportionality requirement. In an e-mail interview with T.K. Rohit, Mr. Kiai said “there are currently serious obstacles to the right to freedom of association that violate international law.” Excerpts from the interview:
Do you think there is enough evidence to be concerned about India’s FCRA regulations?
Clearly there is evidence of a problem, and reason to be concerned. I have received a number of reports over the years from activists and organisations who feel that they have been targeted by the government. I have an equally clear sense that they feel their space to operate freely is closing.
Is the Indian government stifling NGOs?
I believe there are currently serious obstacles to the right to freedom of association that violate international law, and that these obstacles have increased in recent years. I have received a number of complaints about this issue from Indian organisations, and the volume has grown since I began working as Special Rapporteur. I also know that there is quite a lot of activity and debate around this issue in India, with some sources reporting tens of thousands of NGOs losing their licences to receive foreign funding.
At the same time, civil society in India remains vibrant — at least for the moment. India is very important in the UN context. It is the world’s biggest democracy and has a massive and vibrant civil society. India is seen as a leader for other countries, but unfortunately in this area it is leading in the wrong direction.
Your report points out that the FCRA appears to contravene India’s obligations under the ICCPR. What measures can India take in this regard?
There are three possibilities. The first, which can be done tomorrow, is to be more permissive in interpretation of the law. The second, which would take legislative action, is to repeal the law. The third is for a domestic court to find the law unconstitutional or in violation of international law.
Even a democracy and its legislative institutions have to respect the international obligations of the state.
Can’t a country mandate that organisations raise funds internally?
Under international law, governments clearly can’t put a blanket restriction on organisations receiving any foreign funding. Such restrictions are inherently disproportionate. I would also add that the Government of India is a massive player when it comes to overseas development aid — both as a donor and a recipient. Why should it be okay for the government to receive and donate funds, but not for independent organisations?
What’s the way forward?
At the very least, I would like to have a dialogue with the Government of India. They have yet to officially respond to the analysis I submitted, but I would like to hear their views. This dialogue can be formal, informal, or something in between.
The best-case scenario would be for India to invite me to conduct an official country visit, where I can meet with government officials and civil society in person. I requested such a visit in 2014, but the government is yet to respond. I would also be very open to conducting an unofficial visit to the country. In fact, I’ve tried to do this at least twice, but was never able to secure a visa. I would take it as a positive sign of engagement if the Government of India could step in to help facilitate the visa process, so that I can come to the country at least in an unofficial capacity.
And ultimately, of course, I would like to see the Government of India — whether via the executive, legislative or judicial branch — act on my analysis and make the appropriate adjustments to the FCRA.