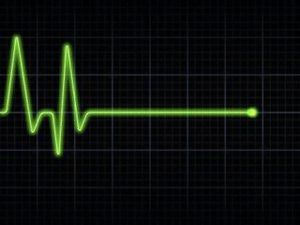10-03-2018 (Important News Clippings)
To Download Click Here.
Patient’s Choice
Living will elevates passive euthanasia
TOI Editorials
In asserting the right to die with dignity and giving legal sanction to passive euthanasia and living wills, Supreme Court has reiterated the individual’s sovereignty over the body. Though the government took the lead in decriminalising suicide and is ready with a draft legislation formalising passive euthanasia, it struck a contradictory note in opposing living wills, essentially a person’s desire to exit from life at a point of no return. Living wills authorise doctors and relatives to exercise passive euthanasia and withdraw life support in the event of terminal illness or slide into a vegetative state or irreversible coma.
The government argument that living wills can be abused by greedy relatives is unconvincing. In passive euthanasia, no individual is given inordinate powers to take a life and safeguards require judicial scrutiny and a medical board comprising a team of doctors to make the recommendation. Choosing death, giving birth, abortion, making love, eating food, wearing clothes, and turning religious are extremely personal choices people make. The state must know where to get off. Choosing not to prolong one’s life artificially is a human right and a humanitarian choice, especially when pain is involved.
A passive euthanasia legislation that does not incorporate living wills is half baked, to put it mildly. Unlike relatives or friends making a choice for a person who has slipped into coma, a living will carries the moral force of a patient’s own choice to not prolong life. Medical ethics demand doctors educate patients and relatives about the implications and effectiveness of life support systems like ventilators, but commercial imperatives of hospitals triumph all too often. Like the privacy judgment, the right to die with dignity is a way for courts to support people living life on their own terms rather than being infantilised by government or exploited by commerce.
Date:10-03-18
Small Mercies
Finally, Supreme Court has acknowledged Hadiya’s right
TOI Editorials
Are women citizens of this nation? Do they have the right to exercise their minds and wills, choose their faiths and their spouses? That question, basic and astounding as it is, has been at the core of the legal ordeal that 24-year-old Hadiya (formerly Akhila Ashokan) has been forced to undergo over the last year.
The Supreme Court has finally ended what the Kerala high court wrought when it declared her marriage to a Muslim man null and void, on the basis of a complaint from her father who alleged that she was being “forcefully converted to Islam”. Akhila, an adult and mentally fit woman, had chosen to convert to Islam, and then chosen her partner Shefin Jahan. This was portrayed as “love jihad”, and NIA has been asked to investigate possible links with Islamic State (IS).
This cloud of aspersions has been allowed to obscure the only relevant fact here: Hadiya’s choice to marry and practise any religion she wants is granted by our Constitution. Nobody has the right to “guard” her or claim her as territory, against her own stated intentions. She is a rights-bearing individual, not a symbol for any community or patriarchal order. NIA is free to probe IS luring or coercing people to join it, but we are not well served by lazy Islamophobic associations that link terrorism and threat with marriages. At long last, the Supreme Court has ended the sham that deprived Hadiya of her liberties.
When Death Comes From Life, Liberty
ET Editorials
It is welcome that a Constitution bench of the Supreme Court has endorsed, through four separate but concurring judgments, the idea of passive euthanasia, subject to stringent conditions against misuse. The right to live should logically encompass the right to stop living — the right to eat does not prevent a man from doing something else in life apart from eating, or the right to sleep does not mean that he can only sleep in exercise of his right. Justice Chelameswar, in his right to privacy judgment, had opined that the right to privacy extends to the right to stop living. More Indians can now die with dignity.
The real challenge is not any analytic difficulty in accepting the soundness of the idea of a living will that allows an individual to direct, in advance, that in conditions that preclude restoration of decent life, technological intervention to prevent death should cease. The challenge lies in ensuring that any such living will is made while the patient was competent to make that determination, in ensuring fair, competent determination that medical science is, indeed, incapable of restoring decent life to the patient on life support systems and in ensuring that the arrangements made to fulfil these two conditions function with integrity so that the best interests of the patient are served. The court has suggested several conditions, including a District Magistrate-appointed medical board to vet the decision of the hospital medical board that life support systems merely prolong a vegetative or painful existence without any hope of redemption.
While these should do for the time being, Parliament should lose no time in legislating on the subject, arriving at safeguard conditions, the means of their enforcement and the penalties for subverting these conditions on medical professionals and family members of the patient undergoing passive euthanasia, after proper deliberation. Helpful suggestions can be found in more than one report of the Law Commission of India. Integrity and ethical conduct of the medical and legal professions need supplementary fortification, on matters beyond passive euthanasia as well.
आखिरकार अपने जीवन पर अपनी मर्जी चलाने की मंजूरी
पांच जजों की पीठ ने चार अलग-अलग आदेश लिखे हैं लेकिन, उनका निष्कर्ष समान है।
संपादकीय
सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय पीठ ने इच्छा मृत्यु के लिए दिशानिर्देश जारी करके उस स्थिति को स्पष्ट कर दिया है जो उसके निर्णय और सरकार के विधेयक के बीच फंसी हुई थी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अरुणा शानबाग बनाम भारत सरकार के मुकदमे में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को सैद्धांतिक रूप से इजाजत देकर सरकार के समक्ष उसकी कार्यविधि निर्धारित करने का दायित्व डाल दिया था। इस बीच सरकार की तरफ से कोई पहल न होते देख कामनकॉज़ नामक गैर-सरकारी संस्था की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं।
इससे यह भ्रम दूर होता है कि असाध्य रूप से बीमार मरीज को जीवन प्रणाली पर न रखने या एंटीबायोटिक न दिए जाने का फैसला लेने का अधिकारी कौन है। अदालत ने स्पष्ट कहा है कि अब गंभीर रूप से बीमार कोई व्यक्ति जीवित रहते हुए यह वसीयत बना सकता है कि उसे एक अवस्था के बाद दवाएं न दी जाएं या उसके शरीर को विशेष मशीन पर न रखा जाए। पांच जजों की पीठ ने चार अलग-अलग आदेश लिखे हैं लेकिन, उनका निष्कर्ष समान है।
इनमें न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा है कि जीवन और मृत्यु अविभाज्य हैं और जीवन प्रतिक्षण परिवर्तित हो रहा है। ऐसे में मरना भी जीवन का ही हिस्सा है। मरीज के करीबी मित्र या रिश्तेदार द्वारा पेश की गई वसीयत के माध्यम से मेडिकल बोर्ड को कोई फैसला लेने में मदद मिलेगी और व्यक्ति अपने जीवन को पीड़ा से मुक्त कर सकेगा। न्यायालय ने इस प्रकार अपने सैद्धांतिक निर्णय को अमली जामा पहनाने का एक साहसिक कदम उठाया है, क्योंकि इस बारे में कार्यपालिका झिझक रही थी।
तमाम तरह के विवादों को जन्म देने वाली कार्यपालिका धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के इस मसले पर फैसला लेने में क्यों झिझकती है यह समझ से परे है। इस लिहाज से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तय दिशानिर्देश व्यक्तिगत आजादी को मजबूत करने वाला है। हालांकि, सरकार ने कहा है कि अब वह भारतीय दंड संहिता की धारा 309 को अपराध के दायरे से मुक्त करने जा रही है। सरकार की यह मंशा व्यक्ति की उसी इच्छा को सशक्त करने वाली है, जिसके तहत वह इच्छामृत्यु का अधिकार प्राप्त करेगा। अब सरकार को बिना देरी के इस विषय में कानून बनाना चाहिए ताकि मेडिकल बोर्ड, न्यायालय और समाज को जीवन और मृत्यु के बारे में एक अहम फैसला लेने में कोई दुविधा न रहे।
सामाजिक एका का अधूरा एजेंडा
(कै.) आर विक्रम सिंह (लेखक भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। )
हमारे राजनीतिक परिदृश्य में संभावनाओं, नेतृत्व एवं विकल्पों की बहुतायत है। इस बहुतायत से हम भलीभांति परिचित हैं और साथ ही इससे भी अवगत हैं कि हमारे पास धार्मिक नेतृत्व भी है, जो धर्म एवं हमारी परंपराओं के बारे में मार्गदर्शन देता रहता है। इन दोनों के मध्य एक बहुत बड़ा रिक्त क्षेत्र है, जो समाज का है। अपने यहां सामाजिक नेतृत्व का अकाल-सा है। समाज का एकीकरण किसी का लक्ष्य नहीं बना। जातियों के बीच बढ़ रहे विभाजन, सामाजिक वैमनस्य को किसी ने लक्षित नहीं किया। कबीर, तुलसी, नानक जैसे संत-महात्मा तो दूर, कोई राजा राममोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर जैसा भी फिर नहीं आया जो जातीय भिन्न्ताओं, सामाजिक विषमताओं और कुरीतियों को संबोधित कर सके। जब लोकतांत्रिक राजनीति ने जातियों को स्वीकार्यता दे दी, तो कोई सामाजिक नेता जातीय सोच के विरुद्ध विद्रोह करने खड़ा नहीं हुआ। हमने देखा है कि आजादी के आंदोलन की आहट मात्र से ही 19वीं और 20वीं सदी में राजनीति ने बड़े नेता पैदा किए, लेकिन गांधीजी के अतिरिक्त कदाचित महामना मदन मोहन मालवीय ही ऐसे नेता बने जिन्होंने राजनीति के अतिरिक्त सामाजिक एजेंडे को भी आगे बढ़ाया। बाबासाहब आंबेडकर का लक्ष्य दलित समाज के दायरे से बाहर नहीं निकल सका। सामाजिक आजादी स्वतंत्रता आंदोलन का भूला हुआ एजेंडा है। समर्थ सामाजिक नेतृत्व न होने से विभाजनकारी प्रवृत्तियों की काट नहीं हो पा रही है। समग्र समाज किसी के एजेंडे में नहीं है। चूंकि सत्ता, पद और अधिकार का लक्ष्य सामने दिखता है, इस कारण राजनीति सर्वाधिक आकर्षक क्षेत्र बन जाती है। राजनीति के लिए व्यक्ति वोटर है। धर्माधिकारियों के लिए व्यक्ति अनुयायी है। आखिर वह समाज ही है जो व्यक्ति, परिवार की चिंता करता है, लेकिन हमारा समाज व्यक्ति को नहीं जातियों, संप्रदायों में देखता है।
सेवानिवृत्त आईपीएस अफसर मनोज कुमार ने हिंदू धर्म के सामाजिक पक्षों, विषेषकर वर्ण व्यवस्था के जातीय पक्ष पर यह जायज-सा सवाल उठाया है कि क्या वर्ण व्यवस्था हिंदू धर्म का आवश्यक अंग है? यदि है तो फिर जाट, गूजर, कुर्मी रेड्डी, नायर आदि किस वर्ण में स्थान पाते हैं? इन्हें क्षत्रिय या किसी वर्ण में क्यों नहीं स्थान दिया गया? यही स्थिति भूमिहार और अन्य अनेक जातियों की भी है। अगर वर्ण व्यवस्था हिंदू धर्म का आवश्यक अंग है तो वे जिनका वर्ण नियत ही नहीं हुआ, क्या वे हिंदू नहीं हैं? वैदिक समाज में तो कर्म आधारित वर्ण विभाजन था। यह जातियों में कैसे रूढ़ हो गया? ऋग्वेद में शूद्र वर्ण का विवरण नहीं है। उसमें जातियां भी नहीं हैं, फिर जातियों का इतना प्रभुत्व हो जाना धर्मसम्मत कैसे हुआ? जो अपना विस्तार नहीं कर सकता, अन्य समाजों को सम्मिलित नहीं कर सकता, वह धर्म संपूर्ण दक्षिण क्षेत्र, सुदूर पूर्व श्रीविजय साम्राज्य एवं पश्चिम में गांधार तक आखिर फैला कैसे? ऐसे बहुत से सवाल धर्माधिकारियों से बनते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। फिर समझ आता है कि दरअसल जवाब देने वाला ही कोई नहीं है। ऐसा लगता है कि सनातन धर्म के उदात्त एवं समावेशी विचारों के बावजूद हमारे धर्म के नियंता इन सवालों के जवाब देने को तैयार नहीं हैं। आवश्यक यह है कि समाज स्वयं निर्णय ले, क्योंकि अगर कुछ नहीं किया गया तो जातीय विषमता की नागिन हमारे राष्ट्र को अनंतकाल तक डसती रहेगी।
जातियों के विभाजन का समापन एकात्म भारत की प्राथमिक जरूरतों में से एक है। सवाल फिर आता है कि नेतृत्व के अभाव में समाज यह निर्णय ले तो कैसे ले? जातियां अपने-अपने नेता बना रही हैं। जातीय पंचायतों में कहीं मोबाइल, कहीं जींस, कहीं डीजे आदि प्रतिबंधित करने जैसी कार्रवाईयां हो रही हैं। चूंकि पंचायतें जातीय हैं इसलिए वे सामाजिक विभाजन की विभीषिका को संबोधित भी नहीं कर सकतीं। विभिन्न् समाजों को जमीनी सच्चाइयों को स्वीकार करते हुए स्वयं के बनाए दायरों को ताेडना होगा। प्रत्येक व्यक्ति, परिवार और समाज का दायित्व है कि अपने परिवेश को परिवर्तित करने का प्रयास करे। हमारा ‘लक्ष्य सामाजिक ऊर्ध्वगामिता की दिशा में होना चाहिए। अगर हम दलित, आदिवासी अथवा पिछड़े समाज के अंग हैं तो सीमाओं को ध्वस्त करते हुए आगे चलें। सामाजिक एकीकरण की शुरुआत कहीं से तो करनी ही होगी। एकीकरण की प्रक्रिया के प्रस्थान बिंदुओं की कमी नहीं।
हिंदू खत्री एवं सिख अलग धर्म में हैं, लेकिन उनके बीच शादी-विवाह एक सामान्य सी बात है। एक धर्म के अंदर की जातियों में तो कोई समस्या ही नहीं होनी चाहिए। महानगरों में जातीय वर्जनाएं टूट रही हैं। युवाशक्ति में बदलाव की सोच प्रबल है। हमारे महानगर विकास के साथ जातीय दीवारों को तोड़ने का भी कार्य कर रहे हैं। नगरीकरण का विस्तार भी इस सामाजिक समस्या को समाधान देता है। राजा राममोहन राय और ब्रह्म समाज आंदोलन द्वारा बंगाल में जातीय विभाजन के समापन की दिशा में किया गया कार्य संपूर्ण देश के लिए आदर्श है। आज बंगाल में कुलीन कायस्थों और ब्राहमणों में प्राय: विवाह हो रहे हैं। मुखर्जी, गांगुली एवं बोस, मजूमदारों आदि भिन्न् जातियों में विवाहों पर बंगाल का सुसंस्कृत समाज आपत्ति नहीं करता। शिक्षा संस्कार का महत्व जातियों से अधिक है। इसी कारण बंगाल के चुनावों में जातियां गौण हैं। परंपरागत लीक से हटकर समाज के एकीकरण, समरसता का वातावरण बनाने का समय हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। कभी स्वामी श्रद्धानंद ने इस दिशा में महती प्रयास किया था। आर्य समाज का तो लक्ष्य ही इन सामाजिक विसंगतियों के समापन का था। हालांकि दलित समाज में वर्जनाएं कायम हैं, फिर भी बौद्ध सभाएं इस दिशा में प्रयास कर रही हैं एवं अनुसूचित समाज की प्रमुख जातियों विशेषकर जाटव, पासी आदि में आपसी विवाहों की संख्या बढ़ रही है। जातीय रूढ़ता के विरुद्ध अगर समग्र समाज नहीं, तो कम से कम समानधर्मी जातियों के एकीकरण की बात तो की जा सकती है। क्यों न समान पेशा और समान सामाजिक-आर्थिक हैसियत वाली अधिकाधिक जातियां एकीकरण की दिशा में आगे बढ़ें? ठीक वैसे ही जैसे उत्तर प्रदेश में क्षत्रिय एवं कुर्मी समाज के सामाजिक सामंजस्य के लिए क्षत्रिय-छत्रपति मंच के जरिए एक पहल हुई। सामाजिक रूप से दोनों समाजों में काफी निकटता है। दोनों को मिलाकर शक्ति और कर्मठता का एक संयुक्त क्षेत्र बनता है। छत्रपति शिवाजी और सरदार पटेल से प्रेरित कुर्मी समाज क्षत्रिय समाज के साथ सामाजिक संबंधों की दिशा में चल सकता है। ऐसा ही अन्य जातियों के बीच भी हो सकता है। ऐसा होने पर दहेज की विभीषिका से निपटना आसान हो सकता है। जातीय बंधन इस समस्या को और विकट बना रहे हैं।
यथास्थितिवादी सोच नई जमीन नहीं तोड़ती, वरन विषमताओं को आश्रय देती है। ऐसी सोच खंडित देश में भी अपना भविष्य खोजने लगती है। यथास्थितिवाद की सुविधाजीवी सोच कभी राष्ट्र निर्माण का बीड़ा नहीं उठाती। बंगाल का क्रांतिधर्मी उदाहरण सामाजिक एकीकरण की मुहिम में एक प्रकाश स्तंभ के समान है। जातियां रहेंगी तो ऊंच-नीच की भावना भी रहेगी। जातीय बाधाएं राष्ट्र की रचनात्मक शक्ति का अपव्यय करती हैं। राष्ट्रीय एकीकरण के यज्ञ की पूर्णाहुति तब होगी, जब समाज जातीय विभाजन को ध्वस्त कर वृहद सामाजिक एकीकरण की दिशा में बढ़ेगा।
चीन से रिश्ते सुधारने की नई पहेली
हर्ष वी पंत, प्रोफेसर, किंग्स कॉलेज लंदन
जिस वक्त हम सोच रहे थे कि भारत अपनी चीन-नीति को पटरी पर ला रहा है, दरअसल हम उन दिनों में लौट चुके थे, जब चीन के साथ हमारे रिश्ते बेहतर हुआ करते थे। खबर है कि आगामी 1 अप्रैल को नई दिल्ली में आयोजित ‘थैंक यू इंडिया’ कार्यक्रम से सरकारी अधिकारियों को दूरी बरतने की बात कहते हुए विदेश सचिव विजय गोखले ने कैबिनेट सचिव को पत्र लिखकर कहा है कि ‘चीन के साथ भारत के रिश्तों के लिहाज से यह समय बहुत संवेदनशील होगा। लिहाजा केंद्र सरकार के मातहत हों अथवा राज्य सरकार के, वरिष्ठ नेताओं या सरकारी अधिकारियों का इसमें शामिल होना उचित नहीं है और इसे रोका जाना चाहिए’। मालदीव में भी नई दिल्ली ने यही तय किया था कि अपने हितों पर जोर देना चीन को उकसाने जैसा होगा, और इसी के बाद अपने कदम पीछे खींचकर चीन को आगे बढ़ने का मौका दिया गया। दिल्ली में भी एक थिंक टैंक को महज इस तर्क पर अपना एक वार्षिक सम्मेलन करने से रोक दिया गया था कि वहां होने वाली चर्चा चीन को नाराज कर सकती थी।
विदेश सचिव गोखले पिछले महीने बीजिंग में थे, जो जाहिर तौर पर संबंधों को ‘री-सेट’ करने के लिए एक तयशुदा यात्रा थी। उसी का यह नतीजा है कि सरकारी स्तर पर बातचीत का एक कैलेंडर तैयार हुआ और संभवत: जल्द ही हमें चीन से कोई उच्च-स्तरीय दौरा भी देखने को मिले। सोच यही है कि पिछले साल डोका ला विवाद ने नई दिल्ली के लिए जो कुछ प्रतिकूल हालात पैदा किए हैं, उसके बाद चीन की नाराजगी को शांत करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए जाने की जरूरत है। इसीलिए भारत ने अपने तईं अतिरिक्त प्रयास करने का फैसला किया है और तिब्बत का मसला जाहिर तौर पर इसमें बाधक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जून में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक के लिए चीन जाने वाले हैं। नई दिल्ली यह मानती है कि चीन की भावनाओं का सम्मान करके ही वह इस दौरे को सफल बना सकती है। आकलन यह भी है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीफ) ने जब आतंकियों की आर्थिक मदद करने के कारण पाकिस्तान को ग्रे-सूची में डाला था, तो चीन ने उसका विरोध नहीं किया था। इसीलिए नई दिल्ली भी बीजिंग के उस रुख का सम्मान करते हुए मेल-मिलाप की सोच रही है।
हालांकि तिब्बत मसले से दूरी बरतना भारत के लिए नई बात नहीं है। नवंबर 2007 में भी तत्कालीन कैबिनेट सचिव ने सभी मंत्रियों को एक खत भेजा था, जिसमें उनको दलाई लामा की ओर से गांधी शांति प्रतिष्ठान द्वारा आयोजित कार्यक्रम से दूर रहने की सलाह दी गई थी। तब यह कयास लगाए गए थे कि तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह संभवत: वाम दलों की नाराजगी शांत करना चाहते हैं, जो भारत की विदेश नीति के वाशिंगटन की ओर झुकने से खफा थे। उस समय कम्युनिस्ट पार्टियां सत्तारूढ़ गठबंधन का हिस्सा थीं और प्रधानमंत्री यह संदेश देना चाहते थे कि नई दिल्ली अब भी भारत-चीन रिश्ते को सर्वोच्च महत्व देती है। तब यह भी कहा गया था कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के सफल दौरे के लिए भारतीय हुकूमत चीन का शुक्रिया अदा करना चाहती है। कुछ मीडिया रिपोट्र्स की मानें, तो उस यात्रा के दौरान चीन ने यह जाहिर किया था कि वह भारत-अमेरिका परमाणु समझौते को लेकर अनुकूल रुख रखता है। तब उस समझौते के लिए नई दिल्ली और वाशिंगटन में बातचीत ही चल रही थी।
मंशा जो भी हो, लेकिन तब भी और आज भी, नई दिल्ली का यह व्यवहार लंबे अरसे से कायम भारत के उस रुख के प्रतिकूल लगता है कि दलाई लामा महज राजनीतिक विद्रोही नहीं, बल्कि देश में व्यापक स्तर पर सम्मानित एक आध्यात्मिक गुरु भी हैं। फिलहाल नई दिल्ली ने इस मसले पर जो रुख अपनाया है, उसे लेकर कई क्षेत्रों में उसकी आलोचना भी होगी। साथ ही, यह खतरा भी है कि भारतीय प्रशांत क्षेत्र में इसका गलत संदेश जा सकता है। इस क्षेत्र में शक्ति संतुलन बनाने के लिए ही तो हमने गणतंत्र दिवस के मौके पर आसियान देशों के शासनाध्यक्षों को बतौर मेहमान बुलाया था। इसके साथ ही पिछले कुछ समय में हमने अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर चतुष्कोणीय गठजोड़ की ओर भी कदम बढ़ाए हैं। इस चतुष्कोणीय गठजोड़ को चीन की सक्रियता पर लगाम लगाने की नजर से भी देखा जाता रहा है।
लिहाजा चीन के प्रति भारत के रुख में आया यह व्यापक बदलाव बहुत से लोगों के लिए हैरत में डालने वाला है। क्या इसमें कोई अन्य कूटनीतिक खेल है, जिसके बारे में अनुमान लगाना अभी शायद मुश्किल है या यह सब सिर्फ इसलिए है कि चीन भारत से ठीक तरह से वार्ता करे या फिर नई दिल्ली जून में मोदी के दौरे से कोई ठोस नतीजे निकालने को लेकर काम कर रही है? सवाल यह भी है कि क्या भारतीय जनता पार्टी साल 2019 के चुनाव से पहले चीन से कोई नाराजगी नहीं मोल लेना चाहती या मीडिया में आक्रामक बयानों के बावजूद हमारे सेनानायक सरकार को कुछ गंभीर नतीजे का संकेत दे रहे हैं?यह सही है किभारत और चीन के रिश्ते का प्रबंधन कुशल तरीके से होना चाहिए, लेकिन चीन की तरफ से आने वाली वास्तविक या आभासी चिंताओं को देखते हुए कदम उठाना आपसी रिश्तों को कोई स्थायित्व नहीं दे सकेगा। इसमें एक खतरा यह भी है कि इससे चीन की विस्तारवादी नीति को ही प्रश्रय मिलेगा। यह सच है कि पुरानी आदतें जल्द पीछा नहीं छोड़तीं, लेकिन यह उम्मीद भी की जानी चाहिए कि भारत ने अपनी पुरानी गलतियों से सबक जरूर सीखा होगा।
Hadiya’s Freedom
It is to be celebrated. But that it came so close to being taken away from her must serve as a warning.
Editorial
Can a 24-year-old woman live and marry according to her wishes, even if that means defying her family and community? The Constitution of India’s answer is an unambiguous yes — an individual’s freedom is among the first principles and guarantees of democracy.
The Supreme Court of India on Thursday upheld this right by striking down a Kerala High Court order of May 2017 that had annulled the marriage of Hadiya, formerly Akhila Asokan, to Shafin Jehan. A much welcome decision, indeed, but the question remains: Did it have to come to this? Did it have to take 10 months of being shuttled from court to court, of being incarcerated in her parental home against her wishes, of being separated from her husband, for Hadiya’s inalienable right to personal freedom to be affirmed?
For Indian women, especially, this has been a disquieting spectacle. They have watched the judiciary endorse a poisonous and patriarchal understanding of the rights of the family over a woman’s freedom. The Kerala High Court, while annulling Hadiya’s marriage, had observed that “a girl aged 24 years is weak and vulnerable, capable of being exploited in many ways” and that “marriage being the most important decision in her life, [it] can also be taken only with the active involvement of her parents”. One of the ways in which democratic institutions empower a citizen is by listening to her, and recognising the validity of her voice. Through the case’s progress, Hadiya had repeatedly and consistently maintained that she had converted to Islam of her own volition, and later married a Muslim man of her choice. Why did the courts then appear to struggle to listen to Hadiya, infantilised as a girl vulnerable to shadowy forces of “love jihad”, to acknowledge her rights to live the life she had chosen?
When in November last year, Hadiya was finally heard in the SC, she was released from her parental custody and allowed to carry on her studies. This order now sets her free to be reunited with her husband, even if an NIA investigation into alleged forced conversions will continue. This newspaper had argued that by putting Hadiya on trial — a woman who has broken no law, nor committed any crime — the courts had allowed a challenge to the fundamental rights guaranteed to India’s citizens. That challenge has been staved off and the SC has steered towards safer ground. Hadiya’s freedom is to be celebrated, but her tribulations should be a reminder to the judiciary of the dangerous course that it nearly embarked on.