
09-10-2020 (Important News Clippings)
To Download Click Here.
In defence of commons
Permission Raj looms over public spaces, right to protest. SC order on Shaheen Bagh fails to recognise this.
TM Krishna , [ Krishna is a musician and author of Sebastian and Sons: A Brief History of Mrdangam Makers.]
For people living in the city of Chennai or followers of Tamil cinema, the word poromboku is not new. An often-heard abuse, it is used to shame an individual, implying that he is good for nothing, useless, unproductive, and valueless. In reality, poromboku is a beautiful expression; a word that means “the commons” referring to everything that we — as a society — own collectively and share with one another. Rivers, lakes, grazing lands, mangroves, marshlands and forests are poromboku. In the context of the urban, it is our streets, parks, beaches, graveyards and playgrounds that all of us have free access to. These spaces are not privately owned and, in a democratic country, everyone irrespective of religion, caste, gender or even nationality, participates in their use. But we also know that this is not entirely true. More often than not, the commons are guarded by religious bigots, caste armies, or the moral police. Yet, we fight doggedly for our shared rights hoping to push back the parochials.
Shaheen Bagh stands tall as a battleground to save our poromboku. But the commons that the women protesters and friends in Shaheen Bagh fought for were not spatial — they were abstract. They were the foundations on which we have built our entire nation. Equality, equity, fundamental rights, liberty, justice and secularism are our shared conceptual poromboku-s. They are not the private properties of a single individual living in this land; neither are they owned by the executive or judiciary. These are the principles of our democracy that we cherish and the values that we defend. The Shaheen Bagh protests were necessary to push back a government that is bent on demolishing our constitutional soul, using every Machiavellian trick in the book.
But the question often asked is whether such protests are also a public nuisance to those who do not share the same opinion or just want to go ahead with their everyday routine. This is a fair question, but needs a nuanced response. Society is not a level-playing field and every institution, including the judiciary, does not treat every protest with the same yardstick. Hence, public order and social tranquillity are not objective notions and are often manipulated by the state.
While the argument that public movement and normal life should not be affected by protests has value, how can we not factor in the utter inequality in the way every institution views public protest and protesters? Within this labyrinth lies social discrimination. Public protests or processions by Dalits, minorities, women, trans people are viewed with disdain but none will dare question protests by powerful caste lobbies, political parties or the religious majority.
The incongruencies do not stop here. In every city, we are asked to obtain police permission for a protest. Inevitably, if the protest is against the government, police or any state institution, the permission is rejected or delayed until the very last moment forcing the organisers to cancel or rush to the court for relief. Constantly challenging the police in the courts is tiresome, leading citizens to just give up. In effect, protests are crushed by the state.
The courts do not seem to be interested in addressing this serious countrywide use of permission raj. It is not just protests; we struggle to obtain permission even for performances in public spaces. The police informally question us about the content of the plays or songs. On one occasion in Chennai, the Casteless Collective band was forced to stop singing a song because it contained the word “Modi”. Since the jallikattu protests of 2017, there is a blanket denial for permission for any gathering at Chennai’s famed Marina beach. “Maintenance of law and order” is used by the state to stifle public questioning. At the very same time, large corporations buy their way into public spaces, erect stages, hoardings and destroy the environment with impunity and without a whimper from our public bodies. Does the esteemed court expect us to come to its doorstep every time these things happen?
Even the idea of designated locations for protest needs to be challenged. Who designates these spaces and on what basis? In a country like India, where the political class does not appreciate being questioned, especially when in power, how does the court expect any fairness in protest space allocations? The consideration will always be: How can we limit its growth, effect and keep it under our control? There is little value in speaking about public inconvenience without addressing the limitations that are placed on our right to protest.
It is also essential to realise that protesting is often a spontaneous act and cannot be bottled by allocations and permissions. A vital quality of protest is public awareness and participation; consequently, public roads cannot be off-limits. Unless we are shaken awake from our slumber by slogans, cheers, demands, songs and hundreds walking the streets, those of us who complain of disruption will never notice the farmer or labourer.
Yes! We are now a democratic country; yet how can we be blind to the lack of freedom and independence and the pervading fear in the hearts of so many? The state is an enormously powerful machine and, in order to force a just response, common people need to apply collective pressure. In this tussle, public spaces are crucial to empower people, make them heard, and bring some parity into the discourse. Therefore, the occupation of highways by citizens whose lives have been torn apart by sexual, corporate and political violence is an important tool and to treat it as a public annoyance is majoritarian browbeating.
There is no doubt that social media plays a huge role in bringing people together and giving power to the collective. But unless public spaces are freely available for demonstrations, we will remain a mute democracy. The Supreme Court had the opportunity to expand the contours of its order keeping in mind reality with all its unevenness, but it remained silent and forgot that democracy thrives in the poromboku!
Scissoring the DNA
The huge potential of the gene-editing tool decided the chemistry Nobel
Editorial
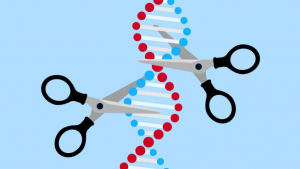
That scientists who pioneered the revolutionary CRISPR-Cas9 gene-editing technology, the biggest game-changer in biology in recent years, will win the Nobel Prize was never in doubt; it was only a question of when and who would get recognised for the work done to develop the tool. The Prize awarded to Emmanuelle Charpentier and Jennifer A. Doudna, just eight years after they developed the tool, has finally ended the speculation of who would win it. But most importantly, this year’s Prize for chemistry has created history by honouring an all-woman team. It all started when Dr. Charpentier discovered an RNA molecule that is part of bacteria’s ancient immune system — CRISPR-Cas — wherein clustered repeated sequences produced by bacteria can remember and destroy viruses by cleaving their DNA. Teaming with Dr. Doudna, she recreated the bacteria’s genetic scissors in a test tube and simplified the tool to make it easier to programme the system to precisely cut specific sites of interest in any DNA, including humans. While the tool is most often used to make a cut in the DNA, newer approaches are being attempted to add or make minor changes to the DNA. All these approaches may at some time in the future make it easy to “rewrite the code of life”.
The gene-editing technology has opened up a vast window of opportunity. In the last six years, the tool has enabled scientists to edit human DNA in a dish and early-stage clinical trials are being attempted to use the tool to treat a few diseases, including inherited disorders/diseases and some types of cancer. Though in 2016 China began the first human clinical trial to treat an aggressive form of lung cancer by introducing cells that contain genes edited using CRISPR-Cas9, the use of the tool has so far been limited to curing genetic diseases in animal models. Last year, a Chinese researcher used the tool to modify a particular gene in the embryo to make babies immune to HIV infection, which led to international furore. Though no guidelines have been drawn up so far, there is a general consensus in the scientific and ethics communities that the gene-editing technique should not be used clinically on embryos. Unlike in the case of humans, the tool is being extensively used in agriculture. It is being tried out in agriculture primarily to increase plant yield, quality, disease resistance, herbicide resistance and domestication of wild species. The huge potential to edit genes using this tool has been used to create a large number of crop varieties with improved agronomic performance; it has also brought in sweeping changes to breeding technologies. The gene-editing tool has indeed taken “life sciences into a new epoch”.
बुनियादी ढांचे के विकास को मिले रफ्तार
जीएन वाजपेयी ,(लेखक सेबी और एलआइसी के पूर्व चेयरमैन हैं)

चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के आंकड़े सामने आने के बाद तमाम संस्थाओं ने भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर आशंकाएं व्यक्त करना शुरू कर दिया। समीक्षाधीन तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर में 23.9 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। इस पर अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, एशियाई विकास बैंक और आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन जैसी संस्थाओं के अलावा स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, मूडी और फिच जैसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों और तमाम दिग्गज अर्थशास्त्रियों ने यही अनुमान व्यक्त किया कि चालू वित्त वर्ष भारत की जीडीपी वृद्धि दर में आठ से 16 प्रतिशत तक की गिरावट आ सकती है। भले ही गिरावट का जो स्तर रहे, लेकिन इससे यही बात जाहिर होगी कि कई वर्षों तक तेज आर्थिक वृद्धि के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था को गिरावट की तपिश झेलनी होगी। तीन दशक तक जोरदार वृद्धि ने लाखों-करोड़ों लोगों को गरीबी के दुष्चक्र से बाहर निकाला है। गिरावट की यह स्थिति अप्रत्याशित आकस्मिक कारणों के चलते उत्पन्न हो रही है। सरकार जीवन, आजीविका और अर्थव्यवस्था के लिए उत्पन्न हुए जोखिम को दूर करने की दिशा में सक्रिय है। अर्थव्यवस्था को पहुंचे भारी नुकसान की तीव्रता का नाता काफी हद तक देश की राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक मोर्चे से जुड़ी ढांचागत विशेषताओं से भी है। अक्लमंदी इसी में है कि नुकसान को कम से कम कैसे किया जाए। इस सिलसिले में मोदी सरकार द्वारा उत्साह और उपयोगिता की दृष्टि से किए जा रहे विभिन्न ढांचागत, क्रमबद्ध और संस्थागत सुधारों का भी संज्ञान लिया जाना चाहिए। नरसिंह राव और वाजपेयी सरकार को जिस किस्म की चुनौतियां झेलनी पड़ी थीं, मौजूदा वक्त भी कुछ उसी किस्म का है, जो अर्थव्यवस्था के लिए दूरगामी सुधारों की मांग कर रहा है। ये सुधार राजनीतिक रूप से संवेदनशील भी हैं। भूमि, श्रम और पूंजी जैसे उत्पादन के तीनों पहलुओं से जुड़े ये सुधार उत्पादकता को बेहतर बनाएंगे। इनसे आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत प्रतिस्पर्धी बढ़त की स्थिति भी बनेगी।
फिलहाल अर्थव्यवस्था मांग, आपूर्ति, निवेश और सकल पूंजी निर्माण जैसे सभी पहलुओं पर चुनौतियों से दो-चार है। इन सबसे निपटने के लिए राजकोषीय गुंजाइश का भी अभाव है। विकसित अर्थव्यवस्थाओं के उलट भारत सरकार राजकोषीय घाटे को लेकर एक हद से अधिक उदार नहीं हो सकती, परंतु उसका बढ़ना तय है। इसका समाधान विकास के सभी माध्यमों को गति देने में ही निहित है। लोग अनिश्चितताओं के चलते खरीदारी के लिए अभी भी बाहर निकलने से कतरा रहे हैं। एक तो उन्हें कोरोना संक्रमण का खतरा है। दूसरे, आय में अनिश्चितता को लेकर भी वे खर्च करने से सकुचा रहे हैं। सरकार ने गरीबों के खाते में जो रकम जमा कराई है, वह भी बैंकों में जमा राशि का स्तर ही बढ़ा रही है। ऐसे में वास्तविक ग्राहक माने जाने वाले निम्न एवं निम्न मध्यम वर्ग के मन में रोजगार को लेकर जो आशंकाएं घर कर गई हैं, उन्हें बाहर करना होगा।
गुणवत्तापरक बुनियादी ढांचे का अभाव भी भारतीय अर्थव्यवस्था को धार देने की राह में एक बड़ा अवरोध है। बेरोजगारी का बढ़ता दायरा भी सामाजिक असंतोष को हवा दे रहा है। संप्रति आधुनिक मौद्रिक सिद्धांत यानी एमएमटी का सहारा लिया जा रहा है। इसमें अर्थव्यवस्थाओं को सुरक्षित रखने के लिए बड़े पैमाने पर प्रोत्साहन पैकेज दिए जा रहे हैं। इसका यही पैमाना है कि अगर अर्थव्यवस्था में शिथिलता महसूस हो तो राजकोषीय घाटे का आकार कोई मायने नहीं रखना चाहिए। साथ ही यदि नॉमिनल जीडीपी वृद्धि देय ब्याज दर से अधिक है तो ऋण राशि किसी समस्या का सबब नहीं होनी चाहिए। भारतीय अर्थव्यवस्था में भारी शिथिलता व्यापक बेरोजगारी, अल्प-बेरोजगारी और क्षमताओं का पूरी तरह उपयोग न होने में प्रतिबिंबित हो रही है। सड़कों, बंदरगाहों, हवाई अड्डों, रेलवे, सार्वजनिक आवास, अस्पताल और स्कूल जैसी तमाम परिसंपत्तियां विकसित करने में इसे भुनाया जाना चाहिए।
वास्तव में इस समय केंद्र सरकार बुनियादी ढांचा विकास के कार्य को पूरी गति से आगे बढ़ाए, भले ही इसके लिए नई मुद्रा ही क्यों न जारी करनी पड़े। सरकार प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार की पेशकश करे। यहां तक कि मनरेगा के तहत होने वाले मामूली से कामों के बजाय उसे बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं से भी जोड़ा जा सकता है। ऐसा करके अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों को तत्काल राहत मिलेगी और आर्थिक अनिश्चितता के बादल छंटेंगे। वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग भी बढ़ेगी। साथ ही साथ इससे लाखों एमएसएमई को जीवनदान मिलेगा। वहीं अर्थव्यवस्था की संभावित वृद्धि को न केवल सहारा, बल्कि तेजी भी मिलेगी।
जहां तक प्रमुख देशों के राजकोषीय घाटे का सवाल है तो वर्ष 2020 में अमेरिका का राजकोषीय घाटा बढ़कर उसकी जीडीपी का 15.3 प्रतिशत, ब्रिटेन का 18.2 प्रतिशत, कनाडा का 12.6 प्रतिशत, जापान का 11.3 प्रतिशत और सिंगापुर का 13.6 प्रतिशत रहा। इन सभी देशों में अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए अतिरिक्त संसाधनों के आवंटन की संभावनाएं अभी भी कायम हैं। अमेरिकी केंद्रीय बैंक के चेयरमैन जेम्स पॉवेल का कहना है कि अर्थव्यवस्था को सहारा देने की कोशिशें रोकी नहीं जाएंगी और ब्याज दरें तब तक नहीं बढ़ाई जाएंगी, जब तक पूर्ण रोजगार की स्थिति बहाल नहीं होती या महंगाई बर्दाश्त के बाहर नहीं चली जाती। यूरोपीय आयोग भी 825 अरब डॉलर के कोरोना राहत पैकेज की तैयारी कर रहा है।
भारत की बात करें तो देश के प्रत्येक राज्य, जिले और शहर में बुनियादी ढांचे की स्थिति कमजोर ही है। ऐसे में सभी को रोजगार दिया जाए और बुनियादी ढांचे से जुड़ी बड़ी परियोजनाएं विकसित की जाएं। कहने का अर्थ यह भी नहीं कि सभी किस्म की सावधानियों को दरकिनार ही कर दिया जाना चाहिए। इसमें सफलता इसी पहलू से तय होगी कि इन परियोजनाओं को कितनी तेजी से फलीभूत किया जाएगा और इनमें संसाधनों के रिसाव को कैसे रोका जाएगा। इन दोनों मोर्चों पर मोदी सरकार ने उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है। हालांकि इस राह में जोखिम कम नहीं हैं, लेकिन उन्हें उठाना ही श्रेयस्कर होगा। कोई वैकल्पिक रणनीति बेहतर परिणाम नहीं दे सकती।
मजदूरों और देश की दशा संवारने वाले सुधार
वरुण गांधी, भाजपा सांसद
मुंबई के लोअर परेल में अपनी चॉल के बाहर बैठे गणेश देसाई की पुरानी यादें ताजा हैं। अंधेरी में अपनी चॉल से दादर के लिए लोकल ट्रेन पकड़ना और लोअर परेल में टेक्सटाइल मिल में काम पर जाना। वहां कानूनी सीमा के बावजूद 12 घंटे से ज्यादा काम करना पड़ता था, लेकिन काम अच्छा चल रहा था। फिर उद्योग पर बुरा समय आया और छंटनी हो गई। देसाई कहते हैं, 1970 के दशक में बॉम्बे भारत को कपड़ा पहनाता था। मैन्युफैक्र्चंरग सेक्टर से बहुत उम्मीदें थीं। यह देश के लिए रोजगार का मुख्य आधार माना जाता था, लेकिन 1970 के दशक की शुरुआत से 1980 आते-आते इस सेक्टर का जोश चुक गया, खासतौर से टेक्सटाइल के मामले में। इस पतन के साथ भारत के कई बडे़ शहरों की चमक खत्म हो गई और उनमें से कुछ नए सांचे में ढल गए।
1980 में मुंबई में संगठित मजदूर शक्ति का जोर चलता था, खासतौर से मशहूर (और अब वीरान) टेक्सटाइल मिलों में। 1980 तक मुंबई के मध्य क्षेत्र में तकरीबन 2.50 लाख कपड़ा मिल मजदूर थे। मजदूर यूनियन लीडर दत्ता सामंत के नेतृत्व में 18 जनवरी, 1982 को शुरू हुई विशाल बॉम्बे टेक्सटाइल हड़ताल 65 से अधिक टेक्सटाइल मिलों के कामगारों की मजदूरी बढ़ाने, बदली कामगारों को नियमित करने और बोनस के लिए की गई थी। 18 महीने तक चली उस हड़ताल से कई मिलें बंद हो गईं, मालिकों ने दूसरे शहरों, प्रांतों में प्लांट लगा लिए, एक लाख कामगारों की छंटनी हो गई। साल 1995 तक शहर में सिर्फ 80,000 कपड़ा मजदूर बचे थे। एक बड़ा औद्योगिक शहर इतिहास में गुम हो गया और उसकी जगह सेवा आधारित अर्थव्यवस्था ने ले ली।
गौतम गौड़ा का मामला देखें, जो अब मुंबई के भोईवाड़ा में रहते हैं, तो 1990 के दशक की शुरुआत में छंटनी के बाद उन्हें बच्चों की पढ़ाई छुड़ाने को मजबूर होना पड़ा था। किसी तरह से चौकीदार या कुली बनकर जिंदगी आगे बढ़ी। आदर्श स्थिति तो यह होती कि भारत के श्रम कानून ऐसे लाचार मजदूरों के हाल पर विचार करते। एक प्रबल राय है कि श्रम कानूनों की भरमार के कारण हमने काफी कुछ गंवाया है। कर्मचारियों की संख्या छह से बढ़कर सात होते ही ट्रेड यूनियन कानून लागू हो जाता है, जो श्रमिक संगठन के गठन की अनुमति देता है। ऐसे कानून से उलटे नतीजे आते हैं, क्योंकि ये उद्यम के विस्तार से बचने और छोटे उद्यम बने रहने के लिए प्रोत्साहन देते हैं। ये कानून भारत जैसे विशाल श्रम बल वाले देश को श्रम का लाभ लेने से रोकते हैं। ऐसे श्रम कानूनों का असर मिला-जुला ही रहा है।
श्रम कानूनों में राज्यों ने भी अपने स्तर पर खूब संशोधन किए हैं। औद्योगिक विवाद अधिनियम में राज्यों ने साल 1995 तक लगभग 113 संशोधन कर दिए थे। टिमोथी बेसली और रॉबिन बर्गीस का अध्ययन इस पर रोशनी डालता है, नियोक्ता-पक्षीय राज्यों में मैन्युफैक्चरिंग में वृद्धि श्रमिक-पक्षीय राज्यों की तुलना में अधिक थी। अगर 1960-95 की अवधि में औद्योगिक विवाद अधिनियम में नियोक्ता-पक्षीय संशोधन नहीं होते, तो आंध्र प्रदेश में शहरी गरीबी का स्तर 1990 के वास्तविक स्तर से 112 प्रतिशत से भी ज्यादा होता। हमारी श्रमिक नीतियों से श्रमिक कल्याण के मामले में पर्याप्त नतीजे नहीं मिले हैं और भारत में निवेश भी प्रभावित हुआ है।
श्रम सुधार के लिए राजनीतिक साहस चाहिए और पिछले दो वर्षों में सरकार ने सुधार शुरू किए हैं। कोड ऑफ वेजेज, 2019 ने मजदूरी और भत्ते संबंधी चार कानूनों को एकीकृत कर दिया है। लैंगिक भेदभाव को रोकते हुए वार्षिक बोनस, भुगतान का तरीका, ओवरटाइम का प्रावधान कर देश भर में न्यूनतम मजदूरी को परिभाषित किया है। स्वतंत्र ठेकेदार, फ्रीलांसर, घर से काम करने वाले कर्मचारियों और अनौपचारिक क्षेत्र के कामगारों तक कानून का विस्तार किया गया है। अब एक फर्म को सिर्फ चार लेबर रजिस्टर (12 से घटाकर) रखना होगा, और सालाना रिटर्न की संख्या भी सिर्फ एक (मौजूदा तीन से घटाकर) होगी।
अगर इन सुधारों को ठीक से लागू किया जाता है, तो कंपनियों को चीन से बाहर निकलने और भारत में रोजगार सृजित करने के लिए प्रोत्साहित करने का आधार तैयार होगा। भारत ने रोजगार सृजन के एक और युग निर्माण की दिशा में अपने कदम बढ़ा दिए हैं।
