
07-04-2025 (Important News Clippings)
To Download Click Here.
 Date: 07-04-25
Date: 07-04-25
IT’S NOT ABOUT WAQF
Protests are actually not about the new law at all. They are about a complete breakdown in trust between govt and Muslims. GOI must take the initiative to rebuild trust, no law is up to this task
R Jagannathan
Last week, the Waqf Amendment Bill 2025 was passed after two marathon days of debate in both houses of Parliament. There are now protests by some Muslim organisations in different parts of the country. Most opposition parties are backing these protests, and some opposition MPs have already petitioned the Supreme Court against the Bill. It is possible that these protests will fade out, but it is equally possible that they will linger on like the protests against the Citizenship Amendment Act.
Protesters say this legislation is unconstitutional since it tinkers with the rights guaranteed under Article 26 of the Constitution, which gives any religious group or denomination the right to “establish and maintain institutions for religious and charitable purposes; to manage its own affairs in matters of religion; to own and acquire movable and immovable property; and to administer such property in accordance with law.”
GOI justification for making changes to the existing Waqf Act is that waqf boards work non-transparently, which has led to many legal tangles, especially since boards could claim almost any property as waqf land. Religious and other properties belonging to non-Muslims were also at stake. Plus the Bill had support from segments of the Catholic community too.
A press release posted by the minority affairs ministry says: “While Waqf properties serve religious and charitable purposes, their management involves legal, financial, and administrative responsibilities that require structured governance. The role of waqf boards and Central Waqf Council (CWC) is not religious but regulatory, ensuring legal compliance and safeguarding public interest. By introducing checks and balances, empowering stakeholders, and improving governance, the Bill sets a progressive and fair framework for waqf administration in India.”
But the real issue is not the Bill at all. It is the near-complete breakdown of trust between GOI and India’s second-largest religious community. Question is, how is it possible for any govt to govern and maintain social harmony when this trust breaks down?
Remember CAA was not about Muslims in India either, but managed to rile them anyway. Today, whether or not the Waqf Bill improves the governance of waqf boards and CWC, large sections of Muslims are convinced that govt is out to get them. And no token gesture, like the Saugat-e-Modi kits given to minorities for Eid, is going to end this mistrust.
This mistrust is being fanned by opposition parties, which want to reap a block vote from the minorities in future elections. But this is no different from saying that BJP wants block votes from Hindus. If there is mistrust, it must be addressed. Tokenism is not going to change anything.
The untrusting state of affairs cannot be ended without moves towards a broader dialogue with Muslims (and Christians). But one must note that the underlying mistrust is between Hindus and minorities. GOI alone cannot end it, even though it is widely presumed that it is batting only for Hindu interests.
Consider the petitions asking for the release of Hindu temples from state control, especially in the south, which the Supreme Court sat on for more than a decade, and then lobbed back to high courts – Modi govt’s lawyer backed the idea. But perceptions cannot be changed that easily.
For starters, GOI should open a dialogue with organisations protesting the Waqf Bill. It can promise to incorporate any genuine demand that does not impact other communities or allows a waqf to relapse into mis-governance.
But what must follow is a broader dialogue between Hindu and Muslim organisations, where each community lays out its grievances and red lines more clearly. Agreements can be reached on the basis of give and take. Issues can range from cow protection to control of lynch mobs, recognition of Islamic iconoclasm, namaz on the streets, and the ethical limits to religious conversion activities. It is pointless to believe that law alone is enough to deal with a breakdown of trust when so many issues remain unresolved and the wounds of partition remain unhealed.
There is also a need for Muslims to introspect about why the community is so resistant to reform. Why does a community of more than 200mn – the third largest in the world – see itself as a victim in any and every situation.
Additionally, Muslims in India cannot presume that only what happens to minorities in India matters; their support for minorities in two neighbouring countries also matters. Many Hindus did not appreciate Muslim opposition to CAA. The Nehru-Liaquat pact was indirectly about ensuring this cross-country support to minorities. How can pluralism be protected in India, if the same cannot be protected in Pakistan, Bangladesh or even Kashmir Valley?
More importantly, if demography is changing in many states (Assam, Kerala, parts of Bengal and UP), it is the emerging Muslim majority in these regions that needs to reassure Hindus and other minorities about safety and security.
In India, majorities are legally decided statewise. But the average district in India has over 2mn population, and the largest district had a population of more than 11mn – Thane, now bifurcated, in 2011. Legal determination of majority and minority becomes irrelevant in areas where all-communities feel unsafe.
The issue, to repeat, is not the Waqf Bill. It is the growing mistrust between two communities. And the process of healing this rift must begin with GOI taking the initiative. Ultimately, the two communities concerned must work out a way to live in amity on the basis of compromise and goodwill. Mistrust cannot be left only to the law to fix.
In BIMSTEC, India’s A Bigger Stakeholder
ET Editorial
India has stepped up. The Bangkok Bimstec summit last week signalled the beginning of a new relationship for Bay of Bengal countries. As the region’s largest economy, India has an important role to make Bimstec work. A year after the charter came into force, focus is on connectivity, security and trade. New Delhi has rolled up its sleeves, announcing 20 initiatives. This suggests it’ll do its part to ensure Bimstec is not just another regional BRICS in the wall.
India is committed to its strategic involvement in the Indo-Pacific region, of which Bay of Bengal countries are key. Its presence in Bangkok, swift post-earthquake assistance to Myanmar, bilaterals with Thailand and Sri Lanka, and conversations on the sidelines with Bangladesh and Myanmar — including the deft handling of Muhammad Yunus’ controversial remarks on India’s northeast states — underscores that India has matured to play prime, but not overbearing, convener. China is the elephant in the room — especially given geopolitical volatility, Beijing’s continued forays in the neighbourhood, and provocative efforts to present China-India as a zero-sum game. This is more than focused engagement and well-meaning high-minded talk.
Zeroing in on digital and energy connectivity for regional development, enhancing physical connectivity, maritime focus for security and openness of the Indian Ocean, connecting UPI and payment systems of member states, exploring local currency trade… India is finally upping its game. Defence, energy and other agreements with Sri Lanka also underscore this. Its efforts in South Asia, the wider Bay of Bengal region and, earlier, in Southeast Asia give a new impetus to its ‘Neighbourhood First’ and ‘Act East’ policies. Reassuring, indeed.
Tragedy of a commons
Courts and the state must not throttle free flow of information
Editorial
While ordering the Wikimedia Foundation to undo changes on the Wikipedia page on Asian News International (ANI), the Delhi High Court said “people at large have a tendency to accept statements made on [Wikipedia’s] web pages … as gospel truth”. In the hearing of the defamation suit that ANI had filed in 2024, the court had taken some questionable positions. For example, it sought the identities of the volunteers who edited the ANI page, whose anonymity the platform allows to protect them from retaliation. When the Foundation sought more time, the court observed: “We will close your business transactions here… We will ask the government to block Wikipedia… If you don’t like India, please don’t work in India.” The Foundation had appealed for its right to safe harbour under the Information Technology Act 2000, but the court concluded in favour of the plaintiff because, it observed, “statements on the page pertaining to the plaintiff are all sourced from … editorials and opinionated pages”. Wikipedia is written and maintained by volunteers who are expected to follow the platform’s guidelines. Unlike newspapers or scientific journals, the encyclopedia does not purport to publish new information; volunteers are instead expected to repeat with attribution or reproduce with references, information originally published elsewhere, with a preference for reputable sources. In this light, the court order is problematic.
Elements of truth today are often mistaken to be someone’s opinions and vice versa. Politicians and government agencies have been known to punish civil society for repeating an allegedly offensive claim rather than address the original claim itself. Opinions are rejected even as data is withheld to deny those who express them opportunities to align them with verifiable facts. In this case, the court had expressed concern for ANI’s credibility, whether volunteers who edited the ANI page had followed the platform’s guidelines in letter and spirit, and whether the opinion as expressed on the page could be allowed to stand. In the process, it established that the Foundation’s ability to maintain the democratic structure that has allowed Wikipedia to become so popular and reliable is limited for India’s users: to the extent of public tolerance for certain opinions. Ultimately, the aforementioned “people’s tendency” and the state’s ability to influence it put Wikipedia and similar decentralised collaborations at risk. That is a tragedy. These collaborations adopted their designs to sidestep the sort of centralised information control that some countries, including India, have sought. Courts and the state would do well to accommodate these collaborative efforts rather than treat them with contempt — and the people should engage with these efforts and their guidelines as well.
Date: 07-04-25
A paradigm shift in mental health policy
Institutional responses to suicides are often individualistic and reductionist.
Sudarshan R. Kottai, [ is Assistant Professor, Department of Humanities and Social Sciences, IIT Palakkad ]
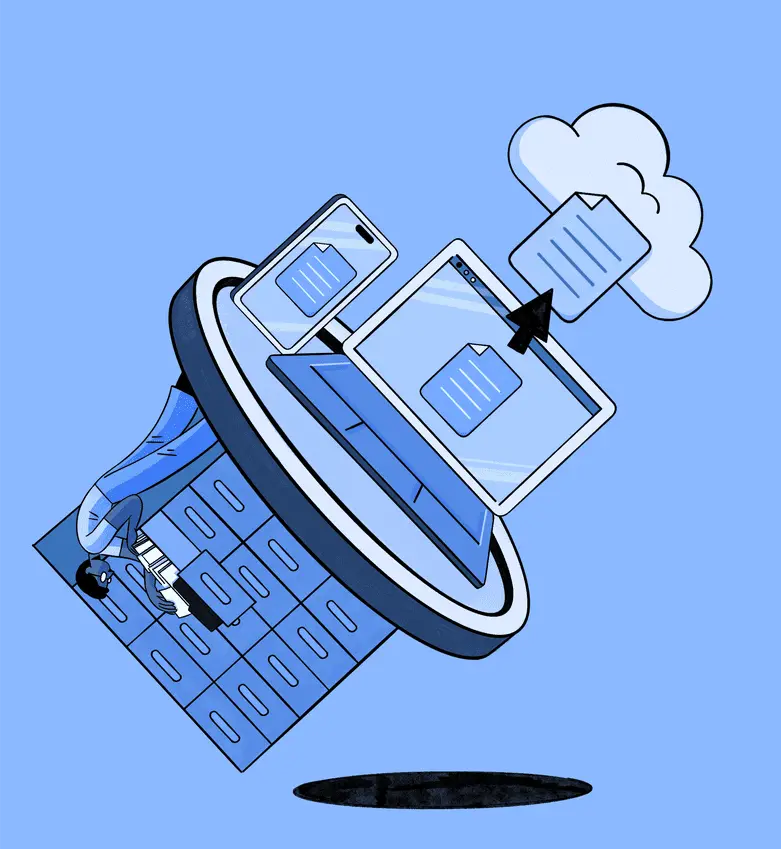
On March 24, the Supreme Court of India formed a National Task Force to prevent the increasing deaths by suicide of students on campuses. It also directed the Delhi Police to register an FIR on the complaints of the family members of two students who had died by suicide while studying at IIT Delhi in 2023. That year, following a spate of deaths by suicide, the IIT Council led by the Education Minister directed IITs to ensure ‘zero tolerance’ to discrimination and provide a robust support system to students.
The institutional response to suicide is often individualistic and reductionist — it is almost always to appoint more psychologists on campuses. The socio-structural determinants of mental health, such as discrimination and biased institutional policies, are almost always left unattended. Even though counselling centres are active at all IITs, with the goals ranging from “creating a suicide-free campus”, “creating a stigma-free and empathetic environment for issues related to mental health” to “creating a campus conducive to happiness and peace of mind for its residents”, psychologists refrain from calling attention to the biased institutional policies that impact mental health.
For example, none of the official websites of the counselling centres at the 23 IITs employ the phrase “queer affirmative” or use trans-inclusive personal gender pronouns. Language is not just a collection of words; it is action. Gender identities, sexualities, and inclusive practices are areas of human experience and action in which language, knowledge, and power intertwine. The way language is employed strongly influences thinking, which, in turn, affects the way people act, bringing power into the equation.
The gender-sexuality exclusionary language points towards non-compliance with the existing legal frameworks and Supreme Court rulings. For example, official forms where gender by default has only two options — male and female — violates equal rights for representation of gender non-binary people that was granted by the Supreme Courtin the 2014 NALSA judgment. In 2023, the Supreme Court launched the Handbook on Combating Gender Stereotypes, recognising the need to use unbiased language, which not only reflects the judge’s interpretation of the law, but also their perception of society.
Research has shown that pronouns are crucial linguistic resources for supporting trans and non-binary students and suggests strategies for a trans-affirming pedagogy such as collecting pronoun information and dealing with pronoun misuse. The deployment of gender pronouns signals identity-safety and promotes the perception that the institution is procedurally fair for sexual and gender diverse people. Using gender-inclusive pronouns and establishing inclusive frameworks and anti-discrimination policies are preventive public mental health care interventions that need to be prioritised as they de-escalate mental distress.
“Teachers talk only about grades. A grade is the parameter by which students are judged as good or bad,” a student said. This is antithetical to the ethic of care that honours and respects the value of just being human. The objective of the classroom should not only be confined to producing intellectual scholarship but also to cultivating compassionate, non-judgemental, and empathetic communities.
Fragile attendance policies implemented idiosyncratically by teachers pose serious challenges to mental health. In order to cultivate cultural safety and empathy in the classroom, it is important that teachers and students interact regularly. In the context of documented institutional discrimination and its fatal mental health impact, classrooms are to be nurtured as safe, kind, and democratic spaces. The current policies on mental health, limited to increasing mental health services, need a paradigm shift to a bottom-up approach focused on the classroom that maps various experiences and nurtures sensitivity to contexts and diversities. Teachers are pivotal in this regard.
It is a major crisis in public mental health ethics that psychologists align with counter therapeutic institutional policies that violate existing constitutional and statutory safeguards. Counselling centres have to mobilise all possible resources at multiple levels so that care becomes the central value. Similarly, embedding ethics of care into institutional policies to respond to avoidable mental distress to make every human life meaningful is more important than landing a human on the moon.
क्षेत्रीय संकीर्णता की राजनीति
संपादकीय
श्रीलंका की यात्रा से लौटकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ओर से रामनवमी के अवसर पर रामेश्वरम द्वीप को तमिलनाडु की मुख्य भूमि और रेलवे नेटवर्क से जोड़ने वाले पंबन पुल का उद्घाटन राज्य के साथ ही देश को मिलने वाली एक सौगात है। अपनी तरह के इस अनोखे समुद्री पुल का निर्माण तमिलनाडु के लिए बड़ी उपलब्धि और गर्व का विषय है।
यह देखना दुखद रहा कि इस अवसर पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने प्रधानमंत्री के साथ मंच साझा करना आवश्यक नहीं समझा। यह ठीक है कि राज्य सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर उनके एक मंत्री उपस्थित थे, लेकिन कोई भी समझ सकता है कि उन्होंने संकीर्ण राजनीतिक कारणों से ही इस कार्यक्रम से दूरी बनाई। यह और कुछ नहीं, सामान्य राजनीतिक शिष्टाचार का उल्लंघन ही है।
स्टालिन ने केवल प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों में अनुपस्थित रहना ही उचित नहीं समझा, बल्कि उन्होंने इस मौके पर परिसीमन का अपना पुराना राग भी फिर से छेड़ा। उन्होंने परिसीमन का मामला उठाकर फिर से यही सिद्ध किया कि वह केंद्र सरकार से एक ऐसे विषय पर तकरार करने के लिए उतावले हैं जिसका फिलहाल कोई औचित्य नहीं बनता।
परिसीमन की नौबत तो तब आएगी जब जनगणना होगी। स्टालिन परिसीमन की तरह से भाषा का मुद्दा भी उठाने में लगे हैं। यह तो बिल्कुल व्यर्थ का मुद्दा है, क्योंकि वह नई शिक्षा नीति के जिस त्रिभाषा फार्मूले का उल्लेख कर यह शोर मचा रहे हैं कि हिंदी थोपी जा रही है, उसमें तो हिंदी का कहीं कोई उल्लेख ही नहीं है।
स्टालिन जिस तरह से परिसीमन, भाषा और केंद्र की ओर से तमिलनाडु की कथित अनदेखी का मुद्दा उठा रहे हैं, उससे यदि कुछ स्पष्ट है तो यही कि वह अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखकर क्षेत्रवाद की संकीर्ण राजनीति करने में जुट गए हैं। देश के अधिकांश क्षेत्रीय दलों की यही समस्या है कि वे राजनीतिक और चुनावी लाभ के लिए क्षेत्रवाद को जानबूझकर हवा देते रहते हैं।
ऐसा करके वे यही प्रकट करते हैं कि उनमें राष्ट्रीय दृष्टि का अभाव है। राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर क्षेत्रीय संकीर्णता की राजनीति करने वाले स्वयं के साथ अपने राज्य की भी राष्ट्र की मुख्यधारा से दूरी बढ़ाते हैं।
यह अच्छा हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी ने स्टालिन की दुष्प्रचार की राजनीति की पोल खोलते हुए न केवल यह कहा कि आखिर वह और उनके सहयोगी अपने हस्ताक्षर तमिल भाषा में क्यों नहीं करते, बल्कि यह भी पूछा कि वह अपने राज्य के छात्रों को मेडिकल की पढ़ाई तमिल भाषा में करने की सुविधा क्यों नहीं दे रहे हैं। यह विचित्र है कि प्रधानमंत्री तो राष्ट्र की प्रगति में तमिलनाडु की भूमिका का उल्लेख करने में लगे हैं और स्टालिन क्षेत्रवाद की राजनीति को भड़काने का कार्य कर रहे हैं।
Date: 07-04-25
शोध और विकास की प्राथमिकता
आदित्य सिन्हा, ( लेखक लोक-नीति विश्लेषक हैं )
चीन की चमत्कृत करने वाली प्रगति में उसके दूरगामी सोच की अहम भूमिका रही है। चीन ने शोध एवं विकास यानी आरएंडडी में काफी पहले से निवेश करना आरंभ कर दिया था। इससे कम लागत में प्रतिस्पर्धी उत्पाद तैयार करने की उसने जो क्षमता हासिल की उससे वह वैश्विक विनिर्माण बाजार का सिरमौर बन गया।
चीन ने सरकारी स्वामित्व वाले उपक्रमों की व्यवस्था से नवाचार केंद्रित आर्थिकी की ओर कदम बढ़ाने आरंभ किए। इसका परिणाम हुआवे, अलीबाबा और बीआइडी जैसी दिग्गज कंपनियों के रूप में सामने आया। ऐसी कंपनियों की सूची अंतहीन दिखती है। चीन अपनी जीडीपी का 2.6 प्रतिशत आरएंडडी पर खर्च करता है जो दर्शाता है कि वह भविष्य की अपनी महत्वाकांक्षी योजनाओं को मूर्त रूप देने के लिए कितना गंभीर है।
भारत ने भी बीते एक दशक के दौरान इस मोर्चे पर काफी प्रगति की है, लेकिन निवेश एवं उत्पादन के लिहाज से वैश्विक प्रतिस्पर्धियों की तुलना में यह अभी भी अपर्याप्त है। भारत अपनी जीडीपी का केवल 0.64 से 0.7 प्रतिशत तक आरएंडडी पर निवेश कर रहा है। चीन का तो ऊपर उल्लेख है ही, जबकि अमेरिका भी अपनी जीडीपी का 3.47 प्रतिशत आरएंडडी पर खर्च करता है।
ये दोनों ही अर्थव्यवस्थाएं भारत की तुलना में बहुत बड़ी हैं तो कुल राशि कितनी विशाल होगी, इसका सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। स्पष्ट है कि इस महत्वपूर्ण मद में सीमित निवेश भारत की संभावनाओं को प्रभावित कर रहा है। सीमित निवेश के बावजूद प्रदर्शन को देखा जाए तो वैश्विक नवाचार परिदृश्य पर भारत ने अपनी छाप छोड़ी है।
ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की 133 देशों की सूची में 2015 में 81वें स्थान पर रहने वाला भारत 2024 में 39वें पायदान पर पहुंच गया। प्रदर्शन में यह उल्लेखनीय सुधार भारत के विस्तार लेते डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर, अकादमिक जगत एवं उद्योग जगत के बीच बेहतर होते जुड़ाव और तेजी से बढ़ते स्टार्टअप इकोसिस्टम को दर्शाता है। हालांकि इस प्रगति में वित्तीय प्रतिबद्धताएं अपेक्षित रूप से मेल नहीं खा रही हैं।
ऐसे में, निजी क्षेत्र को निवेश बढ़ाना होगा। सकल घरेलू उत्पाद की दृष्टि से आरएंडडी में अभी निजी निवेश करीब 36.4 प्रतिशत के आसपास है जबकि अमेरिका और चीन जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में निजी क्षेत्र का यह योगदान 75 से 77 प्रतिशत के दायरे में है। ऐसे में निजी क्षेत्र की सक्रिय सहभागिता के बिना औद्योगिक क्रांति के मामले में अनुकूल परिणाम प्राप्त होने संभव नहीं।
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बीते दिनों चीन से तुलना करते हुई भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम को सही आईना दिखाया है। भारतीय इकोसिस्टम के रुख-रवैये पर उनकी चिंता वाजिब है। भारत में भले ही डेढ़ लाख से अधिक पंजीकृत स्टार्टअप हों, लेकिन इनमें से अधिकांश ई-कामर्स, फूड डिलिवरी और गिग इकोनमी से जुड़े हैं।
इसकी तुलना में चीन का जोर डीप-टेक, एआइ और हार्डवेयर इनोवेशन और देसी टेक दिग्गजों के निर्माण पर है। इसमें भारत के अपेक्षाकृत रूप से पिछड़ने का संबंध केवल आकांक्षाओं से न होकर ढांचागत रूप से जुड़ा है। उद्योग जगत को अपेक्षाओं के अनुरूप कर्मियों का न मिलना, शोध एवं विकास के लिए संसाधनों का अभाव और सीमित पेटेंट पूंजी से जोखिम लेने की वह क्षमता नहीं उत्पन्न हो पाती जो वास्तविक इनोवेशन और दीर्घकालिक निवेश के लिए जरूरी है। ऐसे में, ‘क्या हम आइसक्रीम और चिप्स ही बनाते रहेंगे’ वाली गोयल की टिप्पणी भले ही कुछ तीखी लगे, लेकिन इसमें गहरा मर्म छिपा हुआ है।
स्थितियां बदलने के लिए हमें अपनी प्राथमिकताएं तय कर उन्हें मूर्त रूप देना होगा। सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र द्वारा आरएंडडी में निवेश बढ़ाना इसकी पहली सीढ़ी होगी। हमें सुनिश्चित करना होगा कि आरएंडडी में निवेश दीर्घकालिक आर्थिक वृद्धि को गति देने वाला हो। नवाचार बढ़ाए, नए उद्योगों के उद्भव का आधार बने, उत्पादकता बढ़ाए और उच्चस्तरीय रोजगारों का सृजन करे। भारत जैसी आर्थिकी में यह ऊंची वृद्धि के लिए उत्प्रेरक हो सकता है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा में सुधार के लिए भी आरएंडडी में निवेश आवश्यक है। तकनीकी नवाचार के आधार पर भारतीय कंपनियां ऊंचे मुनाफे वाले अंतरराष्ट्रीय बाजार के फार्मा, इलेक्ट्रानिक्स, हरित ऊर्जा और एआइ जैसे क्षेत्रों में अपनी पैठ बढा सकती हैं।
एक मजबूत आरएंडडी ढांचे के अभाव में भारत विदेशी तकनीकों पर निर्भर होकर वैश्विक आपूर्ति शृंखला में पिछड़ जाएगा। हेल्थकेयर से लेकर जलवायु परिवर्तन और खाद्य सुरक्षा से लेकर स्वच्छ ऊर्जा जैसी चुनौतियों के समाधान में भी आरएंडडी निवेश की उपयोगिता किसी से छिपी नहीं है। इसमें जहां सरकारी निवेश सार्वजनिक प्रणाली और राष्ट्रीय मिशनों में उपयोगी होगा तो निजी क्षेत्र का निवेश किफायती और दायरा बढ़ाने वाले नवाचारों में लाभकारी होगा।
आरएंडी में निवेश बढ़ाकर भारत न केवल घरेलू समस्याओं का समाधान कर सकता है, बल्कि उलझे हुए वैश्विक मुद्दों को सुलझाने का माध्यम भी बन सकेगा। इससे विदेशी निवेश को भी लुभाने में मदद मिलेगी। तकनीकी संप्रभुता में भी इसकी महत्ता है। याद रहे कि रक्षा, अंतरिक्ष, इलेक्ट्रानिक्स और फार्मा जैसे क्षेत्रों में स्वदेशी तकनीकी विकास से ही आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियान को सफलता मिल सकती है। घरेलू आरएंडडी क्षमताओं का विकास आयात पर निर्भरता घटाने के साथ ही आर्थिकी को बाहरी झटकों से बचाने में ढाल का काम करता है। यह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में राष्ट्रीय क्षमताओं को बढ़ाने के साथ ही अकादमिक उत्कृष्टता का भी आधार बनता है।
एक ऐसे दौर में जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ वार का बिगुल बजा दिया है तो एक प्रकार की यह आपदा भारत के लिए नए अवसर लेकर आई है। भारत के प्रमुख प्रतिस्पर्धी देशों पर जहां ट्रंप ने ज्यादा आयात शुल्क लगाया है तो उसकी तुलना में भारत को कुछ रियायत दी है। ऐसे में भारत अपनी क्षमताओं को बढ़ाकर वैश्विक आपूर्ति शृंखला में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा सकता है तो उसकी कुंजी शोध एवं विकास में निवेश बढ़ाने में ही निहित है। भारत के लिए यह निवेश बढ़ाना अब यह कोई विकल्प नहीं अनिवार्यता बन गई है।
शुल्क पर संग्राम
संपादकीय

अमेरिका की जवाबी शुल्क नीति का असर अब दुनिया के बाजार में दिखने लगा है। खुद अमेरिकी बाजार का रुख नीचे की तरफ हो गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे ही विभिन्न देशों पर लगने वाले जवाबी शुल्क की सूची जारी की, वैश्विक बाजार डगमगाने लगे। शुक्रवार को डाउ जोन्स, नेस्डैक और एसएंडपी 500 में औसतन करीब छह फीसद की गिरावट देखी गई। यह गिरावट सभी क्षेत्रों में जारी रही। उसका असर भारतीय शेयर बाजार में भी दिखा। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर यही रुख बना रहा, तो दुनिया में बहुत जल्दी मंदी का दौर शुरू हो जाएगा। वैश्विक शेयर बाजार में इतनी बड़ी गिरावट कोरोना के बाद पहली बार देखी गई है। उधर, जिन देशों पर अमेरिका ने पारस्परिक शुल्क लगाया है, वे भी जवाबी शुल्क लगाने को तत्पर हैं। चीन ने तो तत्काल अपनी प्रतिक्रिया देते हुए उतना ही शुल्क लगा दिया, जितना अमेरिका ने उस पर लगाया है। इस तरह शुल्क संग्राम शुरू होने की आशंका बढ़ गई है। स्वाभाविक ही इस अमेरिकी नीति का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा, जिसकी शुरू से आलोचनाएं हो रही हैं।
शेयर बाजार में गिरावट का अर्थ है कि अर्थव्यवस्था को लेकर निवेशकों का भरोसा कमजोर हुआ है। जिन निवेशकों ने अमेरिकी फेडरल की दरें बढ़ने के चलते भारतीय पूंजी बाजार से पैसे निकाल कर अमेरिकी बाजार में लगाना शुरू किया था, उन्होंने भी पैसे निकालना शुरू कर दिया है। दरअसल, पारस्परिक शुल्क की वजह से अमेरिकी बाजार में पूंजी का प्रवाह ठहर जाने, उत्पादन कमजोर होने और तेजी से महंगाई बढ़ने की आशंका गहराने लगी है। खुद अमेरिका कई चीजों के उत्पादन में दूसरे देशों पर निर्भर है। इसलिए उन पर शुल्क बढ़ेगा, तो अंतिम रूप से वस्तुओं की कीमतें बढ़ेंगी। फिर, बहुत सारी अमेरिकी कंपनियों ने विभिन्न देशों में अपनी उत्पादन इकाइयां लगा रखी हैं। कई मामलों में आंशिक रूप से, तो कई में पूर्ण रूप से वे अपना उत्पादन दूसरे देशों में करती हैं। इस तरह वहां से तैयार होकर आने वाले उत्पाद की कीमतें भी बढ़ जाएंगी। यही प्रक्रिया दूसरे देशों में भी शुरू हो जाएगी। जाहिर है, इससे न केवल अमेरिका, बल्कि पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ेगी। महंगाई बढ़ने का अर्थ है कि लोग अपने जरूरी खर्चों में भी हाथ पीछे खींचना शुरू कर देंगे। इस तरह बाजार में पूंजी का प्रवाह रुकेगा। इसका सबसे बुरा असर विनिर्माण क्षेत्र पर पड़ेगा।
वैसे ही दुनिया अभी मंदी की मार से पूरी तरह बाहर नहीं निकल पाई थी कि ट्रंप प्रशासन की शुल्क नीति ने एक नया चक्रव्यूह रच दिया। कोरोना के बाद सारी अर्थव्यवस्थाएं संघर्ष करती नजर आ रही हैं। उसकी चपेट में अमेरिका भी रहा है। अब भी वहां महंगाई पर पूरी तरह काबू नहीं पाया जा सका है। अगर संस्थागत निवेशकों ने अपना हाथ पीछे खींचना शुरू कर दिया, तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था और लड़खड़ाने लगेगी। अभी अमेरिका को लगता है कि वह पारस्परिक शुल्क के जरिए अपनी पूंजी में बढ़ोतरी और अर्थव्यवस्था में मजबूती ला सकेगा, मगर हकीकत यही है कि इसका सबसे बुरा प्रभाव खुद उसी पर पड़ेगा। इसीलिए वहां शुरू से इस नीति का विरोध हो रहा है। आधुनिक अर्थव्यवस्थाएं तन्हा नहीं रह गई हैं, उनमें परस्पर जुड़ाव है। वे अपने लाभ के लिए नए समीकरण और संगठन बनाती रहती हैं। ऐसे में, कहीं अमेरिका अलग-थलग न पड़ता जाए।
श्रीलंका की की आश्वस्ति
संपादकीय
भारत और श्रीलंका ने पहली बार सैन्य क्षेत्र में गहन सहयोग के लिए ढांचे संस्थागत बनाने के संबंध में शनिवार को रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए। कोलंबो में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके के बीच वार्ता के बाद दोनों पक्षों ने कुल सात समझौतों पर हस्ताक्षर किए। मोदी – दिसानायके वार्ता में 10 से ज्यादा ठोस परिणाम निकले और सबसे महत्त्वपूर्ण तो यह कि दोनों देश सैन्य क्षेत्र में गहन सहयोग को राजी हुए हैं। बेशक, यह फैसला दोनों देशों के रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। इसलिए भी कि यह समझौता श्रीलंका में भारतीय शांति रक्षा सेना के हस्तक्षेप के करीब 35 साल बाद हुआ है। भारत के लिए मोदी का श्रीलंका दौरा इसलिए भी सफल कहा जा सकता है कि दिसानायके ने प्रधानमंत्री मोदी को आश्वासन दिया है कि श्रीलंका अपने भूभाग का इस्तेमाल किसी भी तरह से भारत के सुरक्षा हितों के प्रतिकूल कदमों के लिए नहीं होने देगा। जब-जब पड़ोसी चीन श्रीलंका के साथ दोस्ताना होता है, तब- तब भारत की पेशानी पर चिंता की लकीरें उभरने लगती हैं। लेकिन अब श्रीलंका से स्पष्ट आश्वासन मिलने से भारत को बड़ी राहत का अहसास हुआ है। दरअसल, दोनों पड़ोसी देशों बीच ऐतिहासिक, आध्यात्मिक और आत्मीयता से भरे संबंध रहे हैं, दोनों देशों की साझा बौद्ध विरासत है, दोनों की सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी हुई है, और दोनों परस्पर निर्भर कहे जा सकते हैं। दिसानायके इस बात से वाकिफ हैं। संभवतः यही कारण रहा कि राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए भारत को चुना। मोदी को भी उन्होंने अपना पहला विदेशी मेहमान बनाया और उन्हें श्रीलंका के सर्वोच्च सम्मान ‘मित्र विभूषण’ से भी नवाजा। भारत भी श्रीलंका की मित्रता को खासा तवज्जो देता है, और इसकी पुष्टि इस बात से होती है कि 2014 के बाद से प्रधानमंत्री मोदी का यह चौथा श्रीलंका दौरा था। चाहे 2019 का आतंकवादी हमला हो, कोविड महामारी हो या हाल में आया आर्थिक संकट हो, हर कठिन परिस्थिति में भारत ने श्रीलंका की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया है। श्रीलंका हमारी ‘पड़ोसी पहले’ नीति और ‘महासागर’ दृष्टिकोण से भी हमारे लिए विशेष स्थान रखता है। अलबत्ता, श्रीलंका में तमिलों की आकांक्षाओं और भारतीय मछुआरों के श्रीलंका के जल क्षेत्र में पकड़े जाने जैसे विवादास्पद मुद्दे हैं। उम्मीद है कि इन मुद्दों का सौहार्दपूर्ण समाधान निकालने में भी दोनों पड़ोसी देश सफल होंगे।
Date: 07-04-25
जरूरत मलहम की
संपादकीय
नक्सलियों से गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आप हमारे अपने हैं। हथियार डाल कर मुख्यधारा में शामिल हों। जब कोई नक्सली मारा जाता है, तो कोई भी खुश नहीं होता। दंतेवाड़ा में बस्तर पंडुम महोत्सव में समापन समारोह में शाह ने कहा कि मार्च, 2026 तक नक्सल समस्या को खत्म करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। नक्सलमुक्त घोषित गांवों को एक करोड़ रुपये की विकास निधि देने तथा नक्सलियों की सुरक्षा और पुनर्वास की व्यवस्था सरकार द्वारा सुनिश्चित करने की बात भी उन्होंने की। शाह के बस्तर प्रवास के दरम्यान छत्तीसगढ़ के 86 नक्सलियों ने हैदराबाद में सामूहिक समर्पण किया जिनमें बीस नक्सल महिलाएं भी शामिल हैं। पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव से 1967 में शुरू किसानों के विद्रोह को नक्सलवाद कहा गया। इसमें शामिल लोगों को नक्सलवादी या नक्सल कहा जाने लगा । इन्हें मुख्यतया वामपंथी आंदोलनों से जोड़ा जाता है। जो माओवादी राजनीतिक विचारधारा का पालन करते हैं। सरकार के अनुसार देश में नक्सल प्रभावित जिले सत्रह से घट कर छह रह गए हैं। छत्तीसगढ़, तेलंगाना, झारखंड और ओडिशा में इनकी जड़ें फैली हुई हैं। बिहार के विभिन्न जिलों को नक्सलमुक्त घोषित किए जाने के बावजूद अभी भी दस जिलों में इनका प्रभाव है। सरकार के प्रति नाराजगी और बुनियादी रूरिया की मांग को लेकर ये उग्र प्रदर्शन करते रहे हैं। पिछले दिनों नक्सलियों की सेंट्रल कमेटी ने पर्चा जारी करके सरकार से युद्धविराम की मांग की। नक्सल प्रभावित इलाकों के नौजवान अब बेहतर शिक्षा और रोजगार की तलाश में अपना वक्त लगाना बेहतर मान रहे हैं। जान बचाने के लिए घने जंगलों में भटकने या सुरक्षा बलों का निशाना बनने को वे राजी नहीं हो रहे। गुरिल्ला युद्ध की ट्रेनिंग लेकर हथियारबंद लड़ाकों को लगातार रिहाइशी इलाकों की तरफ जाने से रोका जा रहा है। दशकों से चले आ रहे इस सशस्त्र वामपंथी आंदोलन को नेस्तनाबूद करने को दृढ़संकल्पित केंद्र सरकार सफल होती दिख रही है। हालांकि ग्रामीण और बीहड़ इलाकों तक विकास, सड़कें, विद्यालय और स्वास्थ्य केंद्रों के साथ ही रोजगार के साधनों की ठोस व्यवस्था ही नौजवानों को मतिभ्रम से दूर रख सकती है। मात्र ओजस्वी भाषणों के भरोसे उनके आवेग / गुस्से को रोका जाना मुश्किल है।
Date: 07-04-25
आखिर संशोधन किसलिए
विनीत नारायण
वक्फ संशोधन वक्फ संशोधन बिल, जिसे हाल में भारतीय संसद में पेश किया गया और 2-3 अप्रैल, 2025 को लोक सभा और राज्य सभा से पारित किया गया, देश में गहन बहस का विषय बन गया है। यह बिल 1995 के वक्फ अधिनियम में संशोधन करने और वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को अधिक पारदर्शी और समावेशी बनाने का दावा करता है। सरकार इसे प्रगतिशील कदम के रूप में पेश कर रही है, जबकि विपक्ष और कई मुस्लिम संगठन इसे धार्मिक स्वायत्तता पर हमला मानते हैं। इस लेख में हम इस बिल के समर्थन और विरोध के तर्कों को तटस्थ दृष्टिकोण से देखेंगे और इसके संभावित प्रभावों का आकलन करेंगे।
वक्फ इस्लामी परंपरा है जिसमें कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति को धार्मिक, शैक्षिक या परोपकारी उद्देश्यों के लिए समर्पित कर देता है। भारत में वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन 1995 के वक्फ अधिनियम के तहत होता है, जिसके अंतर्गत राज्य वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद कार्य करते हैं। वक्फ संशोधन बिल, 2024 में कई बदलाव प्रस्तावित हैं, जैसे वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिम और महिला सदस्यों की अनिवार्यता, संपत्ति सर्वेक्षण के लिए कलेक्टर की भूमिका और विवादों में हाई कोर्ट की अपील का प्रावधान। सरकार का कहना है कि यह बिल वक्फ प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही लाएगा जबकि विरोधी इसे वक्फ की मूल भावना के खिलाफ मानते हैं। इस बिल का समर्थन करने वालों का कहना है कि वक्फ बोड़ों में भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन की शिकायतें
लंबे समय से चली आ रही हैं।
देश में 8.7 लाख से अधिक वक्फ संपत्तियां हैं, जिनकी कीमत लगभग 1.2 लाख करोड़ रुपये आंकी गई है, लेकिन इनका उपयोग गरीब मुस्लिम समुदाय के कल्याण के लिए प्रभावी ढंग से नहीं हो पा रहा। कलेक्टर द्वारा संपत्ति सर्वेक्षण और रिकॉर्ड डिजिटलीकरण जैसे प्रावधानों से इन संपत्तियों का बेहतर प्रबंधन संभव होगा। बिल में वक्फ बोर्ड में कम से कम दो महिलाओं और गैर-मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने का प्रावधान भी है। समर्थकों का तर्क है कि इससे बोर्ड में लैंगिक और सामाजिक समावेशिता बढ़ेगी। विशेष रूप से पसमांदा मुस्लिम समुदाय, जो सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़ा है, इस बिल का समर्थन करता है, क्योंकि उनका मानना है कि मौजूदा व्यवस्था में धनी और प्रभावशाली लोग वक्फ संपत्तियों पर कब्जा जमाए हुए हैं। पहले वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला अंतिम माना जाता था, जिसे अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती थी । नये बिल में हाई कोर्ट में अपील का अधिकार दिया गया है, जिसे समर्थक संविधान के अनुरूप और न्यायसंगत मानते हैं ।
उनका कहना है कि इससे वक्फ बोर्ड के मनमाने फैसलों पर अंकुश लगेगा। बिल में यह शर्त भी जोड़ी गई है कि बिना दान के कोई संपत्ति वक्फ की नहीं मानी जाएगी। समर्थकों का कहना है कि इससे उन मामलों में कमी आएगी जहां वक्फ बोर्ड बिना ठोस सबूत के संपत्तियों पर दावा करता था, जिससे आम लोगों को परेशानी होती थी।
वहीं इस बिल के विरोध में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और विपक्षी दलों का कहना है कि यह बिल वक्फ की मूल भावना को कमजोर करता है। वक्फ धार्मिक परंपरा है और इसमें गैर-मुस्लिम सदस्यों को शामिल करना इसकी पवित्रता को नुकसान पहुंचाएगा। बिल में कलेक्टर को वक्फ संपत्तियों का सर्वेक्षण करने और उनकी स्थिति तय करने का अधिकार दिया गया है। विरोधियों का कहना है कि यह सरकारी हस्तक्षेप है, जो वक्फ बोर्ड की स्वायत्तता को खत्म कर देगा। उनका तर्क है कि कलेक्टर, जो ज्यादातर गैर-मुस्लिम हो सकता है, वक्फ के धार्मिक महत्त्व को नहीं समझ पाएगा। विपक्ष का दावा है कि यह बिल संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 का उल्लंघन करता है, जो धार्मिक स्वतंत्रता और धार्मिक संस्थाओं के प्रबंधन का अधिकार देता है।
उनका कहना है कि वक्फ एक इस्लामी परंपरा है, और इसमें सरकारी दखल अल्पसंख्यक अधिकारों पर हमला है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और अन्य संगठनों ने बिल के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन किए हैं। ईद और जुमातुल विदा जैसे अवसरों पर काली पट्टी बांध कर नमाज पढ़ने की अपील इसका उदाहरण है। विरोधियों का कहना है कि यह बिल मुस्लिम समुदाय को अपने ही धर्म से दूर करने की साजिश है।
वक्फ संशोधन बिल के लागू होने से कई सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। यदि यह पारदर्शिता और समावेशिता को बढ़ाता है, तो वक्फ संपत्तियों का उपयोग गरीब मुस्लिमों, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए बेहतर तरीके से हो सकता है। दूसरी ओर, यदि यह धार्मिक स्वायत्तता को कमजोर करता है या सरकारी हस्तक्षेप को बढ़ाता है, तो इससे मुस्लिम समुदाय में असंतोष और अविश्वास बढ़ सकता है। राजनीतिक दृष्टिकोण से यह बिल सत्तारूढ़ एनडीए के लिए जोखिम भरा कदम है। जहां बीजेपी इसे हिन्दू मतदाताओं के बीच वक्फ बोर्ड की कथित मनमानी के खिलाफ एक कदम के रूप में पेश कर सकती है, वहीं सहयोगी दल जैसे जेडीयू टीडीपी और आरएलडी को अपने मुस्लिम समर्थकों के गुस्से का सामना करना पड़ सकता है। मोदी सरकार संसद में बहुमत के चलते इस बिल को अपने पिछले दो कार्यकालों में आराम से ला सकती थी लेकिन तीसरे कार्यकाल में इस बिल को लाकर भाजपा ने सहयोगी दलों को पसोपेश में डाल दिया है। वक्फ संशोधन बिल जटिल मुद्दा है, जिसमें सुधार की आवश्यकता और धार्मिक संवेदनशीलता के बीच संतुलन बनाना जरूरी है। समर्थकों के लिए यह भ्रष्टाचार खत्म करने और वक्फ को आधुनिक बनाने का अवसर है, जबकि विरोधियों के लिए धार्मिक पहचान और स्वायत्तता पर हमला है। सच्चाई शायद इन दोनों के बीच कहीं है। बिल का असली प्रभाव इसके कार्यान्वयन पर निर्भर करेगा। इसे संवेदनशीलता और पारदर्शिता के साथ लागू किया जाता है, तो यह सकारात्मक बदलाव ला सकता है। लेकिन यदि जल्दबाजी या राजनीतिक लाभ के लिए इसे इस्तेमाल किया गया, तो सामाजिक तनाव को और गहरा सकता है। अंततः इस बिल की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि यह वक्फ की मूल भावना को कितना सम्मान देता है, और समाज के सभी वर्गों को कितना लाभ पहुंचाता है।
विश्व व्यापार संगठन के लद गए दिन
हरजिंदर
बहुत से लोगों के लिए वह खलनायक था। भारत में भी, दुनिया के और बहुत से हिस्सों में भी। अब जब वही खो रहा है, तो बहुत से लोगों को उसकी याद सताने लगी है। खासकर उन लोगों को, जिन्होंने अक्सर नए दौर की बहुत सी समस्याओं के लिए डब्ल्यूटीओ को दोषी करार देने की रीत बना ली थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जवाबी टैरिफ की अपनी जिद से दुनिया के बाजार को जो झटका दिया है, उसके बाद से यह जा कहा जाने लगा है कि इससे अच्छी तो डब्ल्यूटीओ वाली व्यवस्था थी।
तीस साल पहले जब डब्ल्यूटीओ की स्थापना की गई थी, तो इसके पीछे की सोच यही थी कि यह संगठन दुनिया को नियम आधारित व्यापार व्यवस्था देगा। इसमें व्यापार के मामले में देशों को अपने हिसाब से मनमानी की छूट नहीं होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक देश से किसी सामान के आयात पर शुल्क लगाएं और दूसरे देश से उसी सामान के आयात पर दूसरा उदाहरण के लिए, भारत ने 2023 में सेब पर लगने वाला आयात शुल्क 70 से घटाकर 50 फीसदी कर दिया। कहा जाता है कि ऐसा अमेरिकी सेब लॉबी के दबाव में किया गया।
सच जो भी हो, इससे वाशिंगटन एप्पल का आयात बढ़ गया। यह एक प्रीमियम सेब है, जिसका बाजार सीमित है। जबकि, आयात शुल्क कम होने का असल फायदा ईरान और तुर्किये के निर्यातकों ने उठाया । ध्यान रहे, इन देशों के सेब हमारे बाजार में हिमाचल प्रदेश और कश्मीर के सेब को टक्कर देने लगे।
डब्ल्यूटीओ का विरोध करने वालों की आपत्तियां इसके अलावा भी थीं। इस संगठन ने सब्सिडी कम करने जैसी कई शर्तें भी रखी थीं, जो अलग-अलग देश पर अलग ढंग से लागू हो रही थीं। जैसे अमेरिका में आज भी हर किसान को हर महीने लाखों रुपये की सब्सिडी दी जाती है, जबकि भारत में किसानों के हिस्से सिर्फ किसान सम्मान निधि की मामूली रकम ही आती है। विरोधियों का यही तर्क था कि इस संगठन ने जो नियम बनाए हैं और जो पूर्व शर्तें हैं, वे माखन-माखन संतो ने खाया, छाछ जगत बापरानी हो वाले अंदाज में विकसित देशों का ही ज्यादा हित साधती हैं।
व्यवहार में सच भी यही था । इसलिए इसे दुनिया के सभी चंद विकसित देशों का षड्यंत्र भी कहा जाता रहा। डर यह था कि ये नियम-कायदे भारत जैसे देशों के कई उद्योगों के लिए मुसीबत बन सकते हैं और किसानों को तो तबाह ही कर सकते हैं।
शुरू में यह होता हुआ दिखा भी, लेकिन डब्ल्यूटीओ के दबावों के अलावा और भी कई कारण थे, जिनसे दुनिया को आर्थिक और औद्योगिक उदारवाद की ओर बढ़ना ही था। इस सबके बहुत से नुकसान भी गिनाए जाते हैं, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया ने जो फायदे दिए, वे कहीं ज्यादा संख्या में थे। और, सबसे बड़ी बात यह है कि धीरे-धीरे एक व्यवस्था उभरी, जो सभी को संतुलन की एक नई व्यवस्था की ओर ले गई।
मगर असल समस्या कृषि व्यापार को लेकर थी और अब भी बनी हुई है। भारत जैसे देशों में जहां आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा आज भी पूरी तरह कृषि पर निर्भर है, वहां बाजार की थोड़ी सी भी ऊंच-नीच किसानों के सामने आजीविका और अस्तित्व का संकट खड़ा कर सकती है। यही वजह है कि भारत ने इसे लेकर काफी संघर्ष किया, जो आज भी किसी न किसी तरह से चल रहा है। डब्ल्यूटीओ सिर्फ नियम-कायदे बनाने वाली संस्था नहीं है, एक तरह से कचहरी का काम भी करती है। जेनेवा में बने उसके भव्य मुख्यालय में नियमों के उल्लंघन को लेकर अपील की जाती है और फैसले भी होते हैं। भारत समेत बहुत सारे देश वहां आज भी तारीख पर तारीख भुगत रहे हैं।
हालांकि, इस सबके बावजूद जिस कृषि व्यवस्था को हमने डब्ल्यूटीओ की आशंकाओं से बचा लिया, उन्हें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मनमानी से उपजी अराजकता से बचाया जा सकेगा या नहीं, यह अभी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता।
डोनाल्ड ट्रंप ने जवाबी टैरिफ का राग छेड़कर सिर्फ विश्व व्यापार संतुलन को ही नहीं बिगाड़ा, विश्व व्यापार संगठन को भी बेमतलब बना दिया है। वैसे कहा जाता है कि यह काम छोटे पैमाने पर तभी चालू हो गया था, जब ट्रंप का पहला कार्यकाल शुरू हुआ था। उस समय य डब्ल्यूटीओ से किनारा काटने की जो प्रक्रिया शुरू हुई, उसे जो बाइडन ने रोकने के बजाय आगे ही ने बढ़ाया। ‘और अब 2 अप्रैल को डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को एक नया मुक्ति दिवस देने की जो घोषणा की है, ह दरअसल डब्ल्यूटीओ से मुक्ति की घोषणा भी है। और अगर अमेरिका के लिए डब्ल्यूटीओ का कोई अर्थ नहीं रह गया, तो बाकी दुनिया के लिए भी इसका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा।
हमें आज डब्ल्यूटीओ की याद इसलिए नहीं सता रही कि उसने दुनिया के व्यापार और लोगों की समृद्धि को नई ऊंचाई देने के लिए कई बड़े काम किए हैं, बल्कि इसलिए आ रही है कि कुछ भी हो, उसके नियम-कायदे थे. , जो भले ही निष्पक्ष न हों, भले ही सबको बराबर का फायदा न पहुंचाते है ते हों, लेकिन वे ऐसे किनारे थे, जिनके बीच विश्व व्यापार की नदी बहती दिखाई दे रही थी। मगर अब एक व्यक्ति के मनमानेपन ने जब इसके बांध तोड़ दिए हैं, तो सब कुछ बाद के हवाले हो गया है। खराब नियमों और अराजकता के बीच किसी एक को चुनना हो, तो ज्यादातर लोग शायद खराब नियमों को चुनना ही पसंद करेंगे । इसीलिए ऐसे बहुत से लोगों को आज डब्ल्यूटीओ की अच्छाइयां नजर आने लगी हैं, जिन्हें पहले इसमें सिर्फ दोष ही नजर आते थे।
विश्व व्यापार में अराजकता आएगी, तो वह सिर्फ देशों का ही कुछ करेगी, ऐसा नहीं कहा जा सकता। तमाम अर्थशास्त्री यहां तक कह रहे हैं कि इसका सबसे ज्यादा नुकसान खुद अमेरिका को हो सकता है, लेकिन फिलहाल अमेरिका को फिर से महान बनाने की जिद्द में जुटे डोनाल्ड ट्रंप की चिंता का यह विषय नहीं है।
डब्ल्यूटीओ का सारा कामकाज सदस्य देशों द्वारा मिलने वाली फीस या हिस्सेदारी से चलता है। समाचार एजेंसी रायटर ने पिछले सप्ताह सूत्रों के हवाले से यह खबर दी थी कि अमेरिका ने इसमें अपना योगदान देना बंद कर दिया है। बाकी देशों को फायदा मिलता न दिखा, तो शायद वे भी यही करेंगे। क्या विश्व व्यापार संगठन को श्रद्धांजलि देने का समय आ गया है ?
Date: 07-04-25
पूर्वी और दक्षिण एशिया को करीब लाने की कवायद
हर्ष वी पंत, ( प्रोफेसर व विदेश मामलों के विशेषज्ञ )
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाल का थाईलैंड और श्रीलंका दौरा भारतीय कूटनीति के लिए कई मायने में महत्वपूर्ण है। एशिया के इस क्षेत्र में लगभग निष्क्रिय हो चुके दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) के बाद क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने वाले एक संगठन की जरूरत शिद्दत से महसूस की जा रही है। ऐसे में, बिम्सटेक इस सहयोग को आकार देने में अहम साबित हो सकता है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी-सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक को- ऑपरेशन (बिम्सटेक) के छठे शिखर सम्मेलन में भाग लेने बैंकॉक गए थे। इससे भारत- थाईलैंड संबंध को भी मजबूती मिली है। उनकी यात्रा से इस बात को भी बल मिला है कि दक्षिण व दक्षिण-पूर्व एशिया के दो भौगोलिक क्षेत्र आपस में जुड़े हुए हैं। दोनों को एक-दूसरे की ताकत का लाभ उठाने का मौका नहीं मिला है। इस सच्चाई को देखते हुए प्रधानमंत्री की यह यात्रा और बिम्सटेक में भारत की बढ़ती सक्रियता विशेष महत्व रखती है।
बिम्सटेक का गठन 1997 में हुआ, लेकिन इसने 2016 में तब गति पकड़ी, जब मोदी ने गोवा में लीडर्स रिट्रीट के लिए संगठन के देशों को आमंत्रित किया। इसके बाद से नई दिल्ली ने समूह को और मजबूत करने के साथ-साथ क्षेत्रीय सहयोग पर ध्यान केंद्रित करने की लगातार कोशिशें की हैं। ज्ञात हो कि मोदी ने बिम्सटेक देशों के नेताओं को 2019 में अपने शपथ ग्रहण में भी आमंत्रित किया था। इसके अतिरिक्त भारत की पड़ोसी पहले नीति, एक्ट ईस्ट नीति ने भी समूह की सक्रियता को जरूरी बना दिया है।
बैंकॉक शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने समृद्ध, लचीला और खुला बिम्सटेक थीम के अनुरूप कई पहलों की घोषणा की। भारत में आपदा प्रबंधन, सतत समुद्री परिवहन, पारंपरिक चिकित्सा के साथ कृषि अनुसंधान और प्रशिक्षण पर बिम्सटेक केंद्र स्थापित किए जाएंगे। युवाओं के लिए एक नया कार्यक्रम- बोधि चलेगा। इसके तहत पेशेवरों, छात्रों, शोधकर्ताओं, राजनयिकों को प्रशिक्षण व छात्रवृत्ति दी जाएगी। भारत ने क्षेत्र में कैंसर उपचार के लिए एक क्षमता निर्माण कार्यक्रम की भी पेशकश की। क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण का आह्वान किया। बिम्सटेक चैंबर ऑफ कॉमर्स की स्थापना और भारत में हर साल बिम्सटेक बिजनेस समिट आयोजित करने की पेशकश की गई है।
बिम्सटेक में निवेश करके भारत यह संकेत दे रहा है कि वह दक्षिण-पूर्व एशिया में बाहरी खिलाड़ी नहीं है। बल्कि वह थाईलैंड-म्यांमार के रास्ते दक्षिण-पूर्व एशिया से नाभिनाल जुड़ा हुआ है। मोदी ने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र बिम्सटेक के केंद्र में है।
यह यात्रा पिछले 12 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली थाईलैंड यात्रा थी। दोनों देशों ने रणनीतिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए। रक्षा पर सहयोग बढ़ाया और दक्षिण-पूर्व एशिया से जुड़नेवाले एक प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजना को गति दी। दोनों देश 1,300 किलोमीटर लंबी राजमार्ग परियोजना में तेजी लाएंगे। यह राजमार्ग म्यांमार के रास्ते पूर्वोत्तर भारत को उत्तरी थाईलैंड से जोड़ेगा।
बहरहाल, प्रधानमंत्री मोदी के श्रीलंका दौरे की एक अलग कहानी है। वहां की अनुरा कुमारा दिसानायके सरकार के बारे में शुरुआती आशंकाओं के बावजूद दिल्ली- कोलंबो संबंध लगातार सुधर रहे हैं। इस दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल को कोलंबो ने स्वीकार भी किया है। इसीलिए किसी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष को दिया जाने वाला श्रीलंका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्र विभूषण नरेंद्र मोदी को प्रदान किया गया। कोलंबो के मध्य में ऐतिहासिक स्वतंत्रता चौक पर मोदी का भव्य स्वागत भी किया गया, जो शायद किसी विदेशी नेता को दिया जाने वाला पहला ऐसा सम्मान था। मोदी ने भी राष्ट्रपति दिसानायके की भूमिका की सराहना की है। दिसानायके ने भारत को आश्वासन दिया कि श्रीलंकाई क्षेत्र को भारत की सुरक्षा के साथ-साथ क्षेत्रीय स्थिरता को हानि पहुंचाने वाली किसी भी गतिविधि के लिए उपयोग करने नहीं दिया जाएगा। वाकई, प्रधानमंत्री की इस यात्रा से पता चलता है कि पूरे क्षेत्र में भारत की भूमिका बढ़ाने की बड़ी जरूरत है।