
05-06-2025 (Important News Clippings)
To Download Click Here.

Date: 05-06-25
Finally, Sense Of Us
Great that GOI’s announced Census. But delimitation & caste questions make it more than just stats
TOI Editorials
Better late than never, as they say -GOI’s finally announced a date for census. But this piece of excellent news comes with a big question mark attached to it. Given that the population count has to end by March 2027, will final results be out before 2029 Lok Sabha elections? This is a politically supercharged question.
If the population count does come in appreciably before, say, early 2029, a delimitation commission can be set up in this LS term itself. But if, like in the previous census, the final population count takes almost two years to publish, 2027 census results won’t likely come in time for the delimitation exercise to finish before 2029 polls. Therefore, census 2027 is not just a vital statistical exercise for the world’s largest democracy, it will also be keenly watched to see whether it changes the dynamics of electoral politics before the next LS polls. It would be best, therefore, if GOI gives a broad idea of the month/year by which final population count can be expected,as well as its plans on a delimitation commission given those dates.
For example, a delimitation commission can start its work before 2029 but GOI may decide to go with existing LS seat structure for the next general elections. That most big states ruled by opposition parties are in the South, which has successfully controlled population growth, and BJP’s political dominance is concentrated in the North and West makes any debate on delimitation fraught. Anything short of clarity will make a polity already characterised by bitter divides even more fractured. India, in a relatively sweet spot economically, simply doesn’t need a hot-blooded political fight, pitting North against South.
Speaking of economics, and hopefully assuming the census doesn’t lead to almighty political rows, the exercise will fill several gaps in understanding and governing India. We don’t have any idea of key numbers. What’s the urban-rural divide, in terms of numbers and living standards? How many Indians are poor enough to qualify for govt benefits like free foodgrain? How have consumption patterns changed? What’s the real story on migration? These are just a few of many vital questions the census will answer.
Caste census? Caste will be enumerated, that’s all we know now. We also know Bihar’s caste census has done little to improve policy and Karnataka’s is mired in controversy. Like delimitation, this is another political red hot potato.

Date: 05-06-25
तकनीकी क्रांतियों के पीछे की सच्चाई
अजित बालाकृष्णन, ( लेखक तकनीक और समाज के बीच संपर्कों के बारे में अध्ययन को समर्पित हैं )
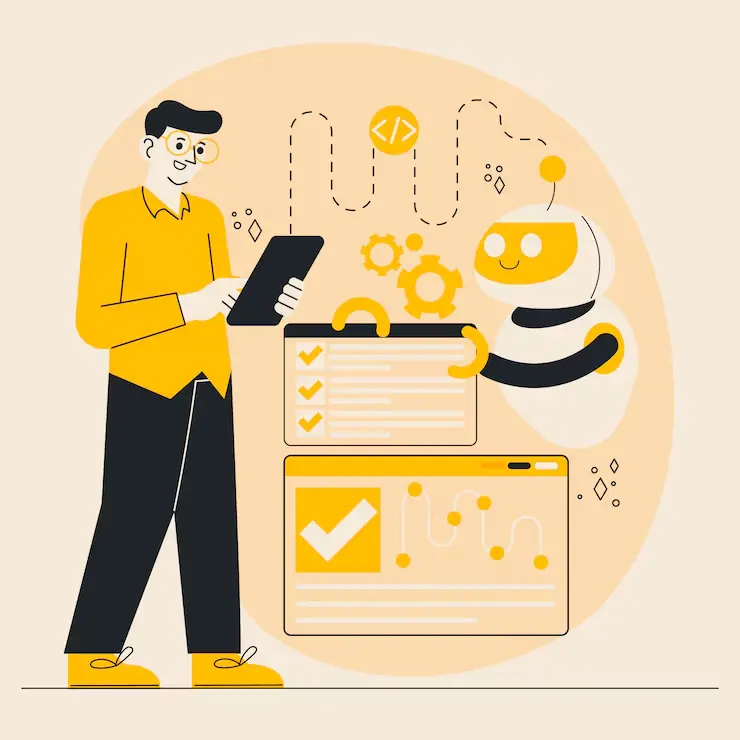
मेरे जीवन में निरंतर चले आ रहे रहस्यों में से एक यह समझने की कोशिश भी रही है कि आखिर इंगलैंड में 18वीं सदी के मध्य में आरंभ हुई औद्योगिक क्रांति, जिसने कताई और बुनाई की मशीनों की शुरुआत की, वह पहले भारत में क्यों नहीं घटित हुई। आखिर भारत उस समय दुनिया में सबसे अधिक कपास के धागे और कपड़े तैयार कर रहा था । मैं जब भी यह सवाल करता हूं तो मुझे उत्तर मिलता है, ‘भारत श्रम की लागत इतनी कम थी कि किसी ने कताई या बुनाई के लिए मशीनों का अविष्कार करने के बारे में सोचा ही नहीं।’
औद्योगिक क्रांति शब्द को ब्रिटिश आर्थिक इतिहासकार अर्नोल्ड टॉयनबी ने 1882 में ऑक्सफर्ड विश्वविद्यालय में एक व्याख्यान में इस्तेमाल किया था और यह बताया था कि कैसे कताई और बुनाई की मशीनों ने इंगलैंड को पूरी तरह से बदल दिया। उनकी बदौलत घरेलू स्तर पर होने वाले उत्पादन में भारी बदलाव आया। घरों और छोटी वर्कशॉप में होने वाला काम अब कारखानों में होने लगा जहां मशीनों के जरिये व्यवस्थित ढंग से बहुत बड़े पैमाने पर उत्पादन होता था। उन्होंने ‘क्रांति’ शब्द का इस्तेमाल किया क्योंकि उन्होंने देखा कि इससे बहुत तेज और भारी बदलाव आया था जिसने समाज को उसी तरह बदल दिया जैसे कि कोई महत्त्वपूर्ण राजनीतिक क्रांति करती है। दूसरे शब्दों में उन्होंने कहा कि केवल मशीनों के इस्तेमाल ने ही नहीं बल्कि आर्थिक, सामाजिक और मानवीय रिश्तों के बुनियादी पुनर्गठन ने इसे एक ‘क्रांति’ में बदल दिया।
काश मैं उस समय श्रोताओं के बीच होता तो खड़ा होकर कहता, ‘आप ब्रिटेन की बहुत अच्छी मार्केटिंग कर रहे हैं श्रीमान टॉयनबी।’ प्रिय पाठको, इससे पहले कि आप सोचें कि मैं इतना बगावती क्यों हूं. कुछ तथ्यों पर ध्यान दीजिए।
यह एक व्यापक मान्यता है कि ब्रिटेन के सूती कपड़ा विनिर्माता इन मशीनों का इस्तेमाल किए जाने से इतना किफायती कपड़ा तैयार करने लगे जिसके चलते केवल वे भारत से सूती वस्त्र का आयात पूरी तरह रोक सके बल्कि वे भारत के कताई बुनाई उद्योग को पूरी तरह नष्ट करने में भी कामयाब रहे।
बहरहाल एक सच जिसका जिक्र इस कहानी में नहीं किया जाता वह यह है कि मैनचेस्टर के कताई – बुनाई कारोबार को फलने-फूलने के लिए ब्रिटिश सरकार ने सन 1700 में कानून पारित किए और आयात शुल्क को बेतहाशा बढ़ा दिया । भारत आने वाले सूती वस्त्र पर उनके प्रकार के हिसाब से 15 से लेकर 75 फीसदी तक आयात कर लगाया गया । इस कपड़े को वहां कैलिको कहा जाता था क्योंकि उसे केरल के कालीकट बंदरगाह से ब्रिटेन भेजा जाता था। चूंकि इससे मांग कम करने को लेकर वांछित असर नहीं पड़ा तो 1720 में दूसरा कानून पारित किया गया ताकि भारत सूती वस्त्र आयात पर पूरी तरह प्रतिबंधित किया जा सके।
इस कानून में यह प्रावधान भी था कि आयातित सूती कपड़े पहनने वाले लोगों पर 15 पाउंड तक का जुर्माना लगाया जा सकता है और ऐसे कपड़े रखने अथवा बेचने वालों पर 200 पाउंड तक के जुर्माने का प्रावधान था। जब ये प्रावधान भी नाकाम रहे तब ब्रिटिश बुनकरों ने कैलिको पहनने वाली महिलाओं पर हमले करके विरोध जताया, उन्होंने उनके कपड़े फाड़े और यहां तक कि उन पर तेजाब भी फेंका गया।
शायद औद्योगिक क्रांति की कहानी के पीछे का सबसे सावधानी से छिपाया गया तथ्य यह है कि आखिर किस बात ने ब्रिटिश सूती वस्त्र निर्माताओं को भारतीय हथकरघा बुनकरों पर अंतिम बढ़त प्रदान की। सन 1800 के आसपास ब्रिटेन अपना अधिकांश कपास अमेरिका के दक्षिण से आयात करता था जिसे हजारों दास अफ्रीकियों की बदौलत एक विशाल बंधुआ मजदूर शिविर में बदल दिया गया था। ये दास अकल्पनीय रूप से कम कीमत पर कच्चा कपास बहुत भारी मात्रा में उपलब्ध कराते थे।
एक बार जब मुझे ये तथ्य पता चल गए तो मैं गहरे अवसाद का शिकार हो गयाः क्या यह संभव है कि मानवता ऐसे तथ्यों की अनदेखी करती रहे और पिछले 200 अधिक वर्षों से यह मानती आ रही हो कि ‘औद्योगिक क्रांति’ जैसे जुमले का इस्तेमाल उन कार्यों को उचित ठहराने के लिए किया जा सकता है जो वास्तव ‘औपनिवेशिक शोषण’ था? ‘तकनीक आधारित विकास’ या ‘तकनीकी क्रांति’ जैसे जुमले तो और भी चिंतित करने वाले हैं। इनका इस्तेमाल उन कदमों के लिए किया गया जो वास्तव में विभिन्न पहलों का मिश्रण थे और जिनमें तकनीक की हिस्सेदारी बेहद कम थी। दूसरे शब्दों में कहें तो क्या हमें उन कई ‘ तकनीकी क्रांतियों’ के पुनर्परीक्षण की जरूरत है जिन्हें हम अब तक राजनीतिक अर्थव्यवस्था के नजरिये से देखते आए थे? कहने का तात्पर्य यह है कि हमें केवल इंजीनियरिंग के लिहाज से ही नहीं, अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र और समाजशास्त्र के नजरिये से अलग साधनों और तरीकों का इस्तेमाल कर उन तमाम तकनीकी क्रांतियों का पुनर्परीक्षण करना होगा, जिनके बारे में हम सभी मानते हैं कि वे घटित हुई हैं।
पहली औद्योगिक क्रांति (18वीं- 19वीं सदी) ने भाप से चलने वाली मशीनें दीं जिन्होंने हाथ से होने वाले उत्पादन की जगह ली। दूसरी औद्योगिक क्रांति (19वीं सदी का अंत और 20वीं सदी) ने बिजली और व्यापक उत्पादन की तकनीक मसलन असेंबली लाइन आदि तैयार कीं। तीसरी औद्योगिक क्रांति जिसे डिजिटल क्रांति कहा जाता है उसने कारखानों में स्वचालन और एकीकृत व्यवस्था के लिए उन्हें कंप्यूटरों और इंटरनेट से जोड़ा। चौथी औद्योगिक क्रांति (उद्योग 4.0 ) का संबंध आर्टिफिशल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स से है। ये एक साथ मिलकर साझा संपर्क और मेधा के क्षेत्र में काम करते हैं। अब पांचवीं औद्योगिक क्रांति उभर रही है।
शायद अब वक्त आ गया है कि महात्मा गांधी की ओर लौटें और उस बात पर ध्यान दें जो उन्होंने स्वराज आंदोलन के समय कही थी, ‘उनका जोर श्रम की बचत करने वाली मशीनरी पर है। लोग तब तक श्रम की बचत करेंगे जब तक कि हजारों लोग बेकार नहीं हो जाते और सड़कों पर भूख से मरने के लिए नहीं फेंक दिए जाते। मैं समय और श्रम बचाना चाहता हूं, मानव जाति के कुछ हिस्से के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए। मैं चाहता हूं कि धन का केंद्रीकरण कुछ लोगों के हाथ में न हो बल्कि सभी के पास धन हो । आज मशीनरी केवल कुछ लोगों की सहायता करती है ताकि वे लाखों लोगों पर शासन कर सकें लेकिन इसके पीछे की प्रेरणा परोपकार नहीं बल्कि लालच है। ऐसा नहीं है कि हमें मशीनरी नहीं चाहिए, लेकिन हम इसे इसके उचित स्थान पर चाहते हैं। जब तक इसे सरल नहीं बनाया जाता है और सभी के लिए उपलब्ध नहीं कराया जाता, तब तक यह हमारे पास नहीं होगी।’
क्या यही वह अगला आंदोलन है जिसे हमें अपनाना चाहिए और जो शायद आज के दिनों में उतना ही अहम हो सकता है जितना कि गांधी के दौर में स्वराज आंदोलन था।
Date: 05-06-25
पर्यावरण बचाने के लिए सबसे पहले प्लास्टिक से बनाएं दूरी
अनिता भटनागर जैन, ( पूर्व आईएएस अधिकारी )

वह क्या है, जो जल में थल में, हम सब में एक ही समय में सभी जगह विद्यमान है? कदाचित हममें से अधिकांश पहले इसका उत्तर देते दैवीय शक्ति। परंतु आज इसका उत्तर है प्लास्टिक ! प्लास्टिक के नैनो कण समुद्रों की अधिकतम गहराई तक, नदियों में, आकाश में 9,500 फीट की ऊंचाई तक भूमि में, यहां तक कि हमारे नमक, शरीर, मां के दूध, शुक्राणु, किडनी, फेफड़ों, दिमाग तक में पाए जाने लगे हैं। विभिन्न आकार-प्रकार में प्लास्टिक अब सब तरफ ऐसे है कि इसकी ओर ध्यान ही नहीं जाता ।
सन् 1972 में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करने और पृथ्वी को संरक्षित करने के लिए स्वीडन से 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस आयोजित करने का सिलसिला प्रारंभ हुआ। इस वर्ष पर्यावरण दिवस का विषय है- ‘वैश्विक प्लास्टिक प्रदूषण का अंत।’ हमारे जीवन के अनेक पहलुओं में प्लास्टिक जरूरी है और उसका कोई विकल्प भी अभी नहीं है। मगर इसके कारण ‘डिस्पोजेबल कंज्यूमर कल्चर’ पैदा हुआ। महज एक बार इस्तेमाल योग्य प्लास्टिक के कारण थ्रो अवे पीढ़ी’ का जन्म हुआ। इससे सबका नुकसान हो रहा है। असहाय पशु-पक्षी भी मनुष्य की गतिविधियों का परिणाम ग्राम भुगत रहे हैं। कुछ वर्ष पूर्व संयुक्तराष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) द्वारा बताया गया था कि विश्व भर में एक मिनट के भीतर 10 लाख प्लास्टिक की बोतलों का उपयोग होता है। यानी एक दिन में 144 करोड़ है न भयावह ? हम पृथ्वी पर प्लास्टिक कचरे की कैसी विरासत छोड़ रहे हैं? शहरों में जल जमाव की समस्या का मुख्य कारण ये प्लास्टिक कचरे ही हैं। आंकड़ों से वास्तविकता अधिक स्पष्ट होकर सामने आती है। वैश्विक प्लास्टिक कचरे में भारत का योगदान 18 प्रतिशत है। हमारे यहां हर दिन करीब 26,000 मीट्रिक टन और देश के 60 मुख्य शहरों में 4,000 से अधिक मीट्रिक टन प्लास्टिक कचरे का सृजन होता है। इनमें से ज्यादातर कचरा खुली जगहों और गड्ढों में पड़ा रहता है।
गौर कीजिए, 99 प्रतिशत प्लास्टिक जीवाश्म ईंधन से तैयार होता है, जो जैविक रूप से कभी नष्ट नहीं होता, यानी प्लास्टिक अमर है। लोगों में यह भ्रांति है कि समस्त प्लास्टिक और अन्य कचरों का पुनः उपयोग हो जाता है। लेकिन पर्यावरण के मुद्दे पर काम करने वाले गैर-सरकारी संगठन सीएसई का कहना है, देश में मात्र 12 प्रतिशत प्लास्टिक का ही पुनः उपयोग हो रहा है और 20 प्रतिशत प्लास्टिक कचरा जलाया जा रहा है। इस दहन से घातक गैस पैदा होती है, जिससे अनेक जानलेवा बीमारियां बढ़ रही हैं। वातावरण में ग्रीनहाउस गैसों में इजाफा हो रहा है और इस सब के फलस्वरूप ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। इस कुचक्र का कोई अंत है?
आखिर इस अजर-अमर दिखते दानव का वध कैसे संभव है? पर्यावरण सुरक्षा दिवस मनाने से कुछ जागरूकता बढ़ी है, लेकिन वास्तविक उपाय निकालने में पता नहीं कितने दशक लग जाएं? आवश्यकता इस बात की है कि सब लोग समाधान का हिस्सा बनें। देश में प्लास्टिक के 30,000 से अधिक उत्पादक उद्यम हैं। इन पर भी इसके विकल्पों के उपयोग करने और प्लास्टिक को एकत्र कर उसे साइिकल करने का दायित्व होना चाहिए। वैसे, जिम्मेदारी तो उद्योग, समाज, नागरिक सभी की है। लेकिन, यदि नागरिक को कर्तव्य समझ में आ जाए, तो बहुत आसानी से स्थिति में व्यापक सुधार लाया जा सकता है। क्या हम विभिन्न आयोजनों में प्लास्टिक वस्तुओं का उपयोग बंद कर सकते हैं? क्या यह संभव है कि हम हवन या पूजा सामग्री प्लास्टिक की थैली में बांधकर नदियों में न फेंके ? क्या हम अपने कूड़े को गीले, कागज, प्लास्टिक आदि श्रेणियों में अलग कर सकते हैं? क्या हम फल, सब्जियां और अन्य सामान कपड़े के थैलों में नहीं ला सकते ? जब हम अपना मोबाइल कहीं ले जाना नहीं भूलते, तो अपनी पानी की बोतल और कपड़े का थैला भी साथ रख सकते हैं?
हम सब अपने और अपने परिजनों के लिए स्वस्थ जीवन चाहते हैं। तो क्या इसी स्वार्थवश अपनी आदतों में हमें बदलाव नहीं लाना चाहिए? बदलाव कठिन हो सकता है, मगर असंभव नहीं। आइए, हम अपने ही दायरे से पर्यावरण बिगाड़ने वाली इस बिल्ली के गले में घंटी बांधकर शुरुआत करें।
