
01-09-2022 (Important News Clippings)
To Download Click Here.
 Date:01-09-22
Date:01-09-22
Level Playing Field
UGC must give Indian universities the same freedoms it’s planning to give foreign universities.
TOI Editorials

Indian universities, both public and private, have to negotiate their way through a thicket of rules and regulations, framed by UGC, AICTE, NMC, BCI, state governments. These rules apply for starting new courses, sanctioning student intake, and various academic and administrative operations. No Western country or even China makes its education institutions jump through so many hoops. And it’s not just independent experts who have raised questions but also Parliament members. The parliamentary standing committee on education has, on more than one occasion, found UGC and other regulators to be overbearing in their approach.
The higher education market in India is already big and will become huge, comparable to China’s, as aspirations grow on the back of a long period of reasonably good GDP growth. There’s a growing demandsupply gap in quality higher education. The better Indian universities can play a key role in bridging this gap, but not if they are burdened with regulations that don’t apply to their foreign counterparts.
The Man Who Tried To Free Countries
ET Editorials
Mikhail Gorbachev’s life was bookended by Stalinism. In the middle was his attempt to nix it. When he was born in 1931, Joseph Stalin’s ‘collectivisation’ had already led up to the Great Famine of 1930-33. By the Great Terror of 1937, the tone for life in the Soviet Union was set. When Gorbachev died on Tuesday, a Stalinist in Russia seeking to regain ‘lost glory’ — for which he blames Gorbachev squarely — continued his invasion of an old Soviet republic.
Hindsight, a funny mirror, portrays Gorbachev as the man who ‘suddenly dismantled’ a global power and counterpole to a superpower. But, in 1985, when he took over from the 73-year-old Konstantin Chernenko, the country was already well on the low road to penury, not helped by a bleeding war in Afghanistan. Chernenko’s predecessor, Yuri Andropov, as KGB chief in 1968, had shared classified data on the conditions of Soviet society with him. So, the 54-year-old already knew there was only one way for his country not to implode: by opening up (glasnost) and restructuring (perestroika). What followed was a free election in 1989 — not seen since the one after the 1917 revolution the Bolsheviks threw out — which accelerated the unfurling. Gorbachev had overestimated his ability to control a project that almost none in the leadership agreed with. A little after Gorbachev visited India in 1986 and 1988, and after signing a landmark deal in 1987 with Ronald Reagan to scrap intermediate-range nuclear missiles, back home, asset-stripping was already on. By Boxing Day 1991, the Soviet Union was gone. As was the Cold War. Gorbachev’s plan was an open, socialist society with ex-Soviet and Warsaw Pact countries free of Stalinism in its various formats. In that, he failed. But not for lack of trying.
महिलाओं को लीडरशिप देने में क्यों झिझकता है समाज
संपादकीय
एक राज्य-सरकार ने आदेश दिया है कि अगर महिला सरपंच की जगह मीटिंग में उसका पति पहुंचता है या फैसले लेता है तो न केवल महिला सरपंच निलंबित होगी बल्कि उसके पति पर भी आपराधिक कार्रवाई होगी। यह केवल एक राज्य की ही नहीं, पूरे देश खासकर उत्तर भारत की समस्या है। अच्छी प्रजातांत्रिक भावना के जरिए देश में 73वें संविधान संशोधन के तहत ग्राम पंचायत को पहली इकाई बनाकर और प्रावधानों को 11वीं अनुसूची में डालते हुए पंचायत-राज व्यवस्था बहाल की गई। फिर एक अन्य समुन्नत सोच के तहत राज्यों में महिलाओं के लिए इन पंचायत संस्थाओं में मुखिया से लेकर जिला-परिषद तक के पदों पर आरक्षण की व्यवस्था की गई। उद्देश्य था गवर्नेंस में महिलाओं की सीधी भागीदारी। लेकिन देखते-देखते ईर्ष्यालु पुरुष-प्रधान समाज ने गैर-कानूनी ‘मुखिया-पति’ जैसा पद खोज निकाला और पत्नी की जगह खुद बाकायदा मीटिंग्स में फैसले लेने लगा क्योंकि पत्नी शिक्षित नहीं थी या पति की दबंगई के आगे विवश थी। पंचायतों की मीटिंग्स में भी पत्नी की जगह बेशर्मी और गुंडई से पति फैसले ही नहीं लेता बल्कि कई जगह पत्नी के हस्ताक्षर भी खुले आम मुखिया पति करने लगा। यानी कानून, संविधान और अनुसूची की मजबूती के बाद भी दोनों उद्देश्य असफल रहे। आखिर क्यों समाज की सोच आज सात दशक बाद भी उतनी ही दकियानूसी है?
जीवट का हारना
संपादकीय
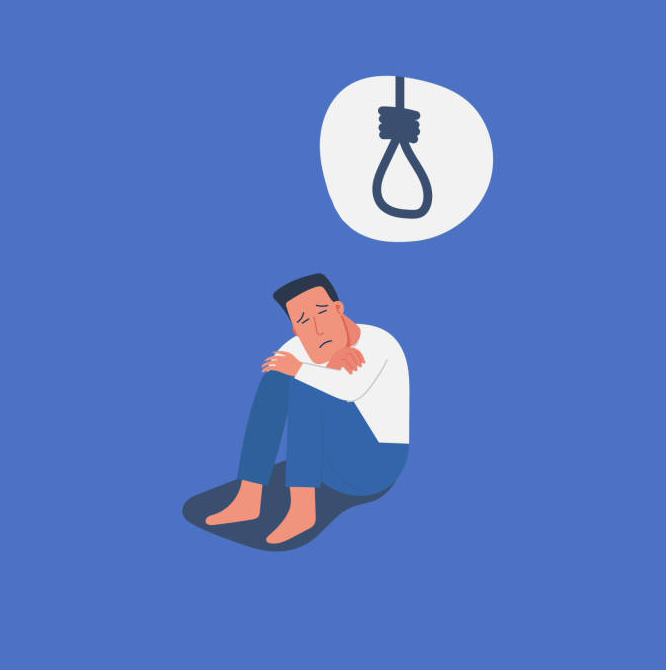
उच्च शिक्षण संस्थानों का साथ लीजिए
बद्री नारायण, ( निदेशक, जीबी पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान )
भारत विकसित होने की राह पर है। अभी हाल में प्रधानमंत्री ने आने वाले पचीस वर्षों में भारत को विकसित देश बनाने का नारा भी दिया है। भारत में इस वक्त दुनिया के किसी भी विकसित देश से कई गुना ज्यादा विकास परियोजनाएं चल रही हैं। गरीबों की जीवन शक्ति, विकास की चाह रखने वालों में क्षमता निर्माण, आधारभूत संरचनाओं का निर्माण, महिला शक्ति निर्माण, सामाजिक संयोजन, आर्थिक समाहितीकरण की अनेक योजनाएं भारत सरकार संचालित कर रही है। साथ ही, जलशक्ति, गतिशक्ति, गरीब कल्याण, किसान कल्याण, इकोनॉमिक कॉरिडोर, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी आंतरिक सुरक्षा, ऊर्जा के क्षेत्र में अनेक परियोजनाएं केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा संचालित की जा रही हैं। इन सभी परियोजनाओं का लक्ष्य भारत को विकासमान महाशक्ति बनाना तो है ही, साथ ही इनसे भारत में विकास का महाआख्यान गढ़ने की कोशिश भी है, जो देश में विकासात्मक हस्तक्षेप और विकास की आकांक्षा व प्रेरणा विकसित कर सके।
लेकिन विडंबना यह है कि विकास के इस अभियान के ईद-गिर्द अभी ज्ञान निर्माण का कार्य नहीं हो सका है। भारतीय राज्य खुद ही अभियान चला रहा है और अभियान को लागू होते हुए खुद ही देख रहा है। इसमें ‘एक तीसरे पक्ष’ की जरूरत है। वह पक्ष हमारे देश के ‘उच्च शिक्षा संस्थान’ हो सकते है, जो अपने-अपने क्षेत्रों के विकास कार्यों और इनसे होने वाले सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक बदलाव का आकलन कर सकते हैं। वे हमारी विकास प्रक्रिया के उपयोगी दस्तावेजीकरण को अंजाम दे सकते हैं।
जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में 1,000 से ज्यादा विश्वविद्यालय हैं, जिनमें 54 केंद्रीय विश्वविद्यालय, 416 राज्य विश्वविद्यालय, 125 डीम्ड यूनिवर्सिटी, 361 निजी विश्वविद्यालय, 159 राष्ट्रीय महत्व के शोध संस्थान, जिनमें अनेक आईआईटी व आईआईएम शामिल हैं। ये सभी देश के विभिन्न भागों में फैले हैं। वन क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र, मरुस्थल, सामूहिक क्षेत्र, हर जगह कोई न कोई उच्च शिक्षा का संस्थान है। इनके साथ कॉलेजों को जोड़ दिया जाए, तो संख्या लाखों तक जा सकती है। उच्च शिक्षा के ये संस्थान भारत में विकास की ‘तीसरी आंख’ बन सकते हैं, जो निरपेक्ष होकर विकास की इस गति को देख सके और उसकी समुचित व्याख्या कर सके।
दुनिया के अनेक देशों में विश्वविद्यालय अपने-अपने मुल्क में विकास के ‘थिंक टैंक’ के रूप में सक्रिय हैं। दुनिया में ऐसे अनेक विश्वविद्यालय हैं, जो अपने समाज और देश में विकासपरक हस्तक्षेप के कारण हो रहे सामाजिक बदलावों के ‘आर्काइव’ और डाटा केंद्र के रूप के सक्रिय तो हैं ही, साथ ही, अपने-अपने समाज में विकास के प्रकाश स्तंभ और विचार केंद्र के रूप में भी कार्यरत हैं।
भारत में उच्च शिक्षा संस्थान मूलत: शिक्षा व डिग्री देने के केंद्र के रूप में कार्यरत हैं। यह ठीक है कि इस प्रक्रिया में वे ऐसे छात्र पैदा करते हैं, जो विकास के इस अभियान में मानवीय शक्ति व एजेंसी के रूप में कार्य कर सकें, किंतु इससे भी आगे बढ़कर इन्हें भारत में विकास के विचार केंद्र के रूप में भी विकसित होने की अपेक्षा की जानी चाहिए। भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों को अपने वजूद में यह एक नया आयाम शामिल करने की जरूरत अभी बाकी है। हमारे उच्च शिक्षा संस्थान विकास के विचार केंद्र एवं तीसरी आंख बन सकें, यह हमारे समय की एक बड़ी जरूरत है।
विकास के प्रयास सिर्फ आर्थिक-प्रशासनिक क्रिया ही नहीं, वरन एक विचार, दर्शन व विवेक के बड़े फ्रेम की भी मांग करते हैं। यह कार्य कोई राजसत्ता अकेले नहीं कर सकती। अभी तक बिना बौद्धिक विचार एवं आकलन के विकास का महायज्ञ किसी भी राष्ट्र में सफलतापूर्वक पूरा नहीं हो सका है। भारत जब आज विकसित राष्ट्र बनने की जद्दोजहद की रहा है, तब भारतीय विश्वविद्यालय इस प्रक्रिया के मूकदर्शक बनकर नहीं रह सकते। उन्हें विकास का न सिर्फ अध्ययन करना होगा, बल्कि विकास में हरसंभव सहयोग भी करना होगा। जिन देशों में तेज आर्थिक विकास हुआ है, उनमें विश्वविद्यालयों की भूमिका व्यापक है। आज हम जहां भी हैं, वहां राज्य या सरकार सक्रिय है। उसकी सक्रियता कई रूपों में है। उनमें एक है – विकास परियोजनाओं का संचालन व उनसे बन रहा लाभार्थी समुदाय। हम जहां भी हैं, वहां के हमारे आर्थिक एवं सामाजिक जीवन में कुछ न कुछ घटित हो रहा है। हमारे दैनिक जीवन में हो रहे इन बदलावों का दस्तावेजीकरण और उन पर गहन शोध की जरूरत है। यह कार्य राजसत्ता अकेले नहीं कर सकती, इसके लिए उच्च शिक्षा संस्थानों को साथ लेना होगा।
शायद इसकी जरूरत आज महसूस की जाने लगी है। भारत सरकार का शिक्षा विभाग देश के कई बड़े विश्वविद्यालयों, आईआईटी एवं आईआईएम का एक संयुक्त पुल तैयार कर रहा है, जो देश के विकास के प्रयासों का नीतिगत आकलन तो करेगा ही, उनके सामाजिक प्रभावों का भी अध्ययन करेगा। साथ ही, ये केंद्रीय महत्व के शिक्षा संस्थान भारत सरकार के विभिन्न विभागों के साथ मिलकर अपने को ‘विकास के थिंक टैंक’ के रूप में स्थापित कर सकेंगे। शिक्षा मंत्रालय विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर भारत में विकास दृष्टि, उनका आकलन और उनके सामाजिक प्रभावों पर अध्ययन करने की महत्वाकांक्षी योजना पर काम कर रहा है। इसे ‘ज्ञान की विरासत’ निर्माण के प्रयास के रूप में देखा जा सकता है।
सचमुच विकास ढांचागत संरचना ही निर्मित नहीं करता, वरन बौद्धिक संपदा भी सृजित करता है, किंतु यह ‘बौद्धिक संपदा’ अभी तक प्राय: असंकलित, अपरिभाषित ही है। हो सकता है, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की यह पहल एक ऐसी बौद्धिक संपदा सृजित करे, जो भविष्य में हमें सार्थक परिणाम दे। ऐसी ‘ज्ञान परंपरा’ राष्ट्र निर्माण की शक्ति भी देगी। इसके लिए जरूरी है कि हमारे देश में उच्च शिक्षा संस्थान सक्रिय होकर आगे आएं और विकास में अपनी भूमिका बढ़ाएं। अभी तक कुछ उच्च शिक्षा संस्थानों के समाज विज्ञान व विकास अध्ययन विभाग इस दिशा में सक्रिय हैं। जरूरत है कि जो उच्च शिक्षा संस्थान जहां भी स्थित हैं, वहां की जिम्मेदारी लें, बदलावों का उपयोगी लेखा-जोखा रखें और अन्य संस्थानों के साथ साझा करें। बेशक, ये संस्थान अगर तीसरी आंख बन गए, तो देश विकास के पथ से जरा भी नहीं भटकेगा।
Date:01-09-22
मुफ्त की सुविधाओं के बजाय क्यों न खर्च के नए नियम बनें
विद्या महांबारे, ( प्रोफेसर, अर्थशास्त्र, जीएलआईएम )
विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा दी जाने वाली मुफ्त सुविधाओं को लेकर पूरे देश में बहस छिड़ी हुई है। मुफ्त सुविधाओं से मतलब उन सेवाओं और उत्पादों से है, जो हुकूमतें अपने तमाम नागरिकों को या कुछ खास लोगों को मुफ्त में मुहैया कराती हैं। हमने हाल ही में किसानों की कर्जमाफी को लेकर एक अध्ययन किया है, जिसको अमूमन विवादास्पद माफी माना जाता है। साल 2001-02 व 2018-19 के बीच देश के 16 प्रमुख गैर-विशेष श्रेणी के राज्यों में से 11 ने 19 बार कृषि कर्ज माफ करने की घोषणा की है। इन राज्यों में केरल, पंजाब, महाराष्ट्र व तमिलनाडु जैसे समृद्ध राज्य भी हैं और उत्तर प्रदेश जैसे पिछडे़ सूबे भी। हमारी गणना के मुताबिक, कर्जमाफी की राशि राज्य सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) की 0.9 प्रतिशत से लेकर 4.6 फीसदी तक थी।
कर्नाटक ने चार बार माफी की घोषणा की, जिसके बाद छत्तीसगढ़ ने तीन बार। चुनाव से पहले तत्कालीन सरकारों ने पांच बार ऐसी घोषणाएं कीं, जबकि 12 बार यह घोषणा घोषणापत्र को लागू करने के एवज में चुनावी जीत के बाद की गई। सिर्फ दो बार कर्जमाफी दो चुनावों की बीच की गई। भारत के दक्षिणी राज्यों (कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, जो अपेक्षाकृत समृद्ध हैं) ने 19 में से नौ बार इस छूट की घोषणा की है, जबकि बिहार और पश्चिम बंगाल ने कभी भी ऐसी घोषणा नहीं की। 60 फीसदी मामलों में यह माफी चुनाव से पहले घोषित की गई, फिर भी तत्कालीन सरकार जनादेश नहीं पा सकी, जो बताता है कि मतदाता समझदार हैं। साफ है, कृषि ऋण माफी न पार्टी की विचारधारा से जुड़ी है और न ही पक्षधरता से, यह विशुद्ध रूप से अवसरवादी राजनीति का उदाहरण है। इससे सबसे बड़े वोटर समूह, यानी किसानों को साधने का प्रयास किया जाता है।
मगर कर्जमाफी जैसी घोषणाओं को लागू करते समय राज्य सरकारों को दुविधा का सामना करना पड़ता है। दरअसल, केंद्र सरकार द्वारा राजकोषीय नियम अपनाने के बाद, ज्यादातर राज्य सरकारों ने 2006 में राजकोषीय उत्तरदायित्व कानून (एफआरएल) को लागू किया, जिसमें यह प्रतिबद्धता जताई गई कि 2009 तक अपने राजकोषीय घाटे को जीएसडीपी की तीन फीसदी से कम रखा जाएगा। हालांकि, घाटे की भरपाई के लिए पहले भी केंद्र इस पर नियंत्रण रखता था कि राज्य बाजार से कितना उधार ले सकता है, फिर भी इस राजकोषीय नियम में फिजूलखर्ची को कम करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। राजकोषीय नियम का पालन न करने पर सरकार की प्रतिष्ठता खतरे में आती है। यहां तक कि समग्र राजकोषीय नियम की उपस्थिति में सरकारें कुल खर्च को बढ़ाए बिना सरकारी खर्च का ढांचा बदल सकती हैं। माफी नीति मौजूदा खर्च तो बढ़ाती ही है, सरकार को पूंजीगत खर्च रोकने को बाध्य भी करती है, जिसमें सिंचाई भी शामिल है, जो कृषि के लिए फायदेमंद मानी जाती है। वित्तीय फिजूलखर्ची को आखिर कैसे रोका जाना चाहिए? यह कहना कठिन है कि कौन सी मुफ्त सुविधाएं जारी रहनी चाहिए और कौन सी नहीं। यह जन-साधारण पर उनके असर से तय होता है। इसके अलावा, सरकारें नए-नए समूहों को आकर्षित करने के लिए भी यह काम कर सकती हैं। हालांकि, हमें नहीं भूलना चाहिए कि लोकतंत्र में चुनी हुई सरकारों के पास इस संदर्भ में फैसले लेने का अधिकार होता है।
ऐसे में, मुफ्त सुविधाओं पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश करने के बजाय बेहतर होगा कि हम खर्च नियम या शून्य राजस्व घाटा नियम अपनाने पर विचार करें। घाटे को संयोजित करते हुए कई देशों ने व्यय नियम अपनाए हैं, जिसमें उनको कई रूपों में सफलता मिली है। मिश्रा एट अल (2021) ने पूंजीगत व्यय से राजस्व खर्च का अनुपात 4-5 की सीमा में रखने संबंधी लक्ष्य बनाने का सुझाव दिया है और पूंजी परिव्यय में वृद्धि की एक विशेष दर को लक्षित करने की बात कही है।
जाहिर है, केंद्र और राज्य सरकारों के लिए खर्च नियम बनाने या शून्य राजस्व घाटा नियम को बहाल करने की व्यावहारिकता का पता लगाने के लिए नए-नए शोध व अनुसंधान होने चाहिए। इससे राजकोषीय ढांचे में कुछ रद्दोबदल की गुंजाइश भी मिल सकेगी।