
05-07-2022 (Important News Clippings)
To Download Click Here.
 Date:05-07-22
Date:05-07-22
Lingering Notes
Cash seems to have a logic-defying appeal. Digitisation may eventually lessen that
TOI Editorials
India’s digital payments landscape, led by the Unified Payments Interface (UPI), is the cynosure of many regulators. In the last two years, the volume of UPI transactions rose over threefold to 46 billion in 2021-22. But concurrently, there’s an anomalous trend. Indians still hold a relatively large share of cash, now one of the highest in the world in relation to GDP. Currency in Circulation (CiC) as a proportion of GDP has grown from 8. 7% in 2016-17 to 13. 7% in 2021-22.
India is not exactly an outlier. Cash has proved surprisingly resilient. A paper by ADB on the trend over 2000-18 in 11 advanced economies showed that Japan, Singapore, South Korea and the US showed a rising trend in CiC to GDP ratio. However, Denmark, Norway and Sweden bucked this trend. One finding that seems to have universal validity is that big shocks such as Covid or the 2008 financial crisis trigger risk aversion among individuals. A consequence is an increase in cash holding.
RBI estimates the annual currency requirement based on the forecast economic growth rate, inflation rate and disposal of soiled notes, among other things. Since 2019, India’s inflation trajectory has trended upwards, which may partly explain why CiC to GDP ratio quickly overshot the pre-demonetisation level. In addition, Covid may have triggered precautionary holding of cash. But none of these factors explains the long-term trend in India’s CiC to private consumption ratio. It was 25. 6% in 2011-20 decade, higher than the 19. 1% recorded for the 1971-2020 phase. Cash has a psychological hold that seems to defy financial logic. For example, India’s currency per capita of Rs 22,752 is about 13% of per capita GDP. This, at a time when high inflation is fast eroding the value of cash.
Even as economists try to decipher the puzzling allure of currency, RBI shouldn’t lose its focus on the digital payments landscape. Its policy choices have been transformative at the grassroots. Progress here will eventually loosen the grip of physical currency in payments.
India needs to scale up direct nutrition interventions
Preconception nutrition, maternal nutrition and child feeding practices in the first 1,000 days of life need priority
Dr. Sheila C. Vir, [ Is a public health nutrition expert and the editor of the book, ‘Public Health Nutrition in Developing Countries’ ]
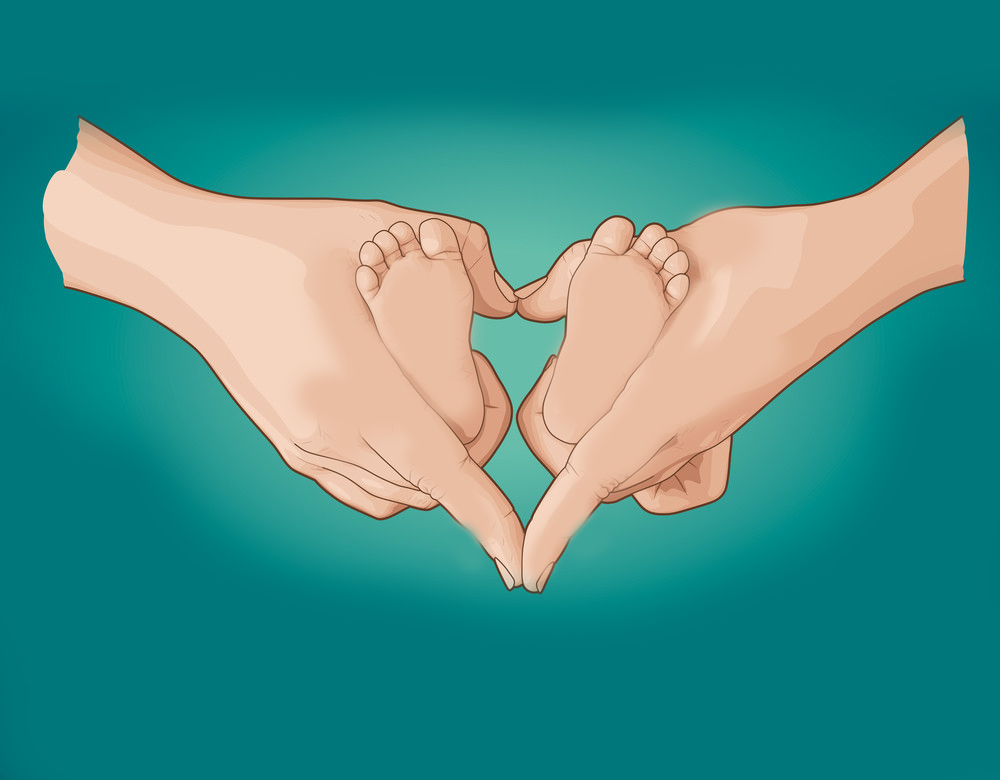
Still, it is disconcerting that even after seven decades of Independence, India is afflicted by public health issues such as child malnutrition (35.5% stunted, 67.1% anaemic) attributing to 68.2% of under-five child mortality. Poor nutrition not only adversely impacts health and survival but also leads to diminished learning capacity, and poor school performance. And in adulthood, it means reduced earnings and increased risks of chronic diseases such as diabetes, hypertension, and obesity.
The good news is that the Government appears determined to set it right — with an aggressive push to the National Nutrition Mission (NNM), rebranding it the Prime Minister’s Overarching Scheme for Holistic Nutrition, or POSHAN Abhiyaan. It has the objective of reducing malnutrition in women, children and adolescent girls.
The Ministry of Women and Child (MWCD) continues to be the nodal Ministry implementing the NNM with a vision to align different ministries to work in tandem on the “window of opportunity” of the first 1,000 days in life (270 days of pregnancy and 730 days; 0-24 months). Global and Indian evidence fully supports this strategy, which prevents the largely irreversible stunting occurring by two years of age. POSHAN Abhiyaan (now referred as POSHAN 2.0) rightly places a special emphasis on selected high impact essential nutrition interventions, combined with nutrition-sensitive interventions, which indirectly impact mother, infant and young child nutrition, such as improving coverage of maternal-child health services, enhancing women empowerment, availability, and access to improved water, sanitation, and hygiene and enhancing homestead food production for a diversified diet.
NHFS data is a pointer
Data from the National Family Health Survey (NFHS)-5 2019-21, as compared to NFHS-4 2015-16, reveals a substantial improvement in a period of four to five years in several proxy indicators of women’s empowerment, for which the Government deserves credit. There is a substantial increase in antenatal service attendance (58.6 to 70.0%); women having their own saving bank accounts (63.0 to78.6%); women owning mobile phones that they themselves use (45.9 % to 54.0%); women married before 18 years of age (26.8 % to 23.3 %); women with 10 or more years of schooling (35.7% to 41.0%), and access to clean fuel for cooking (43.8 % to 68.6%).
But, alarmingly, during this period, the country has not progressed well in terms of direct nutrition interventions. Preconception nutrition, maternal nutrition, and appropriate infant and child feeding remain to be effectively addressed. India has 20% to 30% undernutrition even in the first six months of life when exclusive breastfeeding is the only nourishment required. Neither maternal nutrition care interventions nor infant and young child feeding practices have shown the desired improvement. A maternal nutrition policy is still awaited.
Despite a policy on infant and young child feeding, and a ban on sale of commercial milk for infant feeding, there has only been a marginal improvement in the practice of exclusive breastfeeding (EBF). Child undernutrition in the first three months remains high. Creating awareness on EBF, promoting the technique of appropriate holding, latching and manually emptying the breast are crucial for the optimal transfer of breast milk to a baby. Recent evidence from the Centre for Technology Alternatives for Rural Areas (CTARA), IIT Mumbai team indicates that well-planned breastfeeding counselling given to pregnant women during antenatal checkup prior to delivery and in follow up frequent home visits makes a significant difference. The daily weight gain of a baby was noted to average 30 to 35 grams per day and underweight prevalence rate reduced by almost two thirds.
Another key intervention
NFHS-5 also confirms a gap in another nutrition intervention — complementary feeding practices, i.e., complementing semi-solid feeding with continuation of breast milk from six months onwards. Poor complementary feeding is often due to a lack of awareness to start feeding at six to eight months, what and how to feed appropriately family food items, how frequently, and in what quantity. The fact that 20% of children in higher socio- economic groups are also stunted indicates poor knowledge in food selection and feeding practices and a child’s ability to swallow mashed feed. Where are we going wrong?
So, creating awareness at the right time with the right tools and techniques regarding special care in the first 1,000 days deserves very high priority. We must act now, and invest finances and energy in a mission mode. The Prime Minister can give a major boost to POSHAN 2.0, like he did to Swachh Bharat Abhiyaan, using his ‘Mann Ki Baat’ programme.
There is a pressing need to revisit the system spearheading POSHAN 2.0 and overhaul it to remove any flaws in its implementation. We need to see if we are using opportunity of service delivery contacts with mother-child in the first 1,000 days to the optimum, There is a need to revisit the nodal system for nutrition programme existing since 1975, the Integrated Child Development Scheme (ICDS) under the Ministry of Women and Child and examine whether it is the right system for reaching mother-child in the first 1000 days of life. By depending on the ICDS, we are in fact missing the frequent contacts with pregnant mothers and children that the public health sector provides during antenatal care services and child immunisation services, There is also a need to explore whether there is an alternative way to distribute the ICDS supplied supplementary nutrition as Take- Home Ration packets through the Public Distribution (PDS) and free the anganwadi workers of the ICDS to undertake timely counselling on appropriate maternal and child feeding practices.
We need to systematically review the status, and develop and test a new system that would combine the human resource of ICDS and health from village to the district and State levels. This would address the mismatch that exists on focussing on delivery of services in the first 1000 days of life for preventing child undernutrition by having an effective accountable system.
It is time to think out of the box, and overcome systemic flaws and our dependence on the antiquated system of the 1970s that is slowing down the processes. Moreover, mass media or TV shows could organise discourses on care in the first 1,000 days to reach mothers outside the public health system.
Date:05-07-22
The problem with our university vision
Instead of taking local conditions and market demands into account, India tries to ape the West
Milind Kumar Sharma, [ Is professor at Department of Production & Industrial Engineering, MBM University, Jodhpur, erstwhile, MBM Engineering College, Jodhpur.]
It has now become an annual ritual in India to discuss the international rankings of higher education institutions (HEI) only when global ranking systems such as the coveted QS World University Rankings are announced. The QS World University Rankings rank HEIs on the following components: academic reputation (40%), employer reputation (10%), faculty student ratio (20%), citations per faculty (20%), international faculty ratio (5%) and international student ratio (5%). The international research network and employment outcomes were 0% for this edition.
While it is heartening to see that the number of Indian institutes among the top 1,000 globally has risen to 27 from 22 last year, and that the Indian Institute of Science (IISc), Bangalore, has moved up 31 places to emerge as the highest ranked Indian institute in the 2023 edition, there is no serious debate on the abysmal performance of Indian universities barring the Institutes of Eminence (IOE). IOEs occupy a special place as they are granted more academic and administrative autonomy, and public IOEs get additional funding. Therefore, their dominance in the top 500 in the QS World University Rankings comes as no surprise.
Step-motherly treatment
Among the other HEIs too, there is great inequality. As per the All-India Survey on Higher Education (2019-20), 184 of the 1,043 HEIs in the country are centrally funded institutions. The Indian government generously allocates financial resources to these institutions. However, the financial support provided by State governments to State HEIs is far from adequate even though the number of under-graduate students is largest in State public universities (13,97,527) followed by State open universities (9,22,944) of the total students’ enrollment. State-sponsored HEIs barely manage to pay salaries and pensions.
While the number of universities increased by almost 30.5% in 2019-20 compared to 2015-16, academic and administrative infrastructure has not been strengthened commensurate to this growth. The lackadaisical attitude we see in filling up faculty positions has further worsened the quality of teaching and research in HEIs. In fact, quality education and the world class research output that policymakers expect from State public universities remain elusive as these HEIs have never had financial and other resources to attain academic and professional growth.
On the other hand, the institutions that are generously funded by the Centre perform better than their State-sponsored counterparts on all academic performance indicators — faculty strength, modernised laboratories, building infrastructure, digitised libraries, sponsored research project grants, computing facilities, etc. Therefore, that the State-funded HEIs would not perform well in these rankings was a forgone conclusion. It is a consequence of the unequal and unfair system in the Indian higher education system, where State-sponsored HEIs are provided step-motherly treatment and positioned poorly vis-à-vis centrally funded institutions. No ranking system seems to rationally rank institutions after examining their administrative challenges, infrastructural constraints and financial predicaments; they only pay attention to performance metrics based on academic strengths and other achievements. For India to perform better on these rankings, we need to pay more attention to the State HEIs.
The NEP vision
The National Education Policy (NEP) 2020 has envisaged all HEIs to become multidisciplinary institutions by 2040. The aim is to increase the Gross Enrolment Ratio in higher education, including vocational education, from 26.3% in 2018 to 50% by 2035. The NEP also aims to ensure that by 2030, there is at least one large multidisciplinary HEI in or near every district. This means that single-stream specialised institutions will eventually be phased out.
However, the fact that prominent multidisciplinary universities such as Jawaharlal Nehru University, Delhi University, the University of Hyderabad, and Jamia Millia Islamia have slipped in the QS World University Rankings should compel national think tanks to revisit the NEP’s proposal in this regard. A close study of the QS World University Rankings reveals that single-stream specialised HEIs such as the Indian Institutes of Technology and IISc have performed better than their multidisciplinary counterparts. Eight IITs (Delhi, Bombay, Madras, Kanpur, Kharagpur, Roorkee, Guwahati and Indore) are placed among the top 500 globally, in addition to IISc, Bangalore. IIT-Indore ranked highest among the second-generation IITs by securing the 396th position and IIT-BHU made its maiden presence in the 651-700 band.
A plan in the NEP for multidisciplinary education and research universities is also being contemplated in order to achieve the highest global standards in quality education. While everyone is demanding multidisciplinary education, the performance of the specialised HEIs in the QS World Rankings bears testimony to their superiority over multidisciplinary/multi-faculty institutions. The idea of converting a specialised institution into a multi-faculty university does not seem to augur well for an economy driven by specialist professionals. It would be perplexing if the IITs decided to offer courses in physical education and medicine or the National Law Universities ran undergraduate degree programmes in mechanical engineering.
It is crucial to emphasise here that nobody is averse to the idea of multidisciplinary/multi-faculty education if there is a 15% to 20% flexibility in the total academic strength. But converting all HEIs into multidisciplinary institutions is not an idea that holds water given the unique conditions and demands in India. No study or data support the idea of transforming specialised institutions into multidisciplinary/multi-faculty universities either. Such an idea may have worked in the West where HEIs invest substantial resources in multidisciplinary research through private and public research grants and funding. But a ‘one size fits all’ approach may not be of help to India. The need of the hour is to build and develop our higher education system while taking into account Indian conditions
प्लास्टिक बैन के बीच वैकल्पिक उत्पाद बनें
संपादकीय
पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी निभाते हुए भारत सरकार ने सिंगल यूज़ प्लास्टिक (एसयूपी- एक बार ही प्रयुक्त होने वाला) बैन किया है। एसयूपी के नकारात्मक प्रभावों के बीच ये कदम सराहनीय है। लेकिन चूंकि ऐसा 100 माइक्रोन मोटाई वाला प्लास्टिक आम जीवन में हर कदम पर जुड़ा हुआ है, लिहाजा फैसला लेने के पहले यह सोचना जरूरी था कि इसे किस उत्पाद से विस्थापित किया जाए, जो आर्थिक रूप से समतुल्य भी हो। देश में केवल पेय पदार्थों के पैकेट में प्लास्टिक की 600 करोड़ स्ट्रॉ इस्तेमाल होती हैं। फिर टेट्रा-पैक में बिकने वाले दूध-जूस जैसे प्रोडक्ट में भी इनका व्यापक इस्तेमाल होता है। स्ट्रॉ के लिए कागज और थैले के लिए बांस विकल्प हो सकते हैं, लेकिन क्या सरकार ने सुनिश्चित किया है कि इतने बड़े पैमाने पर बांस का उत्पादन हो और उससे थैले बनाने वाली फैक्ट्रियां उत्पादन प्रक्रिया में आ गईं हों? शायद नहीं। लिहाजा पेय पदार्थों और दुग्ध-उत्पाद बनाने और पैक करने वाली कुछ बड़ी कंपनियों का मानना है कि इस बदलाव से कम से कम पांच से दस रु. कीमतें बढ़ेंंगी। अमूल ने तो पीएमओ को पत्र लिखकर प्रार्थना की कि फैसले को कुछ माह और रोका जाए ताकि वैकल्पिक और उतना ही सस्ता उत्पाद बनना शुरू हो जाए। पर सरकार ने उसे ठुकरा दिया। प्लास्टिक उद्योगों के एसोसिएशंस का कहना है कि उत्पादन में लगे करीब दो लाख लोग रोजगार से वंचित हो जाएंगे, हालांकि ये भी सच है कि कागज-बांस के व्यापक इस्तेमाल से लाखों लोगों को काम मिलेगा। इस फैसले का केवल एक नकारात्मक पहलू है कि क्या देश में वैकल्पिक उद्योग विकसित हो गए हैं। अगर नहीं तो भारत के पेय पदार्थों और दुग्ध सहित हजारों उद्योगों को आयात पर निर्भर रहना होगा।
 Date:05-07-22
Date:05-07-22
हरित कानूनों के लिए लाल संकेत
संपादकीय
राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार ने 2014 में सत्ता में आने के बाद खुद को कारोबार हितैषी साबित करने की कोशिश की है। इसका अपने इस एजेंडे को पूरा करने के प्रयास का एक प्रमुख तरीका पर्यावरण संरक्षण कानूनों में ढील देना है। इस संदर्भ में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के नए प्रस्ताव पर्यावरण सुरक्षा, वायु और जल प्रदूषण से संबंधित तीन कानूनों के दंडात्मक प्रावधानों को कमजोर करते हैं। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मुताबिक इसका मकसद प्रावधानों को गैर-आपराधिक बनाना है ताकि ‘साधारण’ उल्लंघनों के लिए जेल का डर खत्म किया जा सके। मंत्रालय ने कहा कि वह प्राप्त सुझावों पर काम कर रहा है। सरकार ने पहली बार चूक के लिए जेल के प्रावधान (मूल रूप से पांच साल तक) को खत्म करने मगर जुर्माने को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने की योजना बनाई है। दोबारा उल्लंघन करने के लिए जुर्माना ज्यादा व्याख्यात्मक बन गया है क्योंकि यह पर्यावरण को नुकसान के बराबर होगा। अगर चूक करने वाला मूल और अतिरिक्त जुर्माना नहीं चुकाता है तो उसे जेल की सजा होगी। लेकिन यहां भी संशोधनों में प्रस्ताव रखा गया है कि पीडि़त पक्ष फैसला देने वाले अधिकारी के खिलाफ राष्ट्रीय हरित अधिकरण में अपील कर सकता है।
सरकार ने एक पर्यावरण सुरक्षा कोष भी बनाया है, जिसमें संशोधित नियमों के तहत फैसला सुनाने वाले अधिकारियों द्वारा लगाए गए जुर्माने की राशि जमा की जाएगी। इस कोष का इस्तेमाल प्रभावित पक्षों के लाभ के लिए किया जाएगा। सैद्धांतिक रूप से सफेदपोश अपराधों को गैर-आपराधिक बनाना अच्छा है, लेकिन भारत में पैदा होती पारिस्थितिकी चुनौतियों को मद्देनजर रखते हुए पर्यावरण संरक्षण कानूनों को यथासंभव सख्त रखने की पुरजोर मांग की जा रही है। भारत विश्व के उन देशों में शामिल है, जो जलवायु की वजह से आने वाली आपदाओं से सबसे अधिक प्रभावित हैं। उद्योग जगत की लॉबिइंग की ताकत हमेशा बनी रहती है। ऐसे में अपील और छूट की मंजूरियों के एक मानक बनने की उम्मीद की जा सकती है। वह देश जो खुद को जलवायु न्याय के पैरोकार के रूप में पेश करता है, उसका सिद्धांत यह होना चाहिए कि पर्यावरण संरक्षण से कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। हालांकि सरकार ने इस सिद्धांत का लगातार पालन नहीं किया है।
यह बहुत महत्त्वपूर्ण है कि वृद्धि और पर्यावरण को बेहतर बनाए रखने के बीच संतुलन हमेशा कायम रखा जाए। उदाहरण के लिए वर्ष 2014 में सरकार ने कारखानों को प्रदूषण की गंभीर स्थिति वाले आठ क्षेत्रों में स्थापना की मंजूरी दे दी। इसके बाद मझोले आकार के प्रदूषक उद्योगों को पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्रों के 10 किलोमीटर के बजाय पांच किलोमीटर के दायरे में परिचालन की मंजूरी दे दी, ताप विद्युत संयंत्रों के लिए अपशिष्ट निकासी के नियमों में ढील दी गई और पारिस्थितिकी संवेदनशील इलाकों को गैर-अधिसूचित किया गया तथा तटीय नियमन जोन में ढील दी गई। वन भूमि पर सफारी, चिडि़याघर, खनन और अन्य गैर-वन उपयोग की मंजूरी देने के लिए वन अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन सबसे अधिक चिंताजनक हैं।
यह उल्लेखनीय है कि सरकार के पर्यावरण कानून सैद्धांतिक रूप से बड़े और मझोले उद्योगों को ही लाभ पहुंचाते हैं। लेकिन इसने बहुत से छोटे और सूक्ष्म उद्योगों के प्रति कोई उदारता नहीं दिखाई, जो बहुत से सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों पर रोक से कारोबार से बाहर होने के कगार पर हैं। यह भी अहम है कि सरकार पर्यावरण से संबंधित फैसले लेने वाली संस्थाओं में अपनी भूमिका मजबूत करने की कोशिश कर रही है। उदाहरण के लिए इसने राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड में स्वतंत्र सदस्यों की संख्या 15 से घटाकर 3 कर दी है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण के चेयरमैन की नियुक्ति में एक बड़ी भूमिका निभाने के प्रयास पर सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगाई। कुल मिलाकर उद्योग के लिए हरा संकेत भारत के पर्यावरण के लिए लाल दिखाई दे रहा है।
आलोचना का विवेक
संपादकीय
इंटरनेट आधारित सामाजिक मंचों पर मनमाने बयानों, अविवेकपूर्ण, अशोभन और भड़काऊ टिप्पणियों आदि को लेकर लंबे समय से एतराज जताया जाता रहा है। इसे लेकर अदालतें कुछ मौकों पर नाराजगी जाहिर कर चुकी हैं। सरकार ने ऐसे लोगों पर नकेल कसने की भी कोशिश की, पर उसका असर नजर नहीं आ रहा। नूपुर शर्मा मामले में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जेबी पारदीवाला की टिप्पणी को लेकर सामाजिक मंचों पर की जा रही टिप्पणियां इसकी ताजा उदाहरण हैं। न्यायाधीश पारदीवाला ने मौखिक रूप से नूपुर शर्मा को फटकार लगाते हुए कहा था कि उनके असावधानी भरे बयान की वजह से पूरा देश जल रहा है, इसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। उसी टिप्पणी को आधार बना कर सामाजिक मंचों पर उनके खिलाफ व्यक्तिगत हमले शुरू हो गए। स्वाभाविक ही न्यायाधीश उन टिप्पणियों से आहत हुए और एक कार्यक्रम में कहा कि ये हमले ‘एजेंडा संचालित’ हैं और सामाजिक मंच ‘लक्ष्मण रेखा लांघ रहे हैं’। इसलिए इन्हें कानूनी दायरे में लाने की जरूरत है। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों और टिप्पणियों को बड़ी इज्जत के साथ स्वीकार किया जाता है। उन्हें संविधान की रक्षा के लिए जरूरी संकेत के रूप में लिया जाता है। मगर पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि बहुत सारे लोग किसी भी फैसले के विरोध में बेहिचक अपनी राजनीतिक धारणाएं व्यक्त करते हैं।
अदालत के किसी फैसले या निर्देश की रचनात्मक आलोचना से न्यायपालिका को कोई एतराज नहीं, पर जब किसी राजनीतिक मंशा से आलोचना की जाती है, तो उसे लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं माना जाता। न्यायमूर्ति पारदीवाला ने कहा भी कि अगर इसी तरह लोग बेलगाम टिप्पणियां करते रहेंगे, तो न्यायाधीशों का ध्यान इसी बात पर ज्यादा लगा रहेगा कि मीडिया उनके फैसलों को किस नजर से देखता है। इस तरह सामाजिक मंचों की मर्यादा तय करने के लिए नियामक तंत्र गठित करने की जरूरत एक बार फिर संजीदगी से महसूस की गई है। यह ठीक है कि संविधान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, मगर इसका यह अर्थ कतई नहीं कि कोई किसी के भी बारे में मनमाने ढंग से कुछ भी बोल, लिख या कह दे। सामाजिक मंचों पर चूंकि खुली आजादी है कि कोई भी व्यक्ति अपनी सामग्री खुद डाल सकता है, बहुत सारे लोग अभिव्यक्ति की आजादी का बेजा फायदा उठाने का प्रयास करते देखे जाते हैं। जबसे राजनीतिक दलों ने सामाजिक मंचों का उपयोग अपने राजनीतिक प्रचार-प्रसार के लिए करना शुरू किया है, तबसे वहां मनमानी कुछ अधिक ही बढ़ गई है।
सामाजिक मंचों ने निस्संदेह लोगों को एक विशाल रचनात्मक फलक दिया है, उनके जरिए बहुत सारे मसले हल करने में आसानी हुई है, कई रूढ़ियों को तोड़ने में मदद मिल रही है। मगर वहां राजनीतिक प्रतिस्पर्द्धाएं भाषा और अभिव्यक्ति की सारी मर्यादाएं तोड़ती नजर आती हैं। विचित्र है कि इस समस्या का हल खुद सरकार को निकालना है, पर उसके समर्थक भी मर्यादा की हदें लांघते नजर आते हैं। कई बार तो सामाजिक मंचों पर समांतर अदालतें चलाई जाने लगती हैं। फिर यह समस्या केवल सामाजिक मंचों तक सीमित नहीं है, डिजिटल माध्यमों पर चल रहे समाचार चैनलों में भी ‘बेलगाम जुबानें’ दिन भर गूंजती रहती हैं। अभिव्यक्ति की आजादी रचनात्मक आलोचना करने के लिए दी गई थी, न कि अविवेकपूर्ण ढंग से, निराधार, पूर्वाग्रह ग्रस्त होकर कुछ भी कहने, लिखने और छाप-दिखा देने के लिए। बिना विवेक के की गई आलोचना समाज में विकृतियां ही पैदा करती है।
नारी अधिकार को दबाने का कुचक्र
अवनी सबलोक, ( सीनियर रिसर्चर, पब्लिक पॉलिसी रिसर्च सेंटर, नई दिल्ली )
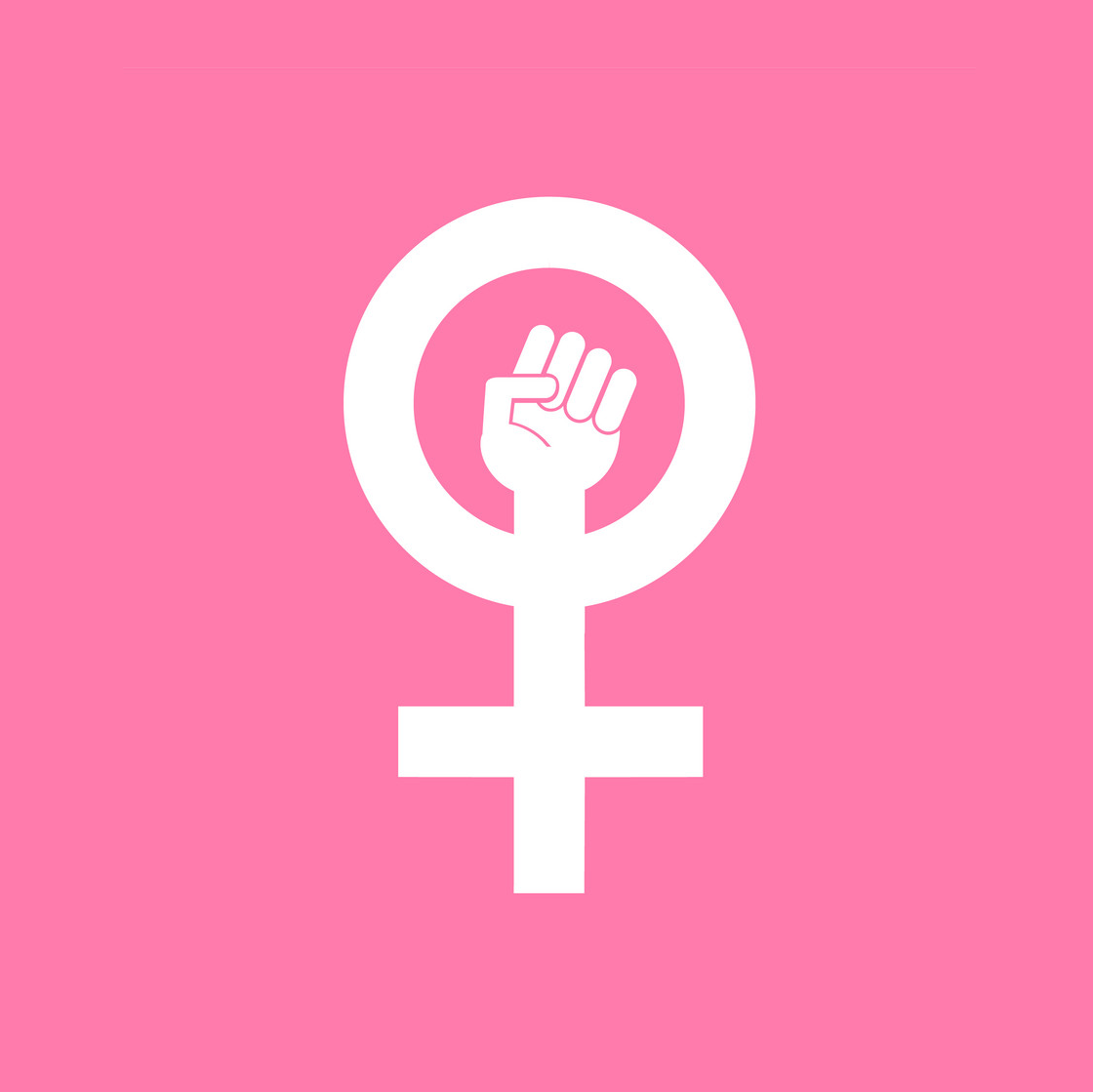
गौरतलब है कि महिलाओं के अबॉशर्न के अधिकार का मामला वर्ष 1973 के ‘रो बनाम वेड’ केस से जुड़ा है। 22 साल की उम्र में सुरक्षित गर्भपात का मामला सुप्रीम कोर्ट में ले जाने वालीं नोर्मा मैककोर्वे को ही ‘रो’ के नाम से जाना जाता है। इस केस में रो वादी थीं और वेड प्रतिवादी। ‘वेड’ का पूरा नाम हेनरी वेड है जो कि डलास काउंटी (टेक्सास) के तत्कालीन जिला अटॉर्नी थे। 1971 में जब रो अबॉशर्न कराने में नाकाम रहीं तो उन्होंने सर्वोच्च अदालत में एक याचिका दायर कर सुरक्षित गर्भपात को आसान बनाने के लिए निवेदन किया। उन्होंने यह भी मांग रखी कि गर्भधारण और गर्भपात का फैसला महिलाओं का होना चाहिए, न कि सरकार का। ठीक दो साल बाद 1973 में सर्वोच्च अदालत की 9 जजों की बेंच ने 1973 में 7-2 के बहुमत से अबॉशर्न को कानूनी दर्जा देने का फैसला सुनाया, जो ‘रो बनाम वेड’ मामले के रूप में प्रचलित हुआ। फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने ना केवल अबॉशर्न को कानूनी मान्यता दी बल्कि राज्यों के उन कानूनों को भी रद्द कर दिया जो अबॉर्शन को अवैध मानते थे। कोर्ट ने गर्भपात को मंजूरी देते हुए इसे स्त्री का मूलभूत अधिकार माना और साथ ही साथ, अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन की भावना के अनुरूप इसे ‘निजता के अधिकार’ (Right to Privacy) से संबद्ध माना। यह ऐतिहासिक फैसला पूरे विश्व में गर्भपात कानूनों के लिए एक बेंचमार्क बन गया। अबॉशर्न पर कोर्ट के फैसले का अमेरिका कई हिस्सों में विरोध हुआ। धार्मिंक संस्थानों और रूढ़िवादी समूहों ने इस फैसले के खिलाफ खूब विरोध किया। इस आंदोलन को ‘प्रो-लाइफ मूवमेंट’ के नाम से जाना जाता है। इस आंदोलन से जुड़े लोग अबॉशर्न को भ्रूण-हत्या से जोड़कर देखते हैं। वहीं दूसरी तरफ महिला संगठनों और नारीवादियों द्वारा मूवमेंट चलाया गया जिसे ‘प्रो-च्वाइस मूवमेंट’ के नाम से जाना जाता है। यह मूवमेंट महिलाओं की पसंद का समर्थन करता है और साथ ही साथ अबॉशर्न को भ्रूण-हत्या नहीं मानता। गर्भपात का विषय स्त्री के ‘जीवन की स्वतंत्रता’ से जुड़ा उसका मूल अधिकार है। बताया जा रहा है कि अमेरिका में गर्भपात का मुद्दा सिर्फ सामाजिक, मानवीय या स्वास्थ्य से जुड़ा नहीं है, बल्कि यह राजनीति से भी प्रेरित है। इसमें रिपब्लिकन पार्टी चूंकि गर्भपात पर रोक लगाने की समर्थक है। इसलिए उसकी सरकार वाले कई राज्यों ने इस पर प्रतिबंध के कानूनी बंदोबस्त किए हैं। मिसिसिपी उनमें से एक राज्य है। वहां 15 हफ्ते से ऊपर के भ्रूण के अबॉशर्न को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है। निश्चित तौर पर, सर्वोच्च अदालत के इस नये फैसले के दूरगामी परिणाम होंगे क्योंकि सामाजिक रूप से यकीनन एक बड़ी आबादी की आजादी प्रतिबंधित हो जाएगी। गर्भपात कराने की कानूनी सुविधा महिलाओं से वापस लिए जाने से उसके सामने तमाम तरह की मुश्किलें खड़ी होंगी। इनमें स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी होंगी। वहीं राजनीतिक रूप से निश्चित तौर पर इसका फायदा रिपब्लिकन पार्टी उठाएगी। उसके समर्थन का आधार मजबूत होगा। माना जा रहा है कि संभवत: इन्हीं कारणों से अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन सर्वोच्च अदालत के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं।
अदालत में इस फैसले को लाने के पीछे अमेरिका में बड़ी संख्या में अबॉशर्न के बढ़ते मामले बताए जा रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक, 2017 की तुलना में 2020 में अबॉशर्न कराने वालों की संख्या बढ़ी। वर्ष 2020 में औसतन हर पांच प्रेग्नेंट महिलाओं में से एक ने अबॉशर्न कराया। अमेरिका के ज्यादातर दक्षिणी और मध्य-पश्चिमी राज्यों में अबॉशर्न को अवैध किया जा सकता है तो वहीं कुछ राज्यों में इसमें छूट दी जा सकती है। एक तरफ जहां अमेरिका सहित कई पश्चिमी राष्ट्र गर्भपात के अधिकारों में कटौती कर रहे हैं, वहीं भारत जायज गर्भपात की सीमा बढ़ा रहा है। इतना ही नहीं बल्कि मोदी सरकार द्वारा अनेकों ऐसी योजनाएं लाई गई हैं, जिससे नारी-सशक्तिकरण को बल मिल सके। निश्चित तौर पर, भारत विश्व के सामने एक सफल उदाहरण प्रस्तुत कर नई दिशा का मार्गदर्शन कर रहा है। गर्भपात-विरोधी कानून नारी-विरोधी सोच का प्रतिबिंब हैं। जरूरत है कि वे सभी देश आत्ममंथन करें, और महिलाओं की आजादी की क्षमता को समझते हुए संकीर्ण विचार से ऊपर उठकर नारी-स्वतंत्रता विरोधी कानूनों में बदलाव लाएं।
ताकि न आए आलोचना की नौबत
हरबंश दीक्षित, ( विधि विशेषज्ञ )
सुप्रीम कोर्ट के दो न्यायमूर्तियों द्वारा की गई अलिखित टिप्पणियां पूरे देश में चर्चा में हैं। नूपुर शर्मा की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान न्यायमूर्तियों द्वारा की गई टिप्पणियों पर सोशल मीडिया में जिस तरह की अवांछित तथा अमर्यादित प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, उन्हें किसी भी सभ्य समाज में स्वीकार नहीं किया जा सकता। एक न्यायमूर्ति ने इस पर घोर आपत्ति की है। बचाव में कुछ लोग यह कह रहे हैं कि वह टिप्पणी अदालती निर्णय का हिस्सा नहीं थी और वे न्यायाधीश के व्यक्तिगत विचार थे। इसलिए लोगों का टिप्पणी करना उनकी अभिव्यक्ति की आजादी का हिस्सा है। वजह तथा परिस्थितियां जो भी हों, लोकशाही में इस तरह का आचरण स्वीकार नहीं किया जा सकता। अन्य संस्थाओं की तरह न्यायपालिका भी लोकशाही का महत्वपूर्ण स्तंभ है और यह हम सभी की साझा जिम्मेदारी है कि अपनी बात कहते समय मर्यादा का कभी उल्लंघन नहीं हो। ध्यान रहे, अभिव्यक्ति की आजादी हमें कभी भी किसी सांविधानिक संस्था की प्रतिष्ठा पर आघात पहुंचाने की छूट नहीं देती है।
अदालती निर्णयों या टिप्पणियों के परिणामस्वरूप मानवता ने बहुत कठिन दौर देखे हैं। मसलन, अमेरिका में ‘डेज्ड स्कॉट बनाम सेन्डफोर्ड’ मामले में तो हालात यहां तक पहुंच गए थे कि अमेरिका में गृह युद्ध छिड़ गया था। बात तब की है, जब हम आजादी की पहली लड़ाई लड़ रहे थे। तब अमेरिका के कुछ राज्यों में दासप्रथा को कानूनी मान्यता हासिल थी और दास किसी दूसरी वस्तु की तरह खरीदे और बेचे जा सकते थे। कुछ राज्य ऐसे भी थे, जिनमें दासप्रथा को गैर-कानूनी घोषित कर दिया गया था। डेज्ड स्कॉट नामक दास मिसौरी में अपने मालिक के साथ रहता था, जहां दासप्रथा वैध थी। एक दिन उसके मालिक उसे लेकर इलिनॉय राज्य गए, जहां दासप्रथा गैर-कानूनी थी। वहां से मिसौरी लौटने पर स्कॉट ने अदालत में अर्जी दी कि उसे स्वतंत्र नागरिक का दर्जा और उससे जुड़े अधिकार दिए जाएं। उसकी दलील थी कि जब वह इलिनॉय राज्य गया, तब वहां दासप्रथा गैर-कानूनी होने के कारण वह आजाद हो गया है और एक बार स्वतंत्र हो जाने के बाद उसे पुन: दास नहीं बनाया जा सकता। मिसौरी की अदालत ने डेज्ड स्कॉट की दलील को अस्वीकार कर दिया। इससे निराश डेज्ड स्कॉट ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट के सामने सवाल खड़ा हो गया कि यदि कोई दास एक बार आजाद नागरिक हो जाए, तो क्या वह पुन: दास हो सकता है? यह कानून के अर्थान्वयन का मामला था और अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट अपने को वहीं तक सीमित रख सकता था, पर अदालत ने कह दिया कि अफ्रीकी मूल के किसी व्यक्ति को, चाहे वह दास हो या नहीं, अमेरिकी नागरिकता नहीं दी जा सकती। यही नहीं, प्रधान न्यायाधीश रोजर टेनी ने एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा कि अमेरिकी संविधान की कभी यह मंशा नहीं थी कि अफ्रीकी लोगों को अमेरिकी नागरिक माना जाए। कोर्ट यहीं नहीं रुका, उसने दासप्रथा को मजबूत करने की कोशिश की, कहा कि मिसौरी समझौते की कुछ बातें दासप्रथा के पालन में बाधा पहुंचाती हैं, इसलिए असांविधानिक हैं। इस तरह अदालत ने किसी दास के आजाद नागरिक बनने के रास्ते बंद कर दिए।
इस निर्णय के बाद की प्रतिक्रिया कल्पना से परे थी। अमेरिकी आबादी के एक हिस्से के मन में गहरा अन्याय-बोध पनपा, जिसकी परिणति अमेरिकी गृह युद्ध के रूप में हुई। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन को इसकी कीमत अपनी आहूति देकर चुकानी पड़ी। अमेरिका ने इससे सबक सीखा, संविधान का 13वां और 14वां संविधान संशोधन लाया गया। 13वें संशोधन द्वारा दासप्रथा समाप्त कर दी गई तथा 14वें संविधान संशोधन द्वारा अमेरिका में रहने वाले हरेक व्यक्ति को नागरिकता का अधिकार दिया गया।
बहुत से लोग अमेरिकी गृह युद्ध के लिए अदालत द्वारा डेज्ड स्कॉट के मामले में की गई गैर-जरूरी टिप्पणी को भी जिम्मेदार मानते हैं। वाकई समस्या तब खड़ी हो जाती है, जब न्यायाधीश के रूप में कार्य करते समय ऐसी गैर-जरूरी टिप्पणी की जाए, जो मीडिया के लिए तो बड़ी खबर बन जाए, किंतु न्यायालय के आदेश का हिस्सा न होने के कारण उसके परिष्करण का कोई रास्ता ही नहीं रहे।
अपने देश में न्यायपालिका के आदेश मंत्राक्षर जितने ताकतवर होते हैं। समाज उनके प्रति सम्मान का भाव रखता है, फैसलों में लिखे अर्द्ध-विराम और पूर्ण-विराम तक पर व्यापक चर्चा होती है। एक-एक हिस्से का क्रियान्वयन किया जाता है और उनके किसी भी हिस्से को हल्के में नहीं लिया जाता। न्यायाधीश के आसन से कही गई हर बात न्यायालय की औपचारिक टिप्पणी होती है। जनमानस उसे कानून और संविधान के बराबर की मान्यता देता है। सभी पक्षों को ध्यान रखना चाहिए कि अनेक लोग उसका उपयोग अपने को मजबूत करने या दूसरे को गिराने के लिए भी कर सकते हैं। कोई कुछ भी कहता रहे, अनेक लोग किसी अलिखित अदालती टिप्पणी को सामान्य टिप्पणी मानने को तैयार नहीं होते हैं। ज्यादातर लोग न्याय के घर से आई हर टिप्पणी को आदर्श मानते हैं।
अदालतों की टिप्पणी और अकादमिक विमर्शों में व्यक्त विचारों में अंतर होता है। अकादमिक विमर्श में की गई टिप्पणी को लोग गंभीरता से नहीं लेते हैं। किसी सिद्धांत की स्थापना करना, उसे नकारना, अपने मंतव्य व्यक्त करना इत्यादि उस विमर्श का हिस्सा होता है और उनकी ताकत भी होती है। इसके ठीक उलट अदालतों की टिप्पणियों को ब्रह्म वाक्य जैसा माना जाता है। अदालत की टिप्पणियों का हवाला देकर अपने पक्ष में या किसी के खिलाफ माहौल तैयार किया जा सकता है और यहां तक कि देश की दूसरी अदालतों की सोच को भी प्रभावित किया जा सकता है।
अदालतों की गैर-जरूरी टिप्पणी का एक नुकसान यह भी है कि उससे एक ऐसे अंतहीन बहस की शुरुआत होती है, जिसका कोई आधार और ओर-छोर नहीं होता है। न्यायालयों की अंतर्निहित सीमा यह है कि वे सार्वजनिक तौर पर अपना बचाव नहीं कर सकते। इसलिए इतिहास ने हमें सबक दिया है कि यह स्वयं न्यायपालिका के हित में है कि अदालतों को किसी के बारे में भी गैर-जरूरी टिप्पणी से बचना चाहिए।